सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि ज्ञान तक पहुंच एक ख़ास सामाजिक-आर्थिक तबके में आने वाले लोगों तक ही रही है। जाति, लिंग, वर्ग, धर्म या अन्य तरह के भेदभाव के चलते वंचित समुदाय लंबे समय तक औपचारिक शिक्षा से दूर रहे हैं। लेकिन इनके पास पीढ़ियों का संचित और अनुभव से आया ज्ञान है जो हमेशा से इनके जीवन का आधार रहा है।
अत्त दीप एकेडमी ऑफ ग्रासरूट लीडरशिप (एजीएल) एक ऐसी पहल है जो ज़मीन पर काम करने वाले लोगों और समुदाय के भीतर छिपे परंपरागत ज्ञान को उभारने का प्रयास करती है। इस ज्ञान का इस्तेमाल कर लोग अपनी आजीविका से लेकर शैक्षणिक, सामाजिक और मानवीय विकास तक की संभावनाएं खोज सकते हैं। समाजसेवी संस्था कोरो द्वारा राजस्थान और महाराष्ट्र के 40 ज़मीनी संगठनों के साथ मिलकर शुरू की गई इस पहल में हम कुछ इस तरह के सवालों के जवाब टटोल रहे हैं – ज्ञान क्या है? ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान विकसित करने का अधिकार किसके पास है? और, सबसे ज़रूरी कि क्या ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में लोगों के अनुभवों का कोई स्थान है? ऐसा करते हुए, इस आलेख में हम ज़मीनी ज्ञान निर्माण के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़े अपने अनुभव और समझ साझा करेंगे।
अलग-अलग इलाक़ों में अलग-अलग तरह की लोक कलाएं, खेल गाने, कहावतें वग़ैरह हैं जो उनके पारंपरिक ज्ञान की झलक देते हैं। गांव में जीवन के जो नैसर्गिक स्रोत हैं, उनके हिसाब से लोग अपना जीवन रच लेते हैं। उदाहरण के लिए मौसम या बारिश का अनुमान एक ऐसी ही चीज है। कितना पानी बरसेगा, और उसमें किस तरह की खेती के लिए कौन सा तरीक़ा सटीक होगा, इसके लिए लोगों के अलग-अलग पैमाने हैं। कई बार जब आप खेतिहर महिलाओं के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि उन्हें अपने ही ज्ञान का अनुमान नहीं होता है। उनके लिए वह सहज होता है। हम लोग बाहर से जाकर देखते हैं तो हमें लगता है कि हां यह अलग है, इसे हम ग्रासरूट नॉलेज कहते हैं। इस आलेख में हमने इसके लिए ज़मीनी ज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया है।
एक उदाहरण के तौर पर, पूर्वी महाराष्ट्र के भंडारा और गोंडिया जिलों में धीवर (मछुआरा) समाज की बात कर सकते हैं। इस इलाक़े में तीन-चार सेंटीमीटर की मछली पाई जाती है जिसे क्षेत्रीय भाषा में कलवली बोलते हैं। ब्रीडिंग सीज़न में, उसके पेट के बीचों बीच एक नारंगी लाइन आ जाती है। इस लाइन को देखकर लोग कहते हैं कि अब कलवली ने श्रृंगार कर लिया है यानी यह धान बोने के लिए सही समय है और अगले पांच-छह दिनों में बरसात होगी।
यह ज्ञान सिर्फ़ मौसम तक सीमित नहीं है। लोगों का यह ज्ञान विभिन्न प्रजातियों के जीवन, स्वास्थ्य और उनके पूरे परिवेश से उसके संबंध तक जाता है।
जब हम संस्थागत तौर पर इस तरह के ज्ञान को संजोने की प्रक्रिया देखते हैं तो संस्था का नज़रिया भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। हमारा अनुभव रहा है कि हम जब ख़ुद जानकार बनकर समस्या हल करने जाते हैं तो हल नहीं मिलता है। लेकिन अगर लोगों के ज्ञान को आधार बनाकर, हम समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मजबूत काम होता है।
ज़मीनी ज्ञान का संरक्षण अलग-अलग तरह के समाधान खोजने में मदद करता है। जैसे कि यह आजीविका के साधन तैयार करने में मददगार होता है। धीवर समुदाय के साथ काम करने के दौरान हमने समुदाय के साथ मिलकर तालाबों को ज़िंदा करने और मछली पालन का काम शुरू किया। दरअसल आजकल तालाबों में मछली उत्पादन कम होता जा रहा है और यह पूरे भारत में हो रहा है। प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन कम होने से मछुआरा समुदाय के सामने जीवन का संकट आ गया है। हमने अध्ययन किया तो पता चला कि तालाब मर रहे हैं। ज़मीन पर जाकर इसकी वजह टटोली और लोगों से पूछा कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है? यहां पानी है और तालाब गहरे भी हैं फिर यहां मछली उत्पादन क्यों नहीं हो पा रहा है?
इन सवालों के जवाब समुदाय ने ही दिए कि सिर्फ़ पानी होने का मतलब तालाब ज़िंदा होना नहीं होता है। तालाब के ज़िंदा रहने के लिए कई तरह की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं, मछलियों, पंछियों का होना ज़रूरी है।

हमने ऐसे तालाबों की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। हमने विषय के जानकारों के साथ चर्चा कर समस्या और समाधान के बारे में जानकारी ली। इसके बाद हमें लगा कि सैद्धांतिक रूप से तो हम समुदाय को बता सकते थे कि तालाब ज़िंदा करने के लिए क्या चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप से, ज़मीन पर यह काम करने के लिए हमें लोगों के साथ बैठना पड़ा। उनसे समझना पड़ा कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कहां कौन सा पौधा उगता है, कितनी गहराई होनी चाहिए, वग़ैरह। आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है कि इन लोगों के पास ये सारी जानकारी थी। सबने मिलकर योजना तैयार की और दो साल में तालाब को ज़िंदा कर दिया।
लोगों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम मछलियों की स्वदेशी किस्मों जैसे शिंगुर, दादाक, सवादा और मोथारी को तालाब में दोबारा लाए। ये प्रजातियां सरकार की राज्य-प्रायोजित योजना के माध्यम से तालाबों को आबाद किए जाने वाली और तेजी से प्रजनन करने वाली कम पौष्टिक कतला और रोहू जैसी मछलियों की तुलना में अधिक कीमत की थीं। लेकिन इसने काम किया और जैसे-जैसे तालाब फले-फूले, पारंपरिक आजीविका भी फली-फूली। इसके बाद क़रीब तीस-चालीस गावों में भी यही तरीक़ा आज़माया गया।
आमतौर पर, वंचित समुदायों के लिए विकास योजनाएं बनाते हुए समाजसेवी संस्थाएं या सरकारों का रवैया सुधारक या आपूर्तिकर्ता वाला होता है। वे देखती हैं कि समुदायों की कमज़ोरियां क्या हैं, उनके पास किस चीज की कमी है। लेकिन ज़मीनी ज्ञान समुदाय की ताक़त है और इसीलिए इस ज्ञान को सहेजा जाना ज़रूरी हो जाता है।
हर समुदाय की परंपरा और भाषा उसकी पहचान होती है। जब कोई भाषा खत्म होती है, तो वह संस्कृति भी खत्म हो जाती है। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, हिंदी पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन गांव की भाषा गांव की सीमा पर ही समाप्त हो जाती है। स्थानीय बोलियां बाहर से जाने वाली संस्थाओं के संचार करने में बाधा बन सकती हैं। साथ ही, परंपरागत ज्ञान रखने वाले लोग भी, अपने से अलग भाषा बोलने वालों पर मुश्किल से भरोसा करते है। इसलिए उनसे उनकी भाषा में बात करना महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्थानीय भाषाओं में पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करके, हम इन संस्कृतियों, पहचानों और इतिहास को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।
इतिहास और पौराणिक कथाएं न केवल किताबों और पत्थरों में संरक्षित हैं, बल्कि संस्कृति की विभिन्न अभिव्यक्तियों में भी संरक्षित हैं।
आराधी, महाराष्ट्र में देवी या देवी के लिए गाए जाने वाले पूजा गीतों की ऐसी ही एक संरक्षित शैली है। इन गीतों में हमारे मातृसत्तात्मक समाज का इतिहास शामिल है।
इस ज्ञान का संरक्षण करने के लिए हम गीतों के साथ-साथ संगीत वाद्ययंत्रों के सामाजिक इतिहास को भी एकत्रित और संरक्षित कर रहे हैं, जिनकी शिल्प संस्कृतियां लुप्त हो रही हैं। बिमानी या तबला कैसे बनता है? इसके लिए चमड़ा कहां से आता है? लकड़ी कहां से आती है? किस जानवर की खाल का उपयोग किया जाता है और वह जानवर कहां पाया जाता है? इन सभी सवालों के जवाबों का दस्तावेजीकरण आगे की पीढ़ियों के लिए काम आने वाला है।
जब लोग अपने पारंपरिक ज्ञान से आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं तो उन्हें गरिमा की भावना महसूस होती है। यह विशेष रूप से उनके लिए सच है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्ति से वंचित रहे हैं। भले ही, उनके पास विशेष ज्ञान हो, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय, उनके साथ होने वाले भेदभाव के चलते उचित सम्मान और अवसर नहीं हासिल कर पाए हैं।
अक्सर लोग रात में जत्रा (मेला) प्रदर्शन देखकर ताली बजाते हैं, लेकिन दिन में उसी गांव में, उसी कलाकार समुदाय के लिए नहाने और पीने का पानी जुटाना मुश्किल हो जाता है। हमारे कुछ लोक-कलाकारों एक अनुभव यह भी रहा कि एक बार उन्हें गांव वालों के साथ बैठाने की बजाय बाहर आंगन में अलग-अलग बर्तन में खाना परोसा गया था।
जब ऐसे समुदायों को उनके ज्ञान की शक्ति के बारे में बताया जाता है और इसे उनके काम में लागू करने के तरीके खोजे जाते हैं, तो उनमें आत्म-सम्मान की भावना होती है – और इससे न केवल वे लोग बल्कि पूरे समुदाय को फ़ायदा होता है।
गरिमा जिम्मेदारी की भावना और सांप्रदायिक चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत में तब्दील हो जाती है। इसे बढ़ावा मिलेगा तो ये नया आत्मविश्वास और नेतृत्व – सामाजिक न्याय, आजीविका और पर्यावरण की बड़ी समस्याओं को हल करने के तरीके खोजेगा।
अत्त दीप से जुड़ी हमारी शुरूआती बातचीत में ही हमने साफ़ समझ लिया था कि ज़मीनी ज्ञान और अकादमिक ज्ञान को हमें दो छोरों की तरह नहीं देखना चाहिए। यह जमीनी कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे ज्ञान धाराओं की पहचान करें और फिर समुदाय के साथ बातचीत के माध्यम से इसे औपचारिक रूप से विकसित करने का काम करें। ऐसा करने के चरण कुछ इस तरह हो सकते हैं:
हम सरकार, मीडिया, शिक्षा जगत, फंडिंग और नीति निर्धारण आदि से जुड़ रहे हैं, ताकि वे इस ज्ञान और अनुभव को समझें और इसे अपनी सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियाओं में शामिल करें। पारंपरिक आर्द्रभूमि प्रबंधन, वन अधिकार आंदोलनों और जाति-विरोधी गीतों के पाठों को गांव से बाहर ले जाने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें संस्थागत बनाया जाना चाहिए, और संरचित किया जाना चाहिए।
जाति-विरोधी गीतों के पाठों को गांव से बाहर ले जाने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें संस्थागत बनाया जाना चाहिए।
इसका एक उदाहरण नवयान महाजलसा एकैडमी का काम है जो शाहिरी (काव्य लेखन) और लोककला पर कोर्सेज बना रही है। ये जितनी भी लोककलाएं हैं, उनकी शुरूआत, इतिहास, इसमें योगदान करने वाले लोगों के नाम, कितने समय से यह चल रहा है, इसके कितने प्रकार होते हैं जैसी तमाम बातें उस सिलेबस में रहेंगी। यहां तक कि वाद्ययंत्रों से जुड़े एक शोध में लुप्त होते जा रहे वाद्यों के बनने के कहानी, उनकी प्रक्रिया और उनका तात्कालिक समाजिक महत्वों को भी यह एकैडमी दर्ज कर रही है। इस तरह की जानकारी को जब विश्वविद्यालयों और उनमें पढ़ने वालों तक पहुंचाया जा सकेगा, तब बात बन सकेगी। इस तरह के जुड़ाव ही, दोनों सिरों को साथ लाना ही एक माध्यम हो सकता है। ज़मीनी ज्ञान के प्रति जो नकारात्मकता और अस्वीकार है, उससे पार पाने का रास्ता इसी में खोजना पड़ेगा।
जमीनी स्तर के लोग खुद को ज्ञान धारक और ज्ञान निर्माता के रूप में नहीं सोचते हैं। लोकप्रिय धारणा यह है कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हम जानकार नहीं हैं। समाज ने ही इस धारणा को पुष्ट किया है। हमें इस ग़लतफ़हमी को दूर करना होगा और लोगों को अपने बारे में अलग तरह से सोचने में सहयोग देना होगा।
—
भारत सरकार ने दिसंबर 2023 में, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। यह योजना वन और निजी भूमि दोनों से प्राप्त, इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादों (एनटीएफपी) पर थर्ड-पार्टी सर्टिफ़िकेशन प्रदान करती है। यह वे उत्पाद हैं जिनका उत्पादन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। योजना का उद्देश्य, स्थायी वन प्रबंधन (सस्टेनेबल फ़ॉरेस्ट मैनेजमेंट) और कृषि वानिकी (खेतों पर पेड़) को बढ़ावा देना और सर्टिफ़िकेशन के माध्यम से वन उत्पादों के बाजार मूल्य को बढ़ाना है।
अब भारत में कई निजी और सरकारी एजेंसियां, सर्टिफिकेट प्रदान कर रही हैं, जैसे कि साल 2003 में शुरू हुई छत्तीसगढ़ सर्टिफ़िकेशन सोसायटी। नई योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के साथ सर्टिफिकेट देने वाली इकाइयों के पंजीकरण को अनिवार्य करना है। साथ ही, राष्ट्रीय कार्य योजना कोड, 2023 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और संकेतकों के आधार पर सर्टिफिकेट प्रदान करके, प्रमाणन एजेंसियों और प्रक्रियाओं को विनियमित करना है।
इससे एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या सर्टिफ़िकेशन से भारत के सात करोड़ हेक्टेयर से अधिक वनों के स्थायी प्रबंधन की व्यवस्था हो सकती है। और, राज्य वन विभागों, वन-निर्भर समुदायों और अपने खेतों पर पेड़ उगाने वाले किसानों को लाभ हो सकता है।
भारत में स्थायी वन प्रबंधन की यह अवधारणा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। भारतीय वन अधिनियम, 1865 के बाद सरकार ने जहाज निर्माण और रेलवे स्लीपर बिछाने के लिए लकड़ी के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए वन भूमि को अपने नियंत्रण में ले लिया था। साल 1864 और 1883 के बीच भारत के पहले वन महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रैंडिस ने सबसे पहले स्थायी वन प्रबंधन की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था।

इसके पीछे विचार यह था कि जंगल से लकड़ी की उचित मात्रा में कटाई की जाए। इसके लिए, प्रत्येक वन प्रभाग को अलग-अलग लकड़ी की वृक्ष प्रजातियों के कार्य मंडलों में विभाजित किया जाना था। प्रत्येक कार्य मंडल को खंडों में विभाजित किया गया। पेड़ों की कटाई के काम को पूरे जंगल में वितरित करके, जंगल का पुनर्जनन सुनिश्चित किया गया और लकड़ी का भंडार बनाए रखा गया। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक सरकार को लकड़ी की लगातार आपूर्ति करना था।
प्रत्येक वन प्रभाग के लिए एक वन कार्य योजना तैयार की जानी थी, जिसमें उपलब्ध लकड़ी की अनुमानित मात्रा का वर्णन किया गया था। इसमें यह भी बताया गया था कि 10 से 15 साल की अवधि में इसकी कटाई कैसे की जाएगी। पहला राष्ट्रीय वन कार्य योजना कोड, जो कार्य योजना तैयार करने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में काम करता था, 1881 में प्रकाशित किया गया था।
लेकिन, लकड़ी के उत्पादन को अधिकतम करने के एकमात्र उद्देश्य को पूरा करने के क्रम में, स्थायी वन प्रबंधन के अन्य पहलुओं, जैसे जैव विविधता और वन-निर्भर समुदायों की आजीविका, को औपनिवेशिक काल में बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया था। सागौन जैसी मूल्यवान लकड़ी देने वाले वृक्षों को वन्यजीव- समृद्ध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोपा गया था, और आज भी भारत के कई बाघ अभयारण्यों में ये बहुतायत में दिखाई पड़ते हैं। हिमालय में देवदार के पेड़ों से इमारती लकड़ी सतलज घाटी जैसे कुछ स्थानों पर इनके ख़त्म होने तक निकाली जाती थी।
आज़ादी के बाद, साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप तक जंगल में देवदार के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई। गोदावर्मन बनाम भारत संघ के नाम से प्रसिद्ध यह मामला भारतीय वानिकी में एक मील का पत्थर था। याचिका निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई के कारण दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जंगल, स्वामित्व की परवाह किए बिना, उसकी कार्य योजना के तहत माना जाना चाहिए। इसका मतलब यह था कि निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई कार्य योजना के अनुसार होगी और इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी।
इस फैसले का निजी भूमि और 1,500 मीटर से ऊपर स्थित जंगलों और उत्तर-पूर्व भारत में वनों की कटाई को कम करने की योजना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जहां इसने पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसका नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि इसने कई राज्य वन विकास निगमों को बेकार बना दिया और किसानों को अपने खेतों में पेड़ उगाने को लेकर प्रोत्साहित नहीं किया।
राज्य वन विकास निगमों की स्थापना साल 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। निगमों का उद्देश्य वन वृक्षारोपण और लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की समुचित तरीके से उत्पादन करना था, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग दिया जा सके।
साल 1996 के फैसले के बाद, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम जैसे कई राज्य वन विकास निगमों की गतिविधियां राल इकट्ठा करने (पाइनस रॉक्सबर्गी से) और जंगल से बचे हुए पेड़ निकालने तक सीमित हो गईं। किसानों को उनके खेतों में पेड़ उगाने में मदद करने के लिए, 1999 में मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई लोक वानिकी योजना सफल नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को भी पेड़ काटने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए नौकरशाही प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता था। वास्तव में, इसने उनके पेड़ लगाने के उत्साह पर गहरा असर डाला।
विश्व स्तर पर, साल 1993 में जर्मनी के बॉन में एक समाजसेवी संगठन के रूप में फारेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल (एफएससी) की स्थापना की गई थी जो एक अग्रणी वन प्रमाणन एजेंसी है। एफएससी का लक्ष्य, दुनियाभर में जंगलों के ऐसे प्रबंधन को बढ़ावा देना है जो पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त, सामाजिक रूप से लाभकारी और आर्थिक रूप से व्यवहारिक हों। अपनी वेबसाइट पर इस काउंसिल का दावा है कि यह प्रमाणन 89 देशों में लगभग 16 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि को कवर करता है।
वर्षों से, वन प्रमाणन का ज़िक्र चिली और पेरू जैसे कुछ देशों में अवैध कटाई को कम करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन मेक्सिको और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे देशों में वनों की कटाई को कम करने वाले एकमात्र कारक के रूप में इसे पहचान नहीं मिली है। वानिकी शोधकर्ता अभी भी प्रमाणन के प्रभावों पर बहस करते हैं क्योंकि सामुदायिक अधिकारों की मान्यता, वन संरक्षण पर नीतियां, इत्यादि जैसे कई अन्य कारक स्थायी वन प्रबंधन को प्रभावित करते हैं।
जब लकड़ी के अलावा अन्य वनोपज की बात आती है तो सर्टिफ़िकेशन का महत्व और भी कम लगने लगता है।
इसके अलावा, सर्टिफ़िकेशन एक महंगी प्रक्रिया है। वियतनाम में बबूल के बागानों के सर्टिफ़िकेशन के मामले में बहुत ही कम लाभ देखने को मिला और वह भी तब जब वृक्षारोपण तीन हज़ार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर किया गया था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि कम जोत वाले किसानों को इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला।
भारत के मामले में, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गनाइजेशन द्वारा कराए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि 2020 में भारत में राउंडवुड की मांग – जो मुख्य रूप से फर्नीचर बनाने, कागज और लुगदी, पैनल और प्लाईवुड और निर्माण के लिए उपयोग की जाती है – लगभग 57 मिलियन क्यूबिक मीटर थी। इसमें से 47 मिलियन घन मीटर मांग को घरेलू स्तर पर पूरा किया गया। इसमें 45 मिलियन क्यूबिक मीटर जंगलों के बाहर के पेड़ों से था और केवल 2 मिलियन क्यूबिक मीटर सरकारी स्वामित्व वाले जंगलों से आया था।
इस संदर्भ में, सर्टिफ़िकेशन एक निरर्थक प्रक्रिया लगती है क्योंकि चिनार, सागौन और नीलगिरी के ब्लॉक वृक्षारोपण मौजूद होने के कारण बड़ी मात्रा में लकड़ी का उत्पादन जंगलों के बाहर के पेड़ों से किया जाएगा। घरेलू इस्तेमाल के लिए लकड़ी ख़रीदने वाले शायद ही प्रमाणित लकड़ी का ध्यान रखते हैं। निर्यात के मामले में देखें तो साल 2020 में सागौन और शीशम की बहुत कम मात्रा- 0.01 मिलियन क्यूबिक मीटर – ही निर्यात की गई। घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित लकड़ी की मांग में किसी भी तरह का बदलाव उन अपेक्षाकृत अमीर किसानों के पक्ष में झुक सकता है जो प्रमाणन का खर्च उठा सकते हैं। यह छोटे किसानों को अपने खेतों में पेड़ उगाने से भी हतोत्साहित कर सकता है।
अन्य वनोपज के मामले में सर्टिफ़िकेशन का महत्व और भी कम प्रतीत होता है। मध्य भारत में महुआ के फूल, साल के बीज और तेंदू के पत्तों जैसी उपज और हिमालय की घाटियों में डोडेंड्रोन फूल और पाइन के कोन एकत्र करके उन्हें स्थानीय स्तर पर बेचा जाता है। इनमें से किसी के भी कच्चे रूप में निर्यात किए जाने का कोई प्रमाण नहीं है।
भारत ने साल 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति से अपनी कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था लेकिन लगभग एक दशक बाद इसमें शायद ही कोई सुधार दिखता है।
विभागों की बात करें तो लकड़ी निकालने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू 1996 के प्रतिबंध अभी भी हैं। उन्हें नवीनतम कार्य योजना कोड के अनुसार कार्य योजनाएं तैयार करनी होती हैं और उन्हें अनुमोदित करना होता है। इसमें लकड़ी की वह मात्रा शामिल होनी चाहिए जिसे जैव विविधता और वन-निर्भर समुदायों की जरूरतों को प्रभावित किए बिना उचित रूप से निकाला जा सकता है। तभी सर्टिफ़िकेशन से वन उत्पादों का निर्यात होने पर मूल्यवर्धन होगा।
वन-निर्भर समुदायों के लिए, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत लगभग 60.5 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। समुदाय, अपने सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) प्रावधानों का उपयोग करके वनोपज निकाल रहे हैं और उनकी बढ़िया मार्केटिंग कर लाभ हासिल कर रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। वनों पर निर्भर लाखों समुदाय अभी भी अधिकारों के बिना, अपनी आजीविका के लिए वन उत्पादों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, समुदायों को दिए गए प्रबंधन अधिकारों के तहत लकड़ी निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वन विभाग मान्यता प्राप्त सामुदायिक अधिकारों के साथ जंगलों में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं।
भारत ने 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति के माध्यम से अपनी कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था। इसने किसानों को पेड़-पौधे आसानी से उपलब्ध कराए और पेड़ों की कटाई और उन्हें दूसरे क्षेत्रों में भेजने पर लगे प्रतिबंध में ढील दी। लेकिन इसके लगभग एक दशक बाद भी कृषि वानिकी में शायद ही किसी तरह का सुधार देखा गया है। हाल ही में, ‘सिव्यर डिक्लाइन इन लार्ज एग्रोफ़ॉरेस्ट्री ट्रीज इन इंडिया ओवर द पास्ट डिकेड’ शीर्षक से एक अध्ययन किया गया जिसमें मैंने भी अपना योगदान दिया था। इस अध्ययन में यह बात सामने आई है कि भारत में खेतों में लगे परिपक्व पेड़ों के भारी कमी देखी गई है। इसके पीछे के कारणों में, फसल पैटर्न में बदलाव, मशीनीकृत खेती और किसानों को किसी भी प्रकार का लाभ ना होना है। अपने खेतों में पेड़ लगाने से किसानों को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होता है।
संक्षेप में कहें तो, वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि वन सर्टिफ़िकेशन से बाजार मूल्य में मामूली वृद्धि होती है लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत खर्चीली है। यह सीमांत किसानों और वन निर्भर समुदायों के लिए किसी भी प्रकार से मददगार नहीं है। इसके अलावा, केवल सर्टिफ़िकेशन से ना तो स्थायी वन प्रबंधन होता है और ना ही कृषि वानिकी को बढ़ाने में मदद मिलती है।
भारत में वनों के क्षरण का कारण वनों का उपयोग खनन, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे जैसे गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए करना है। इसके अलावा आग, मवेशियों के चरने और लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियां भी इसे नुक़सान पहुंचाती हैं।
घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक वनों, जो अपने आपमें महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं, पर वृक्षारोपण न करने की सावधानी बरती जानी चाहिए।
वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका बढ़ाने और वन-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जल-धाराओं और नदियों के प्रवाह जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी वन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। सर्टिफ़िकेशन से अधिक, वनों के प्रबंधन और लकड़ी और अन्य वनोपजों को स्थायी रूप से निकालने के लिए एक अच्छी कार्य योजना की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय कार्य योजना कोड जिसे साल 2014 और अंतिम बार 2023 में संशोधित किया गया था। यह कोड एक कार्य योजना के ज़रिए वनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है जो जैव विविधता, कार्बन पृथक्करण और चराई और जलाऊ लकड़ी संग्रह सहित स्थानीय समुदायों की आजीविका जैसी आवश्यकताओं पर विचार करता है।
कांगो बेसिन में किए गये एक अध्ययन में यह बात स्पष्ट हुई है कि स्थायी वन प्रबंधन के मामले में इमारती लकड़ी की चक्रीय उपज वाली वन प्रबंधन योजना और वन-निर्भर समुदायों के साथ, लाभ को साझा करने वाली एक स्पष्ट योजना, वन सर्टिफ़िकेशन की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हुई है।
लकड़ी की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए जंगलों के बाहर वृक्षारोपण बढ़ाया जा सकता है। इससे प्राकृतिक वनों पर दबाव और उनकी कटाई में कमी आ सकती है। आगे बढ़ने का एक संभावित तरीका यह है कि वन विकास निगमों को बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए और किसानों को अपनी परती या बंजर भूमि पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जल-जमाव वाली और निम्नीकृत भूमि का उपयोग प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसे तेज़ी से बढ़ने और फैलने वाली प्रजातियों के वृक्षारोपण के लिए भी किया जा सकता है।
अंग्रेजों के समय में लगाये गये पाइन और युकिलिप्टस जैसे पेड़ों को धीरे-धीरे हटाकर देशी साल और ओक के पेड़ों को लगाया जा सकता है जो हमारे लिए एक संसाधन हैं।
निम्नीकृत भूमि में सीएफआर वाले समुदायों को उत्पादित लकड़ी से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया के साथ वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अंत में, एक कार्य योजना के अनुसार पेड़ों को काटने, उन्हें दूसरी जगह ले जाने और बेचने की प्रक्रियाओं को सरकारों और किसानों दोनों के लिए आसान बनाया जाना चाहिए।
घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक वनों पर वृक्षारोपण से बचना चाहिए क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। अच्छी कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य के वन विभागों की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। ताकि वे वृक्षारोपण क्षेत्रों की पहचान, गुणवत्तापूर्ण वृक्षारोपण, और पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए प्राकृतिक वनों को संरक्षित करते हुए स्थायी रूप से लकड़ी की कटाई जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम कर सकें।
अंत में, ऊपर दिये गये सुझावों को अपनाने से भारत में स्थायी वन प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और किसानों और इससे राज्य वन विभागों की आय, वन सर्टिफ़िकेशन की तुलना में अधिक बढ़ेगी।
यह लेख मूलरूप से द इंडिया फोरम पर प्रकाशित हुआ था।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में थारू आदिवासी पारंपरिक घरों में रहते हैं। इन घरों की छतें (छप्पर) फूस से बनी होती हैं और दीवारें पेड़ के तनों और मिट्टी से बनाई जाती हैं। जंगल से इकट्ठी की गयी, घर बनाने की यह सामग्री गर्मियों के दौरान हमारे घरों को ठंडा रखती थीं। जंगलों ने हमें हमारा घर बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए और बदले में हमने इसकी रक्षा की।
लेकिन, 1977 में दुधवा नेशनल पार्क के निर्माण के बाद से वन विभाग ने जंगलों तक हमारी पहुंच प्रतिबंधित कर दी है। इसने हमारे आवास को बड़े पैमाने पर बदल दिया है। घास तक पहुंच की कमी के कारण, अब हमारे घरों में टिन की छतें हैं।
इसके अलावा, नेशनल पार्क में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, विभाग ने आधुनिक कॉटेज बनाए हैं जिन्हें वे थारू हट (झोपड़ी) कह रहे हैं। शहर के लोग इन कॉटेज में रहने आते हैं क्योंकि वे थारू संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं।
पार्क के अंदर, विभाग का ऑफिस हमारी संस्कृति और हमारे पारंपरिक पहनावे के बारे में जानकारी दिखाते हैं। और, इसके ठीक उलट हमें हमारा पारंपरिक जीवन जीने से रोकते हैं। मूलरूप से हमारी संस्कृति ही उनके लिए पर्यटन ला रही है लेकिन उससे जुड़ी आय में हमें कोई हिस्सा नहीं मिलता है।
सहबिनया राना थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच की महासचिव हैं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
अधिक जाने: जानें कैसे खेती के लिए थारु समुदाय जलवायु परिवर्तन और सरकारी विभागों से जूझ रहा है।
जब समाजसेवी संस्थाएं अपने काम के प्रभाव (इम्पैक्ट) के बारे में बात करती हैं तो वे भीतर ही भीतर क्या महसूस करती हैं- 
जब फंडर्स अपने उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बता रहे हों, तब समाजसेवी संस्थाएं
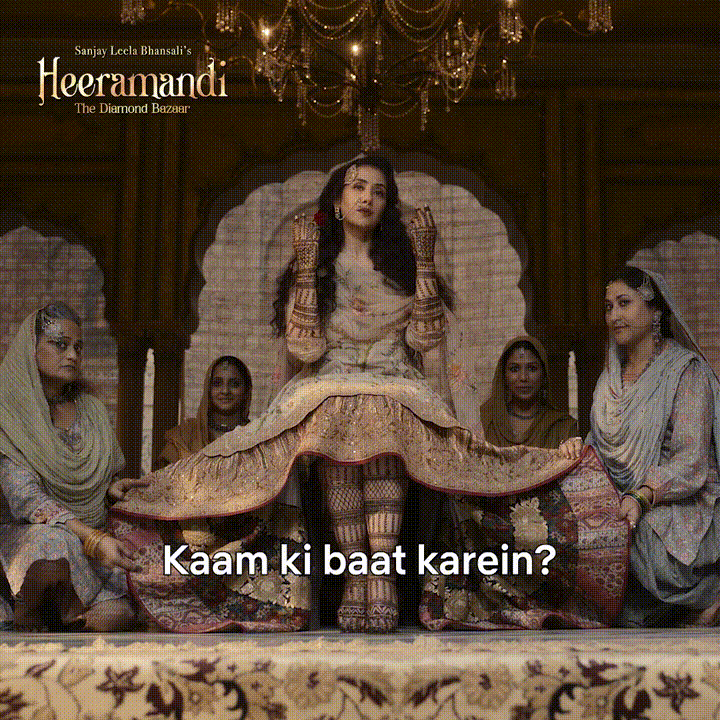
जब अपने पैरों पर चलने के लिए संघर्ष कर रही संस्था को प्रोग्राम रेस्ट्रिक्टेड फ़ंडिंग मिले, और उसे स्वीकार करनी पड़े-

जब फ़ंडिंग ना मिलने का ईमेल मिले-

जब समाजसेवी संस्था समुदाय की कोई नई समस्या खोजकर सामने लाए और उसके पास उसका समाधान भी हो-
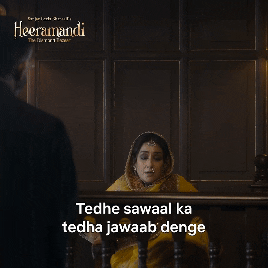
जब कोई कार्यक्रम (प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन) सफलता के साथ पूरा हो जाए-
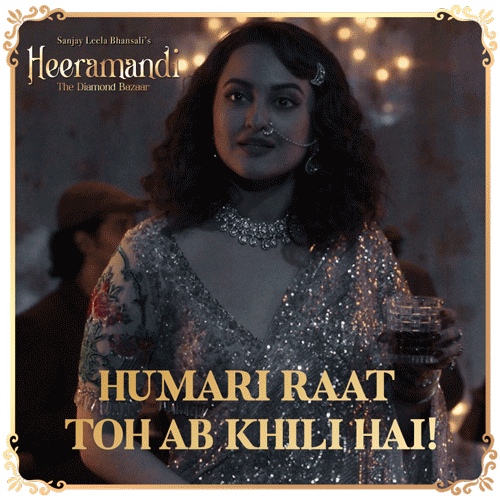
जब एफसीआरए को लेकर सरकार कुछ कहे तो समाजसेवी संस्थाओं को क्या सुनाई देता है-
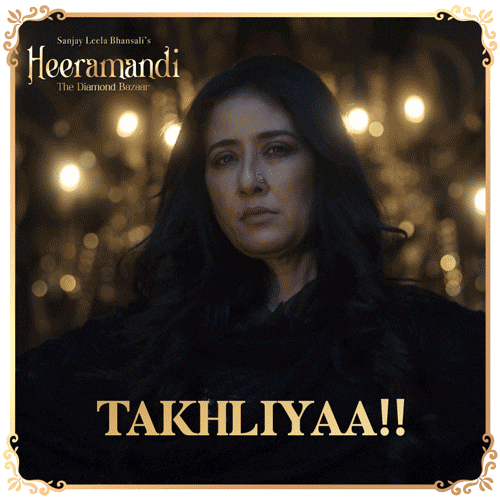
और, कुछ मौक़े ऐसे भी आते हैं जब समाजसेवी संस्थाएं समुदायों की नहीं सुनती हैं, तब समुदाय-

दिल्ली की एक फील्डवर्कर रमा के जीवन के एक दिन की झलक पाने के लिए यह वीडियो देखें। रमा भलस्वा में कूड़ा बीनने वालों की मदद करती हैं। उनके सहयोग से समुदाय ने लकड़ी के चूल्हे से एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल तक का सफ़र तय किया है। ज़मीनी स्तर पर काम करने का पंद्रह वर्षों का अनुभव रखने वाली रमा की सुबह काम से जुड़े फ़ोनकॉल्स और घर के कामों से शुरू होती है। दिनभर का काम निपटाने के बाद शाम में रमा को किशोर कुमार के गीत सुनते हुए चाइनीज़ फ़ूड ख़ाना पसंद है। इस वीडियो में रमा ने अपने काम की प्रकृति के कारण पेशेवर और व्यक्तिगत, दोनों ही जीवनों में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया है। उनका सपना घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं के लिए एक आश्रयगृह बनाने का है। साथ ही, वे राजनीति में सक्रियता से शामिल होकर क्षेत्र की एमएलए बनना चाहती हैं।
मेरा नाम रमा है और मैं अपने पति और दो बेटों के साथ जहांगीरपुरी में रहती हूं। पहले एक आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में और फिर एक आशा कार्यकर्ता के रूप में समुदायों के साथ ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए मुझे लगभग पंद्रह वर्ष हो चुके हैं। वर्तमान में, मैं यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ वायु और बेहतर स्वास्थ्य (सीएबीएच) परियोजना की भागीदार संस्था असर के साथ एक परिवर्तन एजेंट के रूप में काम कर रही हूं। इसके अलावा मैं भलस्वा में लोगों को खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन को अपनाने में मदद करती हूं। भलस्वा उत्तर पश्चिमी दिल्ली में स्थित और एक लैंडफ़िल से घिरा हुआ इलाक़ा है। यहां रहने वाले लोग मुख्य रूप से कचरा बीनने का काम करते हैं। भलस्वा में ज़्यादातर घरों में खाना पकाने के लिए चूल्हे का उपयोग होता है, जिससे घरेलू वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है और खाना पकाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, एलपीजी गैस सिलेंडर एक स्वच्छ विकल्प है। वे न केवल वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करते हैं, बल्कि उपयोग में आसान होते हैं और चूल्हे के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने में लगने वाला समय भी बचता है।
मैं भलस्वा में महिलाओं और पुरुषों के साथ, आग और लकड़ी या कोयले जैसे ईंधन से खाना पकाने के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही हूं। हालांकि, लोग अब भी कई कारणों से इस परिवर्तन को अपनाने से झिझकते हैं जिसमें सबसे मुख्य एलपीजी की ऊंची क़ीमत है। साल 2016 में शुरू की गई, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) खाना पकाने के स्वच्छ तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सिलेंडर की लागत पर भारी छूट देती है। हालांकि, भलस्वा में रहने वाले कई लोगों के पास अभी भी योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक सही दस्तावेज़, जैसे आधार कार्ड और श्रमिक कार्ड वग़ैरह नहीं हैं।
नतीजतन, मेरा काम न केवल खाना पकाने के स्वच्छ तरीक़ों के फ़ायदों पर बात करना है बल्कि पीएमयूवाई योजना को लेकर जागरूकता पैदा करना और इन लाभों को उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज को प्राप्त करने में मदद करना भी है।
सुबह 6:00 बजे: आमतौर पर मेरी नींद फोन की घंटी से खुलती है। अक्सर भलस्वा से हमेशा कोई न कोई यह पूछने के लिए फोन करता है कि मैं उनके पड़ोस में कब आ रही हूं या फिर उसे अपने पीएमयूवाई फॉर्म की स्थिति के बारे में पूछताछ करनी होती है। आज की सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। फोन कॉल की अफ़रा-तफ़री के बीच मैं और मेरे पति परिवार के लिए सुबह का नाश्ता बनाने में व्यस्त थे। हम अपने बच्चों के दोपहर के खाने की भी तैयारी करते हैं। मेरा बड़ा बेटा बारहवीं में पढ़ता है और छोटा वाला आठवीं कक्षा में है। मेरे पास एक कुत्ता भी है जिसका नाम टिमसी है। मेरे एक रिश्तेदार ने मेरे जन्मदिन पर मुझे दिया था। उसे खाना खिलाना और सुबह टहलाना भी जरूरी है। मेरे पति ऑटो चलाते हैं। काम पर जाने से पहले वही उसकी देखभाल करते हैं।
इन सभी कामों में परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी होती है। मुझे लगता है कि उनके सहयोग के बिना प्रति दिन फ़ील्ड में जाकर काम करना मेरे लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता। मुझे वह दिन आज भी याद है जब मैंने पहली बार साल 2011 में आंगनवाड़ी सहायक के रूप में ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू किया था। उस समय मेरा छोटा बेटा केवल एक साल का था। मेरे रिश्तेदार लगातार मुझे इस काम को छोड़ने की सलाह देते थे ताकि मैं अपने बेटे की देखभाल कर सकूं। मेरे भाई ने तो मुझे वेतन के बदले प्रति माह 3 हज़ार रुपये देने का वादा तक कर दिया था। हालांकि, मैंने अपना काम जारी रखा और अपने बच्चे को प्रति दिन अपने साथ काम पर लेकर जाती थी। मैं हमेशा से ही लोगों की मदद करना चाहती थी और मुझे ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में योगदान देने का यही एक तरीक़ा है।
आमतौर पर सुबह, मैं अपने लिए आलू पराठा बनाती हूं ताकि शाम में काम पर से वापस लौटने तक मेरा पेट भरा रहे। मैं इसलिए भी ऐसा करती हूं कि क्योंकि मैं फ़ील्ड पर नहीं खा सकती। अपना नाश्ता ख़त्म करने के बाद एक नज़र पिछली रात तैयार की गई अपनी दिनचर्या पर डालती हूं। ज़्यादातर दिनों में मेरे काम में घर-घर जाकर जागरूकता फैलाने, जन जागरूकता सत्रों का आयोजन करना और पीएमयूवाई के लिए आवेदन करने में लोगों की मदद करना शामिल होता है।
मैं कचरा चुनने वालों के साथ काम करती हूं। वे अपना काम सुबह जल्दी शुरू करते हैं और दोपहर तक अपने घर वापस लौटते हैं। इसलिए मुझे अपनी दिनचर्या उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही बनानी होती है। आज मुझे जन जागरूकता सत्र आयोजित करना है और उसके बाद पीएमयूवाई योजना के लिए आवेदन करने में कुछ महिलाओं की मदद करनी है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा बहुत फेर-बदल करने के बाद मैं तैयार होकर भलस्वा के लिए निकल जाती हूं।
सुबह 10:00 बजे: सबसे नज़दीकी बस स्टॉप मेरे घर से दस मिनट की पैदल दूरी पर है। पंद्रह मिनट के इंतज़ार के बाद एक बस मिलती है जो मुझे सड़क की दूसरी छोर पर उतारती है। कई बार मुझे यह दूरी पैदल ही पूरी करनी पड़ती है लेकिन आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और मैं जल्दी थकना नहीं चाहती हूं। पंद्रह मिनट के इंतज़ार के बाद मैं बस लेती हूं। बस से उतरने के बाद आगे जाने के लिए रिक्शा लेती हूं। उसी दिशा में जाने वाली दूसरी सवारियों के आने तक मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। मैं 11 बजे तक भलस्वा पहुंचती हूं।
भलस्वा एक बहुत बड़ा इलाक़ा है और धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में केवल पश्चिम बंगाल के लोग रहते हैं वहीं कुछ में केवल मुसलमान परिवार ही रहते हैं। भलस्वा में रहने वाले विभिन्न समूह अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं और उनकी अलग-अलग संस्कृतियां हैं, जिन्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में समझ पाना एक मुश्किल काम है। हालांकि आंगनबाड़ी सहायक और आशा कार्यकर्ता के रूप में मेरे काम की अलग चुनौतियां थीं, लेकिन उसके बावजूद भी जिन समुदायों की मैंने सेवा की, उनके साथ मैं काफी आसानी से और जल्दी मजबूत रिश्ते बना लेती थी। लेकिन भलस्वा में मेरी यात्रा कठिन रही है, ख़ासतौर पर इसलिए कि यहां के समुदायों का समाजसेवी संस्थाओं और बाहर से आए लोगों के साथ अनुभव अच्छा नहीं रहा था। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले, स्वयं को समाजसेवी संस्था बताने वाले एक समूह ने स्थानीय लोगों को पांच सौर रुपये के बदले सिलाई मशीन देने का वादा किया था। लेकिन, उन्हें न तो कभी कोई मशीन मिली और ना ही अपने पैसे। इसलिए मेरा काम सबसे पहले उनका विश्वास हासिल करना था। समुदाय की विविधता के कारण भी यह काम पेचीदा हो गया था।
भलस्वा के लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए मैंने ऐसे लोगों से रिश्ता बनाना शुरू किया जिन्हें इलाक़े में लोग जानते थे और इनमें आशा कार्यकर्ताएं भी शामिल थीं। उन्हीं दिनों, मुझे समाजसेवी संस्थाओं को लेकर समुदाय के मन में बैठे संदेह को दूर करने की दिशा में भी काम करना था। ऐसा करने का एक तरीका लोगों की मदद करने के लिए क्षेत्र में समाजसेवी संस्थाओं के मेरे नेटवर्क का उपयोग करना था। उदाहरण के लिए, मैंने 12 साल की एक विकलांग लड़की को व्हीलचेयर दिलवाने में मदद की। मेरे इस काम में मेरी मदद एक ऐसे समाजसेवी संस्था ने की जिनके साथ मैंने पहले काम किया था। समय के साथ इन दोनों तरीक़ों से मैंने समुदाय के लोगों के साथ जल्द ही अपना रिश्ता बना लिया और कुछ ही दिनों में मेरा फ़ोन भलस्वा की उन महिलाओं के नंबर से घनघनाने लगा जिन्हें मेरे मदद की ज़रूरत थी।
सुबह 11:15 बजे: भलस्वा पहुंचकर मैं वहां की स्थानीय दवा दुकान पर जाती हूं जहां मेरी मुलाक़ात कुछ आशा कार्यकर्ताओं से होती है। उनमें से कुछ से मेरी अच्छी दोस्ती है और साथ देने वाली महिलाओं के ऐसे समूह से मुझे प्रेरणा मिलती है। अपने-अपने दिन से जुड़ी बात करने के अलावा हम लोग समुदाय की ओर से आने वाली विशेष शिकायत पर भी चर्चा करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों पहले भलस्वा में आये एक परिवार ने उनसे एलपीजी सिलेंडर के लिए संपर्क किया था और उन्होंने उस परिवार को मेरा मोबाइल नंबर दे दिया है।
दवा दुकान पर मैं कुछ अन्य महिलाओं से भी मिली जिन्हें मैंने अपने एजेंडे के अगले आइटम – सामुदायिक जागरूकता सत्र – पर जाने से पहले सिलेंडर प्राप्त करने में मदद की थी।

दोपहर 12:00 बजे: सामुदायिक जागरूकता सत्रों का आयोजन दवा दुकान के बग़ल वाले मंदिर में होता है। आज लगभग 10–15 महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। उनमें से ज़्यादातर अपने नवजात बच्चों के साथ आई हैं जिन्हें वे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकतीं। एक बार सबके बैठ जाने के बाद मैंने असर द्वारा विकसित टूलकिट निकाला। यह 17 पेज लंबा एक दस्तावेज है जिसमें चित्रों के माध्यम से वायु प्रदूषण और उसके कारणों को समझाया गया है। इसमें लंबे समय तक लकड़ी वाले ईंधन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया है।
इस सत्र के दौरान, मैं चूल्हे के बहुत लंबे समय तक उपयोग के कारण खाना पकाने वाली महिलाओं के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में बताती हूं। इसमें हृदयाघात, फेफड़ों में रुकावट वाली बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर और छोटे बच्चों में तीव्र श्वसन संबंधी बीमारियों जैसी स्थितियां शामिल हैं। महिलाएं इन सत्रों में सक्रियता से भाग लेती हैं और प्रश्न-उत्तर के साथ ही अपने अनुभव भी साझा करती हैं। इन सत्रों के माध्यम से मेरा लक्ष्य न केवल वहां उपस्थित लोगों को सूचित करना है बल्कि मैं चाहती हूं कि वे इन जानकारियों को अपने ऐसे अन्य साथियों से भी साझा करें जो अब भी एलपीजी के इस्तेमाल को लेकर संशय में हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें चूल्हे पर खाना पकाने की आदत हो चुकी है और वे एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर सशंकित रहते हैं। महिलाओं, विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं द्वारा की जाने वाली शिकायतों में एक सबसे आम शिकायत यह होती है कि चूल्हे पर पकाया गया खाना अधिक स्वादिष्ट होता है। गलतफ़हमी को दूर करने के लिए, मैं आमतौर पर उन्हें समुदाय की एलपीजी का उपयोग कर रही अन्य महिलाओं से बात करने के लिए प्रोत्साहित करती हूं। ये महिलाएं बताती हैं कि कैसे अब खाना बनाते समय उनकी आंखें नहीं जलती हैं, और कैसे उनकी सांस संबंधी समस्याओं में भी कमी आई है।
एलपीजी सिलेंडर को अपनाने के कारण भलस्वा के लोगों को एक महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ा है।
एलपीजी सिलेंडर को अपनाने के कारण भलस्वा के लोगों को एक महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ा है। इनमें से अधिकांश लोगों का पेशा कचरा बीनना है और वे ईंधन के लिए इतने पैसे खर्च करने की क्षमता नहीं रखते हैं। इन सत्रों में अक्सर इसी विषय पर बहस और चर्चा होती है। इसका सामना करने के लिए, मैं अक्सर महिलाओं को एलपीजी के इस्तेमाल से लंबे समय में होने वाले फ़ायदों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती हूं। पारंपरिक चूल्हों के लिए लकड़ी और अन्य ईंधन से अपने दैनिक खर्चों का एक हिस्सा बचाकर वे धीरे धीरे एलपीजी रिफिल का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त बचत कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, प्रति दिन 30 से 40 रुपये की बचत कर लेने से इतने पैसे जमा हो सकते हैं कि महीने के अंत में सिलेंडर रीफ़िल का खर्च उठाया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, मैं उनका ध्यान पीएमयूवाई के तहत मिलने वाले लाभों की ओर आकर्षित करती हूं, जिसे आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा 2021 में फिर से लॉन्च किया गया था। पीएमयूवाई के तहत, पहला सिलेंडर और इसे लगाने में होने वाला खर्च हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए मुफ्त है, जिसके बाद वे रियायती दरों पर एलपीजी गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थियों को पहली रिफिल के लिए 1,600 रुपये मिलते हैं, जिसमें 14 किलोग्राम सिलेंडर और इसे लगाने में होने वाला खर्च शामिल है। अगले 12 रिफिल में से प्रत्येक के लिए अतिरिक्त 300 रुपये प्रदान किए जाते हैं। पहले, इन भुगतानों में अक्सर देरी होती थी, लेकिन दोबारा लॉन्च के बाद से, काफी हद तक इसमें सुधार आया है।
पीएमयूवाई के लिए दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया गया है, फिर भी लोगों को सही कागजी कार्रवाई करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
इससे पीएमयूवाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई को पूरा करने के रूप में एक अन्य चुनौती भी सामने आती है। हालांकि पीएमयूवाई के लिए दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया गया है, फिर भी लोगों को सही कागजी कार्रवाई करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आवश्यक दस्तावेजों में से कुछ में राशन कार्ड, पते का प्रमाण, आधार कार्ड या जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं। यदि कोई दूसरे राज्य से दिल्ली आया है – जो भलस्वा में काफी आम है – तो उन्हें निवास प्रमाण पत्र, जैसे बिजली बिल और रेंट एग्रीमेंट की भी आवश्यकता होगी। ऐसे भी मामले हैं जिनमें लोगों के पास किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं है, और इन स्थितियों में प्रवासी कार्ड या श्रमिक कार्ड भी पर्याप्त है।
कल ही, एक महिला जिसके पास कोई भी आवश्यक दस्तावेज नहीं था, उसने योजना के बारे में पूछताछ की। मैंने उससे कहा कि वह अभी भी श्रमिक कार्ड के माध्यम से इसका लाभ उठा सकती है। हालांकि, उसके पास कोई श्रमिक कार्ड भी नहीं था, इसलिए वर्तमान में मैं उसे एक श्रमिक कार्ड दिलाने में मदद कर रही हूं। उसके बाद, पीएमयूवाई के लिए आवेदन करने में मैं उसकी मदद करूंगी।
दोपहर 2:00 बजे: एक बार जागरूकता सत्र समाप्त हो जाने के बाद, अधिकांश लोग दोपहर के भोजन के लिए चले जाते हैं। चूंकि मैं आमतौर पर दोपहर का खाना लेकर नहीं आती हूं इसलिए अपने इस समय का उपयोग लोगों को उनके आवेदन पत्र भरने में मदद करने के लिए करती हूं। मैं उन्हें नज़दीक की ही एजेंसी में अपना आवेदन पत्र जमा करवाने के लिए लेकर जाती हूं। आवेदन पत्र की समीक्षा के बाद एजेंसी वाले लोग आवेदक को ज़रूरी टूल ले जाने के लिए बुलाते हैं और उसके बाद उनके घर सिलेंडर पहुंचाया जाता है।
सारे आवेदकों की सूची की एक प्रति मेरे पास भी होती है जिसमें मैं ज़रूरी दस्तावेजों की अनुपलब्धता वाले विशेष मामलों के लिए एक अलग से टिप्पणी लिखती हूं। उनमें से कुछ मामलों का पता बार-बार लगाना पड़ता है ताकि उनके दस्तावेज सही समय पर तैयार हो सकें। मेरी सहेलियां – अन्य आशा कार्यकर्ताएं – भी इस समय मेरे साथ होती हैं। मेरा सारा काम ख़त्म हो जाने के बाद हम कुछ देर बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं।
दोपहर 4:30 बजे: उस दिन का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं घर के लिए निकल जाती हूं। तब तक शाम के साढ़े चार से पांच का समय हो जाता है। घर लौटने के लिए भी मुझे पहले ई-रिक्शा, बस और फिर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। मैं दवा खाने में शौचालय के इस्तेमाल से बचती हूं इसलिए घर जाते ही सबसे पहले मुझे शौचालय जाना पड़ता है। बाहर शौचालय के इस्तेमाल से बचने के लिए मैं जानबूझ कर कम पानी पीती हूं। ख़ासकर गर्मी में यह ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है और मुझे मतली आने लगती है। लेकिन समय के साथ मुझे अब इसकी आदत हो गई है।
जब तक मैं हाथ-मुंह धोती हूं तब तक मेरा बड़ा बेटा मेरे लिए चाय बना देता है। उस समय तक मेरे पति भी थोड़ी देर के लिए घर आ जाते हैं और हम सब एक साथ बैठकर अपने-अपने दिन के बारे में बातें करते हैं।
शाम 7:00 बजे: कुछ घंटों के आराम के बाद मैं उस दिन के काम की रिपोर्ट तैयार करने के लिए बैठती हूं। जब मैंने असर के साथ काम करना शुरू किया था तब मुझे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना नहीं आता था और मैं केवल लोगों के फ़ोन उठाने और उन्हें फ़ोन करना भर जानती थी। धीरे-धीरे, मैंने कंप्यूटर प्रशिक्षण की कक्षा में नामांकन करवाया और अब मैं अपना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपने फ़ोन में ही एक्सेल का इस्तेमाल कर सकूं। प्रत्येक शाम रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैं व्हाट्सएप पर ही अपनी टीम के साथ उसे साझा करती थी। चूंकि मेरी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं हिन्दी करने के लिए ट्रांसलेशन टूल का भी इस्तेमाल करती हूं। इस कौशल को हासिल करने में सक्षम होने से मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा।
दिन का काम ख़त्म होने के बाद, मैं किशोर कुमार का संगीत और कुछ भजन सुनते हुए आराम करती हूं। शाम में, मैं कुछ समय अपने कुत्ते टिमसी के साथ खेलने में भी बिताती हूं।
भले ही दिन भर का मेरा काम थकाने वाला होता है लेकिन इससे मुझे इस बात की ख़ुशी मिलती है कि मैं भलस्वा में छोटा ही सही लेकिन बदलाव लाने में अपना योगदान दे रही हूं। चूंकि, अब महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी जुटाने में घंटों नहीं लगाने पड़ते इसलिए अब उनके पास मटर बेचने जैसे कामों के लिए समय बच जाता है जिससे उन्हें थोड़ी बहुत अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। इससे उन्हें अपने एलपीजी के रिफ़िल में भी आर्थिक मदद मिल जाती है।
मैं हमेशा से ही समाज और समाज की उन महिलाओं की मदद करना चाहती थी जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को दबाना पड़ता है। भविष्य में मैं चुनाव लड़कर सांसद बनना चाहती हूं ताकि इन समुदायों के लिए बड़े स्तर पर काम कर सकूं। मैं घरेलू हिंसा झेल रही महिलाओं के लिए एक आश्रयगृह भी शुरू करना चाहती हूं।
जैसा कि आईडीआर को बताया गया।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
जीवन के अलग-अलग दौर में युवाओं की प्रेरणा भी अलग-अलग तरह की होती है। यह उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, उनके स्थान, उम्र और साथियों के हिसाब से हमेशा बदलती रहती है।
जब साल 2013 में रीप बेनिफिट की शुरूआत हुई तो हमारा अनुमान था कि युवा अपने समुदाय की समस्याओं के बारे में जानते हैं। लेकिन शायद उन्हें ये समझने में दिक्कत होती है कि अपने ज्ञान और समझ से समस्याओं का समाधान कैसे निकाले जाएं। या फिर, वे समुदाय पर कम और लंबे समय तक के लिए असर डालने वाले प्रयास लगातार कैसे करते रह सकते हैं? इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हमने 12-18 साल आयुसमूह के युवाओं के साथ मिलकर ‘सॉल्व निंजा कम्युनिटीज’ विकसित करनी शुरू कीं। इनका उद्देश्य उस इलाक़े के स्थानीय पर्यावरण और नागरिक मुद्दों के हल खोजने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना था। इन समुदायों को युवा ख़ुद संगठित करते हैं और इनके तरीक़े लचीले और परिवर्तनशील होते हैं जिससे वे अपनी समस्याओं और उनके समाधानों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी समझ सकें।
इन समुदायों को चलाते हुए, अपनी ग़लतियों से हमने सीखा कि युवाओं को उनके उद्देश्य में उत्साह के साथ लगाए रखने का मतलब उनकी बदलती ज़रूरतों के साथ तालमेल बिठाना है। समाजसेवी संस्थाएं युवाओं के साथ सार्थक रूप से जुड़ने के लिए उनकी ज़रूरतों पर कैसे गौर कर सकती हैं, यह आलेख इसी पर बात करता है।
साल 2015 में अपने पायलट प्रोजेक्ट के दौरान हम एक छोटा संगठन थे। उस समय 15 युवा हमसे जुड़े और हमने उन्हें व्यक्तिगत सहयोग दिया। इस दौरान, वे हमसे पूछते थे कि वे समुदाय की समस्याओं को कैसे पहचान सकते हैं और उनका समाधान कैसे किया जाना चाहिए।
एक इंटर्न, श्रिया शंकर, जब नौंवी कक्षा में पढ़ रही थीं तब से हमसे जुड़ी हैं। जब वे कॉलेज पहुंचीं तो उन्होंने अपने इलाक़े में जल प्रदूषण से जुड़े मसलों का हल करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया – ख़ासतौर पर जलस्रोतों में गणेश मूर्ति विसर्जन के कारण होने वाले प्रदूषण को लेकर। उन्होंने अपने समुदाय में इको-फ्रेंडली गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। बाद में, श्रिया की रुचि शिक्षा की तरफ़ हो गई, उन्होंने अनाथालयों में पिछड़े तबके के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने काम से मिली सीख से, श्रिया ने 2021 में शिक्षा से जुड़ी अपनी उद्यमिता यात्रा शुरू की। अब वे हमसे संस्था चलाने, रणनीति और फंडरेजिंग से जुड़े सवाल पूछती हैं – हम उनका संपर्क इन्क्यूबेटरों से करवाते हैं जिससे उन्हें अपनी संस्था चलाने से संबंधित जरूरी जानकारी और मार्गदर्शन मिल सके।
युवाओं को सलाह और मार्गदर्शन की ज़रूरत सिर्फ़ समुदाय चलाने से संबंधित नहीं है। वे एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां वे अपने भविष्य को लेकर अपनी भावनाओं, चिंताओं और डरों पर भी हमसे और एक-दूसरे से बातचीत कर सकें।
जैसे-जैसे समुदाय बड़ा होता जाता है, युवाओं के लिए वह जगह कम होती जाती है जिसमें वे अपने विचार साझा कर सकें।
इस तरह के छोटे समूहों को व्यक्तिगत सहायता देना आसान होता है। लेकिन जब कोई संगठन बड़ा हो जाता है तो व्यक्तिगत संबंध बनाए रख पाना मुश्किल हो सकता है। जैसे-जैसे हमारा समुदाय बड़ा होता जाता है, युवाओं के लिए वह जगह कम होती जाती है जिसमें वे अपने विचार साझा कर सकें, यह बता सकें कि वे कैसे समय से गुजर रहे हैं और सहयोग मांग सकें। ऐसे में अकेलापन लग सकता है और वे इस बात को लेकर भ्रमित हो सकते हैं कि उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर किससे बात करनी चाहिए। अपने एक जैसे अनुभवों को साझा करना, युवाओं को यह एहसास दिलाता है कि वे एक समुदाय का हिस्सा हैं।
हमने ‘अड्डा’ का विचार उनके सामने रखा जो ऐसी सभाएं हैं जहां युवा इकट्ठा हो सकते हैं। ये अड्डे उनके लिए मेंटरशिप और सीखने की जगहें हैं। ये औपचारिक और अनौपचारिक, और ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों हैं। एक उदाहरण से देखें तों हमने तीन पॉलिसी संबंधित अड्डे जालंधर, पंजाब में किए थे जहां युवाओं को अपने इलाक़े में लागू नीतियों की खूबियों-खामियों पर चर्चा करनी थी। समुदाय की एक सदस्य, सिमरन ने हमसे कहा कि वे इसमें भाग लेने से घबरा रहीं हैं कि अगर उन्हें इस मुद्दे के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं हुई तो क्या होगा? वे अपने ज्ञान को लेकर हिचक रहीं थीं और आत्मविश्वास में कमी का सामना कर रही थीं। लेकिन जब उन्होंने अपने साथियों को भाग लेते देखा और महसूस किया कि यहां पर कोई उनका आकलन नहीं कर रहा है तो उनका आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने अपना संवाद कौशल बेहतर किया और जालंधर के अपने समुदाय का नेतृत्व किया। ऐसी जगहें युवाओं को भीतरी समझ हासिल करने और ज्ञान साझा करने में मदद करती हैं।
हमने ख़ुद युवाओं से आंकड़े इकट्ठा किए हैं कि वे किस तरह के अड्डों में रुचि रखते हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य, अपनी स्थानीय संस्कृति और कई तरह की गतिविधियों से जुड़ी बातचीत करते हैं। आपस में स्थानीय स्तर पर, अपने जैसे लोगों से कहानियां साझा करने से वे एक दूसरे पर अधिक भरोसा कर पाते हैं।

हमारी अपेक्षा थी कि एक बार स्थानीय युवा समुदाय बन जाए तो युवा ख़ुद संगठित होंगे और अपने समूहों का नेतृत्व करेंगे। लेकिन वे अपने साथियों के प्रभावित करने, साथ लाने और उनका नेतृत्व करने में कठिनताओं का सामना कर रहे थे। समस्या इस बात से और जटिल बन गई कि हमें जो उनसे उम्मीदें थीं, उनके बारे में हमने उन्हें नहीं बताया था। इससे वे इस को लेकर भ्रमित हो गए कि उन्हें क्या करना चाहिए।
इससे निपटने के लिए, हमने सिस्टम को केंद्रीकृत कर दिया – यानी हमने एक ढांचा और कुछ नियम तय कर दिए जो बताते थे कि समुदाय के सदस्यों और उनके लीडर्स को क्या करना है। हमने स्पष्ट किया कि समुदाय कब मिलेंगे, वे एक-दूसरे से कितना जुड़ेंगे और समुदाय से जुड़ने वालों को कुछ व्यक्तिगत गतिविधियां करनी होंगी – और यह सबकुछ ढेर सारी जवाबदेही के साथ आया था। लेकिन इस तरीक़े की भी अपनी कमियां थीं। इससे कुछ नया होने और रचनात्मकता के लिए बहुत कम जगह बची और, समुदाय और लीडर्स हम पर अधिक निर्भर हो गए।
लेकिन यह बहुत समय तक नहीं चल सका। इससे हमने सीखा कि अगर हम चाहते हैं कि युवा अपने समुदाय का नेतृत्व करें तो बहुत अधिक नियंत्रण या बिल्कुल भी नियंत्रण न होने की स्थितियों से काम नहीं चलेगा। यहां पर एक संतुलन होना चाहिए – इसके लिए शुरूआत के कुछ तरीके और प्रक्रियाएं निर्धारित हो सकते हैं और उसके बाद, जब उन्हें ज़रूरत हो वे अपने मेंटर्स से बात कर सकते हैं। इससे लचीलेपन और बदलाव की गुंजाइश बनती है जिससे लीडर्स अपने फ़ैसले ले सकते हैं। इसीलिए समुदाय से जुड़ाव के जो हमारे दिशानिर्देश थे, हमने उन्हें ख़त्म कर दिया है। अब युवा ख़ुद चुन सकते हैं कि वे किसी समाधान पर व्यक्तिगत रूप से काम करना चाहते हैं या समुदाय के साथ। चुनने की स्वतंत्रता उन्हें रचनात्मक होने और भागीदारी करने के लिए प्रेरित करती है।
सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि जो समाधान पंजाब में कारगर हो, वह बंगलौर में उतना सटीक न बैठे। पंजाब के एक युवा, रवि को पौधे लगाने का बहुत शौक़ है क्योंकि उनके राज्य में ना के बराबर जंगल रह गए हैं। लेकिन यह मुद्दा बंगलौर के लिए उतना प्रासंगिक नहीं रह जाता है, इसलिए वहां के युवा इस तरह के किसी समाधान में उतनी रुचि नहीं लेंगे।
इसी तरह, अगर ग्रामीण पंजाब की लड़कियां मेंटरशिप के लिए आवेदन करती हैं तो उनके लिए अंग्रेज़ी बोलने वाले पुरुष मेंटर की बजाय, एक पंजाबी बोलने वाली महिला मेंटर नियुक्त की जानी चाहिए। युवाओं की उम्र, लिंग, स्थान और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर गौर करना ज़रूरी है।
इस बात की पुष्टि तब हो गई जब हमने आंकड़े इकट्ठा करने के लिए चैटबॉट्स का इस्तेमाल करना चाहा। युवाओं को चैटबॉट पर अपने कामकाज की जानकारी अपडेट करनी होती थी। हमारे साथ काम करने वाले ज्यादातर युवा टियर-2 और टियर-3 शहरों से आते थे। उन्हें चैटबॉट का इस्तेमाल करने में दिक़्क़त हो रही थी – उन्हें चैटबॉट पर प्रभाव (इम्पैक्ट) से जुड़ी, कितने लोगों से वे मिले, उसे प्रमाणित करने वाली तस्वीरें जैसी जानकारियां दर्ज करनी होती थीं। ऐसे माध्यम से नियमित रुप से रिपोर्टिंग करने की आदत डालना मुश्किल था। हमने देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिन युवाओं के साथ काम किया, इससे उनकी विविधताओं का दर्ज कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था।
अब हम अपने चैटबॉट विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में चलाते हैं जिसमें उनकी भौगोलिक स्थिति दर्ज होती है और इससे उन्हें अपने साथियों से संपर्क करने में मदद मिलती है। इस पर जानकारी लेने-देने के साथ बातचीत भी की जा सकती है। वॉइस मैसेज भेजने की सुविधा होने के चलते यह अधिक सुलभ हो गया है। हम समुदाय द्वारा किए गए कामों को नियमित रूप से साझा करते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलता और वे अपनी गतिविधियों और सफलता की कहानियां हम तक पहुंचाने में सक्रियता दिखाते हैं।
सामुदायिक भागीदारी बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन देना कोई नई बात नहीं है। लेकिन युवाओं को उनका काम बेहतर बनाने के लिए सही तरह का प्रोत्साहन दिए जाने की ज़रूरत होती है। यह मान लेना आसान लगता है कि आर्थिक प्रोत्साहन सही तरीक़ा है लेकिन यह बात हर जगह लागू नहीं होती है।
युवा आमतौर पर चार वजहों से समुदायों का हिस्सा बनते हैं – अपने इलाक़े में लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए, भविष्य में काम आने वाले कौशल सीखने के लिए, आर्थिक फ़ायदे के लिए, और समुदाय में बदलाव लाने के लिए। हमें कार्यक्रम या समुदाय में शामिल होने की उनकी वजहों को सफल करना होगा, ऐसा होना उनके लिए साथ काम करते रहने के लिए एक प्रोत्साहन बन जाता है।
उदाहरण के लिए, हमने जो अड्डे शुरू किए हैं, वे युवाओं के लिए भावनात्मक जुड़ाव बनाने और कौशल हासिल करने में मदद करने वाले मेंटर खोजने के स्थान हैं। हम आर्थिक प्रोत्साहन, प्रमाणपत्र, छात्रवृत्ति की जानकारी वग़ैरह भी देते हैं। लेकिन समस्याओं को हल करने की ख़ुशी मनाना, उसे अन्य समुदायों से साझा करना उन्हें समुदाय के लिए बेहतर करने का सबसे अधिक उत्साह देता है। इस तरह सराहा जाना ही उन्हें अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाता है। इन सभी तरीक़ों मिलाजुला रूप युवाओं को भागीदारी के लिए प्रेरित रखता है।
एक मौक़ा ऐसा भी आया, जब युवाओं की जवाबदेही के लिए हमारा उनपर दबाव बहुत अधिक हो गया क्योंकि उनका समाधानों तक पहुंचना, हमारी सफलता का मानक बन गया था। हमने कार्यक्रमों में लेवल शामिल किए जिससे युवाओं को और अधिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रत्येक लेवल पर दस समस्याएं थी और अगले लेवल पर पर जाने के लिए उन्हें कम से कम पांच का समाधान करना था। लेकिन जल्दी ही समुदायों ने पूछना शुरू कर दिया, ‘लेवल्स को पूरा करने के बाद क्या होता है?’ या ‘इससे हमें क्या फ़ायदा होता है?’
एक बार, आठवीं कक्षा के एक छात्र ने हमसे पूछा कि ‘हमसे पर्यावरण को बचाने, जानवरों की देखभाल करने, अपने बड़े-बुजुर्गों का ख़्याल रखने और जाने क्या-क्या करने की उम्मीद की जाती है। हम ये सारे कामों में अच्छा कैसे कर सकते हैं?’ हमने महसूस किया कि एक व्यवस्था के तौर पर, विकास सेक्टर में युवाओं पर जानकारियों को बोझ लाद देने का चलन है और फिर उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इन सभी बातों को अपने जीवन में शामिल करें।
आंकड़ों की बजाय सफलता की कहानियों को महत्व देना, जवाबदेही तय करने के लिहाज़ से बहुत ज़रूरी है।
अब हमने लेवल व्यवस्था ख़त्म कर दी है और इसकी बजाय युवाओं को महीने में 5-6 गतिविधियां करने को कहा है। यह काम या गतिविधि क्या होगी, यह उन पर निर्भर करता है और अगर वे इसमें भाग नहीं ले पाते हैं तो हम उन्हें अलग नहीं करते हैं।
आंकड़ों की बजाय सफलता की कहानियों को महत्व देना, जवाबदेही तय करने के लिहाज़ से बहुत ज़रूरी है। जब कोई शहर, जैसे जालंधर, अच्छा प्रदर्शन करता है – हम इसकी ख़ुशी मनाते हैं और सबको बताते हैं कि कैसे 200 लोगों के एक समुदाय ने 600 घंटों के बराबर मेहनत लेने वाले किसी मुद्दे को हल किया है। इससे दूसरे शहरों को भी प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे में जालंधर जो कर रहा है, अमृतसर भी उसे अपनाता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहयोग से वे अपने आप को इस बात के लिए जवाबदेह तय करते हैं कि अगर सामने वाले ने ऐसा किया है तो हमें भी करना चाहिए।
युवाओं के साथ काम करने वाले संगठनों के लिए, सबसे ज़रूरी यह है कि वे उनकी ज़रूरतों को पहचानते रहे और उसके मुताबिक़ व्यवहार करते रहें। युवाओं को लगना चाहिए कि वे जिस कार्यक्रम या समुदाय का हिस्सा हैं, उससे वे कुछ सीख रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने व्यक्तिगत कौशल विकसित करने के लिए, कुछ समुदाय की भावना खोजने के लिए, और कुछ अपने समुदाय की बेहतरी के लिए समुदायों का हिस्सा बनते हैं। उन पर कोई उद्देश्य थोप देना आसान होता है क्योंकि मानक, कार्यक्रम या फंडर्स यही चाहते हैं। युवाओं को जोड़े रखने के लिए, हमने पहले उनके सीखने को वरीयता देनी होगी और फिर उनके सीखने को उद्देश्य से जोड़ना होगा।
इस आलेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
राजस्थान के दक्षिणी छोर पर बसा, बांसवाड़़ा जिला, गुजरात और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। इस पहाड़ी इलाक़ों में बारिश का पानी जितनी तेजी से आता है, उतनी ही तेजी से निकल भी जाता है। बारिश भी, मुश्किल से एक से दो महीने ही होती है। इसलिए यहां के परंपरागत तालाब किसानों के लिए खेती का एकमात्र स्रोत हैं। लेकिन कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है यानी यह इलाका लगभग साल भर गर्म ही रहता है। तेज गर्मी इन स्रोतों में इकट्ठा हुए पानी को तेज़ी से सुखा देती है।
ऐसे में, खेती करना यहां के किसानों के लिए हमेशा ही संघर्ष से भरा रहा है। आजीविका के लिए लोग अक्सर पड़ोसी राज्यों में मजदूरी के काम के लिए पलायन कर जाते हैं। ये पलायन ज़्यादातर रबी और ख़रीफ़ की फसलों के बीच के समय (मार्च से लेकर जून-जुलाई के दौरान) देखा जाता है, जब यहां आमदनी का कोई जरिया नहीं होता है।
लेकिन हाल ही में तालाब किनारे बसे एक गांव खेरदा और उसके आसपास के गांवों के किसानों ने इलाके की फ़सल विविधता-चक्र को बदला है। उन्होंने जून-जुलाई के समय में बोई जाने वाली मूंग की फसल को मार्च में ही बोना शुरू किया है। मार्च से जून के बीच तालाब में पानी लगभग सूख चुका होता है। इसलिए वे इस दौरान तालाब के किनारे स्थित खेतों एवं तालाब के तल की नमी का उपयोग कर, मूंग की खेती कर रहे है।
मूंग की खेती से फ़सल में विविधता लाना यहां के लिए कारगर रहा है। मूंग कम समय (60 -70 दिन) में तैयार होने वाली फ़सल है। इससे जून-जुलाई की मुख्य फसलों को बोने में अड़चन नहीं आती है। चूंकि ये किसान बाजार में मूंग को समय से पहले उपलब्ध करवा रहे हैं, इसलिए फ़सल बेचने पर सामान्य से लगभग दोगुनी कीमत मिलती है। आर्थिक रूप से मजबूत होने से किसान सामाजिक आयोजनों जैसे विवाह में नूतरे (विवाह वाले घर में पैसे देने की प्रथा) वग़ैरह देने सरीखी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा कर पाते है। साथ ही, इससे मुख्य फसल के लिए बीज, बुवाई आदि का खर्च भी उठाने में सक्षम हो रहे हैं।
इस फसल से पशुओं को चारा भी मिल रहा है। साथ ही, इन महीनों में खेती न होने की वजह से होने वाला पलायन भी अब कम हो गया है। इसके अलावा, इस फसल से किसानों के खेत की उर्वरता बढ़ रही है क्योंकि मूंग की जड़ों में राइज़ोबियम बैक्टीरिया होता है जो भूमि में नाइट्रेट् की मात्रा बढ़ा देता है। इसकी सूखी पत्तियां भी जैविक खाद की तरह काम करती हैं।
इस तरह यह फ़सल आगे की मुख्य फसलों के लिए न केवल जमीन को उर्वर बना रही है बल्कि जल सरंक्षण और लगातार बिगड़ते पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता को बनाए रखने की दिशा में भी काफी मददगार है। मूंग की खेती से जुड़े वाग्धारा संस्था के तकनीकी ज्ञान एवं सहयोग के चलते दो सौ परिवारों के साथ शुरू कर हम लगभग 20 हजार परिवारों तक इस खेती को पहुंचा चुके हैं।
अनीता, पिछले 13 वर्षों से वाग्धारा संस्था के साथ बतौर कम्युनिटी लीडर काम कर रही हैं। वे खेरदा और उसके आसपास के गांवों में सच्ची खेती, जल सरंक्षण एवं समुदायिक अधिकारों को लेकर जागरुकता अभियान चलाती हैं।
सोहन नाथ करीब 25 सालों से सामाजिक क्षेत्र से जुड़े है। वे वाग्धारा के साथ जल सरंक्षण, सच्ची खेती जैसे नवाचारों एवं सामुदायिक कार्यक्रमों में अपनी मुख्य जमीनी भूमिका निभाते हैं।
—
अधिक जानें: इस लेख को पढ़ें और जानें कि कैसे लोगों ने संतुलित भोजन के लिए दाल और सब्ज़ियों की अदला-बदली शुरु की।
अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना सहयोग देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

बीती 29 अप्रैल को, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फुटपाथ के किनारे 50-60 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। तिरपाल चादरों और टिन की छतों वाली इन झुग्गियों में मुख्य रूप से फेरी (पारंपरिक कपड़ा रीसाइक्लिंग) का काम करने वाले लोग रहते थे। इन घरों में रहने वाली महिलाएं दिल्ली के आस-पास के इलाकों में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचती थीं और इन्हें रीसाइक्लिंग बाजारों में बेचकर अपनी आजीविका चलाती थीं।
एमसीडी ने इन झुग्गियों को ध्वस्त करने से पहले किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी थी। अपने सात महीने के बच्चे को गोद में लिए एक छब्बीस वर्षीय महिला का कहना है कि ‘लिखित की तो छोड़िये उन्होंने हमें मौखिक सूचना भी नहीं दी। अब हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे?’ सुबह दस बजे बिना किसी सूचना के बुलडोजर हमारी बस्ती में आ गया और हमारी झुग्गियों को ध्वस्त करके दोपहर बारह बजे तक लौट गया।
एक दूसरे स्थानीय निवासी ने बताया कि, ‘हमें अपना सामान हटाने या कुछ और सोचने तक का समय भी नहीं दिया गया। हमने उनसे पूछा भी कि हमें क्यों हटाया जा रहा है लेकिन उन्हें इसका जवाब देने में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं थी।’
इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का दावा है कि वे कई पीढ़ियों यहां रह रहे हैं और कुछ की झुग्गी तो साल 1982 से यहीं पर है। 62 साल की दुर्गा* कहती हैं कि ‘हमारे बच्चों और उनके बच्चों का जन्म भी यहीं हुआ है। हमारे पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल प्रमाणपत्र जैसे सभी ज़रूरी दस्तावेज हैं।’
दिल्ली की स्लम और झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और स्थानांतरण नीति, 2015 में कहा गया है कि 1 जनवरी 2015 से पहले स्थापित बस्तियों और 1 जनवरी 2006 से पहले अस्तित्व में आई झुग्गियों के निवासियों को वैकल्पिक आवास प्रदान किए बिना नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए, ये आवश्यक दस्तावेज़ उस स्थान पर उनके निवास के प्रमाण हैं, जो उन्हें पुनर्वास सेवाओं के लिए पात्र बनाते हैं। यहीं रहने वाली गौरी* ने अपनी हताशा व्यक्त करते हुए कहा, ‘उन्होंने हमारी त्रिपाल की चादरों को भी फाड़ दिया। क्या वे इन झुग्गियों को खड़ा करने के संघर्ष को समझते हैं? घर की तो छोड़िये क्या सरकार नये त्रिपाल भी देगी?’
झुग्गियों को ध्वस्त करने के बाद यहां रहने वाले लोग अपनी अपनी झुग्गियों के मलबे के नीचे रह रहे हैं। गर्मी और बेमौसम की बरसात से बचने के लिए वे त्रिपाल की चादरें तानना चाहते हैं लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन का डर सता रहा है।
*गोपनीयता के लिए नामों को बदल दिया गया है।
अनुज बहल एक अर्बन रिसर्चर और प्रैक्टिशनर हैं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
अधिक जानें: जानें कि दिल्ली की फेरीवालियों को समय कि क़िल्लत क्यों है।
अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना सहयोग देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।
जब पूरे साल आपकी ना सुनने वाला मैनेजर, बातचीत शुरू करते हुए पूछे कि आप कैसे हैं।
जब आपसे पूछा जाए कि पिछले रिव्यू के बाद, एक साल में आपने क्या-क्या किया (और आप हैं कि जिसे कल से पहले का कुछ याद नहीं है)।

जब आपके लिए ख़ास फ़ीडबैक के नाम पर वे यह बताएं कि आपकी कमियां-कमजोरियां क्या हैं।

जब वे आपसे आपके नए लक्ष्यों (स्ट्रेच गोल्स) के बारे में पूछा जाए और आपने जीवन में पहली बार यह शब्द सुना हो।

अंत में, जब वे आपको संस्था के लिए ज़रूरी और क़ीमती बताते हुए आपकी तारीफ़ करते हैं।

जब वे आपसे कहें कि वे सचमुच यह जानना चाहते हैं कि संस्था आपकी व्यक्तिगत बढ़त में कैसे मदद कर सकती है।

और फिर, आपसे कहा जाए कि वे आपके इस सुझाव से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि वेतन बढ़ाना आपका सहयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है।

और, जब आपका मैनेजर यह स्वीकार करे कि वे आपकी कदर करते हैं लेकिन असल में आपको देने के लिए संस्था के पास पैसे ही नहीं हैं।

लेकिन, वे भविष्य में आपको लीडरशिप रोल में देखते हैं… और, उसके बाद ही आपको ज़्यादा पैसे मिल सकेंगे।

विकास सेक्टर में तमाम प्रक्रियाओं और घटनाओं को बताने के लिए एक ख़ास तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। आपने ऐसे कुछ शब्दों और उनके इस्तेमाल को लेकर असमंजस का सामना भी किया होगा। इसी असमंजस को दूर करने के लिए हम एक ऑडियो सीरीज़ ‘सरल–कोश’ लेकर आए हैं जिसमें हम आपके इस्तेमाल में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर बात करने वाले हैं।
आज का शब्द है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो पीयर का मतलब है साथी और लर्निंग यानी सीखना।
विकास सेक्टर में कई सारी संस्थाएं पीयर लर्निंग कार्यक्रम चलाती हैं और हो सकता है कि आपकी संस्था भी जन-प्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों या फिर किसानों के साथ कम्यूनिटी पीयर लर्निंग कार्यक्रम चलाती हो।
इसके लिए काफी बार अपनी ही कम्यूनिटी या समुदाय से पीयर एजुकेटर या पीयर शिक्षक तैयार किए जाते हैं जो अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग या फिर कार्यक्रम चलाने का काम करते हैं। इससे एक साथ काम करने वाले एक-दूसरे से अलग-अलग गतिविधियों के ज़रिए किसी विषय, विचार या काम के तरीक़ों को समझते हैं। साथ ही इससे सीखने का भी बेहतर माहौल बनता है।
अगर आप इस सीरीज़ में किसी अन्य शब्द को और सरलता से समझना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
—