विकास सेक्टर में तमाम प्रक्रियाओं और घटनाओं को बताने के लिए एक ख़ास तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। आपने ऐसे कुछ शब्दों और उनके इस्तेमाल को लेकर असमंजस का सामना भी किया होगा। इसी असमंजस को दूर करने के लिए हम एक ऑडियो सीरीज़ ‘सरल–कोश’ लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके इस्तेमाल में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर बात करने वाले हैं।
सरल-कोश में इस बार का शब्द है – पोषण। अंग्रेज़ी में न्यूट्रीशन।
विकास सेक्टर में काम करते हुए आपने तमाम संस्थाओं को पोषण से जुड़े प्रयास करते हुए देखा होगा। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारें भी पोषण से जुड़ी तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं। कुछ सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे बताता है कि भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में 35.5% अविकसित, 19.3% कमजोर और 32.1% कम वजन के हैं। इसकी प्रमुख वजह उन्हें सही पोषण ना मिलना है। इससे साफ़ हो जाता है कि पोषण पर बात और काम किए जाने की कितनी ज़रूरत है। सरल कोश के इस अंक में जानते हैं, पोषण क्या है?
विकास सेक्टर में पोषण से जुड़े प्रयासों पर ज़ोर देना न केवल स्वास्थ्य के लिहाज़ से ज़रूरी है बल्कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरणों से समझें तो कुपोषण बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास पर असर डालता है या उनके लिए नियमित रूप से स्कूल जाना मुश्किल बनाता है। इसी तरह से, यह लोगों की कार्यक्षमता को को सीमित कर उनके लिए रोज़गार के मौक़े कम कर सकता है। इसके अलावा, कुछ सामाजिक तबकों में कुपोषित लोगों के साथ भेदभाव भी देखने को मिलता है।
अगर आप इस सीरीज़ में किसी अन्य शब्द को और सरलता से समझना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
—
हम सभी मानते हैं कि दुनिया की समस्याओं की जटिलता और उनका पैमाना इतना बड़ा है कि कोई एक व्यक्ति या संगठन सब कुछ हल नहीं कर सकता है। इसलिए, मिलकर काम करने की जरूरत और महत्व स्पष्ट है। फिर भी, हम असल हालातों में सहयोग होते हुए नहीं देख पाते हैं। इसलिए सवाल यह उठता है कि जब सहयोग के फायदे सभी को समझ में आते हैं तो फिर लोग सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं?
सभी व्यवस्थाओं में, हर लेन-देन के दो पक्ष होते हैं। जैसे प्रकृति में सबसे बुनियादी लेन-देन होता है – खाना या खाया जाना। उस व्यवस्था की सफलता के लिए, शिकार या शिकारी को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि वे किसी बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, उन्हें बस अपनी भूमिका निभानी होती है और वही करना होता है जो वे जानते हैं।
लेकिन केवल वही काम करते रहना जो आप जानते हैं, और अपने ‘स्वार्थी’ दृष्टिकोण से काम करना सामाजिक क्षेत्र में एक सफल इकोसिस्टम नहीं बनाता है। अगर मैं अपने काम में लगा रहूं और कोई दूसरा अपने काम में लगा रहे तो यह एक आदर्श समाधान नहीं है, क्योंकि हमारे सामने यहां एक बड़ा सामाजिक लक्ष्य है।
‘निजी हितों’ की बात तब समझ में आती है जब हम मुक्त बाजारों (फ्री मार्केट्स) के बारे में बात करते हैं और जब वे विफल होते हैं। लेकिन अधिकांश सामाजिक क्षेत्र के सिस्टम ‘मुक्त बाजार’ नहीं होते हैं, और इसलिए ‘अदृश्य हाथ’ इन हितों को बड़े सामूहिक हित के साथ नहीं साध सकता है। कहने का मतलब यह है कि ‘स्वार्थ’ की बात आमतौर पर बाजारों में होती है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में जहां बाजार की तरह खुद-ब-खुद चीजें ठीक नहीं होतीं, वहां स्वार्थ और सामूहिक हित एक साथ नहीं चल सकते।
समाजिक क्षेत्र में सफल होने के लिए, सभी को यह समझना होगा कि वे एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। हमें केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पर ध्यान नहीं देना चाहिए; हमें यह समझना होगा कि दुनिया में बहुत सी ऐसी भी जरूरी चीजें हैं जिन्हें पैसों या आर्थिक पैमानों पर नहीं मापा जा सकता है। एक सही इकोसिस्टम को बनाने के लिए, सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा और यह ध्यान रखना होगा कि हम एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हैं। अकेले हम अपने काम को सबसे अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं।
जब हम यह समझ लेते हैं कि हम एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं तो अगली चुनौती प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच संतुलन बनाने की होती है। जैसे, कब हमें अपने व्यक्तिगत हितों पर ध्यान देना चाहिए और कब पूरे समूह और व्यवस्था के हित में सोचना चाहिए।
सामाजिक क्षेत्र में नए लोग और विचार आ रहे हैं, लेकिन कई बार ये लोग बाजारों की जटिलता और आपसी निर्भरता को ठीक से समझे बिना पहले की तरह प्रतिस्पर्धात्मक नजरिया अपनाते हैं। दुर्भाग्य से, ऐसा नजरिया तब काम नहीं करता जब व्यवस्था जटिल और एक दूसरे पर निर्भर होती है, और सामाजिक क्षेत्र की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें पैसे से नहीं मापी जा सकती हैं।

सामाजिक क्षेत्र में, केवल अलग-अलग संगठनों के बीच ही नहीं, बल्कि एक ही समूह के भीतर भी प्रतिस्पर्धा होती है। उदाहरण के लिए, समाजसेवी संगठनों के बीच संसाधनों (जैसे धन, समय, समर्थन) के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। इसी तरह, फंड देने वाले और फंड प्राप्त करने वाले के बीच भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
जब फंडर और ग्रांटी (फंड देने वाले और फंड प्राप्त करने वाले) के बीच बातचीत होती है तो यह मान लिया जाता है कि फंडर लागत को घटाने की कोशिश करेगा और ग्रांटी इसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस प्रक्रिया में, वे दोनों मिलकर एक समुचित लागत पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, सही लागत तक पहुंचने का यह तरीका बाजार की तरह है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या मोलभाव और बातचीत वाकई में परियोजना की लागत को सही ढंग से तय करने का सबसे अच्छा तरीका है? और शक्ति के असंतुलन (जैसे, फंडर के पास ज्यादा ताकत हो सकती है) के चलते, इस प्रकार की बातचीत से आदर्श समाधान तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।
फंडर और ग्रांटी के रिश्ते में सफलता के लिए सहयोग और सह-निर्माण की सोच अपनाना जरूरी है। लेकिन जब बातचीत चल रही होती है, तब इसे वास्तविकता में लागू करना कठिन हो सकता है क्योंकि विभिन्न कारकों को हमेशा ध्यान में रखना आसान नहीं होता है।
इसलिए, प्रभावी सहयोग के लिए एक बहुत ही सजग और सतर्क मानसिकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम सहयोगी नहीं होते और एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहन कभी भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं होता है।
आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से आप पूरे इकोसिस्टम को एक साथ देख सकें। आप केवल इसके एक हिस्से को ही देख सकते हैं। नतीजतन, आप किसी समस्या को लेकर केवल अपने नजरिए से देख पाते हैं, जो आपके स्थान पर निर्भर करती है। इसलिए, यह पूरा परिदृश्य नहीं कहलाएगा।
यह समझना जरूरी है, कि इकोसिस्टम को पूरी तरह से समझने के लिए आपको दूसरों के नजरिए की जरूरत होती है। जब कई लोग मिलकर अलग-अलग नजरिया बांटते हैं, तब आप पूरे सिस्टम की एक साफ और पूरी छवि पा सकते हैं।
आज के समय में, हमारे क्षेत्र में अधिकांश बातचीत ‘सहयोग कैसे करें’ के मोड में चली गई है, जो एक ऐसा व्यावहारिक तरीका है जिससे हम सभी सहमत हैं। हालांकि, अगर हम सोच-समझ कर देखें तो मुझे लगता है कि सहयोग की राह में सबसे बड़ी और पहली रूकावट एक खास तरह की मानसिकता है! इसे (स्वयं से शुरू करके) सभी प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से और जागरूकता के साथ विकसित करना चाहिए।
सहयोग में मदद करने वाले संसाधन हो सकते हैं। जैसे कि कई स्टेकहोल्डर्स (हिस्सेदारों) के साथ संवाद, लगातार चर्चाएं, परियोजनाओं पर एक साथ काम करना, एक साझा परिवर्तन सिद्धांत विकसित करने के साथ और भी बहुत कुछ। इनका प्रभाव केवल तभी होगा जब हम इस मानसिकता को स्थिति में लाएंगे।
आखिर में, सहयोग न तो ‘स्वाभाविक’ है और न ही ‘अनिवार्य’। यह केवल ‘जानने की बात’ या एक तकनीक और टूलकिट नहीं है। यह एक जागरूक मानसिकता है जो सही ढंग से अपनाई जाए, तभी यह वास्तविक परिणाम दे सकती है।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
मानव जीवन, ऑक्सीजन के लिए पेड़ों पर आश्रित है, इसे लेकर तो बहुत बात होती है लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। हम पेड़-पौधों के अलावा फाइटोप्लैंक्टन नामक सूक्ष्म पौधे जीवों पर भी आश्रित होते हैं जो पृथ्वी पर मौजूदा पचास प्रतिशत ऑक्सीजन उत्पादन और विभिन्न खाद्य, पर्यावरणीय संतुलन का काम करते हैं।
फाइटोप्लैंक्टन ग्रीक भाषा के दो शब्दों, फाइटो (पौधा) और प्लैंकटन (भटकने वाला/ड्रिफ्टर) से आया है। यह एककोशकीय, स्वपोषी, पौधे सरीखे जलीय जीव, महासागर से लेकर मीठे और खारे पानी के विभिन्न जल स्रोतों में रहते हैं। हालांकि ज़्यादातर फाइटोप्लैंक्टन को नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है लेकिन कुछ को देखा जा सकता है, जैसे ट्राइकोडेस्मियम, फिलामेंटस फाइटोप्लैंक्टन। ये प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिंथेसिस) कर जीवित रहते हैं। यही वजह है कि ये महासागरीय जल निकायों की यूफोटिक ज़ोन नाम की 200 मीटर तक की ऊपरी परत तक ही सीमित रहते हैं। यह वह गहराई है जहां तक सूर्य का प्रकाश जलीय वातावरण में प्रवेश करता है और इन सूक्ष्म जीवों तक पहुंचता है। ये जीव जलीय पारिस्थितिकी तंत्र (वाटर इकोसिस्टम) के खाद्य जाल (फूड वेब) के मुख्य उत्पादक होते हैं। दूसरे शब्दों में, जलीय जीवों के खाने का इंतजाम यही सूक्ष्म जीव करते हैं। ये जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें कोशिका संरचना से लेकर आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सामान्य फाइटोप्लैंकटन्स में सायनोबैक्टीरिया, डायटम्स, हरी शालजीव और कोकोलिथोफोर्स शामिल हैं।
कनाडा की डलहौजी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार वर्ष 1950 के बाद से फाइटोप्लैंकटन की वैश्विक आबादी में लगभग 40% तक की गिरावट आई है। हाल ही में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. रॉक्सी मैथ्यू कोल के नेतृत्व में एक अध्ययन किया गया, जो जर्नल ‘जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स’ में प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार भारतीय महासागर में पिछले 6 दशकों में फाइटोप्लैंकटन की संख्या में 20% तक की कमी आई है। अध्ययन से पता चलता है कि पश्चिमी भारतीय महासागर में यह गिरावट पिछले 16 वर्षों में 30% तक हो गई है। इन अध्ययनों को गंभीर रूप से स्वीकारना और इन पर काम करना ज़रूरी है। इनके मुताबिक जलवायु परिवर्तन सिर्फ पानी की कमी, जहरीली हवा तक सीमित नहीं है बल्कि यह सूक्ष्म जीवों को भी प्रभावित कर रहा है। इससे ना केवल मानव जीवन बल्कि जलीय और जमीनी पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन भी बिगड़ रहा है।
फाइटोप्लैंक्टन, जलीय खाद्य जाल में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद बनाते हैं और जनसंख्या में बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इन्हें अन्य सूक्ष्मजीव जैसे जुप्लेंकटन खाते हैं, जिन्हें छोटी मछलियां, अन्य जलीय जीव खाते हैं, और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां जैसे व्हेल खाती हैं। इस तरह यह सूक्ष्म जीव पूरे जलीय तंत्र के भोजन की नींव हैं। तरह-तरह के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस इन्हीं के जरिए जलीय जीवों तक पहुंचते हैं। इनकी संख्या में गिरावट, अन्य जीवों के लिए भोजन की कमी पैदा कर सकती है जिससे उनकी प्रजनन दर में भी भारी गिरावट आएगी और खाद्य जाल और जीवों की बढ़ोतरी प्रभावित होगी।
फाइटोप्लैंक्टन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं जिससे पर्यावरण में इसकी मात्रा संतुलित बनी रहती है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे की जलवायु वैज्ञानिक अदिति मोदी बताती हैं, “फाइटोप्लैंक्टन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इनकी कमी से कार्बन अवशोषण कम हो जाएगा जिससे कार्बन का स्तर बढ़ सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल सकता है और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र और मौसम पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं।”
फाइटोप्लैंक्टन का अहम कार्य जलवायु विनिमयन (क्लाइमेट चेंज) भी है जो एक तय जलवायु चक्र बनाए रखने में और चलाने में मदद करते हैं। इनकी कमी वैश्विक तापमान और चरम मौसमी गतिविधियों को बढ़ा सकती है। यानी, इससे बढ़ता तापमान, लू, आंधी-तूफान, बढ़ते समुद्री जल स्तर जैसी कई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं जो आगे चलकर खेती और उससे जुड़े उद्यमों को प्रभावित कर सकती हैं।

फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ने अथवा फैलने के लिए ठंडे पानी की जरूरत होती है क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। फाइटोप्लैंक्टन, प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जल स्रोत में मिश्रित पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फेट, नाइट्रेट आदि का इस्तेमाल कर अपना भोजन बनाते हैं और बढ़ते हैं। सामान्य रूप से समुद्र की सतह का तापमान गहरे पानी की तुलना में अधिक गर्म होता है, बढ़ती गहराई के साथ पानी ठंडा होता जाता है। मौसम में परिवर्तन के कारण सतह का पानी अधिक गर्म हो रहा है और यह अधिक गर्म सतह एक अवरोध बनाती है। एक ढक्कन की तरह जो ठंडे, पोषक तत्वों से भरपूर पानी को गर्म सतह के पानी के साथ मिलने से रोकता है। इससे, फाइटोप्लैंक्टन को जीवित रहने और बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और उनकी संख्या में गिरावट आती है।
समुद्र के बढ़ते तापमान के अलावा महासागर अम्लीकरण (ओशन एसिडिफिकेशन), और ग्लोबल वार्मिंग ने कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में बढ़ाया है। अब समुद्र इस गैस को अधिक मात्रा में सोखते हैं और परिणामस्वरूप पानी अधिक अम्लीय (एसिडिक) हो गया है जिससे फाइटोप्लैंक्टन तक आयरन जैसे पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं। इससे उनकी कोशिका भित्ति (सेल वॉल्स) कमजोर हो जाती हैं और उनकी बढ़ोतरी और कार्य क्षमता में बाधा आती है। इसके अलावा प्रदूषण, समुद्री लहरों में बदलाव, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन (हार्मफुल एलगल ब्लूम्स), बहुत अधिक मछली पकड़ा जाना जैसे कारक भी फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में गिरावट लाते हैं। गहराई से समझें तो प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक, उर्वरक और कीटनाशक जैसे रसायन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे फाइटोप्लैंक्टन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये प्रदूषक, पोषक चक्रों को बाधित कर सकते हैं, पानी में प्रकाश के प्रवेश को कम कर सकते हैं, और विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ा सकते हैं।
शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने से रोकते हैं और जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन को मार सकते हैं।
मानवीय गतिविधियों के कारण समुद्री लहरों के पैटर्न में बदलाव, जल परिसंचरण (वाटर सर्कुलेशन) को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पोषक तत्वों का वितरण प्रभावित होता है और फाइटोप्लैंक्टन उन तक नहीं पहुंच पाते। साथ ही, शैवाल प्रस्फुटन यानि दूषित पोषक तत्वों के कारण कुछ शैवाल प्रजातियों का बढ़ जाना भी इसकी एक वजह है। शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने से रोकते हैं और जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को मार सकते हैं। ज्यादा मछली पकड़ने से भी समुद्री खाद्य जाल बाधित होता है क्योंकि ज़ूप्लैंकटन का शिकार करने वाली मछलियां कम हो जाती हैं। फाइटोप्लैंक्टन ज़ूप्लैंकटन का चारा हैं, पर्याप्त शिकारियों के बिना ज़ूप्लैंकटन की बढ़ती आबादी से फाइटोप्लैंक्टन की ज्यादा चराई होगी, जिससे उनकी संख्या में कमी आ सकती है।
अदिति मोदी बताती हैं कि “उत्पादकता से भरपूर उष्णकटिबंधीय भारतीय महासागर में, फाइटोप्लैंक्टन की कमी खाद्य आपूर्ति और उन समुदायों की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है जो इस पर निर्भर हैं। भारतीय महासागर एक अत्यंत उत्पादक बेसिन है, जो इसके किनारे बसे देशों के लिए भोजन और आजीविका का बेहतरीन स्रोत है।” फाइटोप्लैंक्टन की कमी से मछलियां कम हो सकती हैं जिससे इस पर आश्रित लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट (जैसे प्रोटीन की कमी) और मछली निर्यात में कमी आ सकती है।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि टूना मछली की उपलब्धता वाले वैश्विक पकड़ क्षेत्र का 20% हिस्सा हिंद महासागर में आता है। यह भारत को विश्व बाजारों में टूना का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले पांच दशकों में हिंद महासागर में टूना उत्पादन की दर में 50-90% की गिरावट आई है। हालांकि इस गिरावट का एक हिस्सा औद्योगिक मछली पकड़ने की गतिविधियों में वृद्धि के कारण है लेकिन यह फाइटोप्लैंकटन की कमी से भी संबंधित है। क्योंकि टूना और अन्य मछलियों का बड़े पैमाने पर वितरण, फाइटोप्लैंक्टन की उपलब्धता और प्रचुरता से जुड़ा है, इसलिए इनकी कमी स्थिति को और गंभीर बना सकती है और अफ्रीका, दक्षिण एशिया में मछली की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जिन समुदायों और देशों के भोजन में मछली अति आवश्यक खाद्य है, इस कमी से उनके भोजन पैटर्न और स्वास्थ्य में बदलाव संभव हैं।
केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की मरीन फिश लैंडिंग्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत के पश्चिमी तट से मछली पकड़ने में कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में महाराष्ट्र ने 45 वर्षों में सबसे कम वार्षिक पकड़ दर्ज की है जिसमें सभी प्रजातियों में तीव्र कमी देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में राज्य में कुल अनुमानित मछली की लैंडिंग (जो मछली पकड़कर बंदरगाहों पर पहुंचती है) 2.01 लाख टन थी जबकि 2018 में यह 2.95 लाख टन थी यानी 32% कमी। इस कमी के लिए पूरी तरह फाइटोप्लैंक्टन ज़िम्मेदार नहीं हैं लेकिन यह अन्य कारण जैसे प्रदूषण, प्लास्टिक वेस्ट, बढ़ता तापमान, मौसमी गतिविधियां आदि में से एक जरूर है। भारत के मछली निर्यात में कमी आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है और मछली व्यापार में कमी होने से मछली पकड़कर या बेचकर जीवन यापन करते समुदायों के लिए भी आर्थिक रूप से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं।
अदिति मोदी बचाव के कदमों को लेकर कहती हैं, “फाइटोप्लैंक्टन में तीव्र और व्यापक वृद्धि मुख्य रूप से पोषक तत्वों और प्रकाश की उपलब्धता से प्रभावित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे भारतीय महासागर में, महासागर के यूफोटिक ज़ोन में पोषक तत्वों की आपूर्ति फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि को सीमित करती है। मानसून प्रणालियां पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ाकर फाइटोप्लैंक्टन के खिलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा महासागर की सतह के तापमान में कमी, पानी की परतों के बीच ऊर्ध्वाधर मिश्रण (वर्टिकल मिक्सिंग) को बढ़ा सकती है, जिससे पोषक तत्वों की आपूर्ति और बढ़ती है, यह घटना अक्सर अरब सागर में सर्दियों के दौरान देखी जाती है। विभिन्न महासागर प्रक्रियाएं, जैसे अपवेलिंग और ऊर्ध्वाधर मिश्रण, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाकर फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि में योगदान करती हैं।”
इन जीवों की जनसंख्या को वापस पुराने स्तर पर ले जा सकने की उम्मीद में हुए शोधों पर अदिति का कहना है, “हाल के शोधों से पता चलता है कि फाइटोप्लैंक्टन की कमी विश्व के महासागरों में भिन्न-भिन्न है। वैश्विक गर्मी, ध्रुवीय इलाकों पर फाइटोप्लैंक्टन के खिलने को बढ़ावा दे सकती है लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कमी का कारण बन सकती है। यदि आप भारतीय महासागर को देखें, तो यह 20वीं सदी से उष्णकटिबंधीय महासागरों में सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। बढ़ती सतह की गर्मी ऊपरी महासागर के ऊर्ध्वाधर मिश्रण को सीमित करती है। इससे गहरे महासागर से पोषक तत्वों की आपूर्ति बाधित होती है और समुद्री फाइटोप्लैंक्टन की प्रकाश संश्लेषण गतिविधि घट जाती है। भारतीय महासागर के रुझानों से जुड़ा व्यक्तिगत अध्ययन दिखाता है कि ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि के साथ वैश्विक गर्मी भारतीय महासागर को एक पारिस्थितिकीय मरूस्थल में बदल सकती है। इससे अलग भी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए विभिन्न पहलों की आवश्यकता है। कृषि में इस्तेमाल होने वाली रासायनिक खाद-कीटनाशकों और उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक कचरे में नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि जैसे पोषक तत्व होते हैं, समुद्र में इनके बहाव को कम करने के प्रयास भी हानिकारक शैवाल को बढ़ने से रोकते हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन निवारण प्रयास, जैसे कार्बन संचित करने की परियोजनाएं और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, महासागर की गर्मी और अम्लीकरण को कम करना भी एक उपाय है।”
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन जीवों को बचाने, बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, एक महत्वपूर्ण पहल संयुक्त राष्ट्र का महासागर विज्ञान दशक है, जो महासागर संरक्षण और जैव विविधता, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन भी शामिल हैं, पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसे ही कई क्षेत्रीय और वैश्विक प्रयास इस दायरे में आते हैं।
आशिका शिवांगी सिंह एक स्वतंत्र लेखिका हैं। आशिका, मानवाधिकार, जाति, वर्ग, लिंग, संस्कृति आदि विषयों पर लिखती रहती हैं।
—
वैश्विक क्रेडिट रेटिंग और शोध फर्म, मूडीज ने जून 2024 में, चेतावनी दी थी कि भारत में पानी की बढ़ती कमी उसके आर्थिक विकास के लिए खतरा बन सकती है। हमारे यहां जल संकट से जुड़े कई जोखिम हैं, जो खेती और उद्योग को प्रभावित कर सकते हैं, और इसके सामाजिक परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। भारत दुनिया का 25 प्रतिशत से अधिक भूजल निकालता है, जो खेती और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कुछ सालों में, इस पानी के बहुत ज्यादा दोहन के कारण लगभग 60 प्रतिशत भारतीय जिलों को पानी की कमी और पानी की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
जलवायु परिवर्तन का पानी पर बड़ा असर पड़ता है और जलवायु परिवर्तन आमतौर पर पानी की कमी या अधिकता की वजह से ही दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने भाषण में ‘हर जगह एक साथ’ जलवायु कार्रवाई किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। भारत की जल सुरक्षा में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर भागीदारी की जरुरत होगी।
सहयोग, औपचारिक या अनौपचारिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी या गैर-बाध्यकारी आदि, अलग-—अलग हितधारकों और कार्यकर्ताओं को एक साथ लाता है। उदाहरण के लिए, सतत विकास लक्ष्य, (SDGs) 2030 पर वैश्विक संकल्प एक गैर बाध्यकारी कानूनी समझौता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन और लोकप्रियता मिली है। वहीं स्थानीय स्तर पर, स्थानीय समूहों की ओर से आपदा प्रबंधन के लिए राहत कार्य की दिशा में प्रयास एक अस्थायी अनौपचारिक सहयोग का एक उदाहरण है।
एचयूएफ (हिंदुस्तान यूनिलीवर फ़ाउंडेशन ) इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग ही एकमात्र स्पष्ट और तत्काल की जरूरत है।
पानी की सुरक्षा पर समग्र और संदर्भ आधारित सहयोगात्मक कार्यवाही के लिए उद्देश्य और सिद्धांत का साफ होना जरूरी है। हम ऐसे कार्यक्रमों को मिलकर बनाते हैं, जिनके लिए अनेक हितधारकों को एक लंबे समय तक मिलकर काम करना हो। सभी कार्यक्रमों में हितधारक की प्रेरणा और ताकत पर आधारित एक साफ लक्ष्य होना चाहिए। जब लक्ष्य पारदर्शी और मापने लायक होते हैं, तो उनके चारों ओर कार्यान्वयन करने वाले डिज़ाइन तैयार हो सकते हैं और मुश्किल बदलाव आसान हो जाते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि सामुहिक ताकत व्यक्तिगत ताकतों से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। यह बात कई बार हमारी प्रोत्साहित की गई साझेदारियों के जरिए साबित भी हो चुकी है। आइए जानते हैं यह कैसे हुआ:-

हमारी सहयोगी संस्था स्वयं शिक्षण प्रयोग (एसएसपी), महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में किसानों के बीच जल वायु परिवर्तन को सहन करने वाले एक एकड़ मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक ‘सखी कैडर’ चला रहे हैं। यह महिला ग्राम प्रतिनिधियों का एक नेटवर्क है। इन सखियों का मुख्य काम है किसानों को जलवायु-संवेदनशील खेती के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्थायी खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना। ज़मीनी प्रतिनिधि होने के नाते, इन सखियों के पास किसानों के साथ एक मजबूत नेटवर्क तो होता ही है, साथ में उनका भरोसा भी होता है। इस वजह से वे स्थानीय पानी के बुनियादी ढांचे से जुड़ी मांगों को जमा करती हैं और फिर स्थानीय पंचायतों के साथ इस बारे में संवाद शुरू करती हैं। इसके अलावा, वे बीजों और इनपुट के लिए बैकवर्ड लिंकेज और बाजारों के लिए फॉरवर्ड लिंकेज को बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि सखियों ने अपने गांवों को बदलने का बीड़ा उठाया है। अपनी अभी तक की समझ के आधार पर वे काफी संख्या में हितधारकों के साथ बातचीत का क्रम बनाएं रखती हैं। उनके सहयोग और जुड़ाव ने सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में एक लाख परिवारों के जीवन को बदल दिया है।
यह बदलाव सिर्फ़ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एसएसपी ने सखियों को स्थानीय सहयोगी के तौर पर तैयार किया। वे क्षेत्र की महिला किसानों की आवाज़ बनी। साथ ही, सीमित संसाधन होने के बावजूद पंचायतों, बाज़ारों, जानकारों और सरकारी संस्थानों से ना केवल जुड़ने की कोशिश की बल्कि उन्हें प्रभावित भी किया।
अलग-अलग योग्यता वाले कई हितधारकों का सहयोग कार्यक्रमों को लंबे समय तक प्रभावी बनाएं रखने के लिए जरूरी है। जैसे एचयूएफ ने एक तरह का सहयोगात्मक संघ बनाया है। इसमें भागीदार के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना ट्रस्ट केंद्र (सीआईपीटी) पंजाब, किसान सहकारी समितियां, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के अकादमिक विशेषज्ञ और सरकार सभी शामिल हैं। इस संघ का उद्देश्य पंजाब के लिए ऐसे जल-संवेदनशील कृषि मॉडल को बढ़ावा देना है जो वहां की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल हों।
हर सहयोगी की एक अहम भूमिका होती है। हर सहकारी समिति अपने किसान समूहों का मार्गदर्शन करती है और ऋण सहायता मुहैया करवाती है। विशेषज्ञ किसानों को नए उपकरणों और खेती के तरीके बताकर मदद करते हैं। जैसे कि मिट्टी की नमी सेंसर का इस्तेमाल, वैकल्पिक पानी देना और सुखाना (एडब्लूडी), और चावल की सीधी बुआई (डीएसआर)। ये तरीके खासकर तब महत्वपूर्ण होते हैं जब ज़मीन का पानी खेती में ज्यादा उपयोग होने के कारण घट रहा होता है। जैसे ही ये जल-संवेदनशील कृषि मॉडल विकसित होते हैं, स्थानीय सरकार उनका समर्थन करती है ताकि इन प्रथाओं को ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएं। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण से पंजाब के 12 जिलों में जल-संवेदनशील खेती के मॉडल को बढ़ावा मिल रहा है।
मुख्य हितधारकों के बीच सहयोग से स्थानीय पानी की समस्याओं को महत्वपूर्ण बना गया है। जो एक बड़ा सामूहिक प्रभाव पैदा कर रहा है।
पानी एक ऐसा विषय है जिसे अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच बांटा गया है, और हर विभाग की अपनी जिम्मेदारियां और बजट आवंटन होते हैं। चुनौती की गंभीरता को देखते हुए, व्यवस्थागत बदलाव की जरुरत है। समय की मांग है कि इन सभी विभागों को बड़े पैमाने पर योजना और क्रियान्वयन के लिए एक साथ लाया जाए।
एचयूएफ के साथी संगठन प्रदान ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रम उषर्मुक्ति के तहत इस क्षेत्र की सात लुप्त होती नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 54 ब्लॉकों में 1,900 से ज्यादा जलग्रहण क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें 7,000 से ज्यादा गांव, 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और पांच लाख परिवार शामिल हैं।
भले ही बड़े सरकारी कार्यक्रम विभिन्न विभागों में बंटे हों, लेकिन एक स्पष्ट और साझा दृष्टिकोण के साथ वे भी परिवर्तनकारी प्रभाव दे सकते हैं।
इस कार्यक्रम को सात स्थानीय गैर-लाभकारी संगठनों और राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की मदद से लागू किया गया। प्रदान ने एक औपचारिक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की जिससे समुदाय, गैर-लाभकारी साझेदार, पंचायतों, और राज्य विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
योजना और कार्यान्वयन में कोई बाधा न आए इसलिए पीएमयू ने प्रमुख सरकारी प्रतिनिधियों से स्वीकृतियां, फंड की रिलीज, संकलन, और सरकारी आदेशों की प्रक्रिया को तय करने के लिए संपर्क किया। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसे राज्य के दूसरे ब्लॉक में भी दोहराया जाए ताकि योजना, कार्यान्वयन, और सरकारी सहभागिता को बढ़ाया जा सके।
भले ही बड़े सरकारी कार्यक्रम विभिन्न विभागों में बंटे हों, लेकिन एक स्पष्ट और साझा दृष्टिकोण के साथ वे भी परिवर्तनकारी प्रभाव दे सकते हैं। उषर्मुक्ति की सफलता सहयोग की शक्ति का एक प्रमाण है।
हितधारकों के बीच सहयोग को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पारस्परिक संबंधों या यूं कहें कि समूह संबंधों पर शोध करने वाले ब्रूस टक्मन ने यह दिखाया कि समूह गठन, तूफान, मानदंड और प्रदर्शन के अहम चरणों से गुजरते हैं। कोई भी सहयोगात्मक पहल संघर्ष और समस्याओं से गुजरने के बाद ही एक सामान्य स्थिति में आकर प्रभावी योगदान देती है।
जैसे-जैसे पारस्परिक संबंध बढ़ते हैं , सक्षम नेता सामने आते हैं जो सहयोग को सफल बनाने में मदद करते हैं। आपस में सफल सहयोग स्थापित करना जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। हर हितधारकों की अलग-अलग इच्छाएं हो सकती हैं जो कभी-कभी टकराती है। एक सहयोगात्मक प्रयास को स्थिर होने में कई महीने या यहां तक कि सालों का समय लग सकते हैं। मजबूत सहयोग उन संगठनों की पहचान होती है जो धैर्यपूर्वक और मिलकर काम करते हैं, ताकि वे एक साझा लक्ष्य को पा सकें।
सहयोग की पहेली को पूरा करने में विज्ञान और कला दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे सहयोग की प्रक्रिया मुश्किल होती है क्योंकि इसमें मानव व्यवहार और कई रुचियां शामिल होती हैं। सहयोगात्मक संघ अपने आप नहीं बनता, बल्कि इसे सावधानीपूर्वक योजना, डिज़ाइन, और देखरेख की जरुरत होती है। सहयोग को सफल बनाने के लिए विशेष कौशल और विशेषज्ञता चाहिए। सहयोग की कला और विज्ञान को कार्यक्रम प्रणाली की मुख्यधारा में लाना अहम है ताकि फंडर्स अपने कार्यक्रमों को एक बड़े साझा उद्देश्य की ओर ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाएं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—



हल्का-फुल्का का यह अंक हमारे साथियों, रजिका सेठ और इंद्रेश शर्मा के अनुभव पर आधारित है।
गौतम भान, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट (आईआईएचएस), बेंगलूरू से जुड़े हैं। वर्तमान में वे एसोसिएट डीन एवं एकेडमिक्स एंड रिसर्च सीनियर लीड के बतौर कार्यरत हैं। वे एलजीबीटीक्यू समुदायों के अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाते रहते हैं। गौतम के प्रमुख शोध कार्यों में दिल्ली में शहरी गरीबी, असमानता, सामाजिक सुरक्षा और आवास पर केंद्रित काम बहुत ही सराहनीय रहा है। फिलहाल, उन्होंने किफायती और पर्याप्त आवास तक लोगों की पहुंच के सवालों पर अपना शोध जारी रखा हुआ है।
गौतम की चर्चित प्रकाशित किताबों में प्रमुख हैं – ‘इन द पब्लिक इंटरेस्ट: एविक्शन्स, सिटिज़नशिप एंड इनइक्वलिटी इन कंटेम्पररी दिल्ली’ (ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2017) और बतौर सह-संपादक ‘क्योंकि मेरे पास एक आवाज़ है: भारत में क्वीयर पॉलिटिक्स’ (योडा प्रेस, 2006) शामिल हैं।
द थर्ड आई के शहर संस्करण में गौतम भान के साथ हमने सरकारी नीतियों के बरअक्स वास्तविकता के बीच शहरों के बनने की प्रक्रिया, शहरी गरीबों की पहचान के सवाल, शहरी अध्ययन एवं कोविड महामारी की सीखें और भारत में शहरी अध्ययन शिक्षा के स्वरूप पर विस्तार से बातचीत की है। पेश है इस बातचीत का अंश:
इस सवाल का जवाब अगर रूपक में दूं तो भारतीय शहरीकरण को इस एक दृश्य से समझा जा सकता है – एक घर जिसके चारों कोनों के ऊपर सरिया की छड़ें एक ठोस स्तंभ से चिपकी हुई दिखाई देती हैं, और जिसकी बिना पलस्तर की गई लाल ईंट की दीवार भविष्य की ओर देख रही होती है। लगभग आधी दिल्ली ऐसी ही है। क्योंकि घर अभी बना नहीं है, बनता जा रहा है। ज़्यादातर लोग घर में रहते हुए इसे बनाते हैं। और यही हमारा शहरीकरण भी है। आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते जाना। इसलिए हमारे शहरीकरण के उपाय एवं प्रयासों को भी इसी धीमी चाल की वृद्धि से परिवर्तन लाना होगा।
वैसे, हमारे यहां पर शहर की एक विचित्र तकनीकी परिभाषा है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां रोज़गार से शहर को परिभाषित किया जाता है – 400 वर्ग किलोमीटर के घनत्व में रहने वाली 5000 जनसंख्या जिनमें से 75% पुरुष गैर-कृषि रोज़गार में हों – इस औपचारिक भाषा में भारत में शहर को परिभाषित किया जाता है।
अब, मैं आपको बताता हूं,
यदि आप इस रोज़गार श्रेणी को हटा दें, तो भारत पहले से ही 60% शहरी क्षेत्र है। ये जो हम कहते रहते हैं ना, “भारत गांव प्रधान देश है। हम केवल 35% शहरी हैं।” नहीं, अब ऐसा नहीं है। और ये कैसी ऊटपटांग सी परिभाषा है जो पुरुषों के रोज़गार के आधार पर शहरों की श्रेणी तय करती है। यह बहुत ही उलझाई हुई परिभाषा है।
भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां रोज़गार से शहर को परिभाषित किया जाता है।
लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि, मूलरूप से, हम शहर को लेकर कभी सहज नहीं हो पाए हैं। आप ट्रेन में बैठे हैं। आपसे किसी ने पूछा, “तुम हो कहां से?” आप कहेंगे, “मैं दिल्ली से हूं।” वे फट से दूसरा सवाल करेंगे, “नहीं, नहीं, असल में कहां से हो, घर कहां है तुम्हारा?” क्योंकि हमारे यहां शहरों से कोई होता नहीं है। यहां लोग सिर्फ आते हैं।
हम (70-80 के दौर में पैदा हुई) वह पहली पीढ़ी हैं जिसने शहर में जन्म लिया है और जिसके ज़ेहन में फौरन गांव नहीं आता। लेकिन, अभी भी इसे मानने में वक्त लगेगा कि लोग शहर के भी होते हैं। शायद एक और पीढ़ी बीत जाने के बाद शहर को लेकर यह सोच पुख्ता हो सके।
अपने फील्ड वर्क के दौरान जब मैं दिल्ली के बवाना औऱ पुश्ता में उन लोगों के साथ काम कर रहा था, जो दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से बेदखल कर, वहां पुनर्वासित किए जा रहे थे, तो एक बात मुझे बिलकुल समझ नहीं आई। वे सुलभ शौचालय में शौच का इस्तेमाल करने के लिए रोज़ाना तीन रुपए दे रहे थे। उनका इलाका शहर का एकदम बाहरी इलाका था। उनके सामने सरसों के खेत ही खेत थे। और वे रोज़ शौच के लिए पैसे दे रहे थे।

हैरानी के साथ उनसे पूछा, “आप शौच करने के लिए हर बार तीन रुपए क्यों देते हैं? आप तो वैसे ही एकदम खुले में हैं।” जवाब देनेवालों में वे पुरूष भी शामिल थे जो दिल्ली के बड़े-बड़े इलाकों में अपने को हल्का करने के लिए दीवरों की तरफ खड़े होकर बेझिझक खुले में शौच करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, “हम गांववाले नहीं हैं, शहरी हैं।” पेशाब करने के लिए सुलभ शौचालय को तीन रुपए देकर हम शहरी कहलाते हैं। मैंने ऐसा कुछ पहली बार सुना था।
शहर के मुकाबले आपका गांव में होना कोई सवालिया निशान नहीं है। शहर में लाखों सवाल हैं – तुम बस्ती में क्यों रहते हो? तुमने इस ज़मीन पर क्यों कब्ज़ा कर रखा है? तुमने यहां झुग्गी कैसे बना ली? इस सवालों के पीछे सरकार यही कहना चाहती है कि तुम यहां कैसे अधिकार मांग सकते हो, अधिकार चाहिए तो अपने गांव जाकर लो। गांव में भूमि सुधार की कम से कम बात तो हो सकती है लेकिन शहर में कोई भूमि सुधार नहीं होता। अब जाकर कहीं-कहीं इसकी शुरुआत हो रही है जैसे उड़ीसा में किया गया है।
अगर आप शहर में गरीब हैं तो आपकी कोई अलग से शिनाख्त, अहमियत या आर्थिक पहचान नहीं होती है। वहीं, आप गांव में गरीब हो सकते हैं और वहां गरीब के रूप में आपकी पहचान स्वीकार्य भी होती है। वहां आप गरीब के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। हमारे यहां लोगों के कल्याण से जुड़ी सारी योजनाएं गांव के लिए होती हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना – नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण सोलर योजना इस तरह की सारी योजनाएं ये सब गांव में सुधार के लिए हैं। ये योजनाएं शहरी गरीब के लिए नहीं है। इन योजनाओं को शहरी नहीं बनाया गया। मतलब गांवों को सारा कल्याण स्कीम दे दो और शहरों को उत्पादन करने दो।
दूसरा गांव को लेकर जो आदर्शवादिता है, रूमानियत है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि ‘असल भारत तो गांव में ही बसता है’, दरअसल, ये दोनों ही बातें गावों और गांववालों के प्रति एक शुद्धता, उन्हें एक खास दर्जेबंदी में रखती हैं। उसके विपरीत शहरी गरीब को एक चालाक की नज़र से देखा जाएगा। उसके प्रति हमेशा यही व्यवहार होगा कि ये कुछ हड़पने के लिए यहां है।

शहर का यहां के गरीबों के प्रति कुछ ऐसा ही रवैया है कि जब तक वे काम करते रहें तब तक वे बहुत अच्छे हैं लेकिन, जैसे ही वे यहां अपना अधिकार मांगने लगें तो वे पराए हो जाते हैं। काम करो, अधिकार की बात मत करो। अपनी सुविधानुसार जब उनका इस्तेमाल करना हो तो लो बिजली ले लो, लेकिन सैनिटेशन के लिए ड्रेन हम नहीं लगाएंगे, पहले कहेंगे बस्ती यहां तक बढ़ा लो, ताकि बाद में उसे तोड़ने का हक भी हमारे पास होगा। 20 साल के लिए बस्ती बनाने के लिए बोल दिया लेकिन पट्टा 10 साल का ही देंगे। शहर अपनी शर्तों पर लगातार उनसे मोल-भाव करता रहता है ताकि कभी वे स्थाई-पन महसूस ही न कर सकें।
इसका असल चेहरा महामारी में एकदम खुलकर सामने आ गया। यही है शहरी गरीब होने का मतलब। आपका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसका लब्बोलुबाब ये है कि आप हर तरह की सोच से बाहर हैं। सरकार और सरकारी योजनाओं की सोच से बाहर हैं। आप उस डेटा से भी बाहर हैं जहां एकाउंट में कैश ट्रांसफर किया जाता है। शहरी गरीब के पास अपना कोई इलाका नहीं, कोई पहचान नहीं, उसे नागरिक होने का भी अधिकार नहीं है। इस सबके लिए हमने इतनी ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। सरकार के लिए ज़मीन महत्त्वपूर्ण है, वो बस्ती में रहने वाले बाशिंदे नहीं देखती। कोर्ट अतिक्रमण की बात करती है। उन्हें ज़मीन और ज़मीन पर अधिकार दिखाई देता है, लोग दिखाई नहीं देते।
मेरे ख्याल से परेशानी का शुरुआती सबब यही है – शहर में एक गरीब नागरिक के रूप में रहना – जिसका शहर की संरचना में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इक्का-दुक्का फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों या ऑटो चलाने वालों की आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। लेकिन, सच तो ये है कि ये फैक्ट्री मज़दूर या ऑटो चलाने वाले हमारे शहरीकरण की पूरी तस्वीर नहीं हैं। एक तो ये सारी आवाज़ें पुरुषों की हैं, उसके ऊपर ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं।
हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि शहरों का निर्माण औद्योगिक क्रांति के सिद्धांतों और उसके साथ हुए औद्योगिक शहरीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन, हमारे यहां औद्योगिक शहरीकरण नहीं है! हमारे शहरी क्षेत्र किसी भी तरह के उद्योग, उद्योग से जुड़े उत्पादन के बिना ही विस्तार पा रहे हैं। वित्तीयकरण के दौर में जहां पूंजी पर अधिकार ही सबकुछ है वहां शहरीकरण किस तरह हो रहा है? अब जिसके पास पूंजी है वही अपनी मनमानी करेगा ऐसे में अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था (इंफॉर्मल इकॉनमी) के ज़रिए ही काम होगा – आप डिलीवरी ब्वॉय ही बनाएंगे, ज़िंदगी भर ज़ोमाटो, स्विगी के लिए खाना और सामान पहुंचाने का काम ही करवाएंगे, कंस्ट्रक्शन की जगहों पर काम करवाएंगें। क्योंकि आपने शहर में उनके लिए कोई और रास्ता ही नहीं बनाया है।
वास्तव में अपनी कक्षा के शुरुआती सेमेस्टर में हम इन्हीं सवालों से क्लासरूम में बात की शुरुआत करते हैं। पहले कुछ हफ्ते स्टूडेंट्स को यही करना होता है कि वे सवाल करें कि कौन शहरी है, शहर क्या है? हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे सवाल पर सवाल करते रहें कि शहर की पहचान कैसे होती है- क्या शहर सामाजिक संबंधों की जगह है, क्या ये एक ऐसी जगह है जहां लोकतंत्र, आधुनिकता और महानगरीय जीवन को लेकर एक निश्चित धारणाएं हैं?
कक्षा में इन सवालों में सबसे खास होता है जाति के सवाल पर बात करना। उनके मन में जो धारणा है कि शहर वो जगह है जहां जाति का कोई महत्त्व नहीं होता, शहर आकर जाति गायब हो जाती है या जहां कोई जाति नहीं पूछता। इसपर बात करना मज़ेदार होता है। खैर, ये सच तो नहीं है लेकिन, उनकी बातें सवाल तो खड़ा करती हैं कि क्या सच में ऐसा है कि शहर में जाति की जकड उतनी गहरी नहीं होती जितनी गांवों में उसकी पकड़ मज़बूत होती है?
भारत में, सरकारी श्रेणियों में गांव और शहर साफतौर पर विभाजित हैं।
अब हम क्लास में जाति के सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल है कि आप गांव और शहर में जाति आधारित अलगाव का आकलन कैसे करते हैं? इसके लिए किस तरह का डेटा आपके पास है? यहां के स्टुडेंट्स को डेटा विश्लेषण के लिए आधुनिक जीआईएस तकनीक के गुर भी सिखाए जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अपनी जीआईएस क्लास में जाइए और शहर के भीतर जाति संरचना का एक नक्शा बना लाइए। वो जाते हैं और वापस आकर कहते हैं कि हम नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? तो वे कहते हैं कि इसके लिए कोई डेटा ही नहीं है। इसपर मेरा सवाल यही होता है तो बताओ कि शहर की जातिगत संरचना पर कोई डेटा क्यों नहीं है?
दरअसल, उन्हें यही बताना है कि सवाल पूछो।
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना की थी न, तो उसका डेटा कहां हैं? अगर, सार्वजनिक नहीं है तो, क्यों सार्वजनिक नहीं है? अब यही सवाल गवर्नेंस की कक्षा में जाकर पूछो कि शहर की जाति जनगणना सार्वजनिक क्यों नहीं है? क्यों हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि हमारे यहां किस जाति के कितने लोग हैं, वे क्या करते हैं?

अब यही सवाल इकॉनोमिक्स की क्लास में लेकर जाओ। वहां वे सवाल करते हैं कि शहर के भूगोल को आर्थिक आधार पर देखने का क्या मतलब होता है? अर्थशास्त्रियों के लिए शहर वो जगह है जहां पूंजी है। शहरी अर्थशास्त्रियों के लिए शहर ज़मीन और उस पर काम करने वाले मजदूरों के बीच की सांठगांठ है जिसे वे अपनी भाषा में समूह अर्थशास्त्र कहते हैं। कक्षा में स्टूडेंट्स को ये सब बताते हुए हम कहते हैं कि “इस बात को समझने की कोशिश करो कि महानगर से जुड़ा एनसीआर आर्थिक क्षेत्र क्यों है, बावजूद वहां नगरपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता?” लेकिन फिर यह भी पूछें कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के भीतर समूह अर्थशास्त्र क्या है? क्या यह ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह इसमें बड़ी कंपनियां और पूंजी के सिद्धांत काम करते हैं?
गवर्नेंस की क्लास में शहर एक सरकारी श्रेणी हो जाता है। वैधानिक शहर या जनगणना का शहर क्या होता है? नगर पंचायत क्या है? क्या ये गांव के लिए है या ये शहर के लिए ही है सिर्फ? इन श्रेणियों को देखकर क्या समझ आता है? इस पर स्टूडेंट्स कहते हैं, “ये सब अलग-अलग नहीं है, ये तो सब एक विस्तार हैं जो बनते-बदलते रहते है, ये सब एक-दूसरे में मिले हुए हैं।” यहां मेरा जवाब होता है, “नहीं, बिलकुल नहीं। नरेगा सिर्फ गांवों में मिलता है। ये विस्तार वाला नज़रिया सुनने में अच्छा लग सकता है लेकिन सरकारी कागज़ों में नरेगा उन्हीं जगहों पर मिलता है जो सरकारी श्रेणी के अनुसार गांव कहलाते हैं।”
एक शहरी अध्ययन से जुड़े शिक्षक होने के नाते मुझे ये बात सुनने में बहुत सुंदर लग सकती है कि सब एक ही हैं, गांव और शहर अलग-अलग थोड़े हैं वे तो एक ही नदी की धारा हैं। लेकिन, ये सच नहीं है। भारत में, सरकारी श्रेणियों में गांव और शहर साफतौर पर विभाजित हैं। आपको ये मानना ही होगा और इसे इसी तरह देखना है।
शहर और गांव के प्रति हमारी बहुत सारी धारणाओं को कोविड महामारी ने बिलकुल ध्वस्त कर दिया है।
क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपके यहां पंचायत है या नगरपालिका। आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं कि नहीं। आपको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की सुविधा मिलती है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) की। आपको नरेगा के तहत काम मिलता है कि कुछ भी नहीं मिलता?
अब, यहां से स्टूडेंट्स फिर पर्यावरण विज्ञान की क्लास में जाते हैं। वहां प्रोफेसर कहेंगे कि, “हमें इन श्रेणियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शहर है क्या गांव है। क्योंकि हवा और पानी के लिए कोई कैटगरी नहीं होती। आप इन्हें सिर्फ इन स्रोतों के भूगोल के ज़रिए ही समझ सकते हैं। बैंगलोर का पानी कावेरी से आ रहा है। इस पानी के रूट को समझो ये ही पानी का भूगोल है।” तो, शहर की कोई एक परिभाषा नहीं है। आप कहां खड़े होकर किस नज़रिए से सवाल पूछ रहे हैं उसी के आधार पर इसका जवाब दिया जा सकता है।
शहर और गांव के प्रति हमारी बहुत सारी धारणाओं को कोविड महामारी ने बिलकुल ध्वस्त कर दिया है। तमाम शहरी अध्ययन एवं शोध के बावजूद शहरों में रोज़ी-रोटी और ज़िंदा रहने का संकट गहराता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि हम अपने शहरों को सही तरह नहीं जान पाए हैं?
कोविड को हमने एक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखकर उसकी बहुत ही सतही, संकीर्ण और गलत पहचान की। अगर हम इसे स्वास्थ्य के साथ-साथ आजीविका के संकट के रूप में देखते तो शायद हमारी स्ट्रैजी कुछ और होती। यहां ‘गलत पहचान’ (मिसरिकग्निशन) शब्द फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक एटिन बलिबार की देन हैं। इसका अर्थ ‘ठीक से न समझने या कुछ न समझने से’ कहीं ज़्यादा हमारे समाज की सत्ता की संरचना की सच्चाई से जुड़ा है – आप किसकी नज़र से देख रहे हैं, उसे किस ढंग से बता रहे हैं। इसलिए, हम जिस ‘गलत-पहचान’ की बात यहां कर रहे हैं वो इस संदर्भ में है कि ‘घर से काम करने की, घर पर रहने की’ जिस सुविधा के आधार पर हम ये बात कहते हैं वो एक खास तरह के शहर की कल्पना पर आधारित है। शहर की एक ऐसी कल्पना जो हकीकत में बिल्कुल अलग है।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही हमारे ‘अर्बन स्टडीज़: शहरी अध्ययन’ की भी समस्या है। आप उस शहर के बारे में बात करते हैं जो आपकी कल्पनाओं में, आपके दिमाग के भीतर है। जहां हर किसी के पास एक औपचारिक नौकरी है, हर कोई दफ्तर जाता है। सभी एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। उनके पास लौटने के लिए घर है। असल में आप उस शहर के बारे में बात नहीं करते जो वास्तव में आपके पास है।
सोचिए, भारत में काम करने वाले दस मज़दूरों में से आठ किसी व्यवस्थित अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े हैं। वे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। उन आठ में से भी चार सार्वजनिक जगहों पर काम करते हैं जैसे – सड़कों पर, कचरे फेंकने के स्थानों पर, निर्माण स्थलों पर, परिवहन और बस स्टेशनों पर काम करते हैं। यहां ‘घर से काम करने का’ लॉजिक सरासर बेबुनियाद है क्योंकि उनका कोई ऑफिस नहीं है। दूसरा, जिसे बाद में लोगों ने समझा और इसपर चर्चा भी की कि भारत में दो-तिहाई परिवार 1.5 स्क्वायर फीट के घरों में रहते हैं। ऐसे में आपस में दूरी बनाए रखने की बात ही उनके लिए बेईमानी है।
महामारी के इस समय में बड़ा सवाल इस बात को समझना कि शहरीकरण के इतिहास के बारे में हम कहां से खड़े होकर बात कर रहे हैं। हमें सिएरा लियोन, केन्या और उन अंतरराष्ट्रीय शहरों के अनुभवों को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए जिन्होंने हमारे जैसे संदर्भों में इबोला जैसी महामारी का सामना किया है। लेकिन, हम तो सुपरपावर हैं और हम सिर्फ लंदन या न्यूयॉर्क के शहरों को ही देखेंगे। हम नहीं सीखेंगे सिएरा लियोन से जिसने इबोला के दौरान शानदार सामुदायिक क्वारंटाइन के मॉडल विकसित किए थे।
उदाहरण के लिए, मुम्बई में चॉल या किसी गली में बने घरों को ही ले लीजिए। इसमें एक प्वाइंट से दूसरे प्वाइंट के बीच जो चार-पांच घर होते हैं उनके अलावा इस बीच की जगह का इस्तेमाल कोई नहीं करता है। इन घरों के लोग वहां अपने कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, बच्चे वहां खेलते हैं। उन्हें हम एक समूह कह सकते हैं, किसी एक यूनिट की तरह। कोविड के दौरान कई समुदायों ने ऐसी जगहों के दोनों प्वाइंट – ऐसे अहातों या गलियों के शुरुआत में और गली जहां खत्म हो रही है वहां साबुन और पानी रखना शुरू कर दिया। अगर, क्वारंटाइन करना है तो वो समूह अपनी जगहों पर इंसानियत के साथ क्वारंटाइन तो कर सकता है। हमारे शहरों को देखते हुए यही सही लॉजिक है कि क्वारंटाइन ज़ोन घर न होकर गली को बनाया जाए। मुख्य बात यही है कि ग्लोबल साउथ के शहर जिसकी एक भिन्न तरह की संरचना होती है, जिसका अपना एक अलग ही इतिहास है उसे देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि ‘घर पर रहें, घर पर रहकर काम करें।’
हमारे यहां शहर या शहरीकरण के विचार पर अमेरिकन और यूरोपीय औद्योगिक शहरीकरण की छाप बहुत गहरी है, जो मूलरूप से ग्लोबल साउथ के शहरों की असलियत से बहुत अलग हैं। इस बात के एहसास ने ही आईआईएचएस और ग्लोबल साउथ थियोरी के जन्म की नींव रखी। मैं जब कैलिफोर्निया विश्वविद्य़ालय, बर्कले में पीएचडी कर रहा था, तब हमें यूरोपीय औद्योगिकीकरण के समय हुए शहरीकरण या नगरीकरण के उदाहरण के आधार पर ही शहरी सिद्धांत पढ़ाया जाता था। हालांकि, ‘ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट’ को देखकर तो पता चलता है कि शहरीकरण के वे सिद्धांत खुद नॉर्थ अमेरिका के देशों में ही कारगर साबित नहीं हुए। आईआईएचएस, का बहुत सारा काम और मेरा खुद का काम इस बात को स्थापित करने में खर्च होता है कि ग्लोबल साउथ (लातिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका) के शहरों के इतिहास में कई तरह की विशिष्टताएं एवं समानताएं हैं। ग्लोबल साउथ शहरी इतिहास का हमारे वर्तमान शहरों के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है।
उदाहरण के लिए, एक बड़ा सच यह है कि हमारे शहर उत्तर-औपनिवेशिक काल की देन हैं। इसमें हमारी स्थानीयता भी शामिल है। जैसे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों एक दूसरे से बिलकुल भिन्न है। दोनों ही इलाकों की अपनी विरासत है, चिन्ह हैं। देखा जाए तो हमारे शहर मुख्य रूप से अनियोजित ही रहे हैं, है ना? वे आर्थिक व्यवस्था एवं स्थानीयता के रूप में बिल्कुल अनियोजित हैं। दिल्ली में हर चार में से तीन व्यक्ति सुनियोजित कॉलोनियों के बाहर रहते हैं। इनके नामकरण को ही देख लीजिए – अनधिकृत कॉलोनी, नियमित कर दी गई अनधिकृत कॉलोनियां, शहरी गांव, ग्रामीण गांव, स्लम एरिया, जेजे क्लस्टर… इसके बावजूद हम योजनाओं के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि सबकुछ हमारे नियंत्रण में है।
दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में एक ऐसे क्षेत्र को ‘शहरीकरण के योग्य क्षेत्र’ के रूप में रेखांकित किया गया है जहां प्लान तैयार होने की तारीख के दिन भी एक-एक इंच ज़मीन पर पहले से ही निर्माण हो चुका था। ये वो इलाका है जिसपर ब्लू लाइन मेट्रो चलती है और जिसे हम पश्चिमी दिल्ली कहते हैं। तो, जो इलाके पूरी तरह से बन चुके हैं, जहां आपकी मेट्रो चल रही है उसे आप शहरीकरण के नाम पर भविष्य की योजनाओं में शामिल कर रहे हैं।
दूसरा, हमें ग्लोबल साउथ के बाशिंदो की मानसिकता को भी समझने की ज़रूरत है। कई लोगों को उनके रोज़मर्रा के जीवन और महामारी से आए संकट में बहुत ज़्यादा नाटकीय बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। बहुमत शहरी भारतीयों के लिए इस तरह के संकट और रोज़मर्रा से जुड़ी परेशानियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। कुछ भारतीयों के लिए ज़रूर ये किसी तिलिस्म के टूटने और वास्तविकता का सामना करने जैसा था लेकिन अधिकांश के लिए महामारी से निकले संकट का अनुभव नया नहीं था। यही वजह है कि 2020 में जब हाइवे पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी और सभी पत्रकार हाइवे पर पैदल अपने घर लौट रहे मज़दूरों से पूछते कि ‘आप क्यों ऐसे जा रहे हैं?’ उनका जवाब होता कि ‘जाना है तो जाना है’। उनकी हिकारत भरी निगाहें उल्टा सवाल कर रही होतीं कि ‘क्या हो गया? यह आपके लिए इतना चौंकाने वाला क्यों है? हम हमेशा से इसी तरह मोल-भाव करते रहे हैं। हमें हमेशा से यही करना पड़ता है।’
इसके पीछे की मंशा यही थी कि कोविड से लोग मर रहे हैं। बिना कोविड के भी लोग मर रहे हैं। फिर भूख और रोज़ी-रोटी की कमी से भी मर रहे हैं। हमारा काम मौत से बचना है। हमारा काम कोविड से मरना नहीं है। मरना नहीं है तो फिर चलना ही हमारे पास एकमात्र उपाय है। यही मेरी सबसे अच्छी संभावना है – वापस गांव लौट जाना। गांव, जहां दो वक्त की रोटी तो इज़्ज़त से मिलेगी।
यह लेख मूलरूप से द थर्ड आई पर प्रकाशित हुआ था।
उम्मीद:

असलियत:
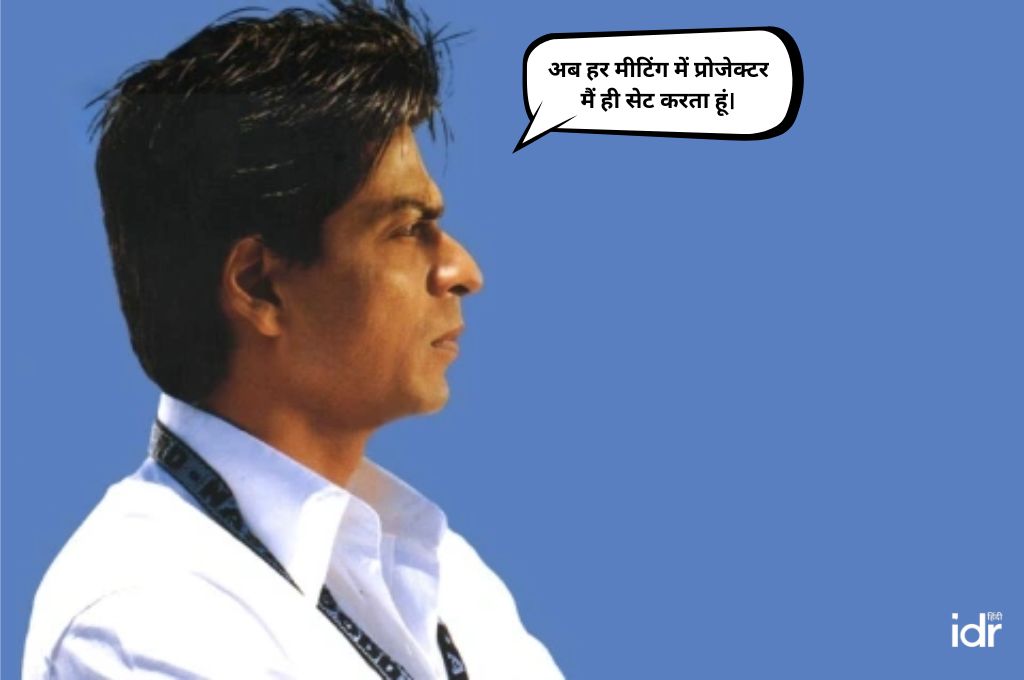
उम्मीद:

असलियत:
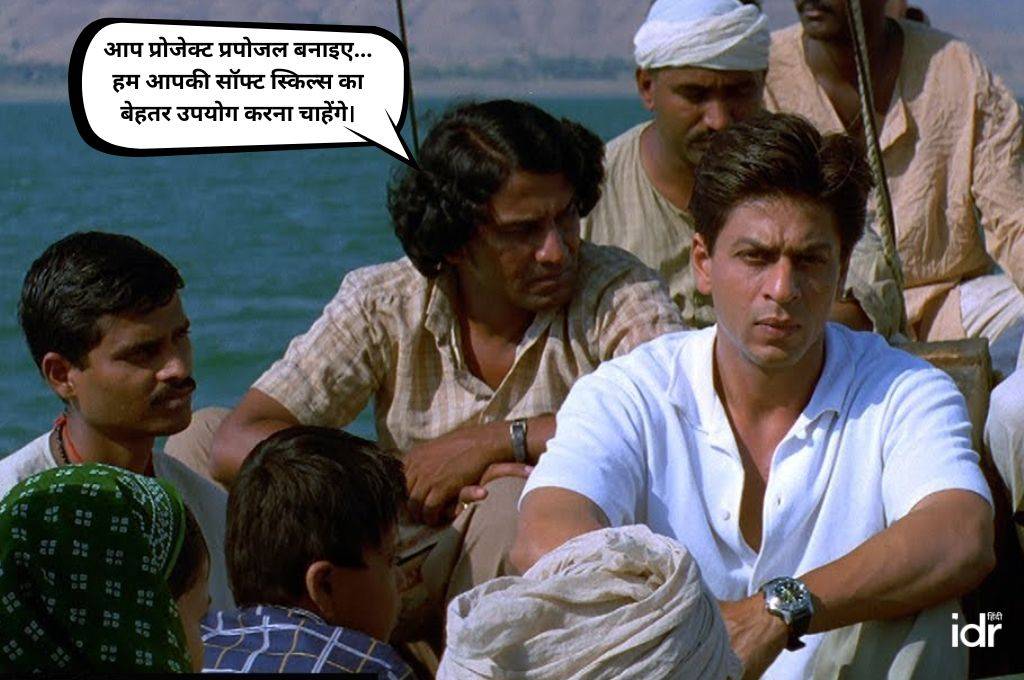
उम्मीद:
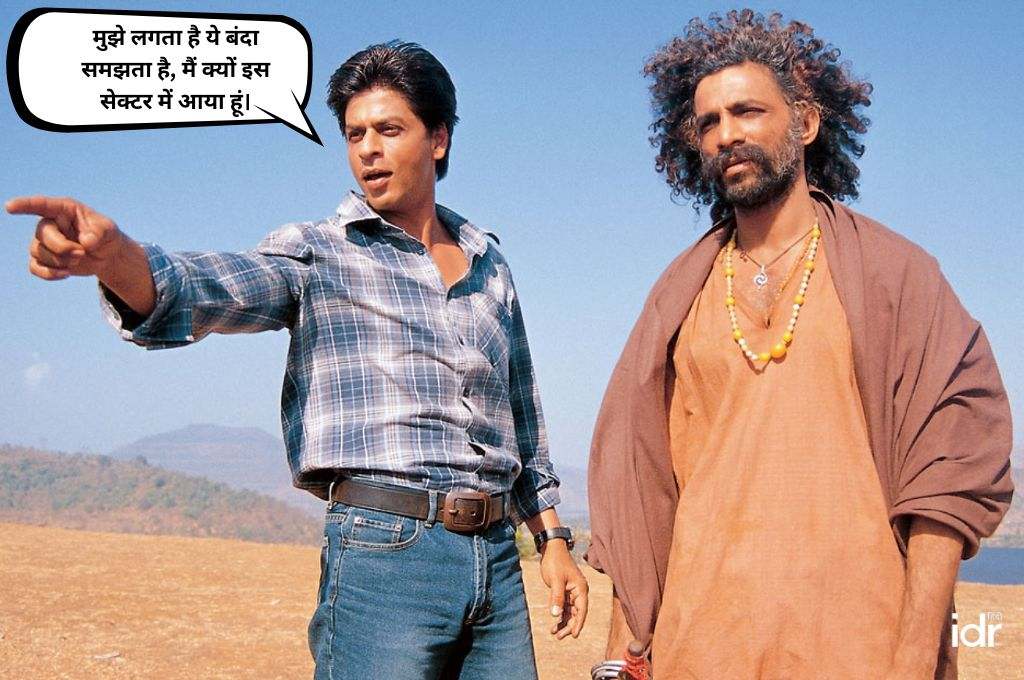
असलियत:

उम्मीद:

असलियत:

उम्मीद:
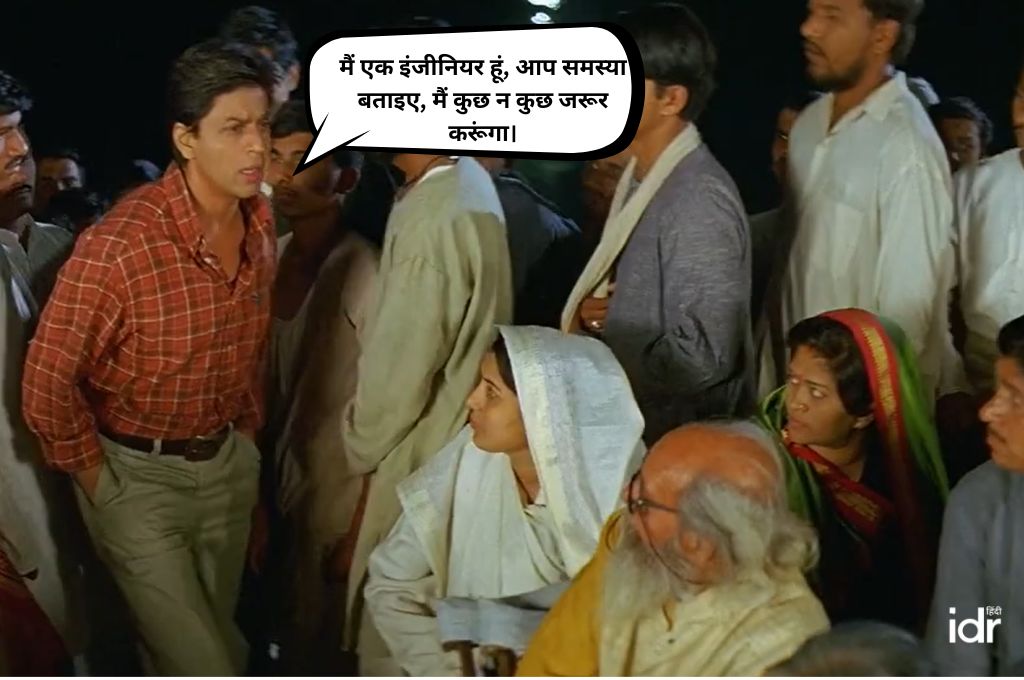
असलियत:

भारत की जनसंख्या लंबे समय से मिथकों और गलत सूचनाओं से परेशान रही है, सीमित संसाधनों को बढ़ती जनसंख्या से जोड़कर देखने वाला वैश्विक दृष्टिकोण अक्सर इसे और बढ़ा देता है। हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। इससे प्रेरित दृष्टिकोण ने एक व्यापक धारणा को जन्म दिया है कि भारत की बढ़ती आबादी, संसाधनों की कमी से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे कई गंभीर वैश्विक मुद्दों की जड़ है। इन गलतफहमियों ने डर को बढ़ाया है और नीतिगत चर्चाओं को नतीजे हासिल ना हो पाने वाली दिशाओं की ओर मोड़ दिया है, जैसे- जनसंख्या नियंत्रण के सख्त उपायों की मांग।
इन वैश्विक मिथकों के अलावा, कम आबादी वाले समुदायों की बढ़ती संख्या को लेकर डर भी फैलाया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण उपायों से जुड़ी भारत के राजनीतिक नेताओं की मांग ने इस चिंताजनक स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया है। इस तरह की झूठी धारणाएं, रूढ़िवादी विचारों को बनाए रखती हैं और नीतिगत निर्णयों पर बुरा प्रभाव डालती हैं। जरूरी मुद्दे जिन पर बात किए जाने की ज़रूरत है, उनसे ध्यान भटकाकर यह सिविल सोसाइटी के काम में बड़ी बाधा डाल सकती हैं। इसी को लेकर, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने मीडिया की व्यापक सहभागिता के जरिये साक्ष्य-आधारित चर्चाओं को बढ़ावा देकर इस नजरिए को नया आकार देने की कोशिश की है। हमने जिन मिथकों को दूर करने की कोशिशें की है, यह लेख उन पर रौशनी डालता है। साथ ही, यह हमारी रणनीति, प्रयास और चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।
आज कई भारतीय राज्यों में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले पुरुष और महिला नसबंदी जैसे उपाय मौजूद हैं। इसके अलावा कई निजी सदस्य विधेयक (प्राइवेट मेम्बर बिल) संसद में पेश किए गए हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण के कड़े उपायों का प्रस्ताव करते हैं, जैसे कि जोड़ों को दो से अधिक बच्चे पैदा करने से हतोत्साहित करना। असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने दो बच्चों की नीति से जुड़ा कानून भी लागू किया है – जहां दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों को सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाता है या पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। जुलाई 2021 में, उत्तर प्रदेश का विधि आयोग उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक लेकर आया जिसमें राज्य की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए निर्देश प्रस्तावित किए गए।
हालांकि इमर्जेंसी (1976-78) के दौरान हुई जबरन नसबंदी जैसे जनसंख्या नियंत्रण के तरीकों की तुलना में ये कदम मामूली लगते हैं, फिर भी ये भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की अधिकार-आधारित भावना के अनुरूप नहीं हैं।
यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से भारत में जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य तरीका नसबंदी रहा है जिसका बोझ महिलाओं पर ज्यादा पड़ा है। ऐसे समय में जब भारत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रजनन आयु वर्ग (15-49 वर्ष) में आता है, गर्भनिरोधन के अस्थायी तरीके जैसे कंडोम आज के समय की मांग हैं, न कि नसबंदी। हालांकि, जनसंख्या चर्चा में गर्भनिरोधक बहुत प्रमुखता से शामिल नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार, भारत में प्रजनन आयु की लगभग 9.4% महिलाओं – यानी लगभग 2.1 करोड़ महिलाओं – के पास गर्भ निरोधकों तक पहुंच या उनका उपयोग करने की एजेंसी नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को यह निर्णय लेने की आजादी हो कि वे बच्चे पैदा करना चाहती हैं या नहीं, कब चाहती हैं और किस अंतराल पर करना चाहती हैं। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसके लिए उठाए गए कदम, कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीतियों का सहारा लिए बिना असरदायक साबित हुए हैं।
यह बताना मुश्किल है कि बढ़ती आबादी पर चर्चा का वैश्विक नीतियों, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। हालांकि, भारत की बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के बीच अनुमानित संबंध पर मुख्यधारा की मीडिया रिपोर्टों के कई उदाहरण मौजूद हैं। यह समस्या को बहुत ही गलत तरीके से दिखाता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बीच संबंध को नजरअंदाज करता है। यह एक तरह से दुनियाभर के सबसे धनी 1% को दोषमुक्त कर देना है जिसका कार्बन उत्सर्जन वैश्विक आबादी के आधे से ज्यादा सबसे गरीब लोगों से भी अधिक है।
ये वजहें, जनसंख्या से जुड़े मिथकों के उभरते ही, उनकी पहचान करने और मिटाए जाने को जरूरी बना देती हैं। हमारे अनुभव के आधार पर, भारत की आबादी के बारे में बार-बार उठ कर आने वाले कुछ मिथक इस प्रकार हैं –
अप्रैल 2023 में, संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया, इस खबर ने दुनियाभर का ध्यान खींचा। इस आंकड़े को अनियंत्रित जनसंख्या विस्फोट के सबूत के रूप में गलत तरह से समझा गया जबकि वास्तव में भारत ने अपनी जनसंख्या वृद्धि में मंदी देखी है। एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर), जो एक महिला द्वारा उसके जीवनकाल में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या है, 1992-93 में 3.4 से घटकर 2019-21 में 2.0 हो गई है। साल 2020 में द लैंसेट में प्रकाशित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 2048 तक 1.6 अरब तक पहुंच सकती है और वर्ष 2100 में यह लगभग 1.1 अरब हो जाएगी। ये रुझान इशारा करते हैं कि भारत, जनसंख्या वृद्धि में ठहराव लाने की सही राह पर बढ़ रहा है।
एक और आम मिथक है कि भारत की जनसंख्या जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। यह गलत धारणा उपभोग के पैटर्न की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज करती है। वैश्विक साक्ष्य बताते हैं कि खासतौर पर विकसित देशों में, जलवायु परिवर्तन जनसंख्या की बजाय उपभोग के पैटर्न से अधिक संबंधित है। ऊंची आय वाले देश जिनकी आबादी कई विकासशील देशों की तुलना में कम है लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में इनकी हिस्सेदारी ज्यादा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की जनसंख्या दुनियाभर की केवल 4% है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 15% है। इसके विपरीत, वैश्विक आबादी के लगभग 17% के साथ भारत, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 7% का योगदान देता है।
आंकड़ों से परे सतत विकास और जिम्मेदार उपभोग पर ध्यान केंद्रित करके, जलवायु परिवर्तन के वास्तविक कारकों पर बात करने वाले नज़रिये को फिर से तैयार किया जा सकता है।
अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुसलमानों की आबादी में बढ़त को लेकर फैलाए जाने वाले डर ने भारत में विभाजनकारी बयानबाजी को बढ़ावा दिया है। इन दावों के उलट, आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में सभी धार्मिक समूहों ने दशकीय विकास दर में गिरावट का अनुभव किया है, पिछले तीस सालों में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की आबादी में गिरावट अधिक स्पष्ट है। 2001 और 2011 के बीच, दशकीय वृद्धि दर में हिंदुओं के लिए 3.1% की तुलना में मुसलमानों के लिए 4.7% की गिरावट आई है। साथ ही, मुसलमानों में टीएफआर 1992-93 में 4.4 से घटकर 2019-21 में 2.4 हो गई।
जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन दर पर धर्म से ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक कारकों में निवेश के स्तर का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, बिहार में हिंदू आबादी की टीएफआर (2.88) केरल में मुसलमानों की टीएफआर (2.25) से काफी अधिक है। ये आंकड़े अल्पसंख्यकों द्वारा जानबूझकर चली गई चाल के मिथक को खारिज करते हैं और आबादी से जुड़े मुद्दों के लिए डेटा-संचालित नजरिये की जरूरत को रेखांकित करते हैं।

पिछले कुछ दशकों में, इन मिथकों को समय-समय पर मुख्यधारा के मीडिया, राजनेताओं और यहां तक कि सिविल सोसाइटी द्वारा भी दोहराया गया है। इसलिए हमारे काम का मुख्य उद्देश्य, सही समय पर व्यापक शोध और डेटा आधारित खंडन जारी करना है, जिसे हमने वैश्विक और घरेलू दोनों मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रकाशित किया है।
हमारी शोध-आधारित मीडिया सहभागिता रणनीति के कुछ प्रमुख घटक इस तरह से हैं-
1. अंदरूनी सहयोग को सुविधाजनक बनाना: हमारी ज्ञान-प्रबंधन टीम, अप टू डेट रिसर्च तैयार करने और उन्हें एकत्र करने का काम करती है। हमारी संचार और मीडिया टीम, इसे हमारे मीडिया नेटवर्क के जरिए डिजाइन करने और फैलाने का काम करती है। तुरंत कार्रवाई से यह तय किया जाता है कि गलत सूचना को शुरुआत में ही दबा दिया जाए और अन्य झूठी कहानियों को पैदा होने से रोका जाए। हम आंकड़ों का विश्लेषण, कंटेंट बनाने और उसके प्रसार के लिए भी तकनीक का लाभ उठाते हैं, जिससे हमारी दक्षता और पहुंच में सुधार हुआ है।
2. जटिल शब्दावली और तकनीकी अवधारणाओं को सरल बनाना: हम भाषा को सरल बनाने, जटिल शब्दों को कम करने और अकादमिक अवधारणाओं को तोड़ने का काम करते हैं। इससे हमें संचार को बेहतर बनाने और कंटेंट के व्यापक उपभोग को बढ़ावा देने में मदद मिली है। भारत की जनसंख्या को लेकर फैली आशंकाओं का मुकाबला करने के लिए, हमने प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन क्षमता (रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी), विभिन्न विकास दरों और जनसंख्या अनुमानों के लिए मौजूदा सांख्यिकीय (स्टेटिस्टिकल) मॉडल जैसी अवधारणाओं को समझाया है। इसके अलावा, हम जनसंख्या गतिशीलता और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर हो रहे वैश्विक शोध पर भी लगातार नजर रखते हैं। हम प्रजनन क्षमता को प्रेरित करने वाली चीज़ों की बेहतर समझ बनाने के लिए जनगणना और एनएफएचएस जैसे सर्वेक्षणों में विभिन्न डेटा संकेतकों (इंडिकेटर्स) के बीच संबंध भी बनाते हैं।
अपने लेखों के माध्यम से, हम इस बात पर जोर देते हैं कि जनसंख्या को अक्सर ‘संख्या’ की समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में यह लोगों से संबंधित है। मानव विकास-विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक संदर्भ-अक्सर आंकड़ों के पीछे की प्रेरक शक्ति है। इन सब के साथ-साथ, फैसले गलतफहमियों के बजाय तथ्यों पर आधारित हों, का नज़रिया लोगों और नीति निर्माताओं दोनों को शिक्षित करने में सहायक रहा है ।
3. मीडिया के लिए संसाधन बनाना: हमारे दृष्टिकोण को हमारे मीडिया-केंद्रित प्रोजेक्ट और बेहतर बनाते हैं, जिसमें परिवार नियोजन संसाधन बैंक जैसी पहल शामिल है। यह परिवार नियोजन, जनसंख्या, और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की दिशा में नई से नई प्रगति, जानकारी और रिसर्च को मीडिया के साथ साझा करने की एक कोशिश है। मौजूदा समय में हम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिक डेटा और जेनरेटिव एआई तकनीक को शामिल करके संसाधन बैंक की सामग्री और डिज़ाइन को अपग्रेड करने पर काम कर रहे हैं।
हमने 50 ऑन-ग्राउंड रिपोर्टों के माध्यम से पूरे भारत में वंचित महिलाओं की आवाज़ का दस्तावेजीकरण करने के लिए पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया (पीएआरआई/परी) के साथ भी साझेदारी की है।
4. नीति निर्माताओं और सरकार के साथ काम करना: हम परिवार नियोजन के लिए अधिकार-आधारित, विकल्प-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए, हम उन्हें अच्छी तरह से रिसर्च किए हुए साक्ष्य-आधारित लेख, रिपोर्ट और नीति विवरण (पॉलिसी ब्रीफ) उपलब्ध कराते हैं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की, ‘रॉब्ड ऑफ चॉइस एंड डिग्निटी: सिचुएशनल असेसमेंट ऑफ स्टिरलाईजेशन कैम्प्स इन बिलासपुर’ के नाम की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट ने नसबंदी सेवाओं के कैंप मोड को बंद करने और परिवार नियोजन में देखभाल के स्तर में सुधार करने के सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नसबंदी सेवाओं के कैंप मोड को बंद करने और परिवार नियोजन में देखभाल के स्तर में सुधार करने के सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सामाजिक और विकास क्षेत्र की अन्य संस्थाओं और संगठनों के साथ हमारे रणनीतिक जुड़ाव ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में गर्भनिरोध के विकल्पों को बढ़ाने में योगदान दिया है। इसमें इंजेक्शन और प्रत्यारोपण (इंप्लांट) की शुरूआत भी शामिल है। इसे स्वास्थ्य अधिकारियों और नीति निर्माताओं के साथ लगातार बातचीत और जुड़ाव से हासिल किया गया है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और नीतियों में भी योगदान दिया है। ये प्रयास तय करते हैं कि हमारी रिसर्च और सिफारिशों को राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल किया जाए, जिससे उनका असर का दायरा बढ़ सके।
साक्ष्य-आधारित काम करने के बावजूद, हमें जनसंख्या से जुड़ी गलत सूचनाओं को सही करने के लिए मीडिया और अन्य सहयोगियों तक पहुंचने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में शामिल हैं:
1. पहले से मौजूद पूर्वाग्रह और गलत धारणाएं: जनसंख्या के मुद्दे से जुड़े कई लोगों के मन में जनसंख्या के लगातार बदलते पहलुओं को लेकर गहरे पूर्वाग्रह या गलत धारणाएं हैं, जिन्हें स्पष्ट सबूत के साथ भी बदलना मुश्किल है। सनसनीखेज मीडिया कवरेज और राजनीतिक बयानबाजी से इसे अक्सर बढ़ावा ही मिलता है। इसके समाधान की दिशा में बढ़ने के लिए हमारा नजरिया लोगों के साथ जल्दी और लगातार जुड़ने का रहा है। हमारा प्रयास, विश्वास पर आधारित रिश्ते बनाने, वेबिनार, कॉल और आपसी चर्चाओं के जरिये निरंतर शिक्षा प्रदान करने का रहता है। दर्शकों की खास चिंताओं और रुचियों को पूरा करने वाले संदेश तैयार करने से भी इन पूर्वाग्रहों को तोड़ने में मदद मिलती है।
2. मीडिया में सनसनीखेज कहानियों को प्राथमिकता: मीडिया आउटलेट अक्सर सनसनीखेज कहानियों को प्राथमिकता देते हैं जो साक्ष्य-आधारित रिपोर्टिंग के बजाय मिथक और गलत सूचनाएं फैलाती हैं। इसलिए, हम पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें उपयोग के लिए तैयार, तथ्य-आधारित कंटेंट मुहैया कराया जा सके जो आकर्षक और खबरों में आने योग्य हो। विशेष कहानियों, इन्फोग्राफिक्स और विशेषज्ञों के इंटरव्यू उपलब्ध कराने से तथ्य आधारित रिपोर्टिंग के साथ मीडिया संस्थाओं के हितों को साथ लेकर चलने में मदद मिल सकती है।
3. डेटा की जटिलता: सांख्यिकीय (स्टेटिस्टिकल) डेटा और जनसंख्या मॉडल की जटिलता आम लोगों के लिए बाधा बन सकती है, जिससे गलत सूचना के लिए जड़ें जमाना आसान हो जाता है। हम, पत्रकारों को डेटा सरल भाषा में समझाकर और स्पष्ट चित्रों और इन्फोग्राफिक्स से दर्शाकर, अवधारणाओं को आसान बनाने की कोशिश करते हैं।
4. राजनीतिक और वैचारिक विरोध: कुछ राजनीतिक और वैचारिक समूह उनके एजेंडे के खिलाफ जाने वाले, खासतौर से जनसंख्या नियंत्रण और अल्पसंख्यक विकास दर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण का विरोध कर सकते हैं। इसलिए, हम आर्थिक विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे सामान्य लक्ष्यों की बात रखते हुए डेटा को गैर-टकरावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
हमारा लक्ष्य खास रणनीतियों के साथ इन चुनौतियों को हल करके, अपने असर को बढ़ाना और यह तय करना है कि सटीक और साक्ष्य-आधारित जानकारी भारत में जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को आकार दे। गलत सूचना और प्रचार के इस दौर में, मिथकों का मुकाबला करने के साथ-साथ जटिल जनसंख्या मुद्दों पर स्पष्टता और सही जानकारी को सामने लाने, और जनता के बीच एक सूचित दृष्टि बनाने वाली जानकारी के प्रसार में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
1. जब हम लीडरशिप मीटिंग में बताते हैं कि ‘हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं का योगदान अनमोल है’… लेकिन मीटिंग के बाद उनकी राय सुनना भूल जाते हैं!
2. जब हम नेतृत्व स्तर के कार्यकर्ता तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देने की बात करते हैं… और उनके ट्रेनिंग सेशन को खुद ही कैंसल कर देते हैं!

3. जब वर्कशॉप में जमीनी कार्यकर्ताओं से सलाह लेने का वादा करते हैं… और उन्हें सिर्फ फीडबैक फॉर्म भरने के लिए बुलाते हैं!

4. जब प्रेजेंटेशन में ‘नेतृत्व/अहम फैसलों में जमीनी कार्यकर्ताओं को शामिल करें’ का स्लाइड दिखाते हैं… लेकिन उन्हें इवेंट में बुलाना ही भूल जाते हैं!

5. जब शीर्ष नेतृत्व/मुख्य लीडरशिप कहे कि ‘जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए सीखने के रास्ते बनाने होंगे’… और वही लोग अपने कमरे में अकेले बैठकर रिपोर्ट्स देख रहे हों!

उमाशंकर साह बिहार के शिवहर जिले के निवासी हैं और इलेक्ट्रिक ऑटो चलाकर अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। उमाशंकर बताते हैं कि सामान्य दिन में खर्च काट कर 800-900 रुपये तक, और कोई खास दिन रहने पर डेढ-दो हजार रुपये तक भी कमाई हो जाती है। ताजा आर्थिक सर्वे के अनुसार, कई आर्थिक पैमानों पर शिवहर जिला अन्य जिलों से पीछे है, जहां रोजगार और स्थानीय स्तर पर आजीविका कमाने के विकल्प बहुत कम हैं।
ऐसे में कभी खुद एक प्रवासी मजदूर रहे उमाशंकर ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को अपनी आजीविका का आधार बनाया है। साह अपने नये रोजगार से खुश हैं, लेकिन उनकी चिंता ऑटो की चार्जिंग को लेकर है। वे कहते हैं कि नई गाड़ी एक बार चार्ज करने पर 120 किमी तक चलती है और उन्हें हर दिन दो बार बैट्री चार्ज करना होता है और यह सुविधा अभी उनके लिए सिर्फ घर पर ही है। बैटरी कम चार्ज रहने पर दूर की सवारी मिले तो सोचना पड़ता है क्योंकि अभी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा नहीं है।
बिहार में किसी भी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहन (इलेक्ट्रिक व्हीकल- ईवी) के लिए सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट वर्तमान में सबसे अहम समस्या है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन नीति में चरणबद्ध रूप से शुरुआती चरण में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक भवनों और संपत्ति पर पांच साल में दो चरणों में 277 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, इस नीति में शुरुआती चरण में वाहनों की खरीद पर आर्थिक सहायता या सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन में 75% तक की छूट का प्रावधान किया गया है।
बिहार में पांच दिसंबर, 2023 को जारी की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगले पांच सालों के लिए प्रभावी है। इसके तहत बिहार ने एक ईवी इकोसिस्टम विकसित करते हुए 2028 तक कुल नए रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 15% और 2030 तक 30% करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल, यह 6.85% है जो देश में नए वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 6.40% से थोड़ा आगे है।
इस पॉलिसी के जारी होने के बाद बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल का गठन किया है और पॉलिसी के तहत सब्सिडी देने के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है।

ईवी थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स में ई-मोबिलिटी स्पेशलिस्ट अर्चित फर्सुले कहते हैं, “बिहार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में बसों और रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है और इसके प्रोत्साहन के लिए 56.54 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है।”
अर्चित कहते हैं, “इलेक्ट्रिक व्हीकल बिहार की अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था और पर्यावरण में अहम योगदान कर सकते हैं। ईवी विनिर्माण उद्योग, रखरखाव और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। ईवी विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश आकर्षित करने से बिहार के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधनों पर निर्भरता कम होने से ईंधन लागत में भारी बचत होगी। इससे राज्य में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है और वायु गुणवत्ता में सुधार संभव है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) के अनुसार, भारत का जीवाश्म ईंधन की वजह से वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वर्ष 2021 में योगदान लगभग 6.8% रहा।” ये साल 2000-2021 में 156% बढ़ा है।
इलेक्ट्रिक बसें कुशल, स्वच्छ और शांत परिवहन प्रदान करके सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर बना सकती हैं। बिहार ईवी नीति का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना है।
बिहार सरकार की एजेंसी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की फेम-2 स्कीम के तहत राज्य में 25 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन कर रही है।
इलेक्ट्रिक बसें दो श्रेणी की हैं– एक नौ मीटर और दूसरी 12 मीटर। इनका लोकप्रिय नाम 9एम और 12एम बसें हैं। हालांकि अत्यधिक लागत और रियायती किराये की वजह से इन बसों को चलाया जाना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए की गई एक खर्चीली कवायद है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) के एक अधिकारी ने बताया, “नौ मीटर बसों के परिचालन में 79 रुपये प्रति किमी खर्च आता है जबकि 12 मीटर बस के परिचालन में 84 रुपये प्रति किमी खर्च आता है। जबकि इन दोनों प्रकार की बसों से करीब 40 रुपये प्रति किमी की दर से राजस्व संग्रहण होता है।” इन बसों का स्वामित्व इसकी निर्माता कंपनी अशोका लिलैंड के पास है और ड्राइवर भी उसी कंपनी का होता है जिसका फेम-2 के तहत परिवहन निगम परिचालन करता है। इन बसों को चलाए जाने के खर्च और इनसे होने वाली कमाई के अंतर की भरपाई केंद्र व परिवहन विभाग की सब्सिडी के जरिए होती है। बस के प्रति किमी परिचालन के हिसाब से बीएसआरटीसी बस ऑपरेटर कंपनी को भुगतान करता है और यात्री परिवहन से हासिल होने वाले राजस्व का काम वह खुद संभालता है।
अर्चित फर्सुले कहते हैं, “यह बात सही है कि इलेक्ट्रिक बसों की अधिक पूंजी लागत इसे व्यापक रूप से अपनाए जाने में एक बाधा है, लेकिन ऐसी कई रणनीतियां हैं जो इनकी लागत को कम कर सकती हैं, जैसे– थोक खरीद यानी कई शहरों या राज्यों में मांग को एकत्रित करके, सरकार निर्माताओं के साथ बेहतर कीमतों पर बातचीत कर सकती है।“

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के ज़रिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करने से वित्तीय बोझ को साझा करने में मदद मिल सकती है। सीधे खरीद की बजाय, सरकार ई-बसों को लीज पर लेने पर विचार कर सकती है। ग्रीनबॉन्ड, जलवायु निधि और रियायती ऋण जैसे नए वित्तीय तंत्रों का उपयोग करके कम ब्याज दरों और अनुकूल शर्तों पर ई-बस खरीद के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान की जा सकती है।
इस संबंध में अर्चित कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड (सीइएसएल) की उस केस स्टडी का उदाहरण देते हैं, जिसमें भारत के प्रमुख महानगरों में इलेक्ट्रिक बसों की एक साथ खरीद करने से परिचालन लागत व सरकार की प्रति किमी सब्सिडी को कम करने में सफलता मिली है।
इलेक्ट्रिक बसों की परिचालन लागत, उसकी ऊंची कीमत और अधिक रखरखाव लागत की वजह से भले ही अधिक हो लेकिन ईंधन लागत के स्तर पर यह अपेक्षाकृत काफी सस्ती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सीएनजी व डीजल बसों के एक किमी परिचालन पर 23.50 रुपये की ईंधन लागत आती है जबकि इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने की लागत प्रति किमी मात्र 14 रुपये आती है।
लंबे रूट में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का किराया डीजल से चलने वाली एसी बसों के बराबर है और ग्राहक से कोई अतिरिक्त किराया नहीं वसूला जाता है। लेकिन जगह-जगह फिलहाल चार्जिंग स्टेशन न होने के कारण बस बीच रास्ते एक दूसरी चार्ज हुई बस से बदल दी जाती है। यात्रियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए इसमें सफर करने को अधिक सुकूनदायक बताया। पटना के दानापुर के रहने वाले 40 वर्षीय विनोद कुमार ने कहा, “इलेक्ट्रिक बसों में सफर बेहतर है और हम इसका इंतजार करते हैं। किराये में भी बहुत फर्क नहीं है।“
केंद्र सरकार ने पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 10 हजार इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए 16 अगस्त 2023 को पीएम ई-बस सेवा योजना शुरू की। इस योजना के तहत पहले चरण में 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 3600 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं, जिसमें बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं। केंद्र सरकार इस योजना के तहत पूरे देश में बसों के परिचालन पर 10 साल के लिए सहायता देगी जिसके तहत 6400 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
पटना में एक टाटा मोटर शोरूम के सेल्स टीम हेड पवन नागपाल कहते हैं, “हमारी कंपनी पांच साल से ईवी सेक्टर में है और इसमें लगातार विकास हो रहा है।“ वे आगे जोड़ते हैं कि “हमारे यहां बिकने वाली 10 में दो से तीन गाड़ियां ईवी होती हैं। ग्राहकों का आकर्षण ईवी की ओर बढ़ रहा है और सरकार की स्कीम से भी वे प्रभावित होते हैं, बिहार सरकार द्वारा जारी की गई ईवी पॉलिसी से हम आशान्वित हैं।”
हालांकि यह ट्रेंड सिर्फ राजधानी पटना का है और राज्य के दूसरे शहरों के बारे में ऐसे दावे नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि बिहार में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कार की बिक्री आधे प्रतिशत से भी कम है।
एक ईवी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वित्त वर्ष 2023-2024 में ईवी बिक्री में 5.5% हिस्सेदारी के साथ बिहार पांचवें नंबर पर है।
इसी तरह पटना के एक दोपहिया ईवी शो रूम एथर के सेल्स मैनेजर प्रियांशु सिंह ने कहा, “भारत सरकार के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के तहत वाहन की खरीद पर 10 हजार रुपये की सब्सिडी फिलहाल मिल रही है। बिहार सरकार की ईवी पॉलिसी आने के बाद उसके पोर्टल के जरिये ग्राहकों का आकर्षण बढ़ने की संभावना है।“ प्रियांशु मानते हैं कि सेल्स बढ़ाने के लिए चार्जिंग प्वाइंट या स्टेशन का नेटवर्क जरूरी है।
एक ईवी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वित्त वर्ष 2023-2024 में ईवी बिक्री में 5.5% हिस्सेदारी के साथ बिहार पांचवें नंबर पर है। दक्षिणी-पश्चिमी राज्यों में जहां दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिक बिक्री का ट्रेंड दिखता है; वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश व असम जैसे राज्यों में पैसेंजर ई-थ्री-व्हीलर की बिक्री का अनुपात ज्यादा है। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का पहले से ही बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। बिहार में दो पहिया वाहनों (13.87%) की तुलना में पैसेंजर ई-थ्री-व्हीलर (83.72%) की बिक्री छह गुना अधिक है।
हालांकि आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि वित्त वर्ष 2018 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 तक बिहार में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेड़ा 39 गुना बड़ा हो चुका है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलग-अलग सेगमेंट के लिए चुनौतियां भी अलग-अलग हैं। जैसे दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के लिए उसकी निर्माता कंपनियों द्वारा चार्जिंग स्टेशन का निर्माण शहरी क्षेत्र में ही किया गया है, ऐसे में शहर से बाहर लंबी दूरी के लिए उन्हें लेकर नहीं जाया जा सकता। यही स्थिति इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के साथ है, जिसके चालक की मजबूरी है कि वे उसे घर पर ही चार्ज कर सकते हैं। बिहार में इलेक्ट्रिक बसों के लिए अभी पटना में एकमात्र चार्जिंग स्टेशन है, जबकि मुजफ्फरपुर व राजगीर इलाकों में उसके लिए चार्जिंग प्वाइंट हैं।
चार पहिया व दो पहिया वाहनों की सेल्स टीम के सदस्यों से बात करने के बाद यह तथ्य उभर कर सामने आया कि उन्हें पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए ग्राहकों की अधिक समझाइश करनी पड़ती है और इसकी वजह उनके प्रोडक्ट में कोई इश्यू होना नहीं बल्कि चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क की कमी होना है। हालांकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ चुनिंदा शहरों में इसके लिए सघन अभियान चलाने व स्कूलों को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे सुझाव भी हैं।
अर्चित फर्सुले कहते हैं, “बिहार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कुछ चुनौतियों के बावजूद रोमांचक राह पर है। उच्च पूंजी लागत, सीमित चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और बैटरी की उपलब्धता से जुड़ी समस्याएं प्रमुख बाधाएं हैं, लेकिन सरकार इससे निबटने के लिए प्रयास कर रही है। नई नीति की एक प्रमुख विशेषता स्थानीय बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देना है, जो भारत में हाल ही में हुई लिथियम खोजों का लाभ उठाएगा और जिससे लागत और आयात पर निर्भरता कम होगी।“ लिथियम ऑयन बैटरी की क्षमता लेड एसिड बैटरी से ज्यादा होती है– जिन पर ज्यादातर ईवी परिवहन चलते थे और आज भी चलते हैं। जहां लेड एसिड बैटरी को रीसाइकल करने में पर्यावरण और स्वास्थ्य को बहुत हानि है, वहीं लिथियम की रिसाइकलिंग रेट 90 से 95% है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर इसे रीसाइकल नहीं करके ऐसे ही जमीन में छोड़ देंगे तो यह उसे बंजर कर सकता है, और इसका निबटान एक बड़ी चुनौती है।
यह स्टोरी इंटरन्यूज अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क के रिन्यूएबल एनर्जी ग्रांट के तहत कवर की गई है।
—