कॉमन्स की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि कुछ संसाधन निजी स्वामित्व में नहीं हो सकते हैं। ये संसाधन मानव जीवन, संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र का आधार होते हैं और इन पर पूरे समुदाय का अधिकार होना चाहिए। जैसे, हवा या समुद्र पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं हो सकता है क्योंकि ये पूरे जीवमंडल का हिस्सा हैं। इसी तरह जल, जंगल और जमीन भी अन्य उदाहरण हैं। हिंदी में भी अधिकांश लोग इनके लिए कॉमन्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन “सामुदायिक संसाधन” या “साझा संसाधन” इसके लिए अधिक उपयुक्त और सरल शब्द हो सकते हैं।
साझा संसाधनों की कई श्रेणियां हैं, जैसे भौतिक, सांस्कृतिक, डिजिटल और परंपरागत ज्ञान।
भौतिक कॉमन्स: ये साझा संसाधन मानव जीवन और पारिस्थितिकी के लिए अहम होते हैं। ये सीधे तौर पर हमारी आजीविका, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों में मददगार होते हैं। इनके महत्व को उदाहरण से समझते हैं-
1. जल संसाधन: नदियां, झीलें और भूजल जैसे स्त्रोत ग्रामीण और शहरी जीवन, दोनों के लिए मायने रखते हैं। साथ ही ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संतुलित करने में सहायक है।
2. वन संसाधन: उष्णकटिबंधीय जंगल, मैंग्रोव और पर्वतीय वन जैसे संसाधन जैव विविधता को संरक्षित करने, आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका का साधन होने के साथ-साथ उद्योगों के लिए भी अहम हैं।
3. तटीय संसाधन: तटीय और अंतर्देशीय मछली पालन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार है। इसके जरिए तटीय और आंतरिक जलीय क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। मछली पालन आर्थिक विकास का हिस्सा है, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में।
4. भूमि संसाधन: सामुदायिक चारागाह, शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र जमीन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थायी पशुधन प्रबंधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय पर्यावरणीय संतुलन में इनकी भूमिका अहम हो जाती है।
एक अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में 2.5-3 अरब लोग अपनी आजीविका और सांस्कृतिक या आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए कॉमन्स पर निर्भर हैं। कॉमन्स खासतौर पर उन लोगों को लाभ देते हैं जो समाज में हाशिए पर हैं, जैसे भूमिहीन किसान या आदिवासी समुदाय। कुल मिलाकर भौतिक कॉमन्स हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए अनमोल हैं। ये केवल संसाधन नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और पारिस्थितिक स्थिरता का आधार हैं। इनका संरक्षण और सतत प्रबंधन मानवता के सामूहिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
डिजिटल कॉमन्स: इसमें ऐसे संसाधन और प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो डिजिटल माध्यम में साझा, स्वतंत्र और सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। ये आमतौर पर सहकारी प्रयासों और सामुदायिक प्रबंधन के माध्यम से तैयार और संचालित किए जाते हैं। जैसे, मुफ्त और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स, मोज़िला फायरफॉक्स और एंड्रायड, या फिर सामूहिक ज्ञान मंच जैसे विकीपीडिया और डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म। ये सॉफ्टवेयर नि:शुल्क होते हैं और उनके सोर्स कोड को कोई भी देख, समझ और संशोधित कर सकता है। डिजिटल कॉमन्स सभी को ज्ञान और जानकारी तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसके साथ ही सामूहिक प्रयास और सह-निर्माण के सिद्धांतों पर आधारित ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर और प्लेटफॉर्म नए विचारों और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
सांस्कृतिक कॉमन्स: सांस्कृतिक कॉमन्स में वे चीजें शामिल होती हैं, जो हमारे विचारों, परंपराओं, रचनात्मकता और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं। इसमें एक समुदाय के लोग अपने रीति-रिवाजों, भाषाओं और कलाओं को साझा करते हैं। उदाहरण के तौर पर त्यौहार मनाना, स्थानीय भाषा में बोलचाल या कला आधारित विभिन्न प्रयास इसमें शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो सांस्कृतिक कॉमन्स समुदायों की पहचान को सुरक्षित बनाए रखते हैं।
डिजिटल और सांस्कृतिक कॉमन्स सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के साथ ही नए विचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित भी करते है। वैसे सामुदायिक संसाधन (कॉमन्स) केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये वैश्विक संसाधनों जैसे वायुमंडल और महासागरों तक फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए वायुमंडल एक ऐसा सामुदायिक संसाधन है, जिसमें ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करने की क्षमता सीमित है। इस विषय में होने वाली बातचीत में “सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों” (सीबीडीआर) के सिद्धांत का जिक्र जरूर होता है। सीबीडीआर के अनुसार जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों में फर्क है। विकसित देशों ने पुरातन समय से ही ज्यादा ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित की हैं, इसलिए उन्हें न केवल उत्सर्जन घटाने में नेतृत्व करना चाहिए, बल्कि विकासशील देशों की मदद भी करनी चाहिए। यह नजरिया वैश्विक स्तर पर सामूहिक संसाधनों की पहचान और उनके न्यायसंगत व टिकाऊ प्रबंधन के लिए एक तंत्र बनाने में मददगार हो सकता है।

सामुदायिक संसाधन साझा उपयोग पर आधारित होते हैं, क्योंकि इन्हें लोगों से अलग करना महंगा या कठिन होता है। साथ ही, ये संसाधन सीमित होते हैं और उपयोग के चलते खत्म हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ओडिशा के नयागढ़ जिले के सुलिया जंगल में जरूरत से ज्यादा दोहन ने इसकी प्राकृतिक पुनर्जीवन दर को प्रभावित किया, जिससे जंगल खत्म हो गया।
इस संदर्भ में, गैरेट हार्डिन ने “कॉमन्स की त्रासदी” की अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि जब संसाधनों का उपयोग सामूहिक होता है, तो लोग अपने स्वार्थ के कारण उनका अति-शोषण करते हैं। हालांकि, हार्डिन के विचारों की आलोचना भी हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता एलीनॉर ओस्ट्रॉम ने दिखाया कि कैसे समुदाय सामूहिक प्रबंधन के प्रभावी तरीके भी विकसित कर सकते हैं। नियम, संस्थान और सहयोगी प्रणालियां बनाकर उपयोगकर्ता संसाधनों के दोहन और पुनर्पूर्ति के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं, जिससे उनके टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।
सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन का एक और दृष्टिकोण कानूनी और नीतिगत ढांचे से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, 2006 का वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) आदिवासी और वन-निवासी समुदायों के परंपरागत भूमि और संसाधन अधिकारों को मान्यता देता है। अधिनियम में ‘सामुदायिक वन संसाधन’ (सीएफआर) की नई श्रेणी भी जोड़ी गई, जो गांव की परंपरागत सीमाओं के भीतर का वन क्षेत्र है।
एफआरए ने वन संरक्षण में एक नया आयाम जोड़ा, जिसमें लगभग 1.79 लाख ग्राम सभाओं को उनके परंपरागत क्षेत्र के भीतर वन, वन्यजीव और जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार दिया गया। इसने संसाधन प्रबंधन में समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित किया।
संसाधनों के प्रबंधन का एक और पहलू सह-शासन है। इतिहासकार पीटर लाइनबॉघ ने “कॉमनिंग” शब्द को लोकप्रिय बनाया, जो संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह साझा जिम्मेदारियों और सहयोगात्मक निर्णय-निर्माण की आवश्यकता पर जोर देता है। भारत के कोरोमंडल तट पर पारंपरिक मछुआरा समुदायों के उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। यहां की मछुआरा परिषदें स्थानीय जल क्षेत्रों में टिकाऊ मछली पकड़ने के नियम बनाती हैं, जैसे कुछ उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाकर संसाधन संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।
साझा संसाधनों का यह मॉडल कोविड-19 महामारी या बाढ़ जैसी आपदाओं में सामुदायिक राहत कार्यों में भी दिखा, जब राशन और अन्य संसाधनों को साझा कर मदद की गई। यह दर्शाता है कि सामुदायिक प्रबंधन और सहयोग टिकाऊ विकास और सामाजिक समृद्धि के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
भारत में कॉमन्स देश की कुल भूमि का लगभग पांचवां हिस्सा हैं और ये ग्रामीणों की आजीविका और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में बहुत अहम हैं। कॉमन्स के तहत आने वाली सार्वजनिक भूमि को भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसे राजस्थान में शामिलात भूमि, ओडिशा में सरबसाधारण और तमिलनाडु में पोरम्बोक कहते हैं। ये भूमि ग्रामीण परिवारों की जीवनरेखा है, क्योंकि इससे उन्हें पानी, ईंधन, चारा और लकड़ी जैसे संसाधन मिलते है। भारत के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में, सामुदायिक संसाधन (सीपीआर) ग्रामीण परिवारों की आय में लगभग 15 से 25 प्रतिशत योगदान करते हैं। सार्वजनिक भूमि के सभी तत्व गरीब और भूमिहीन परिवारों के लिए संकट के समय, यानी प्राकृतिक आपदा, संक्रमण, फसलों के खराब हो जाने जैसी परिस्थितियों में काम आते है। इसकी अहमियत को एक उदाहरण से समझते हैं- राजस्थान के जैसलमेर जिले में ओरण सार्वजनिक भूमि पर बनाए जाने वाले सार्वजनिक वन है। ये पवित्र वन ग्रामीण समुदायों के पारंपरिक नियमों और धार्मिक मान्यताओं के लिए संरक्षित किए जाते हैं। खास बात यह है कि राजस्थान के राज्य पक्षी और भारत के सबसे संकटग्रस्त पक्षियों में से एक सोहन चिड़िया के संरक्षण के लिए ओरण काफी मददगार साबित हुए हैं। इसका एक कारण यह है कि ये वन स्थानीय देवी-देवताओं से जुड़े होते हैं और इनकी देखभाल सामुदायिक सहभागिता से की जाती है।
इसी तरह पश्चिम बंगाल के सुंदरबन मैंग्रोव वन भी हैं, जो सामुदायिक और पारिस्थितिकी उपयोग के लिए संरक्षित हैं। ये मछुआरों की आजीविका का प्रमुख स्रोत हैं और तटीय क्षेत्रों को बाढ़ और कटाव से बचाने में भी अहम भूमिका अदा करते हैं। जैव विविधता के केंद्र सुंदरबन मैंग्रोव में बाघ और अन्य दुर्लभ प्रजातियां निवास करती हैं। इसी के साथ पारंपरिक मत्स्य पालन के लिए ग्रामीण आदिवासी सुंदरबन मैंग्रोव पर निर्भर हैं। ऐसे ही गुजरात में चारागाह, जिसे गोचर भूमि भी कहा जाता है, ग्रामीण समुदायों और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जीवनरेखा की तरह काम करते हैं। ये भूमि सामुदायिक संसाधनों का हिस्सा है और राज्य की पारंपरिक कृषि और पशुधन प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पशुपालक और चरवाहा समुदाय, जैसे मालधारी, अपने मवेशियों को इन चारागाहों में चराते हैं। गुजरात में गिर गाय, भुज कच्छ की भेड़ और गुजराती भैंस जैसी नस्लें चारागाहों पर निर्भर हैं। इसलिए ये स्थानीय लोगों के लिए और भी अहम हो जाते हैं। प्रकृति की नजर से देखें तो इस चराई भूमि से मिट्टी का कटाव रोकने में मदद मिलती है।
भारत में कॉमन्स भूमि, यानी सामुदायिक भूमि की परिभाषा और स्थिति को अभी भी आधिकारिक पहचान नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि इन भूमि संसाधनों का सही प्रबंधन और संरक्षण एक चुनौती बना हुआ है। राज्य कृषि संबंध और भूमि सुधार के अधूरे कार्यों की समिति (2008) ने ग्रामीण सामान्य संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) को परिभाषित किया। इसके अनुसार, सीपीआर “ऐसे संसाधन हैं, जिनके उपयोग के लिए एक पहचान योग्य समुदाय के सभी सदस्यों के अविभाज्य अधिकार हैं।” आसान भाषा में कहें तो सामुदायिक भूमि के संसाधनों का उपयोग हर समुदाय के सदस्य करते हैं और उन्हें कोई भी केवल अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं रख सकता। वैसे, भारत में साल 1998 के बाद से सामुदायिक भूमि के बारे में जानकारी को लेकर बहुत सारे मत और विचार हैं। साल 1998-99 में इन भूमि संसाधनों का आखिरी व्यापक मूल्यांकन किया गया था। तब से अब तक 25 साल बीत चुके है और सार्वजनिक भूमि की वर्तमान स्थिति पर कोई ताजा डेटा तैयार नहीं हुआ है, जो चिंता का विषय है।
भारत में कॉमन्स देश की कुल भूमि का लगभग पांचवां हिस्सा हैं और ये ग्रामीणों की आजीविका और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में बहुत अहम हैं।
वैसे इतिहास में झांके, तो सामुदायिक भूमि को आधिकारिक पहचान देने वाले गंभीर प्रयासों के उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सामुदायिक संसाधनों पर नियंत्रण को कमजोर किया गया। भारत के औपनिवेशिक काल (1858 से 1947 तक) में भूमि का संकुचन और निजी संपत्ति अधिकारों का विस्तार होना शुरू हुआ। इस कारण सार्वजनिक भूमि को निजी भूमि से अलग किया गया और औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने इन पर कब्जा कर लिया। सरकार ने भूमि को राज्य संपत्ति घोषित किया और राजस्व विभाग के तहत इसका अधिग्रहण किया गया। खासतौर पर गांवों के पास की वो भूमि, जो पहले सार्वजनिक संसाधन के रूप में ग्रामवासियों के लिए चराई और दूसरे कामों के लिए उपलब्ध थी, वह अब राज्य की संपत्ति बन गई। इसी दौरान पहले भारतीय वन अधिनियम 1865 के माध्यम से जंगलों और बंजर भूमि को “सुरक्षित जंगलों” के रूप में राज्य संपत्ति घोषित किया गया। इसने आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के जंगलों के अधिकार छीन लिए। जैसे गुजरात की नायक व्यवस्था या दक्षिण भारत की फालो भूमि प्रबंधन व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि, जंगलों को राज्य संपत्ति में बदलना एक प्रकार से कॉमन्स संसाधन का व्यवसायीकरण किए जाने जैसा ही था।
अब अगर न्यायिक दृष्टिकोण से देखें, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 39(बी) कहता है कि, “समाज के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह समाज के सर्वोत्तम भले के लिए काम करे।” यह बात अलग है कि यह अनुच्छेद न्यायिक रूप से लागू नहीं हुआ, पर फिर भी भारत को एक कल्याणकारी राज्य (वेलफ़ेयर स्टेट) बनाने की अवधारणा को मजबूत करने के तौर पर काम आता रहा है। वैसे न्याय की किताब से हटकर सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत भी कहता है कि राज्य को प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण स्वामी नहीं बल्कि केवल एक संरक्षक माना जाता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि राज्य संसाधनों का उपयोग जनहित में करे। सार्वजनिक भूमि की पहचान, उसके उपयोग और दुरुपयोग को लेकर कई मामले न्यायलय तक भी जा चुके है। इसमें सबसे चर्चित मामला साल 2011 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2011 में एक सिविल अपील (जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य) में अपने फैसले में आदेश दिया कि सभी राज्य सरकारों को गांव की आम जमीनों पर अवैध अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने की योजना तैयार करनी चाहिए और गांव के आम इस्तेमाल के लिए इन्हें ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को वापस करना चाहिए।
इस आदेश के संदर्भ में देखें तो सार्वजनिक भूमि प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका को अहम माना जाना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद, पंचायती राज संस्थाओं को गांवों की सार्वजनिक भूमि की रक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत भूमि सुधार, जल प्रबंधन, जल संग्रहण, क्षेत्र विकास, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक संपत्तियों के रखरखाव जैसे विषयों की देखरेख पंचायतों को सौंपी गई है। इसके बावजूद राज्य के राजस्व विभाग और वन विभाग ही सार्वजनिक भूमि प्रबंधन करते हैं। अगर सभी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएं, तो सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और कृषि भूमि का वाणिज्यीकरण जैसे मसले होने ही नहीं चाहिए।
सरकारी आंकड़ों में सामान्य जमीनों के लिए कोई स्पष्ट श्रेणी या समेकित डेटा नहीं है, जिससे इनका सही आकलन मुश्किल हो जाता है। मसलन, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 205 मिलियन एकड़ कॉमन लैंड है, जबकि आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़े इसे 310 मिलियन एकड़ तक बताते हैं। ‘वन’ श्रेणी की अलग-अलग परिभाषाओं ने इन आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर पैदा कर दिया है। खास बात यह है कि भारत में सामान्य जमीनों की आखिरी समीक्षा 1998 में हुई थी। तब से अब तक कोई नया आकलन नहीं हुआ, जिससे इनके मौजूदा हालात को समझना और भी मुश्किल हो गया है। इसी कमी ने कमजोर नीतियों, बढ़ते विवादों और सरकारी निगरानी की कमी को जन्म दिया है।
ये खामियां सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं। इनसे सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन में गहरी प्रशासनिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। मंशा भले अच्छी हो, लेकिन जमीन पर संसाधनों की देखरेख अक्सर खराब ही होती है। इस समस्या को तीन प्रमुख पहलुओं के माध्यम से समझा जा सकता है—
सामूहिक संसाधनों और उन्हें नियंत्रित करने वाले प्रशासनिक निकायों के बीच पैमाने का असंगत होना एक बड़ी समस्या है। उदाहरण के लिए, जिला स्तर के संसाधनों को अक्सर राष्ट्रीय स्तर की प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
उदाहरण – तटीय क्षेत्रों का मामला
भारत के तटीय क्षेत्रों में “तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड)” अधिसूचना के तहत बनाए गए मानचित्र अक्सर गांव-स्तर के विवरणों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे मछुआरा समुदाय अपने तटीय संसाधनों की पहचान और संरक्षण करने में असमर्थ रहता है। राज्य और जिला स्तर पर तैयार तटीय प्रबंधन योजनाओं में समुद्र तट, मछली पकड़ने के गांव और प्रवाल भित्तियों जैसे स्थानीय कारकों की अनदेखी की जाती है।
सामूहिक संसाधनों का प्रबंधन अक्सर ऐसे केंद्रीयकृत निकायों द्वारा किया जाता है, जो स्थानीय परिस्थितियों और समुदायों की वास्तविकताओं से दूर होते हैं।
उदाहरण – वन विभाग और स्थानीय समुदायों के बीच संघर्ष
उदाहरण के तौर पर, वन विभाग का संचालन शहरी केंद्रों से होता है और इसके कर्मचारी, जैसे वन रक्षक, स्थानीय वनों की सुरक्षा में व्यक्तिगत रूप से कम रुचि रखते हैं। “वन अधिकार अधिनियम (एफआरए)” के तहत सामूहिक अधिकारों को मान्यता देने की बजाय, यह अधिनियम अक्सर केवल व्यक्तिगत दावों को प्राथमिकता देता है।
कई सह-प्रबंधन पहलों, जैसे संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, में सामुदायिक संस्थाओं को प्रोत्साहन और स्वायत्तता की कमी रहती है।
उदाहरण – पंचायती राज संस्थाओं की सीमाएं
73वें संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायतों को प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया। हालांकि, इन पंचायतों को न तो पर्याप्त बजटीय आवंटन मिलता है और न ही आवश्यक प्रशासनिक स्वतंत्रता। इसके अलावा, संसाधनों के स्वामित्व और रखरखाव का सही दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की भी कमी है।
अगर समस्या की मूल जड़ पर गौर करें, तो यह शायद इस गहरी मानसिकता में छिपी हो सकती हैं कि स्थानीय समुदाय अपने मामलों को ठीक से नहीं संभाल सकते। इसके परिणामस्वरूप सरकारें या तो इन जमीनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर व्यक्तिगत स्वामित्व में दे देती हैं या फिर इन जमीनों के प्रबंधन को खुद अपने नियंत्रण में ले लेती हैं। ग्राम सभाओं और पंचायतों की भूमिका कमजोर होने से यह स्थिति और बिगड़ती है, जबकि वे कॉमन्स का प्रभावी प्रबंधन कर सकती हैं। आमतौर पर सामूहिक प्रबंधन की आलोचना की जाती है, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि कई बार व्यक्तिगत स्वामित्व या सरकारी नियंत्रण में चलने वाली पहलें भी असफल हो जाती हैं।

झारखंड और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में पेसा अधिनियम (1996) के तहत ग्राम सभाओं को भूमि, वन और जल पर अधिकार दिए गए थे। लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप और खनन गतिविधियों ने ग्राम सभाओं के अधिकार सीमित कर दिए, जिससे स्थानीय समुदायों का स्व-प्रबंधन कमजोर हो गया। इसी तरह कर्नाटक और तमिलनाडु में प्राचीन गांव-आधारित जल प्रबंधन प्रणाली (जैसे ‘कुण्ड’ और ‘एरी सिस्टम’) थी, जिसे स्थानीय समुदाय प्रबंधित करते थे। लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये पारंपरिक व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही हैं।
भारत में सामुदायिक भूमि और संसाधनों के प्रबंधन में कई विशेष समस्याएं सामने आती हैं, जैसे कानूनी अधिकारों की अस्पष्टता और स्थानीय संस्थाओं की उपेक्षा। इन कारणों से दुरुपयोग और अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ती हैं। वहीं राज्य व केंद्र स्तर की संस्थाओं द्वारा बनाई गई नीतियों में अक्सर स्थानीय समुदायों की जरूरतों और उनकी सहभागिता को नजरअंदाज किया जाता है।
आज के समय में सार्वजनिक भूमि की सही पहचान और उसके बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यह न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जरूरी है, बल्कि सामाजिक कल्याण और कमजोर वर्गों की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए भी अनिवार्य है। इसके लिए मजबूत कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता और पारदर्शिता का होना आवश्यक है।
सरकारी नीतियों और न्यायिक आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना और उन्हें जिम्मेदारी देना, इन संसाधनों के साझा उपयोग और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस प्रकार सामुदायिक संसाधनों का कुशल प्रबंधन न केवल एक समृद्ध पर्यावरण, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में भी एक ठोस कदम होगा।
इस लेख को जूही मिश्रा और अंजलि मिश्रा ने तैयार किया है, जिसमें अश्विनी छत्रे के साथ-साथ कांची कोहली और जगदीश राव पुप्पाला के सुझाव शामिल हैं, जो कॉमन ग्राउंड पहल का हिस्सा हैं।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
__
इस वीडियो में मिलिए आशा शिंदे और सना शेख से, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में उमंग महिला उद्योग नामक एक लघु महिला व्यवसाय का नेतृत्व करती हैं। यहां महिलाएं सिलाई और बुनाई से अलग-अलग तरह के उत्पाद तैयार करती हैं। इसमें कई तरह के बैग, स्टेशनरी का सामान, गिफ्ट आइटम और सजावटी चीजें शामिल हैं। आशा और सना बताती हैं कि कैसे वे दिनभर में कच्चा माल खरीदने, प्रोडक्ट डिजाइन करने और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने का काम संभालती हैं, ताकि उनका व्यवसाय प्रगति करता रहे। आशा और सना का उमंग से जुड़ने का सफर अलग-अलग था, लेकिन दोनों में एक बात समान थी- काम के प्रति उनका जुनून और मेहनत का जज्बा। यही वजह है कि आज उमंग एक सफल व्यवसाय बन गया है। काम के साथ-साथ उन्हें अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। उनका सपना है कि एक दिन उमंग हर घर में पहचाना जाने वाला नाम बने, जिससे उनके समुदाय की अन्य महिलाओं को भी स्थायी रोजगार मिले और उनकी जिंदगी बेहतर बन पाए।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—
मेरा नाम गीता है और मैं उत्तराखंड के देहरादून जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हूं। मैं यहीं पली-बड़ी हूं और वर्तमान में अपने पति के साथ रहती हूं। मैं 2022 से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था बुरांस के साथ काम कर रही हूं। यह संस्था उत्तराखंड के दो जिलों—उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों और देहरादून के सुदूर शहरी इलाकों में काम करती है। हम खास तौर पर उन समुदायों और परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराते हैं, जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से कमजोर या वंचित समुदाय से संबंध रखते हैं।
यह मेरी पहली नौकरी है। हालांकि बुरांस के साथ काम शुरू करने के दौरान मेरी पढ़ाई अधूरी थी। तब मैं दसवीं कक्षा तक ही पढ़ी थी। लेकिन संस्था में स्थायी पद के लिए हमारी पढ़ाई पूरी होना आवश्यक है। इसलिए मैंने नौकरी करते हुए ही पत्राचार की मदद से कक्षा 12वीं की परीक्षा दी और अब बैचलर डिग्री पूरी कर रही हूं।
2020 से मैं खुद अवसाद (डिप्रेशन) से जूझ रही हूं। मेरे लिए इसे स्वीकार करना कठिन था, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर अभी भी ढंग से बात नहीं होती। मुझे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परिस्थितियों की कोई जानकारी भी नहीं थी। कोई भी यह नहीं समझ सका कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे पड़ोसियों को लगा कि मुझ पर भूत-प्रेत आ गया है और वे मुझे पुजारी के पास ले गए।
उस समय एक संस्था हमारे इलाके में आती थी। उन्होने मुझे बुरांस के बारे में बताया।फिर वहां की एक सामुदायिक कार्यकर्ता मुझसे जुड़ी और उन्होने मुझे डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में बताया। शुरुआत में मैंने उनकी बात नहीं समझी और मज़ाक में टाल दी। लेकिन अपनी स्थिति को अपनाने और इलाज के सफर ने आज मुझे खुद एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता में बदल दिया है।

बुरांस में काम करने का तरीका अनूठा है। यहां कार्यक्रम और सामुदायिक प्रयास उन लोगों के अनुभवों से प्रेरित होते हैं, जो खुद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, या उनके परिवार का हिस्सा हैं। इसी दृष्टिकोण ने मुझे भी अपनी यात्रा को नए नजरिए से देखने में मदद की। मैंने अवसाद को समझा, उसे स्वीकार किया और फिर उससे निकलने और आगे बढ़ने की राह खोजी।
सुबह 8:00 बजे: समय से उठना मेरे लिए काफी मुश्किल रहा है। लेकिन इस नौकरी ने मेरे जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाने में काफी मदद की। पहले मेरी दिनचर्या बेतरतीब थी—कभी रात भर जागना, कभी दिन में सोना। लेकिन अब हर सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचने की जिम्मेदारी ने मुझे समय के प्रति सचेत बना दिया है। खुद से किए गए छोटे-छोटे वादे— जैसे “8:26 तक ऑफिस पहुंचना है!”—मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। अब देरी होती है, तो मैं परेशान हो जाती हूं।
इस सफर में मेरे पति भी मेरा खूब साथ देते हैं। ऑफिस के लिए देर ना हो जाए, इसलिए वे अक्सर सुबह की जिम्मेदारियां, जैसे चाय और नाश्ता बनाना, खुद ही संभाल लेते हैं। उनका यह सहयोग मेरी दिनचर्या को आसान बनाता है।
सुबह 8.30 बजे: ऑफिस पहुंचते ही मैं सबसे पहले हफ्ते भर की कार्यसूची पर नजर डालती हूं, जिसमें दस्तावेजी काम से लेकर फील्ड विजिट तक की योजनाएं शामिल होती हैं। हमारी साप्ताहिक योजना में विस्तार से बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं को किन क्षेत्रों में जाना है, किन लोगों से मुलाकात करनी है, और किन मामलों में फॉलो-अप करना है। साथ ही, हम उन नए इलाकों के लिए भी रणनीति बनाते हैं, जहां हमें अपना काम शुरू करना है।
आजकल साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच प्रवासी मजदूरों का विश्वास जीतना और भी मुश्किल हो जाता है।
मेरा ज़्यादातर काम फ़ील्ड में ही है। मैं जिस इलाके में काम करती हूं, वह एक औद्योगिक क्षेत्र है, जहां अधिकतर लोग प्रवासी मजदूर हैं और अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। वे नए लोगों से बात करने में भी झिझकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हैं। आजकल साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच उनका विश्वास जीतना और भी मुश्किल हो जाता है।
लोगों से बातचीत करना आसान नहीं होता—वे ‘टेंशन’ (तनाव) शब्द से परिचित हैं और इसे समझते भी हैं, लेकिन जैसे ही मानसिक बीमारी का ज़िक्र आता है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है, “क्या आप मुझे पागल कह रहे हैं?”
मैं उनके इस दृष्टिकोण को समझती हूं, क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी। डिप्रेशन के बारे में मेरी समझ एक विज्ञापन से बनी थी, जिसमें दिखाया गया था कि इसमे लोग अपने दरवाजे बंद रखते हैं और बार-बार एक ही आदत दोहराते हैं । मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता।
मेरी भी यही राय थी कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या का मतलब है कि मैं पागल हूं और मुझे किसी अस्पताल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं गलत थी। जब मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने मुझे अस्पताल जाने की सलाह दी, तो मेरे मन में डर बैठ गया। मुझे लगा कि वे मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे भर्ती कर लेंगे, पागल करार दे देंगे या मुझ पर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी आज़माएंगे। इस डर से मैंने डॉक्टर से सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे नींद नहीं आती और सिर दर्द होता है। उन्होंने दवाइयां दी, लेकिन मैंने उन्हें हफ्तों तक नहीं लिया। मुझे डर था कि कहीं ये दवाइयां सच में मुझे पागल न बना दें।
जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता फॉलो-अप के लिए आते, तो मैं झूठ बोल देती कि मैंने दवाइयां ली हैं, लेकिन वे असर नहीं कर रही। एक बार वो मुझे बिना बताए मिलने आ गयी, तो उन्होंने मेरी ज्यों की त्यों रखी हुई दवाइयों को देख लिया। उन्होंने बिना किसी दबाव के सुझाव दिया कि मैं आधी खुराक से शुरुआत कर सकती हूं। आखिरकार, मैंने दवाइयां लेना शुरू किया। दो-तीन महीने तक दवा लेने के बावजूद, इस दौरान मेरे मन में लगातार नकारात्मक विचार आते रहे। मैं सोचती थी कि कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हो रही?
करीब सात-आठ महीने बाद, मुझे बुरांस से जुड़ने का मौका मिला। यहीं आकर मुझे पहली बार अवसाद और उसके लक्षणों को सही मायने में समझने का अवसर मिला। तब जाकर मैंने जाना कि यह कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक सामान्य बीमारी है,जिसका इलाज संभव है। बस इसे स्वीकार करने की जरूरत होती है।
इस अनुभव से मुझे एहसास हुआ कि मानसिक परिस्थितियों के बारे में जागरूकता और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ भरोसेमंद रिश्ता बीमारी को स्वीकार करने के लिए कितना ज़रूरी है। अन्यथा, लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं- ठीक वैसे ही जैसे मैंने नहीं किया। इसलिए मैं पहले समुदाय के साथ विश्वास का रिश्ता बनाती हूं।
हम लोगों से यह कहने के बजाय, कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है, पहले उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक वैसे ही देखा जाना चाहिए जैसे शारीरिक स्वास्थ्य को। अगर वे बुखार होने पर दवाई लेते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद लेने में हिचक क्यों? कुछ मामलों में मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती हूं, और जब जरूरत पड़ती है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक-दूसरे का सहयोग करके हल निकालते हैं।
दोपहर 1:00 बजे: सुबह काम शुरू करने के बाद दोपहर के खाने का कोई तय समय नहीं रहता। अगर समुदाय में बातचीत और मिलने का काम पूरा हो जाता है, तो ऑफिस आकर खाना खा लेती हूं। पर कई बार यह मौका नहीं मिल पाता। इस दौरान ऑफिस में कुछ कागजी काम भी निपटाने होते हैं। जैसे समुदाय में जिन लोगों से बात हुई है उनका ब्यौरा लिखना, अगर पुराने केस में अपडेट हुई है तो उसकी प्रगति रिपोर्ट बनाना, गंभीर मामलों को प्राथमिकता सूची में शामिल करना।
इलाके की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां समुदाय के लिए और भी ज़्यादा मानसिक तनाव पैदा करती हैं। उनसे बात करने पर मुझे एहसास हुआ कि उन्हें लगता है कि वे इलाज के लायक नहीं हैं।उन्हें कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। अक्सर मैं एक ही परिवार के कई लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते देखती हूं। ऐसे में एक व्यक्ति हमें दूसरे व्यक्ति से भी जोड़ता है, कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है।
संगठन की ओर से मुझे नेपाल के काठमांडू शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में जाने का मौका मिल चुका है। यह मेरी पहली हवाई यात्रा थी।
महिलाएं आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को अपनाने के लिए ज्यादा तैयार होती हैं। लेकिन पुरुषों से इस विषय पर बात करना बेहद मुश्किल होता है। मेरे अनुभव में, केवल दो-तीन प्रतिशत पुरुष ही यह स्वीकार करते हैं कि वे किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं। नशीली दवाओं के उपयोग या घरेलू हिंसा के मामलों में भी वे यह मानने से इनकार करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य इनका एक मूल कारण हो सकता है। जागरूकता की कमी और सही जानकारी न होने की वजह से यह समस्या और जटिल हो जाती है।
अपने अनुभवों के कारण मैं लोगों की बातों में छिपे संकेत जल्दी समझने लगी हूं। जब कोई कहता है कि वो “बहुत सोच रहे हैं,” तो मुझे एहसास हो जाता है कि वे किस मानसिक दबाव से गुजर रहे होंगे।शायद वैसा ही, जैसा मैंने महसूस किया था। जब कोई सिर दर्द की शिकायत करता है, तो मैं समझ सकती हूं कि यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक परेशानी का संकेत भी हो सकता है, जिसे वे छुपा रहे हैं।
बुरांस के पास एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता टूलकिट है, जो हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्तियों की जांच करने में मदद करती है। हमें महीने में दो-तीन बार प्रशिक्षित किया जाता है और किसी भी नई नीति के बारे में सूचित किया जाता है।इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमें समुदायों के साथ बातचीत करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
यह मेरे लिए भी बहुत मददगार है। अपने काम ने मुझे न केवल लोगों की मदद करने का तरीका सिखाया, बल्कि अपनी भावनाओं को संतुलित रखना भी सिखाया है। पहले, जब मैं किसी गंभीर स्थिति का सामना करती थी, तो घबरा जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे मैंने समझा कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान निकल सकता है। अब जब मैं समुदाय में लोगों से मिलती हूं, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करती हूं। इससे न सिर्फ उनकी बातें बेहतर समझ में आती हैं, बल्कि हमारे बीच विश्वास का रिश्ता भी मजबूत होता है। आज इस काम की बदौलत समुदाय में मेरी अपनी एक पहचान बन गयी है।
हालांकि पहले ऐसा नहीं था। नौकरी के शुरूआती दिनों में समुदाय के लोगों के अलावा स्थानीय सरकारी अधिकारियों से बातचीत करने में काफी मुश्किल होती थी। कई बार मुझे अपने कपड़ों और बोलने के तरीके को लेकर झिझक भी महसूस हुई। फिर काम करते-करते मैंने सही ढंग से बात करना और अपनी बात रखना, दोनों सीखा। इसके साथ ही मेरे व्यवहार और पहनावे में भी बदलाव आया।
सालों बाद अब मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अधिकारी अथवा समुदाय के लोगों से पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर पाती हूं। मेरे पास उनके सवालों के जवाब होते हैं।
इतना ही नहीं, हम अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाते हैं। जैसे संगठन की ओर से मुझे नेपाल के काठमांडू शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में जाने का मौका मिल चुका है। यह मेरी पहली हवाई यात्रा थी और मैं अकेली थी। कार्यक्रम से पहले मैं घबरा रही थी, लेकिन मैंने खुद से कहा कि आखिर मैं अपनी कहानी और अनुभव साझा करने के लिए इतनी दूर आयी हूं। खुद को समझाया कि अगर मैंने यह नहीं किया, तो बहुत से लोग जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उस दिन मैंने सैकड़ों लोगों के सामने पहली बार मंच पर मानसिक स्वास्थ्य विषय पर बात की।

शाम 5:00 बजे: कभी-कभी काम में देरी हो जाती है, पर ज्यादातर शाम 5 बजे मेरा काम खत्म हो जाता है। घर पास होने के चलते मैं 10 मिनट में पहुंच जाती हूं। फिर कुछ देर आराम करने के बाद घर के कामों को निपटाती हूं। इस दौरान टीवी या मोबाइल पर गाने लगा लेती हूं। इससे वक्त कब गुजरता है, पता ही नहीं चलता और मन भी शांत हो जाता है।
वैसे तो पूरी कोशिश रहती है कि मेरे काम का असर घर और निजी जीवन पर ना हो, पर फिर भी कुछ बातें जहन में रह जाती हैं तो उन्हें मैं अपने पति के साथ साझा करती हूं।
शुरूआत में जब लोगों से उनके अनुभव सुनने शुरू किए, तो वे मन पर काफी असर डालते थे। पर सालों से समुदाय में एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने का नतीजा है कि अब लोगों की कहानियां मुझे पहले जैसी गहराई से प्रभावित नहीं करती। मैं सीख गयी हूं कि अपने काम और भावनाओं के बीच एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मैं अधिकांश यह कोशिश करती हूं कि जो कुछ भी मैं समुदाय में देखती और अनुभव करती हूं, वह मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर असर न डाले। क्योंकि किसी और की मदद करने की प्रक्रिया में हमें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई घटना मुझे प्रभावित करती है, तो मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे सहकर्मी हैं जिनसे मैं खुलकर बात कर सकती हूं।
जब मैं अकेली थी, तो यह सब बहुत मुश्किल था। पर अब पति मेरी बातों को ध्यान से सुनते और समझते हैं। मेरा परिवार भी है, जिसमें मेरे मां-बाप और भाई-बहन हैं। मुश्किल समय में उन्होने मेरा साथ नहीं दिया था, इसलिए मुझे उनकी बहुत कमी महसूस हुई। इससे मुझे परिवार के साथ की अहमियत समझ आयी।
जब कोई यह महसूस करता है कि उन्हें मानसिक विकार या बीमारी है, तो सबसे पहले वे खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है कि वे मरीजों और उनके परिवारों के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम करें। इसी से उन्हें महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं औरउनके अच्छे-बुरे समय में उनका परिवार साथ है। यह विश्वास और समर्थन ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को ताकत देता है और उनके इलाज की प्रक्रिया को आसान बनाता है।
जैसा कि आईडीआर को बताया गया।
–
मेरा नाम पप्पू कंवर है और मैं बाड़मेर, राजस्थान में रहती हूं। मैं एक समाजसेवी और कार्यकर्ता हूं। बाड़मेर, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ एक क्षेत्र है। यहां जातिवाद और महिलाओं के खिलाफ हिंसा व्यापक रूप से फैले हैं जो हमारे काम को खासतौर पर कठिन बनाते हैं। बीते कई सालों से, मैं महिलाओं और विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रही हूं और चुनौतियों के बावजूद कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूं।
मैंने ‘आस्था महिला संगठन’ नाम का एक महिला समूह बनाया है जिसमें 250 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमने संगठन के तहत कई महिला समूह बनाए हैं। ये मिलकर उन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को बढ़ने से पहले ही हल करने की कोशिश करते हैं जिनका सामना महिलाओं के परिवार कर रहे होते हैं। साथ ही, महिलाएं अब स्थानीय समस्याओं को सुलझाने और तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में एक घटना में, एक नशे में धुत आदमी अपनी पत्नी और मां को नुकसान पहुंचाने वाला था। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया जिन्होंने समय पर आकर हस्तक्षेप किया। हालांकि हम ज़्यादातर समस्याओं का समाधान खुद कर लेते हैं, लेकिन गंभीर परिस्थितियों में पुलिस का सहयोग बेहद जरूरी होता है। यह संगठन ग्रामीण बाड़मेर और इसके आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है।
साल 2003 से, मैं जिला दिव्यांग अधिकार मंच से भी जुड़ी हुई हूं। इस मंच ने विकलांग समुदाय को जिला और राज्य स्तर पर अपनी आवाज उठाने में मदद की है। यह संगठन विकलांग लोगों को बस-रेलवे पास जैसे जरूरी दस्तावेज दिलाने, और उपकरण व अन्य सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है। मैं स्वयं भी शारीरिक रूप से विकलांग हूं, और यह मेरे द्वारा विकलांगों के अधिकारों के लिए की जाने वाली हिमायत का आधार है।
सुबह 6:00 बजे: जब मैं जागती हूं, तो सबसे पहले भगवान से एक अच्छे दिन की प्रार्थना करती हूं। अगर मैंने पिछली रात अपने दिन का शेड्यूल नहीं बनाया होता है तो मैं उसे सुबह बनाती हूं। तैयार होने और अपने घरेलू काम निपटाने के बाद, मैं आमतौर पर बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रीय स्थलों पर जाती हूं। वहां, मैं उन लोगों से मिलती हूं जो सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में देरी का सामना कर रहे हैं, घरेलू हिंसा झेल रहे हैं, या विधवा महिलाएं हैं जिनको समाज ने अलग-थलग कर दिया है – इन समस्याओं की सूची अंतहीन है।
मैं 2002 से बाड़मेर में विकलांग समुदाय के साथ काम कर रही हूं—उन्हें संगठित कर रही हूं, उनकी समस्याओं को लेकर जागरूकता बढ़ा रही हूं, और उन्हें पेंशन, विकलांगता प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद कर रही हूं। शुरुआत में लोग साथ आने से हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें समाज के तानों और आलोचनाओं का डर था। कई बार गैर-विकलांग लोग हमें घूरते थे और भद्दी टिप्पणियां करते थे। लेकिन जैसे-जैसे हमने मिलना और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना शुरू किया, वैसे-वैसे हमने समाज की परवाह करना कम कर दिया। अब हम खुलकर एक-दूसरे से मिलते हैं, अपनी समस्याएं साझा करते हैं और बिना किसी डर के एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें।
यह एक लंबा और दिलचस्प सफर रहा है। साल 1997 में, मेरी एक सर्जरी हुई थी ताकि मैं चल सकूं। सर्जरी के बाद मुझे पूरी तरह से चलना सीखने में एक साल लग गया। यह बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरी मां हमेशा कहतीं, “तुम कर सकोगी, हार मत मानो! लोग जो चाहे कहें, हम तुम्हारी ताकत हैं।” उनकी बातें मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही हैं और मुझे यह एहसास दिलाया कि जैसे मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वैसे ही दूसरों को भी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें।
इन सालों में, हमने एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है और अब सरकार के अधिकारी और पुलिस भी हमारे साथ काम करते हैं।
जब मैंने चलना सीख लिया तो 2003 में मैंने एक एसटीडी बूथ पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में, मुझे परिवार के बाहर किसी से भी सामान्य बातचीत करने का तरीका नहीं पता था। लेकिन समय के साथ, मैंने काम करते हुए सुनकर और बात करके यह सीख लिया। धीरे-धीरे लोग अपनी समस्याएं मेरे साथ साझा करने लगे जिससे मुझे एहसास हुआ कि मैं समाज में किसी न किसी तरीके से योगदान कर सकती हूं। मैंने सोचा “भले ही मैं ज्यादा न कर सकूं, लेकिन मैं कम से कम बुनियादी साक्षरता सिखा सकती हूं।” पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण है – यह लोगों को दुनिया को समझने में मदद करती है।
मैंने समुदाय की महिलाओं से पूछा कि क्या वे पढ़ना-लिखना सीखना चाहेंगी और उन्होंने इसके लिए उत्साह दिखाया। कई महिलाएं पढ़ाई करना चाहती थीं लेकिन कई कारणों से उन्हें इजाजत नहीं थी। इसलिए, मैंने 2005 में एक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जिसमें मैं एक बार में 10–15 महिलाओं को लिखना-पढ़ना सिखाती थी। सिर्फ 15 दिनों में, मैं उन्हें बुनियादी ज्ञान दे पाई। समय के साथ, मैंने करीब 100 महिलाओं को पढ़ना सिखाया। इस सफलता ने मुझे महिलाओं की आय और कमाई की क्षमता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। मैंने उन्हें सिलाई सिखाने का काम शुरू किया और मुफ्त में प्रशिक्षण दिया। मैंने चार बैचों की महिलाओं को प्रशिक्षित किया और अगर उन्हें रात के किसी भी वक्त मदद की जरूरत होती तो मैं उनके लिए वहां रहने की कोशिश करती और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देती। आज, इनमें से कई महिलाएं छोटे सिलाई केंद्र खोल चुकी हैं या दुकानों पर काम करती हैं और अपनी आजीविका कमा रही हैं। यह मुझे बहुत खुशी देती है।

दोपहर 1:00 बजे: मैं आमतौर पर, दोपहर एक बजे के आसपास खाना खाने के लिए रूकती हूं। मेरा काम हर दिन मेरे शेड्यूल के अनुसार बदलता रहता है, लंच के बाद मैं अक्सर दोपहर का बाकी समय क्षेत्र में बिताती हूं – महिला समूहों से मिलती हूं या अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर काम करती हूं।
इस क्षेत्र में हमें जो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, वे कई रूपों में होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले, मुझे अपने मोहल्ले की सड़क की खराब हालत के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा था। मेरी ट्रायसाइकल इस सड़क पर ठीक से नहीं चल पा रही थी। हर दिन काम के बाद मुझे अपनी मां को फोन करके मदद लेनी पड़ती थी ताकि वह मुझे सड़क पार करने में मदद करें। मेरी मां और एक या दो अन्य महिलाएं मुझे घर तक छोड़ने आती थीं। इस क्षेत्र में हर विकलांग व्यक्ति को इस समस्या का सामना करना पड़ता था लेकिन कोई भी इस बारे में आवाज उठाने से डरता था। एक दिन, हम आठ लोग एकजुट हुए और हमारे वार्ड सदस्य के पास गए। हमारी सामूहिक आवाज के कारण, 10-15 दिनों के भीतर सड़क को फिर से बना दिया गया।
मेरे काम का सबसे कठिन हिस्सा विकलांग लोगों की मदद करना है क्योंकि उनमें से कई पूरी तरह से अपने परिवारों पर निर्भर होते हैं।
इन सालों में, हमने एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। अब सरकार के अधिकारी और पुलिस भी हमारे साथ काम करते हैं। शुरुआत में, हमें समस्याओं का समाधान करने का तरीका नहीं पता था लेकिन अब हमने एक सिस्टम विकसित कर लिया है। जब भी कोई नई सरकारी योजना आती है तो हम तुरंत उसकी जानकारी अपने व्हाट्सएप समूहों में साझा करते हैं।
हमारे लिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सभी समुदायों के साथ काम करते हैं, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना। हमारी एक मुख्य प्राथमिकता अपने आसपास की असहिष्णुता को कम करना है क्योंकि कोई भी आर्थिक या आजीविका से जुड़ी समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक लोग सामाजिक बदलाव के लिए एकजुट नहीं होते हैं। हमारे साथ काम करने वाली कई महिलाएं इसे समझती हैं और जातिवादी प्रथाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अब महिला समूह एक साथ खाना खाती हैं जो पहले बाड़मेर में जातिवाद के कारण कल्पना से परे था। मैंने यह बदलाव खुद देखा है।

शाम 4:00 बजे: जब दिन ख़त्म होने लगता है तो मैं आमतौर पर कार्यालय जाती हूं। कुछ काम करती हूं, जो भी बिल चुकाने होते हैं, उन्हें प्रोसेस करती हूं, और विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने या लेने के लिए जाती हूं।
जब मैं कोरो इंडिया में एक फेलो थी तो मैंने कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया जिसमें वी द पीपल अभियान के जरिए संविधानिक मूल्यों और अधिकारों पर भी प्रशिक्षण था। इन कार्यक्रमों ने मुझे महिलाओं और विकलांग लोगों के अधिकारों और योजनाओं के लिए संघर्ष करने की समझ दी। डिजिटल एंपावरमेंट फाउंडेशन के डिजिटल सार्थक कार्यक्रम ने मुझे डिजिटल तकनीक का सही उपयोग करना सिखाया। मैंने कंप्यूटर और स्मार्टफोन का उपयोग करना शुरू किया, जैसे बिजली के बिलों का भुगतान करना और सरकारी लाभ के लिए फॉर्म भरना, और धीरे-धीरे मैंने समुदाय की कई महिलाओं को इन डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया। अब, इस क्षेत्र की कई महिलाएं फोन का इस्तेमाल कर सकती हैं, और कुछ महिलाएं सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का इस्तेमाल करके अपने छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देती हैं। बहुत सी महिलाएं वीडियो देखकर नए कौशल, जैसे खाना पकाना, सीख रही हैं।
हालांकि यह बेहद जरूरी है, लेकिन मेरे काम का सबसे कठिन हिस्सा विकलांग लोगों की मदद करना है क्योंकि उनमें से कई पूरी तरह से अपने परिवारों पर निर्भर होते हैं। इस वजह यह भी है कि उन्हें वैकल्पिक तरीकों के बारे में मालूम नहीं होता है। फोरम के एक सदस्य को खुद से चलने में असमर्थता है और उसे लगातार देखभाल की जरूरत है। हम उसे एक पुनर्वास केंद्र ले गए जहां उसने कंप्यूटर कौशल आसानी से सीखे क्योंकि वह बहुत तेज था। अब, वह इन कौशलों का उपयोग करके आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रहा है। यह अनुभव हमें उम्मीद देता है कि सही समर्थन और अवसरों के साथ और अधिक जिंदगियां बदली जा सकती हैं।
शाम 7:00 बजे: मैं आमतौर पर सात बजे घर पहुंचती हूं लेकिन कभी-कभी मैं काफी देर से पहुंचती हूं। हर रात, मैं अपने दिन के काम की समीक्षा करती हूं। मैं यह सोचती हूं कि क्या अच्छा हुआ और क्या नहीं, और अपने विचारों को डायरी में लिखती हूं। इससे मुझे अपनी प्रगति का आकलन करने में मदद मिलती है और अगले दिन की योजना बनाने में सहूलियत होती है। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि मैं अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करूं और जो काम पूरा करने हैं, उन पर विचार करूं। फुर्सत के समय में, मुझे भजन सुनना पसंद है।
मेरे काम के शुरुआती दिनों में, मुझे बहुत सारे संदेह का सामना करना पड़ा था खासकर क्योंकि मैं एक महिला हूं और शारीरिक बाधा से जूझ रही हूं। लोग अक्सर कहते थे, “वह क्या कर सकती है? वह तो विकलांग है।” अफसोस की बात है कि यह एक वास्तविकता है जिसका सामना हम में से कई लोग रोज करते हैं। लेकिन मैंने उन टिप्पणियों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मेरी मां ने एक बार मुझे याद दिलाया था कि सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होतीं-हर कोई अलग होता है और उसकी अपनी यात्रा होती है। मेरे सामर्थ्य में विश्वास ने मुझे मेरे काम में कठिनाइयों का सामना करने की ताकत दी।
जैसा कि आईडीआर को बताया गया।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—
मेरा नाम प्रीति मिश्रा है और मैं क्वेस्ट अलायंस नाम की संस्था से जुड़ी हूं। मैं झारखंड के जमशेदपुर में रहती हूं। हमारा परिवार बिहार से रांची शिफ्ट हुआ था इसलिए हमारी शुरुआती परवरिश रांची में ही हुई। हम 7 बहनें और एक भाई हैं। मेरे माता-पिता दोनों ही अध्यापन क्षेत्र में रहे थे तो इसलिए शिक्षा के प्रति उनसे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। मेरे पिता हमेशा से ही मेरे आदर्श रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह संघर्ष करते हुए बिना समाज की परवाह किये हमें अपनी जिंदगी जीने दी, ऐसा करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है।
पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मेरी मां को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मेरे माता-पिता को हमेशा लगता था कि लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे आगे चलकर अपने पांव पर खड़ी हो सकें। लेकिन ये सब मेरे माता-पिता के लिए इतना आसान नहीं रहा क्योंकि आसपास के लोगों का भी दबाव रहता था कि इतनी सारी लड़कियां हैं तो इन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं, समय से शादी करके इनको ससुराल भेज देना चाहिए।
लेकिन बावजूद इसके मेरे माता-पिता ने इन सब बातों को कोई महत्व नहीं दिया और यही वजह है कि मैं और मेरी सभी बहनें आज नौकरी कर रहीं हैं और अच्छा कमा रही हैं। आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई जहां मैंने अपना एमबीए करने के साथ-साथ पीजी डिप्लोमा भी किया। तीन साल नौकरी करने के बाद कुछ पारिवारिक कारणों से मुझे रांची वापस आना पड़ा। मैंने रांची में रिसर्च स्कॉलर के रूप में तथा नाबार्ड के साथ कन्सलटेंट के तौर पर लगभग आठ सालों तक काम किया।
पूर्वी सिंहभूम जिले में क्वेस्ट अलायंस संस्था के साथ काम करते हुए मुझे तीन वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। हमारी संस्था झारखंड में स्कूली शिक्षा में सोशल इमोशनल लर्निंग यानि सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा (सेल) पर काम करती है। इस कार्यक्रम में मैं शिक्षकों को सेल पाठ्यक्रम को लागू करने में मदद करती हूं। इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उनका समाधान करना है ताकि बच्चे न केवल किसी भय के बिना सीख सकें बल्कि सीखने के साथ अपनी हर बात भी साझा कर सकें। इसी के चलते मुझे बच्चों के अनुभवों को जानने का मौका मिलता है। भावनात्मक शिक्षा पर आधारित मेरा यह कार्य मुझे भी समय के साथ धैर्य और सहानुभूति जैसे मूल्यों को और नजदीकी से समझने का मौका दे रहा है।
6.00 बजे: मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठ जाती हूं। उठने के बाद मैं घर वालों के लिए चाय बनाने के साथ सुबह के लिए नाश्ते की तैयारी करती हूं। हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे पति के अलावा उनके दो और भाई हैं। सभी की शादी हो चुकी है। सच कहूं तो, संयुक्त परिवार में किस तरह रहा जाता है यह संतुलन बिठाने में मुझे समय लगा। मैं आज़ाद ख्यालों वाली थी और मेरे पिता को यकीन नहीं था कि मैं कभी भी सामान्य विवाहित जीवन और उसकी कई ज़िम्मेदारियों में फ़िट हो भी पाऊंगी या नहीं।
मेरी दो साल की बेटी है। अपनी बेटी को मैं आठ बजे तक तैयार कर देती हूं। मेरे पति पेशे से वकील हैं और इसके अलावा वे एक इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट में मैथ की कोचिंग भी देते हैं।
एक मजेदार बात बताऊं?
मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से मैंने अपनी शादी के लिए आए 30-35 लड़कों को रिजेक्ट कर दिया था। अंत में, परेशान होकर मेरे पिता को मुझसे कहना पड़ा कि ये रिश्ता अब तेरे लिए आखिरी है और अब तुझे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तब जाकर मैं शादी के लिए राजी हुई। मुझे मेरे पति का बहुत सपोर्ट रहता है। जब भी मुझे कहीं जल्दी बाहर जाना होता है या फिर कोई टीम विजिट पर आती है, तो उस दौरान भी वे बेटी को तैयार करने से लेकर उसके खाने तक हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं हमेशा से ही ऐसी सरकारी नौकरी करना चाहती थी जहां मैं नीतिगत निर्णय ले सकूं और मेरे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी हो, ये सब सोचकर मैं आज भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती रहती हूं।
9.00 बजे: अपनी बेटी और घर वालों को नाश्ता कराने के बाद मैं पूर्वी सिंहभूम जिले के अपने स्कूल के लिए निकल जाती हूं। स्कूल पहुंचने पर मैं शिक्षकों व छात्राओं से मिलती हूं और मॉर्निंग असेंबली में शामिल होती हूं। मैं सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली में कोई गतिविधि कराती हूं जिससे बच्चों को मजा आए। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे का जन्मदिन है तो उसको कुछ खास तरीके से मिलकर मनाते हैं जिससे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं।
ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह का व्यक्ति का पेशा होता है, उसका कहीं न कहीं तो उस पर प्रभाव पड़ता ही है। जब मैंने सोशल इमोशनल लर्निंग पर काम करना शुरू किया तो मुझे काफी मुश्किल आईं और समझने में समय लगा क्योंकि पहले मेरा व्यवहार खुद भी कुछ ऐसा था कि हर समय गुस्सा करना तथा बात-बात पर बहस कर देती थी। उस समय मेरे मन में यही बात थी कि मैं बच्चों को सेल के प्रति किस तरह प्रोत्साहित कर पाऊंगी।
मुझे शिक्षा पर काम करना हमेशा ही बेहद पसंद रहा है। जब मैं इस संस्था में आई तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि तुम्हें बच्चों एवं शिक्षकों के साथ सोशल इमोशनल लर्निंग (सेल) को लेकर काम करना होगा। वहां मैंने खुद ही यह शब्द पहली बार सुना था। पहली बार संस्था में मुझे चार दिवसीय सोशल इमोशनल लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। इस प्रशिक्षण में इस बात पर ज्यादा फोकस था कि हम एक इंसान के तौर पर क्या महसूस करते हैं, जब हमें खुशी और दुख होता है तो कैसे हमें यह एक दूसरे के साथ साझा करनी चाहिए। यानि प्रशिक्षण, एक तरह से कहें तो न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी अच्छे से समझते हुए भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके पर केंद्रित था। मैंने इस तरह का अनुभव पहले कभी नहीं किया था जहां हम किसी पाठ्यक्रम के बजाय गतिविधियों के माध्यम से भावनाओं पर अधिक ध्यान दे रहे थे।
तब मुझे समझ में आया कि सोशल इमोशनल लर्निंग में भावनात्मक जुड़ाव पर इसलिए ज़ोर दिया जाता है क्योंकि जब हम खुद इन चीजों पर काम करेंगे तभी बच्चे भी हमसे ज्यादा खुलकर अपनी हर बात साझा कर पाएंगे।

12.00 बजे: स्कूल में हर रोज का तय शेड्यूल होता है कि हर दिन बच्चों के साथ सेल कार्यक्रम में कौन-कौन सी गतिविधियां करवानी हैं। इसको लेकर मैं पहले शिक्षकों से चर्चा करती हूं ताकि सेल को लेकर उनकी चुनौतियों को समझ सकूं। जहां तक सेल कार्यक्रम में शिक्षकों के चयन की बात है तो उसे एक प्रक्रिया के अंतर्गत किया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि इस कार्यक्रम में ऐसे शिक्षकों का चयन किया जाए जो बच्चों के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं और बच्चे भी उनके साथ बेहिचक अपनी बातें साझा करते हों। इसके बाद शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया है जिसमें मुख्य रूप से उन गतिविधियों पर फोकस रहता है जिनके जरिए शिक्षक खुद भावनात्मक शिक्षा को और गहराई से समझ पाएं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक कक्षा में सेल से जुड़ी गतिविधियां कराते हैं।
कक्षा में जाकर ये देखती हूं कि आज बच्चों का हाव-भाव कैसा है। इसके बाद कक्षा में छोटी-छोटी चेक-इन और चेक-आउट गतिविधियां करती हूं। इसमें बच्चे से पूछा जाता है कि आप आज के दिन को किस रंग से जोड़कर देख रहे हैं या फिर आज आपको क्या खाने का मन है, इत्यादि। उनके मूड के अनुसार मैं उनके साथ कोई हंसी-मज़ाक वाली गतिविधि कराती हूं ताकि वे और अच्छा महसूस करें।
सेल के अंतर्गत कक्षा में बच्चों को अपनी समस्यायें या फिर जो वे महसूस कर रहे हैं, उन्हें लिखने को दिया जाता है। इसमें वे घर या फिर उनसे जुड़ी ऐसी कोई समस्या साझा करते हैं। इसकी वजह यह है कि सब बच्चे बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते, इसलिए उन्हें लिखने के लिए कहा जाता है। अगर कोई बच्चा नहीं लिखता है तो उसे भी ध्यान में रखा जाता है ताकि उस पर और काम किया जा सके। बच्चे जब अपनी समस्यायें लिखकर हमें देते हैं तो हम उन सभी को पढ़ते हैं। इसके बाद अध्यापकों और वार्डन के साथ प्रत्येक बच्चे की समस्या पर चर्चा होती है और उसके अनुसार उसका समाधान करते हैं।
ज्यादातर अभिभावक आर्थिक मुश्किलों व समाज के दबाव के चलते अपनी बच्चियों की शादी, पढ़ाई के दौरान ही करा देते हैं।
हमारे स्कूल में आठवीं कक्षा की एक छात्रा है। अपनी आयु के अनुसार ज्यादा बड़ी दिखने की वजह से बच्चे उसको चिढ़ाते थे। अपने चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से वह किसी की भी बात नहीं मानती थी। यहां तक कि सेल गतिविधि में भी वह कभी भाग नहीं लेती थी लेकिन धीरे-धीरे बाकी बच्चों को देखकर उसकी भी रुचि बढ़ी और एक समय ऐसा आया कि वह दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल सामान्य हो गई। आज वो बच्ची दसवीं में पढ़ती है और लगातार उसके साथ बात करने रहने के कारण बेहिचक खुलकर अपनी बात कह पाती है।
अब समय बहुत बदल चुका है और जानकारी के बहुत सारे साधन हो गए हैं। ऐसे में और भी ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों के उनके ज्यादातर सवालों का जवाब मिल पाए।
मैं आज भी अपने आसपास देखती हूं तो ज्यादातर अभिभावक आर्थिक मुश्किलों व समाज के दबाव के चलते अपनी बच्चियों की शादी, पढ़ाई के दौरान ही करा देते हैं। एक बार पास के ही गांव में सुनने को मिला कि हमारे स्कूल की एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना जबरन कराई जा रही है। मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर वहां जाने का निर्णय लिया। हम लोग जैसे ही उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे, वह लड़की खुद से शादी के बीच से भागकर हमें रास्ते में ही मिल गई। उसने हमसे अनुरोध किया कि हम उसकी शादी किसी भी तरह रुकवा दें। हमने पुलिस के सहयोग से उसकी शादी रुकवा दी। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि काश मेरे पास कोई सुपरपॉवर होती जिससे मैं लोगों के अंदर की नकारात्मकता मिटा सकती तो मैं ऐसा कर डालती।
शाम 3.00 बजे: आमतौर पर 3 बजे तक मेरा स्कूल का कार्य समाप्त हो जाता है। मुझे अलग-अलग स्कूलों में जाना होता है तो कई बार देर से भी घर पहुंचती हूं। सेल पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली कहानियां अक्सर लोगों के वास्तविक अनुभवों से होती हैं या इस तरह से लिखी जाती हैं कि छात्र कहानियों में खुद को जोड़कर देख सकें। रास्ते में आते समय भी मैं यही सोचती हूं कि आज क्या नया किया, क्या मजेदार था, कहां और सुधार हो सकता था। ये हमारे काम के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक हम खुद से अपने विचारों में खुलापन नहीं ला पाएंगे, तब तक हम किसी और के जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं खुद दिनभर जब स्कूल में बच्चियों के साथ अलग-अलग गतिविधियों के जरिए उनके मन में चल रही दुविधाओं, समस्याओं का हल निकाल पाती हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अपने अंदर आए भावनात्मक बदलाव से मैं खुद भी कई बार हैरान होती हूं क्योंकि मेरा व्यवहार शायद कभी इस तरह का नहीं रहा था।
शाम 4:00 बजे: घर पहुंचने के बाद, मैं अपनी बेटी के साथ समय बिताती हूं। वह अभी बहुत छोटी है, लेकिन जल्द ही वह ऐसी शिक्षा व्यवस्था में शामिल होगी जहां उन्हें भी आगे चलकर सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं इस बात से खुश हूं। यह हमारे समय जैसा नहीं है जहां शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित होती थी। बेटी के साथ समय बिताने और पूजा पाठ करने के बाद रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मैं और मेरी देवरानियां आठ बजे तक खाना तैयार कर लेती हैं। ससुराल के हर तरह के सहयोग की वजह से ही मैं अपना काम और बेहतर कर पाती हूं। मेरे पति आमतौर पर रात को 10 बजे तक घर पहुंचते हैं। खाना खाने के बाद हम दोनों पूरे दिन में हुई सारी बातों पर आपस में चर्चा करते हैं। यह इसलिए भी हमेशा फायदेमंद रहता है क्योंकि इससे आगे के लिए बेहतर करने का एक आइडिया मिल जाता है।
रात 11.00 बजे: हर दिन मुझे शाम को अपने दिनभर किए काम की रिपोर्ट बनाकर भेजनी होती है। हमारा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें सेल शिक्षक भी जुड़े हैं। हमें बताना होता है कि हमने आज कौन से स्कूल में विज़िट किया और कौन-कौन सी गतिविधियां कराई हैं। इसी तरह शिक्षक भी उसमें अपने अपडेट्स शेयर करते हैं। इसके साथ ही, हमें एक सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी संस्था को प्रतिदिन यह भी अपडेट करना होता है कि दिन में जो गतिविधि कराई उसमें क्या चीजें निकलकर आईं, क्या चुनौतियां रहीं, क्या बेहतर रहा, बच्चियों ने किस तरह से उन गतिविधियों में भाग लिया, इत्यादि। यह सब हमें अपनी आगे की रणनीति बनाने में मदद करता है।
यह सब बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद पर काम नहीं करेंगे, तो फिर छात्रों की मदद कैसे कर पाएंगे? हम उनके लिए सकारात्मक माहौल कैसे बना पाएंगे?
जैसा कि आईडीआर को बताया गया।
यह पोर्टिकस संस्था द्वारा समर्थित 12-भागों की सीरीज का दूसरा लेख है। यह सीरीज बाल विकास के सभी पहलुओं और बच्चों व युवाओं की बेहतर सामाजिक-भावनात्मक स्थिति तय करने से जुड़े समाधानों पर केंद्रित है। साथ ही, यह सीरीज़ इन विषयों पर बेहतर समझ बनाने से जुड़ी सीख और अनुभवों को सामने लाने का प्रयास करती है।
—
ऐतिहासिक रूप से, एनटी-डीएनटी समुदायों या विमुक्त जनजातियों को समाज, सरकार, कानूनों और नीतियों द्वारा हाशिए पर रखा गया है, जिनमें बंजारे, सपेरे, और मदारी जैसे कई घुमंतू समुदाय भी शामिल हैं। इन समुदायों के ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक स्थिति को समझने से उनके संघर्षों की गहराई और निरंतरता का पता चलता है। ब्रिटिश शासन के दौरान, इन पर ‘जन्म से चोर’ होने का ठप्पा लगा दिया गया, जो आज भी पुलिस प्रशिक्षण में मौजूद है। घुमंतु समुदायों को गांवों से बाहर रखा जाता था और उन्हें काम और सम्मान से वंचित किया गया था।
आज भी, ये समुदाय अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनके पारंपरिक व्यवसाय जैसे शिकार, मनोरंजन और देसी दवा आदि या तो गैरकानूनी घोषित कर दिये गए या समय के साथ उनकी मांग कम हो गई, इससे वे और भी हाशिए पर चले गए हैं। सरकारी योजनाएं उनकी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखती, और उन्हें आरक्षण या सामाजिक और आर्थिक उन्नति के अन्य अवसरों से वंचित रखा जाता है। इनकी बिखरी हुई और कम जनसंख्या, सरकार तक उनकी आवाज पहुंचने को और मुश्किल बना देती है। इन्हीं संदर्भों में विभिन्न घुमंतू और विमुक्त जनजाति समुदायों के मंच ‘घुमंतु साझा मंच’ के सदस्य अपनी चुनौतियों को उजागर कर रहे हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाने, उनकी पहचान के महत्व, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य तय करने के लिए जरूरी बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं।
इस वीडियो को बनाने में ज्ञान सिंह, मोइन कलंदर और घुमंतू साझा मंच के अन्य सदस्यों ने योगदान दिया है।
नूर मुहम्मद ‘घुमंतू साझा मंच’ की अगुवाई करते हैं।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—
मेरा नाम संतोष चारण है और मैं पिछले 14 सालों से आशा सहयोगिनी के रूप में काम कर रही हूं। मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आने वाली कपासन नगरपालिका में अपने पति और दो बेटों के साथ रहती हूं। मैंने 2004 से हापाखेड़ी गांव में जमीन पर काम करना शुरू किया। पहले मैं आंगनवाड़ी सहयोगिनी थी और फिर 2008 में आशा सहयोगिनी बन गई। आशा सहयोगिनी के रूप में, मैं गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और नीतियों से जोड़ने में मदद करती हूं और पूरी गर्भावस्था के दौरान उनकी सहायता करती हूं। इसके अलावा, मैं गांव में शिशुओं और बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान भी चलाती हूं। मैं नियमित रूप से स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी करती हूं ताकि समुदाय की स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझा जा सके और उनका समाधान किया जा सके।
सुबह 4 बजे: हर रोज मैं घर में सबसे पहले उठती हूं, पूजा करती हूं और मंदिर जाती हूं। कुछ साल पहले, मैं अपने ससुराल हापाखेड़ी से दो किलोमीटर दूर स्थित कपासन में बस गई। हापाखेड़ी में मैं ससुराल वालों के साथ रहती थी, वहां मुझे हर दिन सुबह 4 बजे उठकर गायों को चारा डालने, बाड़ा साफ करने और उपले बनाने जैसे काम करने होते थे। यह सब मैंने 1998 में शादी के बाद सीखा था। अब कपासन में मुझे गायों की देखभाल नहीं करनी होती, फिर भी मैं सुबह 4 बजे उठती हूं। जब मैंने पहली बार आंगनवाड़ी में काम करना शुरू किया तो मेरे ससुराल वाले चिंतित थे कि मैं घर के कामों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। इसके चलते घर में अक्सर बहसें होती थीं। उन्हें चिंता थी कि अगर मैं घर से बाहर काम करने लगूंगी तो गायों की देखभाल और घर के बाकी काम कौन करेगा। उनकी असहमति के बावजूद मैंने 2004 में हापाखेड़ी के आंगनवाड़ी केंद्र पर काम करना शुरू कर दिया।
उस समय, मैं अपने बेटों को हर सुबह आंगनवाड़ी केंद्र छोड़ने जाया करती थी। मेरी एक दोस्त के ससुर उस केंद्र में काम करते थे और हम अक्सर बातचीत किया करते थे। उनसे मैंने आंगनवाड़ी प्रणाली के बारे में बहुत सीखा और कभी-कभी उनके कामों में मदद भी कर देती थी। एक दिन उन्होंने ही मुझे सहायक पद के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया। मेरे पति मेरे इस फैसले से सहमत थे लेकिन ससुराल वालों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वे चिंतित थे कि अब उनके घर की महिला गांव में जाकर अजनबियों से बात करेगी। इन कारणों ने मुझे, मेरे पति और दोनों बच्चों सहित कपासन शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया।

मैं काम करने के लिए दृढ़ थी क्योंकि मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहती थी। आंगनवाड़ी में खाना बनाने के लिए मुझे 500 रुपये मिलते थे और आंगनवाड़ी सहायक के काम के लिए मुझे और 500 रुपये मिलते थे। इन 1000 रुपयों से सबसे पहले मैंने अपने एक बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवाया लेकिन दूसरे को मैं वहां नहीं भेज पाई। मैंने हेडमास्टर से विनती की और उन्होंने इस शर्त पर मेरे दूसरे बेटे को मुफ्त में पढ़ने की अनुमति दी कि मैं पांच और छात्रों का दाखिला करवाउंगी। मैंने गांव के लोगों को समझाया और आठ बच्चों का दाखिला करवाने में सफल रही। आज मेरे दोनों बेटे कॉलेज तक की पढ़ाई कर चुके हैं।
जब तक मैं मंदिर से घर वापस आती हूं, मेरे पति जाग चुके होते हैं और मैं उनके लिए नाश्ता बनाती हूं। इसके बाद मैं हापाखेड़ी जाने के लिए बस स्टॉप की ओर निकल जाती हूं और अपना दिन शुरू करती हूं।
सुबह 7 बजे: बस मुझे हापाखेड़ी से थोड़ी दूरी पर छोड़ती है। गांव तक जाने के लिए कभी मैं रिक्शा लेती हूं, कभी पैदल भी चली जाती हूं। इन पैदल यात्राओं के दौरान मुझे अक्सर आस-पास के गांवों की महिलाएं, खेतों की ओर जाती हुई मिल जाती हैं। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें करते हैं। मैं अक्सर उनसे उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पूछती हूं और उन्हें नोट करती हूं।
इन दिनों मैं लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने में उनकी मदद कर रही हूं ताकि उन्हें सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा मिल सके।
मैं गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाती हूं। राजस्थान के सरकारी केंद्रों में प्रसव पूरी तरह से मुफ्त होता है। कुछ साल पहले, हमारे इलाके में एक डॉक्टर जो हर प्रसव के लिए 500 रुपए की रिश्वत मांगता था। आशा कार्यकर्ताओं ने अनिच्छा से उसे पैसे देना स्वीकार भी कर लिया था क्योंकि हम प्रसव में कोई जटिलता नहीं चाहते थे। वह डॉक्टर जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले 1400 रुपयों की स्वीकृति भी करता था। कई बार तो पैसे न देने पर वह इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता था। यह स्थिति काफी समय तक चली।
मेरे अलावा अन्य आशा कार्यकर्ताओं ने भी स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस मामले पर जांच शुरू की गई।
एक बार, मैं एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिला को अस्पताल लेकर आई, वह परिवार डॉक्टर को 500 रुपये देने में सक्षम नहीं था और केवल 300 रुपये ही दे सकता था। जब मैंने डॉक्टर के निजी कमरे में 300 रुपये दिए तो उन्होंने 500 रुपये से कम स्वीकार करने से मना कर दिया। मैं परिवार के पास वापस गई और उनसे 200 रुपये और लाने को कहा। महिला के पति ने कहा कि उसे पैसे जुटाने के लिए घर जाकर कुछ अनाज बेचना पड़ेगा। यह सुनकर मैंने फिर से डॉक्टर से 300 रुपये लेने की विनती की। यह सुनकर डॉक्टर ने गुस्से में मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे धक्का दे दिया। इससे मैं भी बहुत गुस्से में आ गई, मैंने डॉक्टर की शर्ट पकड़ी और उसे कमरे से बाहर खींच लिया। फिर मैंने नवाचार, जो कपासन में स्थित एक गैर-सरकारी संगठन है और जिससे मैं 2008 से जुड़ी हुई हूं, को फोन किया। जल्द ही, उपखंड मजिस्ट्रेट सहित वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए। यह घटना जयपुर तक पहुंच गई और सरकार ने इसकी जांच शुरू की। मुझे जयपुर बुलाया गया और विधानसभा के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, हर स्क्रीन पर मैं खुद को देख रही थी। मेरे अलावा अन्य आशा कार्यकर्ताओं ने भी स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस मामले पर जांच शुरू की गई। वह डॉक्टर तो अब सेवानिवृत्त है लेकिन उसकी पेंशन रोक दी गई है।
12 बजे दोपहर: गांव में काम खत्म करने के बाद, मैं कुछ समय कागजी काम करने में बिताती हूं। जैसे-जैसे राजस्थान में आयुष्मान कार्ड का वितरण बढ़ रहा है, आशा कार्यकर्ताओं के लिए कागजी काम भी काफी बढ़ गया है। हर परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करना और उन्हें अपलोड करना लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है। हमें इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि कोई भी गलती या देरी, लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कर सकती है। मेरे बड़े बेटे ने मुझे फॉर्म भरने में मदद की है क्योंकि पोर्टल अंग्रेज़ी में है और मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाती।
2 बजे दोपहर: सुबह का फील्डवर्क खत्म करने के बाद, मैं दोपहर के भोजन के लिए घर लौटती हूं। ज्यादातर मैं एक घंटे के भीतर ही वापस चली जाती हूं ताकि कुछ और काम निपटा सकूं या किसी आपात स्थिति में मदद कर सकूं। आज मुझे हाप्पागिडी वापस जाना होगा ताकि बाकी आयुष्मान कार्ड के फॉर्म फाइल कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि मैं रात 10 बजे के आसपास तक घर लौटूंगी। भले ही हमारे आधिकारिक काम के घंटे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हैं, ज्यादातर आशा सहयोगिनियां पूरे दिन काम करती हैं। कई बार हमें रात में भी कॉल आता है ताकि किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा सके।
हम प्रदर्शन के लिए जयपुर गए थे, जहां प्रशासन ने सूचित किया कि वे अगले बजट में हमारा वेतन बढ़ा देंगे। हालांकि, उन्होंने सिर्फ 200 रुपये ही बढ़ाए।
साल 2008 में आशा सहयोगिनी के रूप में काम शुरू करने से पहले, मैं चार साल तक आंगनवाड़ी केंद्र में काम कर चुकी थी। फील्डवर्करों की काम करने की स्थितियों पर मैंने अक्सर चिंताएं जताई है। 2009 में मुझे आशा सहयोगिनी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संघ साल में दो बैठकें आयोजित करता है, जहां हम अपने सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। ये मुद्दे अक्सर भुगतान में देरी से संबंधित होते हैं। कुछ समय पहले हमने वेतन बढ़ाने के लिए प्रदर्शन किया था। उस समय, हम हर महीने 1600 रुपये कमाते थे जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों को जोड़ने के लिए मिलने वाले बोनस शामिल नहीं थे। हम प्रदर्शन के लिए जयपुर गए थे, जहां प्रशासन ने सूचित किया कि वे अगले बजट में हमारा वेतन बढ़ा देंगे। हालांकि, उन्होंने सिर्फ 200 रुपये ही बढ़ाए।
प्रदर्शनों को और प्रभावी ढंग से संगठित करने के लिए, हमारा एक ऑनलाइन ग्रुप चैट है जिसमें कपासन, रश्मी आदि ब्लॉक की ग्राम पंचायतों से आशा सहयोगिनियां जुड़ी हुई हैं। किसी भी बैठक, शिकायत या प्रदर्शन के बारे में अपडेट इस समूह में पोस्ट किए जाते हैं, और पंचायत स्तर पर चयनित आशा सहयोगिनियां फिर गांव में अन्य सभी को सूचित करती हैं।
वर्तमान में, संघ एक और भुगतान से संबंधित समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। चूंकि हमारा अधिकांश काम, जैसे कि आयुष्मान कार्ड के लिए फॉर्म जमा करना, ऑनलाइन होता है, हमें अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज करने के लिए 600 रुपये के भत्ते का अधिकार है। लेकिन मार्च से हमें यह नहीं मिल पाया है।
यह पहली बार नहीं है जब मैंने गलत के खिलाफ विरोध किया है। मेरे पति पहले शराबी थे, लेकिन छह साल पहले उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। शराब पीने के बाद वो अक्सर मुझे मारते थे। एक बार, उन्होंने कुछ दिनों तक शराब के अलावा कुछ भी नहीं खाया या पिया और बहुत हिंसक हो गए। तब मैंने तय किया कि मुझे इसका समाधान निकालना होगा। मुझे पता चला कि कुछ दिनों में एक सरकारी अधिकारी गांव का दौरा करने वाली हैं, और मैंने सोचा कि यह अपनी आवाज उठाने का अच्छा मौका होगा। मैंने गांव में उन सभी महिलाओं से बात की जो इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रही थीं। हम सबने एक बैठक की और एक याचिका पर हस्ताक्षर करके समस्या को अधिकारी के सामने लाने का फैसला किया।
मेरी सुरक्षा को लेकर मेरा परिवार चिंतित था क्योंकि मैं एक आशा सहयोगिनी थी और आपात स्थितियों से निपटने के लिए रात में अक्सर गांव में निकलना पड़ता था।
जब अधिकारी आई, तो मैंने शिकायत बताने के लिए अपनी बारी का इंतजार किया, वहां भीड़ में कई लोग अपनी शिकायतें बताने के लिए उत्सुक थे। जब रात के 10 बज गए और वह जाने ही वाली थीं, तब मैंने माइक छीनने का फैसला किया। जब मैंने अपनी और गांव की अन्य महिलाओं की पीड़ा को सुनाना शुरू किया, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे साथ आई अन्य महिलाएं भी रोने लगीं। अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। जब उन्हें पता चला कि गांव में शराब की दुकानें कानूनी समय से ज्यादा देर तक खुली रहती हैं, तो उन्होंने उनका लाइसेंस जब्त करने का फैसला किया। गांव की सभी शराब की दुकानें जल्द ही बंद हो गई। इसके बाद मेरे पति शराब नहीं खरीद पाए, लेकिन इससे मेरे लिए एक और चुनौती खड़ी हो गई। गांव के पुरुष, जो अक्सर शराब पीते थे, मुझसे नाराज हो गए।
मेरी सुरक्षा को लेकर मेरा परिवार चिंतित था क्योंकि मैं एक आशा सहयोगिनी थी और आपात स्थितियों से निपटने के लिए रात में अक्सर गांव में निकलना पड़ता था। उन लोगों में से एक, जिसकी शराब की दुकान थी, मेरे घर आया और मुझसे कहा कि मैं एक कीड़ा हूं जिसे नाली में होना चाहिए। इस पर मैंने जवाब दिया, “जब कीड़ा लकड़ी में लग जाता है तो वह लकड़ी पूरी तरह खराब हो जाती है।” उन्हें अब तक अपना शराब का लाइसेंस वापस नहीं मिला और मैंने अपना काम वैसे ही जारी रखा है।
रात 10 बजे: आज भी मैं रात 10 बजे के आस-पास घर पहुंची। थकी होने के बावजूद, मुझे अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है, जो मेरे लौटने का इंतजार कर रहा होता है। सभी के लिए खाना बनाने में मुझे आधा-पौना घंटा लगता है, उसके बाद मैं सोने चली जाती हूं। जब मैं घर पर होती हूं तब भी मेरा फोन साइलेंट नहीं रहता, ताकि किसी डिलीवरी या आपातकालीन कॉल को मिस न करूं। खाली समय में मुझे भजन सुनना, नाचना और गाना पसंद है।
कुछ साल पहले, नवाचार द्वारा आयोजित एक बैठक में बताया गया था कि उत्पीड़ित लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने उत्पीड़न को दूर करने के लिए कदम उठाएं। यह तब की बात है जब मेरे पति शराब पीते थे और मैं अपने ससुराल में रहती थी। ऐसी ही एक अन्य बैठक में मुझे यह भी बताया गया कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह काम करने का अधिकार है। इन दोनों बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला और मैंने अपने जीवन को बदलने और अपने आस-पास के लोगों की भी मदद करने का निश्चय किया। 14 साल बाद, मैं बहुत बेहतर कर रही हूं और मेरा परिवार खुश है। कभी-कभी गांव के लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, लेकिन मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ‘मैं’ बनने में बहुत समय लगा और मुझे गर्व है कि मैं कौन हूं। मैं एक दिन सरपंच बनना चाहती हूं और गांव और गांव की महिलाओं की और भी बेहतर तरीके से मदद करना चाहती हूं।
जैसा कि आईडीआर को बताया गया।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
दयामनी बरला, एक आदिवासी कार्यकर्ता और पत्रकार हैं और हमेशा ही आदिवासी मुद्दों पर अपनी बात मुखरता से रखती आई हैं। इस इंटरव्यू में दयामनी बरला बताती हैं कि उनका बचपन भी बहुत संघर्षों से भरा रहा और उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद से संघर्ष करना पड़ता था।
दयामनी बताती हैं कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद पत्रकारिता और एक्टिविज्म क्षेत्र को चुनना इसलिए बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि जिस तरह से बच्चों, महिलाओं, युवाओं के साथ काम होना चाहिए था, उस तरह से नहीं हो पाया है। वे कई अलग-अलग अखबारों व पत्रिकाओं से जुड़ी रही हैं।
दयामनी, इस इंटरव्यू में संविधान और उसमें दिए गए अधिकारों के प्रति युवाओं के जागरूक होने पर जोर देती हैं। इंटरव्यू में वह बताती हैं कि उन्होंने विभिन्न आंदोलनों के ज़रिए जल, जंगल और जमीन जैसे मुद्दों पर न केवल पूंजीपतियों बल्कि सरकार से भी अपनी बात मनवाई।
उनका मानना है कि पढ़ने-लिखने के साथ-साथ युवाओं को राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। इसके पीछे का कारण वो बताती हैं कि जब युवा विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में चुनकर जाते हैं तो उनके पास संवैधानिक तौर पर आम नागरिकों की भलाई के लिए नीतियों के निर्माण व बदलाव लाने की ताकत होती है। दयामनी बरला, कई पुरस्कारों से भी सम्मानित रही हैं।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
बिहार में आदिवासियों के झारखंड आंदोलन से अपनी पहचान बनाने वाले मधु मंसूरी हंसमुख का नाम जितना दिलचस्प है, उनके जीवन का सफर भी उतना ही रोचक रहा है। बचपन से ही इन्हें लोकगीतों का शौक रहा है। आगे चलकर इन्होंने झारखंड बनने के आंदोलन में अपने गीतों के ही ज़रिये लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई।
पद्मश्री सम्मान से नवाजे जा चुके लोकगीत कलाकार मधु मंसूरी हंसमुख ने आईडीआर के साथ अपनी बातचीत में बताया कि कैसे छोटी सी उम्र से ही इन्होंने लोकगीत के ज़रिये न केवल आंदोलन में अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि इस हुनर को अपना हथियार बनाकर झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा और चेतना भी प्रदान की। इस इंटरव्यू में हंसमुख, झारखंड आंदोलन से जुड़े अपने खट्टे-मीठे अनुभवों को साझा करते हुए इस बात पर भी जोर देते हैं कि कैसे झारखंड में अपार खनिज संसाधनों के बावजूद आज भी यहां के युवा रोज़गार के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
मेरे पिता जी का नाम अब्दुल रहमान और मां का नाम मनी परवीन था। मैं 15—16 महीने का ही था जब मां का देहांत हो गया। उनके गुजर जाने के बाद मुझे दूध नहीं मिल पा रहा था और मैं हर दिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन तबियत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि सबको लगा कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे घर के आंगन में रख दिया गया और धीरे—धीरे वहां गांव वालों की भीड़ भी जमा हो गई। उसी समय वहां से गांव में रहने वाला ग्वाला, शिव शंकर गुजर रहा था। मेरे घर के बाहर भीड़ देखकर वह भी वहां आ गया। लोगों ने उसे बताया कि इस बच्चे को मां का दूध नहीं मिल पाया है इसलिए ये मरने वाला है।
शिव शंकर ने वहां खड़े लोगों से कहा, “तुम लोग मेरी बात सुनकर मुझे पेड़ से बांधकर मारोगे पर कोई बात नहीं! पर मेरी बात मानो, और मुझे इस बच्चे को महुआ की थोड़ी सी शराब पिलाने दो क्योंकि इससे यह ठीक हो जाएगा।” इस पर सब मान गए। उसने मुझे थोड़ी सी शराब पिलाई। उस वक्त तो मैं होश में नहीं आया लेकिन करीब 4 घंटे बाद मुझे होश आ गया। ये एक चमत्कार ही था और वो शराब मेरे लिए अमृत बन गई। इसके बाद मुझे अक्सर शराब के घूंट पिलाए जाते थे। करीब 8 साल की उम्र तक मैं अमृत समझकर शराब पीता रहा। उसका नशा इतना ज्यादा हो जाता था कि कई बार मैं खुद चलकर घर नहीं आ पाता था। वह समय अच्छा था। गांव में राजनीति नहीं थी, इसलिए कोई भी आदिवासी या फिर दूसरे समुदाय के लोग मुझे घर लेकर आ जाते थे। घर लाकर वो मेरे पिता जी से कहते, “अरे ये बच्चा तो मधुआ हो गया है।” यानि नशे में मदहोश। बस इसी मधुआ से मेरा नाम मधु हो गया। हालांकि ये नाम इस्लामिक नहीं है पर फिर भी मेरा नाम मधु ही हो गया।
कुछ समय बाद मेरी देखभाल के लिहाज से पिता जी ने दूसरी शादी कर ली। मैं अपनी नई मां को मौसी मां कहता था। उनका पहले से ही एक बेटा यानि मेरा सौतेला भाई भी था। हम तब साथ ही रहते थे।
इसके बाद रांची के हाई स्कूल के एक शिक्षक कुलदीप सहाय जो रांची में पढ़ाते थे, उनके खेतों में मेरे पिता जी काम करने के लिए जाते थे। एक रोज मैं स्कूल से छुट्टी के बाद अपने पिता के पास पहुंचा। स्कूल से आने पर बहुत भूख लगी थी तो वहां पहुंचकर मैं पिता जी से हंसते हुए घर की चाबी मांग रहा था। तभी कुलदीप सहाय वहां आए और मेरा हाथ पकड़ते हुए मेरे पिता से बोले, “अब्दुल रहमान, आज से मैं तुम्हारे बेटे का नाम मधु मंसूरी हंसमुख रख रहा हूँ।“
फिर पिताजी ने जब मेरा एडमिशन छठवीं कक्षा में करवाया, तो उन्होंने स्कूल में मेरा यही नाम दर्ज करवा दिया, और मैं बन गया मधु मंसूरी हंसमुख।
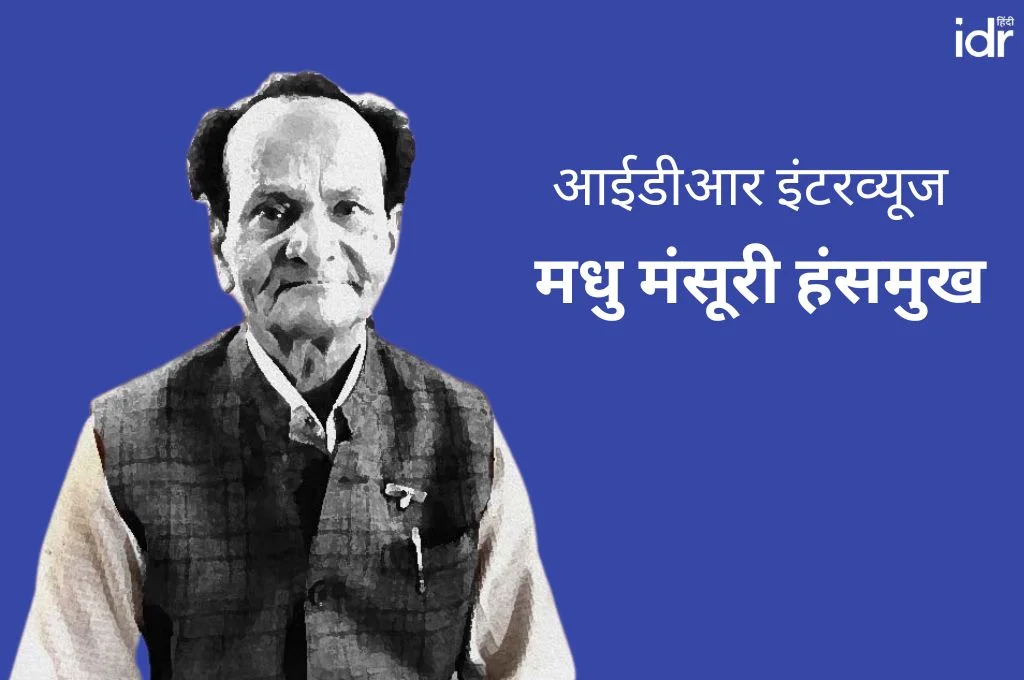
मेरी संगीत में तो बचपन से ही रूचि थी। मैंने 8 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर गाना गाया था। 2 अगस्त 1956 में हमारे प्रखंड के नामी गांव रातू में वहां के महाराज प्रखंड कार्यालय के शुभारंभ कार्यक्रम में आ रहे थे। तब वहां के आयोजक इस कार्यक्रम के लिए लोकगायकों की तलाश कर रहे थे। मैं स्कूल में गीत गुनगुनाया ही करता था, ये बात मैट्रिक क्लास में पढ़ने वाला दिल अहमद जानता था। कार्यक्रम के बारे में जब उसे मालूम चला तो उसी ने आयोजकों को मेरे नाम का सुझाव दिया और बाद में वही मुझे कार्यक्रम में भी लेकर आया। उस समय मैंने स्टेज पर पहला लोकगीत गाया, जिसे सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे ईनाम में 10 रुपए दिए। उस वक्त 10 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी।
10 रुपए हाथ में होने के बाद भी मुझे कोई खाना खिलाने को तैयार नहीं था।
10 रुपए मिलने के बाद मैंने सोचा कि अब कुछ खाया जाए, क्योंकि कार्यक्रम में शामिल होने की जल्दी की वजह से मैं बिना खाना खाए ही आ गया था और, बहुत भूख भी लग रही थी। लेकिन 10 रुपए हाथ में होने के बाद भी मुझे कोई खाना खिलाने को तैयार नहीं था। इसके पीछे समस्या यह थी कि उस समय 1 आने की कीमत में चाय और 1 आने में पकौड़ा आ जाता था। अगर मैं एक चाय और एक पकौड़ा खाता और अपने साथी को भी खिलाता, तब भी होटल वाले के पास लौटाने के लिए 9 रुपए 12 आना नहीं थे। इसलिए हम भूखे ही आ गए।
जब हम घर पहुंचे तो मैंने पिता जी को 10 रुपए दिए। उन्होंने दिल अहमद से पूछा कि मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा गीत गाया कि महाराजा ने उसे 10 रुपए दिए, जबकि मैं तो धूप में सारा दिन काम करता हूं, तब जाकर 1 रुपया दिन का मिलता है। वो बात मैं आज भी नहीं भूल पाया हूं।
बस ऐसे ही मेरे करियर की शुरुआत हुई। जब लोगों को महाराज वाले कार्यक्रम के बारे में पता चला तो और लोग भी मुझे अपने यहां गीत गाने के लिए बुलाने लगे। दिल अहमद ही मुझे हर जगह ले जाया करता था। कई बार तो कार्यक्रम इतने ज्यादा और इतनी दूर होते थे कि हम 6-7 दिन तक घर ही नहीं आ पाते थे। वैसे मैं पढ़ाई में भी अच्छा था।
ऐसा ही एक बार तब हुआ जब शिक्षा मंत्री हमारे स्कूल आए और उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने स्कूल के रजिस्टर में लिख दिया कि जब तक यह बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, तब तक इसकी स्कूल फीस नहीं लगेगी। इससे मैं बहुत खुश था।
साल 1968 में मेरे सौतेले भाई की सरकारी नौकरी लग गई। तब तक मैं भी कक्षा दसवीं की परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास हो गया था। लेकिन भाई की नौकरी लगने के बाद मेरी मौसी मां (सौतेली मां) पिता जी से अलग हो गई और अपने बेटे के साथ रहने लगी। इस घटना के बाद से मैं पढ़ नहीं पाया।
उन दिनों बिहार में रह रहे आदिवासी अपने लिए अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे। यह आंदोलन सालों से चल रहा था। उस दौर में झारखंड आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए औरतें बच्चों को पीठ पर बांधकर ले जाती थीं, आदमी तपती धूप में भी नारे लगाते थे। जब मैं इस आंदोलन का हिस्सा बना तब मेरी उम्र 12 साल थी। मैं किसी क्रांतिकारी के तौर पर आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि अपने गीतों की वजह से शामिल हुआ। असल में झारखंड आंदोलन को ध्यान में रखते हुए 12 साल की उम्र में ही मैंने एक गीत लिखा, यह नागपुरी बोली का गीत था। झारखंड पार्टी के महासचिव लाल रणविजय नाथ शाहदेव मुझे अपने साथ लेकर गए। फिर मैंने वही गीत नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक (खूंटी) में पहली बार गाया। गाने का भावार्थ था, “सालों तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब अफसरों के गुलाम हैं।”
लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इसके बाद से ही यह सिलसिला शुरू हो गया। मैं आंदोलन के मोर्चों में शामिल होता गया, गीत गाता रहा और मेरे गीतों से युवाओं और आदिवासियों को बहुत प्ररेणा मिलती रही। 22 अगस्त 1967 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मैं रांची, ऐसे ही एक कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचा था और तभी वहां दंगा भड़क गया। मैंने उस दंगे को अपनी आंखों से देखा। लोगों को खून से लथपथ, जलते—मरते देखा। उस घटना ने मुझे झकझोर दिया। 2—3 दिन बाद जब मैं घर आया तो मुझे नींद नहीं आई। रात को खाना खाकर मैं लिखने बैठ गया। एक ही रात में मैंने उस दंगे से प्रभावित होकर एक कविता लिखी। यह कविता मेरे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत रही है।
मार्च 1964 में मेरी शादी हो गई और 1970 आते तक मेरी नौकरी लग गई। आंदोलनकर्ता मुझे खोजते रहते बावजूद इसके मैंने 4 साल तक नौकरी की। जब उन्हें आखिरकार मेरी नौकरी के बारे में पता चला तो बोले, “कहां तुम नौकरी के चक्कर में फंस गए, तुम्हें तो हर दम हमारे साथ रहना चाहिए।” मैं भी आंदोलन का हिस्सा बने रहना चाहता था। इसलिए अक्सर मोर्चे और सभाओं में गीत प्रस्तुति के लिए पहुंच जाता था। इस वजह से परिवार भी परेशान था और नौकरी करना भी मुश्किल हो गया।
मैं कई दिनों तक घर से दूर और नौकरी में गैरहाजिर रहता था जिसके कारण मुझे नौकरी से निकालने तक की नौबत आ गई थी। हालांकि झारखंड आंदोलन का हिस्सा बनने के बाद से लोग मुझे पहचानने लगे थे। इसलिए मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और खेलमंत्री से मुलाकात की। उनकी मदद से चेयरमेन को एक पत्र पहुंचाया गया। जिसमें बाद चेयरमेन ने मेरे पक्ष में आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर मैं कार्यक्रमों में शामिल होने के कारण नौकरी पर नहीं आता हूं तो उस दिन का मेरा वेतन काट लिया जाए पर नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद मैं महीने में 12 से 14 दिन तक ऑफिस नहीं जा पाता था पर इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। घर से भी इतने ही दिनों तक दूर रहता रहा।
आज मेरे 4 बेटे हैं, सभी पढ़े-लिखे हैं लेकिन वे सभी बेरोजगार हैं। मैं झारखंड आंदोलन का हिस्सा था इसलिए बिहार सरकार ने मेरे बेटों को नौकरी नहीं दी। झारखंड राज्य बन गया पर यहां भी उनके लिए रोजगार नहीं है।
आंदोलन का हिस्सा बनकर मैंने सैकड़ों गीत गाए, युवाओं और आदिवासियों को एक करने का प्रयास किया। अपने गीतों से उन्हें सही राह दिखाता रहा। लोगों से मुझे प्यार और सम्मान मिला पर इन सबके बीच नौकरी बर्बाद हो गई, परिवार बर्बाद हो गया और समय भी बर्बाद हुआ।
मुझे इस आंदोलन से बहुत कुछ मिला भी है। इसी की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे। मेरे गीतों को सराहना मिली। मेरे नागपुरी बोली के लोकगीत रिकॉर्ड भी किए गए। इसी के फलस्वरूप, सरकार की ओर से मुझे पुरस्कार के तौर पर सिमडेगा में जमीन देने की घोषणा हुई। तब मैंने कलेक्टर से मिलकर कहा कि ये जमीन देकर हमको लोगों की नजरों से मत गिराओ। मैंने वो जमीन नहीं ली। इसके बाद सम्मान के तौर पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री करमचंद्र भगत ने भी जमीन देने का ऐलान किया लेकिन मैंने मना कर दिया। अगर आज मेरे पास वो जमीन होती तो उसकी कीमत करोड़ों में होती।
मेरे गीतों को सुनकर शिबू सोरेन खुश होकर बोले, “ऐ मंसूर साहब, हमारे तीर की धार और तुम्हारे गीत का धार से अलग राज्य बनकर रहेगा।”
बाद में जब झारखंड राज्य बन गया तो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मुझे सम्मानित किया और मेरे जिले में ही मुझे 4 एकड़ जमीन दी। यह सम्मान मैंने स्वीकर कर लिया। इसकी एक वजह है। असल में 1975 में मैं आंदोलन से जुड़े एक कार्यक्रम में गीत प्रस्तुत करने रामगढ़ गया था। उस कार्यक्रम में धनबाद के नेता एके राय और उनके साथ शिबू सोरेन यानि हेमंत सोरेन के पिता जी भी आए थे।
मैंने वहां जो गीत गाए उन्हें सुनकर शिबू सोरेन बहुत खुश हुए और बोले, “ऐ मंसूर साहब, हमारे तीर की धार और तुम्हारे गीत का धार से अलग राज्य बनकर रहेगा।” यही उनकी और मेरी पहली मुलाकात थी। इसके बाद हम कार्यक्रमों के दौरान दिल्ली, कोलकाता और बहुत सी जगहों पर भी मिलते रहे। इस तरह से झारखंड आंदोलन में शामिल होने के बाद मुझे बहुत नाम, इज्जत, लोगों का प्यार और सराहना मिली।
मैंने 300 से ज्यादा गीत गाए और इन्हीं गीतों ने मुझे पद्मश्री सम्मान तक भी पहुंचाया।
मैंने हमेशा से ऐसे गीत लिखे, जिनसे युवाओं को सही दिशा मिल सके। मैंने अपने गीतों में आदिवासियों के हक की बात की। जब झारखंड राज्य बन रहा था तब हम सभी को बहुत सारी उम्मीदें थीं। मैंने इन्ही उम्मीदों को गीत के बोल में बांधा था। पर आज महसूस होता है कि राज्य को लेकर जो सपने देखे थे, वो पूरे नहीं हुए हैं।
इस राज्य के पास बहुत कुछ है। यहां 28 तरह के खनिज हैं, सबसे ज्यादा प्रकृतिक संपदा है, लेकिन उनका कोई सही उपयोग नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को अनाज का दाना नहीं है। ऐसे में भूखा आदमी पाप करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा। इसी उग्रवाद में राज्य के बहुत सारे युवा शामिल हो रहे हैं। बाबू लोगों की कलम गलत दिशा में चल रही है। शोषण कोई सहन नहीं करता तो यही कारण है कि कुछ युवा लोग उग्रवादी बन रहे हैं। खनिज और खजाना के असली मालिक गैर झारखंडी लोग बने हुए हैं। हालांकि, अभी भी सब बदलने का समय है।
रोजगार के लिए राज्य में कपड़ा मिल खोली जा सकती है। यहां बॉक्साइट का खजाना है, उसका उपयोग करके एल्युमीनियम का कारखाना खोल सकते हैं। चीनी मिल, पेपर मिल बनाए जा सकते हैं। यहां इतने संसाधन हैं कि दवा बनाने की कंपनियां खुल सकती हैं। अगर ये सब होता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे वे ना तो पलायन करेंगे ना ही उग्रवादी बनेंगे। असल में हमारे पास नेतृत्व की सोच नहीं है। नेता सोचते हैं कि छोटे लोगों को काम मिलेगा तो ये क्यों हमारी जी हुजूरी करेंगे।
कितने ही सारे नेता हैं जो जेल जा चुके हैं, घोटालों में उनके नाम सामने आ रहे हैं। आम जनता के पास अपनी जरूरतें पूरी करने लायक संसाधन तक नहीं है। लोगों को दवाएं नहीं मिल रहीं, खेतों में सिंचाई का साधन नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, सरकारी स्कूल तो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं।
हमने आंदोलन के समय ये सपना तो नहीं देखा था। मैं तो नौजवानों के लिए बहुत से गीत लिख चुका हूं अब उनका सक्रिय होना जरूरी है।
इस आलेख को तैयार करने में स्मरिणीता शेट्टी ने सहयोग किया है।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
डॉ. नरेंद्र गुप्ता एक सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सक और प्रयास नाम के स्वयंसेवी संस्था के संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने लगभग 40 सालों से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में भील मीना आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार के लिए काम किया है। वह जन स्वास्थ्य अभियान के राष्ट्रीय आयोजकों में से एक, और राजस्थान में इसके संयोजक हैं।
डॉ. गुप्ता ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ढांचे को डिज़ाइन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कार्य समूह के गठन में अहम भूमिका निभाई जिससे पंचायती राज संस्थान की भूमिका और स्पष्ट हो सकी। साथ ही वह भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्य समूह के सदस्य थे जिसमें उन्होंने दवाओं और खाद्य सुरक्षा पर काम किया। राजस्थान में निशुल्क दवा योजना की शुरुआत में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
डॉ. गुप्ता ने आईडीआर से अपने स्वास्थ्य के काम से संबंधित सफ़र कि बात की। उन्होंने राजस्थान में लोगों में स्वास्थ्य की समझ को बदलने के प्रयास के बारे में बताया।भारत में राइट टू हेल्थ और निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं की ख़ासा ज़रूरत क्यों है और इन्हें बढ़ावा देने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए।
स्वास्थ्य का काम करने शुरू करने के लिए चित्तौड़गढ़ जिला एक चुनौती भरा इलाक़ा क्यों है और यहां स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ काम करना क्यों ज़रूरी था।
नेशनल रुरल हैल्थ मिशन लॉन्च होने से स्वास्थ्य पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडीचर (जेब से खर्च) कैसे कम हो सकता है, और कैसे निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत कई गुना कीमत पर मिलने वाली दवाई अब मुफ्त में उपलब्ध होती है।
अगर आपके पास राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इंप्लॉयमेंट, राइट टू फूड, फॉरेस्ट राइट एक्ट सब कुछ है तो स्वास्थ्य पर क्यों नहीं?
भारत की बहुत बड़ी आबादी को आज भी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं होती – हर परिवार के लिए डॉक्टर तय होना चाहिए और घर से कुछ ही दूरी पर छोटी से बड़ी बीमारी के लिए स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध होने चाहिए।5.5.
जन स्वास्थ्य अभियान साल 2000 में भारत आया जिसके अंतर्गत सभी स्वास्थ्य से जुड़ी लड़ाई जैसे राइट टू हेल्थ और फ्री मेडिसिन का कैंपेन राजस्थान में शुरू हुआ।