वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राजिम केतवास, छत्तीसगढ़ के पिथौरा क्षेत्र से हैं। उन्होंने केवल 19 वर्ष की उम्र में संयुक्त मध्य प्रदेश में एकता परिषद के साथ जमीनी स्तर का काम शुरू किया था। इसके बाद वह शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में भिलाई में श्रमिक आंदोलन से जुड़ी। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में काम के दौरान उन्होंने समझा कि महिलाओं, विशेषकर दलित और आदिवासी महिलाओं के जीवन पर जाति और पितृसत्ता किस तरह अमानवीय असर डालती है।
इन अनुभवों को आधार बनाकर उन्होंने अपने संगठन दलित आदिवासी मंच की स्थापना की, जो ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के सम्मानजनक जीवन और अधिकारों के लिए कार्यरत है। यह संगठन जातीय हिंसा, वनाधिकार, प्रवासी श्रमिक, मानव तस्करी, महिला हिंसा, और जेंडर जैसे मुद्दों पर काम करता है। राजिम पूरे राज्य में समानता, न्याय और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष की एक मजबूत आवाज के रूप में जानी जाती हैं।
इस बातचीत में वह सामाजिक क्षेत्र में अपने काम की शुरुआत से लेकर खुद का संगठन बनाने और समुदाय के साथ काम के बारे में विस्तार से बता रही हैं।
अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। सामाजिक क्षेत्र में आपके काम की शुरुआत कैसे हुई?
हम मूल रूप से ओडिशा के बरगढ़ के हैं। मेरी मां छत्तीसगढ़ के पिथौरा से थीं। हम बहुत गरीब परिवार से थे और मां-पिताजी मजदूरी करके घर चलाते थे। उसी दौरान पिताजी बीमार पड़े और इलाज न मिल पाने से उनका निधन हो गया। सबसे छोटा भाई तब मां के पेट में ही था। पिताजी के परिवार ने मां को बहुत प्रताड़ित किया और घर पर कब्जा कर लिया। ऐसे समय में नाना-नानी हमें वापस पिथौरा ले आए, जहां हम आज भी रहते हैं।
पिथौरा आने के बाद भी हमारी स्थिति नहीं बदली। मां यहां भी मजदूरी करने जाती थी। उन्होंने सराइपाली के एक मिशनरी स्कूल के हॉस्टल में हमारा दाखिला करवा दिया। वहां मेरा मन नहीं लगा। आठवीं के बाद मैं वापस घर आ गई और मां के साथ मजदूरी करने लगी। उसी दौरान ‘जन जागृति’ संस्था से जुड़े किसी व्यक्ति ने बताया कि तिल्दा में सामाजिक कार्य की ट्रेनिंग होती है। मैं उस समय खुद भेदभाव का शिकार होने के बावजूद समाजसेवा या दलित मुद्दों को नहीं समझती थी। इसके लिए मेरी मां ने पीतल के बर्तन गिरवी रख के बीस रुपए का इंतजाम किया और मैं ट्रेनिंग के लिए गयी।
तिल्दा की ट्रेनिंग में हमने तीन महीने थ्योरी और तीन महीने प्रैक्टिकल की पढ़ाई की। इसके लिए मुझे बस्तर भेजा गया था। उस दौरान मैंने बस्तर और दंतेवाड़ा के अंदरूनी इलाकों में काम किया, जो परिवर्तन संस्था को पसंद आया और उन्होने मुझे साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया। इस तरह परिवर्तन पहली संस्था थी, जिसके साथ मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम की शुरुआत की थी।
काम के दौरान जब हम किसी के घर जाकर उनसे कुछ पूछते थे, तो वे मुंह बनाकर अंदर चले जाते थे। स्थानीय लोग गोंडी, हल्बी आदि बोलियां बोलते थे जो हमसे अलग थी। हमारा पहनावा भी उन्हें पसंद नहीं था। हमने सोचा कि आखिर कैसे इनसे दोस्ती की जाए? वहां की महिलाएं केवल एक कपड़ा पहनती थी। तो हमने भी ब्लाउज और पेटिकोट पहनना बंद किया और उन्हीं का पहनावा अपनाया। उनके साथ ही हम जंगल जाते, महुआ, लकड़ी आदि चुनकर लाते। फिर मैं धीरे-धीरे उनके साथ हल्बी और गोंडी बोलना भी सीख गई। कभी-कभी कुछ स्थानीय लड़कियों को मैं अपने साथ फिल्म दिखाने भी ले जाती थी।

मुझे धीरे-धीरे इसमें बहुत मजा आने लगा। मैं तब केवल 17-18 साल की थी, तो बस इतना ही सोचती थी कि वहीं रहना, वहीं सोना, वहीं खाना और वहीं नाचना है। ये वो समय भी था जब बड़े पैमाने पर जंगल कट रहे थे और जंगलों पर अधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। जगदलपुर के पास आसना में मिटकी बाई, कला दीदी जैसी कार्यकर्ताएं मौजूद थी, जो जंगलों की कटाई के विरोध में पेड़ों से चिपक जाती थी। हम लोग भी उनसे मिलने गए। लेकिन हमारी समझ उतनी विकसित नहीं थी। फिर धीरे-धीरे समझ आने लगा कि समाज में क्या सब गलत चल रहा है। हम वहां के गोंड, भत्री, हलवा आदि आदिवासी समुदायों के साथ काम कर रहे थे। तब वहां अधिकांश लोग आदिवासी ही थे।
मध्य प्रदेश के श्रमिक आंदोलन और ट्रेड यूनियन से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ?
1989 में परिवर्तन संस्था के साथ काम करने के दौरान ही पहली बार शंकर गुहा नियोगी से मुलाकात हुई थी। हमें बताया गया था कि वह आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं थे। रात में जब वह आए, तो बिल्कुल साधारण कपड़ों में चुपचाप हमारे पैरों के पास ही सो गए। उनके करिश्माई व्यक्तित्व से हम बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने हमें पोस्टर-पैम्फलेट दिए, जिनके जरिये हमने जाना कि दुनिया में दो वर्ग हैं- एक मजदूर और एक मालिक, एक शोषित होने वाला और एक शोषण करने वाला। फील्ड में इन्हीं मुद्दों और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बारे में हम लोगों को बताते थे। हमारा यह काम उन्हें पसंद आया, और उन्होंने मुझे श्रमिक आंदोलन से जुड़ने के लिए कहा।
मैं जब आंदोलन से जुड़ी तो वहां अकेली महिला थी। पुरुष साथियों के साथ साइकिल पर फैक्ट्रियों में जाना, महिला मजदूरों से बात करना, उन्हें श्रमिक अधिकारों के बारे में बताना—यही मेरा काम था। हम उन्हें बताते थे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी छटनी में सबसे पहले उन्हें बाहर किया जाता है और अकुशल मजदूर की श्रेणी में रखा जाता है। हम हर तरह का काम वक्त-बेवक्त बिना कुछ कहे करते हैं और शारीरिक शोषण का खतरा भी सदा बना रहता है। इस तरह हम महिला मजदूरों के साथ मीटिंग कर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और संगठन के बारे में बताने का काम करते थे।
उस समय महिला मजदूरों के बीच काम करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। पुरुष, महिलाओं के साथ बातचीत में सहज नहीं हो पाते थे और महिलाओं की भी यही स्थिति थी। कंपनियां मजदूरों का जमकर शोषण कर रही थी। उनके साथ मारपीट और डराने-धमकाने की घटनाएं बहुत आम थी। थोड़ा भी विरोध करने पर वे अन्य जगहों से मजदूरों को ले आते थे। इन सबके बीच महिला मजदूरों की स्थिति और ज्यादा खराब थी।
मानव-श्रम जैसे मुद्दे पर जहां पुरुषों को ही ज्यादा महत्व मिलता है, वहां एक महिला होने के नाते काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। भाषा और व्यवहार जैसी कई चीजें होती हैं, जो कई बार असहज हालात बना देती हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन में काम करना हो तो सशक्त होना पड़ता है। मैं भी वहां काम करते-करते सब तरीके अच्छे से सीख गयी थी और खुद को दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतिकारी समझती थी। हम लोग हर चीज में माहिर थे। हड़ताल, रैली-धरना-प्रदर्शन, जेल जाना। हम किसी भी काम से पीछे नहीं हटते थे। नियोगी जी कहते थे, “तुम जितना मार खाओगे, उतना फौलाद बनोगे। जितना जेल जाओगे, उतना मजबूत बनोगे। जेल हमारे लिए ही बना है।” हम पुलिस से कभी भी भागे नहीं, कभी भी डरे नहीं। मैं उन्नीस बार जेल गयी हूं और बहुत मार भी खायी है।
1991 में नियोगी जी की हत्या के बाद लाखों मजदूर भिलाई में जुटे और संगठन व आंदोलन दोनों को मजबूती मिली। हमने जब 1992 में कंपनियों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ करो या मरो का अभियान छेड़ा, तो राज्य की तरफ से बहुत हिंसा हुई। इसमें करीब 16 मजदूर मारे गए। एक प्रदर्शन के दौरान मुझे भी पुलिस ने बहुत पीटा था। मैं गटर में गिर गयी इसलिए शायद बच गयी। सरकार ने मजदूरों के खिलाफ जैसे एक मुहिम छेड़ रखी थी। उन्हें जबरन घर से उठा लिया जाता था, उनके घर तोड़ दिये जाते थे और हजारों की संख्या में उनके लीडरों को जेल में डाल दिया जाता था। तकरीबन दो साल तक उन्हें जेलों में बंद रखा गया था। इसी समय आंदोलन में बिखराव भी आया और यह अलग-अलग धड़ों में बंट गया। नियोगी जी जो कहते थे कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो जायें। लेकिन उसके उलट सारे उद्योगपति एकजुट हो गए और एक तरह से उन्होने पूरे संगठन को खत्म कर दिया।
बतौर महिला सामाजिक कार्यकर्ता, आपको ट्रेड यूनियन में पुरुषों के बीच काम करने के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
ट्रेड यूनियन में एक महिला कार्यकर्ता के रूप में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। यूनियन में हमें कोई मानदेय नहीं मिलता था—सिर्फ मेस में खाना, और जहां जगह मिल जाए वहां सो जाना। एक घटना आज भी मुझे याद है। एक कंपनी के मजदूरों को 3–4 महीने से वेतन नहीं मिला था और उनमें से एक का बच्चा गंभीर रूप से बीमार था। जब ठेकेदार हमसे नहीं मिला, तो मैंने वाचमैन से कहा कि उससे कहे कि उसकी बहन ओडिशा से आई है। जब वह बाहर आया और मैंने मजदूर के बच्चे का जिक्र किया, तो उसने मेरे चरित्र पर अभद्र टिप्पणी की—“तुम्हारी क्या इज्जत है, तुम तो हजारों पुरुषों के साथ घूमती हो।” यह सुनकर मैं टूट गई। यूनियन साथियों ने बाद में कंपनी के बाहर बड़ा विरोध किया, लेकिन ऐसी टिप्पणियां बार-बार होती थी जिनसे हर बार उबरना मुश्किल था।
हड़तालों के दौरान मजदूरों की कई जरूरतें सामने आती थी— बीमार बच्चों के लिए दवाएं, राशन, दूध, कॉपी-किताबें आदि। उस समय डॉक्टर बिनायक सेन यूनियन ऑफिस में हर सोमवार मजदूरों के लिए साप्ताहिक क्लीनिक चलाते थे। वह मुझे जानते थे और मेरे काम का सम्मान करते थे। वहीं की एक संस्था आरसीडीआरसी के राजेंद्र कुमार उनके अच्छे दोस्त थे। उन्हें बिनायक ने मेरे काम और मजदूरों के हालातों के बारे में बताया और कहा कि राजिम की मदद करनी चाहिए। तब उन्होने हर महीने मुझे 500 रूपए देना तय किया, जिसका इस्तेमाल मजदूर साथियों की जरूरतों के लिए किया जा सके।

जब यूनियन के पुरुष साथियों को इसका पता चला तो मुझ पर वेतन भोगी होने के आरोप लगाए गए। मुझे मंच संचालन और अन्य जिम्मेदारियां मिलनी बंद हो गयी। मैं पूरी मेहनत के साथ यूनियन का काम करती थी। ऐसे में यह मेरे लिए सबसे बड़ी आहत करने वाली घटना थी। इसके बाद मैं ट्रेड यूनियन से अलग हो गयी और वापस पिथौरा आ गई। इसी दौरान मैंने अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी भी की, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथी थे। इसे लेकर भी मुझे अपने परिवार से बहुत लड़ना पड़ा था।
किसी भी महिला के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन, पुरुष की तुलना में बहुत मुश्किल होता है। आप भले ही पुरुषों के समान संघर्ष करें, लाठी खाएं या जेल जाएं, पुरुषों के लिए किसी महिला की लीडरशिप स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। ट्रेड यूनियन हो या अन्य संस्थाएं, पुरुष अमूमन महिलाओं की लीडरशिप स्वीकार नहीं कर पाते हैं। शायद एकबार वे किसी ऊंची जाति की महिला को स्वीकार कर भी लें, क्योंकि वहां पर उनकी जाति की सत्ता भी काम करती है। लेकिन एक आदिवासी या दलित महिला के लिए यह कई गुना मुश्किल होता है, चाहे वह कितनी भी शिक्षित या काबिल हो।
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के और ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रयासों को आप कितना जरूरी मानती हैं और आज उन्हें कहां देखती हैं?
वामपंथी दलों और ट्रेड यूनियनों के समान ही छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा को भी एकता की कमी का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। हम नारा तो लगाते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो, लेकिन देखिये ना कितना विभाजन है, कितने सारे धड़े बन गए हैं। अभी भी वे इलाकों को लेकर ही उलझते रहते हैं, आपस में कोई तालमेल ही नहीं रहा। यह ठीक है कि हर संगठन की अपनी पहचान होती है, लेकिन सबके जुटने का मंच तो साझा होना चाहिए जिससे बड़ी ताकत बने।
छत्तीसगढ़ में लगातार नए कारखाने लगते जा रहे हैं। इनमें से कई जब घाटे में जाते हैं तो बंद कर दिये जाते हैं। इन्हें लगाने के लिए कितने गांव-समुदाय विस्थापित होते हैं और फिर एक दिन वे बंद हो जाते हैं। अगर ट्रेड यूनियनों और जन संगठनों में एकता होती तो इस बात को जोर-शोर से उठाया जा सकता था कि नए कारखाने लगाने की बजाय पहले बंद पड़े कारखानों को शुरू किया जाए। इन बंद कारखानों के मालिकों ने जाने कितने मजदूरों का सालों का वेतन नहीं दिया है। इसी तरह विस्थापित लोगों के पुनर्वास और सही मुआवजे जैसे मसले भी दबे ही रह जाते हैं।
ट्रेड यूनियन में एक महिला कार्यकर्ता के रूप में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। यूनियन में हमें कोई मानदेय नहीं मिलता था—सिर्फ मेस में खाना, और जहां जगह मिल जाए वहां सो जाना।
मुझे ये भी लगता है कि जन संगठनों और ट्रेड यूनियनों के कमजोर होने में एनजीओ का भी बड़ा हाथ है। पहले लोग अपनी समस्याओं के लिए जन-संगठनों के पास जाते थे। इससे लोगों का संगठन से आपसी रिश्ता और विश्वास भी बनता था। अब हर मुद्दे पर काम करने के लिए कोई एनजीओ है, तो लोग उनके पास जाते हैं। संगठनों के साथ उनका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी था। सबसे जरूरी है कि समुदाय अपने मुद्दों पर जागरूक हो सके। उसे अंदर से जब तक महसूस नहीं होगा कि उसकी जमीन, उसके संसाधन, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, तब तक आप कितनी भी ट्रेनिंग-वर्कशॉप कर लें, वह संघर्ष नहीं करेगा।
एक सामाजिक कार्यकर्ता की चुनावी राजनीति में भागीदारी को लेकर आपके क्या विचार हैं?
मुझे लगता है कि ये जरूरी है। जनक लाल ठाकुर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से 5 बार विधायक बने थे। मैं खुद भी 2003 में विधायक का चुनाव लड़ी हूं। हम जीने के अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद ही तो नियोगी जी का हत्याकांड हुआ था। ऐसे संघर्षों में हमारा, यानी मजदूरों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जरूरी होता है। जब हमारा अपना कोई सांसद या विधायक बनता है, तो वह हमारी आवाज बनता है।
यह केवल सांसद या विधायक तक ही सीमित नहीं है। गांव के सरपंच भी हमारे बीच से हों, तो वे हमारे मुद्दों को उठाते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे कौन है, किसे अवासीय योजना का लाभ मिले या किसे पेंशन मिलनी चाहिए। राजनीति में हमारे लोग होते हैं तो वे हमारा खयाल भी करते हैं। इस तरह राजनीति और सामाजिक संघर्ष साथ-साथ ही चलता है।
नियोगी जी ने जब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया था तो उनका सपना ऐसे सुंदर छत्तीसगढ़ का था, जहां शोषण नहीं बल्कि बराबरी होगी। उन्होने ‘संघर्ष और निर्माण’ का नारा दिया था। इसका अर्थ है अधिकारों के लिए खिलाफत के साथ-साथ, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका के लिए आधारभूत ढांचे भी बनाना, जिसके लिए राजनीतिक दखल जरूरी हैं। मेरा मानना है कि बिना निर्माण के कोई भी संघर्ष पूरा नहीं हो सकता।
आपके संगठन दलित आदिवासी मंच की शुरुआत कैसे हुई? इस यात्रा के बारे में बताएं?
ट्रेड यूनियन छोड़ने के बाद जब मैं पिथौरा आई तो यहां पर बंधुआ मजदूरी एक बड़ा मुद्दा था। उस समय 5 हजार से अधिक बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया था। तब मैं किसी संगठन में नहीं थी लेकिन मैंने इस मुद्दे पर स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ये 1997 की बात है। हमारा नारा था, ‘जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है।’ इस नारे के साथ बैलों के सींग पर लाल रंग लगाकर हमने 28 हजार एकड़ जमीन जोती थी। पूरे सराइपाली बसना और पिथौरा में हमने जमीन सत्याग्रह शुरू किया था। हम कहते थे, ‘जमीन दो या जेल भेजो।’ इसमें भी हमने खूब धरने-प्रदर्शन किए।
मेरा मानना था कि हमारी अपनी एक पहचान है, इसलिए हमारा अपना संगठन भी होना चाहिए। इसी सोच के साथ 2007 में हमने दलित आदिवासी मंच बनाया। तब मेधा पाटकर ने दिल्ली में जंतर मंतर पर एसईजेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र) के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें हमारे संगठन से 100 लोग गए थे, जो एक महीने तक वहीं रहे। ये हमारे साथियों के लिए संगठन और संघर्ष को समझने का बहुत अच्छा मौका था। वहां से आने के बाद हमने एक बड़ा सम्मेलन किया और दलित आदिवासी मंच की सार्वजनिक घोषणा की थी।
हमने बंधुआ मजदूरी के मुद्दे से काम की शुरुआत की लेकिन हम यह समझते थे कि सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। किसी को जब बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है तो पीछे रह गए उसके परिवार को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसके घर की महिलाएं, बच्चों की शिक्षा, परिवार की सामाजिक सुरक्षा सभी इससे प्रभावित होते हैं। समय के साथ हमारा कार्यक्षेत्र भी बढ़ता गया और मुद्दे भी। घरेलू हिंसा, बंधुआ मजदूरों को छुड़ाना, योजनाओं की लोगों तक पहुंच के लिए ग्राम सभाओं के साथ काम, स्वरोजगार, वन अधिकार और मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर हम अभी काम कर रहे हैं।
ग्रामीण इलाकों के संगठन जेंडर के मुद्दे से दूर ही रहते हैं, लेकिन आपके संगठन के लिए यह एक प्रमुख मुद्दा है। आपने यह कैसे तय किया और इसकी क्या चुनौतियां थी?
जेंडर पर काम की प्रेरणा मुझे अपने अनुभवों से मिली। हमने शुरुआत संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से की, क्योंकि हर कार्यक्रम में पुरुष ही दिखाई देते थे। हम पुरुषों से कहते थे कि जब महिलाएं घर की पूरी जिम्मेदारी निभा सकती हैं, तो वे सामाजिक कार्य में भी बराबरी से हिस्सा ले सकती हैं। इसके लिए हम घर-घर गए, महिलाओं के साथ बैठकर बात की, उनके साथ खाना बनाया, चाय बनाई और इसी प्रक्रिया में उन्हें संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

जब संगठन में महिला-पुरुष साथ आने लगे तो हम समय-समय पर घरेलू हिंसा और महिलाओं के अन्य मुद्दों पर भी बात करने लगे। छोटे-छोटे उदाहरणों के साथ हम उनसे काम के विभाजन और महिला-पुरुष समानता जैसे विषयों पर बात करते थे। मेरा मानना है कि बदलाव की शुरुआत घर के अंदर से होती है। इसलिए हम भी अपने संगठन से जुड़े घरों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। महिला स्वास्थ्य, उनके लिए पौष्टिक खाना, शिक्षा आदि जैसे विषयों पर हम लगातार संगठन में बात करते हैं।
समाज में कई तरह की गलत धारणाएं हैं। जैसे अक्सर सास-बहू के संबंध के संदर्भ में यह बात कही जाती है कि महिला ही महिला का शोषण करती है। हम इन धारणाओं पर भी समुदाय से बात करते हैं कि यह सब सत्ता की बात है, अंततः उस महिला के पीछे भी पति या बेटे के रूप में कोई पुरुष ही होता है। ऐसा ही मसला महिलाओं के जमीन के स्वामित्व का भी है। हमने वन अधिकार पर अपने काम के दौरान इस पर बहुत ध्यान दिया है। हम लगातार महिलाओं के अधिकार के लिए ये बात उठाते रहे हैं कि जंगल कौन जाता है या वनोपज कौन इकट्ठा करता है। इसी सोच के साथ हम कई जगहों पर महिलाओं के नाम पर वन अधिकार के व्यक्तिगत पट्टे भी बनवा पाए।
समुदाय के साथ विश्वास कायम करना किसी भी जन संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। यह आप कैसे करती हैं?
मुझे स्थानीय स्तर पर बहुत लोग जानते हैं। जब आप लगातार लोगों से मिलते हैं, उनकी तकलीफों और मुद्दों को सुनते हैं, तो एक विश्वास कायम होता है। हमारे क्षेत्र में घरेलू हिंसा के मामले बहुत आम हैं, और अक्सर इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। हम लोगों से कहते हैं कि पति-पत्नी के बीच मारपीट कोई निजी बात नहीं, बल्कि सामाजिक मसला है। हाल के वर्षों में बेडरूम के भीतर यौन हिंसा के मामले भी बढ़े हैं। कई लड़कियां इसे किसी से कह नहीं पाती हैं। इसलिए हम उन्हें आपस में दोस्ती करने और एक भरोसेमंद सहेली बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसे हम ‘केयर एंड शेयर’ कहते हैं। बात करने से कई बार उनकी आधी परेशानी कम हो जाती है।
महिला हिंसा के मामलों में बड़ी समझदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करना होता है। कई बार मारपीट के तुरंत बाद महिला बोलती है कि पति को जेल में डलवा दो। लेकिन फिर वही महिला बोलेगी कि अब उसे छुड़वा दो। ऐसे में हम तुरंत कुछ नहीं करते, उन्हें बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं और उनकी पूरी बात सुनते हैं। उसके बाद उनकी इच्छा के अनुसार कदम उठाते हैं।
मुद्दा चाहे महिला हिंसा का हो, जमीन का हो या कुछ और, हम यह कोशिश करते हैं कि जब अपनी समस्या के लिए लोग हमसे मदद मांगें तो हम उनके साथ हों। इसी से रिश्ता बनता है और आपसी विश्वास कायम होता है। मेरा और संगठन के कुछ अन्य साथियों का नंबर गांव-गांव में फैला हुआ है कि कोई बात हो जाए तो तुरंत फोन करो। वे भी जानते हैं कि राजिम दीदी और संगठन के साथी जरूर आएंगे।
सामाजिक कार्य के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका में युवा महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है?
मुझे लगता है कि पुरानी पीढ़ी की महिलाओं के अनुभव नई पीढ़ी के साथ बांटने से हमारे गांवों में अच्छी नेत्रियां पैदा हो सकती हैं। आज के समय में दूसरी पंक्ति के लीडर्स तैयार करना बहुत जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि अपने गांव में ऐसे लीडर पैदा हों जो मुद्दों को उठा सकें। इसके लिए उन्हें पता होना चाहिए कि कमिश्नर, तहसीलदार या अन्य अधिकारियों से कैसे बात करें, थाने में कैसे बात करें। इन सबसे लोग आज भी बहुत डरते हैं। ये डर तभी निकलेगा जब हम ये समझेंगे कि ये थाना और ये अधिकारी हमारे प्रति जिम्मेदार हैं। एक अच्छे नेता का अंदर से जागरूक रहना और काम के प्रति जुनून बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी की लड़कियों को मेरा यही संदेश है कि एक सामाजिक सोच के साथ छोटे से छोटे मुद्दे पर काम करें, गांव में लोगों के अंदर जोश और जुनून पैदा करें। आप जरूर सफल होंगी।
—




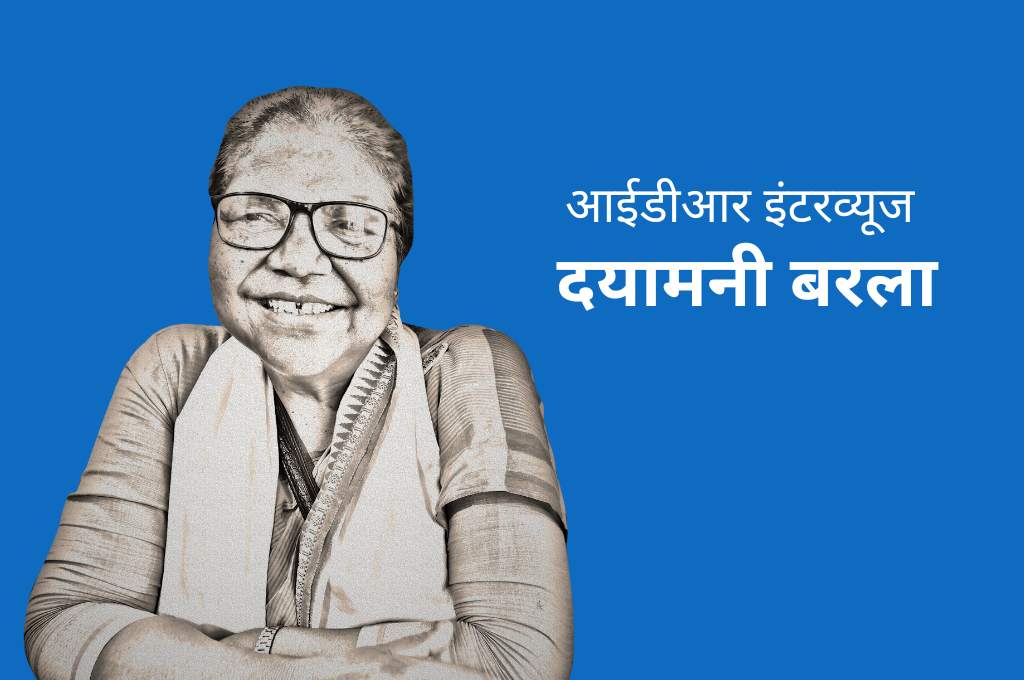

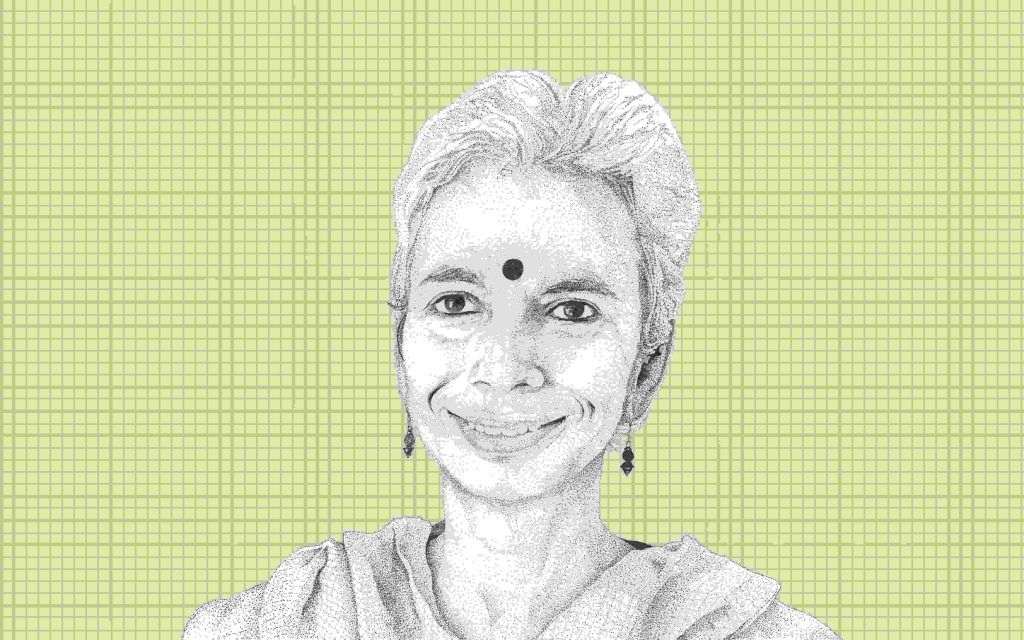
गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपके ईमेल का पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *