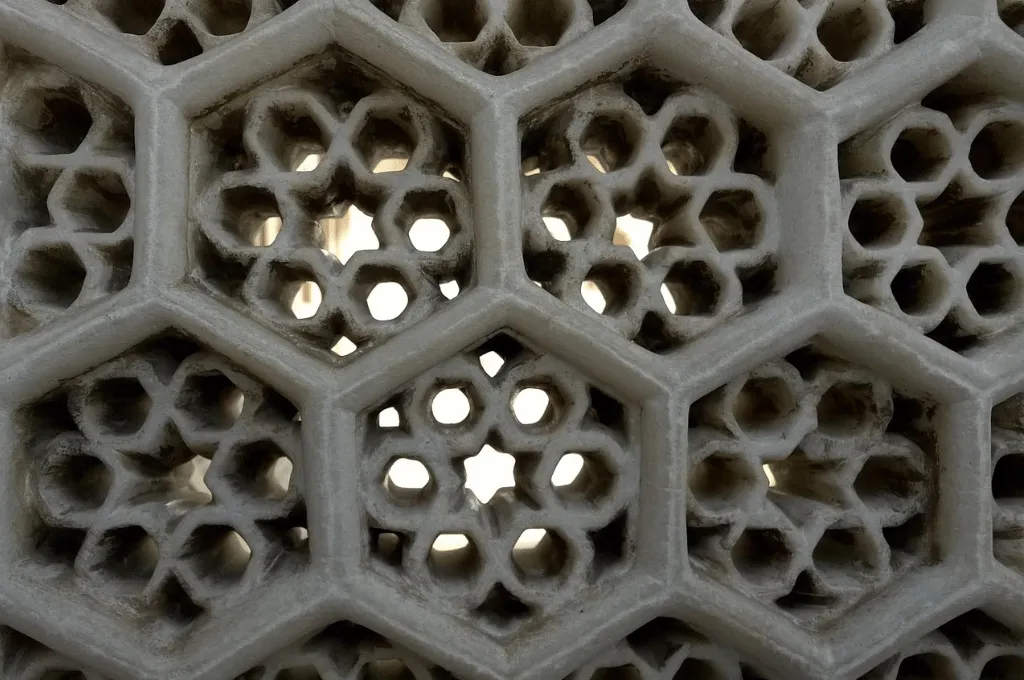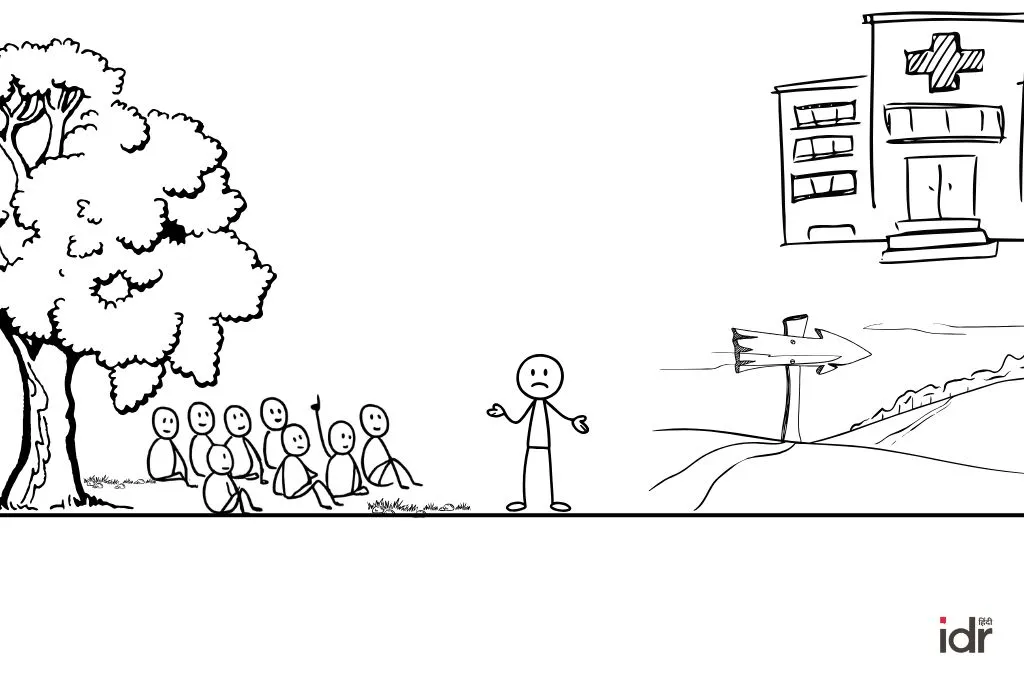संस्थाओं के लिए फंडरेजिंग के कुछ कारगर उपाय
भारत में हजारों गैर-लाभकारी संस्थाएं अपने सीमित संसाधनों और गहरी प्रतिबद्धता के साथ सामाजिक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रहती हैं। लेकिन जब संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता की बात आती है, तो अधिकतर संस्थाएं वित्तीय अनिश्चितता से जूझती हैं।
हाल ही में एटीई चंद्रा फाउंडेशन की रिपोर्ट ‘कैसे रणनीतिक निवेश एनजीओ की फंडरेजिंग सफलता और लचीलापन बढ़ा सकते हैं (2025)’ ने सामाजिक क्षेत्र की एक चिंताजनक तस्वीर पेश की है। इस सर्वेक्षण में सामने आया कि लगभग आधी संस्थाओं के पास तीन महीने से भी कम का रिजर्व फंड (ऐसा पैसा जो संकट के समय वेतन, किराए और आवश्यक खर्चों के लिए सुरक्षित रखा जाता है) बचा था। वहीं, बाकी आधी संस्थाएं बीते तीन वर्षों में कोई अतिरिक्त फंड नहीं जुटा सकी।
ये आंकड़े बताते हैं कि जब फंडिंग रुकती है, तो उसका असर केवल संस्थाओं पर नहीं, बल्कि उन हजारों जिंदगियों पर भी पड़ता है जिनके लिए वह काम कर रही होती हैं। इसलिए वित्तीय लचीलापन (संस्था की आर्थिक अस्थिरता से उबरने और काम को जारी रखने की क्षमता) केवल बचत नहीं, बल्कि एक सोच और रणनीति है।
आत्मा संस्था के अंतर्गत हम ‘फ्यूचर ऑफ इम्पैक्ट’ (एफओआई) कार्यक्रम के तहत विभिन्न संस्थाओं की बेहतरी के लिए उनके साथ क्षमतावर्धन कार्यक्रम चलाते हैं। इस लेख में ऐसे व्यावहारिक उपाय साझा किए गए हैं, जिनसे संस्थाएं खुद को एक बेहतर वित्तीय भविष्य के लिए तैयार कर सकती हैं।
1. रिजर्व फंड बनाना शुरू करें
अभी भी अधिकांश संस्थाएं केवल ग्रांट्स (वित्तीय सहायता जो किसी संस्था, सरकार, फाउंडेशन या दाता द्वारा किसी विशेष कार्य, परियोजना या उद्देश्य के लिए दी जाती है) पर निर्भर रहती हैं। संकट की घड़ी में किसी भी संस्था को 3 से 6 महीने तक चलाए रखने के लिए रिजर्व फंड (ऐसा पैसा जो संकट के समय वेतन, किराए और आवश्यक खर्चों के लिए सुरक्षित रखा जाता है) स्थिरता प्रदान करता है। यह एक बार में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे हर साल थोड़ा-थोड़ा करके जोड़ा जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों में संचालन की निरंतरता और भावी रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने हेतु संस्थाओं के लिए एक मजबूत रिजर्व फंड नीति आवश्यक है। यह नीति दस्तावेज रिजर्व फंड के निर्माण, रख-रखाव और उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- रिजर्व फंड का उद्देश्य संगठन को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है ताकि किसी आपात स्थिति, धन की अस्थायी कमी या भविष्य के योजनागत निवेशों के लिए तैयारी की जा सके।
- रिजर्व फंड में कम से कम 3 से 6 महीनों के औसत संचालन खर्च के बराबर राशि बनी रहनी चाहिए।
- रिजर्व फंड का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में या बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बाद किया जाना चाहिए। प्रत्येक निकासी का उद्देश्य, राशि और पुनःस्थापना योजना दस्तावेज में दर्ज होनी चाहिए।
- यदि रिजर्व फंड से कोई राशि निकाली जाती है, तो उसे 1-2 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से पुनः जोड़ा जाए।
- रिजर्व फंड की सालाना समीक्षा की जाए, ताकि पर्याप्त राशि सुनिश्चित की जा सके। वित्त समिति या बोर्ड इसकी निगरानी और जरूरत अनुसार संशोधन करे।
इंचारा फाउंडेशन की एथेना अरान्हा बताती हैं कि एफओआई कार्यक्रम से जुड़ने के बाद उन्होंने वित्तीय असुरक्षा को दूर करने के लिए कई ठोस कदम उठाए — जैसे पूर्णकालिक अकाउंटेंट की नियुक्ति, लेन-देन की नियमित समीक्षा, और बोर्ड को तिमाही वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब संस्था न केवल बजट को लेकर अधिक आत्मविश्वासी है, बल्कि फंडर्स के सामने अपनी जरूरतें भी स्पष्टता से रख पाती है।
2. फंडिंग स्रोतों में विविधता लाएं
संस्थाओं के लिए केवल एक या दो फंडर पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण हो सकता है। संस्थाएं आमतौर पर 3–4 विभिन्न स्रोतों से फंडिंग प्राप्त करती हैं। उदाहरण के लिए, सीएसआर ग्रांट्स, फैमिली फाउंडेशन, व्यक्तिगत दानदाता, और सरकारी या अंतरराष्ट्रीय फंडिंग इत्यादि।

यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए जा रहे हैं ताकि आप अपनी संस्था के लिए नए फंडर जोड़ सकें:
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें: गाइडस्टार इंडिया, सीएसआरबॉक्स, संहिता, दसरा जैसी वेबसाइट्स पर नियमित फंडिंग अवसर साझा किए जाते हैं।
- नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लें: एनजीओ एक्सपो, सीएसआर सम्मेलन या क्षेत्रीय नेटवर्क मीटिंग्स में संपर्क बनाएं। नैसकॉम फाउंडेशन या इम्पैक्ट कलेक्टिव जैसे स्थानीय नेटवर्कों से जुड़ें।
- लिंक्डइन और सोशल मीडिया का प्रयोग करें: सीएसआर लीड्स, फाउंडेशन्स और डोनर संस्थाओं के अपडेट्स को सक्रिय रूप से ट्रैक करें।
- सालाना रिपोर्ट को रणनीतिक दस्तावेज बनाएं: सालाना रिपोर्ट सिर्फ गतिविधियों का लेखा-जोखा न हो, बल्कि यह भी दिखाए कि संस्था ने किन डोनर्स के साथ मिलकर कौन-से लक्ष्य तय किए और उन्हें किस स्तर तक हासिल किया। यह दृष्टिकोण फंडर्स के साथ भरोसे और दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत बनाता है।
- वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करें: संस्था के खातों में वित्तीय पारदर्शिता सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि फंडर्स के भरोसे की नींव भी है। आय-व्यय का स्पष्ट और समयबद्ध रिकॉर्ड इस भरोसे को और दृढ़ता देता है।
- व्यक्तिगत दाताओं से संवाद बनाए रखें: न्यूजलेटर जैसे माध्यमों से नियमित रूप से संस्था के काम की प्रगति, लाभार्थी कहानियों और प्रभाव को साझा करें। यह सार्वजनिक धन (जो सरकार या किसी सार्वजनिक संस्था के पास करों, शुल्कों, दान, या अन्य सार्वजनिक स्रोतों से आता है और जिसका उपयोग जनहित जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास परियोजनाओं आदि में किया जाता है) के प्रति जवाबदेही दर्शाता है और व्यक्तिगत दाताओं के साथ भरोसे पर आधारित दीर्घकालिक संबंध बनाने में मदद करता है।
- नियमित दान और सामुदायिक फंडरेजिंग को अपनाएं: नियमित दान (रेकरिंग गिविंग) और सामुदायिक फंडरेजिंग एक ऐसी रणनीति है, जहां संस्था अपने स्वयं के समुदाय — जैसे स्थानीय नागरिक, लाभार्थियों के परिवार, स्वयंसेवक आदि से छोटी-छोटी रकम जुटाती है। उदाहरण के लिए, कुछ संस्थाएं हर त्योहार पर अपने समुदाय से नियमित योगदान प्राप्त करती हैं, जिससे सालभर की स्थिरता बनी रहती है। इससे संस्था को फंडिंग के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी भी प्राप्त होती है।
यूथ ड्रीमर्स फाउंडेशन से रिया कुमार बताती हैं कि सीएसआरबॉक्स, गिव डॉट डू और लेट्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़ने से उन्हें फंडिंग की दिशा में काफी स्पष्टता मिली और नए फंडर्स तक पहुंचना आसान हुआ। नतीजतन कुछ ही महीनों में 40 से अधिक संभावित फंडर्स से संपर्क कर 50 लाख से अधिक की सीएसआर फंडिंग जुटाई गई।
3. फंडर्स के साथ वास्तविक लागत (ट्रू कॉस्ट) पर बात करें
कई बार संस्थाएं केवल प्रोजेक्ट आधारित बजट साझा करती हैं और संचालन के वास्तविक खर्चों को नजरअंदाज कर देती हैं। अब समय है कि फंडर्स के साथ वास्तविक लागत (यानी संस्था की पूरी लागत, जिसमें अप्रत्यक्ष खर्च जैसे दफ्तर का किराया, तकनीक, प्रशासन आदि शामिल हों) पर खुलकर बातचीत की जाए।
अब कई फंडर्स ऑर्गनाइजेशनल डवेलपमेंट (संस्था की आंतरिक क्षमता निर्माण) पर आधारित ग्रांट देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप अपनी जरूरतों को स्पष्ट और पेशेवर ढंग से प्रस्तुत करें। यह संवाद संस्था को कोर फंडिंग (मूलभूत संचालन खर्च के लिए फंडिंग) की दिशा में ले जा सकता है।
इस विषय पर हर हाथ कलम संस्था के हर्ष कोठारी बताते हैं कि पहले वह केवल प्रत्यक्ष परियोजना लागतों पर ही बात करते थे, क्योंकि अधिकांश दानदाता ओवरहेड्स को स्वीकार नहीं करते थे। एफओआई कार्यक्रम से उन्हें यह समझ मिली कि ‘वास्तविक लागत’ पर भी प्रभावशाली और रणनीतिक संवाद किया जाना चाहिए। अब उन्होंने अपने बजट में संचालन, मानव संसाधन, तकनीक और निगरानी जैसी अप्रत्यक्ष लागतों को भी स्पष्ट रूप से शामिल करना शुरू किया है। उन्होंने रिपोर्टिंग को प्रभाव आधारित बनाया और दानदाताओं से पारदर्शिता और डेटा के साथ संवाद किया। इस बदलाव के परिणामस्वरूप उन्हें एक संस्थागत अनुदान और कई एचएनआई फंडर्स से पूर्ण लागत आधारित समर्थन मिला। यह अनुभव उनके लिए एक अहम सीख बना कि जब संगठन स्पष्टता, प्रमाण और विश्वास के साथ संवाद करते हैं, तो दानदाता भी उनका साथ देने को तैयार रहते हैं।
4. वित्तीय स्थिति की मासिक समीक्षा करें
वित्तीय लचीलापन तभी आता है, जब संस्था के फाइनेंशियल हेल्थ (संस्था की आर्थिक स्थिति और संतुलन) की नियमित निगरानी की जाए। कई सफल संस्थाएं हर महीने अपनी नकद स्थिति, फंडिंग गैप (जरूरत और उपलब्धता में अंतर) और रिजर्व फंड की समीक्षा करती हैं। संस्थाओं को अपनी बोर्ड मीटिंग्स के लिए वित्तीय रिपोर्ट को नियमित एजेंडा में शामिल करना चाहिए। टीम के साथ महीने में एक बार खर्चों और फंडिंग पर बातचीत करें, ताकि समय रहते उचित निर्णय लिए जा सकें।
वित्तीय लचीलापन तभी आता है, जब संस्था के फाइनेंशियल हेल्थ की नियमित निगरानी की जाए।
सनराइज लर्निंग संस्था की चारू सिंह अपना अनुभव साझा करते हुए बताती हैं कि पहले उनकी संस्था में वित्तीय रिपोर्टों की नियमित आंतरिक समीक्षा नहीं होती थी। यानि जब तक ऑडिट पूरा होता, तब तक वित्तीय वर्ष का आधा हिस्सा बीत चुका होता था। कार्यक्रम से समझने के बाद उन्होंने 2024–25 में कार्यक्रमवार लागत और फंडिंग का विश्लेषण शुरू किया, ताकि सरप्लस और घाटे की स्थिति स्पष्ट हो सके। 2025–26 में उन्होंने हर खर्च और आय स्रोत को बेहतर वर्गीकरण के साथ दर्ज करना शुरू किया, जिससे वित्तीय निर्णय अधिक सटीक और पारदर्शी बन सकें।
5. दीर्घकालिक वित्तीय रणनीति बनाएं
हर साल फंडिंग के लिए भाग-दौड़ करने के बजाय, संस्थाओं को 3 से 5 वर्षों की एक स्पष्ट वित्तीय रणनीति बनानी चाहिए। इसमें यह तय किया जाए कि हर साल संस्था अपने रिजर्व फंड को कितना बढ़ाना चाहती है, किन स्रोतों से फंडिंग बढ़ाई जा सकती है और किन नए डोनर्स से जुड़ने की संभावनायें हैं। साथ ही, यह भी समीक्षा करें कि क्या संस्था के खर्च व्यावहारिक और प्राथमिकताओं के अनुसार हैं, या उनमें किसी तरह के सुधार की जरूरत है।
यह रणनीति केवल डायरेक्टर या फाइनेंस टीम तक सीमित न हो, बल्कि पूरी संस्था इसे समझे और अपनाए। इसके साथ ही वित्तीय लचीलापन विकसित करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं:
- कम संसाधनों में काम करना अच्छी बात है, लेकिन दीर्घकालिक क्षमता और स्थिरता को प्राथमिकता देना जरूरी है।
- केवल ऑडिट रिपोर्ट्स के बजाय रणनीतिक निर्णयों को महत्व दें।
- एक वर्ष की परियोजना फंडिंग से स्थायी बदलाव संभव नहीं हो सकता; उसके लिए भरोसे और साझेदारी की जरूरत होती है।
यह बदलाव केवल संस्थाओं से नहीं, सभी हितधारकों से अपेक्षित है।
इसलिए फंडर्स से अपेक्षा है कि संस्थाओं के साथ मिलकर दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं और लचीली फंडिंग सुनिश्चित करें। संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसे संगठनों के साथ सक्रिय संवाद बनाएं और बिना शर्त फंडिंग जुटाने की दिशा में ठोस प्रयास करें।
स्टेट स्ट्रीट फाउंडेशन की वाइस प्रेसीडेंट व सीनियर ग्रांट्स मैनेजर, डॉ. मीनू भांभानी बताती हैं कि उनकी संस्था बिना शर्त फंडिंग में विश्वास रखती है, जिससे एनजीओ अपनी जरूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं — चाहे वह नेतृत्व विकास हो, प्रणाली सुधार या नई चुनौतियों पर त्वरित प्रतिक्रिया। वह बताती हैं कि जब वे फंड के उपयोग से सीमाएं हटाते हैं, तो यह लचीलापन संस्थाओं को ही नहीं बल्कि पूरे सामाजिक क्षेत्र को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाता है।
आत्मा में हम फंड को केवल सहायक भूमिका के रूप में न देखकर, इसे अपने दैनिक संचालन का एक मुख्य हिस्सा मानते हैं। अपनी संस्था में मेरे (स्नेहा अरोड़ा) द्वारा हर महीने वित्तीय टीम की समीक्षा की जाती है, जिसमें बजट बनाम वास्तविक खर्च, नकद प्रवाह, बैंक बैलेंस और अनुपालन से जुड़े कार्यों पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है। इन समीक्षाओं की मदद से यह समझने में मदद मिलती है कि भविष्य में पैसों के लेन-देन में कोई परेशानी या रुकावट आ सकती है या नहीं। इससे संस्था की लीडरशिप टीम फंडिंग या नियमों से जुड़ी अनिश्चितताओं के लिए पहले से बेहतर तैयारी कर सकती है।
अंततः जिस तरह कॉर्पोरेट क्षेत्र में संगठनात्मक विकास और वित्तीय स्थिरता को व्यवसाय की आधारशिला माना जाता है, वैसे ही गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए भी वित्तीय लचीलापन केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभाव की निरंतरता की शर्त है। जब संस्थायें मजबूत होती हैं, तो देश की समावेशी और सतत विकास को भी बल मिलता है।
—
अधिक जानें
लेखक के बारे में
- तरुणा राव आत्मा संस्था में बतौर सीनियर कंसलटेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एवं कम्युनिकेशन्स से जुड़ी हुई हैं। तरुणा एक विकास पेशेवर हैं, जिन्हें आईटी, शिक्षण, संचार और ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता संसाधन-संग्रहण, साझेदारी निर्माण, रणनीतिक संचार और ब्रांड निर्माण में है। वह मानती हैं कि प्रभावशाली संवाद और साझेदारी किसी भी सामाजिक पहल की दिशा और पहुंच को व्यापक बना सकते हैं।
- स्नेहा अरोड़ा पिछले 6 वर्षों से आत्मा संस्था में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे फंडरेजिंग, गवर्नेंस और कम्युनिकेशन टीमों का नेतृत्व करती हैं। उनके पास निजी और विकास सेक्टर में लगभग 15 वर्षों का अनुभव है। स्नेहा ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया है और स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग और कॉरपोरेट फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में काम कर चुकी हैं। उन्हें वर्ष 2022 में अक्युमन फेलो चुना गया था।