भारत में कुपोषण निर्मूलन के प्रयासों में बीते सालों में बड़े स्तर पर बदलाव आया है। 1993 की राष्ट्रीय पोषण नीति (नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी या एनएनपी) में पोषण संबंधी सीधे प्रयासों के समान ही, सामाजिक दिशा में अप्रत्यक्ष प्रयासों पर भी जोर दिया गया। पोषण संबंधी सीधे प्रयासों में कार्यक्रमों का विस्तार, फूड फोर्टिफिकेशन और किफायती पौष्टिक खाने की उपलब्धता जैसे विषय आते हैं। इसी तरह सामाजिक प्रयासों में खाद्य सुरक्षा बेहतर बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा द्वारा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने से जुड़े प्रयास आते हैं। 2018 में इसका विस्तार पोषण अभियान के रूप में हुआ जिसमें पोषण पर केंद्रित प्रयासों पर जोर दिया गया। इसके बाद 2021 में भारत सरकार मिशन पोषण 2.0 लेकर आई जिसमें कुपोषण के विरुद्ध पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवा और किशोरी योजना (एसएजी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का साझा प्रयोग तय किया गया।
कुपोषण समाप्त करने के लिए मिशन पोषण 2.0; सेवाओं के पोषण पक्ष पर अधिक ध्यान देने, सेवा आपूर्ति तंत्र में बेहतरी लाने और सम्मिलित प्रयासों के लिए वातावरण बनाने पर बल देता है। एक ऐसा वातावरण जो नागरिक के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के साथ बेहतर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दे।
पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे के जन्म से लेकर शुरुआती 1000 दिनों तक मां और शिशु, दोनों को जरूरी स्वास्थ्य सहयोग मिले। यह समय उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे अहम माना जाता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभियान चार आधारों पर काम करता है—तकनीक का इस्तेमाल, साझा कार्य-योजना, व्यवहार में बदलाव पर संवाद और क्षमता निर्माण।
पोषण पर झारखंड की स्थिति
इन सभी प्रयासों के बाद भी झारखंड में कुपोषण एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) -5 के अनुसार राज्य में बच्चों में कम लंबाई (स्टंटिंग) का आंकड़ा 40% है जो एनएफएचएस-4 में 45% था। इसी तरह दुबलेपन (वेस्टिंग) में 29% से 22% की कमी दर्ज की गयी है, लेकिन 6-59 महीने के 67% बच्चों में खून की कमी (एनीमिया) पाई गयी है।
बीएमआई या शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक के आधार पर झारखंड में 26.2% महिलाओं का वजन कम है और 11.9% महिलाओं में अधिक वजन की समस्या मौजूद है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के संदर्भ में ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। गर्भावस्था में मां का वजन कम होने के प्रभाव भ्रूण के असंतुलित विकास, जन्मदर में कमी और शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी तत्काल और दूरगामी समस्याओं के रूप में दिख सकते हैं।

गरीबी और खाद्य असुरक्षा के कारण राज्य को पोषण और स्वास्थ्य संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच, उचित सफाई व्यवस्था न होना और विशेष रूप से महिलाओं में साक्षरता की कमी से ये और बढ़ जाती हैं। इसी तरह बारिश पर निर्भर खेती, खाने की आदतों में पारंपरिक तरीकों का प्रभाव, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियां जैसे कारण इन्हें प्रभावित करते हैं। इनके साथ समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव, स्वास्थ्य और शिशु देखभाल को लेकर महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता सीमित करता है। इसका असर मां और शिशु के स्वास्थ्य पर भी होता है।
1. सेवाओं की आपूर्ति, निगरानी और रेफरल की चुनौतियां
(क). जमीनी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रभावी नियोजन से समुदाय के स्तर पर ही कुपोषण का सामना किया जा सकता है। शुरुआत में ही कुपोषण के मामलों की पहचान और प्रबंधन के लिए व्यवस्थित योजना और स्वास्थ्य व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण जरूरी है। इस संदर्भ में जमीनी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शुरुआत से ही बड़ा मुद्दा रहा है।
गर्भावस्था के समय और जन्म के बाद मां और शिशु का वजन मापना, और उनके विकास पर नजर रखना, पोषण से जुड़े सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण मानक हैं। झारखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के वजन माप की दर (वेइंग एफिशिएंसी) काफी कम है, जिसके कई कारण हैं। जैसे वजन नापने की मशीन के प्रयोग की सही जानकारी न होना, बच्चे की उम्र के अनुसार विकास चार्ट पर वजन दर्ज ना करना, बच्चे के विकास में गिरावट और कुपोषण पर नजर रखने के तय नियमों का पालन ना करना जैसी कमियां जमीन पर लगातार देखने को मिलती हैं। ये दिक्कतें सीधे तौर पर जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से जुड़ी हैं। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों में कई जरूरी बातें भी पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाई हैं जैसे कि गर्भावस्था में सही तरह से वजन बढ़ना, जरूरी सेवाओं के साथ आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम का सेवन करना, और असंक्रामक बीमारियों पर ध्यान देना, वगैरह।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिशु विकास की निगरानी सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन के विकास (ग्रोथ) चार्ट के प्रयोग और घरों का दौरा करने से जुड़ी जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही, उन्हें गर्भवती माताओं, बच्चों व खयाल रखने वाले लोगों को आवश्यकतानुसार परामर्श और काउंसलिंग देने के लिए भी उचित प्रशिक्षण की जरूरत होती है। झारखंड में इस पर तत्काल ध्यान देने और ढांचागत रूप से सोचने की जरूरत है। मासिक बैठकों में भी कुपोषण पर नीतिगत और निर्णायक चर्चाओं से ज्यादा प्रशासनिक मामलों पर ध्यान दिया जाता है। इस कारण कई जगहों पर जमीनी कार्यकर्ताओं में कुपोषण के आंकड़ों की सटीक सूचना देने के प्रति उदासीनता आती है, जो कुपोषण की कम रिपोर्टिंग के रूप में दिखता है।
(ख). स्थानीय स्तर पर सेवाओं की पहुंच
आंगनवाड़ी सेंटर अक्सर गांव में ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पहुंचना आसान होता है या जो सड़कों से जुड़े होते हैं। लेकिन पहाड़ी और दुर्गम इलाकों की महिलाओं और बच्चों को इन तक पहुंचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) और शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवस (यूएचएनडी) गांवों और शहरी बस्तियों (स्लम) में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी सेवाएं पहुंचाने के महत्वपूर्ण मंच हैं। इनकी सफलता सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), आशा और आंगनवाड़ी कर्मी जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं, सामुदायिक प्रतिनिधियों और सही जगह के चुनाव, सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता, लोगों के प्रबंधन हेतु अन्य भागीदारों के आपसी सहयोग पर निर्भर करती है। हालांकि जमीन पर इसकी साफ कमी दिखती है, जो वजन नापने के अप्रभावी तरीकों और अपर्याप्त परामर्श के रूप में सामने आती है।
इसी तरह शिशु और मातृ सुरक्षा (एमसीपी) कार्ड का सही प्रयोग नहीं किया जाता जिसमें विकास निगरानी चार्ट के हिस्से को खाली छोड़ दिया जाता है। एमसीपी कार्ड, संवाद का एक माध्यम है जो जमीनी कार्यकर्ता से मां तक बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से जुड़ी उचित जानकारी, निर्देश और परामर्श पहुंचाता है। एमसीपी कार्ड का यह उद्देश्य जमीन पर पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता है।
(ग). कुपोषण उपचार केंद्र में रेफरल
कुपोषित बच्चे की पहचान होने पर उसे कुपोषण उपचार केंद्र (एमटीसी) में भर्ती करवाना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समक्ष बड़ी चुनौती है। बच्चे के परिवार को लगभग दो हफ्तों के लिए उसे एमटीसी में भर्ती करने के लिए तैयार करना मुश्किल होता है। देखभाल करने वालों और आशा कर्मी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन के होने के बावजूद कई लोग रेफरल की सलाह नहीं मानते हैं। इसका एक मुख्य कारण मां और परिवार पर खेती, घर और पशुओं की देखभाल जैसी जिम्मेदारियों का होना भी होता है। इन तथ्यों की जानकारी सभी को है लेकिन जमीन पर व्यवहारिक उपाय खोजना और उन्हें व्यवस्थागत समाधानों में शामिल किया जाना अभी बाकी है।
कई प्रखंडों में एमटीसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) के स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं और वे जिला अस्पताल में ही होते हैं, इस कारण दूर दराज के इलाकों के परिवारों के लिए कुपोषित बच्चों को एमटीसी ले जाना और कठिन हो जाता है।
2. समुदाय को एकजुट करने और बच्चों की देखभाल के तरीकों से जुड़ी चुनौतियां
(क). पूरक आहार की निम्न दर
एनएफएचएस-5 के अनुसार केवल 39% बच्चों को ही समय से पूरक आहार मिल पाता है। पूरक आहार वे खाद्य पदार्थ हैं जो पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए 6 महीने से अधिक उम्र के शिशु को स्तनपान के साथ-साथ दिये जाते हैं। इस विषय पर विशेष रूप से महिलाओं के साथ सामुदायिक संपर्क से खान-पान के तरीकों में सुधार देखने को मिलता है। स्थानीय पौष्टिक सामग्रियों के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारियों के प्रसार से इसे और बेहतर किया जा सकता है। इसके भी साक्ष्य मिलते हैं कि 7 महीने से 3 साल तक की आयु के बच्चों के लिए सामुदायिक स्तर पर पालनाघर (क्रेच) के कार्यक्रम पोषण संबंधी प्रयासों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। विशेष रूप से दूर-दराज के इलाकों के उन कामकाजी लोगों के लिए जिन्हें बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल ले जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं।
(ख). किशोरियों से जुड़ी समस्याएं
कुपोषण और खून की कमी (एनीमिया) किशोरियों के बीच एक बड़ी समस्या है। साथ ही उन्हें गरीबी, लैंगिक असमानता, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और शिक्षा संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना होता है।
जीवन के हर महत्वपूर्ण चरण या ‘क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ साइकल’ पर प्रयास किए जाने की जरूरत है।
पोषण, केवल बच्चे या एक तय उम्र तक सीमित नहीं है, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे जीवनकाल के अनुसार प्रयास किए जाने (लाइफसाइकल बेस्ड अप्रोच) की जरूरत है। इसमें शिक्षा, खेल, कौशल विकास और सामुदायिक सहयोग जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब एक कुपोषित लड़की बड़ी होती है, और फिर बाल विवाह के कारण कम उम्र में ही मां बन जाती है तो उसके बच्चे के कुपोषित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसमें फिर जीवन बचाने, जीवन की गुणवत्ता और शिक्षा जैसे पहलू आगे जुड़ते चले जाते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए जीवन के हर महत्वपूर्ण चरण या ‘क्रिटिकल स्टेज ऑफ लाइफ साइकल’ पर प्रयास किए जाने की जरूरत है।
3. समुदाय के अधिकारों और प्रशासनिक व्यवस्था तक पहुंच बढ़ाना
(क). जवाबदेही के स्थानीय तंत्र
पोषण संबंधी कार्यक्रमों के मूल्यांकन यानी जवाबदेही तय करने के संस्थागत प्रबंध तो किए गए हैं, लेकिन इसमें ग्राम सभा और पंचायतों के जरिये समुदाय को जोड़ने की जरूरत है। सरकार की तरफ से यह प्रावधान किया गया है कि पंचायत अपने क्षेत्र में पोषण संबंधित काम की निगरानी करे। इनमें भोजन की उपलब्धता, आंगनवाड़ी सेंटर व जमीनी कार्यकर्ता का काम और पहले एक हजार दिन में मां और बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं।
स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन बहुत प्रभावी हो सकता है और इसके ना होने से जिन लोगों तक यह कार्यक्रम नहीं पहुंचते हैं, वे छूट ही जाते हैं। उनकी अगली पीढ़ी में भी कुपोषण, बालविवाह, कम उम्र की गर्भावस्था जैसी समस्याएं आने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए आखिरी व्यक्ति तक सेवाएं या लास्ट माइल सर्विसेस पहुंचाने के लिए यह बहुत जरूरी है।
(ख). डिजिटल तकनीक और पीछे छूटते समुदाय
आधार से जुड़ी तकनीकी समस्याओं जैसे बायोमैट्रिक का मिलान ना होने या दस्तावेजों की कमी या मोबाइल नंबर लिंक ना होने से कई लोग पीडीएस, मनरेगा और पेंशन जैसी आधारभूत सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। पोषण ट्रैकर में फेस रिकग्निशन सिस्टम यानी चेहरे से मिलान करने की प्रणाली को शामिल किए जाने से कई महिलाएं और बच्चे आंगनवाड़ी से मिलने वाले सूखे राशन या टेक होम राशन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और परिवार अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।
यह सीधे रूप से संवेदनशीलता से जुड़ा है कि क्या तकनीकी कारणों से किसी जरूरतमंद को इन सेवाओं से वंचित किया जाना चाहिए। तकनीकी और आर्थिक पहलू अपनी जगह हैं, लेकिन देश के जिन लोगों के लिए यह किया जा रहा है, उन्हें केंद्र में रखकर इन कार्यक्रमों के बारे में सोचे जाने की जरूरत है।
झारखंड सरकार, विशेष रूप से 6-59 महीने के बच्चों में कुपोषण और एनीमिया के उन्मूलन के लिए समर (एसएएमएआर) नामक कार्यक्रम चला रही है। पोषण कार्यक्रमों के केन्द्रित प्रयासों और डिजिटल माध्यमों पर विशेष ध्यान दिये जाने के बाद भी राज्य में कार्यान्वयन से जुड़ी कई समस्याएं हैं। इनके संदर्भ में जमीनी कार्यकर्ताओं का उचित प्रशिक्षण, कार्यक्रमों का सही व समय पर मूल्यांकन और उनमें स्थानीय प्रशासनिक निकायों की भागीदारी, समुदाय से बेहतर संवाद, और तकनीक का प्रयोग जैसे कुछ प्रमुख बिन्दु हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
इन सभी को देखते हुए स्थानीय समुदायों के अनुरूप जमीनी कार्यान्वयन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो समुदाय की पोषण संबंधी जरूरतों और जरूरी स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति तंत्र की दक्षता के बीच संतुलन कायम कर सके।
इस लेख में साझा की गयी जानकारी और विचार पूर्णतया लेखक के निजी विचार हैं।
—




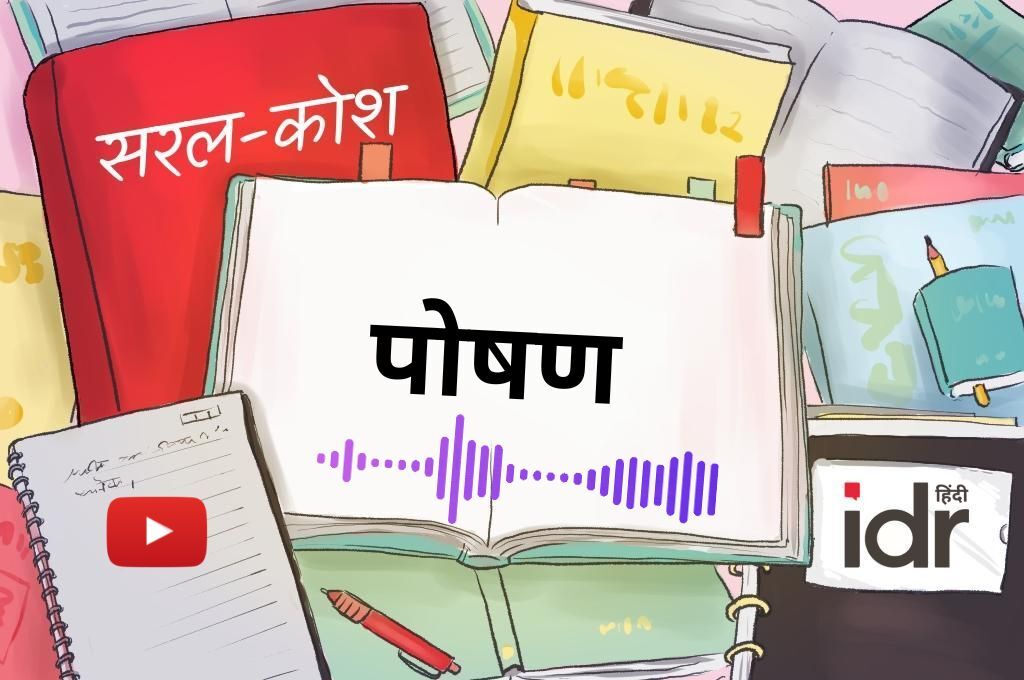
गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपके ईमेल का पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *