अमूमन देखा जाता है कि मूलनिवासी और आदिवासी समुदायों को राज्य की विकास परियोजनाओं का दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। कई परियोजनाओं के तहत बांध निर्माण, खनन के लिए जमीन और जंगलों के अधिग्रहण जैसे फैसलों ने इन समुदायों की पारंपरिक आजीविका और जीवनशैली को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में स्थित, पुणे जिले के अंबेगांव ब्लॉक में रहने वाले कातकरी, ठक्कर और महादेव कोली समुदायों ने भी इस तथाकथित विकास की भारी कीमत चुकाई है। लेकिन हमारी कहानी प्रतिरोध, एकजुटता और तंत्र की चुनौतियों के विरुद्ध अडिग संकल्प की अहमियत को दर्शाती है।
पीढ़ियों से कातकरी समुदाय घोड़ और बुबरा नदियों में मछली पकड़ने पर निर्भर था, जबकि महादेव कोली समुदाय आसपास की जमीन पर धान, गेहूं और सब्जियां उगाकर जीवन यापन करता था। मैं स्वयं महादेव कोली समुदाय का सदस्य हूं। वर्ष 1972 में कृष्णा बेसिन पर डिंभे बांध परियोजना की शुरुआत हुई। वर्ष 2000 में जब यह बांध तैयार हुआ, तब तक इसके कारण इन दोनों समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहद लचर हो चुकी थी।
जैसे-जैसे बांध में पानी भरना शुरू हुआ, आसपास की उपजाऊ जमीनें उसकी जलधारा की चपेट में आने लगी। वर्ष 2000 में जब बांध के फाटकों की स्थापना हुई, तब तक 25 गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से विस्थापित हो चुके थे। इनमें से 12 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए थे, जिससे सैकड़ों परिवारों की जमीन और आजीविका उनसे छिन गयी। कातकरी समुदाय के पास जलाशय में मछली पकड़ने के जो सीमित अधिकार थे, वर्ष 2006 तक वह भी बाहरी ठेकेदारों द्वारा हथिया लिए गए। इस तरह यह समुदाय लगातार हाशिये पर धकेला जाता रहा। स्थायी आवास, नियमित आय और गुजारे लायक खेती या मछली पकड़ने के अभाव में कई परिवारों को मजदूरी करने पर विवश होना पड़ा। वह आसपास के ईंट-भट्ठों में काम करने लगे। यह एक ऐसा पेशा था, जिसने उन्हें कर्ज और बंधुआगिरी के दुष्चक्र में कैद कर दिया।

हमारी पहले से ही लचर स्थिति एक अव्यवस्थित और असमान पुनर्वास प्रक्रिया से और बदतर हो गयी। इसके तहत विस्थापित समुदायों को जमीन और रोजगार के व्यवहारिक विकल्पों से वंचित कर दिया गया। उदाहरण के लिए, बहुत से परिवारों में केवल सबसे उम्रदराज पुरुष को ही पुनर्वास में भूमि का अधिकार दिया गया। इससे परिवारों में आंतरिक कलह बढ़ती गयी और बहुत से घरों को विस्थापित होकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
इन चुनौतियों के बीच कातकरी, ठक्कर और महादेव कोली जैसे आदिवासी समुदायों ने अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट होकर संघर्ष का बिगुल बजाया। यह संघर्ष आसान नहीं था। हमारे सामने अनेक बाधाएं थी, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। समय के साथ हमें बहुत सी लड़ाईयों में जीत भी मिली। इस आंदोलन में हमारे साथ जिले से बाहर के मछुआरे, अन्य आदिवासी समूह, शिक्षाविद और नागरिक समाज के संवेदनशील लोग भी जुड़ते चले गए। यह हमारे संघर्ष और एकजुटता की दास्तान है।
1. साझा संघर्ष के लिए संगठित प्रयास
एक समय था जब कातकरी समुदाय के लोग घोड़ और बुबरा नदियों की उथली धाराओं में छोटी जालियों से मछलियां पकड़ते थे। लेकिन जब बांध बना, तो जलाशय की गहराई और फैलाव इतना बढ़ गया कि मछली पकड़ने के लिए बड़ी नावों और भारी जालों की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे संसाधन जुटाना इन मछुआरों की पहुंच से बाहर था। यह अकेली मुश्किल नहीं थी। जैसे-जैसे बांध के निकट जमीन सिमटती गयी, वहां रहने वाले परिवारों को अपने भू-अधिकारों को लेकर अनिश्चितताओं और विवादों का सामना करना पड़ा। इसका प्रमुख कारण था पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत जमीन पर साझा मालिकाना हक।
वर्ष 2006 में, इस संकट से जूझ रहे 19 गांवों के लोगों ने एकजुट होकर डिंभे बांध के जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की मांग उठायी। उनके सामूहिक रूप से संगठित होने की राह सरल नहीं थी। शुरुआत में प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना और अपनी बात उन तक पहुंचाना, चाहे आंदोलन से हो या समझौते से, एक बड़ा संघर्ष था। लेकिन जब मछली पकड़ने से वंचित रहने के कारण हमारा सामाजिक और आर्थिक संकट गहराने लगा, तो समुदाय के लोगों ने एक सहकारी संस्था की स्थापना की- डिंभे जलाशय श्रमिक आदिवासी मच्छीमार सहकारी सोसाइटी। आज इस संस्था में 300 से अधिक परिवार शामिल हैं, जो विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. विभिन्न हितधारकों की भागीदारी
हमने पुणे जिले के तत्कालीन मंडल आयुक्त, प्रभाकर करंदीकर को अपने सहकारी बोर्ड के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। वे हमारी मांगों के प्रबल समर्थक होने के साथ-साथ डिंभे बांध क्षेत्र गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अगुवा भी रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मत्स्यजीवियों की आजीविका को पुनर्स्थापित करना था, जिसमें सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा शोध और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी की गयी थी। यह पहल विशेष रूप से उन 38 गांवों पर केंद्रित थी, जो बांध के जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं। श्री करंदीकर ने इन सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने और राजस्व, सहकारिता, आदिवासी विकास तथा मत्स्य विभागों की सरकारी योजनाओं के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।
इस व्यापक नेटवर्क के सहयोग से अपनी आवाज को मुखर बनाना हमारी प्रमुख रणनीतियों में से एक था। मुंबई स्थित सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सेक्योरिटी जैसे संगठनों द्वारा हमें क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, शोध और जानकारी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान किए गए। वहीं, रोटरी क्लब पुणे ने हमें नौकाएं और जाल उपलब्ध कराए, जिससे समुदाय पारंपरिक नदी मत्स्य पालन से आगे बढ़ते हुए गहरे जलाशयों में मछली पकड़ने की ओर अग्रसर हुआ। इसके साथ ही, आईआईटी बॉम्बे जैसे शैक्षणिक संस्थानों ने केज (पिंजरा) कल्चर जैसी उन्नत मत्स्य तकनीकों को लागू करने में हमें तकनीकी सहायता प्रदान की।
केज (पिंजरा) कल्चर ने हमारे सामूहिक प्रयास की सफलता में निर्णायक भूमिका निभायी। इस तकनीक में छोटी मछलियों को एक बारीक जाल में रखा जाता है, जो एक जलमग्न फ्रेम से बंधा होता है। मछलियों को तब तक आहार दिया जाता है जब तक वह विकसित नहीं हो जाती और फिर उन्हें मानसून के अंत में जलाशय में छोड़ दिया जाता है। यह विधि न केवल मछलियों को बांध के तेज प्रवाह में बह जाने से बचाती है, बल्कि उन्हें बड़ी मछलियों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। इस तकनीक से जलाशय में रोहू, कतला और मृगल जैसी प्रमुख भारतीय कार्प प्रजातियों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग और आईआईटी बॉम्बे से प्रशिक्षण प्राप्त कर कातकरी समुदाय ने इस विधि में निपुणता हासिल की, जिससे डिंभे बांध उनके लिए सतत आजीविका का स्रोत बन गया।
केज (पिंजरा) कल्चर को अपनाने से डिंभे जलाशय श्रमिक आदिवासी मच्छीमार सहकारी सोसाइटी ने सतत मत्स्य प्रबंधन का एक आदर्श मॉडल पेश किया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से मछुआरे अब डिंभे बांध पर सहकारी संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लेने आते हैं। इससे न केवल समुदाय की साख सुदृढ़ हुई है, बल्कि हमारे सामूहिक प्रयास को भी देशभर में पहचान मिली है।
3. अधिकार, पहचान और नीतिगत बदलाव की वकालत
डिंभे जलाशय श्रमिक आदिवासी मच्छीमार सहकारी सोसाइटी का गठन महज एक शुरुआत थी। क्षेत्र के अन्य आदिवासी समुदायों के सहयोग से कातकरी समुदाय ने अपने मत्स्य अधिकारों को लेकर अपनी आवाज उठाना जारी रखा। जहां एक ओर सामूहिक संगठन की स्थापना और उन्नत मत्स्य तकनीकों को अपनाने के हमारे प्रयास सफल साबित हुए, वहीं दूसरी ओर हमने अपने अभियान के माध्यम से आजीविका अधिकारों को भी संबोधित करना शुरू किया।

क. सामुदायिक वनाधिकारों के लिए संघर्ष
बांध की अप्रवाही जलधारा (बैकवाटर) के फैलाव से कुछ बस्तियां एक तरफ आरक्षित वन और दूसरी ओर पानी के बीच फंस गयी थी। उदाहरण के लिए, भीमाशंकर अभयारण्य में अब बैकवाटर संरक्षित वन क्षेत्र से महज 200 मीटर की दूरी पर पहुंच गया है, जिससे किसानों की खेती योग्य भूमि में भारी कमी आयी है। साथ ही, वन का संरक्षित दर्जा उन्हें पीढ़ियों से जारी परंपरागत खेती करने और गैर-काष्ठ वन उपज (एनटीएफपी) इकट्ठा करने से रोकता है।
जब 1985 में भीमाशंकर अभयारण्य की स्थापना हुई थी, तब हमने वन संरक्षण का समर्थन किया था। हम तब भी जानते थे कि कुछ किसानों की जमीन उस क्षेत्र के भीतर थी। लेकिन बांध के कारण खेती पर प्रतिबंध और फिर वन विभाग द्वारा वन उपज से भी वंचित किए जाने के बाद हमारे पास आजीविका के बहुत सीमित साधन रह गए हैं। इसीलिए, हम वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत सामुदायिक वनाधिकारों की मांग करते हैं, ताकि वन भूमि का सतत उपयोग संभव हो सके।
वन की सामुदायिक देखभाल से न केवल शोषण को रोकने और संरक्षण को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, बल्कि आगजनी की घटनाओं की रोकथाम और वृक्षारोपण की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। वर्ष 2010 से अब तक हमने अनेक सामुदायिक दावे दायर किए हैं, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला है। जहां एक ओर अधिकारियों में मामले की समझ और रुचि का अभाव है, वहीं वन विभाग को यह संदेह है कि स्थानीय समुदायों को अधिकार देने से वह अपनी नियंत्रण-शक्ति खो सकता है। इससे हमारे अधिकारों की लड़ाई लंबी होती जा रही है।
ख. कानूनी लड़ाइयों में सक्रिय भागीदारी
वर्ष 2006 से 2014 तक डिंभे जलाशय श्रमिक आदिवासी मच्छीमार सहकारी सोसाइटी के सदस्य डिंभे जलाशय में पांच साल के पट्टे पर मत्स्य पालन करते थे। यह पट्टा पहले सालाना 56,000 रुपए पर निर्धारित था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,21,000 रुपए कर दिया गया। यह राशि 300 से अधिक सदस्य परिवारों के सहयोग से जुटाई जाती थी, जिनकी मछलियों की बिक्री नासिक, पुणे और मुंबई जैसे बाजारों में होती थी। लेकिन वर्ष 2015 में नीतिगत बदलाव के कारण पट्टे की राशि अचानक बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गयी, जिससे यह पूरी तरह मछुआरों की पहुंच से बाहर हो गयी। स्थिति तब और बिगड़ गयी जब सरकार ने 1,000 हेक्टेयर से बड़े जलाशयों के पट्टे क्षेत्र के बाहर के निजी ठेकेदारों को देना शुरू कर दिया।
हमारा उद्देश्य आज तक पूरी तरह साकार न हो पाया हो, लेकिन हमने काफी कुछ हासिल किया है।
इस निर्णय को चुनौती देते हुए, हमने 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मत्स्य पालन के लिए खुली निविदा प्रणाली (ओपन टेंडर) की मांग की। सुनवाई के दौरान सरकार ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि हम याचिका वापस ले लें तो हमें विशेष मत्स्य पालन अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन हमें फिर भी पट्टे के लिए 7 लाख रुपए सालाना रकम चुकानी पड़ेगी। चूंकि हमारे लिए एकमुश्त भुगतान संभव नहीं था, इसलिए हमने सालाना दो किश्तों में भुगतान का समझौता किया। इस कानूनी लड़ाई के माध्यम से हमने अपने सहकारी संगठन के लिए विशेष मत्स्य पालन अधिकार सुरक्षित किए, जिससे हमारी आजीविका सुरक्षित हुई। लेकिन इस जीत की खुशी बस कुछ ही दिन बरकरार रही।
2024 में सरकार ने पट्टे की राशि बढ़ाकर 24 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी और निविदा (टेंडर) प्रक्रिया को फिर से बाहरी ठेकेदारों के लिए खोल दिया। इस फैसले ने हमें वापस वहीं धकेल दिया, जहां से बाहर निकलने के लिए हमने सालों कड़ी मेहनत की थी। यही कारण है कि हम इस नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसने हमारे सहकारी संगठन के लिए मत्स्य पालन को एक बार फिर से अत्यंत कठिन बना दिया है।
ग. सरकारी विभागों के साथ साझेदारी
डिंभे जलाशय श्रमिक आदिवासी मच्छीमार सहकारी सोसाइटी ने अपनी कानूनी लड़ाइयों के साथ-साथ नीतिगत पैरवी को भी समान महत्व दिया। वर्ष 2015 में संस्था ने महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग से संवाद स्थापित किया। हमने क्षेत्र के अन्य जलाशयों, जैसे खेड तालुका का चासकामन बांध और जुन्नर का माणिकडोह बांध, तक मत्स्य संचालन का विस्तार करने हेतु एक करोड़ रुपए की सहायता राशि सुरक्षित की। इस वित्तीय सहयोग के जरिए सहकारी संस्था ने आदिवासी समुदायों को प्रशिक्षण दिया, उपकरणों का वितरण किया और उनकी मत्स्य पालन पद्धतियों को सुदृढ़ किया। इसका प्रभाव केवल कुछ गांवों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र में बदलाव की लहर आयी।
हमारे आंदोलन की बुनियादी नींव
हम उस जमीन के मूल निवासी हैं जो अब बांध के पानी में डूबी हुई है। इसलिए उसके संसाधनों पर हमारा नैसर्गिक अधिकार है। इसी सिद्धांत पर हमारा आंदोलन भी टिका हुआ है। भले ही हमारा उद्देश्य आज तक पूरी तरह साकार न हो पाया हो, लेकिन हमने काफी कुछ हासिल किया है। हमारे प्रयासों ने एक जन आंदोलन की नींव रखी है, जो केवल डिंभे बांध या कृष्णा बेसिन तक सीमित नहीं है। हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा कर रहे हैं, जिन्होंने इस मुहिम की नींव रखने और उसे सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभायी है:
- एकता और प्रतिनिधित्व: आदिवासी भूमि अपनी प्रकृति में विशिष्ट होती है। हमारे आंदोलन की मांगें व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय सामुदायिक अधिकारों पर केंद्रित हैं। हमारा विश्वास है कि जब समुदायों को वन और मत्स्य संसाधनों का अधिकार सौंपा जाता है, तो इससे पर्यावरणीय संतुलन और दीर्घकालिक संरक्षण की राह आसान हो जाती है। यही विचार अनेक समुदायों के लिए प्रेरणा बना और उन्होंने हमारे संघर्ष का साथ दिया। हमारे सामूहिक संगठन के समावेशी दृष्टिकोण ने कातकरी, महादेव कोली, ठक्कर जैसी विभिन्न आदिवासी जातियों के साथ-साथ क्षेत्र के मुस्लिम परिवारों को भी एक मंच पर लाने का काम किया। यह व्यापक एकता हमारे संवाद और संघर्ष दोनों की ताकत बनी, जिससे हमारी बात न केवल मजबूती से रखी जा सकी बल्कि सबका प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हुआ।
- रणनीतिक अभियान: डिंभे जलाशय श्रमिक आदिवासी मच्छीमार सहकारी सोसाइटी की रणनीति ने कानूनी कार्रवाई, नीतिगत पैरवी और जमीनी स्तर पर जन समर्थन को एकजुट कर बहुपक्षीय चुनौतियों का सामना करने में सफलता पायी। हमने गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी कर उन संसाधनों और विशेषज्ञों तक पहुंच बनायी, जो अमूमन हम जैसे सामूहिक संगठनों को आसानी से नहीं मिलते। इस समग्र दृष्टिकोण ने हमें तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को पार करने की क्षमता दी। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि हमारी आवाज सुनी जाए और हमारी मांगों पर कार्रवाई हो।
- समकालीन, सतत तकनीक का उपयोग: केज कल्चर जैसी सतत तकनीकों को अपनाने से न केवल समुदाय की आजीविका में सुधार हुआ, बल्कि हमारे प्रयासों की दीर्घकालिक उपयोगिता भी सिद्ध हुई। इसके साथ ही, हमने लंबे समय से अपनी जमीन, जंगलों और जलस्रोतों की अंधाधुंध उपभोग और दोहन से रक्षा की है। सतत विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण के कारण हम सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों तरह के हितधारकों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे।
- संघर्षशीलता: बांध से उत्पन्न चुनौतियों और शुरुआती सरकारी उपेक्षा के बावजूद, समुदाय की अडिग प्रतिबद्धता ने इस आंदोलन को दशकों तक जीवित रखा। डिंभे जलाशय श्रमिक आदिवासी मच्छीमार सहकारी संस्था जैसे सामूहिक संगठन की स्थापना ने हमारे संघर्ष को दिशा और आवाज दी। कातकरी समुदाय सहित अन्य जनजातीय समूहों ने बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई। उदाहरण के लिए, पारंपरिक नदी मत्स्य पालन से जलाशय मत्स्य पालन की ओर रूख करना।
डिंभे जलाशय श्रमिक आदिवासी मच्छीमार सहकारी सोसाइटी की यात्रा यह दर्शाती है कि सामूहिक प्रयासों से ही व्यवस्थागत अन्याय का सामना किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि विकास के नाम पर होने वाले उत्पीड़न, विस्थापन और हाशिये पर धकेले जाने के बावजूद, आदिवासी और ग्रामीण समुदायों ने न केवल संघर्ष किया है, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता भी स्वयं तैयार किया है।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—




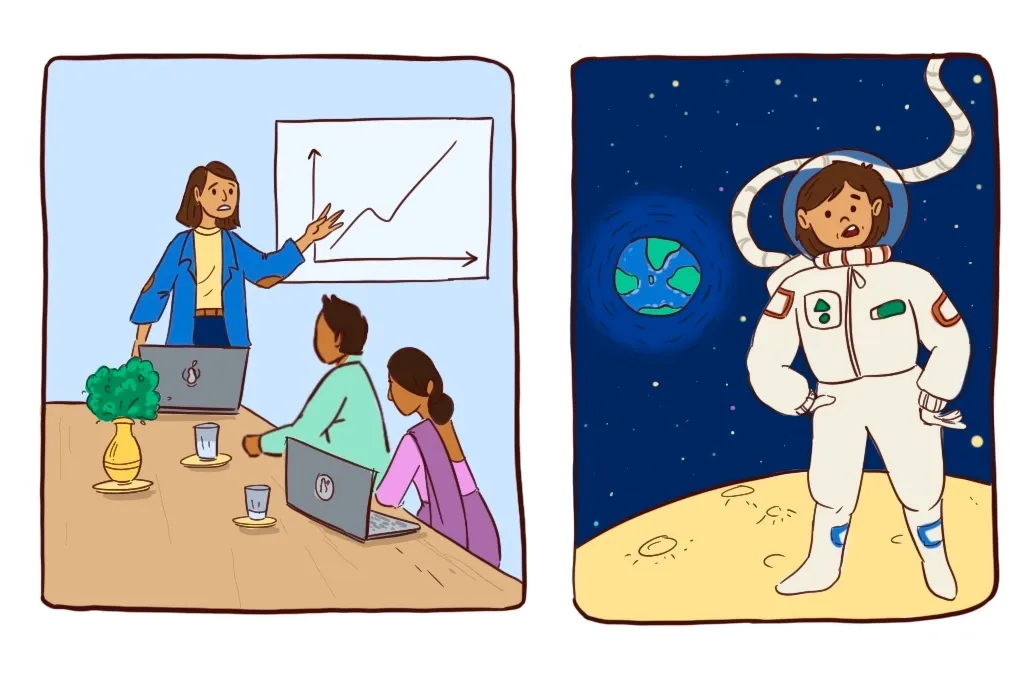

गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपके ईमेल का पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *