देविका सिंह एक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल विशेषज्ञ हैं और मोबाइल क्रेचेज की संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। यह एक ऐसा संगठन है, जिसने देश भर में निर्माण स्थलों (कंस्ट्रक्शन साइट) पर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए बाल देखभाल सेवाओं की शुरुआत की थी। उन्होंने 1969 में राजघाट के पास मीरा महादेवन द्वारा शुरू किए गए पहले क्रेच में एक स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया था। उस समय यह संस्था औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं हुई थी। जिस दौर में श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए क्रेच की कल्पना भी नहीं की जाती थी, देविका ने जमीनी स्तर से उनके लिए एक देखभाल प्रणाली की बुनियाद रखी। उनकी यह पहल प्रवासी श्रमिकों के साथ देश भर में घूमती रही और धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर के एक आंदोलन में बदल गयी।
आईडीआर के साथ हुई बातचीत में वे बता रही हैं कि उन्होंने कैसे इस कार्यक्षेत्र में कदम रखा, कंस्ट्रक्शन साइटों पर क्रेच बनाने के शुरुआती दिन कैसे थे और भारत में बाल देखभाल व सामाजिक समता से जुड़ी नीतियों में क्या बदलाव आए हैं।
हम आपके शुरुआती वर्षों के बारे में जानना चाहेंगे। क्या आप हमें यह बता सकती हैं कि आपको किस बात ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया?
मेरे लिए बच्चों के साथ काम करना कोई सोची-समझी योजना नहीं थी। मेरी सबसे शुरुआती यादें लाहौर की हैं, जो अब पाकिस्तान में है। वहां मैं रात को सोने से पहले अपनी मां से कहानियां सुना करती थी—कभी तारों की, कभी दूर देशों की, तो कभी किसी नन्हे जीव की।
विभाजन के बाद हमारा परिवार कुछ समय दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक शरणार्थी शिविर में रहा। उस समय हालात बहुत अनिश्चित थे। लेकिन फिर भी हमें खेलने-कूदने और अपना बचपन जीने की पूरी आजादी दी गई। हमारे माता-पिता ने कठिन समय में भी हमें यह भरोसा दिलाया कि हम सुरक्षित हैं और उन्हें हमारी परवाह है।
वहीं से मेरे अंदर सुरक्षा और देखभाल की गहरी भावना घर कर गयी। यही भावना मेरे लिए बचपन को समझने का आधार भी बनी। मुझे महसूस हुआ कि एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि वह सुरक्षित महसूस करे और उसकी बात को सुना-समझा जाए। इसी एहसास ने मुझे बच्चों के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया।
मेरी पढ़ाई भारत के साथ-साथ विदेश में भी हुई। शादी के बाद मैंने कोलकाता के लोरेटो कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स के छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। वहीं पहली बार एक बहुत बड़ा फर्क मेरी नजरों के सामने आया—कॉलेज की दीवारों के भीतर रहने वाले संपन्न छात्र और बाहर सड़कों पर घूमते बच्चे। इसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने सोचना शुरू किया कि कैसे अपने काम में हर सामाजिक-आर्थिक तबके की महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सामने लाया जा सकता है।
इसी सोच के साथ मैं जल्द ही दिल्ली आ गयी। मैंने छानबीन करना शुरू किया कि कौन लोग सड़क पर रहने वाले बच्चों और वंचित समुदायों के साथ काम करते हैं। तभी एक दोस्त ने मुझे मीरा महादेवन से मिलवाया। उन्होंने उस समय जो काम शुरू किया था, वही आगे चलकर ‘मोबाइल क्रेचेज’ बना। मीरा ने मुझे अपने द्वारा शुरू किए गए क्रेच में कुछ समय बिताने को कहा।
कंस्ट्रक्शन साइट पर बने उस क्रेच में पहला दिन मेरे लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। हर तरफ सिर्फ बच्चे थे—कुछ भूखे, कुछ रोते हुए और कई बिना कपड़ों या छत के। उनकी मांएं वहीं पास में ईंटें ढोने और मलबा हटाने का काम कर रही थीं और बच्चे बिलकुल अकेले थे। हमारे पास कोई बड़ी योजना नहीं थी। अगर कुछ था तो बस एक तंबू, कुछ जरूरी सामान और यह पक्का इरादा कि हमें कुछ करना होगा। शुरुआत एकदम सरल रही। हमने बच्चों को गोद में उठाया, उन्हें खाना खिलाया, नहलाया-धुलाया और बस इतना सुनिश्चित किया कि वे दिन भर सुरक्षित रहें। उस दिन का अनुभव मेरे साथ रह गया। मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं जान गयी थी कि मैं हमेशा यही काम करना चाहती हूं।
हमारी शुरुआत पूरी तरह जमीनी और सहज थी। हमारा कोई तय मॉडल नहीं था। पहला क्रेच वर्ष 1969–70 के आस-पास राजघाट के सामने एक तंबू में शुरू हुआ था। मीरा के पति गांधी शांति प्रतिष्ठान में गांधी शताब्दी प्रदर्शनी के निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। मीरा खुद गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुई थी। इसलिए वह इस बात से सहमत नहीं थीं कि एक ओर गांधी के लिए एक भव्य इमारत बनायी जा रही है और दूसरी ओर उसी स्थल पर मजदूरों के बच्चों की कोई परवाह नहीं कर रहा है। वे चुप नहीं रही और तुरंत सवाल उठाया, “जब यहां बच्चों की अनदेखी हो रही है, तो हम गांधी के सम्मान की बात आखिर कैसे कर सकते हैं?”
वह इस बात पर अड़ गयीं कि इसके समाधान के लिए कुछ कदम उठाया जाए। उन्होंने ठेकेदार को इस बात के लिए मनाया कि वह बच्चों के लिए कम से कम एक तंबू लगा दे, ताकि वे पूरे समय खुले में न रहें। वह हमारा पहला क्रेच था।
जो बात उस समय को खास बनाती थी, वह थी उस दौर की भावना। देश नया-नया आजाद हुआ था। हमारे पास एक नया संविधान था, जिसमें बराबरी और न्याय के मूल्यों की बात की जा रही थी। लोग देश की हालत को गंभीरता से समझना चाहते थे। वे लगातार यह सोच रहे थे कि हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? यह एक तरह का साझा आत्मचिंतन था। यह जानने की ललक कि हम किस तरह का राष्ट्र बन रहे हैं। जैसे गांधी के आदर्श और एक आजाद देश की नई ऊर्जा मिलकर कुछ रचने की राह पर थे। यह भारत के इतिहास का वह दौर था, जब हर कोई मिलकर एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की कोशिश में जुटा हुआ था।
इस काम ने मुझे न्याय और सामाजिक बराबरी को करीब से समझने का मौका दिया।

जब आपने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, उस समय आपके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का क्या मतलब था? क्या उस दौर में भी लोग इस विषय पर सोचते या बात करते थे?
सच कहूं तो शुरुआत में हमें खुद भी ठीक से नहीं पता था कि ‘प्रारंभिक बाल विकास’ (ईसीडी) का क्या अर्थ होता है। उस समय न तो शिक्षा का अधिकार था और न ही ईसीडी को लेकर कोई स्पष्ट चर्चा होती थी। हमारे लिए बात बस इतनी सी थी कि बच्चों को कंस्ट्रक्शन साइटों पर यूं ही बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। हम ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे वहां रहने वाले सभी बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दी जा सके। जो काम हम कर रहे थे, वही आगे चलकर ईसीडी की बुनियाद साबित हुआ।
चूंकि इससे पहले किसी ने भी निर्माण स्थलों पर इस तरह का काम नहीं किया था, इसलिए हमारी क्रेच की कल्पना भी एकदम मध्यमवर्गीय सोच से प्रेरित थी, जहां सब कुछ साफ-सुथरा, व्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है। लेकिन फिर हमें पता चला कि कंस्ट्रक्शन साइट जैसी जगहों पर हर दिन एक नई आपात चुनौती सामने आती है। वहां काम करने का मतलब था रोजमर्रा की जरूरतों से जूझना—कभी पानी लाना, कभी खाना जुटाना, कभी बच्चों के लिए चटाई, कपड़े या दवाइयों का इंतजाम करना।
हमें रोते, बिलखते या दस्त जैसी परेशानियों से जूझ रहे बच्चों की तत्काल जरूरतों को समझना होता था। हम उन्हें उठाकर साफ करते थे, खाना खिलाते थे, कपड़े पहनाते थे और उन्हें एक छत देने की कोशिश करते थे। उनकी माताएं वहीं पास में ईंटें उठाकर मचान चढ़ रही होती थी। ऐसे में बच्चे या तो इधर-उधर घूमते रहते थे या उनकी पीठ से बंधे होते थे, जो खतरनाक था।
शुरुआत में हम जो भी सामान इस्तेमाल करते थे, उसे एक लोहे के बक्से में समेटकर शाम को ठेकेदार के पास रख दिया जाता था। हमारे पास सीमित और जुगाड़ू साधन थे, लेकिन हम उनसे काम कर पा रहे थे। धीरे-धीरे इसी अस्थायी, चलते-फिरते मॉडल ने ‘मोबाइल क्रेच’ का रूप ले लिया, जहां देखभाल को किसी तय ढांचे की बजे जरूरत के हिसाब से ढाला जाता था।
उस समय कई मजदूर विभाजन के बाद विस्थापित हुए परिवारों से थे। उनके पास न कोई स्थायी पता था, न कागजात। ऐसे में उनके लिए अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कराना एक बड़ी चुनौती होती थी। दरअसल राज्य की तमाम व्यवस्थाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या राशन प्रणाली) इन प्रवासी जिंदगियों को ध्यान में रखकर नहीं बनायी गयी थी।
हमने पहले ही यह समझ लिया था कि बच्चे अक्सर बनी-बनायी व्यवस्थाओं के दायरे से बाहर रह जाते हैं। नीति-निर्माण की चर्चाओं में उनका जिक्र बहुत बाद में आया। बाद में जब आंगनवाड़ी जैसी योजनाएं शुरू हुई, तब भी उनके पास संसाधनों की भारी कमी थी। हमारा काम केवल किसी सामाजिक कमी की भरपाई नहीं था। यह उस हकीकत को सामने लाने का एक प्रयास था, जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था।
जब आपने मोबाइल क्रेचेज की शुरुआत की, तब आपको शुरुआती दौर में किन चुनौतियों से जूझना पड़ा था? और अब जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं, तो उस समय की कौन-सी बुनियादी कमियां साफ नजर आती हैं?
चुनौतियां तो बहुत थी। सबसे पहले तो रोजमर्रा के साधन (पानी, खाना, कपड़े) जुटाने की ही मशक्कत थी। जिन महिलाओं को क्रेच चलाने के लिए तैयार किया जाए, उन्हें ढूंढना भी उतना ही मुश्किल काम था।
लेकिन शायद सबसे बड़ी चुनौती थी भरोसा जीतना। माताओं के लिए यह बहुत बड़ा फैसला था कि वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को किसी अजनबी के पास छोड़ दें। उनका डर जायज भी था। उधर ठेकेदार भी हमें लेकर उलझन में रहते थे। अक्सर चौकीदार हमें साइट पर घुसने से ही रोक देते थे। अगर किसी दिन हम साइट पर मौजूद किसी इंचार्ज से बात करने में सफल भी होते, तो हमें उन्हें बार-बार समझाना पड़ता कि हम सरकार से नहीं हैं और न ही हम कोई जांच या निरीक्षण करने आए हैं। वे हमें शक की निगाह से देखते—ये कौन लोग हैं? कहीं कोई रिपोर्टर तो नहीं? कोई सरकारी जांच टीम तो नहीं? इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हमें उन्हें यह भरोसा दिलाने में समय लगा कि हम बच्चों की देखभाल के लिए सिर्फ एक कोना, थोड़ी सी जगह और थोड़ा पानी चाहते हैं।
माताओं की हिचकचाहट तो और भी संजीदा थी। कई महिलाओं ने अपने बच्चों को कभी किसी बाहरी व्यक्ति के पास नहीं छोड़ा था। वे हमसे पूछती, “इन्हें क्या खिला रहे हो? ये खाना किसके हाथों से बना है?” कई बार जात-पात से जुड़े सवाल भी पूछे जाते थे। जैसे, “मेरे बच्चे को उसके पास मत बैठाना” या “ये कपड़ा मत इस्तेमाल करो। क्या पता किसी मरे हुए बच्चे का हो।” वे हमारे लाए कपड़ों को लेकर आशंकित रहती थी। उन्हें डर लगता था कि वो कपड़े कहीं गंदे या अशुभ न हो। कभी-कभी उन्हें लगता कि उनके बच्चों को हमारी नजर लग जाएगी।
माताओं के लिए यह बहुत बड़ा फैसला था कि वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को किसी अजनबी के पास छोड़ दें।
हमें समझ में आया कि उनकी इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास बोलकर अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जब कोई समुदाय पीढ़ियों तक समाज के हाशिये पर रहता है, तो वे उपेक्षा और डर के कारण रक्षात्मक सोच से जुड़े कुछ तौर-तरीके अपना लेते हैं। इसलिए हमने कभी जल्दबाजी नहीं की और धीरे-धीरे अलग उपाय अपनाए। उदाहरण के लिए, माताओं के पास बैठना, बिना किसी जजमेंट के उनकी बात सुनना, रोज के फैसलों में उन्हें शामिल करना और हर दिन, लगातार, वहां मौजूद रहना। इससे धीरे-धीरे हमारे रिश्ते मजबूत हुए।
एक और बड़ी चुनौती थी—प्रवासन की अस्थिरता। कई बार श्रमिक परिवार अचानक कोई जगह छोड़ देते थे। एक दिन बच्चा हमारे पास क्रेच में होता और अगले ही दिन कहीं और चला जाता। इन बच्चों को पहले से ही शुरुआती स्कूलिंग नहीं मिलती थी, न उनके पास कागजात होते थे और वे अलग-अलग भाषाएं बोलते थे। सरकारी स्कूल उन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं थे। न तो उनकी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कराने के लिए कोई व्यवस्था थी और न ही एडमिशन की प्रक्रिया या ट्रांसफर सर्टिफिकेट में उनके लिए कोई प्रावधान था।
तब हमें समझ आया कि हमें खुद बच्चों और उनके परिवारों को ट्रैक करना होगा। अपने स्तर पर पूछताछ करना, पता लगाना, उनकी अगली साइट तक पहुंचना और ये समझना कि वे कहां और क्यों जा रहे हैं। इस दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि ये सभी बच्चे सिस्टम के लिए तकरीबन अदृश्य थे। यहीं से हमने यह सोचना शुरू किया कि सिर्फ एक जगह क्रेच बना देना काफी नहीं है। हमें एक ऐसा मॉडल बनाना होगा, जो श्रमिकों के साथ हर जगह जा सके और उनके जीवन से तालमेल बिठा पाए।
समय के साथ जैसे-जैसे हमारे केंद्र बढ़े, वैसे-वैसे यह काम भी अधिक लोगों की नजर में आने लगा।

क्या कभी ऐसा कोई क्षण आया जब आपको लगा कि नीतियों (पॉलिसी) में भी आपके काम का संज्ञान लिया जाने लगा है?
कंस्ट्रक्शन साइटों तक पहुंचना और प्रवासी मजदूरों की जिंदगी को समझ पाना एक धीमी प्रक्रिया थी। वहीं से हमारा ध्यान धीरे-धीरे इस ओर गया कि इनके जीवन पर किन कानूनों, नीतियों और ढांचागत व्यवस्थाओं का असर पड़ता है। ये सवाल हमें उन लोगों, पहलों और आंदोलनों से जोड़ने लगे, जो पहले से चल रहे थे।
वर्ष 1971 के आस-पास हमारी मुलाकात मजदूर और श्रमिक अधिकारों से जुड़े कार्यकर्ताओं से हुई। उस समय सुभाष भटनागर और उनकी पत्नी जैसे लोग प्रवासी मजदूरों के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। शुरुआत में मोबाइल क्रेचेज इस प्रक्रिया का औपचारिक हिस्सा नहीं था। लेकिन जब हमने श्रमिकों की जिंदगी को गहराई से समझने की कोशिश की, जैसे उनकी कमाई, उनका प्रवास, उनके काम से जुड़े ठेके, अनुबंध और अनिश्चितता, तब हम इस समूह के संपर्क में आए। यहीं से यह साफ हुआ कि बच्चों की देखभाल का सवाल श्रमिकों के जीवन के समग्र ढांचे से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, आपको प्रवास, अंतर्राजीय श्रम, नियम-कानून और उनकी खामियों को समझना पड़ेगा। यहीं से ‘क्रेच’ की अवधारणा ने धीरे-धीरे श्रमिक अधिकारों की नीतियों में अपनी जगह बनानी शुरू की।
इन प्रयासों और सामूहिक आवाजों का असर यह हुआ कि आगे चलकर 1979 में अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम बना। इस कानून में यह प्रावधान जोड़ा गया कि अगर मजदूर किसी साइट पर तीन महीने या उससे अधिक समय तक काम करने वाले हैं, तो वहां उनके बच्चों के लिए क्रेच बनाना और उसे बनाए रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। बाद में, जब 1996 में भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम लागू हुआ, तो उसमें भी कार्यस्थलों पर क्रेच को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया।
कंस्ट्रक्शन साइटों तक पहुंचना और प्रवासी मजदूरों की जिंदगी को समझ पाना एक धीमी प्रक्रिया थी।
कभी-कभी यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कैसे जमीनी स्तर पर उठाए गए एक छोटे से कदम (कंस्ट्रक्शन साइट पर बच्चों को सुरक्षित माहौल देना) का इतना व्यापक असर हो सकता है। नीति-निर्माण से जुड़े उस विमर्श में शामिल होने से हमारे काम को मान्यता मिली और मोबाइल क्रेचेज और प्रारंभिक बाल देखभाल पर एक गंभीर चर्चा की शुरुआत हुई। उसी दौरान देश भर में आंगनवाड़ी कार्यक्रम (आईसीडीएस) की रूपरेखा भी तैयार हो रही थी, जिसमें यूनिसेफ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमने इसमें ‘आंगनवाड़ी–कम–क्रेच’ मॉडल तैयार करने में सहयोग दिया। यही वह समय था जब स्वास्थ्य, पोषण और शुरुआती शिक्षा को एक साथ जोड़कर देखने की सोच आकार ले रही थी।
यह भारत की सामाजिक नीति और संस्थाओं के निर्माण की शुरुआती यात्रा थी। लेकिन इन्हीं शुरुआती बैठकों और विचार-विमर्शों के कारण मोबाइल क्रेचों जैसी मुहिम को गंभीरता से लिया जाने लगा। फिर मीरा ने प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी के दौरान इंदिरा गांधी को हमारे क्रेच का दौरा करवाया। उस दिन के बाद से हमें उन चर्चाओं का हिस्सा बनाया जाने लगा, जहां बच्चों की देखभाल, पोषण और शिक्षा को लेकर नीतियां बनायी जाती थी।
यह बात भी हमारे पक्ष में गयी कि हमने अपनी ओर से यह पड़ताल की हुई थी कि उस समय बच्चों के लिए कौन-कौन सी सरकारी योजनाएं मौजूद थी। उस शुरुआती दौर में भी हमने इस बात का अध्ययन किया था कि बच्चों की जरूरतें क्या हैं और किन बच्चों तक प्रशासनिक व्यवस्था पहुंच ही नहीं पाती है।
जब आप अपने सफर को देखती हैं, तो यह काम आपके लिए क्या मायने रखता है? और आप क्या चाहती हैं कि लोग इससे क्या सीखें और आगे लेकर जाएं?
इस काम की शुरुआत किसी सोच-समझकर बनायी गयी योजना से नहीं हुई थी। सब कुछ बहुत साधारण ढंग से शुरू हुआ था। हमें बच्चों की जरूरतें दिखी और लगा कि उस बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे यह काम सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहा। हमें समझ आने लगा कि यह उन तमाम लोगों की बात है, जिन्हें समाज ने लंबे समय से अनदेखा किया है। जब आप थोड़ा ठहरकर सोचते हैं, तो कुछ सवाल अपनेआप उभरने लगते हैं। जैसे, जो इमारतें बन रही हैं, जो सफाई हो रही है, जो खाना बन रहा है—ये सब कौन कर रहा है? और उनके परिवार कहां हैं? अगर आप बच्चों की देखभाल की बात करना चाहते हैं, तो फिर आपको मजदूरी की बात भी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको प्रवासन की, कम दिहाड़ी में पूरे दिन काम करने वाली औरतों की बात करनी पड़ेगी। आपको उनके घरों की, रहने की जगहों की, वे क्या खाते हैं जैसे पहलुओं की बात करनी पड़ेगी। आपको यह समझना पड़ेगा कि वे क्यों उस सामाजिक व्यवस्था को नजर ही नहीं आते हैं, जिसे उनके लिए बनाया गया है।
इस काम ने मुझे सिखाया कि सुनने (लिसनिंग) के क्या मायने हैं। सिर्फ लोगों की कही हुई बातों को नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी जो कहती है, उसे भी। मैं चाहती हूं कि लोग इसी बात को साथ लेकर आगे बढ़ें। आपके अंदर सुनने की और जटिलताओं के बारे में सोच पाने की क्षमता होनी चाहिए। आप किसी चीज से केवल इसलिए मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको तुरंत या आसान जवाब नहीं मिल रहे हैं।
आपको किसी के लिए मसीहा नहीं बनना है। यह सोचकर काम करने मत निकलिए कि आप कुछ ठीक करने जा रहे हैं। आप सीखने आए हैं। जब आप यह समझ जाएंगे, फिर यह काम आपको बदलेगा भी और गहराई से प्रभावित भी करेगा। कुछ सवाल बार-बार सामने आएंगे—बच्चे कहां चले गए? वे बार-बार क्यों जगह बदलते हैं? जो कानून बने हैं, क्या वे सच में काम कर रहे हैं? लेकिन इन सभी सवालों के साथ जूझना भी इस काम का ही हिस्सा है।
मैं चाहती हूं कि लोग ये बात कभी न भूलें कि आपकी मौजूदगी बहुत मायने रखती है। किसी जगह हर रोज लौटना, लगातार मौजूद रहना और वहां टिके रहना। यही सोच मोबाइल क्रेचेज की नींव है। यह किसी मॉडल या नीति से नहीं, बल्कि देखभाल और शुरुआती शिक्षा के मूल्यों पर आधारित है।
जब आप किसी की ईमानदारी से देखभाल करते हैं, तो आपके लिए वो रास्ते भी खुल जाते हैं, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
–





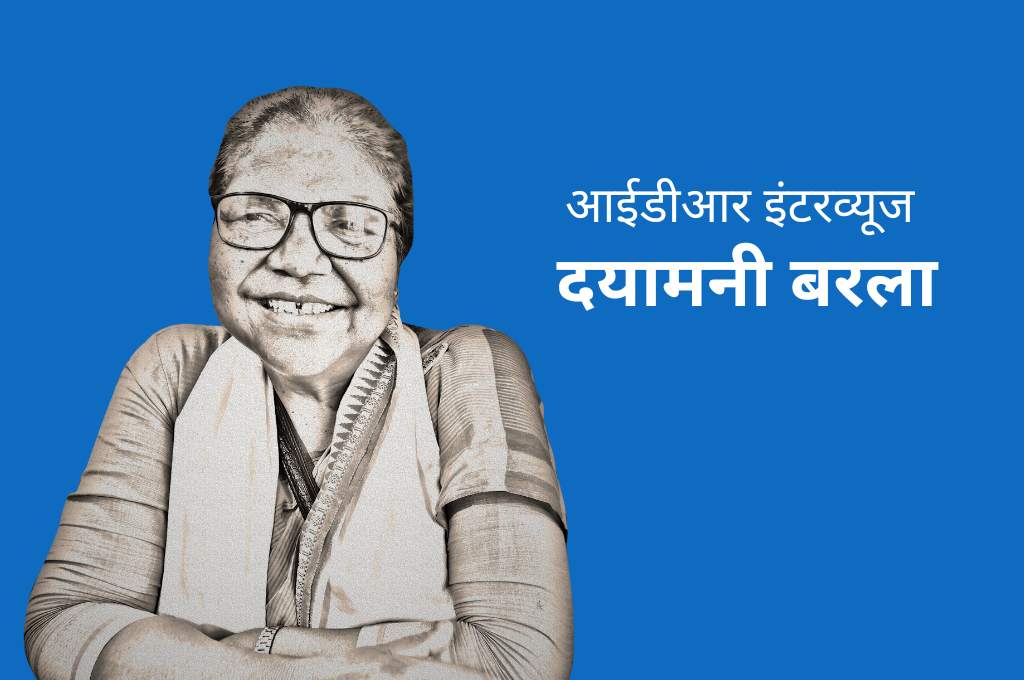
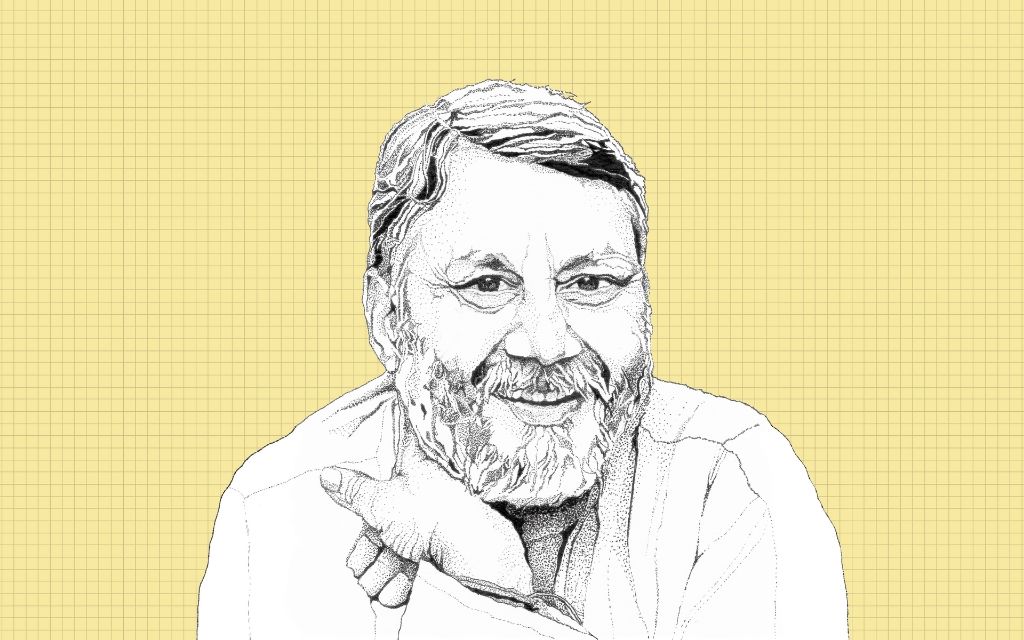
गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपके ईमेल का पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *