1. जब महिला किसान दिवस पर लोग शुभकामनायें दे रहे होते हैं।
2. लेकिन जब ऑनलाइन ‘किसान’ शब्द सर्च करने पर सिर्फ किसान पुरुषों के बारे में ही जानकारी आए।

3. जब ट्रैक्टर वाला, महिला किसान से खेत जोतने के ज्यादा पैसे मांगे।

4. जब तमाम वायदों के बावजूद भी पंचायत सिंचाई की व्यवस्था न करे।

5. जब अपनी फसल का जायज़ दाम मांगने के बावजूद आढ़ती अपनी बात पर ही अड़ा हो।

6. एक महिला किसान जो घर का काम निपटाकर खेत में काम करने आती है और फिर उसे घर जाकर काम करने की चिंता सताये…

7. जब गांव में कृषि विकास पर चर्चा हो रही हो और उस चर्चा में केवल पुरुष किसानों को ही न्यौता मिले।

8. जब गांव की बेटियां कृषि विज्ञान की पढ़ाई करने में रुचि दिखाएं और घर के पुरुष उन्हें टीचर बनने की सलाह दें…

बंगाल में 1770 के अकाल में महुआ ने कई लोगों की जान बचायी थी। एक रिकॉर्ड के अनुसार, 1873-74 में बिहार के खाद्य संकट में भी ये महुआ ही था जिसने यहां के बहुत लोगों को जीवित रखा था। पहले गांव के लोग 3-4 महीने, एक समय महुआ खाकर रहते थे। इसमें पौष्टिकता भरपूर होती है। हमें लगता है कि यह सब अब पहले की बात है। महुआ का महपिट्ठा, लट्टा, महरोटी, खीर, भूंजा, मड़ुआ का लड्डू, नमकीन बनता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बचपन में उन्होंने इसे खाया है। लेकिन अभी भी ये जीवित हैं।
इस साल जून में, गया ज़िला के बाराचट्टी थाना के कोहबरी गांव में सहोदय ट्रस्ट के प्रांगण में, महुआ और मड़ुआ पर ग्रामीण लोगों के साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें डोभी प्रखंड के नक्तैया गांव की दो ग्रामीण महिलाओं – सुमंती देवी और कौशल्या देवी ने सहोदय आकर महुआ से कई तरह के स्थानीय व्यंजन पारंपरिक तरीके से बनाए और हम लोगों को सिखाये। उन्होंने महुआ का महपिट्ठा, महरोटी, लट्टा या लड्डू, खीर, और भूंजा बनाए। महपिट्ठा, और महरोटी, महुआ और मड़ुआ को आटा के साथ मिलाकर, दोनों ओर से पलास के पत्ते चिपकाकर, पानी के भाप से सिंझाये (पकाए)। उसी तरह महुआ को मिट्टी के चूल्हा पर मिट्टी के खपड़ी में सूखा भूनकर, और भूंजा तीसी को मिलाकर और कूटकर, लट्टा और लड्डू बनाये। उसी तरह महुआ को भूंजकर उसमें लहसुन और मिर्च मिलाकर भूंजा बनाया। दूध में महुआ को सिंझाकर लाजवाब खीर भी बनायी। हम सब लोगों और सहोदय के बच्चों ने भी इसे बनाने की प्रक्रिया सीखी।

सहोदय की रेखा ने ग्रामीणों को मड़ुआ के आटा से लड्डू और नमकीन बनाना सिखाया। लड्डू पहले तीसी या घी में भूंजकर, गुड़ के पाग में बनाया जाता है। स्वाद के लिए मूंगफली का दाना मिला सकते हैं। नमकीन भी मड़ुआ के आटे को गूंथदकर छोटे-छोटे टुकड़े निमकी (नमकपारे) के आकार का काटकर, सेंधा नमक मिलाकर, तीसी के तेल में फ्राई किया जाता है। इस तरह आप एक पारंपरिक, पौष्टिक, और जैविक खाद्य पदार्थ को न केवल जीवित रख रहे हैं बल्कि इसका सेवन करके अपने स्वास्थ्य को संरक्षित और मजबूत भी कर रहे हैं और कई बीमारियों से अपने शरीर को बचा रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के मूल तत्वों के प्रदूषण के कारण मौसम और तापमान में अनुपातहीन बदलाव ने पूरी पृथ्वी पर जीवन को खतरे में डाल दिया है। कई जीव-जंतु तो विलुप्त हो चुके हैं। इसका असर हमारे स्वास्थ्य, व्यवसाय और खेती पर साफ दिखाई देता है। इसलिए हमें अपने जंगलों और स्थानीय जैव विविधता को बचाने के साथ-साथ इन्हें समृद्ध करने की हर कोशिश करनी चाहिए। हमें खेती के पुराने पारंपरिक जैविक तरीके अपनाने होंगे। प्राकृतिक स्थानीय फल-सब्जियों और औषधियों को फिर से अपने जीवन और समुदाय से जोड़ना होगा। रासायनिक या कृत्रिम रूप से संसाधित खाद्य पदार्थ अपनी थाली से हटाने होंगे। इन सब में हमारे पुराने पेड़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। महुआ ऐसा ही एक पेड़ है जिससे हमारे लोग पहले लगभग 2-3 महीने तक प्राकृतिक, जैविक और पौष्टिक खाद्य पदार्थ फूल के रूप में सेवन करते थे, लेकिन अब भूलते जा रहे हैं या लगभग भूल ही गए हैं। इसके बीज के तेल से सब्ज़ी और अन्य व्यंजन बनाते थे। यह तेल गर्मी में लू से बचने में भी काम आता है। बहुत ही कम लोग अभी भी इस ज्ञान, अनुभव और कौशल का उपयोग करते हैं।
महुआ की दो प्रजातियां हैं। एक जो ज़्यादा मीठा होता है, उसको चुनकर और धूप में सुखाकर रखते हैं। व्यंजन बनाने से पहले उसको अंदर से साफ़ करते हैं। इसके फूल अप्रैल महीने में आना शुरू होते हैं और मई के पहले सप्ताह तक सारे फूल झड़ जाते हैं और पेड़ में नई पत्तियों के साथ फल आते हैं। ये फल जून में तैयार होते हैं और झड़ते हैं। इनके फल से बीज निकालकर उससे तेल निकाला जाता है। बीज को स्थानीय भाषा में डोरा कहते हैं।
इस साल, पिछले साल की तुलना में फूल कम आये हैं। शायद पेड़-पौधे भी किसी साल अपने आप को आराम देते हैं या फिर मौसम में परिवर्तन का असर भी एक वजह हो सकता है। लेकिन सभी पेड़-पौधों की उत्पादन क्षमता पहले से घटी है, ऐसा यहां के स्थानीय किसान सोचते हैं। महुए के पेड़ भी पहले से घटे हैं और अब बहुत कम लोग इसे लगाते हैं क्योंकि ये फल-फूल देने लायक होने में 10-15 वर्ष का समय लेते हैं। महुआ के उपयोग और पेड़ों में कमी, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए सकारात्मक नहीं है।
जेठ के महीने में एक त्यौहार आता है जिसका नाम सरहुल है जिसमें महुए के पेड़ की पूजा, महुए से ही बने व्यंजन से होती है। ये पर्यावरण-हितैषी संस्कृति भी अब विलुप्त होती जा रही है। मड़ुआ, मिलेट के जैसे महुआ से भी हमारे समाज, समुदाय, प्रकृति और स्वस्थ्य का गहरा रिश्ता रहा है जो कमजोर हो गया है। हम लोग इससे बने व्यंजन को अपनी थाली में शामिल कर न केवल अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं बल्कि अपने स्थानीय जैव विविधता पर निर्भर न जाने कितने जीव जंतुओं, और आब-ओ-हवा को जीवित, सुंदर और शुद्ध रखने में सहयोग कर रहे हैं।
साथ ही, इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी क्योंकि हम लोग अपने घर की कई जरूरतों, जैसे खाना, तेल, लकड़ी, जानवरों के लिए चारा के लिए बाजार पर निर्भरता को कम करेंगे। महुए से कई जैविक खाद्य पदार्थ और व्यंजन बनाकर स्थानीय व्यवसाय करके, इसे एक टिकाऊ जीविका का साधन भी बना सकते हैं। इससे मानव और प्रकृति के अन्य जीवित तत्वों के बीच के सम्बन्ध समृद्ध होंगे और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में मददगार साबित होंगे।
यह लेख मूलरूप से युवानिया पर प्रकाशित हुआ था।
भारतीय न्यूजरूम्स में वंचित लिंग, जाति और समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। मुख्यधारा के विकास संबंधी विमर्श में उनके अनुभवों और कहानियों को अक्सर नजर अंदाज कर दिया जाता है। इन समुदायों के दृष्टिकोण की यह व्यवस्थागत अनदेखी, उनके विकास से जुड़ी चुनौतियों के असल कारणों को अस्पष्ट कर देती हैं।
ऑक्सफैम इंडिया और न्यूज़लॉन्ड्री के 2019 के एक अध्ययन में पाया गया है कि:
विमर्श के इस मौजूदा स्वरूप को बदलने के लिए, एक वैकल्पिक मीडिया की तत्काल जरूरत है। एक ऐसा मीडिया जो वंचित तबकों के जबानी इतिहास, उनकी आवाज और उनके जीवन के अनुभवों से बने समुदाय-संचालित नजरिए और साक्ष्यों पर केंद्रित हो। समाजसेवी संस्थाओं ने इस अंतराल को भरने के लिए कई प्रयास किए हैं। सामुदायिक रेडियो जैसे स्थानीय माध्यमों से शुरुआत कर, इन संस्थाओं ने हाल ही में डिजिटल मीडिया में कदम रखा है जिसका इस्तेमाल अब भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा करता है। यहां कुछ ऐसे तरीकों पर बात की गई है जिनसे गैर-लाभकारी मीडिया आउटलेट कम प्रतिनिधित्व वाली आवाजों और मुद्दों को आगे ला रहे हैं:
परिप्रेक्ष्य-संचालित दृष्टिकोण, लोगों के दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर बनते हैं जो उनके जीवन पर गैर-बराबरी, हाशिये पर पहुंचने और अन्य व्यापक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के असर को एक जगह केन्द्रित कर देखते हैं। इस तरह के प्रयास मुख्यधारा की चर्चाओं से दूर मौजूद लोगों को, मीडिया में उनके अनुभवों को समझने और प्रसारित करने के तरीके पर फिर से नियंत्रण पाने में सक्षम बनाकर, उन्हें इन चर्चाओं में सक्रिय भागीदार बनने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया (परी), खुद को एक ‘जीवंत पत्रिका और एक दस्तावेज संग्रह’ बताता है जो भारत के ग्रामीण इलाकों के नजरियों को इकट्ठा करता है। परी ग्रामीण भारतीयों के लेख, वीडियो और ऑडियो रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और कहानियां अक्सर बताने वाले की जुबान में होती हैं।
आंकड़ों के साथ, तथ्य-आधारित कहानियां कहना, प्रमाणों के साथ उपेक्षित मुद्दों, इलाकों और सामाजिक क्षेत्रों को सामने लाने में मदद करता है। यह, तकनीकी साक्ष्य – जैसे विकास पर सरकारी आंकड़ों – को व्यापक जनता के लिए उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करता है। साथ ही विभिन्न समूह जिनके हित इससे जुड़े होते हैं, उनके हितों को सामने लाने और प्रासंगिक बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, इंडियास्पेंड एक डेटा-आधारित पत्रकारिता मंच है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जेंडर और जलवायु परिवर्तन जैसे विशिष्ट संदर्भों वाली दृष्टि के आधार पर भारत की सामाजिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आंकड़े प्रसारित करता है।
विकास-केंद्रित विशिष्ट मीडिया संसाधन सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों, बाधाओं और प्रगति के बारे में बताते हैं। इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू (आईडीआर) जैसे मंच और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के डाउन टू अर्थ जैसे प्रकाशन विशिष्ट मीडिया एजेंसियों के उदाहरण हैं। यह सक्रिय रूप से भारत में विकास क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर नजरियों को नया आकार दे रहे हैं और हाशिए के समुदायों की जरूरतों पर रौशनी डाल रहे हैं। जमीनी संगठनों के साथ मिलकर काम करके और सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर वह ऐसा कर पाते हैं। यह मॉडल इस आधार पर संचालित होता है कि गैर-लाभकारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के पास अनुभव आधारित प्रचुर ज्ञान मौजूद है, और मुख्यधारा के विकास संवाद में और अधिक बारीकियों को शामिल करने के लिए इसे व्यापक रूप से फैलाए जाने की जरूरत है।

मीडिया की पहुंच बढ़ाने के लिए गैर-लाभकारी संस्थाएं दो अलग-अलग तरीकों से ईकोसिस्टम के स्तर पर प्रयास कर रही हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल प्रकाशन द थर्ड आई सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रीय विषयों पर समुदाय के लोगों के साथ व्यक्तिगत निबंध और साक्षात्कार का मेल करता है। जमीनी स्तर तक ज्ञान पहुँचाने के लिए नारीवादी दृष्टिकोण के साथ अपनी मूल संस्था निरंतर ट्रस्ट के कई दशकों के जुड़ाव के आधार पर, यह जमीनी संगठनों में ऑफलाइन प्रशिक्षण और अनुभवों से मिली शिक्षा का आदान-प्रदान भी आयोजित करता है। इसी तरह, प्वाइंट ऑफ व्यू (पीओवी) अपने विभिन्न कार्यक्षेत्रों में लेख और शोध पत्र प्रकाशित करता है, जो ज्ञान प्रणालियों, डिजिटल नैतिकता, महिलाओं, क्वीयर समुदायों और विकलांग लोगों सहित हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही, पीओवी इन समुदायों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम भी चलाता है और समावेशी सरकारी नीतियों की हिमायत करता है।
तमाम प्रयासों के बावजूद, ये गैर-लाभकारी (मीडिया) संस्थाएं अभी भी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारत में निजी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कमाई के लिए सब्सक्रिप्शन और पेवॉल पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं। हालांकि, गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए ऐसे मॉडल अपना पाना चुनौतीपूर्ण है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि इन संस्थाओं का उद्देश्य महत्वपूर्ण जानकारियों और ज्ञान को आम जनता के लिए सुलभ और सहज बनाना है। सामाजिक क्षेत्र या विकास क्षेत्र से मिलने वाली फंडिंग का विकल्प भी इनके लिए मुश्किल होता है।
इस तरह की पहलों के लिए आर्थिक सहयोग हासिल करने में चुनौतियों का कारण यह हो सकता है कि इन संस्थाओं के परिणाम अक्सर क्रमिक होते हैं, उनमें व्यवहारिक परिवर्तन शामिल होते हैं, और इसलिए उन्हें मापना कठिन होता है। ऐसे में जहां बहुत से फंडर्स तुरंत दिखाई देने और मापे जा सकने वाले परिणामों को प्राथमिकता देते हैं, यह नुकसानदायक साबित होता है। हालांकि इनमें से कई संस्थाएं लंबे समय में प्रभाव दिखाने के अवसरों से लाभान्वित हो सकती हैं, लेकिन उनके पास अक्सर दूरगामी कार्यक्रम बनाने और उनके नतीजे हासिल करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। लंबी अवधि के उपयोग के लिए निर्धारित फंडिंग के लचीले रूपों तक पहुंच इन गैर-लाभकारी संस्थाओं को फलने-फूलने और बड़े पैमाने पर प्रभाव हासिल करने में मदद कर सकती है।
ज्ञान का प्रसार और मीडिया की पहुंच और असर को बढ़ाने के क्षेत्रों को लेकर यह आम धारणा हैं कि इन्हें फंडिंग मिलने में मुश्किलें आती हैं। जैसे-जैसे डिजिटल मीडिया का विकास जारी है, दुष्प्रचार और गलत सूचना, नई नीतियों और कानूनी व्यवस्थाओं और परिदृश्य में बदलाव सहित अभूतपूर्व चुनौतियों के कारण यह धारणा और भी मजबूत हो गई है।
गैर-लाभकारी (मीडिया) संस्थाएं अभी भी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं।
भारत में विविध भाषाई और सामाजिक-सांस्कृतिक समूहों के लिए काम करने वाला विविध डिजिटल मीडिया और संचार परिदृश्य, आज के समय की मांग है। इस पर काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए व्यक्तिगत स्तर पर समाजसेवा, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और लचीलेपन के साथ एक मजबूत फंडिंग पाइपलाइन बनाने में मदद कर सकती है। उन्हें फंड करने से इस बात पर भी ध्यान दिया जा सकता है कि उनका काम विकास की चुनौतियों को हल करने में कैसे योगदान देता है और उनके द्वारा चलाए जाने वाले सकारात्मक परिणामों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करता है।
समुदाय-संचालित नजरिए और प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर-लाभकारी मीडिया की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें समाजसेवियों से मिलने वाली पूंजी बहुत मददगार साबित हो सकती है:
क्षमता निर्माण में सहायता: गैर-लाभकारी मीडिया संस्थानों में विविध समुदायों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यबल को तैयार करने के लिए क्षमता-निर्माण की पहल बहुत जरूरी है। यह पहल उपेक्षित और हाशिए के समुदायों के लिए सशक्त कहानीकार और रचनाकार बनने के अवसर पैदा करती है, जिससे मौलिक और प्रथम-व्यक्ति दृष्टिकोण के लिए मुख्यधारा में शामिल होने का बेहतर रास्ता बनता है।
प्रसार के नए रूपों में निवेश: जानकारी और ज्ञान तक हाशिये के समुदायों की पहुंच आसान और प्रासंगिक बनाने पर काम करने में गैर-लाभकारी संस्थाएं सबसे आगे रही हैं। बहुभाषी और मल्टीमीडिया प्रसार को आर्थिक सहयोग देकर कुछ सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को पार किया जा सकता है जो बड़े पैमाने पर पहुंच बनाने में बाधा डालती हैं। इसका मतलब उन नई पहलों का सहयोग करना है जो यह तय करती हैं कि विकलांग लोगों जैसे हाशिए के समुदायों भी इनमें शामिल हैं।
प्रौद्योगिकी और नवाचार को आर्थिक सहयोग देना: पारंपरिक तरीकों से डिजिटल होने के बदलाव और नए मीडिया उपकरणों के विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है। बड़े, लाभकारी मीडिया प्लेटफार्मों के वर्चस्व वाले प्रसार परिदृश्य में गैर-लाभकारी संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बने रहने के लिए तकनीकी समाधानों में निवेश करना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे, कई भाषाओं में अधिक पॉडकास्ट और ऑडियो-विज़ुअल रिपोर्टिंग को फंड करने से गैर-लाभकारी संस्थाओं को ऐसा कंटेन्ट तैयार करने में मदद मिल सकती है जो अधिक सुलभ और प्रासंगिक है।
हालांकि गैर-लाभकारी मीडिया संगठन तुरंत नतीजे नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनका दूरगामी असर वंचित समुदायों के दुनिया को देखने के नजरिए की उपेक्षा करने वाले गैर-बराबरी वाले समाज में महत्वपूर्ण हो सकता है। वे जनता की भलाई के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकने वाले ज्ञान के भंडार (रिपोजिटरीस) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फंडर्स और समाजसेवियों के लिए इन संस्थाओं को पहचानना और इनमें निवेश करना महत्वपूर्ण है।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—

“जब दिव्यांग लोगों के साथ काम करना शुरू किया तो पहले डर लगता था कि इनके साथ कैसे काम करेंगे। एक साथी जो देख नहीं पाते थे, एक दिन बिना पूछे मैं उनका हाथ पकड़ कर उन्हें सड़क पार करवाने लगा। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन बाद में समझाया कि पहले विकलांग व्यक्ति से पूछें कि उन्हें मदद की जरूरत है भी या नहीं, उन पर दया ना करें।“ राजस्थान में यूथ फॉर जॉब्स के प्रोग्राम लीड मेहताब सिंह, अपने अनुभव से मिली सीख को कुछ इस तरह बताते हैं। विकलांग-जन पर दया करने की बजाय उनकी काबिलियत पर भरोसा कर उनके साथ बेहतर काम किया जा सकता है।
यूथ फॉर जॉब्स अपने ग्रासरूट्स एकेडमी प्रोग्राम के जरिए देश के कई राज्यों के गांवों और ब्लॉक में काम कर रही है। यह देखने, सुनने, बोलने और शारीरिक रूप से बाधित विकलांग-जन को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने का काम शिक्षा और सरकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने के माध्यम से करते हैं। विकलांग-जन के साथ काम करने के अपने सालों के अनुभव के आधार पर वे बताते हैं कि विकलांग-जन के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए कई पहलुओं पर विचार करने की जरूरत होती है। विकलांग-जन को कई तरह के गहरे पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, खासकर जमीनी स्तर पर। उनकी ज़रूरतें अलग हैं जिन्हें प्रोग्राम के साथ प्रभावी ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। यह तय करने के लिए, संस्थाओं को अपने प्रोग्राम में कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
यूथ फॉर जॉब्स की संस्थापक मीरा शिनोय कहती हैं कि कार्यक्रमों में विकलांग-जन यानि जिस समुदाय के साथ हम काम कर रहे हैं, उनकी आवाज का होना जरूरी है। हाशिए पर मौजूद हर समुदाय की ही तरह विकलांग-जन में भी अपने समुदाय की बेहतरी के लिए काम करने की प्रबल इच्छा होती है, इसका सकारात्मक इस्तेमाल, हमारे कार्यक्रमों को और सटीक बनाने में कारगर साबित होता है। उनके जीवन की हकीकतों से निकलकर आने वाले सुझाव और समाधान अक्सर हम नहीं सोच पाते हैं। इस बात को यूथ फॉर जॉब के साथ करौली में काम कर रहे शाहिद मोहम्मद इस तरह कहते हैं – संस्था ‘विकलांगों के लिए और विकलांगों द्वारा’ की विचारधारा के साथ काम करती है।
मेहताब बताते हैं, “ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विकलांग-जन को खुद संदेह रहता है कि वे कोई काम कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन जब वे सफलतापूर्वक स्वयं काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें खुद पर विश्वास बनता है। वे इलाके के बाकी विकलांग-जनों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। अगर हम एक जिले के व्यक्ति के पास जाकर कहें कि हम उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में और रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं तो वो शायद हमारा यकीन न करें। लेकिन अगर वे किसी अन्य विकलांग व्यक्ति से मिलते हैं जो उन्हें यही जानकारी देता है, तब वे विश्वास कर लेते हैं।“
ग्रासरूट फैलो प्रह्लाद बेनीवाल जो खुद विकलांग हैं, कहते हैं कि उन्हें इसकी तरफ सबसे पहले इसी बात ने आकर्षित किया था कि यह विकलांग व्यक्तियों द्वारा और उन्हीं के लिए काम करने वाला प्रोग्राम है।

समुदाय की जरूरत को समझना न केवल किसी कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिहाज से जरूरी होता है, बल्कि उसे जमीन पर लागू करने में भी इसकी अहम भूमिका है। मेहताब कहते हैं, “हमें पहले यह पहचानना होता है कि कैंडिडेट की जरूरतें क्या हैं। जैसे अगर वह 18 साल से कम उम्र का है तो उसे उचित शिक्षा कैसे मिले यह तय करना होता है। 18 से अधिक उम्र वाले के लिए यह पहचानना होता है कि उसे किसमें रुचि है, उसकी विकलांगता किस तरह की है, और उसे किस कौशल के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसी तरह यदि किसी की उम्र ज्यादा हो तो यह देख पाना कि क्या कोई स्वरोजगार की ट्रेनिंग उसके लिए ज्यादा सही रहेगी।“
विकलांग-जन की जरूरतों को पहचानने को लेकर शाहिद कहते हैं, “हमें इसका भी ध्यान रखना होता है कि उनकी शिक्षा का मौजूदा स्तर क्या है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो उच्च शिक्षा पा चुके होते हैं, ऐसे में उसी स्तर का रोजगार भी उनके लिए खोजना होता है। वे जिनका शिक्षा-स्तर रोजगार के लिए नहीं होता, उन्हें उनकी रूचि के मुताबिक स्वरोजगार से जोड़ना होता है। मेहताब उदाहरण देते हैं कि एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को एक सरकारी योजना के तहत ई-रिक्शा दिलवाया और फिर उसे किराए पर दे दिया गया ताकि उसकी आय बनी रहे।
इन प्रयासों के बावजूद, यह हमेशा संभव है कि किसी व्यक्ति को कार्यक्रम से मिलने वाले किसी भी विकल्प में रुचि न हो, ऐसे में यह पता लगाना भी महत्वपूर्ण है कि उनका सहयोग कैसे किया जाए। मेहताब इसे समझाने के लिए एक विकलांग युवती का उदाहरण देते हैं जो अपने हाथों का उपयोग नहीं कर पाती है, इस कारण उसे प्रोग्राम द्वारा मिलने वाली नौकरियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उसे खेलों में रुचि थी, इसलिए वह राज्य स्तरीय पैरालंपिक टीम से जुड़ी और कई पुरस्कार भी जीते।
अक्सर विकलांग-जनों को, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में काफी दिक्कतें सामने आती हैं। उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम, पता, पति या पिता का नाम और जन्मतिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां कई बार गलत दर्ज हो जाती हैं। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिंक नहीं होने या फिर गलत लिंक होने से उन्हें ठीक करने में भी समस्याएं आती हैं। शाहिद बताते हैं कि बहुत से लोगों को यूडीआईडी कार्ड या दिव्यांगता सर्टिफिकेट के बारे में पता भी नहीं होता है जो कि विकलांग-जन के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए जरूरी होता है। हम लोगों को इसके बारे में और सरकारी योजनाओं पर अपडेट करते हैं और यूडीआईडी कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज बनवाने या ठीक कराने में उनकी सहायता करते हैं। इसके लिए हमें हर जगह उन्हें और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को भी साथ लेकर जाना होता है, ताकि हम उन्हें यह प्रक्रिया सिखा सकें और वे यह खुद कर पाने में सक्षम हो सकें।
केवल रोजगार या शिक्षा ही नहीं, सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना और इनसे जोड़ने में सहायता करना भी विकलांग-जन की एक अहम जरूरत है। इससे भी समुदाय का विश्वास हासिल हो पाता है और उनके साथ ज्यादा सहजता से काम हो पाता है।
विकलांग-जन के लिए प्रभावी कार्यक्रम डिजाइन करने के साथ-साथ, उन्हें जमीन पर अमल में लाने वाली एक कुशल और संवेदनशील फील्ड टीम का होना भी जरूरी है। टीम की ट्रेनिंग ऐसी होना जरूरी है जो उन्हें जमीनी चुनौतियों के तत्काल समाधान खोजने और परिस्थितियों के अनुसार काम के तरीकों में बदलाव लाने में सक्षम बनाए।
मीरा, अपने काम में फील्ड टीम और समुदाय के प्रशिक्षण के लिए असरदार ट्रेनिंग मॉड्यूल को बहुत महत्वपूर्ण बताती हैं, साथ ही वह उनमें लचीलापन होने को भी जरूरी बताती हैं। वे कहती हैं, “पहले साल हमने अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में वह चीजें डाली जो हमें उनके लिए जरूरी लगी, इसके बाद तुरंत ही समुदाय से हमें सुझाव आने लगे कि उन्हें क्या काम की चीज लगी और क्या नहीं। फिर अगले साल हमने समुदाय से पूछा कि उन्हें क्या जरूरी लगता है और फिर हमने उसी अनुसार नए ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए गए। आज समुदाय के लोग ही सारा कॉन्टेंट फिर से बना रहे है जो कि पूरी तरह से उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है।” वे इसमें आगे जोड़ते हुए कहती हैं कि मूल कॉन्टेंट उनके द्वारा ही बनाया जाता है हमारी भूमिका उसमें मुख्य रूप से तकनीकी सहयोग देने की होती है।
प्रशासन से साझेदारी, विकलांग-जन के लिए स्थानीय स्तर पर सरकारी आर्थिक सहायता तक पहुंच को भी आसान बनाती है।
शाहिद बताते हैं, “केवल संस्था का ही संवेदनशील होना काफी नहीं है। वे कंपनियां जिनके साथ वे रोजगार के लिए काम करते है, उनसे भी समय-समय पर बातचीत करनी होती है। हमें लगातार लोकल मार्केट को स्कैन करते रहना होता है, और एम्प्लॉयर (संभावित रोजगार देने वाले) को अपने प्रोग्राम की जानकारी देनी होती है। समय-समय पर हम उनकी विकलांग-जन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने पर भी काम करते हैं और उन्हें एक तय ट्रेनिंग अवधि के लिए विकलांग-जन को रोजगार देने के लिए प्रेरित करते हैं।” शाहिद बताते हैं कि वे विकलांग कैंडीडेट और एम्प्लॉयर के बीच संवाद को लेकर भी काम करते हैं और उनकी टीम के आपसी तालमेल के लिए ट्रेनिंग आयोजित करते हैं।
स्थानीय प्रशासन और समुदाय के साथ साझेदारी जमीन पर काम करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बारे में मीरा बताती हैं कि उनकी फील्ड टीम जिला, ब्लॉक और पंचायत के अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद करती है। साथ ही, यह आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सहायक और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आदि से भी लगातार संपर्क में रहती है। इससे क्षेत्र के अधिक से अधिक जरूरतमंद विकलांग-जनों तक पहुंच बन पाती है और उनसे जुड़ना संभव हो पाता है। साथ ही, क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता तय करने के लिए रचनात्मक तरीके भी अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए असिस्टिव टेक (जैसे व्हीलचेयर, टैबलेट आदि) के वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित कर संबंधित सरकारी अधिकारियों को बुलाना, इससे उनका काम भी नजर में आता है और विकलांग-जन की जरूरतें भी पूरी होती हैं। प्रशासन से साझेदारी, विकलांग-जन के लिए स्थानीय स्तर पर सरकारी आर्थिक सहायता तक पहुंच को भी आसान बनाती है, जो प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के लिए मुश्किल होता है।
संस्थाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि समाज में विकलांग-जन के प्रति पूर्वाग्रह तो मौजूद हैं ही, साथ ही माता-पिता भी उनके प्रति ज्यादा चिंतित रहते हैं और संभव है कि उन्हें काम करने की अनुमति न देना चाहें। मेहताब कहते हैं कि ऐसे में दिव्यांग साथी, परिवारों को समझाने की भूमिका बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के अपने अनुभव के आधार पर वे बताते हैं कि विकलांग महिलाओं को घर से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं मिलती है – न शिक्षा के लिए और न ही रोजगार के लिए। प्रह्लाद बताते हैं, “माता-पिता भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित रहते हैं और पूछते हैं कि अगर उन्हें कोई कठिनाई आती है तो क्या होगा। हम उन्हें अन्य महिला दिव्यांगों से जोड़ते हैं और काम के लिए प्रेरित करने के लिए उनकी कहानियां साझा करते हैं। कुछ मामलों में उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को साथ में रोजगार भी दिलवा देते हैं।”
मेहताब कहते हैं कि कभी-कभी किसी विकलांग महिला की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, इसलिए हम पति-पत्नी दोनों को एक ही स्थान पर रोजगार दिला देते हैं, जैसे राशन की दुकान पर।
अपने काम में आने वाली चुनौतियों के बारे में मीरा कहती हैं कि नियोक्ता (एम्प्लॉयर) को यह समझा पाना कि किसी विकलांग को रोजगार देने से उनके काम पर नकारात्मक असर नहीं होगा, यह एक बड़ी चुनौती है। छोटे और मझोले उद्योगों में नियोक्ताओं को समझा पाना और मुश्किल होता है, बड़ी कंपनियां तो फिर भी अपने सीएसआर लक्ष्यों के चलते कुछ सहयोग दे देती हैं। इन्हें देखते हुए हमें इसका खास खयाल रखना होता है कि हमारी ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले विकलांग युवा अपना काम अच्छी तरह से कर पाएं। समुदाय की जरूरतों का खयाल रखने के साथ-साथ नियोक्ता को नुकसान ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखना होता है। विकलांग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं जैसे पूर्वाग्रहों का मुकाबला करना भी एक बड़ी चुनौती है।
जमीनी चुनौतियों को लेकर शाहिद बताते हैं, “रोजगार के संदर्भ में विकलांग-जन में शिक्षा का स्तर एक बड़ी चुनौती है, खासकर कि ग्रामीण इलाकों में। प्राइमरी या मिडिल तक तो वो फिर भी गांव के स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर हाई स्कूल और आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल पास में नहीं होते हैं। विकलांग-जन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और इस कारण अधिकांश मामलों में उनकी आगे की पढ़ाई रुक जाती है। रोजगार देने वाले भी कम से कम दसवीं तक पढ़े लोगों को ही लेना चाहते हैं, ऐसे में उनके लिए रोजगार के मौके तलाश पाना मुश्किल होता है। गांवों में और छोटी जगहों पर रोजगार के मौके वैसे ही कम होते हैं ऐसे में विकलांग कैंडीडेट के पास के शहर में हम उनके लिए काम खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपना घर छोड़कर एक अंजान जगह पर अकेले रहना या गांव से शहर रोज आना-जाना भी उनके लिए मुश्किल होता है।” शाहिद बताते हैं कि कुछ मामलों में वे कैंडीडेट के परिवार के अन्य व्यक्ति जो विकलांग नहीं है को भी उसी जगह रोजगार दिला देते हैं ताकि उनकी जरूरतों का खयाल उनका ही कोई परिवार जन रख सके।
विकलांग-जन के लिए काम करने के लिए उत्साहित युवाओं और संस्थाओं को मीरा सुझाव देतीं हैं कि “विकलांग-जन के लिए काम करने का जज्बा होना सबसे पहली जरूरत है। इसके बाद यह समझना जरूरी है कि इस क्षेत्र में अलग-अलग पहलुओं पर बहुत काम किए जाने की जरूरत है। इसलिए यह पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन से पहलू हैं जिन पर काम नहीं किया जा रहा है या जिन पर और काम किए जाने की जरूरत है। जहां पहले से ही काफी काम हो रहा है उसे ही करने से बचें, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि आपके काम के लगातार और स्थाई रूप से चलते रहने (सस्टेनेबिलिटी) की गुंजाइश बनी रहे।“
—
भारत कौशल रिपोर्ट 2021 एक चिंताजनक स्थिति को सामने लाती है: इसके अनुसार भारत के लगभग आधे स्नातक (ग्रेजुएट्स) रोजगार के लिए अयोग्य माने जाते हैं। खुली बेरोजगारी यानि अवसरों की कमी के कारण होने वाली बेरोजगारी के आंकड़े जो 2012 में 2.1% थे, 2018 में बढ़कर 6.1% हो गए। भारत के श्रम बल सर्वेक्षणों के 45 सालों में, यह सबसे उच्चतम दर है। अलग-अलग शैक्षणिक स्तरों पर युवा बेरोजगारी की दरें तेजी से बढ़ रही हैं। उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12) तक की शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं के लिए यह दर 10.8% से बढ़कर 23.8% हो गई है। उच्च शिक्षा लेने वाले लोगों के लिए तो स्थिति और भी चिंताजनक है। साल 2022-23 के दौरान, स्नातकों की बेरोजगारी की दर 19.2% से बढ़कर 35.8% हो गई, जबकि स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) के लिए यह आंकड़ा 21.3% से बढ़कर 36.2% हो गया है।
इस कड़वे सच से जाहिर है कि भारत में कौशल विकास को एक नई नजर से देखने और इसके दोबारा मूल्यांकन की जरूरत है, ताकि रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि कौशल कार्यक्रम प्लेसमेंट की ओर ले जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत बड़ी चुनौतियों को उजागर करती है जो अभी भी हल नहीं हुई हैं। आजकल, कौशल कार्यक्रम अक्सर तात्कालिक समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों को एक साथ लाने की जरूरत ज्यादा है। शिक्षा और कौशल के बीच एक महत्वपूर्ण खाई है-एक ऐसा अंतर जो अनगिनत लोगों को नौकरी बाजार के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं करता है।
इस समस्या से निपटने के लिए, भारत की शिक्षा प्रणाली में सीखने की प्रक्रिया की शुरूआत में ही ऐसे व्यावहारिक कौशल शामिल करने चाहिए जो रोजगार के लिए जरूरी हैं। साथ ही, कौशल विकास में लगे लोगों को शिक्षा प्रणाली के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ना होगा, ताकि व्यावहारिक कौशल को कक्षाओं में शुरू से ही शामिल किया जा सके। शिक्षा और कौशल के बीच की खाई को पाटना जरूरी है, ताकि शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार हो सके जो युवाओं को वास्तविक जीवन की चुनौतियों और रोजगार के अवसरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सके।
भारत में सरकारी शिक्षा प्रणाली न केवल खराब तरीके से लागू की गई है, बल्कि इसमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण की भी कमी है। यह केवल तात्कालिक रटने की शिक्षा तक सीमित रह गई है। यह प्रणाली अक्सर पुराने पाठ्यक्रमों और संदर्भ से हटकर सैद्धांतिक जानकारी पर जोर देती है, जिससे छात्रों को वास्तविक जीवन के कौशल निखारने का मौका नहीं मिलता। नतीजतन, स्नातक करने के बाद युवा नौकरी बाजार की जरूरतों के लिए तैयार नहीं होते हैं।
शिक्षा प्रणाली आमतौर पर 12 साल के चक्र के हिसाब से चलती है, जिसके बाद उच्च शिक्षा के रास्ते खुलते हैं। स्नातक डिग्री के लिए तीन साल और, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरटीआई) या पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग अवधि होती है। इस तरह औपचारिक शिक्षा के लिए 12 से 15 साल का समय लगता है। इसके विपरीत, कौशल प्रशिक्षण को अक्सर तात्कालिक समाधान के रूप में देखा जाता है- यानि संक्षिप्त पाठ्यक्रमों से तुरंत नतीजे मिलने का वादा किया जाता है। वैसे तो माइक्रो-क्रेडेंशियल्स का अपना महत्व है, लेकिन यह दृष्टिकोण शिक्षा प्रणाली में मौजूद संरचनात्मक खामियों का समाधान नहीं करता।
माध्यमिक विद्यालय यानि कक्षा पांचवी से आठवीं, बच्चों को काम-काज की दुनिया से रूबरू करवाने का सही समय है।
उदाहरण के लिए, आईटी कंपनियों में चैट एग्जीक्यूटिव की भूमिका एक समय में उच्च आकांक्षा वाला पद हुआ करता था, लेकिन अब इसे एंट्री-लेवल माना जाता है। इस भूमिका के लिए मजबूत अंग्रेजी कौशल की जरूरत होती है जिसमें व्याकरण और शब्दों का सही इस्तेमाल शामिल है और यह तुरंत नहीं सीखा जा सकता है। एक भाषा सीखने में सालों का अभ्यास और अनुभव लगता है। साथ ही, एक चैट एग्जीक्यूटिव में आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें अस्वीकृतियों को संभालने की क्षमता और प्रभावी संवाद कौशल भी होना चाहिए। ये क्षमताएं केवल ज्ञान पर निर्भर नहीं करती बल्कि इसमें व्यक्तित्व विकास और भावनात्मक लचीलापन भी अहम हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली सही ढंग से नहीं सिखा पाती है, और कौशल विकास कार्यक्रम से भी इन्हें तुरंत नहीं सुधारा जा सकता है।
इसी तरह इलेक्ट्रीशियन या प्लंबर आदि जैसी तकनीकी भूमिकाओं के लिए, कुछ बुनियादी कौशल-जैसे कि गणितीय और व्यवसाय विशेष से जुड़ी क्षमताओं को शुरुआती शिक्षा के दौरान आसानी से विकसित किया जा सकता है। इन भूमिकाओं के लिए अंकगणित और समस्या समाधान के कौशल की जरूरत होती है, जिन्हें केवल अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा प्रभावी ढंग से नहीं सिखाया जा सकता। पारंपरिक रूप से, ये कौशल अनुभवी विशेषज्ञों के साथ लंबे समय तक काम करने के बाद आता है जो स्वाभाविक लेकिन कम औपचारिक तरीका है।
हालांकि ज्ञान और जानकारी अहम है, लेकिन व्यावहारिक कौशल को जल्दी सिखाना, सीखने को और ज्यादा प्रासंगिक बना सकता है। माध्यमिक विद्यालय यानि कक्षा पांचवी से आठवीं, बच्चों को काम-काज की दुनिया से रूबरू करवाने का सही समय है। वे जो विषय पहले से पढ़ रहे हैं, यह उन्हीं के जरिए हो सकता है ताकि सीखने की प्रक्रिया ज्यादा विषयों की समझ देने वाली और व्यावहारिक बन सके। उदाहरण के लिए, वास्तविक दुनिया के प्रोजेक्ट्स-जैसे कि कक्षाओं या शौचालयों के निर्माण को पाठ्यक्रम में शामिल करने से बच्चे माप, निर्माण, रसायन विज्ञान (जैसे कि टाइल्स जैसी सामग्रियों का चिपकना) और अन्य व्यावहारिक विज्ञान सीख सकते हैं। इससे बच्चों को व्यावहारिक संदर्भ में ज्ञान मिलेगा।

इस समय कौशल विकास कार्यक्रम कई सीमाओं में बंधे हुए हैं। इनमें सबसे अहम किसी कौशल को सीखने के लिए बहुत सीमित समय दिया जाना और व्यापक शैक्षिक यात्रा के साथ उन्हें असंगत तरीके से जोड़ना है।
अवास्तविक अपेक्षाएं – आमतौर पर कौशल विकास कार्यक्रमों में 18 से 29 साल के युवा वयस्क शामिल होते हैं। उनके लिए वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता कौशल जैसे अहम प्रशिक्षणों को महज 50 घंटों में पूरा करने की कोशिश की जाती है। इस जल्दीबाजी वाले नजरिए में यह मान लिया जाता है कि ये जटिल और महत्वपूर्ण कौशल जल्दी सीखे जा सकते हैं जो अवास्तविक है। औसत स्किलिंग मॉड्यूल जरूरी ज्ञान को छोटा करके, कम समय में ज्यादा से ज्यादा सत्रों में भरने की कोशिश होती है। किसी असेंबली लाइन की तरह यहां प्रतिभागियों से उम्मीद की जाती है कि वे सीमित समय में ही बहुत सारी जानकारी को आत्मसात करें।
बुनियादी कौशल और बारीकियों की कमी – यह समस्या शुरुआती शिक्षा के दौरान मजबूत बुनियादी ज्ञान की कमी के कारण और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वित्तीय साक्षरता और डिजिटल दक्षता जैसे महत्वपूर्ण कौशल छठवीं से बाहरवीं कक्षा तक सिखा दिए जाएं, तो बच्चों में एक गहरी और बारीक समझ पैदा होगी। इससे बाद में मिलने वाला पेशेवर कौशल प्रशिक्षण और प्रभावी होगा। कौशल प्रशिक्षण केवल 18 साल की उम्र के बाद ही दिया जाए तो कई मामलों में इसे देरी भी माना जा सकता है। सरकारी निकायों, सीएसआर पहलों और यहां तक कि शैक्षिक संगठनों द्वारा डिजाइन किए गए ये कार्यक्रम अक्सर प्रभावशीलता से ज्यादा लागत और दक्षता को प्राथमिकता देते हैं। बिना बुनियादी ज्ञान के, छोटे-छोटे कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अक्सर कम प्रभावी होते हैं और सीखने वाले ज्ञान को आत्मसात कर उसे लागू करने के लिए संघर्ष करते हैं।
डिजिटल असमानता – ज्यादातर छात्रों, खासकर निम्न-आय वाले परिवारों के युवाओं के पास जरूरी डिजिटल टूल्स जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप कम्प्यूटर नहीं हैं। उनके पास मोबाइल फोन हो सकते हैं और वे वीडियो देख सकते हैं लेकिन असली शिक्षा और कौशल पाने के लिए ज्यादा इंटरैक्टिव और आकर्षक डिजिटल अनुभवों की जरूरत होती है। पहुंच की यह कमी बहुत से युवाओं को उनके कौशल कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही नुकसान में डाल देती है। इससे उनके लिए आधुनिक नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना और सफल होना कठिन हो जाता है।
कई सरकारी पहलों के बावजूद, व्यावसायिक प्रशिक्षण सीमित, वर्गवादी और नकारात्मक धारणाओं से ग्रस्त है। इसके कारण पारंपरिक शैक्षणिक तरीकों को प्राथमिकता दी जा रही है जबकि वे रोजगार की गारंटी नहीं देते हैं। इसके अलावा, कई कौशल विकास कार्यक्रम, जिन्हें आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों या टियर-II और टियर-III शहरों के युवा उपयोग करते हैं, उनमें खराब गुणवत्ता, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कम प्लेसमेंट जैसी समस्याएं हैं। इससे रोजगार की समस्या और बढ़ जाती है।
पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती यह है कि कुछ पेशों में सीखे गए कौशल की कीमत, अकुशल कार्यों की तुलना में कम होती है। कौशल प्रशिक्षण के बाद भी, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए नौकरी का बाजार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ये ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी संयुक्त मासिक आय 40 से 50 हजार रुपए है। इन परिवारों की आय घरेलू काम या शहर में ऑटो-रिक्शा चलाने जैसी नौकरियों से अर्जित होती है। ये युवा अक्सर पॉप कल्चर, विज्ञापनों और शहरी, उच्च वर्ग की जीवनशैली से प्रभावित होते हैं जिससे अपने भविष्य की आय के लिए उनकी अपेक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं। लेकिन जब वे अपनी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के बाद नौकरी पाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें निराशा होती है क्योंकि वे केवल 12 से 15 हजार रुपए प्रतिमाह की नौकरियां ही हासिल कर पाते हैं। उनकी अपेक्षाओं और कौशल के बाजार मूल्य के बीच का यह अंतर उन्हें गहरी निराशा में डाल देता है। इस समस्या का समाधान एक समग्र दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है क्योंकि केवल कौशल प्रशिक्षण या शिक्षा कार्यक्रम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं।
कौशल विकास कार्यक्रमों को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए, उन्हें सीखने की एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, जो जितना जल्दी हो सके शुरू हो और क्रमिक रूप से विकसित होती रहे।
काम की गरिमा बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण हो सबके लिए जरूरी – अगर कम उम्र से ही कई तरह के कौशलों से परिचय हो जाए तो इससे कुछ खास तरह कामों के प्रति ज्यादा सम्मान पैदा हो सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे सभी छात्रों के लिए व्यापक शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह, शिक्षार्थियों को नर्सिंग, कॉस्मेटोलॉजी और अन्य कुशल व्यवसायों में करियर बनाने के रास्ते बताए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ड्राइविंग को एक वैध उद्यमिता के अवसर के रूप में मान्यता देना या घरेलू काम के महत्व को समझना तभी संभव होगा जब इन कौशलों को शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सामान्य बनाया जाए। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को करियर विकल्प तलाशने और उसका सम्मान करने का मौका मिले, न कि केवल उन करियर विकल्पों का जो ‘व्हाइट-कॉलर’ माने जाते हैं। काम की गरिमा तभी हासिल होगी जब हर तरह के कौशल को सभी को समान रूप से सिखाया जाएगा।
मूल्य-आधारित शिक्षा और कौशल विकास को एक साथ आगे बढ़ाना चाहिए – भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित और भाषाओं जैसे विषयों को भी याद कर लेने पर जोर दिया जाता है, यहां तक कि प्रारंभिक शिक्षा में भी यही होता है। यह जापान जैसे दूसरे देशों की प्रणालियों से पूरी तरह अलग है, जहां शिक्षा के पहले पांच साल शिष्टाचार और व्यवहार पर केंद्रित होते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि एकीकृत मूल्य-आधारित शिक्षा और कौशल विकास अभाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, न कि केवल एक सैद्धांतिक बात। छठवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं में स्पष्ट दिशा-निर्देश और संरचित कार्यक्रम स्थापित करके, स्कूल धीरे-धीरे पाठ्यक्रम में कौशल और मूल्यों को एकीकृत कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्र न केवल शैक्षणिक रूप से सक्षम हों बल्कि आवश्यक जीवन कौशल और नैतिक आधार भी पा सकें।
कौशल प्रशिक्षण की सफलता दर का गंभीर पुनर्मूल्यांकन जरूरी है, क्योंकि कई कार्यक्रम अपनी प्रभावशीलता को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं।
कुछ गिने-चुने उदाहरण हैं, जहां मूल्य आधारित शिक्षा को कौशल विकास के साथ मिलाने की कोशिश की गई है। ऋषि वैली एक प्रभावशाली स्कूल है जो इस बात का उदाहरण है कि कैसे शिक्षा को सफलतापूर्वक मूल्यों और कौशल के साथ जोड़ा जा सकता है। उनका मॉडल, जो अपने समग्र दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता पर ध्यान देता है बल्कि मूल्यों और नैतिक विकास पर भी जोर देता है। इसी तरह, मोंटेसेरी शिक्षण विधियां, विशेषकर प्री-किंडरगार्टन (नर्सरी से पहले की) शिक्षा में, कम उम्र से ही अनुभवात्मक शिक्षा और आलोचनात्मक सोच कौशल के विकास पर जोर देती हैं। व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त होने पर भी इन विधियों को मुख्यधारा की शिक्षा में अभी तक पूरी तरह से अपनाया नहीं गया है।
कुछ स्कूलों में, बोर्ड पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में कौशल शिक्षा को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के लिए, सौंदर्य प्रशिक्षण देने वाले कार्यक्रमों में, सफाई और माहवारी जैसे महत्वपूर्ण जीवन पाठों के साथ व्यावहारिक कौशल को जोड़ने पर चर्चा की जा रही है।
हालांकि, ये सफलताएं उन लोगों तक सीमित हैं जो इस तरह की शिक्षा तक पहुंच सकते हैं और ये प्रणालीगत बदलाव को नहीं दर्शाती हैं। अगर स्कूल शिक्षा को कौशल प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाए, वर्तमान कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, और धन को व्यापक, रचनात्मक पहलों की ओर मोड़ा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की जा सकती है । गैर-लाभकारी संगठन और डोनर्स यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे व्यावसायिक कौशल को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए निवेश का समर्थन करेंगे, ताकि भविष्य के कौशल विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके। इसके अलावा, कौशल प्रशिक्षण की सफलता दर का गंभीर पुनर्मूल्यांकन जरूरी है, क्योंकि कई कार्यक्रम अपनी प्रभावशीलता को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं। आखिर में, धन को संकीर्ण, कार्य-विशिष्ट प्रशिक्षण से ज्यादा समग्र और रचनात्मक परियोजनाओं की ओर स्थानांतरित करना चाहिए-जैसे कि बुनियादी ढांचे पर आधारित शिक्षा के अवसर-जो समस्या-समाधान और टीमवर्क जैसे महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने में मदद कर सकते हैं, और छात्रों को आधुनिक श्रमशक्ति के लिए बेहतर तैयार कर सकते हैं।
गैर-लाभकारी संगठन, लाभ के लिए काम करने वाली संस्थाएं और फंड देने वाली संस्थाएं कौशल प्रशिक्षण के लिए मिलने वाले सीएसआर और अन्य प्रकार के फंड की हिमायत कर सकती हैं, ताकि उसी समुदाय के भीतर स्कूली शिक्षा में निवेश भी शामिल हो सके। इसके अलावा जो समाजसेवी संगठन स्कूलों के साथ काम करते हैं, उन्हें अपने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक और अन्य कौशल शामिल करने चाहिए। अगर हम शुरुआत से ही शिक्षा प्रणाली में कौशल को शामिल करें तो छात्र एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। यह उन्हें भविष्य के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तैयार करता है। इस दृष्टिकोण से ज्यादा सक्षम और बेहतर श्रमशक्ति का निर्माण हो सकेगा।
गैर-लाभकारी संगठन स्कूली पाठ्यक्रम में मूल्य-आधारित शिक्षा और कौशल को शामिल करने पर भी जोर दे सकते हैं, जिसे अक्सर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनदेखा कर दिया जाता है। इससे छात्रों को न केवल नौकरियों के लिए बल्कि सार्थक करियर और जिम्मेदार नागरिकता के लिए भी तैयार किया जा सकेगा।
मौजूदा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कम सफलता दर की वास्तविकता का सामना कर सामाजिक क्षेत्र को इस पर काम करने की जरूरत है जिसका कारण कमजोर बुनियादी शिक्षा है। कई संस्थाएं 70-80% प्लेसमेंट दर का दावा करती हैं जबकि ऑडिट से पता चलता है कि वास्तविक सफलता दर लगभग 20-35% के करीब है। यह असमानता दर्शाती है कि संस्थानों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और स्कूलों में ही अलग-अलग स्तरों पर कौशल को शामिल करना चाहिए। केवल आधारभूत कमजोरियों को दूर करके ही हम अगले कुछ सालों में सफलता दर को सुधारने का यथार्थवादी लक्ष्य बना सकते हैं।
सरकार और सामाजिक क्षेत्र को कौशल प्रशिक्षण बजट को सीधे नियोक्ताओं को संकीर्ण, कार्य-विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए देने की बजाय, इन निधियों को व्यापक रचनात्मक पहलों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, बुनियादी ढांचे पर खर्च का एक बड़ा हिस्सा शिक्षार्थियों को व्यावहारिक परियोजनाओं, जैसे वास्तुशिल्प डिजाइन सिखाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे छात्रों को टीमवर्क, समस्या-समाधान और रचनात्मकता जैसे जरूरी कौशल सिखाने के साथ-साथ शैक्षणिक विषयों का ज्ञान भी मिलेगा।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—







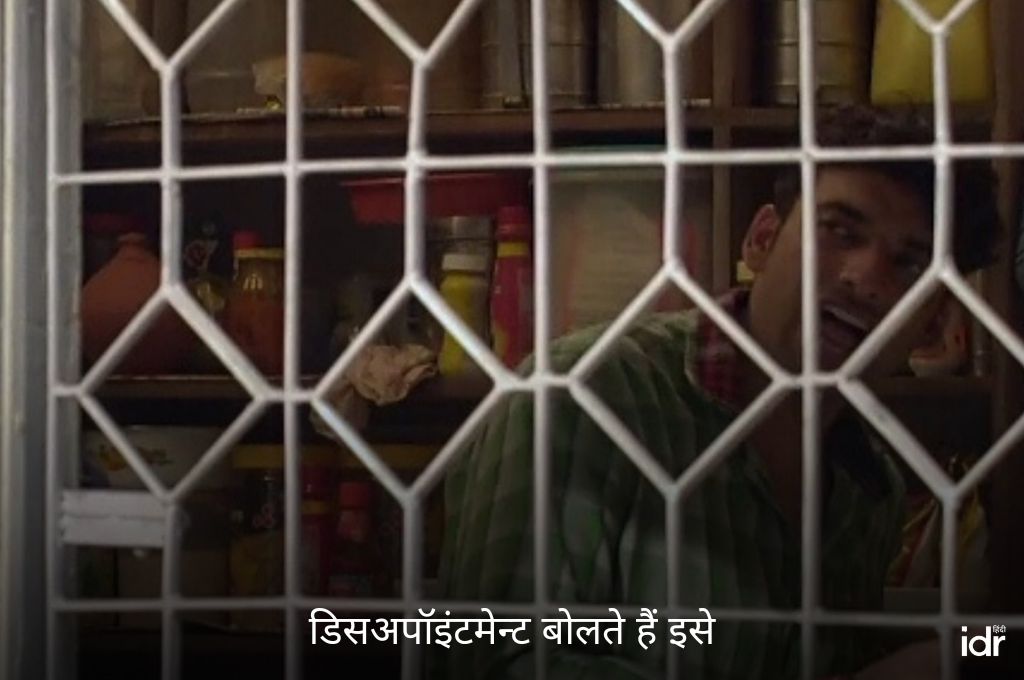
दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक, ब्रह्मपुत्र, असम राज्य से होकर बहती है। यह राज्यभर में फैली लगभग 3,000 बड़ी और छोटी आर्द्रभूमियों का घर है, जो 1,400 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। स्वाभाविक रूप से, ये जल प्रणालियां कई पक्षियों और जानवरों का घर हैं। साथ ही, वे इसमें और इसके आसपास रहने वाले समुदायों के लिए आजीविका का एक स्रोत भी हैं। वर्षा जल से भरने वाले स्रोत, ज्यादा पानी में होने वाली फसलों जैसे धान वगैरह उपजाने में मददगार होने के साथ-साथ मछली पकड़ने के क्षेत्र भी हैं, क्योंकि यहां कई तरह की मछलियां पाई जाती हैं।
मछली असम की संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है। उदाहरण के लिए, कई समुदाय जैसे कैबार्ता अपनी पहचान मछली पकड़ने के इर्द-गिर्द ही परिभाषित करते हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही अनियमित वर्षा, औद्योगिक प्रदूषण और जरूरत से ज्यादा मछली पकड़े जाने जैसे कारणों के चलते इनका पेशा अब खतरे में है। यह फोटो निबंध, राज्य की अलग-अलग नदियों के किनारे बसे जिलों में रहने वाले, कैबार्ता समुदाय के लोगों के जीवन पर बात करता है। यह बताता है कि कैसे समुदाय बदलते सामाजिक और भौगोलिक वातावरण में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है।

असम में कैबार्ता समुदाय ब्रह्मपुत्र के नदी क्षेत्रों में निवास करता रहा है। उनके नाम का अर्थ है -‘वे लोग जो पानी से अपनी आजीविका कमाते हैं।’ ऐतिहासिक रूप से, वे भारत में असम, बंगाल, बिहार और ओडिशा के साथ-साथ नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में भी रहते आए हैं। कैबार्ता पारंपरिक रूप से मछुआरे, नाव चलाने वाले और किसान होते हैं। समुदाय को व्यवसाय के आधार पर उपजातियों में भी विभाजित किया गया है: जलिया कैबार्ता (मछली पकड़ने और नाव चलाने का काम करने वाले लोग) और हलिया कैबार्ता (जो खेती का काम करते हैं)। असम के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में, इस समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है और इसके सदस्य कामरूप जिले के सुआलकुची, हाजो, बामुंडी और ज़िलगुरी जैसे कस्बों और गांवों में कैबार्ता टोलों में रहते हैं। शिक्षाविद बताते हैं कि कैबार्ता जिन इलाकों में रहते हैं, उसकी वजह उनकी निम्न सामाजिक स्थिति के साथ-साथ ऐतिहासिक रूप से भूमिहीन होना भी है। इन परिस्थितियों के बावजूद, अपने कौशल के कारण वे आजीविका कमाने में कामयाब रहे हैं।

हालांकि, बीते कुछ सालों में, जलवायु परिवर्तन उनकी जीवटता के लिए खतरा बनकर उभरा है और उनके आर्थिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर रहा है।
मिट्टी के कटाव और बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण खेती को होने वाले नुकसान ने इन द्वीपों में कई लोगों के लिए खेती करना मुश्किल बना दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इससे उपजातियों के बीच व्यावसायिक मतभेद भी मिट गए हैं जिससे जलिया के साथ-साथ हलिया समूह को भी मछली पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
कामरूप के हलोगांव गांव के महलदार (मछुआरा समुदाय के प्रमुख) दीपेन दास कहते हैं, “यहां के लोगों को मछली पकड़ने से मुश्किल से ही काम भर की आय हो पाती है। ऐसे में आप मछली पकड़ने या ना पकड़ने वाली जातियों के ऐतिहासिक उपविभाजन के बने रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?” दीपेन कहते हैं कि आजकल आर्थिक हताशा, कैबार्ता लोगों को प्रजनन के मौसम (अप्रैल से मध्य जुलाई) में भी मछली पकड़ने पर मजबूर करती है। इस समय असम सरकार की ओर से सार्वजनिक जल निकायों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

चूंकि इन द्वीपों में आजीविका खतरे में है, इसलिए जीवनयापन के साधन के रूप में मछली पकड़ने पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। दीपेन के अनुसार, “यहां तक कि (कैबार्ता की तुलना में अधिक वित्तीय सुरक्षा वाले समूहों समेत) परंपरागत रूप से मछली ना पकड़ने वाले समुदाय कोलकाता से बेहतर उपकरण खरीद रहे हैं और ब्रह्मपुत्र में मछली पकड़ने के व्यापार को सीख रहे हैं।” हालांकि, मछली पकड़ने की प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बावजूद, मछली की प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। दीपेन कम प्रजनन दर की वजह न केवल जलवायु परिवर्तन बल्कि तेजी से हो रहे शहरीकरण, जैसे मुख्य गुवाहाटी और न्यू गुवाहाटी के बीच नए पुलों के निर्माण को मानते हैं। विभिन्न देशों में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि पुल निर्माण का नदियों और नालों के जलीय जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कैबार्ता समुदाय के सदस्यों की आर्थिक स्थिति पूरे राज्य में और यहां तक कि एक ही जिले के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, कामरूप के सुआलकुची में रहने वाले कैबार्ता लोग उसी जिले के हाजो, हलोगांव और ज़िलगुरी में रहने वाले लोगों से बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन सुआलकुची की समृद्धि का श्रेय स्वदेशी रेशम बुनाई उद्योग को जाता है। सुआलकुची में कैबार्ता लोगों ने अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षित करने और उन्हें बेहतर (व्हाइट-कॉलर) नौकरियां हासिल करने के लिए प्रेरित करने के साथ, अपनी आय के साधन बढ़ाने के लिए ज्यादा फायदा देने वाले रेशम बुनाई के पेशे को अपनाया है।
यह देखना दिलचस्प है कि मछली पकड़ने की बजाय बुनाई को प्राथमिकता देने ने भी, समुदाय में लैंगिक मानदंडों को कमजोर करने में मदद की है। सुआलकुची में पुरुषों के साथ-साथ महिला बुनकर भी हैं। यह मछली पकड़ने से एकदम उलट है जहां लैंगिक भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं। इसमें कैबार्ता महिलाएं मछली पकड़ने से पहले और बाद की गतिविधियों में तो शामिल होती हैं, लेकिन वे मछली पकड़ने में सीधे तौर पर शामिल नहीं होती हैं। समुदाय के सदस्य बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि नदियां महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं होती हैं। लेकिन हाजो की महिलाएं इसका अपवाद हैं क्योंकि उनके गांव में नदी तक पहुंचना आसान नहीं है, और मछली पकड़ने का काम तालाबों, आर्द्रभूमि और दलदलों में किया जाता है।

हाजो में कैबार्ता समुदाय के लोग नदी तक अपनी सीमित पहुंच और सीमित आर्थिक विकल्पों की तुलना सुआलकुची से करते हुए कहते हैं कि “उनकी पहुंच नदी तक है। हमें छोटे जलस्रोतों से जो मिल पाता है, वही मिल पाता है।”

एक समय गर्व की वजह रहा मछली पकड़ने का व्यवसाय, अब असम के कैबार्ताओं के लिए लंबे समय तक स्थाई आजीविका देने वाला काम नहीं रह गया है। इसलिए अब युवा पीढ़ी आजीविका के दूसरे विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो रही है जिन्हें पाना मुश्किल है। यह कहानी, पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने वाले उन कई समुदायों की कहानियों में से एक है जो किसी तरह अपने सांस्कृतिक इतिहास को बचाए हुए हैं। लेकिन उनकी पहचान पर आए इस खतरे को टालने में कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है।
मानो कि औद्योगिक प्रदूषण, प्रतिस्पर्धा और जल स्रोतों का नुकसान पर्याप्त नहीं था कि कैबार्ता को सरकार के दबाव का भी सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार की नीयत सही है लेकिन मछली पकड़ने की अवधि के साथ-साथ, कुछ खास तरह के जालों के उपयोग पर असम सरकार के प्रतिबंधों ने स्थिति को और खराब कर दिया है। समुदाय के सदस्य अक्सर प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना जैसी योजनाओं के असफल वादे के बारे में बोलते हैं, जिसके तहत असम सरकार मछली ना पकड़े जाने के महीनों में 1,500 रुपये देती है।
ऐसे समय में, जब सरकार देश में नीली क्रांति और मत्स्य पालन क्षेत्रों को विकसित करने पर जोर दे रही है, तब उसे उन लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जिन्होंने तमाम बाधाओं को पार करते हुए पीढ़ियों से नदियों के किनारे जीवनयापन किया है। असल में, उनका ज्ञान मछली उद्योग के निर्माण की हर उस योजना के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जिसकी कल्पना सरकार करती है।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—
देश में जब विकसित भारत की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा था, उस समय यह महसूस किया गया होगा कि स्वस्थ भारत के बिना विकसित भारत बेमानी है। यही कारण है कि आज विकसित भारत के नारे से पहले स्वस्थ भारत का नारा दिया जाता है। दरअसल यह स्वस्थ भारत का नारा देश के नौनिहालों को केंद्र में रख कर गढ़ा जाता है क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो हम समृद्ध देश की संकल्पना को साकार कर पाने में सक्षम होंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में भारत के बच्चे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे कुपोषण मुक्त और स्वस्थ हैं? हालांकि सरकारों की ओर जारी आंकड़ों में कुपोषण के विरुद्ध जबरदस्त जंग दर्शाई जाती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अभी भी हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं और पांच साल तक की उम्र के अधिकतर बच्चे कुपोषण मुक्त नहीं हुए हैं।
वर्ष 2022 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें दौर के दूसरे चरण की जारी रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण की तुलना में मामूली सुधार हुआ है लेकिन अभी भी इस विषय पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। भारत में अभी भी प्रतिवर्ष केवल कुपोषण से ही लाखों बच्चों की मौत हो जाती है। सर्वेक्षण के अनुसार करीब 32 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषण के कारण अल्प वजन के शिकार हैं। जबकि 35.5 प्रतिशत बच्चे कुपोषण की वजह से अपनी आयु से छोटे कद के प्रतीत होते हैं। दरअसल बच्चों में कुपोषण की यह स्थिति मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिलाएं एनीमिया की शिकार पाई गई है। जिसका असर उनके होने वाले बच्चे की सेहत पर नजर आता है। रिपोर्ट के अनुसार 15 से 49 साल की आयु वर्ग की महिलाओं में कुपोषण का स्तर 18.7 प्रतिशत मापा गया है।

देश के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक देखी गई है उसमें राजस्थान भी आता है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से बेहद कमजोर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में यह स्थिति और भी अधिक गंभीर है। राज्य के अजमेर जिला स्थित नाचनबाड़ी गांव इसका एक उदाहरण है। जिला के घूघरा पंचायत स्थित इस गांव में अनुसूचित जनजाति कालबेलिया समुदाय की बहुलता हैं। पंचायत में दर्ज आंकड़ों के अनुसार गांव में लगभग 500 घर हैं। गांव के अधिकतर पुरुष और महिलाएं स्थानीय चूना भट्टा पर दैनिक मज़दूर के रूप में काम करते हैं। जहां दिन भर जी तोड़ मेहनत के बाद भी उन्हें इतनी ही मज़दूरी मिलती है जिससे वह अपने परिवार का गुज़ारा कर सकें। यही कारण है कि गांव के कई बुज़ुर्ग पुरुष और महिलाएं आसपास के गांवों से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते है। समुदाय में किसी के पास भी खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है। खानाबदोश जीवन गुजारने के कारण इस समुदाय का पहले कोई स्थाई ठिकाना नहीं हुआ करता था। हालांकि समय बदलने के साथ अब यह समुदाय कुछ जगहों पर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थाई रूप से निवास करने लगा है। लेकिन इनमें से किसी के पास ज़मीन का अपना पट्टा नहीं है।
वहीं शिक्षा की बात करें तो इस गांव में इसका प्रतिशत बेहद कम दर्ज किया गया है। यह इस बात से पता चलता है कि गांव में कोई भी पांचवीं से अधिक पढ़ा नहीं है। जागरूकता के अभाव के कारण युवा पीढ़ी भी शिक्षा की महत्ता से अनजान है। गरीबी और जागरूकता की कमी के कारण गांव में कुपोषण ने भी अपने पांव पसार रखे हैं। इस संबंध में गांव की 28 वर्षीय जमुना बावरिया बताती हैं कि गांव के लगभग सभी बच्चे शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। गरीबी के कारण उन्हें खाने में कभी भी पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं हो पाता है। घर में दूध केवल चाय बनाने के लिए आता है। वे बताती हैं कि उनके पति घर में ही कागज़ का पैकेट तैयार करने का काम करते हैं। जिससे बहुत कम आमदनी हो पाती है। ऐसे में वह बच्चों के लिए पौष्टिक आहार का इंतजाम कहां से कर सकती हैं? वे बताती हैं कि गांव के अधिकतर बच्चे जन्म से ही कुपोषण का शिकार होते हैं क्योंकि घर की आमदनी कम होने के कारण महिलाओं को गर्भावस्था में संपूर्ण पोषण उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिसका असर जन्म के बाद बच्चों में भी नज़र आता है। वे स्वयं एनीमिया की शिकार हैं।
वहीं 35 वर्षीय अनिल गमेती बताते हैं कि वे गांव के बाहर चूना भट्टा पर दैनिक मज़दूर के रूप में काम करते हैं। जहां उनके साथ उनकी पत्नी भी काम करती है। लेकिन गर्भावस्था के कारण अब वह काम पर नहीं जाती है क्योंकि उसे हर समय चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने शरीर में पोषण और खून की कमी बताई है। अनिल कहते हैं कि पहले मैं और मेरी पत्नी मिलकर काम करते थे तो घर की आमदनी अच्छी चलती थी। लेकिन गर्भ और शारीरिक कमज़ोरी के कारण अब वह काम पर नहीं जा पा रही है। ऐसे में घर की आमदनी भी कम हो गई है। अब उन्हें चिंता है कि वह पत्नी को कैसे पौष्टिक भोजन खिला पाएंगे? अनिल कहते हैं कि डॉक्टर ने दवाईयों के साथ साथ विटामिन और आयरन की टैबलेट भी लिख दी थी जो अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध भी हो गई, लेकिन साथ ही डॉक्टर ने पत्नी को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन भी खिलाने को कहा है जो उन जैसे गरीबों के लिए उपलब्ध करना बहुत मुश्किल है। वे कहते हैं कि इसके अच्छे खाने की व्यवस्था करने के लिए मुझे साहूकारों से कर्ज लेना पड़ सकता है। जिसे चुकाने के लिए पीढ़ियां गुजर जाती हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से बेहद कमजोर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में स्थिति और भी गंभीर है।
गांव की 38 वर्षीय कंचन देवी के पति राजमिस्त्री का काम करते हैं। वे बताती हैं कि उनके तीन बच्चे हैं। दो लड़कियां हैं जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हैं जबकि बेटा गांव के आंगनबाड़ी में जाता है। देखने में उनका बेटा काफी कमज़ोर लग रहा था। वे बताती हैं कि पति की आमदनी बहुत कम है। ऐसे में बच्चों के लिए पौष्टिक खाने की व्यवस्था करना मुमकिन नहीं है। वह आंगनबाड़ी जाता है जहां खाने के अच्छे और पौष्टिक आहार उपलब्ध होते हैं जिसके कारण उसके अंदर इतनी भी ताकत है। कंचन कहती हैं कि गांव में गरीबी के कारण लगभग सभी बच्चे ऐसे ही कमजोर नजर आते हैं। घर की आमदनी अच्छी नहीं होने के कारण परिवार न तो बच्चों का और न ही गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा पाता है। एक अन्य महिला संगीता देवी कहती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र के कारण गांव के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुछ हद तक पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो जाता है। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कर गांव के बच्चों को कमज़ोर होने से बचा लिया है।
वास्तव में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की यह स्थिति भयावह है। जिसे दूर करने के लिए एक ऐसी योजना चलाने की ज़रूरत है जिससे गर्भवती महिलाएं और बच्चों को सीधा लाभ पहुंचे। इस कड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्ता और सहायिका सराहनीय भूमिका अवश्य निभा रही हैं। लेकिन इस बात पर भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भूख और कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए 1975 में शुरू किया गया आंगनबाड़ी अपनी स्थापना के लगभग पांच दशक बाद भी अब तक शत-प्रतिशत अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर सका है?
यह लेख मूलरूप से चरखा फीचर्स पर प्रकाशित हुआ था।
आपको बताया गया है कि अगले दो दिनों में आपको एक ग्रांट प्रपोजल बनाना है। इसमें बताना है कि अगले पांच सालों के लिए आपकी संस्था की क्या योजनाएं हैं, अभी आप क्या असर डाल पा रहे हैं, और यह भी बताइए कि कैसे इस ग्रांट के ना मिलने से आपकी संस्था धराशायी हो सकती है।
आपकी मैनेजर डेडलाइन से दो घंटे पहले:
एक ग्रांट के लिए लगभग सालभर तक मेलबाजी करने के बाद डोनर ने आपकी संस्था को फंड न देने का फैसला किया है। इसकी एकमात्र वजह ये है कि इस पूरे वक्त में उनके सीएसआर गोल्स बदल गए हैं और अब वो आपकी संस्था के साथ मेल नहीं खाते।
आपके को-फाउंडर्स एक दूसरे को देखकर:
बोर्ड के सदस्यों की सलाह है कि आपको दूसरी पीढ़ी की लीडरशिप बनानी चाहिए। उन्हें फंडरेजिंग, डाइवर्स टीम मैनेज करने, ऑफिस वर्क कल्चर बनाने जैसी बातों के लिए तैयार करना चाहिए।
आपकी सीईओ जो ऐसी किसी पोजीशन के लिए कैंडिडेट के अप्लाई करते ही छुट्टी पर जाने की योजना बना लेती हैं:
आप हेल्थ बेनेफिट्स या सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं क्योंकि आप महीनों से ओवरटाइम काम करते आ रहे हैं। आपकी मैनेजर कहती हैं कि वो आपके सहयोग की कद्र करती हैं।
आपकी प्रतिक्रिया:
आपकी मैनेजर आपसे आपकी संस्था के आउटकम्स से जुड़े आंकड़े बताने वाली 60 पेज की रिपोर्ट लिखने के लिए कहती हैं। आप आंकड़ों में सीधे दिखने वाली गलतियां करते हैं और आपके बार चार्ट्स किसी को समझ नहीं आ रहे हैं।
आपकी मैनेजर:
आपकी मैनेजर, आखिरकार अपने साथियों (कर्मचारियों) की शिकायत से तंग आ चुकी हैं। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अभी मौजूद सारा फंड वह एक टीम रिट्रीट पर खर्च करेंगी जो जयपुर के एक फैंसी हेरिटेज होटल में होगी:
…और इसका प्रमाण है

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।