मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढ़ोने) का काम करने वाले दलित समुदाय के लोगों को एक प्रकार के जातिगत और व्यवस्थागत भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। इस भेदभाव के प्रति बेजवाड़ा विल्सन ने पुरज़ोर आवाज़ उठाई है। पीढ़ियों से इसी काम को करने वाले एक ऐसे ही दलित परिवार में जन्म लेने वाले विल्सन बचपन से ही अपने लोगों को इस अमानवीय प्रथा का शिकार होते देख रहे थे। इस अन्याय को देख अपने अंदर पैदा हुए आक्रोश और ग़ुस्से के कारण ही उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया।
बेज़वाड़ा ने एक ज़मीनी स्तर का आंदोलन शुरू किया जिससे हाथों से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन हो सके। उस आंदोलन का नाम था सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए)। 1993 से आज तक, एसकेए ने देश भर में वालंटियरों की मदद से सामाजिक और कानूनी लड़ाई जारी रखी है जिसकी वजह से हज़ारों दलितों को इस अमानवीय प्रथा से आज़ादी मिली है। सन 2016 में बेज़वाड़ा विल्सन को दलितों के जन्मसिद्ध मानवीय गरिमा के अधिकार को वापस लेने के अथक प्रयासों के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
आप लगभग तीन दशक से अधिक समय से सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए) चला रहे हैं। एक आंदोलन को शुरू करने और उसे इतने लम्बे समय तक चलाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है?
इसके निर्माण के लिए कोई ठोस प्रयास किये गए हों ऐसा नहीं है। संघर्ष ज़रूर रहा है – वास्तविक संघर्ष। ग़ुस्सा और पीड़ा भी थी जिससे आंदोलन को उभर कर आने की जगह मिली। हमने इतना ज़रूर किया कि ग़ुस्से को मज़बूती दी और उसे एक दिशा दी। और इसी ग़ुस्से ने आगे चलकर सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन का रूप ले लिया।
एसकेए रजिस्टर्ड भी नहीं है क्योंकि यह औपचारिक संस्था नहीं है – यह एक आंदोलन की धारा है – और इस धारा में लोग जुड़ते जाते हैं। आज पूरे देश में लगभग 4,800 वालंटियर हैं।
आज भी हमें इस बात से ग़ुस्सा आता है – आज भी यह समस्या क्यों मौजूद है (हाथ से मैला ढोने की समस्या), इतने सालों के अथक प्रयास के बावजूद भी? आज से ३५ साल पहले इसी ग़ुस्से के कारण हमने अपना यह आंदोलन कर्नाटक में शुरू किया था। और आज भी महिलाओं को शौचालय साफ़ करता देख उतना ही ग़ुस्सा आता है। उम्र, तजुर्बे या समय के साथ कुछ भी नहीं बदला।
हम लोगों को संगठित करने के लिए अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं; हम केवल अपने अंदर के इस ग़ुस्से को सही दिशा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस अन्याय के प्रति हमारे जैसा ही ग़ुस्सा रखने वाले लोगों को जब हमारी यह दिशा सही लगती है तो वे हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं।
शुरुआती दौर में आपने इस अमानवीय प्रथा के अन्याय के प्रति लोगों को किस प्रकार जागरूक करना शुरू किया?
हमारी सबसे बड़ी समस्या भाषा को लेकर थी। दरअसल इस विषय और मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास किसी तरह की भाषा नहीं थी। समय के साथ साथ हम आज़ादी, पुनर्वास और उन्मूलन (हाथ से मैला ढोने का) जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर बात करने लगे लेकिन ये सभी शब्द बाद में आए। जब हमने शुरू किया था तब हम केवल इतना जानते थे कि कोई भी इस काम को करने के लिए मजबूर नहीं है और न ही उसकी ऐसी कोई मजबूरी होनी चाहिए जिससे कि वह हाथों से मैला ढ़ोने का काम करे।
तब से अब तक का सफर काफी लम्बा रहा है। इस सफर के दौरान, कभी मंथन हुआ है, कभी कुछ फट पड़ा है तो कभी लड़ाइयाँ और बहसें भी हुई हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमें एक बात समझ में आई कि हमें ग़ुलाम बना दिया गया है।
इस बात की समझ और इसका एहसास होने से पहले हम यह मान चुके थे कि हम केवल ग़ुलामी ही कर सकते हैं। ग़ुलामी की अपनी इस स्थिति का ज़िम्मेदार हम खुद को ही मानते थे। हम बेरोज़गार थे और हमारी न तो कोई आशा थी और न ही सपने। हम अनपढ़, कमजोर और गरीब लोग थे।
फिर 1991 में – बाबासाहेब अम्बेडकर के शताब्दी महोत्सव में – मैंने इन मुद्दों पर उनका लिखा हुआ कुछ पढ़ा। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम मैला ढोने वाले इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम गरीब, कमज़ोर या अनपढ़ हैं या हमने मैला ढोने का काम खुद से चुना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ने हमें मैला ढोने वाला बनाया है। तब हमनें यह समझा कि किसी ने हमें बन्दी बना के रखा हुआ है, वर्णव्यवस्था ने हमें यहां लाकर खड़ा किया है। और इसमें पितृसत्ता जुड़ जाने से हमारे समुदाय की महिलाओं का हाल और भी बदतर कर दिया है। तब हमने यह सवाल पूछा: हम इस सब के खिलाफ कैसे लड़ें?
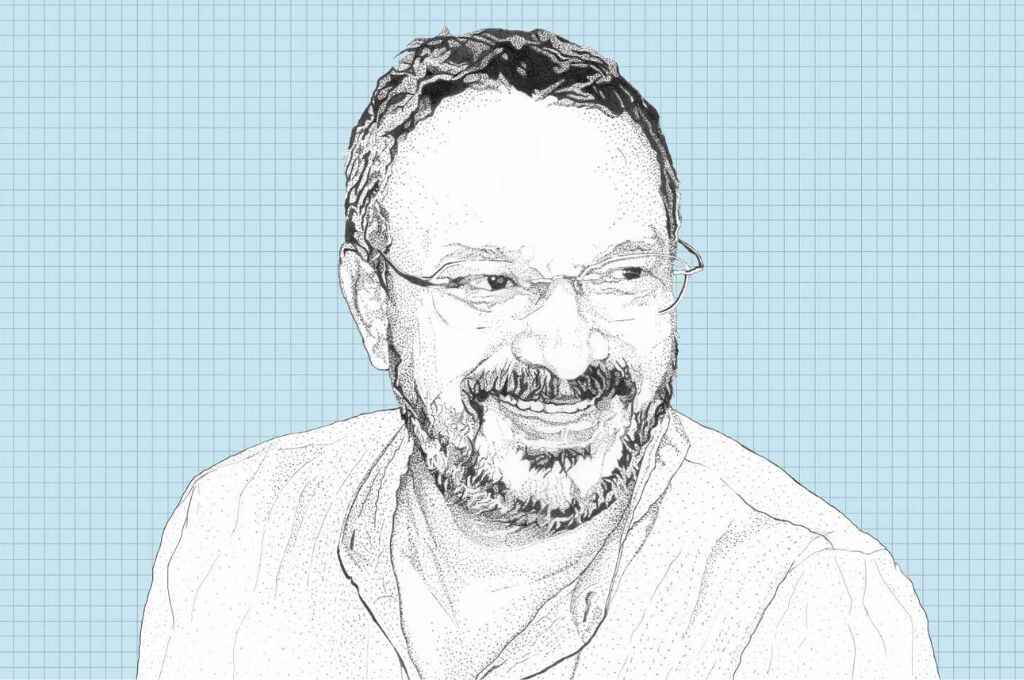
जल्द ही मैला ढोने वाले समुदाय के अलावा दूसरे समुदायों ने भी एकजुटता दिखाई क्योंकि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के ख़िलाफ़ है। एकजुटता और दूसरों के सहयोग से हमें बल मिला।
मुक्ति की शुरुआत तब हुई जब हाथ से मैला ढोने वालों ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ी।
समुदाय ने मुद्दे को समझना भी शुरू किया। कोई किसी दूसरे का मल साफ़ नहीं करना चाहता परन्तु परिस्थितियों की वजह से वे ऐसा कर रहे थे। जब हम नें उनसे कहा “जब और लोग दूसरों का मल साफ़ किये बिना जी रहे हैं, तो तुम भी उसके बिना क्यों नहीं जी सकते?” तो वे सोचने पर मजबूर हुए। जो समुदाय अभी तक चुप था उसने खुल कर बोलना शुरू किया। मुक्ति की शुरुआत तब हुई जब हाथ से मैला ढोने वालों ने इस मुद्दे पर खुद अपनी चुप्पी तोड़ी और मुखर हो कर बोलना शुरू किया।
और जब लोगों का मुद्दे में विश्वास बढ़ा वह अपने आप ही आंदोलन से जुड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे और उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि “हम सब क्या कर सकते हैं?”
क्या हम जा कर कुछ शौचालय तोड़ डालें? चलो! नहीं? अच्छा, हम मैले की टोकरी तो जला ही सकते हैं। प्राधिकारियों को एक ज्ञापन देते हैं। हो गया! जब हम ये सब कर रहे हैं तो क्या हम चुप्पी बनाये रखें? कम से कम नारे लगाते हैं। कुछ नारे बनाते हैं! और ऐसे बात आगे बढ़ती गयी – सब कुछ संगठित रूप से, स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता जाता है – फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है। फिर थोड़ा और।
मैंने और मुझ जैसे ही एसकेए के अन्य वरिष्ठ लोगों ने आंदोलन को एक दिशा दी है। लोगों को अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ना अच्छा लगता है। हम उन्हें कहते हैं “कुछ समय तक इस दिशा में चल कर देखते हैं, अगर कामयाबी नहीं मिली तो आपकी सुझाई दिशा में चलेंगे। यदि पहली दिशा में चल कर कामयाब हुए तो आप जब भी तैयार हों, शामिल हो जाइएगा। इसके पीछे का यह दर्शन है कि ‘किसी को भी पीछे न छोड़ें’।
कई दशकों से आप इस मुद्दे पर काम करते आ रहे हैं। क्या आपने सरकार की प्रतिक्रिया में फ़र्क देखा है?
बदलाव तो आया है लेकिन इस बदलाव की गति बहुत धीमी है। शुरुआत में सरकार ने न तो ज़रा भी दिलचस्पी दिखाई और न ही इस दिशा में कोई प्रयास किया। समय के साथ इसमें बदलाव आया है। पर सरकार का हमेशा वही एक एजेंडा नहीं बना रह सकता। उनकी क्षमता और स्थायित्व सिर्फ पाँच साल का है। पाँच साल के बाद वे अपना पैटर्न बदल देते हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी ऐसा ही करती हैं – हर 6-7 साल में अपना पैटर्न और ध्यान का केंद्र बदल देती हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी लड़ाई लगातार जारी रहनी चाहिए और अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें बिना रुके काम करना होगा।
यदि सरकार के अंदर एजेण्डे और प्राथमिकताएँ बदलती हैं आप गति कैसे बनाए रखते हैं?
सरकार कहेगी कि समस्या ख़त्म हो चुकी है – वह लोगों को इसका अहसास भी दिला देती है और लोग सरकार की बातों पर विश्वास भी कर लेते है। लेकिन यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लगतार लोगों को इस बात की याद दिलाते रहे कि समस्या ख़त्म नहीं हुई है।
हम जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे, मीडिया से बात करेंगे। और इस सब के दौरान औरतें – हाथ से मैला ढोने वाली औरतें – केंद्र में होंगी। उनके शब्दों में दूसरे लोगों की बातों से ज़्यादा ताक़त है। जब ये औरतें लोकतांत्रिक सरकार से सवाल करती हैं और न्याय मांगती हैं और जब वो कहती हैं कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन हो, लोगों को उनकी बात सुननी ही पड़ती है।

आपने मैला ढोने के कानून को बदल डाला। आपने ये कैसे किया?
आंदोलन ने कानून बदलने के लिए सरकार पर दबाव डाला। पहलेपहल हम सरकार के प्रतिनिधियों से 2010 में मिले और मैन्युअल स्केवेंजिंग एक्ट के प्रारूपण में शामिल हुए। तीन साल बाद जब 2013 में यह एक्ट लागू हुआ तब हमें लगा कि हमारा काम हो गया। और हमने सरकार के साथ बातचीत बंद कर दी। पर जब अमल करने की बात आयी तो कुछ भी नहीं बदला क्योंकि नौकरशाही का रवैया और व्यवहार पहले जैसा ही था।
कानून के उल्लंघन के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी पर क़ानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।
सबसे बड़ी विडम्बना है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के ऊपर कानून का उल्लंघन करने के लिए कानूनी कार्रवाही नहीं की गयी है – एक भी अधिकारी को सजा नहीं मिली। कुछ मामलों में एफ़आईआर दर्ज की गयी हैं पर वे अभियोग लगने के चरण तक नहीं पहुंची हैं; आरोप पत्र दायर किये गए हैं पर वे मुक़दमे के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं।
2013 में इस एक्ट के लागू होने से पहले हमने 20 साल तक लड़ाई लड़ी। तब से अब तक नौ साल से ज़्यादा बीत गए हैं और आज हमें लगता है कि हम रुक गए हैं। एक भी व्यक्ति को सज़ा नहीं हुई है। बहुत से मामलों में ज़िला अधिकारी /कलेक्टर अपराधी है – वह व्यक्ति जिसके अपने ज़िले में हाथ से मैला ढ़ोने का काम होता है और वह उसे रोकता नहीं है।
अगर आप ऐसे तीन कलेक्टरों को एक हफ्ते के लिए भी जेल भेज दें तो तुरंत ही सब कुछ बदलता नज़र आएगा। आज वे अपनी जान बचा रहे हैं लेकिन उनके कारण इतने लोग उनकी सीवर की लाइन और सेप्टिक टैंक साफ़ करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं।
जब किसी को इस प्रथा या काम से मुक्ति मिल जाती है तब आपको कैसा महसूस होता है?
जब कोई मुक्त हो जाता है तो हम उस बदलाव का उत्सव नहीं मनाते हैं। यदि 10 लोग इस काम को छोड़ पाते हैं हम न तो किसी तरह का जश्न मनाते हैं और न ही उनकी वाहवाही करते हैं। क्योंकि इस पेशे से निकल के आना उनका अपना निर्णय है इसलिए वे जश्न मनाएं या न मनाएं यह निर्णय भी उन्हीं का होना चाहिए।
दूसरा, यह हमारी सफलता नहीं बल्कि उनकी सफलता है, उनके परिवार की सफलता है। इसलिए हमने कभी इस संख्या की गिनती नहीं की। लोग हमसे पूछते हैं: एसकेए ने कितने लोगों को इस काम से मुक्ति दिलवाई है? हम कहते हैं हमें नहीं मालूम। हम कभी गिनते नहीं हैं। हमें यह पता है कि कितने लोग अभी भी हाथ से मैला ढोने का काम कर रहे हैं। हम उस संख्या को गिनते हैं और ट्रैक करते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य उस संख्या को शून्य तक पहुंचाना है। दूसरों की तरह हमारा उद्देश्य गिनती को बढ़ाना नहीं है। हम चाहते हैं कि गिनती घटती रहे।
हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के प्रयासों के बारे में हमें बताइये।
पुनर्वास के लिए किसी भी तरह के अच्छे प्रयास नहीं हुए हैं। आप महिलाओं को दो भैसें और कुछ पैसा देकर ये नहीं मान सकते हैं कि वे खुश हो जाएंगी। 5,000 साल पुरानी प्रथा और रवैए को बदलने की कोशिश के लिए पुनर्वास और रोज़गार के मायनों की समग्र और स्पष्ट समझ होनी चाहिए।
आप को गांव-गांव जा कर हर एक महिला की क्षमता की पहचान करनी होगी। आप कौशल का परीक्षण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने कौशल विकसित करने के अवसर नहीं मिले हैं। आपको क्षमता ढूंढ़नी होगी। आपको देखना होगा कि उनमें कितनी हिम्मत है। ऐसा करने के लिए आपको उनके पास जाना होगा, उनकी ताकत को समझना होगा और ये देखना होगा कि वे क्या कर सकती हैं। और आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं न कि सिर्फ कुछ पैसा दे दें।
भारत में सरकार पुनर्वास को सिर्फ पैसे से जोड़ कर देखती है।
बात सिर्फ पैसे की नहीं है। जिस मदद की ज़रूरत है उसमें पैसा सबसे अंत में और सबसे कम ज़रूरत की चीज़ है। पर भारत में, सरकार पुनर्वास को सिर्फ पैसे से जोड़ कर देखती है। वे 10 लाख देती है वो भी ऋण के रूप में।
या एक महिला को दो भैंसें या बकरियां, एक ऑटोरिक्शा या ऐसा ही कुछ दे देंगे ताकि उसपर उसे बिठा कर उसकी फोटो ले सकें। आप ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह इस गाड़ी को चला कर अपना खर्चा चला पायेगी जब कि इससे पहले उसने ऐसा कभी किया नहीं है? इससे बेहतर है कि आप उन्हें वाजिब अच्छी मासिक आय दें जिससे उनकी जीविका चल सके।
सरकार को हाशिये पर खड़े लोगों के प्रति समाज के रवैये और व्यवहार को बदलने की कोशिश भी करनी चाहिए। अपनी तरफ़ से हम यही कहना चाहते हैं कि इस देश के लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि हाथ से मैला ढोने वालों ने हम सबके लिए सब्सिडी प्रदान की है – उनके काम का आर्थिक लाभ हम सब ने उठाया है।
इस देश के लोगों को यह समझने की ज़रूरत है की हाथ से मैला ढोने वालों ने हम सब को सब्सिडी प्रदान की है।
इसलिए, हम उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, हम उनकी भरपाई कर रहे हैं। सालों तक, हमने उनसे लिया है। इन महिलाओं ने प्रति घर मात्र 30 रूपया महीना पर हमारे शौचालय साफ़ किये हैं। ये एक दिन के काम के लिए सिर्फ एक रूपया हुआ!
इन महिलाओं ने आपको बुनियादी सेवाएं दी हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप इसकी भरपाई करें। लेकिन सरकार का रवैया ऐसा नहीं है। सरकार इसे सब्सिडी के रूप में देखती है, जैसे यह एक मुफ़्त का उपहार हो।
मध्य वर्ग भी इस बात को नहीं समझता है। उसके लिए सब कुछ यहीं पर आ के रुकता है कि “मुझे कुछ मिलना चाहिए।” और इस तरह की सोच समाज के लिए बहुत ख़राब है। कोई ख़ुशी नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कोई मानवता नहीं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
और जानें
- इस प्रदर्शनी को देखें जिसमें दुनिया भर के सफ़ाई कर्मचारियों की कहानियां हैं।
- ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट से जानिये कि हाथ से मैला ढोने वालों के बारे में और किस प्रकार उनके साथ तंत्रानुसार भेदभाव जारी रहता है।
- भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा से जुड़े एक्ट और निर्णयों के बारे में पढ़िए।
और करें
- अन्याय की शिकायत दर्ज कराएँ, आन्दोलन से जुड़ें या हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए अपना समय दें।





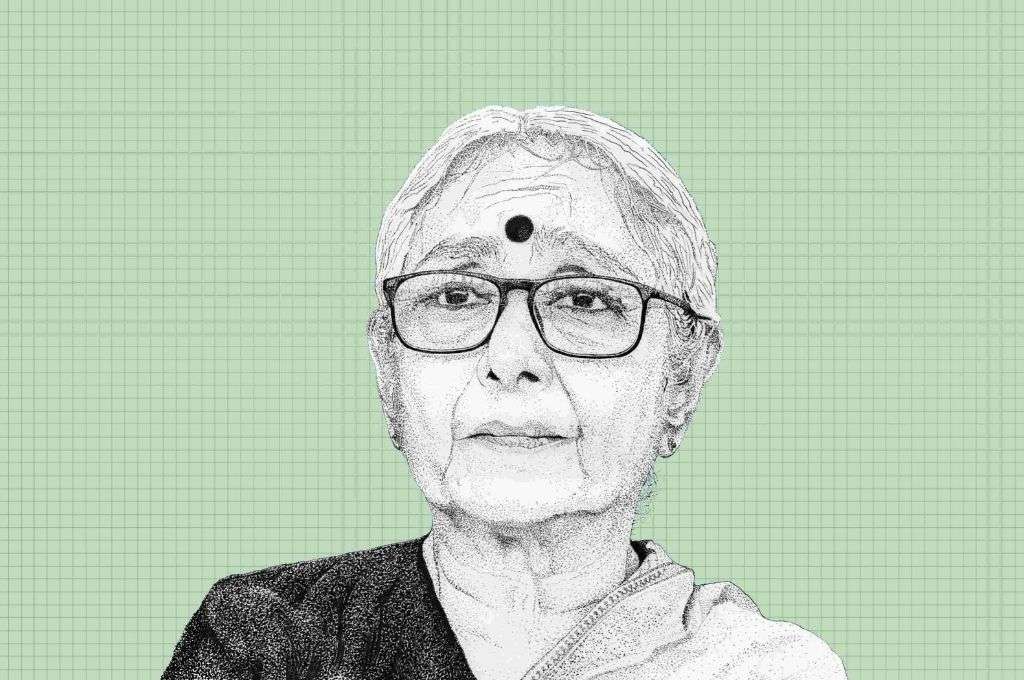

गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपके ईमेल का पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *