
लद्दाख के चांगथांग पठार में में घुमंतू चरवाहे वसंत ऋतु में अपनी पश्मीना बकरियों के झुंडों के साथ प्रवास करते हैं। लेकिन गर्मियां आते-आते इन परिवारों की कई महिलाओं को जननांग के हिस्से में खुजली, संक्रमण और तेज जलन जैसी परेशानियों की शिकायत के चलते लेह लौटना पड़ता है।
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी दिंचिन डोलकर अक्सर घुमंतू महिलाओं से जुड़े ऐसे मामले देखती हैं। वह बताती हैं, “कुछ दिन पहले दो महिलाओं को लेह के सोनम नोरबू अस्पताल रेफर किया गया था। वहां भीड़ होने के चलते उन्हें एक प्राइवेट क्लिनिक में भेजा गया। जांच में यीस्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूटीआई) मिलने पर उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं दी गयीं।”
लेकिन इलाज से मिलने वाली राहत अस्थायी होती है। दिंचिन बताती हैं, “ये संक्रमण बार-बार लौट आते हैं। इसका सीधा संबंध प्रवास के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियों और साफ पानी की कमी से है।”
लद्दाख की घुमंतू महिलाओं के लिए ये संक्रमण केवल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा नहीं, बल्कि तेजी से शुष्क होते मौसम की चेतावनी भी है। पैंतालीस वर्षीय कुंजेस डोलमा हर सुबह अपनी भेड़ों को चराने के लिए पैदल निकलती हैं। वह इस काम को छोड़ नहीं सकती हैं। उनका कहना है, “दोपहर में इतनी गर्मी होती है कि भेड़ों को बाहर ले जाना मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे इतना पसीना निकलता है कि शाम तक सिरदर्द शुरू हो जाता है।”
कुंजेस पानी साथ लेकर चलती हैं जो अक्सर काफी नहीं होता है। वह कहती हैं, “पहले इन रास्तों के दोनों ओर ग्लेशियर दिखते थे और झरने भी खूब बहते थे। अब तो कई जगह एक बूंद पानी तक नहीं मिलता। रूपशू घाटी के कुछ चरागाह रास्तों पर अब भी नदियां बहती हैं, लेकिन ऊपर की तरफ पानी बहुत कम हो गया है।”
पानी की कमी और लगातार पसीने के कारण महिलाओं के लिए साफ-सफाई बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। कुंजेस को हाल ही में एक स्थानीय स्वास्थ्य शिविर में यीस्ट संक्रमण के इलाज से गुजरना पड़ा था। इस दौरान उन्हें पांच दिनों के लिए पेसारी (योनि में लगाने वाली दवा) दी गयी थी।
चांगथांग के घुमंतू बाशिंदे प्रवास के रास्तों पर पानी के अलग-अलग स्रोतों पर निर्भर होते हैं। कुछ जगहों पर सरकार ने बोरवेल और सौर पंप लगाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी छोटी-छोटी प्राकृतिक धाराओं पर ही भरोसा जताते हैं। कुंजेस कहती हैं, “अगर सोलर पंप चल रहा हो, तो सही रहता है। लेकिन अक्सर नल ही खराब हो जाते हैं और फिर पंप किसी काम के नहीं रहते।”
चाय बेचने वाली स्टैनजिन डोलकर बताती हैं कि पिछले साल त्सो कर झील के पास जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए सौर पंप अब बमुश्किल ही काम करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंता लुंडुप जम्यांग कहते हैं, “कभी वायरिंग खराब हो जाती है, तो कभी मोटर में कीचड़ अटक जाता है। हर जाड़े के बाद जमने के कारण पाइप फट भी जाते हैं।”
मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक सोनम लोटस के अनुसार हिमालय लगातार गर्म हो रहा है। वह बताते हैं, “अब जुलाई और अगस्त में तापमान 34–35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।” मद्धम हवा और नमी की कमी गर्मी को और तीव्र बना देते हैं और ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ जाती है। वह आगे जोड़ते हैं, “पिघला हुआ पानी तेजी से सिंधु घाटी में बह जाता है और लद्दाख सूखा ही रह जाता है।”
स्वास्थ्य कार्यकर्ता कुंजेस डोलमा के भारी कपड़ों को भी उनकी हालात का जिम्मेदार मानते हैं। वे उनसे कहते हैं कि पहले याक या भेड़ की ऊन से बने कपड़े हवादार होते थे। लेकिन अब प्रचलित सिंथेटिक कपड़ों में हवादार होने की गुंजाइश नहीं होती। कुंजेस कहती हैं, “वे हमारे काम को नहीं समझते। शाम को लौटने तक ठंडी हवाएं तेज हो जाती हैं। इसलिए हमें इन परतों की जरूरत पड़ती है।”
कपड़ों की इन परतों (जिसमें कमीज, स्वेटर, जैकेट और एक से ज्यादा पतलून शामिल होती हैं) में गर्मी के साथ-साथ पसीना भी होता है। प्रवास के सफर के दौरान इन्हें शायद ही कभी धोया जाता है, जिससे फंगल संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है।
लेह में जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने वाले स्वास्थ्य शिक्षक मोहम्मद भैरक कहते हैं कि स्वच्छता का पानी से सीधा संबंध है। वह बताते हैं, “जब हम घुमंतू महिलाओं से नहाने या मासिक धर्म के दौरान सफाई के बारे में बात करते हैं, तो वे चुप रहती हैं। फिर वे पूछती हैं कि पानी कहां से लायें? ऐसे में कई महिलाएं महीनों तक नहाए बिना रहती हैं।”
आशा कार्यकर्ता सैनिटरी पैड बांटती हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं अब भी कपड़ा ही इस्तेमाल करती हैं। भैरक बताते हैं, “और कभी-कभी वह भी बिना धोए, क्योंकि उनके पास उसे साफ करने और दोबारा इस्तेमाल करने लायक पानी ही नहीं होता।”
लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संक्रमण जांचने के लिए प्रयोगशालाएं नहीं हैं। वे बताते हैं, “हम सिर्फ कुछ साधारण जांचें कर सकते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन, पेशाब, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह।”
लेह के सोनम नोरबू अस्पताल की स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ पद्मा डोलमा पुष्टि करती हैं कि अब अधिक महिलाएं बार-बार होने वाले योनिक या सर्वाइकल संक्रमण की शिकायत लेकर आती हैं। वे बताती हैं, “पहले पानी उपलब्ध था और तापमान भी ठीक होता था। लेकिन अब बढ़ती गर्मी और सूखते स्रोतों के बीच, पूर्वी लद्दाख में लगातार यात्रा में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वच्छता बड़ी चुनौती बन गयी है। मैंने दिल्ली में ऐसे जितने मामले देखे थे, उससे अधिक मामले अब लद्दाख में देखती हूं।”
सफीना वानी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। यह लेख 101 रिपोर्टर्स पर मूल रूप से प्रकाशित आलेख का संपादित अंश है।
यह लेख अंग्रेजी में पढ़ें।
—
अधिक जानें: पढ़ें, उत्तर त्रिपुरा के गौर समुदाय की पलायन यात्रा कैसी रही है।
धैर्य बनाए रखना और किसी को बताये बिना समस्या सुलझाना।

हर हफ्ते नई ट्रेनिंग…पहले ‘सशक्तिकरण’, फिर ‘री-सशक्तिकरण’, फिर ‘ट्रांस-फॉर्मेटिव सशक्तिकरण’। कभी-कभी लगता है, कम्युनिटी से ज्यादा हम ही सशक्त हो रहे हैं।

स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट, मल्टी-लेवल एप्रोच, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच…और इसके बाद एक और पीपीटी जिससे डोनर खुश है, भले ही टीम कन्फ्यूज हो।

फील्ड से रसीदें जमा करना, मैनेजमेंट को संतुष्ट करना और फिर भी बजट बचा हो तो एक और ट्रेनिंग का सुझाव देना। कुल मिलाकर आप रसीद और पर्चियों में ही फंसे रहते हो।
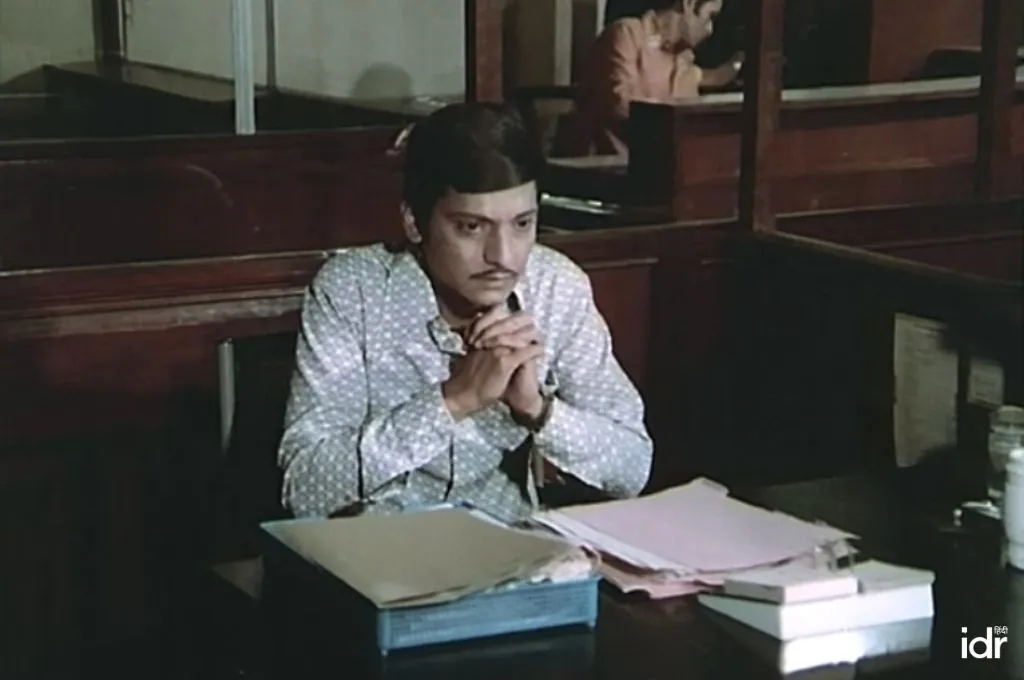
हमारी कैपेसिटी मीटिंग में बनती है, फील्ड में नहीं।

जब फील्ड में कोई मुद्दा हो, डाटा कम मिले, आउटपुट घटे या टीम सवाल पूछे तो केवल एक ही समाधान – कैपेसिटी बिल्डिंग करवा दो।

अब भारत में परमाणु खनिज (जैसे यूरेनियम, थोरियम), महत्त्वपूर्ण खनिज और रणनीतिक खनिज (जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व) की नई खनन परियोजनाएं शुरू होंगी तो उनके लिए आम जनता से राय लेने या जनसुनवाई करने की जरूरत नहीं होगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि यह परियोजनाएं “राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा जरूरतों तथा रणनीतिक विचारों” से जुड़ी हैं।
आठ सितंबर, 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने नए कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में यह बात कही है। ओएम में कहा गया, “मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), 2006 के प्रावधानों के अनुसार और राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता तथा रणनीतिक विचारों को देखते हुए निर्णय लिया है कि खनिज एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग बी में अधिसूचित परमाणु खनिजों और भाग डी में अधिसूचित महत्त्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों से जुड़ी सभी खनन परियोजनाओं को जनसुनवाई से छूट दी जाती है।”
खनिज एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 में पहली अनुसूची के तहत परमाणु खनिज और महत्त्वपूर्ण व रणनीतिक खनिजों की नई परिभाषा तय की गई है। भाग-बी में यूरेनियम और थोरियम युक्त खनिज जैसे मोनाजाइट, पिचब्लेंड, रेर अर्थ वाले खनिज, फॉस्फोराइट, बीच सैंड से मिलने वाले इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन और सिलिमेनाइट को रखा गया है।
वहीं, भाग-डी में 24 महत्त्वपूर्ण खनिज शामिल किए गए हैं, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, गैलियम, इंडियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, रेयर अर्थ (बिना यूरेनियम-थोरियम), टंग्स्टन, टैंटलम, टाइटेनियम, वैनाडियम, पोटाश, फॉस्फेट, सेलेनियम, टेल्यूरियम, रेनियम और प्लेटिनम समूह के तत्वों के साथ-साथ बेरिलियम, कैडमियम, टिन और जिरकोनियम जैसे खनिज शामिल हैं। यह संशोधन साफ करता है कि भविष्य की ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी जरूरतों को देखते हुए भारत इन खनिजों को रणनीतिक संसाधनों की श्रेणी में रख रहा है।
जनसुनवाई की छूट को लेकर मंत्रालय (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयने यह तर्क दिया है कि, “13 मार्च, 2025 को एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किया था, जिसके तहत सभी महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खनन परियोजनाओं पर “आउट ऑफ टर्न” विचार करने की व्यवस्था की गई, ताकि इन प्रस्तावों की मंजूरी (क्लीयरेंस) तेजी से दी जा सके। यह ओएम इसलिए जारी किया गया था क्योंकि ये महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज देश के कई क्षेत्रों की प्रगति के लिए जरूरी हैं, जिनमें हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा शामिल हैं। ये भारत की 2070 तक ‘नेट जीरो’ की प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए भी अहम हैं।
भारत में ईआईए, 2006 कानून विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन के लिए बनाया गया था। यह तय करता है कि किसी परियोजना से पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को क्या असर होगा और परियोजना शुरू करने से पहले किन शर्तों का पालन करना होगा।
इस कानून के तहत बड़ी और राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं (जैसे कोयला खदानें, बड़े उद्योग, बड़े बांध) आदि को ए श्रेणी परियोजनाओं में रखा जाता है और इनकी मंजूरी केंद्र सरकार देती है। वहीं, अपेक्षाकृत छोटे आकार की परियोजनाओं को बी श्रेणी में रखा जाता है, जिनका मूल्यांकन सामान्य तौर पर राज्य स्तर पर होता है।

आईआइए कानून के तहत किसी भी परियोजना को स्क्रीनिंग यानी यह तय करना कि परियोजना को ईआईए की जरूरत है या नहीं, स्कोपिंग यानी किन-किन बिंदुओं पर पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाए और जनसुनवाई स्थानीय लोगों और हितधारकों की राय जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है।
जनसुनवाई सबसे अहम हिस्सा है, जिसमें प्रभावित क्षेत्र की जनता से राय ली जाती है और जनसुनवाई के मिनट्स (रिपोर्ट) को परियोजना प्रस्ताव में शामिल करना अनिवार्य होता है। हालांकि, राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं या रणनीतिक रूप से अहम परियोजनाओं को इन दायरे से बाहर रखा गया है।
अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यही छूट परमाणु, महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खनन परियोजनाओं को दे दिया है और कहा है कि ये परियोजनाएं “राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा जरूरतों तथा रणनीतिक विचारों” से जुड़ी हैं।
पर्यावरण मंत्रालय ने जारी अपने ताजा ओएम में बताया है कि यह छूट हाल ही में रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा किए गए अनुरोध के बाद दी गई है।
जारी ओएम में मंत्रालय ने कहा है कि उसे 4 अगस्त, 2025 को उन्हें रक्षा मंत्रालय से एक प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईईईएस) का इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। इनका उपयोग निगरानी और नेविगेशन सिस्टम जैसे रडार और सोनार, संचार और डिस्प्ले उपकरणों जैसे लेजर और एवियोनिक्स, हथियारबंद वाहनों में माउंटिंग सिस्टम, प्रिसीजन गाइडेड गोला-बारूद और मिसाइल गाइडेंस तकनीक में किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आरईईएस स्थायी चुंबकों के निर्माण के लिए जरूरी हैं, जो रक्षा उपकरणों की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन भारत में इन खनिजों का भंडार बेहद सीमित है और दुनिया के कुछ ही देशों में इसका उत्पादन होता है, जिससे आपूर्ति पर बड़ा जोखिम है। इस चुनौती को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने मांग की है कि महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों से जुड़ी खनन परियोजनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट मानते हुए इन्हें पर्यावरण मंजूरी के दौरान जनसुनवाई की प्रक्रिया से छूट दी जाए।
वहीं, परमाणु ऊर्जा विभाग ने भी 29 अगस्त 2025 को पर्यावरण मंत्रालय को भेजे गए पत्र में बताया कि बीच सैंड खनिज मोनाजाइट से प्राप्त थोरियम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए संभावित ईंधन है, जबकि पहले चरण के लिए यूरेनियम खनन अनिवार्य है। विभाग ने जोर दिया कि इसके लिए देश में नए यूरेनियम और बीच सैंड खनिज भंडारों का तेजी से दोहन जरूरी है। इसी कारण विभाग ने मांग की है कि खनिज एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग-बी में सूचीबद्ध परमाणु खनिजों की खनन परियोजनाओं को शीघ्र ऑपरेशनलाइज करने के लिए 14 सितंबर 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना के तहत जनसुनवाई से छूट दी जाए।
हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि “इन परियोजनाओं की समीक्षा केंद्रीय स्तर पर की जाएगी, चाहे खनन पट्टा क्षेत्र कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो।”
जारी ओएम में कहा गया है, इन खनन परियोजनाओं की ईआईए या ईएमपी रिपोर्ट में अन्य पहलुओं के साथ-साथ स्थानीय बस्तियों/जनसंख्या पर प्रभाव, सामाजिक ढांचा (जैसे चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं), कौशल विकास और रोजगार अवसर, लोक शिकायत निवारण प्रणाली आदि का विवरण शामिल होना जरूरी होगा। ताकि संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति प्रस्ताव की व्यापक समीक्षा कर सके और उपयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाई जा सके।
ओएम में कहा गया है, “इस योजना को लागू करने के लिए परियोजना प्रस्तावक पर्याप्त वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएंगे और उन्हें पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल किया जाएगा।”
यह लेख मूलरूप से डाउन टू अर्थ हिंदी पर प्रकाशित हुआ था।
पार्वती* एकडेढ़ साल के बच्चे की मां हैं। वह कहती हैं कि “मेरा घर किसी ऐसी भट्टी जैसा लगता है जिसे मैं बुझा नहीं सकती।” वह चेन्नई के औद्योगिक इलाके में रहती हैं। टिन की चादर वाली छत के नीचे उनके घर में आधी रात के बाद भी दिन भर की गर्मी बनी रहती है। आमतौर पर जिन घरों में हवा का प्रवाह कम हो, प्रदूषण अधिक हो या ठंडक न हो, वहां रहने वाली माताओं में अवसाद, तनाव और चिंता जैसी समस्याओं के बढ़ने की संभावना अधिक होती है। इसका सीधा असर उनके शिशुओं की देखभाल पर पड़ता है।
अत्यधिक गर्म माहौल में रहने से गर्भवती महिलाओं में जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है: जैसे बच्चे के मृत पैदा होने का खतरा लगभग 1.13 गुना अधिक, जन्मजात विकृतियां 1.48 गुना अधिक और हीटवेव के दौरान गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताएं 1.25 गुना तक बढ़ सकती हैं। वहीं मानसिक स्वास्थ्य पर भी गर्मी का असर साफ दिखता है: देश भर में किए गए कई अध्ययनों में पाया गया है कि तापमान बढ़ने के साथ बुजुर्गों में अवसाद और मानसिक तनाव के मामले बढ़े हैं। ताइवान में, तापमान में सिर्फ 1°C की वृद्धि से अवसाद के गंभीर मामलों में सात फीसदी तक बढ़त देखी गई है।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में समय से पहले जन्मे शिशुओं की मृत्यु से जुड़े 91 प्रतिशत मामले प्रदूषण से संबंधित होते हैं। वहीं उन परिवारों में, खासकर जो हवादार घरों में नहीं रहते हैं, अक्सर त्वचा संबंधी समस्याओं (हीटरैश) और श्वास संबंधी रोगों की शिकायत आम होती है।
ये रुझान राष्ट्रीय स्तर पर हुए उन अध्ययनों से मेल खाते हैं, जिनमें पाया गया है कि निरंतर वायु प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक कुप्रभाव छोड़ता है। भारत में हर पांच में से एक महिला प्रसव के बाद होने वाले अवसाद यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन (22%) से गुजरती है। तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में यह आंकड़ा बढ़कर हर चार में से एक (26%) महिला में पाया जाता है। इसके बावजूद, ज्यादातर महिलाओं को जरूरी देखभाल या कोई औपचारिक सहायता नहीं मिल पाती है। जिन माताओं के बच्चे विकलांग होते हैं, उनके लिए स्थिति और मुश्किल होती है। सेवाओं की कमी, सामाजिक रूढ़ियां और भावनात्मक अकेलापन जैसे कई पहलू देखभाल से होने वाली शारीरिक थकान को और बढ़ा देते हैं।
साल 2024-25 में, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में किए गए अपने एक शोध के तहत, मैंने तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में 391 माताओं के साथ एक सर्वे किया। इसका उद्देश्य यह समझना था कि जलवायु संकट उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। इसके अलावा, मैंने इनमें से छह माताओं के साथ लंबे और गहन साक्षात्कार भी किए। इनका उद्देश्य बढ़ती हीटवेव और वायु प्रदूषण के बीच बच्चों की देखरेख से जुड़ी उनकी जिम्मेदारियों, आर्थिक दबाव और मानसिक बोझ के अनुभवों को बेहतर तरीके से समझना था।
तमिलनाडु देश के सबसे तेजी से गर्म होते राज्यों में शामिल है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन दशकों में यहां का सालाना अधिकतम तापमान हर साल 0.02-0.04°C तक बढ़ा है। हालिया सालों में, कई जिलों में गर्मियों में तापमान 42°C के पार भी गया है। चेन्नई में, अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के कारण शहर का तापमान हरियाली वाले इलाकों की तुलना में +3-4°C अधिक रहता है। इससे मौजूदा तनाव बढ़ता है, भीतरी इलाकों में सूखा लंबे समय तक बना रहता है और तटीय इलाकों में उमस बढ़ जाती है।

लता* चेन्नई के बाहरी इलाके में एक ईंट भट्ठे के पास रहती हैं और एक साल के बच्चे की मां हैं। वे कहती हैं कि “यह हवा किसी धीमे जहर जैसी है। इसमें बच्चे के लिए सांस लेना तक भारी हो जाता है। जब वह सोता है तो मैं उसकी नाक ढक देती हूं। लेकिन मैं हवा को कब तक ढंक सकती हूं? उसे इस हवा में सांस लेने से कैसे रोकूं?”
प्रदूषण और बढ़ती गर्मी का असर केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, माताओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हुए शोध लगातार बताते हैं कि अत्यधिक गर्मी का प्रभाव माताओं के खराब मानसिक स्वास्थ्य के रूप में भी देखने को मिलता है, जिसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी शामिल है। हमारे अध्ययन में न्यूरोटिपिकल बच्चों की माताओं के साथ-साथ विकलांग बच्चों की माताओं को भी शामिल किया गया था। इनमें से 65 प्रतिशत माताओं में हल्के से मध्यम स्तर के अवसाद के लक्षण दिखाई दिए। वहीं, विकलांग बच्चों की माताओं में इसकी दर और गंभीरता दोनों अधिक थीं। सामाजिक रूढ़ियां, बढ़ी हुई देखभाल की जरूरतें और सीमित सामाजिक समर्थन उनके मानसिक बोझ को और बढ़ा देते हैं।
इन अधिकांश मामलों में पिता की भूमिका समान जिम्मेदारी संभालने से ज्यादा केवल आर्थिक सहारा देने तक ही सीमित रहती है। लेकिन आमतौर पर उनकी आय के बावजूद, परिवार लगातार आर्थिक दबाव का सामना करते हैं। जैसा कि एक मां ने बताया, “मेरे पति की फैक्ट्री वाली नौकरी से मुश्किल से ही हमारा गुजारा चल पाता है।”
जलवायु संकट और सीमित संसाधनों के चलते माताएं अक्सर घर में ही समाधान खोजने का प्रयास करती हैं। जब अनौपचारिक बस्तियों में बिजली जाती है तो वे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क बनाए रखती हैं। इसके माध्यम से वे सरकारी योजनाओं की जानकारी, पानी के टैंकर की उपलब्धता और ठंडक के उपाय जैसी जानकारियां भी आपस में साझा करती हैं। ग्रामीण मदुरै में महिलाएं ठंडक के लिए जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करने के पारंपरिक तरीकों को दोबारा अपना रही हैं। इसका एक उदाहरण सूती कपड़े को नीम और हल्दी के पानी में भिगोकर लगाना है, ताकि गर्मी से होने वाले बुखार जैसी परेशानियों को कम किया जा सके। इस तरह के उपाय किफायती और स्थानीय संस्कृति में स्वाभाविक रूप से रचे-बसे होने के साथ-साथ न्यूनतम संसाधनों के सहारे आसानी से बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकते हैं।।
तमिलनाडु के पास नीतिगत ढांचा मौजूद है, लेकिन घरेलू स्तर पर नवजात बच्चों की माताओं की देखभाल से संबंधित प्रयासों की कमी है। ऐसी परिस्थिति से जुड़े कुछ उपाय हैं:
तमिलनाडु तात्कालिक कदम के तौर पर माताओं की देखभाल को केंद्र में रखते हुए कूलिंग सब्सिडी दे सकता है। ठंडक बच्चों को सोने में मदद करती है, स्तनपान को आसान बनाती है और गर्मी से जुड़ी मानसिक तकलीफ को कम करती है।
तमिलनाडु की हीट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी (2024) पहले ही वंचित समुदायों के लोगों को रिफ्लेक्टिव छतों और ठंडी सतहों के निर्माण के लिए सहयोग देती है। इस रणनीति में नई माताओं की देखभाल के उद्देश्य को शामिल करना और उनके घरों तक पहुंचाने के लिए इसे बढ़ाना, स्वास्थ्य के लिहाज से तेजी से बेहतर परिणाम दे सकता है।
रिफ्लेक्टिव छतों वाली चादरें (जिन पर सफेद या हल्के रंग की कोटिंग होती है) जैसे उपाय घर के भीतर का तापमान 2–5°C तक कम कर सकते हैं। इनके प्रयोग से गर्मी के कारण बच्चों की नींद में आने वाली बाधा लगभग 30 प्रतिशत तक घट सकती है। इसके अलावा, माताएं मिट्टी के बने कूलर और मिट्टी के ही बर्तनों से बनाए गए ठंडक समाधानों (ज़ीर पॉट फ्रिज) का इस्तेमाल करती हैं जो ग्रामीण बाजारों में आसानी से उपलब्ध हैं। ये बिजली के बगैर, पानी और खाने-पीने की चीजों का तापमान कम रखते हैं और बिजली कटने पर स्टोर किए गए मां के दूध को सुरक्षित भी रखते हैं। लेकिन इन सरल उपायों को राज्य स्तर पर समर्थन देने वाली कोई व्यवस्था मौजूद नहीं हैं। कम संसाधन वाले क्षेत्रों में नई माताओं को इस तरह की चीजें उपलब्ध करवाना उनके लिए गर्मी से निपटने में मददगार हो सकता है।
आशा कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों और शहरी अनौपचारिक बस्तियों में माताओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं से संपर्क का पहला बिंदु होती हैं। लेकिन उनके प्रशिक्षण माॉड्यूल में जलवायु से जुड़े देखभाल जोखिम की जानकारी शामिल नहीं होती है।
आशा कार्यकर्ताओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन और गर्मी से जुड़े तनाव के लक्षण पहचानने का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
जलवायु से होने वाली चुनौतियां रोजमर्रा की हकीकत बनती जा रही हैं चूंकि आशा कार्यकर्ता पहले से कामकाज का भारी बोझ झेल रही हैं, इसलिए इसे उनके लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय, जैसे-जैसे जलवायु से होने वाली चुनौतियां रोजमर्रा की हकीकत बनती जा रही हैं, वैसे-वैसे उनके प्रशिक्षण में गर्मी से होने वाली बीमारियों की पहचान, सुरक्षित हाइड्रेशन के तरीके, घरों के भीतर हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास (जैसे गीले कपड़े से धूल को रोकना) और गर्मियों में आपातकालीन स्तनपान जैसी जानकारियां शामिल की जानी चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन और गर्मी से जुड़े तनाव के लक्षण पहचानने का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए एडिनबरा पोस्टनेटल डिप्रेशन स्केल (ईपीडीएस) जैसे छोटे और मान्य उपकरण को तमिल में उपलब्ध करवाया जा सकता हैं।
देश भर में, राज्य सरकारें गर्मियों में बढ़ते तापमान से निपटने के लिए अपने हीट एक्शन प्लान पर काम कर रही हैं। अहमदाबाद में इसकी शुरूआत हुई और अब इसे ओडिशा और तेलंगाना में भी अपनाया जा चुका है। इन योजनाओं में पूर्व चेतावनी सिस्टम, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और हाइड्रेशन व गर्मी से बचाव पर सार्वजनिक सुझाव दिया जाना शामिल है। तमिलनाडु का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पहले ही हीट अलर्ट जारी करता है। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाकर संदेशों को साधारण और लागू किए जा सकने योग्य निर्देशों में बदलकर उन घरों तक पहुंचाया जा सकता है, जो अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं।
चूंकि माताएं पहले से ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए जिला स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित व्हाट्सएप समूह मददगार हो सकते हैं। इन पर माताओं को समय पर आसानी से समझ आने वाले अपडेट दिए जाने चाहिए। जैसे, “सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक धूप से बचें”, “पानी के बर्तन छाया में रखें” या “छतों को गीले जूट के बोरे से ढकें।” कलंजियम समुगा वनोली जैसे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के जरिए हीटवेव से जुड़ी देखभाल के टिप्स, हाइड्रेशन के संदेश और माताओं के मानसिक स्वास्थ्य के स्व-निरीक्षण जैसी जानकारियों को स्थानीय बोली-भाषा में प्रसारित किया जा सकता है। यह चैनल पहले से ही, खासकर ग्रामीण और तटीय इलाकों में, आपदा तैयारी और जलवायु चुनौतियों से निपटने की क्षमता पर जोर देता है।
जैसे-जैसे तमिलनाडु में राष्ट्रीय औसत से अधिक गर्मी पड़ने लगी है और इसके शहरी व औद्योगिक क्षेत्र, गर्म और प्रदूषित होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे महिलाओं (खासकर कम आयवर्ग से आने वाली माताओं) पर देखभाल से जुड़ी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है।
*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदल दिए गए हैं।
यह अध्ययन हार्वर्ड सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मित्तल इंस्टीट्यूट के सहयोग से, हार्वर्ड टीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर किया गया है। इसमें किसी प्रकार का हित का संघर्ष नहीं है।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—
विकास सेक्टर में सक्रिय लघु स्तर के बहुत से गैर-लाभकारी संगठन अक्सर सीमित संसाधनों के साथ काम करते हैं। हाल के वर्षों में ऐसी संस्थाओं के लिए कई तकनीक-आधारित समाधान उभरे हैं, जो उनके काम को अधिक कुशल, प्रभावी और डेटा-केंद्रित बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। फिर भी इनकी संरचना, बुनियादी उद्देश्य और उन्हें अपनाने की प्रक्रिया में अनेक चुनौतियां हैं, जिन्हें गहराई से समझने और दूर करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने एक डिजिटल टूल के जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि:
इस लेख में हम लघु संस्थाओं के लिए तकनीक-आधारित समाधानों से जुड़ी जरूरतों, चुनौतियों, संभावित उपायों और उनसे मिली सीख पर गौर करेंगे, जो हमारे समन्वय और अवनी के व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित हैं।
बहुत सी लघु संस्थाओं का अधिकांश काम आज भी पारंपरिक विधियों पर आधारित हैं, जहां फील्ड वर्कर कागजों में डेटा दर्ज करते हैं, जिन्हें बाद में रिपोर्ट में बदलने में कई हफ्ते लग जाते हैं। इस प्रक्रिया में न केवल समय का नुकसान होता है, बल्कि मानवीय त्रुटियां भी अपरिहार्य हो जाती हैं। जैसे – समुदाय के किसी व्यक्ति का गलत फोन नंबर दर्ज होना या तिथियों में गड़बड़ी हो जाना, जो बाद में उनसे संपर्क स्थापित करने में बाधा बनते हैं। नतीजतन, संस्थाओं को अपने रोजमर्रा के कामों में रुकावट का सामना करना पड़ता है।
उदाहरण के लिए, हमारे साझेदार संगठनों में से एक संस्था प्रोजेक्ट पोटेंशियल बिहार के किशनगंज जिले में पीएमजेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के जमीनी कार्यान्वयन पर पूरी तरह कागजी दस्तावेजीकरण के तहत काम कर रही थी। इसके अंतर्गत लगभग 24 फील्ड कॉर्डिनेटरों द्वारा 12 ग्राम पंचायतों से प्राप्त 12,900 आवेदनकर्ताओं की एंट्री को तकरीबन 500-600 पन्नों में दर्ज किया जा रहा था। ऐसे में संस्था के लिए यह जानना आसान नहीं था कि किसका आयुष्मान कार्ड बन चुका है, कितने कार्ड अब भी प्रक्रिया में हैं और कितने लोग वास्तव में इसका उपयोग कर पा रहे हैं।
लेकिन जब डिजिटल दस्तावेजीकरण का इस्तेमाल किया गया, तो संस्था अपने फील्ड वर्करों के साथ यह आंकड़ा साझा करने में सक्षम हुई कि वे दैनिक रूप से कितने कार्ड बना रहे हैं और कितने कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। इससे उनके रोजमर्रा के काम तो आसान हुए ही, वे मापन-योग्य आंकड़ों के अनुसार अपनी प्लानिंग भी करने लगे। जैसे, अगर उनके पास छह महीने में 15,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य है, तो वे उससे कितने दूर हैं या उन्हें अपनी योजना में क्या बदलाव करने चाहिए। इसका सीधा असर संस्था की संचालन क्षमता पर दिखा, जो 30% तक बढ़ गयी। साथ ही वास्तविक समय में डेटा ट्रेकिंग की अवधि भी सात से घटकर एक दिन हो गयी।
देश के दूर-दराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं, जैसे बिजली और इंटरनेट की अनियमित उपलब्धता डिजिटल समाधानों को अपनाने में एक प्रमुख बाधा बनती है। ऐसे में अधिकांश डिजिटल टूल जो केवल ऑनलाइन मोड में काम करते हैं, इन क्षेत्रों के लिए व्यावहारिक नहीं रह जाते।
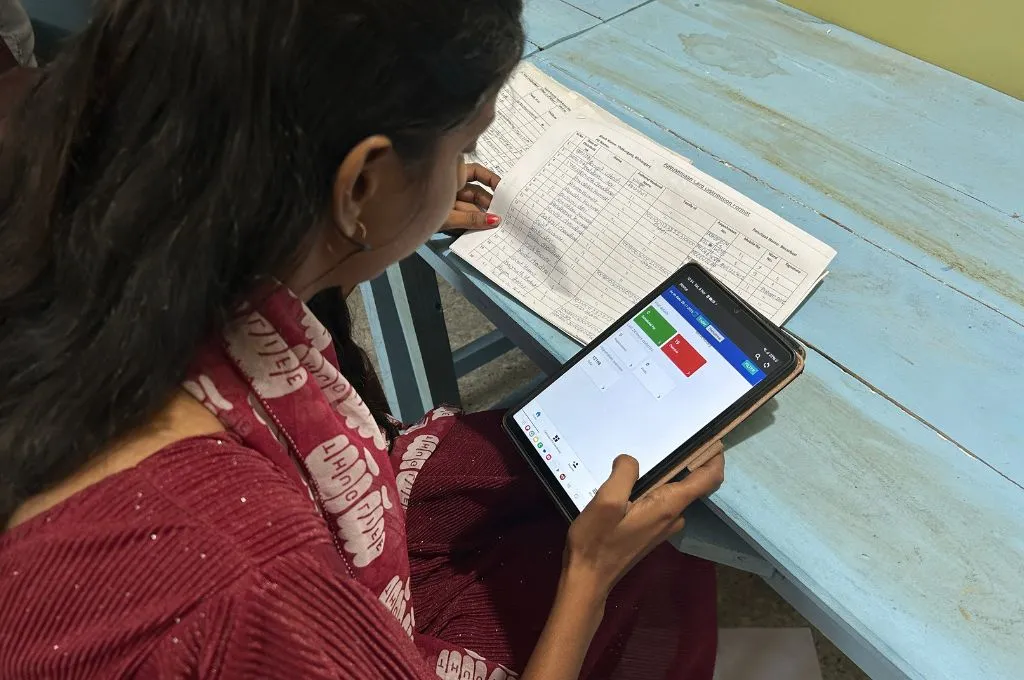
अपने शुरुआती दिनों में हमने महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में काम करने वाली एक संस्था का दौरा किया था। उन्हें डेटा ट्रैकिंग, फॉलो-अप और निर्णय लेने में सहयोग के लिए ऐसा समाधान चाहिए था, जो इंटरनेट पर निर्भर न हो। जैसे-जैसे हमने अन्य संस्थाओं से बात की, हमें समझ आया कि यह चुनौती लगभग हर उस संस्था के लिए आम है, जो ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रों, कस्बों या महानगरों में भी घर-घर जाकर काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में बिजली और इंटरनेट की उपलब्धता भले ही बेहतर हुई है, लेकिन यह अभी भी निरंतर रूप से भरोसेमंद नहीं है। ऐसे में ऑफलाइन काम करने वाले डिजिटल टूल जो डेटा संग्रह, विश्लेषण और निर्णय की पूरी प्रक्रिया में साथ न छोड़ें, कहीं अधिक व्यावहारिक और प्रभावी साबित होते हैं।
लघु संस्थाओं के लिए किसी भी डिजिटल टूल को अपनाने से पहले यह बेहद जरूरी है कि वे अपनी वास्तविक जरूरतों को गहराई से समझें। किसी भी टूल का चयन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि संस्था किस समस्या का समाधान चाहती है और उस समाधान के लिए कौन-सी डिजिटल सुविधा वास्तव में उपयोगी होगी। इससे संस्था यह पहचान सकती है कि उन्हें डिजिटल टूल में किन विशेषताओं की आवश्यकता है, जैसे:
स्पष्ट जरूरतों की पहचान ही किसी भी सफल तकनीकी हस्तक्षेप की पहली शर्त होती है। इसलिए संस्थाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी टूल को अपनाते समय उसकी भाषा, डिजाइन और उपयोगिता को अपने स्थानीय संदर्भ में परखें।
अमूमन संस्थाएं किसी सॉफ्टवेयर या एप्लिकेशन (एप) को मुहैया करवाने वाली एजेंसी, व्यक्ति या लाइसेंस से बंध जाती हैं। इसके अलावा, लघु स्तर की संस्थाओं के लिए अपने सीमित बजट के साथ एक सॉफ्टवेयर या एप में अलग से निवेश करना हमेशा संभव नहीं होता है।
ऐसे में संस्थाएं एक अच्छे ओपन-सोर्स टूल का उपयोग कर सकती हैं। ये टूल सीमित संसाधनों वाली संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, अनुकूलनीय और सशक्त बनाते हैं। साथ ही संस्थाएं अपनी परियोजनाओं और डेटा प्रबंधन की आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें अनुकूलित कर सकती हैं। इनके प्रयोग का एक उद्देश्य यह भी है कि संस्था किसी एक व्यक्ति या एजेंसी पर अति-निर्भर नहीं रहती है। इस पहलू को हम डिजिटल टूल के स्थाई समाधान बन जाने की तरह भी समझ सकते हैं, जिसमें ओपन-सोर्स एक अहम भूमिका निभा सकता है।
मालिकाना अधिकारों की शर्त न होने के कारण ओपन-सोर्स टूल में किसी तरह की भारी-भरकम लाइसेंसिंग कीमत भी शामिल नहीं होती है। संस्थाएं इसे चलाने के लिए किसी समझौते से बंधे रहने के लिए बाध्य नहीं होती हैं। जैसे, वे अपने डेटा के लिए सरलता से क्लाउड-होस्टिंग का विकल्प भी चुन सकती हैं। इसके अलावा, अगर कोई संस्था एक ओपन-सोर्स टूल का सफलतापूर्वक उपयोग करती है, तो अन्य संस्थाएं भी इस टूल को अपनाने के लिए प्रेरित होती हैं।
जब कोई संस्था किसी तकनीकी सहयोगी (वेंडर/प्रोवाइडर) के साथ काम करती है, तो उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह केवल उपभोक्ता भर न बनी रहे बल्कि उसके चयन की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाए। अक्सर संस्थाएं कोई आकर्षक या जटिल तकनीक अपना लेती हैं, जबकि उनकी जरूरत कहीं अधिक सरल होती है। उदाहरण के लिए, किसी संस्था के लिए एक साधारण व्हाट्सऐप चैटबॉट ही डेटा संग्रह या संवाद के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन वे किसी महंगे, अतिरिक्त फीचर्स वाले एप में निवेश कर देती हैं, जिसकी जरूरत उन्हें वास्तव में नहीं होती है।
ऐसे में संस्थाएं शुरुआती चरण में ही अपने तकनीकी साझेदार को यह सुझाव दे सकती हैं कि टूल को बहुत जटिल रूप में न विकसित किया जाए। इसके बजाय, पहले सीमित फीचर्स के साथ एक कार्यशील मॉडल तैयार किया जाए, जिसे फील्डवर्कर आसानी से अपना सकें। जब वे टूल के बुनियादी स्तर पर सहज रूप से काम करने लगें, उसके बाद वे धीरे-धीरे नए फीचर्स की ओर बढ़ सकते हैं।

निरंतर प्रतिक्रिया देने से टूल का उपयोग अधिक व्यावहारिक, प्रासंगिक और दीर्घकालिक बनता है। उदाहरण के लिए, अवनी बनाते समय हमारी टीम ने बहुत सारा समय जमीनी संस्थाओं और फील्डवर्करों के साथ बिताया। उनसे मिले इनपुट के आधार पर हमने तय किया कि हमें अपना यूजर-इंटरफेस एकदम सरल रखना है, जिसमें डेटा एंट्री के लिए कम से कम टाइपिंग की जरूरत हो। इसके अलावा हमने सिंगल और मल्टी फीचर, फॉन्ट, बटन के चयन आदि जैसे पहलुओं को बनाते समय भी उनके इनपुट पर पूरा ध्यान दिया।
जब लघु संस्थाएं डिजिटल टूल या सॉफ्टवेयर अपनाने की सोचती हैं, तो उनके लिए यह समझना उतना ही आवश्यक है कि वे किस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं, जितना यह जानना कि वे कौन-सा टूल वे उपयोग कर रही हैं। जिस तरह ओपन-सोर्स संस्थाओं को अपने संसाधनों पर नियंत्रण और स्वायत्तता देता है, उसी तरह एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव उन्हें लचीलापन, किफायत और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है।
अक्सर संस्थाओं के कार्यक्रम अलग-अलग विषयों पर केंद्रित होते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी हर परियोजना के लिए यह लगता है कि उन्हें एक नया डिजिटल टूल चाहिए। लेकिन यदि वे अपनी जरूरतों का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह साफ होगा कि इन सभी कार्यों की कुछ जरूरतें साझा हैं (जैसे ऑफलाइन मोड, स्थानीय भाषा, सरल इंटरफेस आदि), और कुछ जरूरतें कार्यक्रम-विशिष्ट हैं (जैसे फॉर्म, रिपोर्ट, इंडिकेटर आदि)।
अवनी के माध्यम से हमने जाना कि यदि संस्थाएं यह समझ लें कि उनके काम का कौन-सा हिस्सा साझा है और कौन-सा विशिष्ट, तो वे बार-बार नया एप्लिकेशन बनवाने की बजाय एक साझा, कॉन्फिगरेबल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे न केवल लागत घटती है, बल्कि रखरखाव, प्रशिक्षण और अपग्रेड का काम भी सरल हो जाता है। इसलिए डिजिटल तकनीक अपनाते समय संस्थाओं को यह स्पष्ट दृष्टि रखनी चाहिए कि वे एक ऐसे लचीले और साझा प्लेटफॉर्म में निवेश कर रही हैं, जो उनके बदलते कार्यक्रमों के साथ विकसित हो सके और लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे।
अक्सर संस्थाओं में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत कॉर्डिनेटर या मैनेजर निर्देश जारी करते हैं और बड़े निर्णय लेते हैं। वहीं जमीनी कार्यकर्ता केवल डेटा इकट्ठा करने की भूमिका तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन अगर हम जमीनी कार्यकर्ता को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करें, तो प्रोग्राम के समग्र ढांचे को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी सरकारी योजना के कार्यान्वयन में आमतौर पर फील्ड वर्कर केवल लोगों का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर उनके पास एक ऐसा सरल डिजिटल टूल हो जिसमें वे स्पष्ट रूप से अपने काम का लेखा-जोखा देख पायें, तो वे खुद अपने काम को ट्रैक करते हुए अपनी जवाबदेही तय कर सकते हैं।
संस्थाओं को हमेशा अपने फील्ड वर्करों से यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वे एक टूल के जरिये क्या करना चाहते हैं और उनका काम किस तरह सुगम बन सकता है। जब संस्थाएं अपने फील्ड कार्यकर्ताओं की जरूरतें जानने का प्रयास करती हैं, तो उनके लिए डिजिटल टूल अपनाने की प्रक्रिया अपने आप सहज हो जाती है।

टूल का जमीनी प्रयोग जितना विविध होगा, उसे बेहतर बनाने के लिए उतनी ही अनुभवात्मक प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। इस कड़ी में हमने शुरुआत में अपने टूल के अलग-अलग उपयोगकर्ताओं (यूजर) के साथ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। हमने बहुत से फील्ड वर्करों को लॉग-इन से लेकर डेटा एंट्री तक हर छोटे-बड़े पहलू को बारीकी से समझाया। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक प्रशिक्षण सत्रों के दौरान हमने उपयोगकर्ताओं को प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने से लेकर डेटा दर्ज करने तक हर चरण विस्तार से सिखाया। ऐप के यूजर इंटरफेस में किए गए छोटे-छोटे बदलाव, जैसे अंग्रेजी और हिंदी के बीच भाषा बदलने का विकल्प, उपयोगकर्ताओं के अनुभव को कहीं अधिक सहज और सुविधाजनक बनाने में बेहद प्रभावी साबित हुए।
निर्णय लेने के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि टूल ऐसा हो जो हर चरण में सभी प्रतिभागियों से संवाद बरकरार रखे। जैसे-जैसे वे फॉर्म में आगे बढ़ते जाते हैं, एप उन्हें लगातार फीडबैक देने का काम कर सकती है। यह दोतरफा संवाद के लिए भी सहायक होता है। साथ ही, इससे एक फील्ड वर्कर को यह भी समझ में आता है कि वे जिस कार्यक्रम के तहत सर्वे या डेटा संग्रहण कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है और वह कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है। यह संस्थाओं के भीतर पदानुक्रम (हायरार्की) की तय अवधारणाओं को भी संबोधित करता है। जब आप एक फील्ड वर्कर के हाथ में एक ऐसा टूल देते हैं, जिसमें उन्हें भी कॉर्डिनेटर और मैनेजर की तरह समान डैशबोर्ड नजर आता है, तो उनके अंदर स्वामित्व की भावना को बढ़ावा मिलता है।
तकनीक और समाज का रिश्ता परस्पर है। जिन लघु संस्थाओं के लिए डिजिटल समाधान बनाए जा रहे हैं, वही इन समाधानों के शिल्पकार भी हैं। एक लघु संस्था में नेतृत्व पंक्ति के साथ-साथ फील्ड वर्कर के अनुभव, उनकी सीमाएं, सहज भाषा जैसे सभी पहलू प्रभावी तकनीकी समाधान की बुनियाद हैं। अवनी जैसे ओपन-सोर्स टूल इस विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास हैं कि हमें संस्थाओं के काम को जटिल नहीं, सरल बनाना है और उनकी निर्णय लेने के तंत्र को केंद्रीकृत से साझी प्रक्रिया में बदलना है।
—
साल 2019 में जब हमने लेडबाय की शुरुआत की थी, तब हमारे पास कोई तय मार्गदर्शिका नहीं थी। हम में से कोई शिक्षण में प्रशिक्षित नहीं था और न ही हम शिक्षण विधियों के विशेषज्ञ थे। हमारे पास बस एक गहरी जिज्ञासा थी, आपनी समझ थी और यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं को ऐसे परिवेश मिलने चाहिए, जहां उनकी मुश्किलों से इतर उनकी महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान दिया जा सके।
लेडबाय भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए नेतृत्व, करियर और उद्यमिता प्रोग्राम संचालित करता है। ये ऐसे कार्यक्रम हैं, जो वर्षों तक उनकी जरूरतें सुनते और समझते हुए, उनके साथ मिलकर विकसित किए गए हैं।
योजना से नहीं, सुनने से शुरुआत करें। डिजाइन करने से पहले प्रश्न पूछें। एक बार नहीं, लगातार। और सुनने की प्रक्रिया को कभी रुकने न दें। सुनने से प्रासंगिकता बनती है, और प्रासंगिकता से विश्वास।
काम के पहले साल में इस बात का मतलब था लंबी-लंबी टेलीफोन बातचीत, अनगिनत व्हाट्सएप संदेश, ईमेल संवाद और विस्तृत फीडबैक फॉर्म। समय बीतने के साथ यही प्रक्रिया एक संगठित, मुक्त–स्रोत स्वयंसेवी कार्यक्रम में बदल गयी, जिसमें कोई भी व्यक्ति देशभर में कहीं भी मुस्लिम महिलाओं के साथ पांच संरचित साक्षात्कार करने के लिए साइन अप कर सकता था। आज यही स्वयंसेवी-आधारित फीडबैक प्रणाली हमारे सुनने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के प्रमुख तरीकों में से एक है। यही हमें बताती है कि किस पहलू को बनाए रखना है, किसे संशोधित करना है, और किसे पूरी तरह छोड़ देना है।
लेकिन सुनने का अर्थ केवल बाहरी समुदाय तक सीमित नहीं है। लेडबाय में हम हर कार्यक्रम यह मानकर विकसित करते हैं कि प्रतिभागी हमारे साथ मिलकर उसका सह-निर्माण करेंगे। न केवल अपनी सीख के लिए, बल्कि उन प्रतिभागियों के लिए भी जो आने वाले वर्षों में इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। हमारे कोहॉर्ट में सिर्फ शिक्षार्थी नहीं, संरक्षक भी हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सफलता से ज्यादा असफलता पर विचार करें, ताकि आने वाले कल को मजबूत किया जा सके।

अक्सर हाशिए पर धकेले गए समुदायों के लिए बनाए गए कार्यक्रम सत्ता के उन्ही ढांचों को दोहराते हैं, जिन्हें वे तोड़ना चाहते हैं। इस कड़ी में वे आकर्षक रिज्यूमे, ‘सही’ डिग्री, ‘सही’ जवाब या संभ्रांत भाषा तलाशते नजर हैं।
हमने सीखा है कि कार्यक्रमों को केवल प्रमाण-पत्रों के आधार पर नहीं, बल्कि भरोसे को केंद्र में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए। समय के साथ हमें एहसास हुआ कि किसी व्यक्ति के भाषा-ज्ञान या प्रेजेंटेशन कौशल की तुलना में उसकी लगन और दृढ़ता को पहचानना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने अब तक हजारों आवेदकों का साक्षात्कार किया है। इस प्रक्रिया में हमने अपने सवालों को इस तरह विकसित किया है कि हम समझ सकें उनका नजरिया क्या है, वे क्या करना चाहते हैं और आगे बढ़ने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कितनी गहरी है।
कई प्रतिभाशाली लोग कौशल की कमी से नहीं, बल्कि आत्म-संदेह, सामाजिक रूढ़ियों या अकेलेपन के कारण पीछे रह जाते हैं। इसी वजह से चयन प्रक्रिया में बाहरी चमक-दमक नहीं, बल्कि इच्छा-शक्ति और उद्देश्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें दृढ़ता और स्पष्ट मंशा की तलाश करनी चाहिए। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब यह सही तरह किया जाता है, तो उसका असर साफ दिखता है। उदाहरण के लिए, बहुत से ऐसे प्रतिभागी जो शुरुआत में हिचकते हैं, आगे चलकर हमारे सबसे मजबूत साथी बनकर उभरते हैं।
हमारे कई उत्कृष्ट एल्यूमनाई ऐसे हैं, जिनका आत्मविश्वास पहले भले कमजोर था, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की उनकी इच्छा बेहद प्रबल थी। वे भले ही मुखर सार्वजनिक वक्ता न हों, पर अपने परिवारों में आवाज उठाने में पीछे नहीं रहते थे। उदाहरण के तौर पर, भोपाल की 24 वर्षीय आफरीन फेलोशिप के शुरुआती दो सत्रों में लगभग चुप रही। लेकिन अंत तक वह ग्रुप प्रेजेंटेशन लीड करने के साथ-साथ सामुदायिक कार्यक्रमों की मेजबानी भी कर रही थी। आज वह नए प्रतिभागियों के मेंटर की भूमिका निभाती हैं। सना, जिन्होंने लेडबाय से जुड़ने से पहले कभी रिज्यूमे तक नहीं लिखा था, एक वैश्विक टेक कंपनी में नौकरी पाने में सफल हुई और अब स्वयं एक फैसिलिटेटर के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
हमारा उद्देश्य इन प्रतिभागियों के जीवन को ‘साकार’ करना नहीं था। हमारा काम था उस बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, जिस पर वे मजबूती से चल सकें। उदाहरण के लिए, हर सत्र की शुरुआत में होने वाली 20-मिनट की पल्स चेक। यानी खुले संवाद-स्थल, जहां प्रतिभागी ईमानदारी से साझा कर सकते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या उन्हें परेशान कर रहा है। विश्वास की नींव पड़ने में अमूमन लंबा समय लगता है। लेकिन जब वह भरोसा स्थापित हो जाए, तो यही उनके अनुभव का सबसे खास हिस्सा बन जाता है। तकरीबन हर सर्वे में उन्होंने हमें यह बात बताई है।
सबसे अहम नतीजे अक्सर सामग्री से नहीं, बल्कि साथियों के समूह, एल्यूमनी नेटवर्क और अपनत्व की भावना से उपजते हैं।
हमारे पास लगातार आने वाला एक महत्त्वपूर्ण फीडबैक यह है कि लेडबाय का समुदाय ही इसकी धड़कन है। हम इसे ‘ट्राइब फॉर लाइफ’ कहते हैं, और यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। हमारे पुराने साथी अक्सर मेंटर, सलाहकार, वक्ता और फैसिलिटेटर के रूप में लौटकर आते हैं। वे सत्र आयोजित करते हैं, एक-दूसरे के लिए फंडरेज करते हैं, नौकरी के अवसर साझा करते हैं, और एक-दूसरे के लिए रिकमेंडेशन लिखते हैं। कुल मिलाकर, वे हमेशा एक-दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं।
उनका यह अपनापन संयोग नहीं, बल्कि सोच-समझकर की जाने वाली एक कोशिश है। हमने सीखा है कि समावेशन का असली अर्थ कार्यक्रमों का विस्तार नहीं, बल्कि रिश्तों को गहराई देना है। यही कारण है कि हम अपने हर प्रोग्राम में छोटे, स्थिर समूह (पॉड्स) बनाते हैं, जो एक-दूसरे की जवाबदेही तय करने के साथ-साथ एक-दूसरे को समर्थन भी देते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि हर ज़ूम सत्र में कोई न कोई परिचित चेहरा मौजूद हो। और इसी वजह से हम निजी कहानी और व्यक्तिगत अनुभवों को नेतृत्व कौशल का अभिन्न अंग मानते हैं। जब हम अपनी कहानी सुनाते हैं, तो हम खुद को अपनाने की दिशा में पहला कदम भी आगे बढ़ाते हैं।
अक्सर हाशिए पर धकेले गए समुदायों के लिए बनाए गए कार्यक्रम सत्ता के उन्ही ढांचों को दोहराते हैं, जिन्हें वे तोड़ना चाहते हैं।
बीते कुछ वर्षों में हमें भारतीय मुस्लिम महिलाओं की आंतरिक विविधता को भी ध्यान से समझना पड़ा है। तमिलनाडु की एक महिला की चुनौतियां उत्तर प्रदेश की एक महिला की चुनौतियों से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। सिर्फ भाषा में नहीं, बल्कि पूर्वाग्रहों, नेटवर्क तक पहुंच और पारिवारिक ढांचों तक में भी। भविष्य के लिए डिजाइन करने का अर्थ है इन विविधताओं को पहचानना और उन्हें एक जैसा मानकर नजरअंदाज न करना।
हमने यह भी देखा है कि सुगमता (एक्सेस) आकांक्षा को कैसे आकार देती है। कुछ महिलाओं के पास अपने लक्ष्यों के बारे में पहले से स्पष्टता होती है। वहीं उनमें से कुछ यह भाषा खोज रही होती हैं कि वे क्या चाहती हैं और क्यों। लेकिन जैसे ही वे एक सहयोगी, खुद से मेल खाते समूह से मिलती हैं, तो उनमें तेजी से बदलाव आता है। जैसे एक प्रतिभागी ने हमे बताया, “जब तक मैं यहां नहीं आई थी, तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे (जीवन में) और अधिक चाहने की भी अनुमति है।”
कार्यक्रमों के लिए परफेक्ट होना नहीं, बल्कि उत्तरदायी होना जरूरी है। फीडबैक लूप, पल्स चेक, और वास्तविक समय में किए गए सुधार किसी भी आकर्षक डेक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। असली प्रभाव तब दिखता है जब प्रतिभागी स्वयं आगे बढ़कर मेंटर, फैसिलिटेटर या एडवोकेट बन पाते हैं।
हम अपने 1200+ पूर्व छात्रों के साथ हर वर्ष पल्स चेक करते हैं, ताकि समझ सकें कि उनकी जरूरतें क्या हैं। हम उन्हें ओरिएंटेशन और ग्रेजुएशन सत्रों में आमंत्रित करते हैं और पैनलिस्ट या फैसिलिटेटर के रूप में वापस जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम उनसे यह भी उम्मीद करते हैं कि वे अपने साथियों का मार्गदर्शन करें, अपने अनुभव साझा करें और उनकी आवाजों को आगे ले जाने के लिए एक मंच तैयार करें।
हम जानते हैं कि सभी लोग हर समय सक्रिय रूप से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब उनमें से किसी एक को भी मदद की जरूरत होती है (जैसे रिज्यूमे पर सुझाव, कार्यस्थल पर कोई कठिन बातचीत या बस धैर्यपूर्वक किसी की बात सुन लेना), तो हम हमेशा मौजूद होते हैं। और उससे भी बढ़कर, हमारे प्रतिभागी एक-दूसरे के लिए मौजूद होते हैं।
यह एक तरह से समावेशन का अभ्यास है। न कोई औपचारिक चेकलिस्ट, न सप्ताह भर चलने वाला अभियान। सिर्फ रोजाना की वह प्रतिबद्धता, जिसमें उन आवाजों को केंद्र में रखा जाता है जो अक्सर हाशिए पर रह जाती हैं।
निश्चित तौर पर हमसे गलतियां भी हुई हैं। हम अब भी सीख रहे हैं कि बड़े स्तर पर एलुमनाई एंगेजमेंट को कैसे प्रबंधित किया जा सकता है। हमारे पास कोई परफेक्ट मॉडल नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। लेकिन हमारे पास एक दृढ़ संकल्प है। हमारे पास प्रतिभागियों को सुनने का, यथास्थिति बदलने का और लगातार जमीन पर बने रहने का इरादा है। जिन महिलाओं को जीवन भर सामाजिक प्रणालियों से बाहर रखा गया हो, उनके लिए निरंतरता मायने रखती है। इसलिए उनके पास बार-बार लौटकर आना, चाहे हमारे पास सभी जवाब न हों, एक ऐसे भरोसे की नींव डालता है जिससे बदलाव उत्पन्न हो सकता है।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—





हमने लगभग 5-6 साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। तभी हमारे काम में कक्षाओं और समुदायों में काम करते हुए, बच्चों को सुनते हुए, शिक्षकों के साथ मिलकर सीखते हुए, प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ समस्याओं के हल ढूंढते हुए, और राज्य व्यवस्था के जरिए बड़े बदलाव (या रुकावटें) समझने की कोशिश करते हुए प्रयास करना शामिल हुआ।
साल 2022 में हम सिंपल एजुकेशन फाउंडेशन (एसईएफ) की शिक्षक व्यावसायिक विकास टीम का हिस्सा बने और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली (एससीईआरटी) के साथ काम करना शुरू किया। हमने इस विश्वास के साथ काम किया कि असली बदलाव भीतर से ही आता है। इस दौरान हमने यह समझा कि शिक्षकों और बच्चों को उनकी जरूरतों और अनुभवों के मुताबिक बनाए गए समाधानों की आवश्यकता होती है। यही वह समय था जब हमारे रास्ते थोड़े अलग हुए। अब हममें से एक शिक्षक प्रशिक्षण के बड़े अनुभवों को डिजाइन करता है ताकि राज्य स्तर पर प्रशिक्षण ज्यादा अर्थपूर्ण और उपयोगी बन सकें। दूसरा लाखों शिक्षकों और छात्रों से मिले डेटा को समझने, उनकी प्रगति पर नजर रखने और जमीनी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए सिस्टम बनाता है।
एक साथ मिलकर, हम इस प्रश्न से जूझते रहे हैं कि स्थानीय संदर्भ को खोए बगैर किसी समाधान को बड़े पैमाने पर प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है?
सरकारी व्यवस्थाओं के साथ काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए मानकीकरण और संदर्भीकरण के बीच संतुलन बनाना, हमेशा एक बड़ा सवाल बना रहता है। मानकीकरण से काम का पैमाना, गुणवत्ता और पहुंच बढ़ती है – लेकिन इसका खतरा है कि इसमें अलग-अलग जगहों की विशिष्ट जरूरतें अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। वहीं, संदर्भीकरण काम को जमीनी स्तर पर उपयोगी और असरदार बनाता है – लेकिन इससे एकरूपता और स्थिरता कम हो सकती है।
राज्य सरकारों के साथ हमारे काम में यह तनाव सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक है – यह हमारे रोज के निर्णयों में दिखाई देता है। 2021 तक हम 7 से 8 स्कूलों में प्राचार्यों, शिक्षकों और माता-पिता के साथ काम कर रहे थे। इसके बाद जब हमारा काम बढ़कर 1000 स्कूलों तक पहुंचा तो हमें यह तय करना था कि हमारे कार्यक्रम का फोकस शिक्षक, प्राचार्य या माता-पिता यानी किस हितधारक पर केंद्रित होगा? राज्य के लिए शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाते समय भी हमें यह सोचना पड़ा कि क्या सभी शिक्षकों को समान प्रशिक्षण दिया जाए या विषय, ग्रेड और क्षेत्र के अनुसार इसे प्रासंगिक बनाया जाए। इसी तरह, जब हम किसी शिक्षण रणनीति को एसईएफ के स्कूलों में अच्छा काम करते देखते हैं, तो सवाल उठता है – क्या इसे सभी स्कूलों में अपनाया जाए, या हर जगह के हिसाब से बदला जाए? क्या एक ही तरह का कक्षा अवलोकन उपकरण सभी कक्षाओं में इस्तेमाल हो, या ग्रेड, विषय और स्थान के अनुसार बदले?
समय, संसाधन और पहुंच की सीमाएं हमें समझौते करने पर मजबूर करती हैं – बहुत ज्यादा स्थानीय मॉडल सीमित रह जाते हैं, और बहुत व्यापक मॉडल अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। इसलिए चुनौती यह नहीं है कि किसी एक को चुना जाए, बल्कि यह है कि दोनों को कैसे संतुलित रखा जाए। यही संतुलन हमारी रोज की सोच और काम को दिशा देता है।
बड़े पैमाने पर शिक्षकों के लिए असरदार प्रशिक्षण बनाना जरूरी भी है और मुश्किल भी। शिक्षा का परिदृश्य और बच्चों की जरूरतें पहले से कहीं तेजी से बदल रही हैं। शिक्षकों को अपने तरीकों को उपयोगी तरह से बदलने के लिए निरंतर, उच्च-गुणवत्ता वाले सीखने के अवसरों की आवश्यकता है। लेकिन राज्यभर के लाखों शिक्षकों तक प्रासंगिक और रुचिकर प्रशिक्षण पहुंचाना आसान नहीं है।
इन संदर्भों में हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी – बिखराव। हमने पाया कि दर्जनों हितधारक – सरकारी विभाग, एससीईआरटी संकाय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या डाइट (डीआईईटी) प्रोफेसर, और एनजीओ – सभी एक ही समूह के शिक्षकों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण तैयार कर रहे थे। हर कोई कुछ अच्छा लाता था, पर दिशा और दृष्टिकोण अलग थे। हालांकि कुछ में तो सामग्री उपयोगी और गहन थी लेकिन कुछ में शिक्षकों की आवाज ही गायब थी। नतीजतन सभी कार्यक्रम एक-दूसरे से अलग लगते थे और उनमें एक साझा दृष्टि का अभाव था।

इसे हल करने के लिए हमने शिक्षक योग्यता ढांचा (टीसीएफ) बनाया – एक साझा ढांचा जो बताता है कि अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक को कौन-से ज्ञान, कौशल और सोच की जरूरत है। यह ढांचा नौ महीने में विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ मिलकर, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय शोध के आधार पर और हजारों शिक्षकों की राय के साथ बना।
इसके साथ हमने राज्य के साथ एक मानकीकृत प्रशिक्षण प्रक्रिया भी बनाई – जिसमें हर प्रशिक्षण एक जरूरत विश्लेषण से शुरू होता है और शिक्षकों व डाइट प्रोफेसरों के साथ मिलकर बनाया जाता है। मतलब हमने ‘कैसे बनाना है’ को तय किया, ‘क्या बनाना है’ को नहीं।
जब दिल्ली में प्रशिक्षण विकेंद्रीकृत हुआ तो हर जिले ने जरूरत पहचानने, टीसीएफ से जोड़ने, सह-डिजाइन करने और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने की इसी प्रक्रिया को अपनाया। नतीजा – हर जिले ने अपनी जरूरत के अनुसार मॉड्यूल बनाए, पर साझा शैक्षणिक मानकों के साथ। कहीं शिक्षकों के तनाव प्रबंधन पर ध्यान था, कहीं तकनीक के उपयोग पर।
इस पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी। यह प्रक्रिया एक ऐसी नींव बन गई जिससे स्थानीयता और मजबूत हुई। सार्वजनिक प्रणालियों में मानकीकरण का मतलब सबको एक जैसा बनाना नहीं है – यह एक साझा शुरुआत बनाना है। इससे सब एक ही भाषा बोलते हैं, समान परिणाम मापते हैं और जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। हमारे लिए टीसीएफ और प्रशिक्षण की मानक प्रक्रिया एक कम्पास की तरह हैं – जो हमें एक दिशा में रखता है, चाहे इलाका कोई भी हो।
सार्वजनिक प्रणालियों में यह आम है कि एक राज्य में सफल चीज, दूसरे में काम न करे – खासकर तकनीक। हर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, डेटा प्रणाली और प्रशिक्षण तंत्र अलग होता है। अगर कोई सिस्टम बिल्कुल स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बना है तो वह दूसरे राज्य में बेकार हो सकता है।
हमने एक प्रशिक्षण डेटा प्रणाली में अपने पहले प्रयास के साथ इसका अनुभव किया। जब शिक्षक योग्यता ढांचे ने दिल्ली के प्रशिक्षण तंत्र को रूप दिया तो हमें 13 कार्यक्रमों में 70,000 से ज्यादा शिक्षकों के प्रशिक्षण और नतीजों को ट्रैक करने के लिए सिस्टम चाहिए था। इसके लिए हमारा समाधान कम्पास एमआईएस बना। कम्पास एमआईएस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन (एम एंड ई) को सक्षम बनाता है।
इसने दिल्ली में अच्छा काम किया। हर शिक्षक, मेंटर और प्राचार्य का एक मास्टर डेटाबेस बनाया गया, जिसमें उनका क्षेत्र, जिला और कार्यक्रम जुड़ा था। इससे डेटा अपने आप भर जाता और सब कुछ सुचारू चलता।
लेकिन जब इसे दूसरे राज्यों में ले गए – तो समस्याएं शुरू हुईं।
इस तरह, जो प्रणाली दिल्ली में सफल और कारगर थी, वह अन्य राज्यों में नहीं चल पाई। हमने सीखा कि हमें सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली बनानी होगी जो हर जगह कारगर हो। अब हम इस सवाल – ‘हम एक राज्य के हर विवरण को कैसे पकड़ते हैं?’ के बजाय यह सोचने लगे – ‘इस प्रणाली के किन हिस्सों को सबके लिए उपयुक्त रहना चाहिए, और किन हिस्सों को स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बदले जाने के लिए खुला रहना चाहिए?’
अगर कोई सिस्टम बिल्कुल स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बना है तो वह दूसरे राज्य में बेकार हो सकता है।
इसका जवाब इंटरवेंशन डिजाइन पर वापस जाने में निहित है। हमने कम्पास को उसके मूल में हस्तक्षेप के डिजाइन के साथ फिर से बनाया। यह तय किया कि प्रशिक्षण प्रणाली के उद्देश्य को परिभाषित करने वाले तत्व – डेटा कैसे एकत्र किया गया था, गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की गई थी, परिणामों पर कैसे नजर रखी गई थी – हर जगह स्थिर रहे। इस मूल के आसपास, हमने लचीले मॉड्यूल बनाए जो राज्यों को अपनी वास्तविकताओं के अनुकूल बना सकते हैं:
इससे हर राज्य को स्थिरता और आजादी दोनों मिली। कोर समान रहा, पर तरीका स्थानीय बना। पंजाब ब्लॉक स्तर तक सुविधा प्रदाता जोड़ सका, जबकि अन्य राज्य धीरे-धीरे डेटा जोड़ रहे हैं।
सबक – बहुत ज्यादा स्थानीयकरण आपको सीमित कर देता है। असली प्रासंगिकता का मतलब है – कोर डिजाइन स्थिर रखना, बाकी में लचीलापन देना।
जैसा कि आलेख की शुरूआत में जिक्र किया गया है कि हमने मानक और स्थानीय संदर्भों में आसानी से फिट होने वाले समाधानों को लेकर प्रयास किए हैं। अपनी इस यात्रा में हमने समझा है कि मानकीकरण और प्रासंगिकता के संतुलन तक एक बार में नहीं पहुंचा जा सकता है – यह निरंतर प्रक्रिया है। सालों तक प्रयास, गलतियां और दोबारा प्रयास करने के कई चक्रों से गुजरकर हमने तीन बातें सीखीं जो इस संतुलन की दिशा में ले जाती हैं:
ये विचार सिर्फ दिल्ली या पंजाब के लिए नहीं हैं – हर संगठन को यह सोचने की जरूरत है कि बिना प्रासंगिकता खोए कैसे बढ़ा जाए, और निरंतरता और संदर्भ दोनों के लिए कैसे डिजाइन किया जाए। इस संदर्भ में इन बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना चाहिये:
इन चरणों वाली व्यवस्था को हम रणनीति कह सकते हैं। रणनीति किसी तय योजना का नाम नहीं, बल्कि सहानुभूति और साक्ष्य के साथ अनुकूलन की क्षमता है। डेटा और शिक्षकों की वास्तविक जरूरतों के बीच संतुलन ही असली रणनीति है। इसी तरह, परिवर्तन कोई एक बार की घटना नहीं है – यह लगातार सीखने की प्रक्रिया है। जब हम केवल अपनी धारणाओं पर चलते हैं, तो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनकी हकीकत छूट जाती है। इसलिए हम सुनते रहते हैं, सुधारते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं।
—
देश के 25 लोग हमें बता रहे हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, उन्हें क्या ध्यान आता है जब वे इन दो शब्दों को एक साथ सुनते हैं: नारीवादी शिक्षा।
द थर्ड आई में हम इन सवालों से इस विचार पर आपका ध्यान लाना चाहते हैं कि ज्ञान और सीखना सिर्फ एक विशेषाधिकार नहीं है। ये केवल वो जानीमानी प्रक्रिया नहीं है जिसमें ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होता है, जो जानते हैं उनसे, उनकी ओर जो नहीं जानते हैं। हमारा प्रस्ताव है, कि ज्ञान हमारे इतिहास में, हमारी यादों में, हमारे शरीर में वास करता है। अपने जेंडर, कामनाओं/ इच्छाओं और अपनी दुनिया का हम जो मतलब या फिर मूल निकालते हैं या देते हैं उसमें ये बस्ता है। इस तरह, ये फिल्म जो भी हमें बताया और समझाया गया और जो भी निष्कर्ष या समझ हमने अपनी तरफ से बनाई, उन दोनों को साथ बुनकर एक नए तरह के ज्ञान की रचना की तरफ इशारा करती है।
आपके और हमारे बीच ज्ञान की एक नई कल्पना की बातचीत शुरू करने के लिए, हमारी तरफ से ये एक शुरुआत है। इसके निर्माण में आप भी हमारे साथ आएं।
यह लेख मूलरूप से द थर्ड आई पर प्रकाशित हुआ था।
जल, जंगल, जमीन, भाषा, और पारंपरिक रीति-रिवाज यानी सामुदायिक विरासत और संसाधन या ‘कॉमन्स’, भारत में करोड़ों लोगों के जीवन, आजीविका और संस्कृति से जुड़े हैं। ये केवल उपयोग की वस्तुएं नहीं हैं बल्कि सामाजिक रिश्तों और पारंपरिक ज्ञान से भी इनका सीधा संबंध है। वन्य जीवन और जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी) भी इनमें शामिल हैं जो समुदायों के जीवन का अटूट हिस्सा हैं। लेकिन जैसे-जैसे कॉमन्स पर नियंत्रण केन्द्रीकृत हो रहा है, वैसे-वैसे समुदायों की भागीदारी सीमित होती जा रही है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं हैं कि कॉमन्स का प्रबंधन कौन करे बल्कि यह भी है कि क्या जो समुदाय इन्हें पीढ़ियों से संभालते आए हैं, वे खुद इससे जुड़े निर्णय लेने के हकदार माने जाते हैं?
इस सवाल का सीधा संबंध ग्राम-सभाओं से है। ग्राम-सभाएं संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त पहली इकाइयां होती हैं जहां समुदाय सीधे निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि अधिकांश ग्राम-सभाओं का आयोजन औपचारिकताएं और कागजी कार्यवाही पूरा करने तक ही सीमित रह जाता है। यहां पर सामुदायिक संसाधनों, पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे जरूरी मुद्दों पर ठोस चर्चा कम ही होती है। यही वजह है कि ग्राम-सभाओं को सशक्त बनाना और उनके एजेंडे को कॉमन्स और समुदाय की जरूरतों पर केंद्रित करना आज जरूरी हो गया है।
देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले उदाहरण बताते हैं कि जब समुदायों को अधिकार, जानकारी और नेतृत्व का अवसर मिलता है तो वे कॉमन्स की रक्षा न केवल बेहतर ढंग से करते हैं, बल्कि भविष्य के लिए स्थाई तरीके भी स्थापित करते हैं। लेकिन जब ये उनकी पहुंच से बाहर होने लगते हैं तो इनका विपरीत प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है।
राजस्थान में गांवों की गोचर, ओरण और शामलात जमीनें कभी पूरे समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी थीं। लेकिन हाल के वर्षों में पशुपालन में कमी आने के बाद से इन्हें बंजर मान लिया गया और इन पर अतिक्रमण बढ़ने लगा। कुछ जगहों पर गांव के ही ताकतवर लोग टुकड़ों में इन्हें बांटने लगे तो कहीं पर इन जमीनों का औद्योगिक या संस्थागत उपयोग किया जाने लगा। इसी तरह झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहां जंगल भोजन, दवा, ईंधन और सांस्कृतिक परंपरा के स्रोत हैं; वहां खनन और अन्य परियोजनाओं ने बड़े पैमाने पर विस्थापन और पारिस्थितिक नुकसान किया है। जंगलों का कटना सिर्फ पेड़ों का नुकसान ही नहीं होता बल्कि यह ज्ञान, रिश्तों और संसाधनों की पूरी श्रृंखला को प्रभावित करता है।
ओलाखान ट्रस्ट के निर्देश ओर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पारस बंजारा बताते हैं कि कॉमन्स की इस टूटन में बाहरी हस्तक्षेपों की एक बड़ी भूमिका तो है ही, लेकिन समुदायों के भीतर मौजूद जाति और जेंडर आधारित असमानताओं से यह और गहरा जाती है। राजस्थान के कई गांवों में गोचर जमीन पर पहला अधिकार उन्हीं का होता है जिनके पास पहले से निजी जमीनें हैं। घुमंतू समुदायों और दलित परिवारों को या तो इस जमीन से बेदखल कर दिया जाता है या उन्हें गांव की बैठकों में बुलाया ही नहीं जाता है। अगर बुलाया भी जाता है तो उनकी बात को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता है। झारखंड सहित कई राज्यों में ऐसी ही तस्वीर ग्राम-सभा की बैठकों में सामने आती है। इस संदर्भ में पीएचआईए फाउंडेशन के निदेशक जॉनसन टोपनो बताते हैं कि महिलाएं बैठकों में आती हैं लेकिन बोलती नहीं क्योंकि गांव के फैसले अब भी कुछ गिने-चुने पुरुष ही लेते हैं। खासकर जमीन, खनन और बाहरी हस्तक्षेप जैसे मामलों में महिलाओं की उपस्थिति तो होती है पर उनके फैसले निर्णायक नहीं माने जाते हैं।
कॉमन्स की उपयोगिता से आगे उन्हें जीवन के अभिन्न हिस्से की तरह देखना ग्रामीण समुदायों की विशेषता रही है। उन्हें परंपराओं और पुरखों के इतिहास से जोड़कर देखने वाला नजरिया, समुदायों को भावनात्मक रूप से भी उनसे जोड़ता है। ऐसे में ग्राम सभाएं उस साझा मंच की तरह काम करती हैं जहां लोगों की चिंताएं, संगठित होकर कुछ करने की दिशा में आगे बढ़ पाती हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं।
पारस बताते हैं कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के हस्तिनापुर गांव में एक समय चारागाह की जमीन पर जब कब्जे बढ़ने लगे तो गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि इसे बचाएंगे। इसके लिए सबसे पहले राजस्व रिकॉर्ड से जमीन की सीमा तय की गई और उसे गांव की दीवारों पर सार्वजनिक रूप से चस्पा किया गया। गांव की भागीदारी से कांटेदार झाड़ियों की बाड़बंदी की गई, मनरेगा के तहत तालाब खुदवाया गया, और तीन महीने के लिए पशु चराई पर सामूहिक रोक लगाई गई। गांव वालों ने खुद बारी-बारी से निगरानी की और आज यह जमीन न केवल हरी-भरी है, बल्कि पूरे गांव के लिए उपयोगी है।

ग्राम-सभा की सक्रियता सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहती, समुदाय और गांव के विकास से जुड़े जरूरी फैसलों पर मुखरता से बात रखना भी ग्राम-सभा का महत्वपूर्ण काम है। यहां पर ग्राम-सभाओं को सक्रिय करने के अर्थ और इसे कैसे किया जाए, यह भी समझना जरूरी है। सबसे जरूरी यह है कि समुदाय यह जाने कि ग्राम-सभा के संसाधन क्या हैं, अर्थात कितनी राजस्व भूमि है, कितनी सामुदायिक भूमि है, कितना वन क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, और पानी, मछली और वनोपज के स्रोत क्या हैं आदि। जब इन सबको मिलाकर देखते हैं तो समुदाय के सामने ग्राम-सभा के संसाधनों और अधिकार क्षेत्र की व्यापकता उजागर हो पाती है। समुदाय के पारंपरिक अगुवाओं जैसे विभिन्न आदिवासी समुदायों में पाहन, जोग मांझी, पुजार, मानकी और देवां आदि का समुदाय में एक प्रभाव होता है। लोग इन्हें सुनते हैं, ऐसे लोगों को ग्राम सभा की आधिकारिक समितियों से जोड़ना भी ग्राम-सभा को सक्रिय और मजबूत करने में कारगर सिद्ध होता है।
जॉनसन बताते हैं कि झारखंड के गुमला जिले के लुपुंग पाट गांव को इसके उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। असुर आदिवासी समुदाय के इस गांव में जब ग्राम-सभा को सक्रिय करने की इन प्रक्रियाओं को अपनाया गया तो वह वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) प्राप्त करने में सफल हुए। झारखंड में ऐसी कई सक्रिय ग्राम सभाओं के उदाहरण मौजूद हैं जहां समुदाय ने खुद अनुशासन कायम किया है। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम-सभा ने यह नियम बनाया कि अगर कोई परिवार लगातार दो-तीन बैठकों में शामिल नहीं होता है तो अगली बैठक उसी परिवार के घर होगी और उसकी व्यवस्था भी वही करेंगे। इस तरह की सामुदायिक निगरानी ने ग्राम-सभा को जीवंत बनाए रखा है।
ग्राम-सभा का मतलब केवल बैठकें करना भर नहीं है। जब हम कहते हैं कि “हम ही सरकार हैं” तो इसमें ग्राम विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, मॉनीटरिंग समिति जैसी लगभग आठ समितियां शामिल होती हैं। इन समितियों को सक्रिय करने से ही ग्राम-सभा समुदाय के साथ मिलकर सशक्त रूप से काम कर सकती है। जब किसी व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष या सदस्य है तो उसमें जवाबदेही का भाव आता है। फिर वही लोग ग्राम-सभा में सवाल करते हैं और सवालों के जवाब ही उस क्षेत्र का विकास तय करते हैं। इस तरह जब एक सक्रिय ग्राम सभा से वार्ड मेम्बर या पंचायत प्रधान जैसे चुने हुए लोग आगे जाते हैं तो वो पंचायती व्यवस्था में स्पष्टता के साथ समुदाय की बातें रखने में सक्षम हो पाते हैं।

इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता सियाराम हलामी बताते हैं कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के मेंढा-लेखा गांव में सामुदायिक वन अधिकार के तहत गांव के लोग खुद तय करते हैं कि जंगल से कब, कितनी और किस तरह वनोपज ली जाएगी। इससे जो आमदनी होती है; उसका उपयोग गांव के स्कूल, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को बनाने या सुधारने में होता है। यहां “हमारा गांव, हमारे जंगल” सिर्फ नारा नहीं, एक कार्य संस्कृति बन चुकी है।
ओडिशा की चिल्का झील में जब मछुआरों की आजीविका पर कॉर्पोरेट हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो स्थानीय समुदायों ने संगठित होकर सहकारी समितियों के जरिए झील का प्रबंधन अपने हाथ में लिया। आज वे खुद तय करते हैं कि मछली पकड़ने के नियम क्या होंगे, और कैसे झील की पारिस्थितिकी का संतुलन बना रहेगा।
वर्ष 1992 में हुए संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को स्थानीय स्व-शासन की प्राथमिक इकाई और सामुदायिक संपत्तियों के संरक्षक के रूप में स्थापित करके, कॉमन्स के लिए सामुदायिक निर्णय लेने की रूपरेखा को मजबूत किया। वर्ष 1996 का पेसा अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था) इस व्यवस्था का विस्तार पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों (अनुसूचित जनजाति क्षेत्र) में करता है।
इसके बाद के दशकों में कई कानूनों ने सामुदायिक अधिकारों और सामूहिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत किया है, जैसे:
हालांकि, सामुदायिक भूमि का शासन राज्यों के अनुसार अलग-अलग होता है क्योंकि भूमि और पानी राज्य सूची में आते हैं। वहीं, वन समवर्ती सूची में आते हैं और केंद्र व राज्य दोनों द्वारा देखे जाते हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य कॉमन्स को अलग तरह से परिभाषित और शासित करता है।
ओडिशा, उदाहरण के लिए, पांचवीं अनुसूची वाला राज्य है और वहां सामुदायिक भूमि की कई श्रेणियां दर्ज हैं — जैसे गोचर (चराई भूमि), रक्षित (सुरक्षित भूमि), और सरब-साधारण (सामान्य भूमि)। लेकिन राज्य ने अभी तक पेसा के नियम नहीं बनाए हैं जिससे समुदायों और पंचायतों की सामूहिक संरक्षकता असुरक्षित रह जाती है।
इसके अलावा, कॉमन्स की सुरक्षा के लिए बने कई कानूनों को कुछ जगहों पर कमजोर समुदायों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य वाला फैसला कॉमन्स के संरक्षण के लिए था, लेकिन कई मामलों में इसका इस्तेमाल दलित और घुमंतू समुदायों को उनकी भूमि से बेदखल करने में किया गया है।

यहां तक कि जहां पेसा और एफआरए लागू हैं, वहीं दूसरे कानून इनके प्रावधानों को कमजोर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के भूमि राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र हेतु भूमि आवंटन) नियम, 2007 के तहत ‘सरकारी भूमि’ को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है, जिससे चरागाह भूमि का विचलन हो रहा है।
इसके बावजूद, कई जगहों पर समुदायों ने कानूनों का इस्तेमाल करके अपने सामुदायिक अधिकारों को स्थापित किया है और सामूहिक शासन प्रणालियों को पुनर्जीवित किया है।
कई राज्यों में संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन की नींव रखी तो गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह काम आसानी से नहीं चलता। इस समझाते हुए सेवा निकेतन के कार्यक्रम प्रबंधक सीतल कुमार बताते हैं, साल 2006 में एफआरए लागू होने के बाद, ओडिशा के कालाहांडी जिले में प्रशासन ने चार वर्षों में लगभग 120 ग्राम सभाओं को सामुदायिक वनाधिकार के पट्टे जारी किए। लेकिन इनमें से कई पट्टे गांवों तक पहुंचे ही नहीं, और जहां पहुंचे भी, वहां समुदायों को यह समझाने की कोई प्रक्रिया नहीं थी कि इन अधिकारों का उपयोग कैसे होगा। इस खालीपन को देखते हुए उन्होंने और ओडिशा जंगल मंच के साथियों ने गांव-गांव जाकर समझाना शुरू किया कि सीएफआर का मतलब क्या है, इससे कौन-कौन सी जिम्मेदारियां आती हैं और इससे गांव क्या बदल सकता है।
यह चुनौती केवल ओडिशा की नहीं है। जॉनसन टोपनो बताते हैं कि झारखंड जैसे राज्यों में पेसा और एफआरए दोनों पर ग्राम सभाओं के साथ पर्याप्त काम नहीं हुआ है, इसलिए अधिकार तो दिए गए लेकिन उन्हें कैसे लागू किया जाए, यह समझ विकसित नहीं हो पाई। कई जगह तो गांवों के पास भूमि के आधिकारिक रिकॉर्ड भी नहीं थे। सीमाएं पेड़ों, पत्थरों, नदी-ढलानों की सामुदायिक स्मृति में थीं, लेकिन राजस्व नक्शों में नहीं। साल 2006 के एफआरए में हाथ से बने साधारण नक्शे मान्य थे, लेकिन साल 2012 में अनिवार्य जीआईएस मैपिंग लागू होने के बाद, कई जगह अधिकारियों ने तकनीकी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर जंगल की सीमा कम कर दी। सीतल बताते हैं कि कालाहांडी में इससे निपटने के लिए ग्राम सभाओं ने अपने स्तर पर जीपीएस लेकर जंगल की परिधि नापी—13-15 किलोमीटर तक पैदल चलकर सीमा-बिंदु दर्ज किए। भले इसमें त्रुटियां हों, लेकिन इससे समुदायों के पास अपना ठोस प्रमाण तैयार हुआ।

यह भी देखा गया कि कुछ जगह अधिकारियों ने खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाकर रिकॉर्ड बाद में बदल दिए। लेकिन वन विभाग की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती। गैर-काष्ठ वन-उत्पाद बेचने के लिए ट्रांजिट परमिट भी वही जारी करता है। कालाहांडी में एक ग्राम सभा को यह परमिट पाने में दो साल लगे। इसी वजह से ग्राम सभाओं का संगठित होना और भी जरूरी हो जाता है। कालाहांडी की महासमिति तकनीकी सहायता देती है, लेकिन निर्णय गांवों में खुली बैठकों में लिए जाते हैं, जैसे बांस या तेंदू पत्ता काटने की मजदूरी कितनी होगी, कितना पैसा संरक्षण में लगेगा और ग्राम सभा के पास कितना रहेगा। पहले तेंदू पत्ता, विभाग 50 पत्तों के 3.40 रुपये में लेता था और 7 रुपये में बेच देता था। अब ग्राम सभाएं सामूहिक रूप से मोलभाव कर बेहतर कीमत पर खुद बेच रही हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी महा-ग्राम सभा यही प्रक्रिया अपनाती है, ताकि लाभ सीधे परिवारों तक पहुंचे।
भारत के कई हिस्सों में समुदाय अपने साझा संसाधनों- जंगल, चराई भूमि, पानी, खेती की जमीन को मिलकर बचा रहे हैं। यह काम केवल कानूनों या योजनाओं से नहीं होता बल्कि उस साझेदारी से होता है। इसमें गांव वाले खुद नियम बनाते हैं, पालन करते हैं, और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलते भी हैं। सिक्किम के लाचेन और लाचुंग में ‘जुम्सा’ नाम की स्थानीय व्यवस्था है जो जंगल और पवित्र उपवनों की रक्षा करती है जहां कोई बाहरी दखल नहीं, निर्णय पिपोन और गांववासियों की सहमति से होते हैं। वहीं महाराष्ट्र और ओडिशा में कई ग्राम सभाएं मिलकर महा-सभा बनाती हैं, ताकि तेंदू पत्ता जैसे जंगल उत्पादों की बिक्री सामूहिक रूप से तय हो सके और लाभ गांव में ही रहे। इन उदाहरणों से साफ है कि रास्ता कहीं बाहर से नहीं आता बल्कि वही समाधान टिकाऊ होता है जिसे लोग स्वयं मिलकर बनाते और निभाते हैं। इसलिए कानून, योजनाएं और नीतियां जितनी जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी है लोगों की आवाज, उनका अधिकार, और उनकी साझेदारी।
सृष्टि गुप्ता और तनुप्रिया सिंह ने इस लेख में योगदान दिया है।
*इस लेख के कुछ हिस्सों को प्रकाशन के उपरांत 19 नवम्बर 2025 संशोधित किया गया है।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—