जब तक जातिगत समुदायों की कोई जानकारी ही नहीं होगी तो उनके विकास की तैयारी कैसे होगी?
बीती गर्मियों में किए गए अपने एक ट्वीट में एक्टिविस्ट बेजवाड़ा विल्सन ने लिखा था कि भारत में पिछले पांच वर्षों में सीवर और सेप्टिक टैंक में मरने वाले श्रमिकों की संख्या 35 फ़ीसदी तक घट गई है। विल्सन सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय कर्ताधर्ता हैं। यह हाथ से मैला ढोने (भारत की सबसे निचली जाति के लोगों को सौंपा गया काम जिसपर 2013 में प्रतिबंध लगा दिया गया था) की प्रथा समाप्त करने की मांग करने वाले सफाई कर्मचारियों का एक संघ है।
विल्सन ने अपने ट्वीट में लिखा था कि “आंकड़ों में हेराफेरी करने की बजाय जीवन बचाना ज़्यादा आसान होता।” लेकिन जाति पर आधारित आंकड़ों के साथ तो हेराफेरी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जाति-आधारित असमानताओं पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध ही नहीं हैं।
भारत में हाथ से मैला ढ़ोने की परम्परा अब तक क्यों जारी है? सरकार सीवर की सफ़ाई का मशीनीकरण कर इस अमानवीय प्रथा पर रोक क्यों नहीं लगा देती है, जैसा कि इसने संकेत दिया है कि यही इसका उद्देश्य रहा है? इसका उत्तर गहरे तक जमी उस गैर-बराबरी में है जो विकास से जुड़ी चर्चाओं और आंकड़ों दोनों में साफतौर पर दिखाई देती है।
जातिप्रथा, गरीबी और अलगाव को पैदा करती है और इसकी उपस्थिति कई सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स – एसडीजी) में साफ़ देखी जा सकती है। जातिगत भेदभाव के सबूत स्पष्ट होने के बावजूद, विकास लक्ष्यों के संदर्भ में तरक्की को दिखाने वाले वे आंकड़े बहुत थोड़े हैं जो जाति पर आधारित ग़ैर-बराबरी की बात करते हों। भारत को आज़ाद हुए सात दशक से भी अधिक का समय बीत चुका है लेकिन जाति पर आधारित भेदभाव और ग़ैर-बराबरी, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूपों में, विकास के प्रयासों को प्रभावित कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर जाति-आधारित आंकड़ों की भारी कमी है।
आंकड़ों की कमी का वास्तविक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसा हमने ऊपर दिए उदाहरण में देखा। इस ग़ैर-बराबर दुनिया में जिन लोगों की गिनती नहीं होती, वे महज़ गुमशुदा आंकड़े नहीं हैं। अपने कमजोर लोगों की गणना करने में विफल लोकतंत्र उन लोगों को ही मताधिकार से वंचित कर देता है, जिन्हें लोकतंत्र की सबसे अधिक ज़रूरत होती है।
जाति को नज़रअंदाज़ करने से करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं
समस्या कितनी गम्भीर है? दुनियाभर में करोड़ों लोग पहले से निर्धारित और अत्यंत असमान सामाजिक वर्ग या जाति व्यवस्था में जन्म लेते हैं। ये व्यवस्थाएं ही इन लोगों को जीवन भर मिलने वाले अवसरों का निर्धारण करती हैं।
यदि इन्हें एक देश मान लिया जाए तो दलितों की कुल संख्या दुनिया के सातवें सबसे बड़े देश की आबादी के बराबर है (और यदि हम उन लोगों को भी शामिल कर लें जिन्होंने बौद्ध या इस्लाम धर्म अपना लिया है लेकिन अब भी उन्हें दलितों में ही गिना जाता है तो ये विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले चौथे देश हो जाएंगे)। दलितों को वंश-आधारित भेदभावों जैसे जाति या जाति जैसी ही अन्य व्यवस्थाओं से निकलने वाली छुआछूत और अपमान आदि का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार, अधिसूचित समुदायों या विमुक्त जातियों (1971 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली) के लोगों की कुल संख्या लगभग 15 करोड़ है। ये लोग मुख्य रूप से खानाबदोश वर्ग में आते हैं और भारत के अधिकारिक आंकड़ों से बाहर होते हैं।
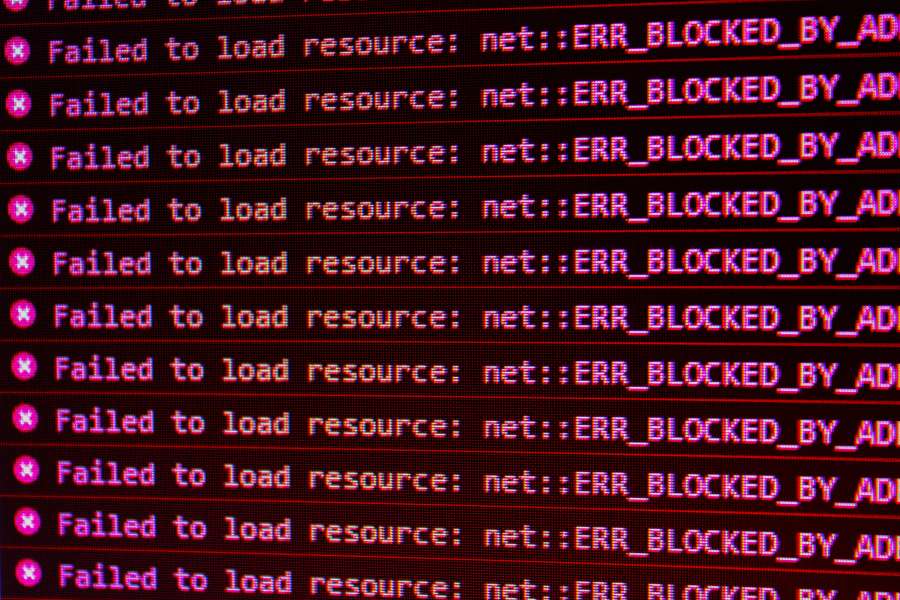
भारत में अधिकारिक आंकड़ा लोगों को या तो अनुसूचित जाति (निचली जाति के लोग जिनमें दलित भी शामिल हैं) या ग़ैर-अनुसूचित जाति (सवर्ण जातियों का समूह जिनमें उच्च जाति के हिंदू और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग शामिल होते हैं) में वर्गीकृत करता है। ये वर्ग आंकड़ों की विषमता पर प्रकाश डालते हैं। ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ की श्रेणी में आने वाले लोग भारत की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं और इनके एक बड़े तबके का जीवन अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाले लोगों के जीवन स्तर के समान ही होता है।
निजी अनुसंधान एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से भारत में गरीबी और असमानता की एक अधिक साफ़ और पूरी तस्वीर सामने आती है। घरेलू स्तर पर उपभोग का आंकड़ा आय की तुलना में जीवन-स्तर को मापने के लिए एक अधिक मज़बूत और कारगर तरीक़ा होता है। इस आंकड़े को यूनीवर्सिटी ऑफ़ मेरीलैंड और एक समाजसेवी थिंकटैंक नेशनल काउन्सिल ऑफ़ अप्लाइड एकनॉमिक रिसर्च के इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे द्वारा प्राप्त किया जाता है। हालाकि इनके आंकड़े ग़रीबी और असमानता को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, पर सरकार एडवोकेसी या नीति परिवर्तन के लिए इस आंकड़े को स्वीकार नहीं करती है।
जाति के वर्ग में शामिल न हो पाने का प्रभाव
वर्ग से संबंधित आंकड़ों की कमी मौजूदा ग़ैर-बराबरी को दिखाती है और उसकी पुष्टि करती है। इसके लिए आर्थिक और सामाजिक शक्ति के ऐतिहासिक स्त्रोत, भूमि का उदाहरण लेते हैं। हम नहीं जानते हैं कि भूमि स्वामित्व के मौजूदा आंकड़े में जातियों का क्या अनुपात है। किस जाति के पास अधिक भूमि है? आज़ादी के सात दशकों में किस जाति के लोग अधिक भूमिहीन हो गए?
वर्ग से संबंधित आंकड़ों की कमी मौजूदा ग़ैर-बराबरी को दिखाती है और उसकी पुष्टि करती है।
हमारे पास इससे जुड़ी जानकारी नहीं है कि प्रत्येक जाति के कितने लोगों को सरकारी कल्याणकारी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है? हम एसडीजी के आधार पर जाति स्तर पर होने वाली प्रगति पर नज़र नहीं रख सकते हैं। हमारे पास उपलब्ध सीमित आंकड़े हमें यह बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों का जीवन स्तर बदतर है। उदाहरण के लिए, औसतन, अनुसूचित जाति की महिलाओं की औसत आयु, राष्ट्रीय औसत आयु से 14.6 वर्ष कम है। लेकिन हम नहीं जानते कि अनुसूचित और अन्य पिछड़ी जातियों के रूप में समूहीकृत हजारों विविध जातियों/समुदायों में यह आंकड़ा बदतर है या बेहतर। कितने बाल श्रमिक किस जाति से आते हैं? कितने बेघर दलित या अनुसूचित और अधिसूचित जनजाति के हैं? जातीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा क्या कहता है? अधिक और बेहतर आंकड़े इकट्ठा किए बिना हम इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं और न ही असमानताओं को दूर करने के लिए किसी भी तरह की नीतियां ही विकसित कर सकते हैं।
जाति की उपेक्षा कर विकास को नकारना
यह कोई संयोग नहीं है कि भारत सरकार अलग-अलग जातियों की गणना करने वाले आंकड़े को इकट्ठा करने या प्रकाशित करने का विरोध करती है। हम क्या गिनते हैं और क्या नहीं यह हमारे मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है। जाति की जानकारियों पर आधारित विकास ढांचे की कमी- गुणवत्ता के स्तर पर और राजनीतिक रूप से- उस ढांचे से अलग है जो अन्य पहचान कारकों, उदाहरण के लिए लिंग आदि, की उपेक्षा करता है। एक सामाजिक श्रेणी के रूप में लिंग की महत्ता को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। लेकिन जाति का सवाल, विकास और इससे जुड़े लोगों और कर्तव्य-वाहकों दोनों के लिए, अब भी एक अभिशाप बना हुआ है।
उदाहरण के लिए, नीति आयोग (भारत की नीति और नियोजन प्राधिकरण) और भारत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार एसडीजी स्थानीयकरण का भारतीय मॉडल, बड़े पैमाने पर जाति की वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है। इस प्रक्रिया में यह एक असंभव स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और वो है, जातिगत वास्तविकताओं को नज़रअन्दाज़ करके विकास के लक्ष्यों का स्थानीयकरण करना। इसी प्रकार, घोर गरीबी और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की एक हालिया रिपोर्ट आई है जिसका उद्देश्य है उन लाखों सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जिनके पास सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं या तो उपलब्ध नहीं हैं या वे इन तक पहुंच नहीं पाते हैं। पर यह रिपोर्ट बुरी तरह विफल हो जाता है क्योंकि यह जाति, नस्ल, लिंग, धर्म और यौन झुकावों की चर्चा ही नहीं करता जिनके आधार पर लोग सामाजिक लाभों से वंचित कर दिए जाते हैं।
विश्व स्तर पर, लैक ऑफ़ डेवलपमेंट (विकास की कमी) सामाजिक विकास प्रयासों के डिजाइन, योजना निर्माण एवं उसे लागू करने तथा उसके मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख रूपरेखा रही है। ऐसी धारणा है कि धीरे-धीरे ही सही लेकिन विकास अंततः उन लोगों तक पहुंचेगा जो हाशिए के आख़िरी छोर पर हैं। हालांकि सबूत इसके विपरीत हैं। किसी को पीछे नहीं छोड़ने के एजेंडे के (लीव नो वन बिहाइंड एजेंडा) बावजूद हम विकास को समान रूप से सभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं।
ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाली जातियों के अधिकांश लोगों के लिए, प्रासंगिक और गहराई से अध्ययन कर तैयार किए आंकड़े उपलब्ध करवा सकने में व्यवस्था का इनकार भारत को एसडीजी हासिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। जाति को मापने के लिए आंकड़े की मौजूदगी या ग़ैर-मौजूदगी हमारे ढांचे और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। अक्सर हमारे सामने वही आंकड़े आते हैं जिनमें व्यवस्थागत तरीक़े से लोगों और समुदायों को लगातार बाहर ही रखा जाता है। इसे ठीक करने के लिए मेरी राय है कि हम ‘डिनायल ऑफ़ डेवलपमेंट’, विकास से जानबूझ कर दूर रखने वाली नज़र या लेंस, को दिमाग़ में रखें। भारतीय उपमहाद्वीप में यह लेंस असमानता और अभाव के मूलभूत कारण (पर्सिसटेंट स्ट्रक्चरल रीजन) को समझने के लिए जातिगत नजरिए को अहम दर्ज़ा देगा और इससे जाति पर बेहतर डेटा डिज़ाइन और संग्रह भी मुमकिन हो पाएगा।
यह लेख मौलिक रूप से द डाटा वैल्यूज डायजेस्ट में प्रकाशित हुआ था।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
लेखक के बारे में
- अरुण कुमार एक सामाजिक परिवर्तन कन्सल्टंट, रिसर्चर और लेखक हैं। उन्होंने सामाजिक उद्देश्यों वाले कई संगठनों के साथ बहुत ही व्यापक स्तर पर काम किया है। उनका अकादमिक लेखन हाशियाकरण और प्रतिरोध की सबाल्टर्न सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के बारे में हैं। वहीं सामाजिक विकास से जुड़े अपने लेखन में वह जाति, जलवायु परिवर्तन, प्रवास और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में शहरी गरीब नेक्सस की बात करते हैं। अरुण ज्यादातर समय लंदन में रहते हैं।









