उमाशंकर साह बिहार के शिवहर जिले के निवासी हैं और इलेक्ट्रिक ऑटो चलाकर अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। उमाशंकर बताते हैं कि सामान्य दिन में खर्च काट कर 800-900 रुपये तक, और कोई खास दिन रहने पर डेढ-दो हजार रुपये तक भी कमाई हो जाती है। ताजा आर्थिक सर्वे के अनुसार, कई आर्थिक पैमानों पर शिवहर जिला अन्य जिलों से पीछे है, जहां रोजगार और स्थानीय स्तर पर आजीविका कमाने के विकल्प बहुत कम हैं।
ऐसे में कभी खुद एक प्रवासी मजदूर रहे उमाशंकर ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को अपनी आजीविका का आधार बनाया है। साह अपने नये रोजगार से खुश हैं, लेकिन उनकी चिंता ऑटो की चार्जिंग को लेकर है। वे कहते हैं कि नई गाड़ी एक बार चार्ज करने पर 120 किमी तक चलती है और उन्हें हर दिन दो बार बैट्री चार्ज करना होता है और यह सुविधा अभी उनके लिए सिर्फ घर पर ही है। बैटरी कम चार्ज रहने पर दूर की सवारी मिले तो सोचना पड़ता है क्योंकि अभी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा नहीं है।
बिहार में किसी भी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहन (इलेक्ट्रिक व्हीकल- ईवी) के लिए सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट वर्तमान में सबसे अहम समस्या है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन नीति में चरणबद्ध रूप से शुरुआती चरण में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक भवनों और संपत्ति पर पांच साल में दो चरणों में 277 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, इस नीति में शुरुआती चरण में वाहनों की खरीद पर आर्थिक सहायता या सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन में 75% तक की छूट का प्रावधान किया गया है।
बिहार में पांच दिसंबर, 2023 को जारी की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगले पांच सालों के लिए प्रभावी है। इसके तहत बिहार ने एक ईवी इकोसिस्टम विकसित करते हुए 2028 तक कुल नए रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 15% और 2030 तक 30% करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल, यह 6.85% है जो देश में नए वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 6.40% से थोड़ा आगे है।
इस पॉलिसी के जारी होने के बाद बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल का गठन किया है और पॉलिसी के तहत सब्सिडी देने के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है।

ईवी थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स में ई-मोबिलिटी स्पेशलिस्ट अर्चित फर्सुले कहते हैं, “बिहार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में बसों और रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है और इसके प्रोत्साहन के लिए 56.54 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी किया गया है।”
अर्चित कहते हैं, “इलेक्ट्रिक व्हीकल बिहार की अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था और पर्यावरण में अहम योगदान कर सकते हैं। ईवी विनिर्माण उद्योग, रखरखाव और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। ईवी विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश आकर्षित करने से बिहार के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधनों पर निर्भरता कम होने से ईंधन लागत में भारी बचत होगी। इससे राज्य में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है और वायु गुणवत्ता में सुधार संभव है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) के अनुसार, भारत का जीवाश्म ईंधन की वजह से वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वर्ष 2021 में योगदान लगभग 6.8% रहा।” ये साल 2000-2021 में 156% बढ़ा है।
इलेक्ट्रिक बसें कुशल, स्वच्छ और शांत परिवहन प्रदान करके सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर बना सकती हैं। बिहार ईवी नीति का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना है।
बिहार सरकार की एजेंसी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की फेम-2 स्कीम के तहत राज्य में 25 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन कर रही है।
इलेक्ट्रिक बसें दो श्रेणी की हैं– एक नौ मीटर और दूसरी 12 मीटर। इनका लोकप्रिय नाम 9एम और 12एम बसें हैं। हालांकि अत्यधिक लागत और रियायती किराये की वजह से इन बसों को चलाया जाना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए की गई एक खर्चीली कवायद है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) के एक अधिकारी ने बताया, “नौ मीटर बसों के परिचालन में 79 रुपये प्रति किमी खर्च आता है जबकि 12 मीटर बस के परिचालन में 84 रुपये प्रति किमी खर्च आता है। जबकि इन दोनों प्रकार की बसों से करीब 40 रुपये प्रति किमी की दर से राजस्व संग्रहण होता है।” इन बसों का स्वामित्व इसकी निर्माता कंपनी अशोका लिलैंड के पास है और ड्राइवर भी उसी कंपनी का होता है जिसका फेम-2 के तहत परिवहन निगम परिचालन करता है। इन बसों को चलाए जाने के खर्च और इनसे होने वाली कमाई के अंतर की भरपाई केंद्र व परिवहन विभाग की सब्सिडी के जरिए होती है। बस के प्रति किमी परिचालन के हिसाब से बीएसआरटीसी बस ऑपरेटर कंपनी को भुगतान करता है और यात्री परिवहन से हासिल होने वाले राजस्व का काम वह खुद संभालता है।
अर्चित फर्सुले कहते हैं, “यह बात सही है कि इलेक्ट्रिक बसों की अधिक पूंजी लागत इसे व्यापक रूप से अपनाए जाने में एक बाधा है, लेकिन ऐसी कई रणनीतियां हैं जो इनकी लागत को कम कर सकती हैं, जैसे– थोक खरीद यानी कई शहरों या राज्यों में मांग को एकत्रित करके, सरकार निर्माताओं के साथ बेहतर कीमतों पर बातचीत कर सकती है।“

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के ज़रिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करने से वित्तीय बोझ को साझा करने में मदद मिल सकती है। सीधे खरीद की बजाय, सरकार ई-बसों को लीज पर लेने पर विचार कर सकती है। ग्रीनबॉन्ड, जलवायु निधि और रियायती ऋण जैसे नए वित्तीय तंत्रों का उपयोग करके कम ब्याज दरों और अनुकूल शर्तों पर ई-बस खरीद के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान की जा सकती है।
इस संबंध में अर्चित कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड (सीइएसएल) की उस केस स्टडी का उदाहरण देते हैं, जिसमें भारत के प्रमुख महानगरों में इलेक्ट्रिक बसों की एक साथ खरीद करने से परिचालन लागत व सरकार की प्रति किमी सब्सिडी को कम करने में सफलता मिली है।
इलेक्ट्रिक बसों की परिचालन लागत, उसकी ऊंची कीमत और अधिक रखरखाव लागत की वजह से भले ही अधिक हो लेकिन ईंधन लागत के स्तर पर यह अपेक्षाकृत काफी सस्ती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सीएनजी व डीजल बसों के एक किमी परिचालन पर 23.50 रुपये की ईंधन लागत आती है जबकि इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने की लागत प्रति किमी मात्र 14 रुपये आती है।
लंबे रूट में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का किराया डीजल से चलने वाली एसी बसों के बराबर है और ग्राहक से कोई अतिरिक्त किराया नहीं वसूला जाता है। लेकिन जगह-जगह फिलहाल चार्जिंग स्टेशन न होने के कारण बस बीच रास्ते एक दूसरी चार्ज हुई बस से बदल दी जाती है। यात्रियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए इसमें सफर करने को अधिक सुकूनदायक बताया। पटना के दानापुर के रहने वाले 40 वर्षीय विनोद कुमार ने कहा, “इलेक्ट्रिक बसों में सफर बेहतर है और हम इसका इंतजार करते हैं। किराये में भी बहुत फर्क नहीं है।“
केंद्र सरकार ने पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 10 हजार इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए 16 अगस्त 2023 को पीएम ई-बस सेवा योजना शुरू की। इस योजना के तहत पहले चरण में 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 3600 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं, जिसमें बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं। केंद्र सरकार इस योजना के तहत पूरे देश में बसों के परिचालन पर 10 साल के लिए सहायता देगी जिसके तहत 6400 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
पटना में एक टाटा मोटर शोरूम के सेल्स टीम हेड पवन नागपाल कहते हैं, “हमारी कंपनी पांच साल से ईवी सेक्टर में है और इसमें लगातार विकास हो रहा है।“ वे आगे जोड़ते हैं कि “हमारे यहां बिकने वाली 10 में दो से तीन गाड़ियां ईवी होती हैं। ग्राहकों का आकर्षण ईवी की ओर बढ़ रहा है और सरकार की स्कीम से भी वे प्रभावित होते हैं, बिहार सरकार द्वारा जारी की गई ईवी पॉलिसी से हम आशान्वित हैं।”
हालांकि यह ट्रेंड सिर्फ राजधानी पटना का है और राज्य के दूसरे शहरों के बारे में ऐसे दावे नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि बिहार में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कार की बिक्री आधे प्रतिशत से भी कम है।
एक ईवी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वित्त वर्ष 2023-2024 में ईवी बिक्री में 5.5% हिस्सेदारी के साथ बिहार पांचवें नंबर पर है।
इसी तरह पटना के एक दोपहिया ईवी शो रूम एथर के सेल्स मैनेजर प्रियांशु सिंह ने कहा, “भारत सरकार के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के तहत वाहन की खरीद पर 10 हजार रुपये की सब्सिडी फिलहाल मिल रही है। बिहार सरकार की ईवी पॉलिसी आने के बाद उसके पोर्टल के जरिये ग्राहकों का आकर्षण बढ़ने की संभावना है।“ प्रियांशु मानते हैं कि सेल्स बढ़ाने के लिए चार्जिंग प्वाइंट या स्टेशन का नेटवर्क जरूरी है।
एक ईवी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वित्त वर्ष 2023-2024 में ईवी बिक्री में 5.5% हिस्सेदारी के साथ बिहार पांचवें नंबर पर है। दक्षिणी-पश्चिमी राज्यों में जहां दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिक बिक्री का ट्रेंड दिखता है; वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश व असम जैसे राज्यों में पैसेंजर ई-थ्री-व्हीलर की बिक्री का अनुपात ज्यादा है। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का पहले से ही बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। बिहार में दो पहिया वाहनों (13.87%) की तुलना में पैसेंजर ई-थ्री-व्हीलर (83.72%) की बिक्री छह गुना अधिक है।
हालांकि आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि वित्त वर्ष 2018 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 तक बिहार में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेड़ा 39 गुना बड़ा हो चुका है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलग-अलग सेगमेंट के लिए चुनौतियां भी अलग-अलग हैं। जैसे दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के लिए उसकी निर्माता कंपनियों द्वारा चार्जिंग स्टेशन का निर्माण शहरी क्षेत्र में ही किया गया है, ऐसे में शहर से बाहर लंबी दूरी के लिए उन्हें लेकर नहीं जाया जा सकता। यही स्थिति इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के साथ है, जिसके चालक की मजबूरी है कि वे उसे घर पर ही चार्ज कर सकते हैं। बिहार में इलेक्ट्रिक बसों के लिए अभी पटना में एकमात्र चार्जिंग स्टेशन है, जबकि मुजफ्फरपुर व राजगीर इलाकों में उसके लिए चार्जिंग प्वाइंट हैं।
चार पहिया व दो पहिया वाहनों की सेल्स टीम के सदस्यों से बात करने के बाद यह तथ्य उभर कर सामने आया कि उन्हें पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए ग्राहकों की अधिक समझाइश करनी पड़ती है और इसकी वजह उनके प्रोडक्ट में कोई इश्यू होना नहीं बल्कि चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क की कमी होना है। हालांकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ चुनिंदा शहरों में इसके लिए सघन अभियान चलाने व स्कूलों को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे सुझाव भी हैं।
अर्चित फर्सुले कहते हैं, “बिहार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कुछ चुनौतियों के बावजूद रोमांचक राह पर है। उच्च पूंजी लागत, सीमित चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और बैटरी की उपलब्धता से जुड़ी समस्याएं प्रमुख बाधाएं हैं, लेकिन सरकार इससे निबटने के लिए प्रयास कर रही है। नई नीति की एक प्रमुख विशेषता स्थानीय बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देना है, जो भारत में हाल ही में हुई लिथियम खोजों का लाभ उठाएगा और जिससे लागत और आयात पर निर्भरता कम होगी।“ लिथियम ऑयन बैटरी की क्षमता लेड एसिड बैटरी से ज्यादा होती है– जिन पर ज्यादातर ईवी परिवहन चलते थे और आज भी चलते हैं। जहां लेड एसिड बैटरी को रीसाइकल करने में पर्यावरण और स्वास्थ्य को बहुत हानि है, वहीं लिथियम की रिसाइकलिंग रेट 90 से 95% है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर इसे रीसाइकल नहीं करके ऐसे ही जमीन में छोड़ देंगे तो यह उसे बंजर कर सकता है, और इसका निबटान एक बड़ी चुनौती है।
यह स्टोरी इंटरन्यूज अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क के रिन्यूएबल एनर्जी ग्रांट के तहत कवर की गई है।
—
कर्नाटक में बच्चों की ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं जिन्हें कन्नड़ में ‘मक्कला ग्राम सभा’ कहा जाता है। ये सभाएं ग्रामीण इलाकों में बच्चों के लिए स्थानीय सरकार यानी ग्राम पंचायत के साथ जुड़ने का एक सक्रिय मंच हैं। साल 2006 में, कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज (आरडीपीआर) विभाग ने एक सरकारी आदेश जारी किया। इस आदेश में यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक ऐसी ग्राम सभा आयोजित करनी होगी जिसमें बच्चे मुख्य सदस्य हों और जो इनसे संबंधित मुद्दों पर केंद्रित हों।
आमतौर पर, एक ‘मक्कला ग्राम सभा’ में पांच से छह गांवों के 150 से 250 बच्चे शामिल होते हैं। छात्रों के अलावा, इस सभा में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ), शिक्षा विभाग का क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी), आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास एजेंसियों के अधिकारी और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
इन सभाओं में बच्चे खुद के, साथियों के तथा अपने स्कूल व समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। उठाए गए सवाल आमतौर पर स्कूल और गांव में बुनियादी ढांचे की जरूरतों या बच्चों की सुरक्षा (जैसे कि उनके स्कूल के पास शराब की दुकानों का होना, या स्कूल परिसर में जुआ और तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों) के बारे में होते हैं।
हर साल नवंबर से जनवरी के बीच 6 हजार से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के हज़ारों बच्चे मक्कला ग्राम सभाओं में हिस्सा लेते हैं। यह लेख “चिल्ड्रन मूवमेंट फॉर सिविक अवेयरनेस” (सीएमसीए) के अनुभवों और सीखों पर आधारित है। सीएमसीए एक नागरिक समाज संगठन है जो 2011 से कर्नाटक में इन सभाओं को सक्रिय और व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए एक कार्यक्रम लागू कर रहा है। सीएमसीए का उद्देश्य इन सभाओं को ऊर्जा प्रदान करना और यह तय करना है कि बच्चे असरदार तरीके से अपनी समस्याओं और विचारों को सामने रख सकें।
बच्चों के प्रति संवेदनशील शासन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे केवल प्राप्तकर्ता न हों बल्कि उनसे संबंधित मामलों और निर्णयों में सक्रिय भागीदार भी हों। हमने जिन स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत की, वे बताते हैं कि ये ग्राम सभाएं उन्हें अपने मसले सामने रखने का मौका देती हैं। चिक्कमंगलूरू की 9वीं कक्षा की छात्रा, रेणुका* कहती हैं, “यह सभा बहुत उपयोगी है। हमारे स्कूल में न तो कंपाउंड है, न ही कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण। जब हमने ये जरूरतें बताईं तो सरकारी अधिकारियों ने वादा किया कि हमारे स्कूल को तकनीकी सुविधाएं दी जाएंगी। अगर हमें ऐसे मंच नहीं मिलते तो हम मौजूदा दिक्कतों के बारे में कभी नहीं बोल पाते।”

हमने जिन पंचायत अधिकारियों से बातचीत की, वे भी ग्राम सभाओं को एक सकारात्मक प्रभाव मानते हैं। बच्चों के नजरिए के महत्व को स्वीकार करते हुए, रामनगर ज़िला पंचायत के सीईओ, डिग्विजय बोडके, कहते हैं, “हमें बच्चों के नजरिए से सोचने की ज़रूरत है ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके। ‘मक्कला ग्राम सभाएं’ हमें यह समझने में मदद करती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है।”
अधिक समावेशी और बच्चों के लिए सुरक्षित मौके प्रदान करने के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों, साथ ही ग्राम सभा में, बच्चों के लिए ‘वॉइस बॉक्स‘ लगाए जाएं।
ये बॉक्स बच्चों को उन मुद्दों और चुनौतियों को व्यक्त करने का मौका देते हैं जिनके बारे में वे सीधे सभा में बोलने में संकोच कर सकते हैं या अगर वे सभा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस तरह, बच्चे अपनी जरूरतों और समस्याओं को सुरक्षित और सहज तरीके से साझा कर सकते हैं।
‘मक्कला ग्राम सभाओं’ ने हमें दिखाया है कि एक नेक इरादों वाली सरकार, मजबूत नीतियां और तंत्र, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों का उचित ध्यान और प्रेरणा, और एक सक्रिय नागरिक समाज मिलकर समुदाय में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, चिक्काबल्लापुरा और हसन जिलों के सरकारी स्कूलों में, ‘मक्कला ग्राम सभाओं’ की चर्चाओं के परिणामस्वरूप स्कूल भवनों की मरम्मत और अन्य सुधार किए गए हैं। बच्चों ने आय प्रमाण पत्र से संबंधित छात्रवृत्तियों तक पहुंच की दिक्कतों के बारे में बताया है। साथ ही पॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रमों और स्कूल के बच्चों और अन्य लोगों के लिए बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान की मांग की है।
चूंकि बच्चों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना, सुनना, और पूरी तरह से शामिल होना जरुरी होता है, ‘मक्कला ग्राम सभाएं’ बच्चों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, बच्चों को बदलाव का एक प्रभावी साधन बनाने के लिए और भी कुछ उपाय हैं।
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी—जैसे कि पंचायत के अध्यक्ष, अन्य निर्वाचित सदस्य, पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ), शिक्षा विभाग के अधिकारी, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी शिक्षिका, और बाल अधिकार एजेंसियां—इन ग्राम सभाओं में उपस्थित रहें। इनकी उपस्थिति ‘मक्कला ग्राम सभा’ को उत्पादक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ये अधिकारी मौजूद होते हैं तभी बच्चों और उनकी देखभाल के लिए जिम्मेदार वयस्कों को सही जानकारी दी जा सकती है। इससे चुनौतियों का समाधान खोजने में मदद मिलती है जैसे कि मुद्दे के समाधान की जिम्मेदारी कौन लेगा और उन मुद्दों के लिए धन कहां से आवंटित किया जा सकता है जो सीधे ग्राम पंचायत से जुड़े नहीं हैं।
हमने जिन बच्चों से बातचीत की, उन्होंने भी इस बात को समझा। 9वीं कक्षा की छात्रा अनीता* कहती हैं, “आज की ग्राम सभा में शामिल होने के बाद मुझे खुशी हुई। यहां सरकारी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हमारी मांगों और चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ विभागों के अधिकारी जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उन्हें भी आना चाहिए था ताकि वे हमारी समस्याओं का समाधान कर पाते।”
बेहतर परिणाम पाने के लिए मक्कला ग्राम सभाओं को बाल विकास और भागीदारी के प्रति ज्यादा समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरुरत है। हम देखते हैं कि मक्कला ग्राम सभाओं में बच्चों की ओर से उठाए गए मुद्दे अभी भी ज्यादातर मौलिक अधिकारों जैसे कि स्कूल की मरम्मत और यह सुनिश्चित करना कि स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचा हो, से संबंधित हैं।
कर्नाटक जैसे-जैसे बच्चों के प्रति संवेदनशील स्थानीय शासन को आगे बढ़ाने वाली नीतियों की ओर बढ़ रहा है तो ऐसे में बच्चों की भागीदारी और निरंतर निगरानी के तंत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें बच्चों की बजट और निर्णय लेने में भागीदारी शामिल है। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि बुनियादी अधिकारों से संबंधित समस्याएं समय पर और लगातार हल की जा सकें। इसके परिणामस्वरूप बच्चों के अनुभव में सुधार होगा और ‘मक्कला ग्राम सभा’ में उनकी भागीदारी ज्यादा सक्रिय होगी। साथ ही, यह बच्चों और स्थानीय सरकार के बीच गहरे और अर्थपूर्ण संवाद की संभावना को बढ़ाएगा। बच्चों के विकास सूचकांकों और उनकी समग्र भलाई पर इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा।
यह बताना अहम है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत होने से बच्चों के प्रति उत्तरदायिता में सकारात्मक बदलाव आया है। हम देखते हैं कि महिला प्रतिनिधि चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालती हैं और बच्चों की ओर से उठाए गए मुद्दों का जल्दी ही समाधान खोजने की कोशिश करती हैं। संस्थागत तंत्र को और मजबूत करने के लिए जरूरी अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति ताकि कार्यान्वयन में सुधार हो सके। इसके अलावा बच्चों की ओर से खुद ऑडिट करना जिससे वे सीधे तौर पर सेवाओं की गुणवत्ता और वितरण पर रिपोर्ट कर सकें। विद्यालयों और अन्य स्थानों पर नियमित बैठकें हों ताकि बच्चे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन पर चर्चा की जा सके।
ग्राम पंचायतों में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत होने से बच्चों के प्रति उत्तरदायिता में सकारात्मक बदलाव आया है।
इसके अलावा, पंचायत विकास अधिकारियों की तरफ से बच्चों को कार्यवाही की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना। साथ ही, मक्कला ग्राम सभा के परिणामों को संबंधित विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना। इससे बच्चों की भागीदारी और भी प्रभावी हो सकती है। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को मान्यता मिलेगी और बच्चों के विकास सूचकांकों के अलावा सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति में भी मदद मिलेगी।
आरडीपीआर विभाग की ओर से जारी सर्कुलर आज एक विस्तृत और प्रभावी दस्तावेज़ है। इसे सालों से काम कर रहीं समाजसेवी संस्थाओं के जमीनी अनुभवों से मजबूत बनाया गया है जो आरडीपीआर को सुझाव के रूप में मिलते रहे हैं। समाजसेवी संस्थाएं जैसे द कन्सर्न्ड फ़ॉर वर्किंग चिल्ड्रेन (सीडब्ल्यूसी), चिल्ड्रेन्स मूवमेंट फ़ॉर सिविक अवेयरनेस (सीएमसीए), प्रकृति फ़ाउंडेशन, ग्रामांतर, चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट (सीआरटी) और नव युवा प्रतिष्ठान सुनिश्चित करते हैं कि मक्कला ग्राम सभाएं चलती रहें।
यहां कुछ कदम दिए गए हैं जो सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओएस) ने उठाए हैं:
अब दूसरे राज्यों के लिए समय आ गया है कि वे मौजूदा नीतियों और पहलों को ध्यान में रखते हुए अपनी ग्राम पंचायतों में बच्चों की ग्राम सभाओं को लागू करें।
जैसे-जैसे बच्चों के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय शासन का उद्देश्य जोर पकड़ रहा है, ऐसे में यह अनूठा मंच एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह एक जांच और समीक्षा बिंदु के रूप में काम कर रहा है। साथ ही, बच्चों के लिए खुशी और आशा के दरवाजे भी खोल रहा है। यह हमारे लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी के महत्व को मान्यता देता है। बचपन में सहभागी लोकतंत्र के ऐसे शक्तिशाली अनुभव न केवल चुनावों और मतदान के दौरान बल्कि जीवन के एक तरीके के रूप में भी सरकार के साथ नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देंगे।
*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदल दिए गए हैं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
माली बनते हैं या पैदा होते हैं? इस प्रसिद्ध सवाल का जवाब जानने के लिए महाराष्ट्र के सतारा में जाएं और निकमवाड़ी गांव के गुलदाउदी और गेंदे के फूलों के खेतों पर नज़र डालें। जहां तक नजर डालो, वहां तक फूलों के रंग-बिरंगे खेत फैले हुए हैं, जिन पर पीले और नारंगी रंग के कालीन बिछे हुए हैं। लगभग दो दशक पहले, कृष्णा नदी बेसिन के इस गांव के किसान केवल दो नकदी फसलें, गन्ना और हल्दी उगाते थे, जिससे औसत उत्पादक का बस गुजारा भर हो पाता था।
हालांकि ये दोनों अब भी उगाई जाती हैं, लेकिन फूल निकमवाड़ी में खुशी और समृद्धि ला रहे हैं।
इसकी शुरुआत 2005 में हुई। धर्मराज गणपत देवकर, जिनकी आयु अब 60 वर्ष है, के नेतृत्व में मुट्ठी भर किसानों ने एक कृषि अधिकारी की सलाह पर ध्यान दिया और विश्वास की एक कठिन छलांग लगाते हुए पहली क्यारी में गेंदा के पौधे लगाए। यह 170 से ज्यादा घरों वाला गांव आज ‘फुलांचा गांव’ (फूलों का गांव) के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 200 एकड़ से ज्यादा भूमि पूरी तरह से फूलों की खेती के लिए समर्पित है। दोपहर की धूप में चमकते फूलों की ओर इशारा करते हुए, 37 वर्षीय किसान विशाल निकम कहते हैं – “यहां किसी भी मौसम में आइये, झेन्दु (गेंदा) और बहुरंगी शेवंती (गुलदाउदी) के फूलों से लदे हरे-भरे खेत देखने को मिलेंगे।”

निकमवाड़ी और उसके आस-पास के गांवों में ‘पूर्णिमा व्हाइट’, ‘ऐश्वर्या येलो’ और ‘पूजा पर्पल’ जैसी आठ किस्म की संकर गुलदाउदी उगाई जाती हैं। गुलदाउदी एक सर्दियों की फसल है, जिसका मौसम दिसंबर से मार्च तक, 120 दिनों का होता है। बारहमासी गेंदा वर्ष भर उगता है। इलाके में फैली सैकड़ों नर्सरियों में से एक, ‘ओम एग्रो टेक्नोलॉजी नर्सरी’ के शालिवान साबले कहते हैं – “’पीताम्बर येलो’, ‘बॉल’ और ‘कलकत्ता येलो’ ग्राहकों की पसंदीदा छह किस्मों में से हैं। हम सालाना करीब 20 लाख पौधे बेचते हैं।”
प्रकृति की सुन्दरता अद्भुत है – यह उपहार सोने के बराबर है। लेकिन इस खजाने को निकालने के लिए, किसी भी कृषि पद्धति की तरह, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है – पौधे लगाना, निराई करना, सिंचाई करना और सुबह से शाम तक फूल तोड़ना। और फिर शाम को बाज़ार के लिए निकलने से पहले पिक-अप ट्रकों में फूल भरना। हालांकि दिन के आखिर में, पैसा ही सुखदायक मरहम बनता है।

प्रति एकड़ लगभग 10 टन की औसत वार्षिक उपज के साथ, निकमवाड़ी के किसान सालाना लगभग 10 लाख रुपये कमाते हैं, जो गन्ने और हल्दी से होने वाली आय से कहीं ज्यादा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कई किसानों ने पानी की अधिक खपत वाली गन्ने की फसल को छोड़ दिया है। किसानों में चीनी मिलों के प्रति अविश्वास गहरा होने के कारण, हाल के वर्षों में गन्ने का रकबा कम हो गया है। उनका कहना है कि चीनी मिल उनकी उपज का वजन करने में धोखाधड़ी करती हैं तथा समय पर भुगतान नहीं करती हैं।
संजय भोंसले (55) ‘पूर्णिमा व्हाइट’ गुलदाउदी के अपने खेत की देखभाल से कुछ समय के लिए छुट्टी लेते हुए कहते हैं – “गन्ना मिलें लोगों को उनके पैसे के लिए 18 महीने से ज़्यादा इंतज़ार करवाती हैं। फूल उगाना फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमें हर हफ़्ते भुगतान मिलता है।” निकमवाड़ी के किसान ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत वे बावड़ियों से पानी प्राप्त करते हैं, जिसका पुनर्भरण कृष्णा नदी से आने वाली नहरों द्वारा होता है। इस तरह के बागवानी नवाचार खेतों को अधिक टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और स्वस्थ बना सकते हैं, तथा प्रकृति के साथ मानव के जटिल अंतर्संबंधों की रक्षा कर सकते हैं। आठ एकड़ के मालिक संतोष देवकर कहते हैं – “आजकल केवल मुट्ठी भर परिवार ही बड़े खेत के मालिक हैं, जो गन्ना उगाते हैं।” फूलों के बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण वे एक एकड़ में गन्ना उगाते हैं।
पुष्प अर्थव्यवस्था में पदानुक्रम चलता है। गुलाब, गुलनार और जरबेरा जैसे फूल अपनी आकर्षक कीमतों के मामले में प्रीमियम स्थान पर हैं, इसके बाद रजनीगंधा और ग्लेडियोलस जैसे बल्बनुमा फूल आते हैं।

गेंदा और गुलदाउदी सबसे निचले पायदान पर हैं। लेकिन निकमवाड़ी में फूलों की भारी मात्रा के कारण इसकी भरपाई हो जाती है। रोज सात पिकअप ट्रकों पर करीब 12 टन फूल, 100 किलोमीटर दूर पुणे के गुलटेकड़ी बाजार भेजे जाते हैं। हालांकि यह गांव मंदिर शहर वाई और जिला मुख्यालय सतारा के करीब है, लेकिन किसान पुणे को प्राथमिकता देते हैं, जहां मांग ज्यादा है। गणेश उत्सव से लेकर दिवाली और गुड़ी पड़वा तक त्योहारों के सीजन में मांग चरम पर होती है।
कृषि अधिकारी विजय वारले का कहना था कि निकमवाड़ी के किसान गुलदाउदी से प्रति एकड़ लगभग 2.5 लाख रुपये कमाते हैं, जबकि गेंदा से प्रति एकड़ लगभग 2 लाख रुपये की कमाई होती है। महाराष्ट्र में फूल एक फलता-फूलता व्यवसाय है, जहां 13,440 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती होती है। यह 1990 के दशक में फूलों की खेती की नीति बनाने वाला पहला राज्य भी है।
पड़ोसी गांवों ने भी फूलों की खेती शुरू कर दी है, लेकिन जो बात निकमवाड़ी को अलग करती है, वह यह है कि यहां हर घर में फूल उगाए जाते हैं, चाहे किसी के पास दो-चार गुंठा (1000 वर्गफीट) हो, या कई एकड़।

यह उनकी सहभागिता की भावना और सामूहिक दृष्टिकोण ही है, जो निकमवाड़ी को एक आदर्श गांव बनाता है। वे एकल फसल उत्पादन के नुकसान से भी अवगत हैं। छोटे-छोटे क्षेत्रों में गन्ना और हल्दी जैसी नियमित फसलें उगाने के अलावा, बहुत से किसान फूलों के खेतों में अजवायन भी उगाते हैं, एक ऐसी जड़ी-बूटी जिसकी विदेशों और भारतीय महानगरों में बहुत मांग है। संजय भोंसले, जिनका पांच एकड़ का खेत बहु-फसल का एक उदाहरण है, कहते हैं – “हम रसोई के लिए धनिया और बेचने के लिए अजवायन की खेती करते हैं। हम 1.5 लाख रुपये खर्च करते हैं और उपज से आय 3.5 लाख रुपये होती है।”
यह लेख मूलरूप से विलेज स्क्वायर पर प्रकाशित हुआ था।
हीरेन कुमार बोस महाराष्ट्र के ठाणे स्थित पत्रकार हैं। वे सप्ताहांत में किसानी भी करते हैं।
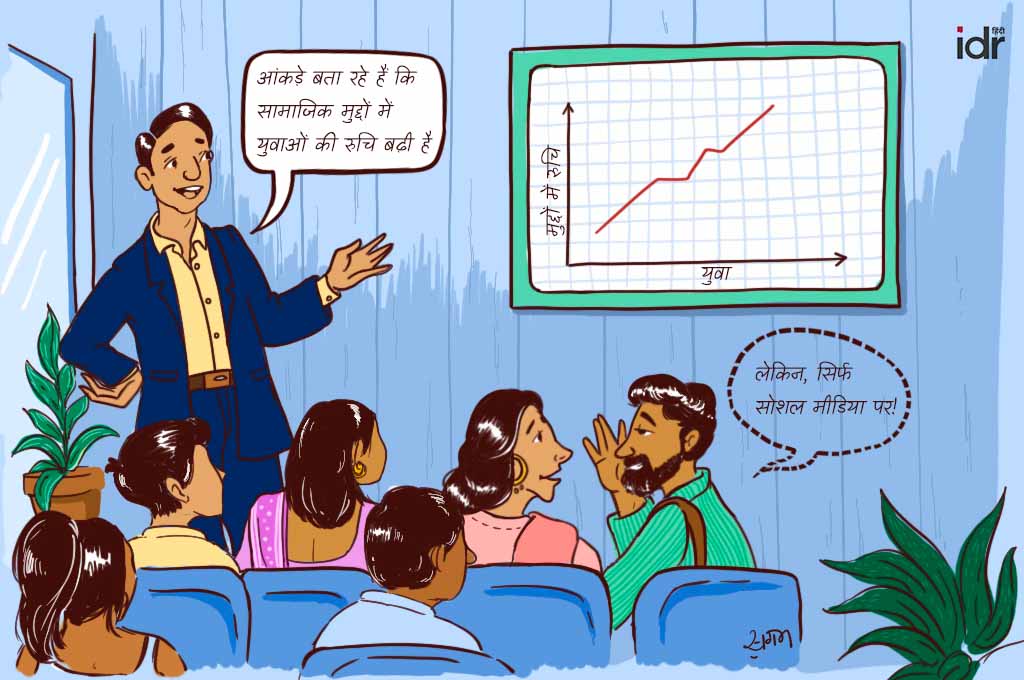
कमोबेश हर जमीनी संस्था अपने सामाजिक प्रभाव को व्यापक बनाने की आकांक्षा रखती है ताकि उनकी सेवाएं और प्रयास, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। विस्तार की इस प्रक्रिया से न केवल वे अपने दायरे को बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे उनकी सामाजिक पहचान भी मजबूत होती है।
हालांकि यह यात्रा उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती है। नवाचार संस्थान, चित्तौड़गढ़ और कोटड़ा आदिवासी संस्थान, उदयपुर जैसी जमीनी संस्थाओं के साथ बातचीत से पता चलता है कि इसमें कई तरह की बाधाएं है।
बढ़ती ज़िम्मेदारियों और बढ़ने काम के बोझ के साथ संस्थाओं के सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं। इसमें प्रभावी प्रबंधन, वित्त, प्राथमिकताएं, नए अवसरों की पहचान, रणनीतिक दृष्टिकोण प्रमुख रूप से शामिल हैं।
जमीनी संस्थाओं के लिए स्थायी और नियमित वित्तीय स्रोत जुटाना हमेशा एक कठिन काम रहा है। नवाचार संस्था के अरुण कहते हैं, “हमारे पास ज्यादातर फंड अन्य संस्थाओं से होकर आते हैं। ऐसे में पहले से ही निर्धारित होता है कि इस धनराशि का उपयोग केवल सामुदायिक गतिविधियों के लिए ही किया जा सकता है। ऐसे में संस्था को बढ़ाने, कार्यकर्ताओं के क्षमता-विकास और अन्य जरूरी पहलुओं के लिए फंड की समस्या बनी रहती है।”
कुछ एनजीओ अपनी कार्यक्षमता और विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय संसाधनों की खोज करने की बजाय अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं का इंतजार करते हैं। वे मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय दानदाता इन आवश्यकताओं को कुछ हद तक समझते हैं। एफसीआरए के मुद्दों के बाद ऐसा करना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।
कोटड़ा आदिवासी संस्थान के निदेशक सरफ़राज का मानना है कि “संस्था का छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है। अन्ना हजारे ने रालेगण सिद्धि जैसे छोटे से गांव में काम किया लेकिन आज वह पूरे भारत के लिए एक मॉडल ग्राम बन चुका है। ऐसे और भी मॉडल ग्राम बनने चाहिए।”
आज कई समाजसेवी संस्थाओं में दीर्घकालिक दृष्टिकोण और स्पष्ट मिशन की कमी दिखती है जो उनके विकास और विस्तार में बाधा बनती है। समाज में स्थायी प्रभाव लाना एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि अक्सर संस्थाएं इस लंबी प्रक्रिया के कारण बदलती सामाजिक चुनौतियों पर तो समुदाय के साथ जुड़कर काम करने के नवाचारों को प्राथमिकता देती हैं। लेकिन इसमें खुद को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई भविष्य की योजनाएं पीछे छूट जाती हैं।

कई एनजीओ बदलती चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालने में असफल रहते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। जमीनी संस्थाएं अभी भी अपने कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का विश्लेषण करने, उन्हें उपयुक्त कार्य-क्षेत्रों में लगाने और उनकी चुनौतियों को समझने पर कम ध्यान देती हैं। बिना उचित कौशल और क्षमताओं के कार्यों का बंटवारा करने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं।
अरुण इस बात पर जोर देते हैं कि “जमीनी संस्थाएं समाज के बीच रहते हुए भी भूमिकाओं में बदलाव (शिफ्ट ऑफ रोल) को समझने की कोशिश नहीं करती हैं। वे अब भी अपने पुराने मिशन पर काम कर रही हैं और कॉम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं।”
उपलब्ध मानव संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की नीति का अभाव संस्थान के विकास में बड़ी बाधा बनता है। इस स्थिति में, संस्थाओं का विस्तार करने का विचार अक्सर इस डर से रुक जाता है कि इससे समस्याएं और भी जटिल हो सकती हैं।
तेजी से बढ़ती तकनीक ने जमीनी संस्थानों की आवश्यकताओं को भी बदल दिया है। अरुण कहते हैं, “आजकल हर संस्था के पास वेबसाइट होना अनिवार्य हो गया है और समुदाय से जुड़ाव के लिए सोशल मीडिया भी ज़रूरी हो गया है।” वे आगे जोड़ते हैं कि “लेकिन तकनीकी रूप से सक्षम प्रोफेशनल्स कम वेतन पर और छोटे इलाकों में लंबे समय तक काम करने के इच्छुक नहीं होते। इसके अलावा, अब इस सेक्टर में भी लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। वे अपने संस्थान से अधिक अपने रिज़्यूमे को मजबूत बनाने को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि प्रोफेशनल होने में कोई बुराई नहीं है लेकिन इस सेक्टर में बदलाव लाने के लिए समय देना पड़ता है। उन्हें हमारी जैसी जमीनी संस्थाओं में रोके रखना वास्तव में एक गंभीर चुनौती है।”
यह भी देखा गया है कि प्रबंधन, फंडिंग प्रपोजल, डेटा विश्लेषण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि में तकनीक का योगदान पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। ऐसे में, कम तकनीकी कौशल वाली संस्थाएं अपने लक्ष्यों को बड़े स्तर पर ले जाने में विफल हो जाती हैं।
संस्थाओं को अपने कार्य को बढ़ाने के लिए बेहतर रणनीतिक योजना, निगरानी, और मूल्यांकन जैसे तरीकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए कर्मचारियों की क्षमता को लगातार बढ़ाना ज़रूरी है। सरफ़राज़ कहते हैं, “ऐसा नहीं है कि संस्थाएं क्षमता-वर्धन पर काम नहीं करती हैं लेकिन इसके तरीके काफी पुराने हैं। हम अभी भी पुराने कंटेंट पर काम कर उसे अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।” कई संस्थाएं क्षमता निर्माण में निवेश करने से इसलिए भी हिचकिचाती हैं क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं।
जटिल सरकारी नीतियां और अनुपालन आवश्यकताएं भी बाधा बनती हैं। कई बार समाजसेवी संस्थाओं पर कठोर सरकारी नियम और प्रतिबंध होते हैं जिससे उनके लिए अपने काम को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। सरफ़राज बताते हैं कि “हमारे पास दो अकाउंटेंट हैं। उनमें से एक तो सारा दिन बस सरकारी नियमों के 12ए, 80जी जैसे कागजों को पूरा करने में ही लगे रहते है। कागजों की जटिलता के चलते कई संस्थाएं एफसीआरए होते हुए भी बाहरी धन नहीं ले पाती हैं।”
अरुण इसमें जोड़ते हैं “जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) की शुरुआत हुई तो एक उम्मीद जगी थी कि वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। लेकिन बाद में कॉर्पोरेट्स ने अपनी पसंद के विषयों पर फाउंडेशन चलाने शुरू कर दिए। इससे स्थानीय मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं के लिए वित्तीय मुश्किलें और बढ़ गईं। सरकार को इस पर भी गहराई से विचार और विश्लेषण करना चाहिए।”
भले ही जमीनी संस्थानों के पास अपनी कई चुनौतियां हैं लेकिन इनकी बेहतर समझ समाधान अथवा विकल्प तलाशने में भी मदद करती है। संस्थाएं चाहे तो अपने रास्ते खोज सकती है जिसमें ये विकल्प आपकी मदद कर सकते हैं –
संस्थाओं को आगे बढ़ने के लिए वित्तीय विविधता को बढ़ावा देते हुए धन जुटाना आवश्यक है। इसमें वे व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट साझेदारी और सरकारी अनुदान जैसे कई तरह के आर्थिक सहयोग को शामिल कर सकती हैं।
इसके साथ स्थायी फंडिंग की एक रणनीति विकसित करनी चाहिए और संभावित दानदाताओं के साथ संबंध बनाना चाहिए। सरफ़राज कहते हैं कि “आजकल धन देने वाले लोगों को डेटा पॉइंट, सटीक विषय बिंदु, मुद्दों पर स्पष्ट विश्लेषण चाहिए। इसके लिए हमें खुद को भी इस तरीके से तैयार रखना चाहिए।” अरुण जोड़ते हैं, “राजस्थान में कई संस्थाओं के विषयवार व्हाट्सप्प ग्रुप बने हुए हैं। जैसे – एसआर अभियान, बाल सरंक्षण अभियान यहां लोग अवसरों को साझा करते रहते है। इसके अलावा, एक सुनियोजित धन के रूप में समुदाय के साथ मिलकर भी आय के स्त्रोत तलाशे जा सकते हैं।”
सरफ़राज़ कहते हैं कि “अगर आपको अपने काम को बढ़ाना है तो ‘एकला चलो रे’ वाली अवधारणा को छोड़ना होगा। आपको अपनी लीडरशिप में युवाओं और मध्यम अनुभवी लोगों को मौका देना चाहिए और उन पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए।” इस पर आई-पार्टनर संस्था में लीडरशिप भूमिका में कार्यरत निशा कहती हैं, “संस्थाओं का किसी एक कुशल नेतृत्व से आगे बढ़ पाना मुश्किल है, इसके लिए और लोग चाहिए होंगे। हमारी संस्था ने अगली पीढ़ी की लीडरशिप को हाल ही में तैयार किया है। हालांकि यह थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। साथ ही, इस प्रक्रिया में बहुत भरोसे और सहनशीलता की आवश्यकता है।”
नेतृत्व विकसित करने के लिए आजकल को-लीड का भी प्रचलन है। संस्था प्रमुख अपने साथ एक साथी को जिम्मेदारियां सौंपते हुए सिखाने का तरीका भी अपना सकते हैं। अरुण इसमें जोड़ते हैं कि “नेतृत्व विकास की आवश्यकता हर स्तर पर है। जमीनी कार्यकर्ताओं को भी संस्थान में अपनी तरक्की का अनुभव होना चाहिए। संस्थाओं को उनके लिए ऊपरी स्तर तक पहुंचने के रास्ते स्पष्ट करने चाहिए। इसके अलावा, अन्य समाजसेवी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग करके भी इस कमी को पूरा किया जा सकता है।”
जमीनी संस्थाओं को यह समझना होगा कि अपने कार्य को बढ़ाने के लिए बेहतर संचार प्राथमिक कड़ी है। इसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग शुरू करना चाहिए। अब सोशल मीडिया और अन्य नेटवर्कों का उपयोग केवल समुदाय तक आपके कार्य को पहुंचाने या जागरूक करने तक सीमित नहीं रह गया है। ये दानदाताओं को आकर्षित करने, सोशल सेक्टर से जुड़े ग्रुप, चैनल, और अन्य संस्थाओं से नेटवर्किंग करने, आपकी तात्कालिक विषयों और आवश्यक अवसरों के बारे में जागरूक रखने का अवसर प्रदान करते हैं।
हालांकि अरुण कहते हैं, “वित्तीय जरूरतों के चलते अभी संस्थाओं के लिए वेबसाइट, ऐप जैसे माध्यमों पर आना आसान नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया माध्यमों पर निरंतर अपडेट रहने से शुरुआत की जा सकती है।”
एनजीओ को सरकारी नीतियों और कानूनी ढांचे की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि वे इन नियमों का पालन कर सकें और अपने कार्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें। इसके लिए वे पेशेवरों या नेटवर्क से मदद ले सकते हैं, जो उन्हें इन नीतियों की समझ में मदद करेंगे। सरफ़राज़ दोहराते हैं कि “इस सेक्टर में अच्छी बात यह है कि यहां हर विषय पर संस्थाएं काम करती हैं। बस आपको अपनी नेटवर्किंग बनानी है। कानूनी ढांचे पर भी काम करने वाले बहुत लोग हैं। जिस तरह आप लोगों की मदद कर रहे हैं, वे भी आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आपको बस उनसे जुड़ने की जरूरत है।”
कुल मिलाकर, जमीनी संस्थाओं को विस्तार करने में चुनौतियों को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इसके लिए रणनीतिक और खुला दृष्टिकोण, लगातार सीखना, सहयोग करना, नेतृत्व विकसित करना और अपने समुदायों के साथ मजबूत संबंध बनाना आदि उनके आगे बढ़ने में सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं।
—

मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले के राजाबाज़ार इलाके में रहती हूं। मुझे बचपन से ही फुटबॉल और क्रिकेट खेलने में बहुत रुचि थी। हालांकि सब इन्हें लड़कों वाले खेल मानते हैं लेकिन मैं 8-10 साल की उम्र से फुटबॉल खेल रही हूं।
हम यहां 5-6 सहेलियां है जिन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है। लेकिन हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना लगभग हर रोज ही करना पड़ता है। हममें से कुछ के परिवार वाले हमारे खेलने के ख़िलाफ़ थे। वहीं, जो भी मान गए उनकी शर्तें कुछ ऐसी थीं – अगर लड़कियां खेलेगी तो उन्हें पूरे कपड़े पहनने होंगे, वे बहुत देर तक घर से बाहर नहीं रह सकतीं हैं, वगैरह-वगैरह। ज्यादातर लड़कियों को ट्राउजर-स्लेक्स पहनकर फुटबाल खेलना पड़ता था। इसके अलावा, सबसे बड़ी शर्त घर के कामों की ज़िम्मेदारी निभाना है जो हम सभी करती हैं। और, फुटबॉल खेलने के साथ भी करती आईं हैं।
पहले मोहल्ले में लड़कियों के लिए अलग से ग्राउंड नहीं था। इसलिए हम लड़कों के साथ खेलते थे। लेकिन जल्दी ही इस पर आसपास के लोग बातें बनाने लगे कि “ये लड़कियां इतनी बड़ी हो गईं हैं और अभी भी ग्राउंड में खेलती हैं। फुटबॉल कोई लड़कियों वाला खेल नहीं है।” लोग हमारे घर वालों को भी ताना मारते थे कि वे हमें बाहर खेलने कैसे भेज सकते हैं?
दोस्त होने और एक जैसी समस्याओं का सामना करने से हम लड़कियों के बीच एक गहरी दोस्ती और समझ बन गई है। इसके कारण हम समस्याओं से निपटने में एक-दूसरे की मदद भी करते हैं। इसी वजह से हम लड़कियों ने अपने समुदाय में होने जा रहे एक बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई, उसके बाद हमें काफी विरोध झेलना पड़ा था। इस मामले को लोकल मीडिया ने भी कवर किया और उसे देखकर ही साल 2019 में आई-पार्टनर इंडिया की टीम आई। हमने उनसे गुजारिश की कि वे हमें प्रोफेशनल तरीके से फुटबॉल खेलना सिखाएं। संस्था ने पहले हमें लैंगिक, सेक्शुअल और प्रजनन स्वास्थ्य, और फुटबॉल के बारे में जानकारी दी। इसके बाद ‘वन टीम वन ड्रीम’ प्रोजेक्ट के तहत हमारी फुटबॉल टीम तैयार हुई।
मैं हमारे टीम की सबसे पुरानी खिलाड़ी हूं लेकिन हमारे कोच को घर पर अब भी बहुत समझना पड़ता है कि “आयशा अच्छा खेलती है, अगर सही कोचिंग मिलेगी तो वो टूर्नामेंट जीत सकती है। वो टाइम से घर आ जाया करेगी।” इसके बाद भी घरवाले तब राजी हुए जब मैंने उनसे कहा कि मैं घर का पूरा काम करके जाउंगी। मैं सुबह उठकर घर के काम में मम्मी की मदद करती हूं, खाना बनाती हूं और उसके बाद ही फुटबॉल खेलने जाती हूं।
शहर से बाहर मैच खेलने के लिए भी हम सहेलियां एक-दूसरे के काम में साथ देती है। वे मेरे कामों की ज़िम्मेदारी अपने सर ले लेती हैं, जैसे – खाना बनाना, सफाई करना वग़ैरह। जब तक मैं टूर्नामेंट से वापस नहीं आती, वे इसे पूरा करती हैं। मैं भी उनके लिए ऐसा करती हूं। लेकिन इन दिक्कतों के कारण कई लड़कियों ने फुटबॉल खेलना ही बंद कर दिया है।
हालांकि अब धीरे-धीरे कुछ बदलाव आ रहा है। फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए 60 से ज्यादा लड़कियां आती हैं। अब हमारी नई टीम, साउथ 24 परगाना जिले के मल्लिकपुर इलाके में है और हम सब भी सप्ताह में तीन बार वहीं खेलने जाते हैं। इसके अलावा हम रेसिडेंशियल फुटबॉल कैंप में भी प्रशिक्षण लेते हैं। घर के कामों के साथ हम 4-5 घंटे ही प्रैक्टिस कर पाते हैं। कोच कहते हैं कि अगर हमें नेशनल लेवल का खिलाड़ी बनना है तो रोजाना आठ घंटे की प्रैक्टिस जरूरी है। लेकिन परिवार वाले अभी भी इसके लिए राजी नहीं हैं।
आएशा परवीन कोलकाता में फुटबॉल खेलती हैं।
—
अधिक जानें: जानें कि सलूंबर की किशोरियों को शादी या खनन में से एक क्यों चुनना पड़ रहा है?
मैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच बाघ अभयारण्य (टाइगर रिजर्व) में सात साल से जंगल गाइड के रूप में काम कर रही हूं। मेरे पति भी अभयारण्य में सफ़ारी जीप ड्राइवर का काम करते हैं। जंगल गाइड की नौकरी में मुझे दिन में दो बार, सुबह 6 बजे और दोपहर 2.30 बजे की सफ़ारी के लिए तुरिया गेट पर रिपोर्ट करना होता है। तुरिया गेट, अभयारण्य के उन तीन गेटों में से एक है जो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में पड़ते हैं जबकि अभयारण्य का बाक़ी हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में आता है।
हर सफ़ारी के लिए हमेशा जरूरत से ज्यादा गाइड और जीप उपलब्ध रहती हैं। इसके लिए वन विभाग एक रात पहले ही सभी जीप के लिए रोस्टर बना देता है। इसमें स्पष्ट होता है कि किस दिन कौन से ड्राइवर का नंबर आएगा। एक बार जब सभी ड्राइवरों को उनका समय (स्लॉट) मिल जाता है तो उनकी जीप के लिए गाइड भी दे दिए जाते हैं। यह क्रमानुसार चलने वाला तरीका है। मान लीजिए कि अगर 1-10 नंबर की बारी सुबह आती है तो दोपहर में 11 नंबर से शुरुआत होगी। इसी तरह, अगली सुबह जिसका नंबर होगा उससे शुरुआत होगी।
एक पूरे सफारी चक्र में लगभग 30-35 जीप होती हैं। हालांकि सभी जीपों की सूची पहले से तैयार कर ली जाती है, लेकिन जब तक सफारी शुरू होने का सही समय नहीं आ जाता, तब तक यह सटीक रूप से अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि वास्तव में उसमें कितनी जीपों और गाइडों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, दोपहर की सफारी का समय तीन बजे है लेकिन मांग के अनुसार जीप शाम चार बजे तक चलती रहती हैं। इसलिए गाइड को शाम 4-4:15 बजे तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता कि कभी कोई ड्राइवर और गाइड किसी काम से कहीं बाहर या फिर बीमार होते हैं। ऐसे में, अगले वाले व्यक्ति का नंबर आगे बढ़ जाता है। यही वजह है कि ड्राइवर और गाइड को हमेशा स्टैंडबाय रखा जाता है।
गाइड प्रति सफारी 500 रुपए कमाते हैं। जब उन्हें टिप मिलती है तो यह उनकी अतिरिक्त आय होती है, इसलिए हम इस तरह का कोई मौक़ा नहीं खोना चाहते हैं। लेकिन अगर गाइड की ज़रुरत न हो तो उन्हें घर वापिस जाना पड़ता है। ऐसा अक्सर होता है। हम एक घंटे तक गेट पर खड़े रहकर देखते रहते हैं कि शायद लास्ट-मिनट बुकिंग के चलते किसी को गाइड या जीप की ज़रुरत पड़े।
सभी ड्राइवरों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो उन्हें रोस्टर की जानकारी देता है और बताता है किसी शिफ़्ट में कितने ड्राइवरों की जरूरत है। ज़्यादातर ड्राइवर तुरिया के पास ही रहते हैं, इसलिए उन्हें गेट तक पहुंचने में बहुत समय नहीं लगता है। लेकिन गाइड के लिए ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जिससे यह पता चल सके कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। वन विभाग भी उनके लिए कोई रोस्टर नहीं बनाता है। अगर वे ना जाएं और किसी गाइड की ज़रुरत पड़ जाए तो वे अपनी बारी और कमाई, दोनों खो देते हैं। वहीं, गेट तक जाकर ज़रूरत न होने की स्थिति में घर लौटने में समय और मेहनत दोनों बरबाद होते हैं, ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए जिन्हें घर के काम भी करने होते हैं।
अगर हमें इस बात का मोटा-मोटा अंदाजा मिल जाए कि किस शिफ्ट में कितने गाइड चाहिए, तो हमारा काम आसान हो सकता है। वन विभाग, कुछ समय का बुकिंग पैटर्न देखकर हमें एक संख्या बता सकता है। इस तरह गेट तक सिर्फ यह जानने के लिए आने-जाने में हमारा समय बरबाद नहीं होगा कि हमारे लिए कोई काम है या नहीं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
अधिक जाने: जानें कि ओडिशा की युवतियों के रोजगार की राह में क्या चुनौतियां हैं।

साल 2021 में, पूर्वी महाराष्ट्र में पड़ने वाले गांव बोरतोला और सांवरतोला की महिलाओं ने, मछली पालन के लिए ग्राम पंचायत से एक तालाब पट्टे (लीज़) पर लिया। हममें से ज्यादातर महिलाएं धीवर समाज से आती हैं जहां पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने का काम पुरुष ही करते आए हैं। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान, जब हमें ईंट-भट्ठे पर काम करने के लिए गांव छोड़ना पड़ा तो हमने भी आजीविका के लिए मछली पालन करने के बारे में सोचा।
बोरतोला का तालाब 4-5 सालों से सूखा पड़ा था। बीच में समुदाय के पुरुषों ने वहां मछली पालन की कोशिश की थी पर सफल नहीं हुए। लेकिन जब हमने यह काम हाथ में लिया तो तालाब में बेहतरी दिखने लगी। हर किसी को आश्चर्य हो रहा था कि हमने यह कैसे किया। तालाब पुनर्जीवन इसका जवाब है।
जब हमने अपना काम शुरू किया तो फाउंडेशन फॉर इकनॉमिक एंड इकलॉजिकल डेवलपमेंट (फ़ीड) संगठन ने हमें तालाब की जैव विविधता को बनाए रखने का महत्व समझाया और हमें बताया कि इसे कैसे दोबारा जीवित किया जा सकता है। उस समय तालाब में कंटीली झाड़ियों और खरपतवार का क़ब्ज़ा था और हमें तालाब में पानी भरने से पहले इन्हें साफ़ करना था। इसके लिए हमने तालाब की तलहटी को ट्रैक्टर से जुतवाया और जलीय पौधे लगाए जिससे मछलियों को भोजन मिल सके और एक स्वस्थ तालाब तंत्र (इकोसिस्टम) तैयार हो सके। हमने खाद के लिए ज़मीन में गाय का गोबर, सुपरफास्फेट्स और यूरिया वग़ैरह भी मिलाया। इस तरह हमने मछली पालन के लिए तालाब तैयार किया।
जब बारिश हुई तो तालाब के पानी का रंग मटमैले भूरे से हरा (पानी पर तैरने वाले जलीय सूक्ष्मजीव, प्लैंकटन के कारण) हो गया। इससे हमें पता चला कि अब मछली के बीज डालने का समय आ गया है। हमने प्रमुख भारतीय क़िस्में रोहू, काला और मृगल जैसी मछलियों का पालन शुरू किया।
मछलियों को खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी महिलाओं ने आपस में बांटी। हम उन्हें धान की भूसी के गोले और सरसों की खली खिलाते थे। हमारे दिए भोजन के अलावा, तालाब में मौजूद वनस्पतियों से मछलियों ने पोषण हासिल किया और बढ़ने लगीं। इतना ही नहीं बारिश के पानी के साथ देसी प्रजाति की कुछ ऐसी वनस्पतियां भी तालाब में पहुंची जो मछलियों के लिए फ़ायदेमंद थीं। इसी के साथ हमने तालाब में मछलियों की नई प्रजातियां भी देखीं।
तालाब की सेहत बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि एक मानक जल स्तर बना रहे। शुरूआत में, किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए तालाब से पानी लेते थे जिसके कारण जल स्तर गिरने लगा। इसके लिए, हमने पंचायत से बातचीत की और कुछ नियम तय किए जो बताते हैं कि किसान कितना पानी ले सकते हैं।
इस बीच, मछलियां बड़ी होने लगीं। यह परखने के लिए कि क्या मछलियां ठीक से बढ़ रही हैं या नहीं, या कहीं उन्हें और पोषक तत्वों की ज़रूरत तो नहीं हैं, हम हर हफ़्ते कुछ मछलियां पकड़ते हैं और उनका वजन करते हैं। अगर उनका वजन कम होता है तो हम पानी में और पोषक तत्व मिलाते हैं। पहले साल एक वयस्क मछली का वजन 500 ग्राम अधिक था। तालाब की अच्छी देखभाल के चलते दूसरे साल यह 2 किलोग्राम और तीसरे साल 3 किलोग्राम तक हो गया। फ़ीड संस्था के लोगों और समुदाय के पुरुषों ने हमें मछली पकड़ना सिखाया। पहले हम डर रहे थे क्योंकि मछली पकड़ने का मतलब था, सीने तक भरे पानी में उतरना और हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। लेकिन हम जल्दी ही सीख गए।
हम बारी-बारी से अपने तालाब की रखवाली भी करते थे क्योंकि लोग बढ़ती हुई मछलियों को चुरा लेते हैं या जानवर भी उन्हें खा जाते हैं। इसलिए, क़रीब तीन महीने तक रात 9 बजे से रात 1 बजे तक टॉर्च और डंडा लेकर जाते थे और तालाब के किनारे बैठते थे। ऐसा तब तक चला जब तक मछलियां बेचने लायक़ नहीं हो गईं।
हम अपने समूह को सरस महिला मत्स्य उत्पादन टीम कहते हैं। जब हमने पहली बार तालाब के पट्टे के लिए ग्राम पंचायत से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, ‘महिलाएं मछली कैसे पकड़ सकती हैं?’ उन्होंने यहां तक कहा कि अगर हम तालाबों में उतरे तो पानी खराब हो जाएगा। लेकिन हम अपनी बात पर अड़े रहे और तीन साल की लीज़ हासिल की। अब हम इसे पांच साल तक बढ़ाना चाहते हैं। हमने तालाब को फिर से जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत की है और चिंता है कि अगर इसे दूसरों को सौंपा गया तो वे इसे खराब कर सकते हैं। तब हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
अधिक जानें: जानें, स्पीति घाटी में स्थानीय सिंचाई प्रणाली की महिला प्रबंधकों के बारे में।




असम में जनवरी के महीने में, फसल कटाई के मौसम के आखिरी दिन को माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है, जिसे भोगली बिहू भी कहा जाता है। इस मौके पर, समुदाय के लोग साथ में मिलकर अच्छी उपज का जश्न मनाते हैं। इस दौरान असम के बरपेटा जिले के एरारतारी गांव में कुछ अनूठी परंपराएं भी निभाई जाती हैं।
त्यौहार की शुरुआत उरूका के साथ होती है, जो माघ बिहू की एक शाम पहले मनाया जाता है। इस रात, पूरा गांव एक आग के अलाव के चारों ओर इकट्ठा होता है और भव्य भोज का आनंद लेता है, जिसे भुज कहते हैं। समुदाय के भोज के लिए बांस, सूखे पत्तों और घास से बने भेलाघर या मेजी बनाई जाती है। भेलाघर एक तरह का अस्थायी ढांचा होता है, जिसमें बैठकर समुदाय के लोग बैठकर भोजन करते हैं। फिर अगली सुबह होते ही इन भेलाघरों को अच्छे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए अग्नि देवता की प्रतीकात्मक प्रार्थना करते हुए जलाया जाता है।
माघ बिहू एकता और उत्सव का समय होता है, और एरारतारी के लोग इस त्यौहार में शांति और सौहार्द की भावना को शामिल कर इसे मनाते हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए पूरे वर्ष, परिवार के बुजुर्ग पुरुषों पर परिवार में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन त्यौहार के दौरान, वे यह जिम्मेदारी युवा पीढ़ी को सौंप देते हैं, जिनका काम एरारतारी के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का होता है। यह इस क्षेत्र की सदियों पुरानी परंपरा है! माघ बिहू के दौरान, आमतौर पर 20 साल की उम्र के युवाओं पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है जिसमें वे अपने समुदाय के बीच होने वाले झगड़ों को सुलझाने का काम करते हैं।
ये झगड़े आमतौर पर छोटी-मोटी बहसबाजी या गलतफहमियों के कारण हो जाते हैं। एरारतारी के निवासी राजीव दास कहते हैं, “एक बार, कोई अपने पड़ोसी से थोड़ी चीनी उधार लेना चाहता था। जब पड़ोसी उन्हें चीनी नहीं दे पाया, तो वह व्यक्ति नाराज़ हो गया। दूसरी बार, एक परिवार के परिसर में लगे पेड़ की एक बड़ी शाखा दूसरे परिवार के घर में गिर गई। इससे बरामदा टूट गया गया, जिससे उनमें झगड़ा हो गया। इस तरह की छोटी-मोटी बेवकूफी भरी बहसबाजी उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी में होती रहती है।”
भुज के बाद, जब रात को सब लोग सो जाते हैं, तो वहां के लड़के भेलाघर से बाहर निकलकर चुपचाप उन घरों में छोटे-छोटे सामान जैसे चप्पल और बर्तन आपस में बदल देते हैं जिनके मालिकों के बीच झगड़ा चल रहा होता है। अगले दिन, घरों में सामान की गुमशुदगी के कारण अफरा-तफरी और हंसी का माहौल बन जाता है , क्योंकि लोग अपने खोए हुए सामान की तलाश कर रहे होते हैं। ये सारी गतिविधियां इसलिए की जाती हैं ताकि लोग आपस के विवादों को भुलाकर फिर से बातचीत शुरू कर पाएं।
ऐसा ही मामला दो परिवारों के आठ साल के दो लड़कों के बीच हुए झगड़े से जुड़ा है। झगड़े की वजह से उनके माता-पिता ने एक-दूसरे पर बच्चे की खराब परवरिश का आरोप लगाया। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों बच्चों के परिजनों ने लगभग चार महीने तक एक-दूसरे से बात नहीं की। उरुका की रात, युवाओं ने दोनों परिवारों की एक कुर्सी और एक चावल मिल की अदला-बदली कर दी। अगली सुबह, उन्हें किसी से मालूम चल गया कि उनका सामान कहां हैं। इसके लिए जब दोनों माता-पिता आपस में मिले और इस लड़ाई पर खूब हंसे, एक दूसरे से माफ़ी मांगी और जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। एरारतारी के निवासी दीप दास कहते हैं, “छोटे-मोटे विवादों को सुलझाना और लोगों के बीच सामंजस्य बढ़ाना अच्छा लगता है।”
करीना बोरदोलोई, प्रोजेक्ट डीईएफवाई में डिजास्टर प्रिपेयर्ड कम्युनिटी स्पेसेज़ (डीआईएसपीईसीएस) कार्यक्रम की प्रोग्राम एसोसिएट हैं।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
—
अधिक जानें: राजस्थान का एक इलाका, जहां बेटियां घोड़ी चढ़ रही हैं।
अधिक करें: लेखक के काम के बारे में विस्तार से जानने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।