
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ने वाली टिब्बी नगर पालिका के लोगों के लिए हरदम बहते नालों और उनकी बदबू से जूझना कोई नई बात नहीं है। यह समस्या 2022 में भी ऐसी ही थी, जब टिब्बी एक ग्राम पंचायत हुआ करती थी और आज इसके नगर पालिका बनने के दो साल बाद भी यह समस्या बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है।
वार्ड नंबर 12 में रहने वाले प्रभुलाल बताते हैं कि यह गंदा पानी बगैर किसी उचित उपचार के तालाबों में पहुंचता है जिसके कारण हमारे जलस्रोतों के पानी से भी दुर्गंध आने लगी है। वे बताते हैं कि “यहां जल निकासी के लिए कोई ठोस व्यवस्था करने की जरूरत है।” वार्ड 12 के एक अन्य निवासी बलवंत राम कहते हैं कि “यहां कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता है।”
टिब्बी में पीने के पानी के रूप में फ्लोराइड की उच्च मात्रा वाला भूजल उपलब्ध कराया जाता है। लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से नहर का पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
टिब्बी अब एक चौराहे पर खड़ा है, नगर पालिका के रूप में अपग्रेड के बाद न तो यह गांव रह गया है और न ही शहर हो पाया है। आज भी, नगर पालिका कार्यालय में स्वीकृत अधिकांश पद खाली हैं जिससे यहां का काम प्रभावित होता है।
टिब्बी नगर पालिका की अध्यक्ष संतोष सुथार कहती हैं, “अगर [राज्य] सरकार स्वीकृत पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेती तो नगर पालिका सुचारू रूप से काम कर सकती थी। ऐसे में जब अधिकारी और कर्मचारी मौजूद ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा?” जब राज्य सरकार ने 20 मई, 2022 को इसे नगर पालिका में अपग्रेड करने की अधिसूचना जारी की थी, तब वे टिब्बी की सरपंच थीं।
जब पंचायत कार्यालय में नगर पालिका कार्यालय स्थापित किया गया तो सरपंच को नगर पालिका अध्यक्ष, उप सरपंच को नगर पालिका उपाध्यक्ष, और 23 पंचायत सदस्यों को पार्षद बना दिया गया।
कई अन्य सरकारी पद बनाए गए लेकिन शायद ही कभी भरे गए। सहायक राजस्व निरीक्षक की अनुपस्थिति में, नगर पालिका के लिए राजस्व उत्पन्न करना भी एक समस्या है। इसी तरह, जूनियर अकाउंटेंट की अनुपस्थिति में उचित हिसाब-किताब रखना मुश्किल हो गया है जबकि स्वास्थ्य निरीक्षक का पद खाली होने के कारण सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। नगर पालिका के पास कोई स्थायी सफाई कर्मचारी नहीं है; सफाई का सारा काम आउटसोर्स किया जाता है।
राजस्थान के स्थानीय स्वशासन विभाग ने हाल ही में सफाई कर्मचारियों के 24,797 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, लेकिन इस प्रक्रिया में नौकरशाही की लेट लतीफी की वजह से टिब्बी जैसी नई नगर पालिकाएं इसमें शामिल नहीं होंगी।
टिब्बी नगर पालिका के पार्षद राममूर्ति खन्ना कहते हैं, “नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों के लिए आवश्यक संसाधनों के उपयोग के लिए उचित व्यवस्था होना ज़रूरी है, लेकिन टिब्बी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। राज्य सरकार ने वाहवाही बटोरने के लिए कई नगर पालिकाएं बनाईं, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ़ मुड़कर नहीं देखा।”
प्रशासनिक गतिरोध के कारण, स्थानीय निवासियों को लगता है कि टिब्बी की स्थिति नगर पालिका की अपेक्षा ग्राम पंचायत के रूप में बेहतर थी।
अमरपाल सिंह वर्मा राजस्थान स्थित स्वतंत्र पत्रकार हैं। यह लेख 101 रिपोर्टर्स पर मूल रूप से प्रकाशित लेख का संपादित अंश है।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
अधिक जानें: जानें कि क्यों भोपाल में झुग्गीवासी आज भी पीएम आवास योजना का इंतज़ार कर रहे हैं?
अधिक करें: लेखक के काम को जानने और उन्हें अपना सहयोग देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में रेलवे और जिला प्रशासन ने 22 दिसंबर 2022 को संयुक्त कार्रवाई करते हुए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के समीप रेलवे की भूमि पर बने 250 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला कर तोड़ दिया था। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद आज भी यहां रह रहे 153 परिवारों को विस्थापित नहीं किया गया है। इस कारण जिले के अन्नूनगर और श्रीराम नगर के लोग ठंड, बारिश और गर्मी में अपने मकानों के मलबे पर तिरपाल बांध कर रहने को मजबूर हैं। शेष परिवार यहां से पलायन कर शहर के दूसरे हिस्सों में चले गए हैं।
गैस पीड़ितों की समस्याओं पर काम कर रहीं भोपाल ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एंड एक्शन की संचालक रचना ढिंगरा ने बताया की अन्नूनगर और श्रीराम नगर गैस और पानी पीड़ित रहवासियों की बस्ती है। गैस पीड़ित उन्हें माना जाता है जो साल 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली जहरीली हवा में सांस लेने के कारण पीड़ित हुए थे। पानी पीड़ित उन्हें माना जाता है जो भोपाल गैस त्रासदी के कई सालों बाद तक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर की जमीन में दफन, जहरीले कचरे और फैक्ट्री के समीप बने तालाब के दूषित पानी का इस्तेमाल करने के कारण पीड़ित हुए हैं।
अन्नूनगर में रहने वाले रफीक कहते हैं, “14 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हमें जमीन नहीं मिली। जब हमारा मकान तोड़ा जा रहा था, तब प्रशासन ने कहा था कि हमें मकान बनाने के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। नगर निगम के कर्मचारियों ने हमें ये भी बताया की अगर हम पीएम आवास योजना के तहत किश्तों में दो लाख रुपये देंगे तो हमें योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिल जाएगा। उस वक्त तहसीलदार ने हमें टोकन नंबर दिया था और कहां था कि दो-चार दिन में जगह बता देंगे, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक हमारे नंबर का कोई अता-पता नहीं है। परिवार में मेरी पत्नी तीन बच्चे और मां हैं। एक साल से हम यहीं तिरपाल बांध कर रह रहे हैं। टोकन लेकर कई बार तहसील गए, मगर अब कोई कुछ नहीं बता रहा।”
इन बस्तियों में ज़्यादातर मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग रहते हैं। पिछले एक साल से यहां लोग बिना बिजली, शौचालय और अन्य संसाधनों के अपने परिवार का पालन कर रहे हैं।
अन्नूनगर की एक और निवासी नजमा कहती हैं, “जब हमारे घर तोड़े जा रहे थे, तब हम चिल्लाते रह गए लेकिन किसी ने नहीं सुना। हमने तिरपाल और कपड़े बांधकर छत बना लिए है, लेकिन जब थोड़ी सी तेज हवा चलती है तो डर लगता है। तेज आंधी में कई घरों के टीन और तिरपाल उड़ जाते हैं। लेकिन हमारी परेशानी को ये अफसर क्या समझेंगे।”
अन्नू नगर में रहने वाले नजब खां ने बताया, “हम सभी परिवार यहां पिछले 30 सालों से रह रहे हैं लेकिन बावजूद इसके अब सभी के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट नहीं डाल सके। पहले तो प्रशासन ने हमें बेघर कर दिया और बाद में हमारा वोट डालने का अधिकार भी हमसे छीन लिया।”
गैस पीड़ित संगठनों ने जनवरी में जिला कलेक्टरेट पहुंचकर 153 परिवारों को विस्थापित किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। उस समय वहां पीड़ित परिवारों की सूची भी सौंपी गई थी। भोपाल जिला कलेक्टर ने पीड़ितों को आश्वासन दिया था कि इन्हें पीएम आवास एवं अन्य जगह पर विस्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक एक भी परिवार को जगह नहीं मिल पाई है।
अंकित पचौरी, द मूकनायक की संपादकीय टीम का हिस्सा हैं।
यह एक लेख का संपादित अंश है जो मूलरूप से द मूकनायक पर प्रकाशित हुआ था।
—
अधिक जाने: जानें भोपाल में झुग्गीवासी आज भी पीएम आवास योजना का इंतज़ार कर रहे हैं।
अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना सहयोग देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।
प्रदीप साना (45) अपने 20 मछुआरे दोस्तों के साथ, हर साल गर्मियों में उत्तराखंड के नानकसागर बांध के पास सूखी जमीन पर मछली पकड़ने के लिए नानकमत्ता आते हैं। प्रदीप कहते हैं – “मैं अपने घर से 30 किलोमीटर दूर सिर्फ़ मछली पकड़ने आया हूँ। यहां बहुत सारे मच्छरों के बीच और बिना रोशनी या बिजली के रहना बहुत मुश्किल है। हमें रात में रोशनी के लिए अपनी बाइक की बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ता है।”
वे अपनी अस्थाई झोंपड़ियां बनाने के लिए, बांध के आस-पास से बांस, लकड़ी और पुआल इकट्ठा करते हैं। इसे बनाने में उन्हें सिर्फ़ एक दिन लगता है, लेकिन ये झोपड़ियां तेज़ हवा और बारिश से सुरक्षित नहीं रहती हैं।

प्रवासी मछुआरे ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए, विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं – जलाशयों में बड़े जाल लगाने से लेकर, उन क्षेत्रों में बांध बनाने तक जहां पानी की गति तेज़ होती है, जो छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए उपयोगी होती है।

मछली पकड़ने में मदद के लिए यांत्रिक उपकरणों का उपयोग सबसे प्रभावी है। जनरेटर के साथ, एक तरफ पानी छोड़ा जाता है, जिससे मछलियां रह गए कीचड़ में फंस जाती हैं और इसलिए उन्हें पकड़ना ज्यादा आसान होता है। इससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मछलियां पकड़ने और ज्यादा कमाई करने में मदद मिलती है।

प्रदीप कहते हैं – “हमारा जीवन संघर्ष से भरा है। यहां आते ही, हमें जनरेटर, ईंधन, जाल और अन्य जरूरी चीजों पर 70-80 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और फिर हमारा ठेकेदार कभी-कभी 10 से 15 दिन बाद तक भुगतान नहीं करता है।”

मौसमी मछली पकड़ने के इस काम में जीवन कठिन है। लेकिन पुरुषों को रोमांच और उपलब्धि का अहसास भी होता है, क्योंकि वे अपने परिवार के लिए आजीविका कमाते हैं। प्रदीप कहते हैं – “मछलियां हर जगह हैं, लेकिन नानकमत्ता में हमें जो मज़ा आता है, वह कुछ और ही है।”
यह लेख मूलरूप से विलेज स्क्वायर पर प्रकाशित हुआ था।
आप एक बड़ी मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ फंडर से हाथ मिलाते हैं (लेकिन अंदर से आप बहुत घबराए हुए हैं)।
सिद्धू: कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें।
जब हर कोई चाय का इंतजार कर रहा होता है, तब आपका सीईओ फंडर की तारीफ के पुल बांध देता है।
सिद्धू: एक के बाद एक, ये लाएं हैं तौहफ़े अनेक।
आप ये बात शुरू करने के लिए सही मौका ढूंढ रहे हैं कि इस साल के लिए आपके संगठन के लक्ष्य इस फाउंडेशन के साथ कैसे पूरी तरह मेल खाते हैं।
सिद्धू: पिछले पैर पर रहते हैं और सही मौके का इंतज़ार करते हैं।
प्रेजेंटेशन के अंत में कमरे में मौजूद सभी लोगों को एहसास होता है कि जिस अनुदान के लिए आप आए हैं, वह आपके संगठन की ज़रूरतों को बस नाम के लिए ही पूरा करेगा।
सिद्धू: आसमान फटेगा तो दर्जी कहां तक सीएगा?
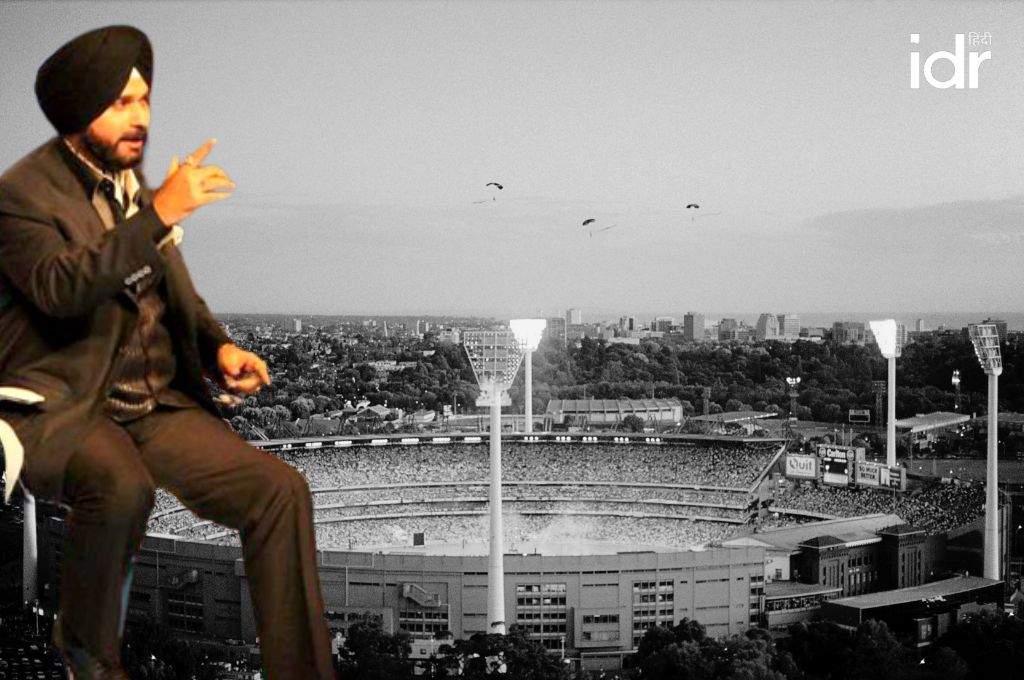
लेकिन आपके पास अपने कार्यक्रम के प्रभाव और समुदाय द्वारा उसके समर्थन से जुड़ी ढेरों कहानियां हैं। निश्चित ही वो काम करेंगी?
सिद्धू: ऐसी आग के सामने तो लोहा भी पिघल जाता है।
हालांकि फाउंडेशन टीम में से किसी ने भी अभी तक कोई सकारात्मक शब्द नहीं कहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सबका समर्थन मिल जाएगा।
सिद्धू: हार के जबड़े से हाथ डालकर निकाल लाये वर्ल्ड कप।
फाउंडेशन के प्रमुख आपसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि अनुदान आ जाएगा, और अगले सप्ताह कागजी कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
सिद्धू: है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो, मौसम बदलना चाहिए।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
ज़मीनी कार्यकर्ता, भारत के गैर-सरकारी संगठनों की रीढ़ की तरह हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा साल 2012 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सिविल सोसाइटी संगठन 27 लाख से ज़्यादा नौकरियां और 34 लाख फुल-टाइम वॉलंटीयर देते हैं। इनमें से ज़्यादातर देशभर में ज़मीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं।
भारत में ज़मीनी कार्यकर्ता कई तरह की परिस्थितियों में काम करते हैं। मसलन, घने शहरी इलाकों से लेकर उन ग्रामीण क्षेत्रों तक, जहां सेवाओं की पहुंच न के बराबर होती है। एक बड़ी संख्या में ज़मीनी कार्यकर्ता, अपनी संस्थाओं की तरफ से समुदाय को समझने और उनके साथ जुड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा उनका काम स्थानीय सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाने का भी रहता है। ये ज़मीनी कार्यकर्ता अपनी संस्था और बाहरी हितधारकों को ज़मीनी हालात की जानकारी देते हैं। यही नहीं, समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों से भी ज़मीनी कार्यकर्ता ही सबसे पहले रूबरू होते हैं।
विकास सेक्टर में ज़मीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद अहम है लेकिन उनकी चुनौतियों पर अक्सर कम ही बात होती है। यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि विकास सेक्टर में काम करने वाले इन ज़मीनी कार्यकर्ताओं की प्रभावशीलता और क्षमताओं को सामने लाने के लिए क्या किया जा सकता है? वे कौन से उपाय हैं जिनसे उनके काम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
ज़मीनी कार्यकर्ताओं के काम और उनकी चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने 40 ज़मीनी कार्यकर्ताओं पर केंद्रित ‘ज़मीनी कार्यकर्ताओं के काम की स्थिति’ बताने वाला एक अध्ययन किया। इसके अलावा इस लेख को तैयार करने के लिए सात अन्य कार्यकर्ताओं के साथ इंटरव्यू भी किए। इसके पीछे हमारी कोशिश थी कि हम उनके नज़रिये और समाधानों को विस्तार से समझ सकें।
अध्ययन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों से आने वाले और शिक्षा, आजीविका और ग्रामीण विकास जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले ज़मीनी कार्यकर्ता शामिल हैं। इस अध्ययन के 43 प्रतिशत ज़मीनी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर की (3 से ज़्यादा राज्यों में सक्रिय) संस्थाओं और 57 प्रतिशत कार्यकर्ता क्षेत्रीय संस्थाओं से जुड़े थे। इनमें से कई ज़मीनी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर की ऐसी बड़ी संस्थाओं का हिस्सा हैं जिनमें 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। हमने जिन ज़मीनी कार्यकर्ताओं का सर्वेक्षण किया, उनमें से ज़्यादातर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अपने से नीचे लोगों को मैनेज करते हैं। यहां तक कि इनमें से 33 प्रतिशत कार्यकर्ता 20 से ज़्यादा लोगों को मैनेज करते हैं।
इस लेख में दी गई जानकारी को हमने अध्ययन के परिणाम और विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख लोगों के साथ हमारी बातचीत से निकाला है।
इस अध्ययन में ज़मीनी कार्यकर्ताओं की छह प्रमुख चुनौतियां निकलकर सामने आईं हैं। अगर उनका समाधान किया जाए तो न केवल कार्यकर्ताओं की क्षमता में आवश्यक बढ़ोत्तरी हो सकती है बल्कि इससे समुदाय पर भी उनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
1. रिपोर्टिंग का बोझ बहुत ज़्यादा है
विकास सेक्टर में डेटा-आधारित रिपोर्टिंग की ज़रूरतों का प्रचलन बढ़ गया है। इसमें फ़ंडर रिपोर्टिंग, निगरानी और मूल्यांकन संबंधी रिपोर्टिंग, नियमित प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग और संचार के लिए भी रिपोर्टिंग का प्रचलन बढ़ गया है। इसका सीधा असर ज़मीनी कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हुए कामकाज के बोझ के रूप में दिखता है। अलवर जिले में आजीविका, पशुपालन और शिक्षा और अधिकारों पर काम करने वाले आनंद ने बताया, “मुझे अपने संगठन में रोज़ाना फ़ील्ड डेटा का प्रबंधन करना पड़ता है। डेटा से जुड़े लगभग 30-32 फ़ॉर्मेट हैं जिन्हें मुझे हर महीने भरना पड़ता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करता हूं। अगर मेरी सहायता के लिए अतिरिक्त लोगों को नियुक्त किया जाए तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा।” सर्वेक्षण में शामिल लगभग आधे (45 प्रतिशत) लोगों ने बताया कि रिपोर्टिंग का कोई एक कॉमन फ़ॉर्मेट नहीं है जिससे मालूम नहीं चलता कि किसी काम को कैसे करना है और उसमें बहुत सारा समय चला जाता है।
हमने जिन कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया, उन्होंने यह भी बताया कि रिपोर्टिंग में कई बार ज्यादा समय लग जाता है जिस वजह से फील्ड का काम प्रभावित होता है
एक प्रमुख गैर-लाभकारी संस्था के लिए काम करने वाले ज़मीनी कार्यकर्ता ने बताया कि उनके पास रिपोर्ट लिखने का कोई तय फ़ॉर्मेट नहीं है, इसलिए हर कार्यकर्ता अपने-अपने तरीके से रिपोर्ट भरता है। हमने जिन कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया, उन्होंने यह भी बताया कि रिपोर्टिंग में कई बार ज्यादा समय लग जाता है जिस वजह से फील्ड का काम प्रभावित होता है। 50 प्रतिशत ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने बताया कि रिपोर्ट लिखने में अपेक्षा से अधिक समय लगता है जिससे उनके लिए समय को मैनेज करना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।
2. काम से जुड़ी कुशलताओं में कमी को पहचानना
अध्ययन में पाया गया कि अलग-अलग सेक्टर से आने वाले ज़मीनी कार्यकर्ताओं को उनके दैनिक कार्यों की क्षमता बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट लिखने का काम बेहतर करना है, 68 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें अपने काम से जुड़ी कुशलताएं और सीखनी हैं, वहीं 63 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें अंग्रेजी सीखने में मदद की ज़रूरत महसूस होती है। उदाहरण के लिए, प्रवासी श्रमिकों के क्षेत्र में काम करने वाले बुंदेलखंड जिले के गोकुल ने कहा, “स्थानीय समुदाय में मेरा काम हिंदी भाषा में होता है जिसका उपयोग पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। लेकिन जब मुझे अपने मैनेजर को अपने काम की रिपोर्ट देनी होती है तो मुझे मेरे निष्कर्षों का अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ता है। मैं इसके लिए गूगल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता हूं लेकिन इसके कारण कई गलतियां हो जाती हैं, जो मेरे लिए एक बड़ी समस्या है।”

3. मैनेजर से पर्याप्त सहयोग न मिलना
महिला सशक्तिकरण और आजीविका क्षेत्र में काम करने वाली नेहा बताती हैं, “हमारे मैनेजर अक्सर ज़मीनी वास्तविकताओं के बारे में नहीं समझ पाते। वे हमारे रोजमर्रा के कार्यों को मैनेज करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं करते हैं। अक्सर जब हम उन्हें कोई सुझाव देते हैं तो भी वे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, भले ही वे सुझावों से सहमत भी हों।” नेहा की तरह, 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि उनके मैनेजर, ज़मीनी स्तर पर उनकी चुनौतियों को नहीं समझते हैं। हमारे इंटरव्यू के दौरान हमें ज़मीनी कार्यकर्ता और उनके मैनेजर के बीच पद क्रम की व्यवस्था भी बहुत स्पष्ट देखने को मिली। ज़मीनी कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर मैनेजर समझते भी हैं तो भी उनकी चुनौतियों पर न के बराबर ही कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के लिए बिहार की सोनी ने बताया, “हमारा ज़्यादातर काम समुदाय में होता है और तय समय रखने के बाद भी इन कामों में अक्सर अधिक समय लग जाता है। समुदाय के लिए हमारे काम की प्राथमिकता उनके अपने कामों के बाद होती है। इसलिए कई बार हमें एक घंटे के काम में चार घंटे भी लग जाते हैं। मगर इस वास्तविकता को मैनेजर नहीं समझ पाते हैं।”
4. स्थानीय सरकारी हितधारकों से समय ना मिलना
सरकारी हितधारकों के साथ काम करने में कितना समय लगेगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। यह अनिश्चितता अधिकांश ज़मीनी कार्यकर्ताओं के दैनिक कार्यों में जुड़ी होती है और अक्सर उनकी कार्य-योजनाओं और जवाबदेही मानकों में इसका हिसाब नहीं होता है। 58 प्रतिशत ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने में अपेक्षा से ज़्यादा समय लगता है।
58 प्रतिशत ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने में अपेक्षा से ज़्यादा समय लगता है।
कार्यकर्ताओं को केवल मीटिंग तय करने में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है और अक्सर मीटिंग शुरू होने के लिए घंटों इंतज़ार भी करना पड़ता है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब वे अधिकारियों के साथ अपनी निर्धारित मीटिंग में पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि मीटिंग रद्द हो गई है। शिक्षा पर काम कर रहे राजगढ़ जिले के राहुल ने बताते हैं कि, “अक्सर, अधिकारियों से मीटिंग तय करने और मीटिंग शुरू होने का इंतज़ार करने में बहुत समय निकल जाता है। इस वजह से अक्सर दूसरे काम छूट जाते हैं।’
अध्ययन में कार्यकर्ताओं ने अपने काम में सरकारी हितधारकों के साथ अधिक समन्वय को लेकर भी बात की है। एक ज़मीनी कार्यकर्ता ने बताया कि अलग-अलग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाइज़रों और सीडीपीओ के साथ काम करते हुए उन्हें रोज़ाना 80 से ज़्यादा एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुपों को मैनेज करना पड़ता है।
इसलिए, हालांकि बाहरी प्रभाव और इकोसिस्टम को बदलने को लेकर शायद उतना कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन संस्थाओं द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के काम से जुड़ी परिस्थितियों को स्वीकार करना और ज़मीनी संभावनाओं को समझना ही समाधान की ओर पहला कदम बन सकता है।
5. समुदायों के साथ नियमित जुड़े रहने के लिए समय का अभाव
जैसे-जैसे डेवलपमेंट इकोसिस्टम में बड़े स्केल पर काम करने पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है, अब इसका प्रभाव स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव को प्रभावित कर रहा है। उदयपुर, राजस्थान में आजीविका के मुद्दे पर काम करने वाले अमित कुमार बताते हैं कि “कुछ साल पहले की तुलना में अब हमें अधिक गांवों और लोगों को कवर करना होता है। ज्यादा सैम्पल बढ़ने से अब हमें उसी समुदाय के सदस्यों से दोबारा मिलने में महीनों लग सकते हैं। परिणामस्वरूप, पहले की तुलना में अब हमारे लिए उनके साथ रिश्ता बनाए रखना संभव नहीं रह गया है।”
ज़मीनी कार्यकर्ताओं के अनुसार समुदायों की अपेक्षाएं भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। उनके पास अब तकनीक के ज़रिये मिलने वाली सूचनाओं और ज़मीनी स्तर पर सरकार की बढ़ती पहुंच ने भी ज़मीनी कार्यकर्ताओं के लिए अपनी मौजूदगी और ज़रूरत को साबित करना मुश्किल बना दिया है।
6. नौकरी में असुरक्षा और अनिश्चित वेतन
इस अध्ययन में शामिल 35 प्रतिशत कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें उनके काम में निश्चित वेतन नहीं मिलता है। यहां तक कि 37 प्रतिशत कार्यकर्ताओं ने नौकरी में असुरक्षा महसूस करने की बात भी मानी है। उन्हें डर है कि एक साल से भी कम के समय में उनकी नौकरी जा सकती है। विकलांगता और लैंगिक मुद्दों पर काम करने वाले, बड़वानी के अमित कहते हैं, “संस्था में मेरा मासिक वेतन 15,000 रुपये है। लेकिन मुझे अपना पूरा वेतन पाने के लिए हर महीने संगठन में काम से जुड़े लक्ष्य हासिल करने होते हैं। ये लक्ष्य हासिल करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इस वजह से, मुझे आमतौर पर लगभग 12,000 रुपये ही वेतन मिल पाता है।” कई ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें संस्था की लगातार बदलती प्राथमिकताओं की वजह से अपनी नौकरी गंवाने का डर है। इस अध्ययन में कुछ ज़मीनी कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो अकेले परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। ऐसे में उनकी नौकरी जाना उनकी आजीविका के लिए बहुत बड़ा जोखिम होगा।

1. अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज को पहचानें
संस्थाओं को ऐसे सिस्टम तैयार करना चाहिए, जहां वे अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति को समझ सकें। उन्हें इस तरह से सक्षम बना पाएं कि वो बिना डरे खुलकर अपने अनुभव साझा कर सकें। एक बार संस्था के तौर पर जब आप अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं की ताकत और कमियों का जान लेंगे तो उनके काम को बेहतर मैनेज कर पाएंगे। साथ ही, समुदाय के साथ उनके संबंधों की स्थिति को समझना भी आपके लिए बेहतर समाधान खोजने में मददगार होगा।
2. चुनौतियों को तीन श्रेणियों में बांटे
3. समाधान लागू करें
आप शुरुआत में सिर्फ़ एक महत्वपूर्ण एक्शन एरिया के लिए समाधान लागू कर सकते हैं। अपनी संस्था में समाधान लागू करने से पहले, अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछें:
हमें उम्मीद है कि इन परिणामों से आप हस्तक्षेप के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगे और अपने सेक्टर के ज़मीनी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले काम को और बेहतर बना पाएंगे।
यदि आपने अपनी संस्था में ज़मीनी स्तर पर प्रभावी समाधान लागू किए हैं तो हम आपसे उनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। हम आपके उन समाधानों को अन्य संस्थाओं और अन्य हितधारकों तक पहुंचाने में मदद करेंगे जिन्हें आपके अनुभवों से लाभ हो सकता है। इसके लिए आप हमसे [email protected] या [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़े।
—
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में ज़मीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए समुदाय के साथ काम करना आसान नहीं रह गया है।समुदाय में लगभग सभी व्यक्ति सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़कर अपनी स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं। किंतु लगातार बदलती नीतियां और उसकी औपचारिकताएं इस सबकी बड़ी वजह बन रही हैं। राज्य में पहले जिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का नाम चिरंजीवी योजना था, अब उसकी जगह आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया है। राज्य में अब आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड बनाए जा रहे हैं। पहले जहां एक परिवार का एक कार्ड बनता था, अब परिवार के हर सदस्य का अलग कार्ड बन रहा है।
लेकिन समस्या केवल कार्ड बनाए जाने तक सीमित नहीं है बल्कि कुछ तकनीकी दिक़्क़तों का भी हमें सामना करना पड़ता है। उनमें से एक प्रमुख है, आधार कार्ड का अपडेट न होना। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति का आधार पर पंजीकृत नाम और जन्म दिनांक बैंक खाते से अलग होते हैं। यह सब एक जैसे नहीं होने के कारण भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ने में परेशानियां होती हैं। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में नाम और जन्म दिनांक एक समान नहीं होते हैं जिसकी वजह से अनेक पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। यहां तक कि उन्हें इन सबके बारे में कई बार जानकारी भी नहीं होती है। जब हम बार-बार जाकर उन्हें इसके बारे में कहते हैं, तब वे आधार कार्ड लेकर उसे अपडेट करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं।
इन सबके चलते कई बार उनका दस्तावेज बनने में भी देरी होती है जिस वजह से वे कई बार योजनाओं का लाभ ही नहीं ले पाते हैं। इसका ख़ामियाज़ा हमें समुदाय के अविश्वास का सामना करते हुए भुगतना पड़ता है।
तारा शर्मा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एराल, चित्तौड़गढ़ में एएनएम के तौर पर पदस्थ हैं।
रामेश्वर शर्मा, समाजसेवी संस्था प्रयास के साथ जुड़कर समुदाय के साथ जुड़कर कार्य करने का 25सालों से अधिक का अनुभव रखते हैं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़े।
—
अधिक जानें: जानें कि बंधेज, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किस तरह से घातक परंपरा है।
भारत ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष की तरह मनाए जाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का नेतृत्व किया था। यह छोटे बीज वाली उन घासों से संबंधित था जिनकी देश में सदियों से खेती और खपत की जाती रही है। ये कठोर, पोषण से भरपूर अनाज, पानी की खपत कम करते हैं और इन्हें रासायनिक खादों-कीटनाशकों की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही, ये अत्यधिक गर्मी और सूखे का सामना कर सकते हैं इसलिए लगातार गर्म होती इस दुनिया में भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के ज़रूरी साधन बन जाते हैं। मोटे अनाजों (मिलेट्स) का उत्पादन बढ़ाने की अनगिनत और प्रमाणिक वजहें हैं। लेकिन मजबूत लग रही सरकारी नीतियों और नेक इरादों के बावजूद, कई महत्वपूर्ण चुनौतियां रास्ते में दिखती हैं।
पूरे देश में इससे जुड़ी परिस्थितियां अलग-अलग हैं, फिर भी पिछले कुछ दशकों में एक सामान्य रुझान कुछ इस तरह का रहा है: कई ग्रामीण समुदाय मोटे अनाजों की खेती से हटकर चावल (धान) की ओर बढ़ रहे हैं और इनमें ज्यादातर हाइब्रिड बीजों का उपयोग कर रहे हैं। अर्थ फोकस फाउंडेशन के साथ काम करते हुए हमने मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास गोंड और बैगा आदिवासी समुदायों को यह करते हुए देखा है। इस बदलाव की वजह बहुत हद तक, धान की खेती के लिए शुरू से अंत तक दी जाने वाली सुविधाओं की एक व्यवस्था है, जो 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान बनाई गई थी। दुर्भाग्य से इसने मोटे अनाजों को असुविधाजनक और अनचाहा बना दिया।
हालांकि हाइब्रिड बीज और सिंथेटिक उर्वरक जैसी चीजों के कारण धान की खेती करना अधिक महंगा है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के जरिए इसकी बिक्री की गारंटी मिलती है। लेकिन, कुछ राज्यों को छोड़ दें तो कम लागत के बावजूद मोटे अनाजों की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए कोई बाज़ार नहीं हैं। धान जैसी हाइब्रिड फसलों के बावजूद भी अगले साल के बीज नहीं मिलता है और हर साल इन्हें ख़रीदना पड़ता है लेकिन मोटे अनाजों के साथ ऐसा नहीं है।

चावल की तुलना में, मोटे अनाजों को उगाने में अधिक श्रम लगता है लेकिन सामुदायिक प्रयास की ज़रूरत कम होती है। अगर धान की फसल की बात करें तो कई परिवार मिलकर इसकी खेती करते हैं, वे इसकी बुआई और कटाई मिलकर करते हैं, जबकि मोटे अनाजों की फसल आमतौर पर एक ही परिवार द्वारा उगाई जाती है।
सावंती बाई का उदाहरण लेते हैं, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार के पास स्थित गांव, मुक्की में अपने पति के साथ रहती हैं। उनकी बेटियां शादी के बाद चली गईं हैं, इसलिए वे अपनी उपज – कोदो और कुटकी बाजरा – खुद ही इकट्ठा करती हैं। हर दिन, सुबह से लेकर रात होने तक, वे हाथ में हंसिया लेकर बैठती हैं, इन घासों को काटती है और छोटे बंडलों में बांधती है।

इसके अलावा, फ़िलहाल मोटे अनाजों की कटाई के लिए किसानों के पास कोई विशेष उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। जब चावल के लिए डिज़ाइन की गई मशीनरी से कटाई की जाती है तो कोदो और कुटकी जैसे छोटे अनाज – जो घास की तरह हल्के होते हैं – टूट जाते हैं और उन्हें नुक़सान होता है। ऐसे में सावंती बाई जैसे किसानों के पास हंसिया लेकर हाथ से कटाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। यह बताता है कि कम लागत वाले और मोटे अनाजों के लिए ऐसे ख़ास कृषि उपकरण विकसित किए जाने की ज़रूरत है जो इस फसल में लगने वाली मेहनत को कम कर सकते हैं।
कुछ मामलों में, धान के लिए इस्तेमाल की जा रही मौजूदा मशीनरी में मामूली बदलाव लाना भी मोटे अनाजों की उपज को आसान बना सकता है। उदाहरण के लिए, धान के थ्रेशर (जो डंठल को अनाज से अलग करता है) में थोड़ा बदलाव कर मोटे अनाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

मोटे अनाजों के मामले में प्रोसेसिंग एक चुनौती हो सकता है। ख़ासतौर पर छोटे अनाजों (माइनर मिलेट्स) जैसे कोदो और कुटकी के लिए जिनमें प्रमुख मोटे अनाजों (मेजर मिलेट्स) जैसे ज्वार, बाजरा, और रागी की तुलना में प्रोसेसिंग के अतिरिक्त चरण होते हैं। इन्हें हाथ से करना बोझिल हो सकता है और यह ज़िम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं पर ही आती है।

अधिकांश प्रोसेसिंग केंद्र बड़े पैमाने पर चलने वाले केंद्र हैं और विभिन्न इलाक़ों में उगाए गए अनाजों को बिचौलियों से ख़रीदते हैं और फिर उन्हें शहरी उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, कान्हा के आसपास उगाए जाने वाले अधिकांश मिलेट्स को बिचौलियों द्वारा लगभग 20 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाता है और बाजरा- प्रोसेसिंग केंद्र नासिक भेजा जाता है। स्थानीय बुनियादी ढांचे की कमी से कठिन परिश्रम बढ़ता है और किसानों की कमाई की संभावना सीमित हो जाती है।
एक समाधान को जांचने के लिए, हमने अर्थ फोकस परिसर में छोटे अनाजों के लिए एक छोटी प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की है। हमने पाया कि अधिकांश परिवार अपने उपभोग के लिए अनाज का प्रोसेसिंग करते हैं। इसके अलावा, कुछ घर जो स्थानीय पर्यटक रिसॉर्ट्स से जुड़े हुए हैं, वे 150 रुपये प्रति किलो तक की ऊंची कीमतें प्राप्त कर पाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की भारी संख्या के कारण क्षेत्र में ऐसे कई रिसॉर्ट हैं, और वे स्थानीय किसानों के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में काम करते हैं।
इसके साथ ही, स्थानीय व्यवसायों को और विकसित करने की भी संभावना भी दिखती है क्योंकि पीसने से पहले अनाजों को धोना, साफ करना और सुखाना आवश्यक है। आटा चक्की की तरह छोटे पैमाने की मिलों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा संचालित स्थानीय व्यवसायों के रूप में भी चलाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में जहां मोटे अनाज के बिचौलिए शामिल नहीं होते हैं, प्रोसेसिंग हमेशा अनाज के भंडारण, पैकेजिंग और वितरण के बाद किया जाता है। आमतौर पर, समुदाय मोटे अनाजों की फसल को मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं और उन्हें कपड़े से बांध देते हैं। वे अनाज बग़ैर संसाधित किए रखते हैं क्यों कोदो में नमी लगने का ख़तरा होता है जिससे फंगस मायकोटॉक्सिन बनता है। ये मायकोटॉक्सिन उल्टी, चक्कर आना और बेहोशी जैसे कई लक्षणों का कारण बन सकते हैं। इसीलिए कुछ किसानों का मानना है कि बारिश के बाद कोदो ज़हरीला हो जाता है। लेकिन इससे जुड़े कुछ स्थानीय उपाय भी हैं जैसे मोटे अनाजों को गुड़ के साथ सुरक्षित करना (शायद नमी सोखने के लिए) या विषैलेपन की जांच के लिए पहले थोड़ा सा पशुओं को खिलाना।
इस प्रकार के मसले, खाद्य सुरक्षा के तरीक़ों को मिलेट वैल्यू चेन के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण बनाते हैं। अगर मोटे अनाजों को उनके उत्पादन और उसके आसपास के इलाक़ों से दूर बेचा जाना है तो उसे ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ कारगर प्रक्रियाओं को स्थापित किया जाना ज़रूरी है ताकि नकारात्मक सार्वजनिक प्रतिक्रिया से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, उचित भंडारण और पैकेजिंग से यह सुनिश्चित होता है कि नमी अनाज के भीतर ना जाए और फ़ंगस को रोका जा सके। भंडारण प्रबंधन (माल लाने, भंडारण और बेचने की व्यवस्था) भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि किस बैच में गड़बड़ है और किसे वापस लिया जाना या नष्ट किया जाना चाहिए।
इन मानदंडों के लागू होने से, मिलेट वैल्यू चेन में ग्रामीण उद्यमों के विकसित होने के मौक़े बनेंगे। उदाहरण के लिए, पड़ोसी जिले मंडला में नर्मदा सेल्फ-रिलायंट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने 2023 में एक मिलेट प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की। यह एफपीसी, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा समर्थित और ज़्यादातर आदिवासी किसानों से जुड़ी है। यह शहरी बाज़ार में स्थापित ब्रांड्स को प्रोसेस्ड मिलेट बेचती है।

मोटे अनाज में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा की मांग को पूरा करने की बड़ी संभावना दिखती है। लेकिन इसके क्षमता आज़माने के लिए, इन्हें व्यापक इकोसिस्टम का सहयोग देने की ज़रूरत है। अगर हम भारत-भर के भोजन में दोबारा मोटे अनाजों को शामिल कराना चाहते हैं तो हमें वैल्यू चेन में दिखाई पड़ रहे इन मुद्दों को हल करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर, फसल उपजाने और उसके प्रोसेसिंग से जुड़े विषयों को। हमें स्थानीय स्तर पर इन्हें प्रोसेस, स्टोर, टेस्ट और पैकेज करने की क्षमता और इंफ़्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है ताकि इनका उत्पादन और वितरण आसान बन सके। संक्षेप में, हमें मोटे अनाजों को लेकर ठीक वैसा ही सहयोगी इंफ़्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, जैसा 1960 में गेहूं और चावल को लेकर बनाया गया था। इस बार, ऐसा करते हुए हमारा उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर पोषण और जलवायु सहज बनाना होना चाहिए।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—

राजस्थान के कई जिलों में दलित जाति के लोगों से भेदभाव और हिंसा आम बात है। इस भेदभाव का एक रूप इस तरह भी दिखाई देता है कि दलित जातियों से आने वाले दूल्हों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले इस कुप्रथा को बदल रहे हैं। यहां दलित समाज की बिंदोरी (शादी की एक रस्म जिसमे लड़का या लड़की अपने परिवार के साथ अपने गांव में जुलूस निकालते है) निकलने पर किसी तरह के सवाल नहीं उठते हैं। इतना ही नहीं, हालिया सालों में इन जिलों में बेटियों को भी घोड़ी पर बैठा कर शादी के लिए ले जाया जाने लगा है।
श्रीगंगानगर जिले को 1994 में विभाजित कर हनुमानगढ़, और फिर 2023 में बांटकर अनूपगढ़ जिला बनाया गया था। भौगोलिक रूप से पंजाब से सटा यह इलाका भले ही तीन जिलों में बंटा है मगर यहां लोगों की सोच एक जैसी है। विवाह के समय घोड़ी पर बैठना केवल पुरुषों का ही अधिकार माना जाता रहा है और अब तक किसी भी समाज ने बेटियों को घोड़ी चढ़ने का हक नहीं दिया है। राजस्थान में तो दलित पुरुषों से भी यह अधिकार छीना जाता रहा है, मगर इस इलाके में दलित हों या सवर्ण सभी बिरादरी के लोग अपने बेटों के साथ-साथ बेटियों को भी घोड़ी पर बैठा कर बिंदोरी निकालते हैं।
शहर-कस्बों से ज्यादा गांवों में बेटियों की बिंदोरी का चलन ज्यादा देखने में आ रहा है। दलित समाज से आने वाले, पोहड़का गांव निवासी मनीराम मेहरड़ा ने अपनी बेटी मूर्ति को घोड़ी पर बैठा कर धूमधाम से बिंदोरी निकाली थी। मेहरड़ा कहते हैं, ‘‘हमने हमेशा सवर्णों के बच्चों को ही घोड़ी चढ़ते देखा था। हमारे परिवार के किसी भी विवाह में कभी कोई घोड़ी नहीं चढ़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि यह ऊंची जाति वालों का ही अधिकार है। हमने भी इसे ही शाश्वत मान लिया था लेकिन अब माहौल बदल रहा है। मैंने बेटे और बेटी दोनों को विवाह के समय घोड़ी पर बैठाया।’’
दलित समाज को किस तरह इस सांस्कृतिक अधिकार से वंचित किया जाता था, इस पर सूरतगढ़ के 79 वर्षीय पत्रकार एवं लेखक करणीदान सिंह राजपूत कहते हैं, ‘‘प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ इलाके में भी जातिगत भेदभाव खूब रहा है। कई उच्च कही जाने वाली जातियों के लोग आज भी दलितों के घर जाने या साथ खाने-पीने से परहेज करते हैं। पारंपरिक रूप से शादी के समय सवर्ण जाति के दूल्हे ही घोड़ी पर चढ़ते आए हैं। दलितों को घोड़ी पर चलने की अपनी इच्छाओं का दमन ही करना पड़ा है।’’
राजपूत कहते हैं, ‘‘पुराने जमाने में घोड़ियां बड़े जमींदारों और ठाकुरों के पास ही थीं। यह उनका स्टेट्स सिंबल था। उच्च जातियों के यहां काम करके आजीविका चलाते रहे दलित, कमेरा (कामकाज करने वाला) वर्ग ने कभी घोड़ी चढ़ने जैसी महत्वाकांक्षा ही नहीं पाली। या यूं कहें कि उन्होंने इस पर सवर्णों का ही अधिकार होने की बात मान ली। अब परिवेश बदल रहा है।’’
समाज की सोच में बदलाव कैसे आया, उस पर दलित समाज के सेवानिवृत जिला आबकारी अधिकारी केसराराम दहिया कहते हैं, ‘‘पिछले कुछ सालों में पंचायतों में आरक्षण तथा शिक्षा की बदौलत दलित समाज की तस्वीर खासी बदली है। अब दलित युवा सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। इसी के साथ जागरुकता भी आई है। इसका असर समाज में नजर आ रहा है।’’
दलित जाति से आने वाले हनुमानगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान राजेन्द्र प्रसाद नायक कहते हैं, ‘‘पिछले एक दशक में कई जगह दलित दूल्हे घोड़ी पर सवार होने लगे हैं लेकिन लड़कियों को घोड़ी चढ़ाने का चलन बीते पांच-छह सालों में बढ़ा है। लगता है, सामाजिक वर्जनाओं के चलते घुट कर रह गईं इच्छाएं अब उछाल मार रही हैं। अब दलित समाज भी बेटियों को घोड़ी पर चढ़ाकर गौरवान्वित होने का मौका नहीं चूक रहा है।’’
हनुमानगढ़ के एडवोकेट दौलत सिल्लू बताते हैं, “हमारे परिवार में कभी कोई लड़का भी घोड़ी नहीं चढ़ा था लेकिन इस साल हमने शादी के समय भतीजी पूजा को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली। हमने उसी चाव से पूजा की शादी की, जिस चाव से लोग बेटों की करते हैं।’’
अमरपाल सिंह वर्मा, एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और राजस्थान में रहते हैं।
—
अधिक जाने: जानें कि राजस्थान के सलूंबर जिले की किशोरियों को शादी या खनन में से एक क्यों चुनना पड़ रहा है?
अधिक करें: लेखक के काम को जानने और उन्हें अपना सहयोग देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।
साल 2006 में शुरू की गई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कानूनी रूप से लोगों को काम करने का अधिकार देती है। यह योजना हर परिवार को जॉब कार्ड के साथ 100 दिनों के काम की गारंटी देकर, गांवों में बेरोज़गारी, गरीबी और अचानक प्रवास जैसी समस्याओं को हल करने के उद्देश्य के साथ लाई गई थी। मनरेगा एक अधिकार-आधारित कानून है जो ग्रामीण भारत के किसी भी कामकाजी उम्र के व्यक्ति को बुनियादी आय प्रदान करता है, ख़ासकर जहां लोगों के पास काम के स्थाई अवसर नहीं होते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में, मांग बढ़ने के बावजूद मनरेगा का बजट या तो घटा है या उतना ही रहा है। बजट में कटौती के अलावा नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और नागरिक संगठनों ने मनरेगा से जुड़े अन्य मुद्दों की ओर भी इशारा किया है, जैसे- कम मजदूरी जिसे बढ़ाया जाना चाहिए, तकनीक के अधिक इस्तेमाल पर जोर, डेटाबेस से श्रमिकों के नाम हटना, और केंद्र सरकार का खराब प्रबंधन। इसके अलावा, योजना में सामग्री की लागत का ज़िम्मा उठाने वाली केंद्र सरकार से अभी राज्यों को 6,366 करोड़ रुपये मिलना बाक़ी है। इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए, सवाल उठने लगे हैं कि क्या नकद हस्तांतरण योजना भी यह काम कर सकती है।
लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोगों की राय क्या है? मनरेगा से जुड़े लोग जैसे श्रमिक, यूनियंस और उनके साथ काम करने वाले सामाजिक संगठन आदि, इसके बारे में क्या सोचते हैं? मनरेगा का लाभ उठाने वालों के लिए इस योजना के चलते किस तरह के बदलाव हुए हैं? और, ज़मीनी स्तर पर लोग इसके बारे में क्या महसूस करते हैं?
विभिन्न ग्रामीण संदर्भों में, मनरेगा श्रमिकों की परिस्थितयां और अनुभव अलग-अलग हैं। आईडीआर ने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में क़ानून के कार्यान्वयन पर काम करने वाले संगठनों और लोगों से बात की।इनमें आजीविका ब्यूरो, राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन (आरएएमयू) और ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्थान (जीएसवीएस) के सदस्य शामिल हैं। लगभग हर जगह यह महसूस किया गया कि ग्रामीण राजस्थान में मनरेगा अभी भी एक आवश्यकता है। राजस्थान एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और यहां आजीविका के अवसरों का अभाव है। राज्य में मनरेगा के तहत लागू की गई परियोजनाओं में जल संरक्षण, सूखे से बचाव और ग्रामीण सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। यह पर्यावरण सहज स्थायी खेती और विकास की बढ़त में मददगार है।
हमने राजसमंद, ब्यावर और अजमेर जिलों में संगठन प्रमुखों, मनरेगा मेट्स (कार्यस्थल पर्यवेक्षकों) और श्रमिकों सहित कई लोगों से बात की। ये सभी ग्रामीण और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए योजना की ज़रूरत आगे भी बने रहने की बात कहते हैं।
श्रमिकों के बीच इसकी प्रासंगिकता और लोकप्रियता के कुछ कारण:
राजस्थान के राजसमंद जिले के कुम्भलगढ़ जैसी जगहों में उद्योग-धंधों की कमी और इलाक़े की भौगोलिक स्थिति के चलते यहां दैनिक वेतन श्रम के मौक़े बहुत कम होते हैं। इस पहाड़ी और चट्टानी भूमि वाले इलाक़े में खेती के लिए उपयुक्त ज़मीन बहुत कम है। राजसमंद जिले का केवल लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा ही खेती योग्य है और कुंभलगढ़ क्षेत्र में तो यह आंकड़ा और भी कम हो जाता है। हालांकि कुम्भलगढ़ किले और हल्दीघाटी से शहर की निकटता के कारण कुम्भलगढ़ में पर्यटन में तेजी देखी जा रही है, लेकिन इससे जुड़ी नौकरियां (हॉस्पिटैलिटी जॉब्स) केवल औपचारिक रूप से शिक्षित लोगों के लिए ही खुली हैं।
दक्षिणी राजस्थान में लगभग 78 प्रतिशत श्रमिक काम की तलाश में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं।
आजीविका ब्यूरो के साथ काम करने वाले धर्मराज गुर्जर के अनुसार, “मजदूरी का मुख्य स्रोत निर्माण कार्य है, जहां अधिक कौशल वाले लोगों (जैसे बढ़ई या पेंटर) को प्रति दिन 500-550 रुपये मिलते हैं, जबकि बाकी लोग 250-300 रुपये कमाते हैं।” इन विकल्पों के अलावा, मनरेगा ही है।
“एक समय, जब जनसंख्या कम थी, शायद यहां आजीविका कमाने के पर्याप्त अवसर थे। लेकिन राजसमंद में अब पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं,” वे आगे जोड़ते हैं। इस वजह से पलायन एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है। राजसमंद और उदयपुर क्षेत्र में आजीविका ब्यूरो के किशोर और महिला कार्यक्रम में काम करने वाली मंजू राजपूत कहती हैं, “हमारे यहां एक कहावत है – पास हुआ तो जिंदाबाद, फेल हुआ तो अहमदाबाद।” आजीविका ब्यूरो द्वारा साल 2014 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, दक्षिणी राजस्थान में लगभग 78 प्रतिशत श्रमिक काम की तलाश में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। “महामारी के बाद से वित्तीय स्थिति और खराब हो गई है, इसलिए अब लोगों ने अपने पूरे परिवार को साथ ले जाना शुरू कर दिया है।”
उम्र के लिहाज़ से भी अब पलायन जल्दी शुरू होने लगा है और इसका एक चक्र बन गया है। अक्सर परिवार की एक पीढ़ी के पुरुषों के वापस आने के बाद, अगली पीढ़ी के पुरुष काम पर चले जाते हैं। मंजू कहती हैं, “महज़ 13-15 साल के लड़के काम की तलाश में पलायन करते हैं। वे लगभग दो दशकों तक काम करेंगे। आमतौर पर यह काम होटलों की रसोई में, हम्माल (भार वाहक) के रूप में, निर्माण कार्य में, और अन्य व्यवसायों में होता है – और फिर वे लौट आएंगे। वैसे तो लोग उम्र के तीसवें दशक में अच्छे से काम करने योग्य होते हैं लेकिन ये प्रवासी जो वापस आते हैं – काम के भारी शारीरिक दबाव और लंबे घंटों के कारण तब तक पूरी तरह से थक चुके होते हैं। उनकी वापसी के बाद, थकान और स्थानीय नौकरियों में आवश्यक कौशल की कमी के कारण अगली पीढ़ी के पास पलायन करने और घरेलू आय में योगदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।
एक मनरेगा कार्यकर्ता, कमला देवी जो आजीविका के उजाला समूह की सदस्य भी हैं, ने जोर देकर कहा कि पूरा परिवार कमाने के लिए काम करता है – कृषि (जो आमतौर पर बिल्कुल भी मशीनीकृत नहीं होती है और इसलिए सभी को काम पर लगना पड़ता है), मनरेगा कार्य और परिवार के युवा पुरुष सदस्यों के प्रवासी कार्य से मिलकर होने वाली आय से लोगों का घरेलू खर्च पूरा होता है। इसलिए, मनरेगा द्वारा प्रदान किया जाने वाला गारंटी काम घरेलू आय के लिए आवश्यक हो जाता है।
इसके अलावा, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के प्रयास में, 2011 में, राजस्थान सरकार ने अधिसूचित किया था कि विशेष रूप से कमजोर समूहों को ग्रामीण गारंटी योजना के तहत 200 दिनों का काम मिलेगा, और इसका अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बारां जिले के खेरुआ और सहरिया आदिवासी और उदयपुर के कथौड़ी आदिवासी उन लोगों में से हैं जिन्हें इस प्रयास का लाभ मिलता है। हालांकि मनरेगा उन समुदायों के लिए एक जीवनरेखा है जो परंपरागत रूप से बंधुआ मजदूरी के अधीन रहे हैं लेकिन उनके लिए भी पूरे 200 दिनों का काम प्राप्त करना दुर्लभ है।
बारां के एक मनरेगा मेट सुरेश सहरिया कहते हैं कि “मनरेगा ने सहरियाओं को प्रवास की कठिनाइयों और दूसरे लोगों की ज़मीनों पर बेहद कम मज़दूरी पर काम करने से बचाया है। हालांकि ज़्यादातर लोगों के लिए अतिरिक्त 100 दिनों का काम प्राप्त करना लगभग असंभव है, और इस अधिकार के लिए हम लगातार लड़ भी रहे हैं। मनरेगा नहीं होगा तो सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के कारण हमारे लिए सम्मानजनक काम पाना मुश्किल हो जाएगा।

मनरेगा महिलाओं और लैंगिक मुद्दों से संबंधित विषयों को सामने लाता है – लैंगिक समानता, सामाजिक ताक़त के समीकरण, आय पर नियंत्रण, कठिन परिश्रम, आने-जाने की आजादी के साथ ग्रामीण और घरेलू दोनों स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता और सार्वजनिक नेतृत्व। पूरे भारत में, महिलाएं मनरेगा श्रमबल का 57.43 प्रतिशत हिस्सा हैं, और 2020-21 को छोड़कर, यह संख्या लगातार बढ़ी है। ऐसा तब भी है जब भारत में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी दर कुल मिलाकर स्थिर हो गई है।
हमने जाना की दो बातें हैं जो महिलाओं को सशक्त महसूस करवाती हैं।
जब पुरुष प्रवास करते हैं तो वे आमतौर पर महिलाओं और अपने परिवारों को पीछे छोड़ देते हैं। मनरेगा महिलाओं के लिए कार्यबल में भाग लेने और आय अर्जित करने का एक तरीका रहा है- ख़ासतौर से वह तरीक़ा जिस पर उनका नियंत्रण है। मनरेगा में महिला श्रमबल की भागीदारी लगातार बढ़ी भी है, खासकर राजस्थान में जहां यह आंकड़ा 68.17 प्रतिशत बैठता है।
कमला देवी हमें बताती हैं कि मनरेगा से महिलाएं अपने घरेलू कामकाज के साथ-साथ कृषि कार्य भी करने में भी सक्षम हैं, वे कहती हैं कि “मनरेगा के तहत, हमें निश्चित घंटों तक रुकने की ज़रूरत नहीं है और काम का कोटा पूरा होते ही हम छोड़ सकते हैं।” हालांकि यह पूरे भारत के लिए सच नहीं है, कई नागरिक समाज संगठनों और श्रम अधिकार समूहों ने राज्य और स्थानीय सरकारी निकायों पर दबाव डाला है कि श्रमिकों को आठ घंटे रुकने के बजाय आवंटित कार्य का कोटा पूरा करने के बाद जाने दिया जाए।
ब्यावर कई खनिज क्रशिंग कारखानों का घर है। यहां मनरेगा ने महिलाओं के जीवन को एक अलग और शायद अधिक स्पष्ट तरीके से प्रभावित किया है। ब्यावर में जीएसवीएस के एक कार्यक्रम अधिकारी, राजेश ढोडावत कहते हैं, “ब्यावर में दिहाड़ी मजदूरों में स्थानीय निवासी और बिहार जैसे राज्यों के प्रवासी श्रमिक दोनों शामिल हैं। यह देखते हुए कि यहां आय का मुख्य स्रोत पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्रियां थीं, स्थानीय और प्रवासी श्रमिक दोनों समान नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। स्थानीय श्रमिकों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी क्योंकि राजस्थानी पुरुष स्वयं दूसरे राज्यों में चले जाते हैं।” इससे श्रमिकों की संख्या अधिक हो गई जिसके कारण मजदूरी दरों और कामकाजी परिस्थितियों को लेकर श्रमिकों के पास मोलभाव की बहुत कम गुंजायश रह गई।
महिलाएं महसूस करती हैं कि घरेलू फ़ैसलों में उनकी भी भागीदारी है क्योंकि वे भी परिवार की आय में सहयोग कर रही हैं।
लेकिन, मनरेगा की शुरुआत के बाद, स्थानीय महिलाओं ने कई कारणों से कारखाने के काम के बजाय इस काम को चुना। काम का उनके घरों से अपेक्षाकृत पास होना, कामकाजी परिस्थितियां कम ख़तरनाक होने के साथ बेहतर मज़दूरी दर मिलना और घरेलू तथा कृषि कार्यों के साथ मनरेगा का काम किए जाने की सक्षमता, इसके प्रमुख कारण थे।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को लगता है कि निर्णय लेने में उनकी हिस्सेदारी है क्योंकि वे घरेलू आय में योगदान दे रही हैं। कुछ महिलाओं ने हमसे कहा, “अपने बच्चों की देखभाल करना आसान है। और जब हमारी आय हमारे पतियों के साथ जुड़ जाती है तो घर चलाना आसान हो जाता है।” वे महिलाएं जिनके पति विकलांग हैं या सिलिकोसिस जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं (जो कि क्षेत्र में आम है लेकिन कम दर्ज़ होती है), बताती हैं कि मनरेगा उन्हें मिलने वाली पेंशन से जुड़ जाता है। जब महिलाएं काम करती हैं तो उनके बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने की अधिक संभावना होती है। ऐसे अध्ययन हैं जो बताते हैं कि मनरेगा के मामले में भी यही स्थिति रही है।
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपना घर संभालती हैं; खाना बनाने, सफाई करने, पानी लाने और भोजन तैयार करने जैसे घरेलू काम करने के साथ चराई और कृषि कार्य भी करती हैं – ये सभी अकेले करने वाले कार्य हैं। मनरेगा स्थल पर, श्रमिक मुख्य रूप से महिलाएं हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वे अधिक स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकती हैं। उजाला समूह, रामू और जीएसवीएस जैसी संस्थाएं वरीयता देकर महिला मनरेगा मजदूरों, मेट, मोबिलाइज़र और यूनियनों/समूहों के ब्लॉक समन्वयकों के साथ मिलकर काम करती हैं। यह न केवल महिलाओं के स्थानीय नेतृत्व का निर्माण करने के लिए है बल्कि उस स्थान का फ़ायदा उठाने के लिए भी है जहां महिलाओं और लड़कियों की संख्या अधिक है।
राजसमंद जिले की मनरेगा कार्यकर्ता, कम्मा देवी ने हमें बताया कि “पुरुषों की निगरानी के बिना महिलाओं को मिलने की जगह नहीं मिलती थी। मनरेगा स्थल पर, हमें अपने घरों से बाहर जाने का अवसर मिलता है, और हम एक-दूसरे से खुलकर बात कर पाते हैं। जब हम एक साथ आते हैं तो हम हंसी-मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना साझा करते हैं, अपनी पारिवारिक समस्याओं के साथ-साथ गांव और पंचायत के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और कभी-कभी लोक गीत भी गाते हैं।
मनरेगा के तहत किया गया श्रम गांव की संपत्ति निर्माण में जाता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में पानी की कमी को कम करने के लिए टांकाओं (तालाबों) को आधुनिक बनाने के लिए मनरेगा का उपयोग किया गया है। मंजू कहती हैं, “जो सड़कें बनाई जाती हैं, और जो काम लोग करते हैं, वह आमतौर पर श्रमिकों के लिए भी एक प्रोत्साहन होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके गांव का बुनियादी ढांचा भी साथ-साथ विकसित हो रहा है।”
एक सामान्य आरोप जो लगाया जाता है, वह यह है कि इस प्रकार बनाई गई संपत्ति और यह काम भी अपने आप में निम्न गुणवत्ता का होता है, जिसे खाइयां खोदने के बराबर माना गया है – उत्पादक नहीं है। हालांकि, यह सच नहीं है। यूएनडीपी द्वारा मनरेगा परिसंपत्तियों के प्रभाव मूल्यांकन से पता चलता है कि वे आय सृजन, अधिक लाभकारी कृषि पद्धतियों की ओर बदलाव और जल संचयन और अन्य संरचनाओं के निर्माण का नेतृत्व करते हैं जो गांव के लिए उपयोगी हैं।
मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह-संस्थापक शंकर सिंह एक कच्चे हिसाब के द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर मनरेगा के प्रभावों के बारे में बात करते हैं। “भीम का उदाहरण लें, जहां 2,000 पंजीकृत श्रमिक हैं। यदि इन सभी श्रमिकों को पूरा काम, पूरा दाम (255 रुपये की पूरी दर पर 125 दिन का काम) मिलता है, तो आप भीम की स्थानीय अर्थव्यवस्था में छह करोड़ रुपये से अधिक जोड़ रहे हैं। और वह पैसा कहां जा रहा है? यह यहां के छोटे दुकानदारों के पास जा रहा है।”

मनरेगा श्रमिक और नागरिक समाज संगठन, जो काफ़ी समय से श्रम और संबंधित मुद्दों पे काम कर रहे हैं, दोनों ही रोजगार गारंटी कानून को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके बावजूद, इस कानून को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो इसकी प्रभावशीलता और श्रमिकों की आजीविका को प्रभावित करती हैं।
एक महत्वपूर्ण मुद्दा, पंचायत सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) और सरपंचों का जॉब कार्ड जारी करने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं होना है, और वे अक्सर बजटीय कमी का हवाला देते हुए जॉब कार्ड जारी करने से बचते हैं। इसके अतिरिक्त, जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को जॉब कार्ड नहीं मिलता है। बीना चौहान, जो ब्यावर में जीएसवीएस के साथ कम्युनिटी मोबलाइजर के रूप में काम करती हैं, कहती हैं कि शहर के आसपास के गांवों में मनरेगा का काम शुरू करना आसान नहीं था। “जिस पहली पंचायत में हम गए, वहां का सरपंच बेहद झिझक रहा था। यहां तक कि जब एक पंचायत ने जॉब कार्ड जारी करना शुरू किया और हम अगली पंचायत में चले गए तो वहां के सरपंच ने इसके खिलाफ पुरुषों को एकजुट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा, ‘आज वे यह मांग रहे हैं, कल यह कुछ और होगा।’’
औसतन एक श्रमिक को केवल लगभग 45 दिन का काम मिलता है।
रामू के पूर्व ब्लॉक समन्वयक ईश्वर सिंह का कहना है कि इस लैंगिक भेदभाव के पीछे भ्रष्टाचार भी छिपा होता है। “कई बार सरपंच, सचिव, अन्य सरकारी अधिकारी और जिन ठेकेदारों को नियुक्त करते हैं उनमें वास्तव में काम करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए पूरे दिन पंचायत कार्यालय में बैठना, मस्टर रोल तैयार करना, काम का ऑडिट करना आदि काम उन्हें करने पड़ेंगे। और, वे इससे बचना चाहेंगे। यहां तक कि जब जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं, तब भी अक्सर पूरे 100 दिनों का काम उपलब्ध नहीं होता है, और श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए काम के लिए पूरा वेतन नहीं मिल पाता है। “मान लीजिए कि केंद्र सरकार आपको प्रति व्यक्ति एक रोटी भेजती है। लेकिन जब तक यह रोटी आप तक पहुंचती है, तब तक इसका एक निवाला ही बचता है। बीच में, सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों और अन्य बिचौलियों ने अपना पेट भर लिया है। जब तक मनरेगा का बजट ज़मीन पर पहुंचता है तब तक उसका यही हाल होता है।”
सिस्टम में भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला हुआ है। काम मांगने के बाद भी श्रमिक अक्सर काम पाने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि या तो उनका नाम मस्टर रोल में नहीं होता है या फिर उन्हें साल में गारंटी 100 दिन से भी कम काम मिलता है। मंजू और जिन अन्य लोगों से हमने बात की, उनके अनुसार औसतन, श्रमिकों को केवल लगभग 45 दिन का काम मिलता है। प्रशासनिक बाधाएं, जैसे कि बैंक खाते खोलने और उपस्थिति दर्ज करने के लिए एनएमएमएस ऐप का उपयोग करने की आवश्यकता भी श्रमिकों को काम के लिए अपना नाम लिखने या भुगतान प्राप्त करने में बाधा डालती है।
इन समस्याओं की गंभीरता और हर स्थानीय समुदाय का उनसे निपटने का तरीक़ा अलग होता है। उदाहरण के लिए, ब्यावर जिले के गांवों में भी योजना के तहत आवंटित कार्य दिवसों की पूरी संख्या प्राप्त करने और पूरी राशि का भुगतान करने में भी बाधाएं आ रही हैं। जब किसी क्षेत्र का नाम ग्रामीण से शहरी में बदल जाता है तो मनरेगा उस पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। इसलिए, भीम में महिला श्रमिकों को इस साल की शुरुआत में विरोध करते हुए पाया गया था – भीम को ग्राम पंचायत से नगर पालिका में पुनर्वर्गीकृत किया गया था, और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना (शहरी रोजगार गारंटी योजना) अभी तक वहां लागू नहीं की गई थी। इस प्रकार, भीम और ब्यावर दोनों में श्रमिकों ने अपनी मांगों को उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा भी लिया।
मनरेगा से जुड़ी जमीनी स्तर की समस्याओं को स्वीकार करना और श्रमिकों के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है ताकि चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और योजना के कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके।