आंध्र प्रदेश के चित्तूर के पास थवनमपल्ले मंडल, थोडाथारा गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर विजय कुमार अपने अगले मरीज को अंदर आने के लिए आवाज़ देते हैं। डॉक्टर कुमार थोड़े गर्व के साथ उनके बारे में बताते हैं कि “मेरी जानकारी में ये सबसे अनुशासित व्यक्ति हैं।” तब तक रेड्डीयप्पा रेड्डी अंदर आए और डॉक्टर कुमार के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। साठ वर्ष के रेड्डीयप्पा ने बताया कि “दस साल पहले मुझे पता चला कि मुझे मधुमेह है। मैंने डॉक्टर कुमार की सलाह मानी। अब मैं हर रात खाना खाने के बाद आम के बगीचे तक टहलने जाता हूं।” उनके बारे में डॉक्टर कुमार कहते हैं कि रेड्डी इस क्लिनिक में आने वाले बाक़ी मरीज़ों के लिए एक प्रेरणा हैं।
2013 में अपोलो फ़ाउंडेशन की पहल, टोटल हेल्थ इनीशिएटिव ने थवनमपल्ले मंडल की 32 ग्राम पंचायतों के 195 गांवों में एक सर्वे किया। इसके लिए हमने 31,453 लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े आंकडे जुटाए और पाया कि इनमें से 6.2 फ़ीसदी लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। साथ ही ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि 16.7 फ़ीसदी पुरुष और 12.2 फ़ीसदी महिलाएं मोटापे से ग्रस्त हैं जिसके चलते मधुमेह का ख़तरा बढ़ जाता है।
गांवों की तुलना में शहरों में मधुमेह फैलने की दर दोगुनी है लेकिन थवनमपल्ले मंडल में यह बड़ी चिंता का विषय है।
हाल ही में थवनमपल्ले मंडल में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या में 10.1 फ़ीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन अब भी यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कम है। एनल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित 2021 मेटा-एनालिसिस के अनुसार, साल 1972 में ग्रामीण और शहरी भारत मधुमेह पीड़ितों की दर क्रमशः 2.4 फ़ीसदी और 3.3 फ़ीसदी थी। 2015 आते-आते यह आंकड़ा बढ़कर क्रमश: 15 और 19 फ़ीसदी पर पहुंच गया।
चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में 7 करोड़ 47 लाख लोग मधुमेह के शिकार हैं। गांवों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में मधुमेह के मामले दोगुने अधिक हैं।
टोटल हेल्थ इनीशिएटिव पर लौटें तो इसका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से थवनमपल्ले मंडल है और इस इलाक़े में यह बीमारी गंभीर चिंता का विषय है। यहां मोबाइल क्लिनिक की एक इकाई चलाने वाले डॉक्टर वी भार्गव कहते हैं कि “पिछले महीने मैं 600 लोगों से मिला था जिनमें से 200 लोग मधुमेह के मरीज़ थे।” इस बीमारी की चपेट में आने वाले ज़्यादातार लोगों की उम्र 50 वर्ष से अधिक होती है। यदि इसकी तुलना राष्ट्रीय आंकड़ों से करें तो 2009 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि 54 फ़ीसदी लोग 50 की उम्र में पहुंचने से पहले ही इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इस अध्ययन से यह तथ्य भी सामने आया है कि भारतीय लोगों में मधुमेह के लक्षण उनके पश्चिमी समकक्षों की तुलना में लगभग एक दशक पहले से ही दिखाई देने लग जाते हैं।

थवनमपल्ले में सैटेलाइट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर टी स्वर्ण का कहना है कि “भारत के गांवों का वातावरण बदल रहा है जिसकी शुरूआत यहां के खान-पान से होती है।”
2016 में उत्तर-पश्चिम तमिलनाडु के कृष्णागिरी में एक अध्ययन किया गया जिसमें शोधकर्ताओं ने इस समस्या के मुख्य कारणों की पहचान की। उनका कहना है कि “लोगों के खान-पान में आया बदलाव मधुमेह के बढ़ते मामलों की मुख्य वजह है।” बेशक गावों में अब ‘सिटी फूड्स’ जैसे ढेर सारी शक्कर वाला सोडा और मिठाइयां या ट्रांस-फ़ैट से भरे चिप्स और बेकरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ी है लेकिन यह इस समस्या का मुख्य कारण नहीं है। इन इलाक़ों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा राशन की दुकानों पर मुफ़्त में बंटने वाले चावल को इसका ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। दरअसल मुफ़्त में मिलने वाला यह चावल अब लोगों का मुख्य आहार बन गया है।
डॉक्टरों का कहना है कि कृष्णागिरी से 150 किमी से भी कम दूरी पर स्थित थवनमपल्ले में भी लोगों का मुख्य आहार अब चावल हो चुका है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में मधुमेह की दर अधिक है। संभव है कि इसका मुख्य कारण सफ़ेद चावल का सेवन हो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा) अधिक होता है। इसे पानी में पका कर कांजी (चावल का दलिया) तैयार किया जाता है। स्टार्च वाले यह चावल शरीर में रक्त शर्करा (ब्लड-शुगर) के स्तर को बढ़ा देते हैं।
अरगोंडा में आयुष क्लिनिक की प्रमुख डॉक्टर एम गायत्री बताती हैं कि “स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं कि चावल के बिना उनका खाना अधूरा है।” उनका मुख्य उद्देश्य भूख शांत करना है क्योंकि ज़्यादातर लोग फल और मांस आदि नहीं खा सकते हैं। मौसमी सब्ज़ियां खाई जाती हैं लेकिन भोजन का ज़्यादातर हिस्सा चावल होता है और सब्ज़ी की मात्रा बहुत कम होती है। चावल से तैयार खाना सस्ता होता है और इसे खाने से लोगों का पेट भर जाता है। इसी तरह डॉक्टर भार्गव कहते हैं, “खेतों में काम करने वाले मज़दूर घर से सुबह आठ बजे निकलने से पहले ऐसा कुछ खाना चाहते हैं जिससे उन्हें दिन भर भूख न लगे।” इन इलाक़ों में गेहूं की खेती नहीं होती है इसलिए आमतौर पर लोग रोटियां नहीं खाते हैं। वहीं डॉक्टर स्वर्ण जोड़ते हैं कि “लोगों का ऐसा मानना है कि सुबह के समय चपाती खाने से शरीर में गर्मी पैदा होती है।”
टोटल हेल्थ इनीशिएटिव से जुड़े डॉक्टरों को यह आशंका है कि शारीरिक गतिविधियों में आई कमी और खान–पान की आदतों में आ रहे बदलाव भी मधुमेह के बढ़ते मामलों का कारण हो सकते हैं।
चावल ने रागी और बाजरा जैसे अनाजों की जगह ले ली है जो पहले थवनमपल्ले में भोजन का हिस्सा हुआ करते थे। डॉक्टर भार्गव कहते हैं, “हम लोग अब भी रागी के पकौड़े बनाते हैं लेकिन बदलते स्वाद के कारण अब रागी और चावल के आटे का अनुपात (2:1) उल्टा हो गया है। वह बताते हैं कि “मैं अपने खाने में जितना सम्भव हो सके उतनी मात्रा में पत्तेदार और हरी सब्ज़ियां शामिल करता हूं। साथ ही मैंने चाय पीनी बिलकुल बंद कर दी है (ज़्यादातर गांवों में लोग बहुत अधिक मीठी चाय पीते हैं।)” हालांकि डॉक्टर भार्गव अब भी पीडीएस पर निर्भर हैं और ब्राउन या लाल चावल नहीं खा पाते हैं जो कभी इस इलाक़े का पारम्परिक खाना था। ‘शहरी भोजन’ की सूची में शामिल हो जाने के कारण अब इन अनाजों की क़ीमत बहुत अधिक बढ़ गई है।
पारंपरिक चावल को बढ़ावा देनी वाली चेन्नई स्थित संस्था स्पिरिट ऑफ़ द अर्थ की प्रमुख जयंती सोमासुंदरम कहती हैं कि “भारत में हरित क्रांति के आने से पहले हमारे खाने में सौ अलग-अलग क़िस्म के चावल शामिल थे। वे थूयामल्ली, कातुयनम और मापिल्लई चम्पा जैसी क़िस्मों की तरफ़ इशारा करती हैं। सोमासुंदरम बताती हैं कि “1950 और 60 के दशक में ऐसी धारणा थी कि सम्भ्रांत लोगों द्वारा खाया जाने वाला सफ़ेद चावल सबसे अच्छा होता है। मोटा अनाज खाने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सफ़ेद चावल बड़ी चीज़ थी।” कर्नाटक स्थित संस्था सहज समृद्ध के संस्थापक कृष्ण प्रसाद कहते हैं मिलिंग तकनीक में आए सुधार के कारण चावलों की चमक और उसकी सुगंध में बढ़ोतरी हुई है। इससे लोगों को लगने लगा है कि ये चावल उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। वे 1960 के दशक में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा इलाक़े को याद करते हुए कहते हैं: “कपास और मूंगफली जैसे नक़दी फसलों के लिए लोकप्रिय होने से पहले इस इलाक़े के लोग खारी मिट्टी वाले अपने खेतों में कई क़िस्म के चावल उगाते थे।”
थोडाथारा में रहने वाली मधुमेह की मरीज़ आर इंद्राणी हमारा ध्यान इस बात पर ले जाती हैं कि इतने वर्षों में केवल लोगों के खान-पान में ही बदलाव नहीं आया है। वे कहती हैं, “मुझे ऐसा लगता है कि वे फसलें जो हम उगाते हैं उनमें आए बदलाव ने भी हमारी जीवनशैली को प्रभावित किया है।” पहले थवनमपल्ले में पारम्परिक रूप से गन्ने की खेती होती थी और यहां के लोग गुड़ उत्पादक थे। इंद्राणी आगे कहती हैं, “हमारे पास गन्नों के खेत भी थे। लेकिन अब बहुत कम ऐसे खेत बचे हैं। यहां के अन्य किसानों की तरह हमने भी 10 एकड़ में आम की खेती शुरू कर दी है। गन्ने की खेती में लगातार पानी और श्रम की खपत होती है वहीं आम एक मौसमी फल है और इसकी खेती में मेहनत भी कम लगती है।” टोटल हेल्थ के डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि लोगों की शारीरिक गतिविधियों में आई कमी और उनके खान-पान में आया बदलाव मिलकर मधुमेह के मामलों के बढ़ने की वजह बन रहे हैं। इंद्राणी विडंबना वाली हंसी हंसते हुए कहती हैं कि “मैं जो आम उगाती हूं उसे खा नहीं सकती हूं।”
इंद्राणी को अपने मधुमेह का पता एक साल पहले ही चला जब वह नेत्र जांच शिविर में अपनी आंखों की जांच करवाने गई थीं। डॉक्टर गायत्री बताती हैं कि “यहां लोग नियमित जांच को लेकर उतने गम्भीर नहीं है। जब तक उन्हें कोई शारीरिक समस्या दिखाई नहीं देती है जैसे कि पेशाब में अनियमितता वग़ैरह होना, तब तक वे नहीं आते हैं। इनका रवैया भी बचाव उपायों को बहुत गंभीरता से नहीं लेने वाला है।”
इसी तरह डॉक्टर स्वर्ण हमें बताते हैं कि “अक्सर जब लोग हमारे पास आते हैं तो उनका शुगर लेवल पहले से ही 11 प्रतिशत (सामान्य स्तर 6.5 प्रतिशत होता है) पहुंच चुका होता है। ज्यादातर मामलों में हो सकता है कि वे कई वर्षों से मधुमेह से पीड़ित हों लेकिन उन्हें इसकी जानकारी अब हुई है।”
2019 में पब्लिक हेल्थ फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि भारत में 15–49 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक दो में से एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित होता है और उसे इसकी जानकारी नहीं होती है। इस अध्ययन में यह भी सामने आया कि गांवों में रहने वाले पुरुषों में मधुमेह का खतरा अधिक होता है।
निचले से मध्यम स्तर का ख़तरा पैदा करने वाले मधुमेह का इलाज महत्वपूर्ण है ताकि इसे गंभीर होने से रोका जा सके।
डॉक्टर गायत्री कहती हैं, “लोगों को इस बात का डर होता है कि अगर उन्होंने एक बार दवाइयां लेनी शुरू कर दीं तो उन्हें यह जीवन भर लेनी पड़ेंगी। आमतौर पर लोग दवाइयों पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं।”
सभी डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि मधुमेह के पहले की स्थिति अर्थात् इससे बचाव और नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे बचाव के कई उपायों में एक उपाय पारम्परिक खान-पान को दोबारा चलन में लाना है। पारंपरिक खान-पान में विविधता होती है और चावल इसका मुख्य हिस्सा नहीं होता है। ऐसा करने से मधुमेह की रोकथाम में मदद मिल सकती है।
सबसे बड़ी मुश्किल शारीरिक गतिविधि को लेकर लोगों के रवैये में है। देश के किसी अन्य ग्रामीण और शहरी इलाक़े की तरह थवनमपल्ले में भी शारीरिक श्रम का संबंध जाति व्यवस्था से है। अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार के लोग अपने कामों के लिए लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं। इससे उनकी शारीरिक गतिविधियों में कमी आ जाती है।
इसके अलावा लोगों में निचले से मध्यम स्तर का ख़तरा पैदा करने वाले मधुमेह का इलाज महत्वपूर्ण है ताकि इसे और अधिक गंभीर होने से रोका जा सके। जैसा कि इस वर्ष किए गए राष्ट्रीय एनसीडी सर्वेक्षण के परिणामों में देखा गया है, पर्याप्त जांच, नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। साथ ही मधुमेह को लेकर लोगों को यह समझाना भी आवश्यक है कि यह जीवनशैली से जुड़ी बीमारी है। जीवनशैली से जुड़े बदलावों की जानकारी के मिलने पर लोग स्वयं को मधुमेह से ग्रसित होने से बचा सकते हैं।
इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।
—
प्रेमा गोपालन स्वयं शिक्षण प्रयोग (एसएसपी) की संस्थापक हैं। एसएसपी पुणे में स्थित एक स्वयंसेवी संस्था है जो गांवों में महिलाओं द्वारा संचालित उपक्रमों से संबंधित काम करती है। खेती, पोषण, साफ ऊर्जा, स्वास्थ्य और साफ-सफाई जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए एसएसपी ने बीते कुछ सालों में महिलाओं को इस तरह सशक्त बनाया है कि वे अपने समुदाय की समस्याओं को सुलझा सकें।
आईडीआर के साथ अपने इस इंटरव्यू में प्रेमा गोपालन एक ऐसी व्यवस्था (इकोसिस्टम) बनाने की बात कर रही हैं जो महिलाओं को ज़िम्मेदारियां उठाने में सक्षम बनाता है। साथ ही उन्होंने स्थायी आजीविका के तौर पर कृषि की भूमिका पर भी बात की है। इसके अलावा गोपालन ने किसी आपदा को तेज़ी से होने वाले विकास (फ़ास्ट-फ़ॉर्वर्ड विकास) के अवसर के रुप में इस्तेमाल किये जा सकने की संभावनाओं का भी ज़िक्र किया है।

जब 2020 के मार्च में महामारी की पहली लहर आयी तब जिस इलाक़े मराठवाड़ा में हम काम करते हैं, वहां छोटे और पिछड़े किसान बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इनमें से ज़्यादातर किसान अपनी फसलों की कटाई नहीं कर पाए थे। यहां तक कि जिनकी फसलें कट चुकी थीं वे भी लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट उपलब्ध न होने के चलते इसे बाज़ार तक नहीं ले जा सके थे।
महाराष्ट्र में ओस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर और नांदेड़ ज़िले की औरतें किसान हैं। वे फसलें उगाती हैं लेकिन इन्हें मंडी (बड़े बाज़ार) ले जाकर फसल बेचने का काम पुरुष ही करते हैं। ये मंडियां अक्सर ज़िले के बड़े कस्बों में स्थित होती हैं। इसका सीधा मतलब है कि किसानों को न केवल अपनी फसल बेचने के लिए वहां जाना पड़ता है बल्कि अपने घर की ज़रूरत का सामान आदि भी वे यहीं से ख़रीदते हैं। समुदाय के लोग औरतों को इतनी दूर की यात्रा करने की इजाजत नहीं देते हैं। इस तरह वे अपने खेतों में तो काम करती हैं लेकिन वे ये ज़रूरी फ़ैसले नहीं ले सकती हैं कि क्या बेचना है, कहां बेचना है और कितने में बेचना है। महामारी के बाद एसएसपी ने इन औरतों को सामूहिक व्यवसाय शुरू करने और उन्हें उद्यमों का रूप देने में मदद की। यह सम्भव हो सका क्योंकि हम लोग आजीविका/उद्यमों के लिए एक लोकल इकोसिस्टम बनाने पर एक दशक से भी अधिक समय से काम कर रहे थे। हम लोग पिछले छह सालों से महाराष्ट्र की महिला किसानों के साथ काम कर रहे हैं। इस दौरान हमें महसूस हुआ कि महाराष्ट्र में महिलाओं को बड़े पैमाने पर खेतिहर मजदूर के रूप में काम पर रखा जाता है। राज्य में कुल खेतिहर मज़दूरों का 79 फीसदी महिलाएं हैं। खेती-किसानी का सारा काम करने के बावजूद ज़मीन का मालिकाना हक न होने के कारण सरकार इन्हें किसान नहीं मानती है।
एक बार जब महिलाएं किसान बन गईं तो उन्होंने खेती से संबंधित फ़ैसले लेने भी शुरू कर दिए।
हमने इस समस्या को सुलझाने के लिए महिलाओं के परिवार वालों से बातचीत की और महिलाओं के लिए पारिवारिक ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर नक़दी फसल के बदले खाद्य फसलों को उगाने की अनुमति मांगी। अगर परिजन इसके लिए मान जाते थे तो हम महिलाओं को सलाह, तकनीकी प्रशिक्षण, बीज के लिए सरकारी सब्सिडी हासिल करना, खाद और पानी को बचाने के तरीक़े वगैरह सुझाते थे और उन्हें बाज़ार से जोड़ने का काम करते थे।
एक बार किसान बनने के बाद महिलाएं किसानी से जुड़े फ़ैसले भी लेने लग जाती हैं। वे तय करती हैं कि कौन सी फसल उगानी है, कितनी उगानी है, किसे बेचना है और किसे घर पर ही रखना है। वे खेती के बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थीं। बस वे यह नहीं जानती थीं कि इन्हे बेचना कैसे है। सामाजिक प्रतिबंधों के चलते वे बेहतरीन किसान होने के बावजूद अपनी फसल को बाज़ार तक ले जाने में सक्षम नहीं थीं। और समझने वाली बात है कि एग्रीगेशन, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग के बग़ैर अनाज को बड़े बाज़ारों में बेचना सम्भव नहीं था।
महामारी के दौरान लॉकडाउन और आवागमन में लगी रोक के चलते बाज़ार के तौर-तरीक़े बदल गए। अब वे हाइपर-लोकल हो गए और वहां गांव के ही या ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी गांव के लोग ख़रीद-बिक्री करने लगे। यह एक बड़ा बदलाव था। हमने यह देखना शुरू किया कि महिलाएं इस बदली हुई परिस्थिति का फ़ायदा कैसे उठा सकती हैं। हमने उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे अपने एक-एकड़ ज़मीन पर की जाने वाली खेती से आगे बढ़कर पूरे गांव के लिए सब्ज़ी और अनाज उगाने के बारे में सोचना शुरू करें। एक एकड़ ज़मीन पर होने वाली फसल महामारी के दौरान उनके परिवार के लिए पर्याप्त थी। इनमें से कई महिलाएं पहले से ही बीजों के उत्पादन और बिक्री का काम कर रही थीं। अगर किसी किसान के पास बीज हों तो वह कई महीनों तक परिवार का भरण-पोषण कर सकती है और कुछ पैसे भी कमा सकती है। बीज उत्पादन की तरह ही इन्होंने पशुपालन पर भी ध्यान देना शुरू किया। इस काम के लिए उनकी वरीयता में छोटे जानवर जैसे बकरी और मुर्गियां होती हैं क्योंकि इनसे जल्दी कमाई होने लगती है।
इस स्थिति का और अधिक फ़ायदा उठाने के लिए हमने इन किसानों को सामूहिक-स्तर के व्यवसाय करने के लिए एकत्रित किया। महिलाओं ने 200 से अधिक औरतों वाले समूह बनाकर क्लस्टर इंटरप्राइज बनाए। ये अपनी उपज को इकट्ठा कर आस-पास के बाज़ारों में ऊंचे और उचित मूल्यों पर बेचते थे। चूंकि ये बाज़ार या तो साप्ताहिक थे या फिर उनके गांव से अधिकतम 20 किमी की दूरी पर ही स्थित थे इसलिए महिलाओं के परिवारों को इनके बाहर जाने पर आपत्ति नहीं थी।
बिक्री का अनुभव मिल जाने के बाद कुछ महिलाएं और कुशल उद्यमी बन गईं और अपनी उपज बेचने के लिए दूर के बाज़ारों में भी जाने लगी। इसके बाद उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा।
महामारी के पहले ज़्यादातर महिलाएं गांवों में रहकर ही ग़ैर-कृषि गतिविधियों जैसे किराने की दुकान, ब्यूटी पार्लर और स्टेशनरी की दुकान वग़ैरह चलातीं थीं। बीते दो दशकों से सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वयं-सहायता समूहों के लिए दिए जाने वाले सहयोग से यह धारणा प्रबल हो गई थी कि केवल खेती से इतर या ग़ैर-कृषि गतिविधियों से ही विकास हासिल किया जा सकता है। शुरूआत में एसएसपी ने भी इसी सोच पर चलते हुए महिलाओं को बड़े पैमाने पर ग़ैर-कृषि गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। लेकिन कोविड-19 ने इस सोच और काम को बेमानी और ग़ैर-ज़रूरी बना दिया।
भोजन, राशन और स्वास्थ्य सुविधाएं लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य सेवाओं में शामिल थे जबकि अन्य व्यवसायों को इससे बाहर रखा गया था। इसलिए आपदा में मिले इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए हमने डेयरी, दलहन और जैविक खाद का उत्पादन करने और उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने सरीखे बड़े पैमाने के व्यवसायों की शुरुआत की। अकेले 2020 में ही हम लोगों ने खेती-किसानी करने वाली 10,000 से अधिक महिलाओं को बाज़ार का मुख्य हिस्सा बनने के लिए राज़ी कर लिया। दूध संग्रह केंद्रों की स्थापना हुई और इसके साथ ही महिलाओं को अपने फ़ोन पर इसकी क़ीमतों और भुगतान से जुड़ी जानकारियां मिलने लगीं। ऐसा होने से उनकी आय पर उनका नियंत्रण बढ़ने लगा।
और, कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री की दुनिया में प्रवेश से इन गांवों की एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन (कृषि उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया) में भी बदलाव आया।
महामारी के पहले एसएसपी के पास भारत के विभिन्न राज्यों में भूकम्प, बाढ़ और सुनामी जैसी भीषण आपदाओं से निपटने का दो दशकों से ज़्यादा का अनुभव था। हमारे अनुभवों से हमने यह सीखा था कि कोई भी संकट विकास को तेज करने का एक अवसर होता है। महामारी से पुरुष और महिलाएं समान रूप से प्रभावित हुए थे इसलिए दोनों ही चीजों को अलग तरीक़े से करने के लिए तैयार थे। नतीजतन इस आपदा से महिलाओं को अगुआई करने का मौक़ा मिला क्योंकि उनके अंदर अपने समुदाय के प्रति सेवा और कार्य का भाव अधिक प्रबल होता है। जहां सामान्य परिस्थितियों में उन्हें पीछे रहने को बाध्य किया जाता है वहीं संकट की घड़ी में उनके काम को स्कूल के शिक्षकों या ग्राम पंचायत के सदस्यों जैसे समुदाय के सभी प्रभावशाली सदस्यों द्वारा सराहा जाता है।

कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में कोई अंतर नहीं था। इस स्थिति ने हमें महिलाओं के नेतृत्व वाले बल सखी-टास्क फ़ोर्स बनाने के लिए प्रेरित किया। इन बलों ने ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने की तैयारियां और उसके असर से हुए आर्थिक नुक़सान से उबरने के लिए काम किया। हम 500 से अधिक गांवों में 5,000 सदस्यों को टास्क फ़ोर्स में शामिल कर सके। यह पहली बार था जब लोग महिलाओं की अगुआई को स्वीकार कर रहे थे।
महामारी ने डिजिटल तकनीक की अहमियत की ओर भी ध्यान दिलाया है। जहां कोविड-19 के दौरान महिलाएं राहत कार्य, सुरक्षा, जागरूकता और टीकाकरण जैसे कामों में जुड़ी थीं। वहीं लॉकडाउन वाले दिनों में उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर होने का महत्व समझ में आया। महामारी के पहले हमने उन्हें डिजिटल उपकारणों के इस्तेमाल के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित किया था लेकिन तब वे इसके लिए तैयार नहीं थीं।
दस साल पहले हमने माइक्रोफ़ाइनांस, कौशल विकास और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के लिए सामाजिक उपक्रम तैयार किया था। इस प्रक्रिया में हमने इन महिलाओं को उद्यमी और अगुआ बनने में सक्षम करने पर ध्यान दिया था। आर्थिक सशक्तिकरण और लीडरशिप तैयार करने में किया गया हमारा निवेश सार्थक रहा।
जब महामारी आई तो महिलाओं ने ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। हम भले ही आगे की योजनाओं को लेकर आशंकित थे लेकिन महिलाएं नहीं। इन महिलाओं को अपने समुदायों की ज़रूरतें समझने, राहत कार्यों को शुरू करने, मनरेगा योजना के तहत अपने समुदाय के लोगों के लिए राशन और नौकरी जैसे सरकारी लाभ मुहैया करवाने के तरीक़ों की जानकारी थी और इसीलिए ये अपने लोगों की मदद कर पाईं। हमने सिर्फ़ एक इकोसिस्टम बनाया था लेकिन महिलाएं इसका इस्तेमाल जानती थीं और उन्होंने इसका ज़िम्मा ले लिया।
जब एसएसपी ने आजीविका का काम शुरू किया तो अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की तरह ही हम भी महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी सर्विस वग़ैरह का प्रशिक्षण देने पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन जल्द ही हमें एहसास हो गया कि सिर्फ़ प्रशिक्षण मिलने से इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है–इससे उन्हें अपना काम शुरू करने में मदद नहीं मिलती है। इसलिए एक दशक पहले हम लोगों ने अपना रास्ता बदला और महिलाओं के अंदर छिपे उद्यमियों की पहचान के लिए उनके गांवों में व्यावसायिक शिक्षण (रूरल बिज़नेस एजुकेशन) शुरू किया। व्यवसायी मानसिकता एक महत्वपूर्ण चीज है और महिलाओं को व्यवसायियों की तरह सोचने के लिए प्रेरित कर पाना, हमारे मामले में काम कर गया।
लगभग पांच साल पहले जब महिला किसानों की एक बड़ी संख्या ने कृषि के इस मॉडल को अपनाया तब हमने इन महिलाओं को एक बार फिर से कृषि को एक उपक्रम के तौर पर देखने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे-धीरे हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण और माइक्रोफाइनेंस को कम कर दिया। अधिकांश स्वयंसेवी संस्थाएं और नबार्ड जैसी सरकारी एजेंसियां भी ग्रामीण और सुदूर इलाक़ों में ग़ैर-कृषि उद्यमों तक सीमित हो गई थीं। ये संस्थाएं इस विचार से प्रभावित थीं कि पैसा सिर्फ़ शहरों में है और कुशल लोग भी शहरों में ही मिलते हैं। इसलिए उन्होंने शहरी कौशलों और शहरी उपक्रमों के तरीकों की नक़ल की और उसे ग्रामीण भारत में लागू कर दिया। नतीजतन, खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था के महत्व का सही मूल्यांकन नहीं हुआ और इस क्षेत्र में निवेश में कमी आने लगी। हम सब जानते हैं कि खेती-किसानी की हालत बहुत नाज़ुक है और इसे सहारे की ज़रूरत है। लेकिन अपने काम के अनुभवों से हमने पाया कि यदि महिलाओं को आर्थिक सहयोगियों के रूप में गंभीरता से लिया जाए और कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों को आजीविका का मुख्य साधन बनाया जाए तो हमारे पास अवसरों की कमी नहीं है।
एसएसपी इससे कोई अलग नहीं था। जब 2015 में मराठवाड़ा में सूखा पड़ा तो महिलाओं ने हमसे कहा कि उनके पास खाने के लिए नहीं है। उस समय हमने सही मायनों में उनके साथ खेती से जुड़े काम करना शुरू किया। हम सबसे पहले परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिर्फ़ रसोई और घर के बगीचों पर ध्यान देने की बजाय हमने तय किया कि महिलाओं को खेतों में जाकर फसल उगाना चाहिए। उन्हें अपनी उगाई फसल ही खानी चाहिए और इसे जैविक, पानी के कम खर्च और कम लागत वाले तरीक़े से ही करना चाहिए। हम लगातार अपने काम के प्रभाव का आकलन कर रहे थे और हमने पाया कि पहले जहां केवल 10 प्रतिशत परिवार ही अपने खेतों में उगायी सब्ज़ियों और फसलों का इस्तेमाल करते थे वहीं अब यह आंकड़ा 70 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। परिवार के लोगों को यह एहसास होने लगा कि वे पहले से अधिक स्वस्थ हो गए हैं। इसलिए साल दर साल लोगों के लिए खेती के इस मॉडल को अपनाना आसान हो गया। नतीजतन, 2016 से 2020 तक हमारे पास एक लाख से अधिक संख्या में ऐसे छोटे और पिछड़े किसान परिवार थे जिनमें महिलाएं खेती करती थीं।
हमें निजी क्षेत्र में उपलब्ध क्षमताओं का भी उपयोग करना चाहिए जिसमें महिला किसानों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और अन्यक्षमताएं हैं।
हमारा शुरूआती उद्देश्य खाद्य सुरक्षा था। लेकिन जल्द ही हम इस बात को समझ गए थे कि एक बार अपने परिवारों के लिए खेती शुरू करने के बाद महिलाएं बड़े पैमाने पर इस काम को करने के साथ ही बाज़ारों के लिए भी उसी स्थाई तरीक़े से खेती कर सकती हैं। यही वह समय था जब हमने महिलाओं को सही मायनों में किसानों के रुप में देखना शुरू किया और उन्हें खेती और फ़ूड वैल्यू चेन में आगे बढ़ाया। यहां वे खेतिहर से आगे बढ़कर उत्पादकों में शामिल हो जाती हैं और खरीद, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अब अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर दिया है। उन्हें लगने लगा है कि महिलाओं को संगठित करने के काम में उन्होंने जो प्रयास किया है, उसे अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। यहां से महिला किसान उत्पादक संगठन खेती और उससे जुड़े व्यवसाय जैसे मुर्गी पालन और डेयरी जैसे काम करना शुरू कर देंगे।
कोविड-19 ने कृषि से जुड़े उपक्रमों और अनिवार्य न होने वाले व्यवसायों के बीच की समझ और विभाजन को और साफ़ किया है। ऐसे उपक्रम जो खेती से जुड़े हुए नहीं थे, उन्हें भारी नुक़सान हुआ और वे बंद हो गए। सिर्फ़ कृषि-संबंधित उद्यम ही खुद को बचा पाए क्योंकि कृषि सिर्फ़ खाद्य सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक स्थायी और टिकाऊ आजीविका है।
अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां हमने ऐसे चार किसान उत्पादक कंपनियां बनाई हैं जिनकी कर्ताधर्ता महिलाएं हैं। महिलाएं दाल और अनाज सरीखे स्थानीय उत्पादों का महत्व बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना भी कर रही हैं। उन्होंने वर्मीकम्पोस्ट जैसे उत्पादन भी शुरू कर दिये हैं। अब हम इन कामों की जटिलता को बढ़ा रहे हैं। इसमें अब हम पानी का मुद्दा भी जोड़ रहे हैं जिसके तहत उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके समुदायों में जल के स्त्रोत और उनका प्रबंधन स्थायी है। अब हमारा ध्यान इस पर ही है।
हमें निजी क्षेत्र में उपलब्ध क्षमताओं का भी उपयोग करना चाहिए। इसमें ऐसा बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षमताएं हैं जो महिला किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। एसएसपी में हम लोग 2006 से ही टेक कम्पनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम बायोगैस तकनीकों, सौर प्रकाश की मार्केटिंग जैसे मामलों में महिलाओं की मदद कर सकें। हालांकि हमने पहले से स्थापित और नई शुरू होने वाली (स्टार्ट-अप्स), दोनों ही तरह की कंपनियों के साथ साझेदारी की है। लेकिन हम स्टार्ट-अप को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इनके साथ मिलकर हम लोग क़ीमत, फ़ंडिंग और उत्पाद की खूबियों को ध्यान में रखकर ग्रामीण समुदायों के लिए नए उत्पाद तैयार कर सकते हैं।
एसएसपी आजीविका के लिए इकोसिस्टम तैयार करने का तरीक़ा अपनाता है। इसका मतलब यह है कि हम महिलाओं को प्रशिक्षण देने के जाल में नहीं फंसते हैं। सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं दोनों में ही प्रशिक्षण पर बहुत अधिक ध्यान देने का चलन है। संगठनों को यह समझना चाहिए कि केवल प्रशिक्षण से कुछ नहीं होता है। आपको फाइनेंशियल और मार्केट लिंक भी मुहैया करवाने की ज़रूरत है। इसके बिना किसी तरह की उद्यम क्षमता नहीं पैदा की जा सकती है।
इसके बाद अगला महत्वपूर्ण कदम महिलाओं को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक़ दिलवाना है ताकि लोग उन्हें उत्पादक और किसान के रूप में देख सकें। ज़मीन पर मालिकाना हक़ मिल जाने से महिलाओं को उन मुख्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगता है जिनके हक़दार केवल ज़मीन के मालिक होते हैं। महिलाओं को किसानों और उत्पादकों के रूप में स्वीकार किए जाने की ज़रूरत है। फसल के चुनाव आदि का फ़ैसला उन्हें ही लेने दिया जाना चाहिए।
आजीविका से उद्यम तक ग्रामीण महिलाओं ने एक लम्बा सफ़र तय किया है। उन्हें मुख्य पड़ावों पर समुदायिक सहायता प्रणाली (कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम) से लाभ मिलेगा जिसमें उनका परिवार, साथ काम करने वाले उद्यमी और संस्थाएं शामिल हैं। दानकर्ताओं और सुविधा प्रदाताओं को भी इसका श्रेय जाता है क्योंकि वे भी इस महत्वपूर्ण और समावेशी इकोसिस्टम के सह-निर्माता हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि महिलाओं को केवल आय अर्जित करने वाले, छोटे स्तर का कर्ज़ लेने वाले या स्वरोजगार करने वालों के रूप में न देखा जाए बल्कि अर्थव्यवस्था के भावी सहायकों और जिम्मेदारों के रूप में देखा जाए। वह वक्त आ गया है जब हमें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए।
यह इंटरव्यू उपमन्यु पाटिल के योगदान से पूरा हुआ।
इस इंटरव्यू को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
22 दिसम्बर 2021 को बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम 2021 संसदीय कमेटी को चर्चा के लिए भेजा गया। यह अधिनियम लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम क़ानूनन आयु को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की सिफ़ारिश करता है। साफ है कि इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह की प्रथा पर अंकुश लगाना है। लेकिन इस बात के सबूत न के बराबर हैं कि केवल एक क़ानून बनाकर ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि लड़कियों की शादी की क़ानूनी उम्र 18 साल होने के बावजूद देश भर से बाल विवाह की ख़बरें आती रहती हैं। ऐसे में सवाल किया जा सकता है कि क्या क़ानून का सहारा लेना ही बाल विवाहों को रोकने का एकमात्र कारगर रास्ता है?
यूनिसेफ़ द्वारा निर्धारित बाल विवाह की परिभाषा पर गौर करें तो “एक ऐसा विवाह जिसमें लड़की या लड़के की उम्र 18 वर्ष से कम हो, बाल विवाह कहलाता है। इसमें औपचारिक या अनौपचारिक, दोनों तरह की वे व्यवस्थाएं शामिल हैं जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एक-दूसरे के साथ शादीशुदा जोड़े की तरह रहते हैं।” बाल विवाह समाज में गहरे बैठी सामाजिक-सांस्कृतिक रूढ़ियों और लैंगिक असमानता का परिणाम है जिसका नुक़सान सबसे अधिक लड़कियों को उठाना पड़ता है।
भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों की परवरिश का अंतिम लक्ष्य अक्सर उनकी शादी होता है। आमतौर पर उन्हें सिर्फ़ घर के कामों तक ही सीमित रखा जाता है और उनसे पढ़ाई-लिखाई करने या नौकरी करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसलिए उनकी शादी हो जाने तक परिवार वाले उन्हें आर्थिक बोझ की तरह देखते हैं। यही कारण है कि लड़कियों की शादी जल्दी करवा देना न केवल परम्परा के अनुसार सही माना जाता है बल्कि आर्थिक रूप से भी अधिक व्यावहारिक होता है। इसके अलावा ग़ैर-शादीशुदा संबंधों से गर्भधारण का ख़तरा भी एक ऐसी वजह है जो लड़की की शादी में रुकावट पैदा कर सकती है। इससे वे अनिश्चित समय के लिए परिवार पर एक आर्थिक बोझ बन जाती हैं। इन तमाम वजहों के चलते ज्यादातर समुदाय बाल विवाह को एक समस्या नहीं बल्कि समाधान मानते हैं।
ग़ैर-क़ानूनी होने के बावजूद भारत में बाल विवाह को सामाजिक मंज़ूरी मिली हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) ने हाल ही में अपने पांचवें दौर का सर्वेक्षण जारी किया है। इस सर्वेक्षण में भारत की 20 से 24 साल आयुसमूह की शादीशुदा महिलाओं में से एक चौथाई महिलाओं की शादी 18 साल से कम उम्र में होने की बात सामने आई है। एनएफएचएस द्वारा इससे पहले 2015–16 में यह सर्वे किया गया था जिससे हालिया सर्वे की तुलना करें तो बाल विवाह के मामलों में बहुत ही मामूली कमी आने का पता चलता है। ऐसा तब है जब मौजूदा बाल विवाह क़ानून को लागू हुए चार दशक से अधिक का समय बीत चुका है। हालांकि 2005–06 और 2015–16 के बाल विवाह के आंकड़ों पर गौर करें तो असरदार कमी देखने को मिलती है लेकिन इसमें क़ानून की बजाय शिक्षा के बेहतर मौकों एवं अन्य कारकों का योगदान अधिक प्रतीत होता है।1

लड़कियों की शादी की क़ानूनी उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने के इस प्रस्ताव के कई दुष्परिणाम हो सकते हैं।
पार्ट्नर्स फ़ॉर लॉ इन डेवलपमेंट द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार मौजूदा बाल विवाह क़ानून के तहत दर्ज मामलों में से 65 फ़ीसदी घर से भागने (ज़रूरी नहीं कि इसमें शादी ही कारण हो) के चलते दर्ज करवाए गए थे। इनमें से ज़्यादातर शिकायतें असहमत माता-पिता या परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थीं। इन मामलों में क़ानून का ग़लत इस्तेमाल उन जोड़ों को परेशान करने के लिए किया गया जिनकी शादियां क़ानूनन सही हैं। ये आंकड़े इस बात की आशंका पैदा करते हैं कि विवाह की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने से उन युवाओं की संख्या बढ़ेगी जो इस तरह के उत्पीड़न से बचने के लिए जल्दी विवाह का विकल्प चुन लेते हैं। इसके साथ ही इससे लोगों के पास अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाहों के विरोध के लिए एक और साधन उपलब्ध हो जाएगा।
पारिवारिक क़ानून के सुधार के विषय में 2008 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की गई थी कि लड़के एवं लड़कियों दोनों के लिए ही विवाह की समान उम्र 21 साल नहीं बल्कि 18 साल होनी चाहिए। इसके पीछे का तर्क दिया गया था कि यदि सभी नागरिक 18 की उम्र में मतदान कर सकते हैं, अभिभावक बन सकते हैं और अपराध करने की स्थिति में वयस्क की श्रेणी में रखे जाते हैं तो उन्हें 18 साल में शादी करने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? इस बात की पूरी संभावना लगती है कि नए क़ानून से ज़्यादातर महिलाओं की चुनाव या पसंद की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है।
वर्तमान सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में लोग न केवल जल्द से जल्द बेटियों की शादी करवा देना चाहते हैं बल्कि अगर हो सके तो बेटियां पैदा ही नहीं करने का विकल्प चुनते हैं। हमारे पितृसत्तात्मक समाज की मान्यताओं को बदले बग़ैर विवाह की क़ानूनी उम्र को बढ़ाना माता-पिता में ‘बोझ’ वाली भावना को मज़बूत बना सकता है। इसके चलते गर्भ में ही या जन्म के तुरंत बाद लड़कियों को मार दिए जाने जैसी कुप्रथाओं में वृद्धि हो सकती है।
दुनिया भर में बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए कई सफल रणनीतियां अपनाई गई हैं। नीचे ऐसे ही कुछ उपायों का ज़िक्र है जो भारत जैसे देश में कारगर हो सकते हैं।
हम 2008 लॉ कमीशन के सुझाव का समर्थन करते हैं। यह लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शादी की न्यूनतम आयु समान कर, 21 की बजाय 18 साल करने की बात करता है। अगर लोग 18 साल की उम्र में मतदान कर सरकार चुन सकते हैं तो उन्हें अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार भी इसी उम्र में मिल जाना चाहिए।
इस बात के साफ प्रमाण हैं कि लड़कियों को उनकी शिक्षा पूरी करने का मौक़ा मिले तो उनकी शादी में देरी होती है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनती हैं। एनएफ़एचएस-4 की रिपोर्ट के मुताबिक़ स्कूली शिक्षा प्राप्त न करने वाली लड़कियों के लिए शादी की औसत उम्र जहां 17.2 साल है वहीं 12वीं या उससे अधिक पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए विवाह की औसत उम्र 22.7 साल है। शिक्षा लड़कियों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने और गरिमापूर्ण जीवन जीने के योग्य बनाती है। इसके अलावा, इससे लड़कियों को अपनी मर्ज़ी से शादी करने और शादी में यौन संबंध बनाने या बच्चा पैदा करने के अपने अधिकार को क़ायम रखने की समझ भी मिलती है।
किशोर लड़कियों में आर्थिक रूप से सक्षम हो सकने का विश्वास जगाने के लिए उनकी क्षमता एवं कौशल निर्माण में निवेश करना बहुत आवश्यक है।
बाल विवाह का संबंध शिक्षा के निचले स्तर, ग़रीबी और ग्रामीण आवास से जुड़ता है। एनएफ़एचएस-4 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाली ऐसी लड़कियां जो गरीब घरों से हैं और जिन्हें शिक्षा नहीं मिली है, उनकी शादी 18 वर्ष से पहले किए जाने की संभावना ज्यादा होती है। सरकार को लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई की राह में आने वाली रुकावटों पर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और एक ऐसी व्यवस्था बनाने की दरकार है जिससे लड़कियों की शिक्षा में किया गया निवेश माता-पिता के लिए उपयोगी साबित हो सके।
लड़कियों को उनके इकनॉमिक पोटेंशियल यानी अर्थव्यवस्था में उपयोगी हो सकने का यकीन दिलाने के लिए किशोरवय से ही उनकी क्षमता एवं कौशल निर्माण में निवेश किया जाना बहुत आवश्यक है। आर्थिक सशक्तिकरण से अक्सर लोगों को अपने घरों में अधिक महत्व मिलता है और वे अपने भविष्य से जुड़े फ़ैसले लेने में सक्षम और ज़िम्मेदार माने जाने लगते हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर लड़कियां कम उम्र में होने वाली शादी के लिए मना कर सकती हैं और परिवार में बोझ की तरह भी नहीं देखी जाती हैं। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिए जाने की ज़रूरत है कि लड़कियों एवं महिलाओं के लिए काम के ऐसे सुरक्षित अवसर बनाए जाएं जिनसे उनकी आय भी हो सके।
बाल विवाह को समाप्त करने की कोशिशों में एक तरीक़ा टारगेटेड एसबीसीसी में निवेश करना हो सकता है। एसबीसीसी में सामान्य माने जानी वाली सामाजिक और व्यवहारगत रूढ़ियों की पहचान कर और उन पर बात कर उन्हे बदलने की कोशिश की जाती है। इसका एक उदाहरण शादी से जुड़े फ़ैसलों में लड़कियों एवं लड़कों को बाहर रखे जाने का है।
पॉप्युलेशन फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया की प्रमुख एसबीसीसी पहल ‘मैंहूं’ के नतीजे बताते हैं कि इन संदेशों के जरिए बाल विवाह से जुड़े ख़तरों के बारे में जागरूकता बढ़ी है। साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले माता-पिता और लड़कियों के व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। हमें व्यापक स्तर पर एसबीसीसी जैसी पहलों की ज़रूरत है। बेहतर होगा अगर इन्हें स्थानीय स्तर पर राजनीतिक, सामुदायिक या धार्मिक नेताओं का समर्थन हासिल हो। ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले संस्थागत भेदभाव और कमतर समझे जाने वाली धारणाओं से छुटकारा दिलाने पर काम किया जा सके।
बाल विवाह का शिकार सबसे अधिक पिछड़े समुदायों की लड़कियां बनती हैं। एनएफ़एचएस-4 के अनुसार सामान्य वर्ग की महिलाओं की शादी देर से होती है। सामान्य वर्ग में 25–49 वर्ष की औरतों की शादी की औसत आयु 19.5 साल है। यह आंकड़ा अन्य पिछड़े वर्ग की औरतों के लिए 18.5 साल, अनुसूचित जनजातियों के लिए 18.4 साल एवं अनुसूचित जातियों के लिए 18.1 साल है। हमें बड़ी संख्या में ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों की ज़रूरत है जो विशेष रूप से पिछड़े समुदायों की लड़कियों, युवा महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक संस्थानों, शिक्षा, सूचना, पोषण और स्वास्थ्य (यौन, प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य सहित) सेवाओं से जोड़ने का काम करे।
विवाह के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद राज्य सरकारों ने इस फ़ैसले को लागू करने के लिए बहुत कम काम किया है। इसलिए सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सभी तरह की शादियों (कानूनी, धार्मिक और परम्परागत संबंध), जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करवाना अनिवार्य हो ताकि इससे शादियों और नवविवाहितों की उम्र पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह को संभव बनाने और अधिकृत करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।
बाल विवाह को समाप्त करने के लिए उठाया गया कोई भी कदम लड़कियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए होना चाहिए, ख़ासकर ऐसी लड़कियों के लिए जिनका बाल विवाह होने की सम्भावना अधिक होती है। हमें दंडात्मक कार्यवाहियों और क़ानूनी तरीक़ों से अलग हटकर उन तरीक़ों के बारे में सोचना होगा जो बाल विवाह को बढ़ावा देने वाली पितृसत्तात्मक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को बदलने में मददगार साबित हों।
—
फुटनोट:
इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।
—
31 जून 2021 को महामारी के दिनों में असंगठित मज़दूरों के संघर्षों से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई हुई। इसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों का डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस फ़ैसले के जवाब में अगस्त 2021 में सरकार ने असंगठित मज़दूरों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की।
ई-श्रम का लक्ष्य और इसके पीछे का विचार काफ़ी अच्छा है। ऐसा कोई भी व्यापक आँकड़ा नहीं है जो भारत भर में अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले मज़दूरों से जुड़ी जानकारियाँ प्रदान करता हो। हालाँकि ई-श्रम पोर्टल पर मज़दूर का नाम, पेशा, पता, शैक्षणिक योग्यता, कौशल के प्रकार और परिवार की जानकारी उपलब्ध होती है। इसमें निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूर, घरेलू सहायक, रेहड़ी-पटरी वाले, ब्यूटिशियन, वेटर, रिक्शा चालकों के साथ ऐसे अन्य मज़दूर शामिल होते हैं जिन्हें अमूमन सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और नीतियों के बारे में मालूम नहीं होता है और वे इन फ़ायदों से वंचित रह जाते हैं।
सरकार ने ई-श्रम रजिस्ट्रेशन के लिए देशव्यापी जागरूकता अभियानों में काफ़ी धन निवेश किया है। इसके लिए जगह-जगह इसके प्रचार में बैनर लगाए गए हैं और ज़मीनी स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। खबरों के रिपोर्ट के अनुसार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नवम्बर 2021 के अंत तक असंगठित क्षेत्र के 380 मिलियन मज़दूरों में से 91 मिलियन मज़दूरों ने इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। हालाँकि ये सब आँकड़े हैं। सच्चाई यह है कि ई-श्रम रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है और इसके फ़ायदों को लेकर मज़दूर वर्ग में ढ़ेरों भ्रम और आशंकाएँ हैं।
ई-श्रम पोर्टल पर सेल्फ़-रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नम्बर आवश्यक है। यह योग्यता प्रवासी मज़दूरों के लिए अपने आप में एक बड़ी समस्या है क्योंकि अपने काम के कारण इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। और इसी कारण वे समय-समय पर अपना सिम कार्ड भी बदल लेते हैं। दिल्ली में असंगठित मज़दूर संघों के लिए बनाए गए संगठन दिल्ली श्रमिक संगठन के संस्थापक सदस्य रमेंद्र कुमार का कहना है कि “प्रवासी मज़दूर अपने मोबाइल नम्बर को स्थायी नहीं मानते हैं। वे कई कारणों से अपने नम्बर बदलते रहते हैं। जैसे कि अपने गाँव वापस जाने पर वे अपना नम्बर बदल लेते हैं, कई बार उनका मोबाइल गुम जाता है या चोरी हो जाता है। कई मामलों में ऐसा भी होता है कि यदि उनके काम करने वाले इलाक़े में जियो का नेटवर्क बेहतर है तो वे अपना वोडाफ़ोन का सिम फेंककर जियो का नया सिम ख़रीद लेते हैं।”

अगर मज़दूर के पास आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल फ़ोन नहीं है तो उसे इलाक़े के अनुमंडल पदाधिकारी के दफ़्तर में जाकर अपना मोबाइल दोबारा लिंक करवाना होता है। इसके लिए उसके बायोमेट्रिक सत्यापन की ज़रूरत होती है जिसकी अपनी चुनौतियाँ हैं। कुमार बताते हैं कि “बहुत लम्बी लाइन होती है और एक दिन में केवल 60 मज़दूरों का ही आधार लिंक हो पाता है। इसका दूसरा विकल्प सार्वजनिक सेवा केंद्रों पर जाना है।”
ऐसे भी कई मामले हैं जहां कई मज़दूर एक ही जगह रहते हैं और एक ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार एक मोबाइल नम्बर से तीन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन फिर बैंक अकाउंट की समस्या खड़ी हो जाती है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक चालू खाता होना ज़रूरी है जो मज़दूर के अपने आधार कार्ड से जुड़ा हो। सरकार द्वारा शुरू की गई जन धन योजना के तहत पिछले कुछ सालों में मज़दूरों के बैंक खाते खुले थे लेकिन उनमें से अधिकतर खाते निष्क्रिय अवस्था में हैं।
अन्य मामलों में उनके बैंक अकाउंट उनके आधार से नहीं जुड़े होते हैं। हक़दर्शक नागरिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने वाला एक संगठन है। इस संगठन के लिए मुंबई में ई-श्रम रजिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी उठाने वाले केदार अन्नम बताते हैं कि “लोगों के पास अक्सर अपना निजी बैंक अकाउंट नहीं होता है। वे सामूहिक बैंक अकाउंट से अपना काम चलाते हैं। इसलिए यदि किसी मज़दूर ने सामूहिक बैंक अकाउंट के नम्बर का इस्तेमाल करके अपना ई-श्रम कार्ड बनवाया है तो हम उसी नम्बर से उसकी पत्नी के लिए नया कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम इसे स्वीकार नहीं करता है।”
शीला दिल्ली के सरिता विहार में घरेलू सहायिका है। वह अपना ई-श्रम कार्ड बनवाना चाहती है क्योंकि उसने अपने सहकर्मियों से इससे होने वाले आर्थिक फ़ायदों के बारे में सुना था। उसके लिए पैसा अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि महामारी के दौरान उसकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उसे काम से निकाल दिया गया।
हालाँकि अपनी उम्र की वजह से ही शीला का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। वह 60 साल की है और ई-श्रम पर केवल 16 से 59 साल के बीच के लोगों का ही रजिस्ट्रेशन सम्भव है। भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले प्रवासी मज़दूरों पर लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनोमिक्स में शोध कर रही हर्षिता सिन्हा हमें बताती हैं कि “बहुत सारे लोग छूट जाएँगे क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में 60 साल की उम्र से ज़्यादा के मज़दूर भी काम करते हैं।” कम-आय वाले लोगों के पास सेवानिवृति का विकल्प नहीं होता है। यह एक ऐसा बिंदु है जिसपर नीति निर्माताओं का ध्यान नहीं गया है। अन्नम चेतावनी देते हुए कहते हैं, “ऐसा कई बार होता है जब मज़दूर के आधार कार्ड पर उसकी जन्मतिथि ग़लत लिखी होती है। इसलिए चाहे उनकी वास्तविक उम्र कुछ भी हो, ग़लत काग़ज़ के कारण उनका रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पर नहीं हो पाता है।”
सबसे दिलचस्प स्थिति वह होती है जब मज़दूर बिना किसी अधिक परेशानी के ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अन्नम कहते हैं, “ऐसे जवान मज़दूर जो किसी संघ या समूह का हिस्सा होते हैं उनके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़े होते हैं। 35 से अधिक उम्र वाले मज़दूरों को इसमें परेशानी होती है।” कुमार अपनी सहमति जताते हुए कहते हैं कि “औपचारिक रूप से शिक्षित और डिजिटल ज्ञान रखने वाले मज़दूरों का संघर्ष कम है।”
हालाँकि ई-श्रम की पूरी अवधारणा ही अनौपचारिक श्रमिकों की आबादी का डेटाबेस तैयार करना है लेकिन बावजूद इसके इसमें रजिस्ट्रेशन की योग्यता को लेकर कई तरह के संशय हैं। अन्नम कहते हैं, “सबसे बड़ी चिंता पोर्टल पर की गई वर्गीकरण से जुड़ी है। चूँकि कुछ पेशों के लिए निश्चित श्रेणी तय नहीं की गई है इसलिए हमें एक साझे पेशे पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम नहीं जानते हैं कि निर्माण क्षेत्र में सहायक के रूप में काम करने वाले मज़दूर को किस श्रेणी में रखा जाएगा। ‘सहायक’ नाम से एक आम श्रेणी है लेकिन वह सिर्फ़ कपड़ा उद्योग में काम कर रहे कपड़ा मज़दूरों के लिए है। सफ़ाई, निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में सहायक वाली श्रेणी नहीं है। जब लोगों को सूची में अपना पेशा दिखाई नहीं पड़ता है तब वे ‘सहायक’ वाली श्रेणी चुन लेते हैं।” अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि अनौपचारिक रोज़गार में अक्सर दोहरा काम होता है और चूँकि पोर्टल की सूची में दूसरे पेशे वाली श्रेणी उपलब्ध नहीं है इसलिए लोग ग़लत विकल्प चुन लेते हैं।
सिन्हा इस बात से सहमत हैं कि श्रेणियों में मज़दूरों का एक अलग प्रतिनिधित्व हो सकता है जिसे पहचाने जाने की ज़रूरत है, “ड्राइवर, घरों में सफ़ाई का काम करने वाले लोग या बड़े-बड़े घरों में काम करने वालों के सहायक के रूप में काम करने वाले लोगों को घरेलू काम की श्रेणी में डाला जाता है। इसकी वजह से उनके प्रतिनिधित्व में थोड़ा बदलाव आ जाता है। एक दूसरी समस्या है कि कुछ श्रेणियों का हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद ग़लत है। जैसे कि अगर आप निर्माण वाली जगह पर कारीगरी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उसके लिए ई-श्रम पोर्टल पर किसी तरह की श्रेणी उपलब्ध नहीं है।”
इसके अलावा भी कई समस्याएँ हैं। ऐसे मज़दूर जिनका प्रॉविडेंट फंड अकाउंट है वह अपना रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पर नहीं कर सकते हैं। हालाँकि ऐसे लोगों की पहचान करना आसान नहीं है। हक़दर्शक के ऑपरेशंस के एसोसियेट वाइस-प्रेसिंडेट संजय परमार कहते हैं कि “दो प्रकार के पीएफ़ खाता धारक हैं: ऐसे लोग जो स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और वो लोग जो कांट्रैक्ट पर काम करते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग तीन महीने एक जगह तो छः महीने दूसरी जगह काम करते हैं इसलिए उनका पीएफ़ अकाउंट बदलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि वे जिस कम्पनी में काम करते हैं वहाँ सरकारी नियमों के तहत उनके पीएफ़ अकाउंट खुल तो जाते हैं लेकिन नियोक्ता उनमें पैसे जमा नहीं करवाते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पर करवाने में मदद करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहले औपचारिक क्षेत्रों में काम किया है और वे पीएफ़ के हक़दार रह चुके हैं लेकिन अब नहीं हैं।”
परमार बताते हैं कि “कभी-कभी लोग झूठ भी बोलते हैं। उनका पीएफ़ अकाउंट सक्रिय होता है लेकिन वे मुकर जाते हैं। पीएफ़ पोर्टल पर इन चीजों की जाँच की सुविधा नहीं है।”
मज़दूरों के मन में आशंका है लेकिन उन्हें उम्मीद भी है। दिल्ली के पश्चिम विहार में निर्माण कार्य करने वाले उमेर सिंह ने कहा कि “मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा कि उनके खाते में पैसे आते हैं।” वह घरेलू सहायिका का काम करने वाली अपनी पत्नी का भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सरिता विहार के घरों में काम करने वाली पुष्पा ने भी इसी उम्मीद में ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसने कहा कि वह किसी ऐसे आदमी को जानती है जिसके एक जानने वाले को ई-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद अकाउंट में पैसे मिले हैं।
इस भ्रम का कारण ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 1.5 करोड़ मज़दूरों के खातों में आने वाले वह 1,000 रुपए है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान सभा चुनावों के पहले प्रत्येक मज़दूर को दिए थे। यह पैसा उन प्रवासी मज़दूरों के खातों में भी आया था जो दिल्ली जैसे पास के राज्यों में रहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से स्थानीय समुदाय के लोगों में एक झूठी उम्मीद पैदा हो गई है।
हालाँकि कई मज़दूर अब भी सावधान हैं। सिन्हा बताती हैं कि “मैंने मज़दूरों को कहते सुना है कि ‘आप लोग हमसे हमारी जानकारियाँ ले रहे हैं; इससे हमें कोई समस्या तो नहीं होगी न? क्या हमारे पैसे कटेंगे? हमें क्या मिलेगा?’” ऐसी अफ़वाहें भी उड़ाई गई कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों के खाते से पैसे कट गए। इन अफ़वाहों ने आग में घी का काम किया और मज़दूरों के मन में बैठी आशंकाएँ और अधिक प्रबल हो गईं।
इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि ई-श्रम जैसे डिजिटल उत्पाद श्रमिक और मज़दूर वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। ई-श्रम ‘कार्ड’ एक सॉफ़्ट कॉपी होती है। ऐसा संभव है कि रजिस्ट्रेशन के बाद किसी को उसका भौतिक कार्ड न मिल पाए। अन्नम कहते हैं कि “कार्ड पीडीएफ़ फ़ाइल के रूप में आती है और अक्सर लोग इसकी महत्ता नहीं समझते हैं। हमें इस पीडीएफ़ का प्रिंट निकालकर उन्हें देना पड़ता है ताकि उन्हें इस बात की तसल्ली हो कि उन्हें कुछ मिला है।”
ई-श्रम के फ़ायदों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों में अस्पष्टता होने के कारण इससे मदद नहीं मिल पाती है। जन साहस हाशिए के मज़दूरों के अधिकारों की सुरक्षा पर काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है। इसके तेलंगाना इकाई में काम करने वाले मोहम्मद असद का कहना है कि “हम लोगों को लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अब तक का एकमात्र फ़ायदा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा से मिलने वाला बीमा है। इस बीमा के तहत दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए की राशि और दुर्घटना के कारण विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। लेकिन समुदाय के लोगों का मानना है कि भविष्य में ज़्यादा फ़ायदा ई-श्रम से मिलेगा।” पोर्टल पर उपलब्ध बाक़ी सब पहले की योजनाएँ हैं, इन योजनाओं में जीवन ज्योति योजना या आयुष्मान भारत योजना है। इनका लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रत्येक योजना के पोर्टल पर जाकर अलग-अलग आवेदन करना पड़ता है।
लेकिन ई-श्रम की लोकप्रियता से इंकार नहीं किया जा सकता है। मुश्किलों और इसकी जटिलताओं के बावजूद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेवा केंद्रों और कैम्पों में मज़दूरों की भीड़ लगी होती है। जन साहस के माइग्रेंट्स रेज़िल्यन्स कलैबरेटिव में सामाजिक सुरक्षा की प्रमुख गरिमा साहनी ने कहा कि “हमें शायद यह देखकर आश्चर्य हो सकता है कि लोग एक ऐसे कार्ड के लिए क़तारों में क्यों खड़े हो रहे हैं जो सिर्फ़ एक बीमा का वादा करता है। लेकिन हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पेंशन पाने की कोशिश में लगा दिया पर उन्हें फिर भी उनका पेंशन नहीं मिला। या फिर लोगों ने अपने बीओसीडबल्यू कार्ड के लिए सरकारी दफ़्तरों के हज़ार चक्कर लगाए लेकिन उन्हें उनका कार्ड नहीं मिल पाया। अगर सरकार उन्हें किसी काम के अनुभव, स्थायी पता या ऐसे ही हज़ार तरह के काग़ज़ों के बिना ही कार्ड दे रही है तो वे लेंगे ही।”
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
परोपकार पर होने वाली चर्चाएँ मुख्य रूप से उच्च आय वर्ग वाले लोगों (हाई नेट वर्थ इंडिविजूअल्स या एचएनआई) या अपने कॉर्प्रॉट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से देने पर केंद्रित होती है। हालाँकि आँकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में इन दोनों ही प्रकार के अनुदान में किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई है। और निकट भविष्य में इन रुझानों में भारी बदलाव की उम्मीद के कई कारण उपलब्ध हैं।
शायद यही वह अवसर है जब हम नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाले छोटे आकार के अनुदानों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वर्तमान में 144 देशों वाली विश्व अनुदान सूची (वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स) में भारत 124वें स्थान पर है। औसतन भाग लेने वाले केवल 22 प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि उन्होंने इस साक्षात्कार1 के पहले पिछले एक महीने में किसी को दान दिया, किसी अजनबी की मदद की, किसी अच्छे काम में स्वेच्छा से समय दिया या तीनों ही काम किया है। तुलना करने पर यह बात सामने आई है कि हमारे दक्षिण एशियाई पड़ोसी इस काम में हमसे बहुत आगे हैं। अनुदान की इस वैश्विक सूची में पाकिस्तान 91, बांग्लादेश 74, नेपाल 52, और श्रीलंका 27वें स्थान पर है।
हालाँकि एक तरह की आशा है कि व्यक्तिगत दान के क्षेत्र में वृद्धि आएगी। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से इस व्यापक होते बाज़ार का पूरा लाभ उठाने की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। हाल ही में परोपकार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर काम करने वाले लोगों के नेटवर्क फ़िलैन्थ्रॉपी फ़ॉर सोशल जस्टिस एंड पीस (पीएसजेपी) ने भारत में व्यक्तिगत दान पर एक अध्ययन करवाया था। उस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं।
भारत में अनौपचारिक दान सांस्कृतिक और धार्मिक परम्पराओं का एक मुख्य हिस्सा है। दान को हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों में अनिवार्य माना गया है। दानउत्सव के वालंटियर वेंकट कृष्णन का कहना है कि “यह सामाजिक क्षेत्र को दिया जाने वाला औपचारिक दान नहीं है जिसपर हम अपनी नज़र रखते हैं। धार्मिक/आध्यात्मिक और सामुदायिक संगठनों द्वारा दिए जाने वाले अनौपचारिक दान की मात्रा अगर औपचारिक दान से ज़्यादा न हो तो उसके बराबर है। इसके अलावा सीधे तौर पर किए जाने वाले दान भी होते हैं जिसमें ज़रूरतमंद की पैसे या अन्य रूप से मदद करना शामिल होता है। उदाहरण के लिए घरेलू सहायक या ड्राइवर के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना।”
सत्त्व के एवरीडे गिविंग इन इंडिया रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में निजी स्तर पर दिए जाने वाले दान की राशि पाँच बिलियन डॉलर है जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक दान से आता है। बाक़ी का बचा हुआ 10 प्रतिशत अनौपचारिक दान स्वयंसेवी संस्थाओं के हिस्से में जाता है जिसे ‘खुदरा परोपकार’ (रिटेल फ़िलैन्थ्रॉपी) भी कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार सालाना इसके ऑनलाइन माध्यम में 30 प्रतिशत और ऑफ़लाइन माध्यम में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।
हाल के दिनों में क्राउडफ़ंडिंग, वेतन भुगतान और मैरथॉन के माध्यम से फंडरेजिंग जैसे तरीक़े काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। इसके अलावा भारत में व्यक्तिगत स्तर पर दान को बढ़ावा देने वाला दानउत्सव भी है जिसकी शुरुआत 2009 में ‘जॉय ऑफ़ गिविंग वीक’ से हुई थी। यह दान का सप्ताह भर चलने वाला उत्सव है। इस उत्सव के पहले साल में दस लाख लोगों ने हिस्सा लिया था जिनकी संख्या अब बढ़कर साठ या सत्तर लाख हो गई है। और हम जानते हैं कि इन दानकर्ताओं में ज़्यादातर लोग निम्न आय वर्ग से आते हैं जिनमें ऑटो चलाने और शहरी इलाक़ों की स्वयं सहायता समूह की औरतें शामिल हैं।
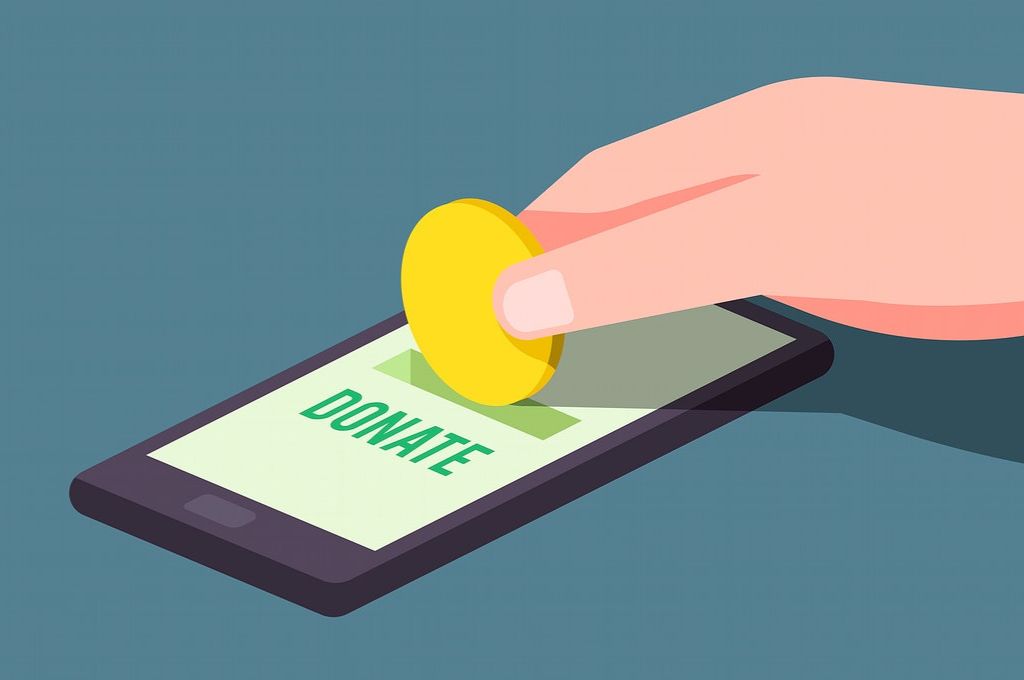
चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) भारत में बड़े पैमाने पर खुदरा धन जुटाने वाली पहली स्वयंसेवी संस्था थी। लेकिन इसकी सीईओ पूजा मरवाहा का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा के कारण क्राई की कमाई कम हो रही है। उनका कहना है कि इन संगठनों के पास पर्याप्त धन होता है जिससे वे अपना ब्रांड तैयार कर लेते हैं। इसलिए धन के वैकल्पिक स्त्रोत के अभाव में भारतीय स्वयंसेवी संस्थाएँ इस क्षेत्र में उतर भी नहीं पाती हैं। फंडरेजिंग के लिए आवश्यक धन की मात्रा को देखते हुए भारतीय स्वयंसेवी संस्थाओं में डर का माहौल है।
इसका फ़ायदा यह है कि स्थानीय संगठनों के पास अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा फंडरेजिंग के लिए विकसित ढाँचों का लाभ उठाने का विकल्प होता है। एडूकेट गर्ल्स की ऐलिसन बुख़ारी का कहना है कि “अब क्षमता में वृद्धि होगी क्योंकि अब दानकर्ताओं और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। ज़्यादातर शहरों में मैरथॉन का आयोजन होता है, अब घर-घर जाकर फंडरेजिंग का तरीक़ा स्थापित हो चुका है, कॉल सेंटर के माध्यम से धन उगाही अब प्रचलन में है…मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही उस स्तर पर पहुँच जाएँगे जब ‘लोकल बेहतर है’ का संदेश सुनने को मिलेगा और स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएँ अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विकसित और स्थापित तरीक़ों का प्रयोग शुरू कर देंगे।”
भारत में कुछ सबसे बड़े ऑनलाइन क्राउडफ़ंडिंग प्लैटफ़ॉर्म मिलाप, केटो और इम्पैक्टगुरु हैं। केटो के 70 प्रतिशत दानकर्ता भारतीय हैं और ये बड़े शहरों में रहते हैं और इनकी उम्र 25 से 45 के बीच है। फ़ंडिंग का ज़्यादातर हिस्सा परियोजनाओं और सेवा-उन्मुख संगठनों को जाता है न कि मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों या संगठनात्मक समर्थन को।
केटो के वरुण सेठ बताते हैं अगले पाँच सालों में भारत के चालीस लाख स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलने वाली ऑनलाइन दान में बहुत अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। बड़े स्तरों पर दान देने वालों को यह आसान लगता है। उनका कहना है कि “यह फंडरेजिंग का सस्ता और कुशल तरीक़ा है। छोटे स्तर पर काम करने वाले संगठनों को इसमें समस्या हो रही है क्योंकि वे इंटरनेट की दुनिया में नए हैं।”
लेकिन पूजा मरवाहा आगाह करते हुए कहती हैं कि क्राउडफ़ंडिंग और ऑनलाइन दान से संबंधित आँकड़े वास्तविक हैं पर इनका आकार इतना छोटा है कि ऑनलाइन दान के पाँच गुना बढ़ जाने के बावजूद भी प्राप्त धनराशि अपेक्षाकृत बहुत कम होगी।
वेंकट कृष्णन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि “आने वाले कुछ सालों में क्राउडफ़ंडिंग, चेकआउट चैरिटी और ई-पेय प्लैटफ़ॉर्म में बहुत अधिक वृद्धि होगी और वेतन देने/काम पर रखने जैसे दान के पारम्परिक तरीक़े भी खुद को ऑनलाइन की तरफ़ मोड़ेंगे। गाईडस्टार इंडिया की पुष्पा अमन सिंह का कहना है कि हम अब तक कुल क्षमता के एक चौथाई हिस्से तक भी नहीं पहुँच पाएँ हैं।”
भारत में व्यक्तिगत दान को बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान है लेकिन भारतीयों को ऑनलाइन लेन–देन पर भरोसा नहीं है।
पुष्पा सुंदर का मानना है कि जब तक तकनीक एक सार्वभौमिक चीज़ नहीं हो जाती तब तक व्यक्तिगत तौर पर दिए जाने वाले दान की तुलना में ऑनलाइन दान का महत्व कम ही रहेगा। स्मॉल चेंज की सारा अधिकारी कहती है कि क्राउडफ़ंडिंग का ध्यान सामाजिक क्षेत्रों पर नहीं है, स्वयंसेवी संस्थाएँ अपने प्रचार-प्रसार के काम में अच्छी नहीं हैं और कुछ संस्थाओं को यह महत्वहीन लगता है। वे सोचते हैं कि क्राउडफ़ंडिंग से मिलने वाली छोटी राशि के लिए इतनी मेहनत नहीं की जानी चाहिए और उन्हें इसके बजाय सीएसआर के माध्यम से फंडरेजिंग में निवेश करना बेहतर विकल्प लगता है।
दूसरी तरफ़ सेंटर फ़ॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फ़िलैन्थ्रॉपी की इंग्रिद श्रीनाथ कहती हैं कि भारत में व्यक्तिगत दान को बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान है लेकिन भारतीयों को ऑनलाइन लेन-देन पर भरोसा नहीं है। हालाँकि भारत में मध्यवर्ग दूसरी चीजों के लिए ऑनलाइन लेन-देन करना शुरू कर चुका है लेकिन उनके बीच दान के लिए उपलब्ध ऑनलाइन प्लैटफ़ॉर्म को लेकर अब भी जानकारी की कमी है। वेंकट कृष्णन कहते हैं कि इसे अभी पूरी तरह से अनियंत्रित क्राउडफ़ंडिंग स्पेस के बेहतर नियंत्रण, बेहतर तकनीकी इंटरफ़ेस और ऐसे ही कुछ प्रयासों से ठीक किया जा सकता है।
रिपोर्ट में भारत में व्यक्तिगत दान के स्तर को और बेहतर करने के लिए कई तरीक़ों के बारे में बताया गया है।
स्वयंसेवी संस्थाओं में विश्वास की कमी कई भारतीयों के लिए एक समस्या रही है। गाइडस्टार इंडिया, सीएएफ इंडिया, दसरा, गिवइंडिया, केयरिंग फ्रेंड्स जैसी कई संस्थाएँ है जो स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रमाणित/सत्यापित करने और उन्हें मान्यता देने का काम करती हैं। ये संस्थाएँ दानकर्ताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को उचित सेवाएँ देती हैं और उन्हें मिलवाने का काम करती हैं। इससे व्यक्तिगत स्तर पर दान देने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव आने में मदद मिल सकती है।
इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं से संबंधित अधिक से अधिक जानकारियाँ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। स्वयंसेवी संस्थाएँ अपने वित्तीय मामलों को सार्वजनिक बना सकती हैं। इससे भुगतान में कमी या ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों में उस संगठन विशेष की भूमिका जैसे भ्रम दूर किए जा सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में नागरिक समाज के योगदान को केंद्र में रखकर बनाए गए संदेश भी लोगों के बीच विश्वास पैदा कर सकते हैं।
सारा अधिकारी के अनुसार दान में छोटी राशि माँग कर भी अविश्वास को दूर किया जा सकता है।
अधिकारी यह भी कहती हैं कि भारत में व्यक्तिगत स्तर पर दान देने वाले लोगों के बीच संवाद की कमी है। और साथ ही लोगों में सामाजिक क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए प्रेरणा की भी कमी है। वह अपनी बात बढ़ाते हुए कहती हैं कि जहां स्वयंसेवी संस्थाएँ इस काम को बेहतर कर सकती हैं वही सामाजिक क्षेत्रों के बारे में बताने वाली कहानियों के माध्यम से पारम्परिक और ऑनलाइन मीडिया भी इस काम में अपना योगदान दे सकती हैं। इंग्रिद श्रीनाथ भी ऑनलाइन दान को बेहतर बताने वाले स्त्रोतों की कमी को एक समस्या मानती हैं।
इंग्रिद श्रीनाथ के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर मिलने वाले दान की सम्भावना को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें स्वयंसेवी संस्थाओं के क्षमता निर्माण में बहुत अधिक निवेश की ज़रूरत है। बड़े संगठनों के पास क्षमता निर्माण के लिए धन उगाहने के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं। लेकिन भारत में स्वयंसेवी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या पाँच से भी कम होती है और इनमें शायद ही कोई फंडरेजिंग का विशेषज्ञ होता है। उन्हें फंडरेजिंग के सभी पहलुओं विशेष रूप से ऑनलाइन फंडरेजिंग में प्रशिक्षित होने की ज़रूरत है।
इंग्रिद श्रीनाथ मानती हैं कि “किसी भी तरह के विश्वसनिय आँकड़े ख़ासकर व्यक्तिगत दान से जुड़े विश्वसनीय आँकड़ों की गम्भीर कमी से भारत को बहुत नुक़सान पहुँचा है।” “इसलिए हम अपनी सामूहिक प्रवृति और कुछ मीडिया खबरों का सहारा लेते हैं।” व्यक्तिगत दान के लिए पारिस्थितिकी निर्माण में नियमित और विश्वसनीय आँकड़े मददगार साबित हो सकते हैं।
विकास क्षेत्र छोटे स्तर पर मिलने वाले व्यक्तिगत दान की तुलना में धनवान लोगों या फ़ाउंडेशनों द्वारा मिलने वाले दान को अधिक प्राथमिकता देता है। उनका ऐसा विश्वास है कि धनवान लोगों या फ़ाउंडेशनों द्वारा मिलने वाले दान अधिक रणनीतिक होते हैं और ये इन्नोवेशन को संचालित करते हैं। हालाँकि परोपकार के इस रूप पर इनकी अति-निर्भरता से जुड़े नुक़सान अब सामने आने लगे हैं।
क्या पैसे के मालिकों को नीतियों को भी प्रभावित करना चाहिए? क्या यह लोकतांत्रिक है?
अति-धनवान या कॉर्पोरेट परोपकार से धन शायद ही कभी ऐसे आंदोलनों में जाता है जो धन के ग़ैर-अनुपातिक संचय को चुनौती देते हैं। इसके अलावा, दानकर्ता अक्सर उन स्वयंसेवी संस्थाओं के काम को प्रभावित करते हैं जिन्हें वे दान देते हैं। क्या पैसे के मालिकों को नीतियों को भी प्रभावित करना चाहिए? क्या यह लोकतांत्रिक है? मानव अधिकार या सामाजिक न्याय संगठनों के मामले में यह विशेष रूप से विवादास्पद हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ़, छोटे दान के रूप में सामान्य व्यक्तियों से मिलने वाला समर्थन अधिकार-आधारित कामों की वैधता को मजबूत कर सकता है। पुष्पा सुंदर का कहना है कि आपके कारणों में विश्वास करने वाले सामान्य लोगों द्वारा किया जाने वाला दान आगे के मार्ग को मज़बूत करता है। “स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने लोगों से इसके लिए अपील करने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। सरकार के लिए गुमनाम रूप से दी गई छोटी धनराशि छोटे दान का विरोध कठिन होता है।”
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह स्थिति सटीक है। अधिकारों और न्याय पर काम करने वाले संगठनों को सरकार शक की नज़र से देखती है। जिसके कारण एचएनआई, अन्य संस्थाएँ और कम्पनियाँ ख़ुद का नाम इन संगठनों और अभियानों से जोड़ने से बचती हैं। इस अंतर को भरने के लिए व्यक्तिगत दान के विकास और क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।
—
फ़ुटनोट:
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
8 अप्रैल 2022 को माननीय न्यायमूर्ति एएम खानविलकर सर्वोच्च न्यायालय के कोर्टरूम-3 में आए और अपनी उस कुर्सी पर बैठे जो न्यायालय के प्रतीक चिन्ह के नीचे लगी हुई थी। इस प्रतीक चिन्ह में चक्र, अशोक स्तंभ और महाभारत से लिया गया आदर्श वाक्य ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ शामिल है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि आख़िर में जीत के लिए केवल धर्म (या सच्चाई) ही काफ़ी है। जस्टिस खानविलकर जिस मामले पर फ़ैसला सुनाने बैठे थे, उस पर बहस और सुनवाई शीतकालीन सत्र में हो चुकी थी और न्यायपीठ अपना फ़ैसला सुरक्षित कर चुकी थी। उस दिन कुछ पत्रकारों, वकीलों और एकाध दर्शकों के अलावा अदालत में ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। कुछ देर की शांति के बाद जज ने गंभीर और उदास कर देने वाला यह फ़ैसला सुनाया कि विदेशी अनुदान स्वीकार करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है।
हालांकि कई लोगों को इस फ़ैसले का आभास पहले से ही था लेकिन कुछ लोगों को अब भी उम्मीद थी कि शायद अदालत इस मुद्दे पर उदार नज़रिया अपनाएगी।
भारत सरकार ने भारतीय राजनीति में विदेशी एजेंसियों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए 1976 में फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) यानी विदेशी अनुदान (विनियमन) अधिनियम लागू किया था। साल 1984 में ग़ैर-लाभकारी संगठनों या स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी अनुदानों को भी इसमें शामिल करने के लिए इस अधिनियम का विस्तार किया गया। 2010 में चुनावी प्रक्रियाओं की बजाय स्वयंसेवी संस्थाओं पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से इस क़ानून के स्वरूप और लक्ष्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया। यह परिवर्तन नई प्रस्तावना में शामिल किया गया, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थानों से जुड़े संदर्भों के साथ-साथ मुख्य प्रावधानों के उन सभी संदर्भों को भी हटा दिया गया था जो राजनेताओं की बजाय स्वयंसेवी संस्थाओं की गतिविधियों पर केंद्रित थे।1

2020 में इस क़ानून को और अधिक सख़्त बनाया गया और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के सामने निम्न मांगें रखी गईं:
• मिलने वाली राशि सबसे पहले दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) के गेटवे खाते में प्राप्त करें।
• प्रशासनिक ख़र्चों के लिए उपलब्ध विदेशी अंशदान को कम करें।
• एफ़सीआरए फंड का पैसा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को देना बंद करें, भले ही उनके पास एफ़सीआरए के लिए मंज़ूरी क्यों ना हो।2
उचित परामर्श प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ही इन बाधक बदलावों को लागू करने से स्वयंसेवी संस्थाएं नाराज़ हो गईं। ये संस्थाएं पहले से ही अपने ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर चल रहे अभियानों से जूझ रहीं थीं और क़ानून में आए तेज रफ्तार बदलावों ने इनकी चाल और बिगाड़ दी। ऐसा तब हुआ जब इनके सामने महामारी के कारण देशभर में फैली अव्यवस्था से निपटने की चुनौती थी। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसे अपने मौलिक अधिकारों का हनन माना और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।
जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, तिरुवनंतपुरम जैसे याचिकाकर्ताओं ने गेटवे खाते की ज़रूरत का विरोध किया। केयर एंड शेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, विजयवाड़ा के नोअल हार्पर और नेशनल वर्कर वेलफ़ेयर ट्रस्ट, सिकंदराबाद का मानना है कि नई दिल्ली में एसबीआई की मुख्य शाखा (एनडीएमबी) में एफ़सीआरए गेटवे के लिए खाता खुलवाने का यह निर्देश पूरी तरह से एकतरफा है और इस फ़ैसले से नौकरशाही की बू आ रही है। इससे पूरे देश की स्वयंसेवी संस्थाओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि इन खातों को नई दिल्ली की एक विशेष शाखा में खोलने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, पुनरानुदान पर लगाया गया प्रतिबंध भी अनुचित है क्योंकि इससे स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए एक दूसरे का सहयोग करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह यह क़ानून अनुच्छेद 19 में निहित सहयोग के मौलिक अधिकार का हनन करता है। पंजीकरण के समय सभी ट्रस्टियों द्वारा अपना आधार दिए जाने की आवश्यकता को सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का उल्लंघन माना गया है।3 इसलिए इस समूह ने अदालत से पहले की स्थिति ही बहाल करने का अनुरोध किया जिसके तहत स्वयंसेवी संस्थाएं किसी भी स्वीकृत बैंक में अपना मुख्य एफ़सीआरए खाता रख सकती हैं और एफ़सीआरए पंजीकरण वाली दूसरी संस्थाओं को पुनर्दान कर सकती हैं।
सरकार ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा है कि विदेशी अनुदान राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल हो सकता है इसलिए इनके उपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। इन कड़े प्रतिबंधों के बावजूद हर साल विदेशों से आने वाले अनुदानों में लगातार वृद्धि हो रही है। अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने दान का हिस्सा हस्तानांतरित करने के कारण उनके आवंटन के ऑडिट का काम मुश्किल हो जाता है। साथ ही, इसके चलते लोकहित पर खर्च होने वाले धन का एक बड़ा हिस्सा अब व्यय का लेखाजोखा रखने वाली व्यवस्था पर खर्च होने लगा है। सरकार ने यह भी कहा है कि व्यापक स्तर पर पाए गए ग़ैर-अनुपालन (कम्प्लायन्स) के कारण 19,000 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं की अनुज्ञप्तियां (लाइसेंस) रद्द कर दी गई हैं। इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए एसबीआई ने ऐसी पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं जिनकी मदद से दूर-दराज बैठे लोग भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाकर बहुत सारे लोगों ने सफलतापूर्वक अपना खाता खुलवाया भी है। सरकार ने यह भी दावा किया है कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं केवल अनुदान की राशि के लेनदेन में शामिल थी जिससे अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ इनके ख़ास ग्राहक संबंध बन गये। अंत में, सरकार ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को विदेशी अनुदान लेने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं था और विधायिका इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित करने या अपनी निगरानी में आंशिक रूप से लागू करने का अधिकार रखती है।
अदालत का फ़ैसला सरकार के रुख का समर्थन करता है। इस फ़ैसले में कहा गया कि एसबीआई ने लोगों को गेटवे खाता खोलने में मदद के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं और अपने आप में भी इसकी आवश्यकता का औचित्य है। इस फ़ैसले में यह भी कहा गया कि भारत की संप्रभुता को अनुचित विदेशी प्रभावों से बचाने की ज़रूरत थी और विधानमंडल द्वारा उठाए गए इस कदम को ग़लत नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा इस बात में कोई दम नहीं है कि इस परिवर्तन ने साथ काम करने, अभिव्यक्ति और आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है या यह कि यह आवश्यकता ही एकतरफा है। इस मामले में अदालत ने एकमात्र मामूली सी छूट देते हुए कहा कि ट्रस्टी एफ़सीआरए पंजीकरण के समय पहचान पत्र के रूप में अपनी आधार संख्या देने के बजाय पासपोर्ट दे सकते हैं।
क़ानूनी तर्कों के अलावा 132 पृष्ठों वाले इस आदेश में कई अतिरिक्त टिप्पणियां भी शामिल हैं जो पूरी तरह से अदालत में सरकार की प्रस्तुतियों पर आधारित हैं, जैसे:
सरकार के ये दावे नॉन-प्रॉफिट सेक्टर की एक भ्रामक तस्वीर पेश करते हैं जो बीते 50 सालों से अधिक समय से लाखों गरीब और हाशिए पर जी रहे भारतीयों की मदद करता आ रहा है। इन ग़लत धारणाओं को विस्तार से देखते हैं:
सरकारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी योगदान 2009–10 में 10,292 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018–19 में 16,457 करोड़ रुपए हो गया। यह 10 सालों में 1.6 गुना बढ़ा है। औसत वार्षिक वृद्धि दर मात्र 5.4 प्रतिशत है जो मुद्रास्फीति की वार्षिक दर से कम है। अगर इन आंकड़ों को मुद्रास्फीति (सरकार के सूचकांक का उपयोग करते हुए) के अनुसार समायोजित किया जाता है तो प्राप्त आंकड़ा इशारा करता है कि असल में विदेशी अनुदान में पिछले 10 वर्षों में कमी आई है।
स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए क़ानून ‘उल्लंघन’ का संदर्भ वास्तव में एफ़सीआरए रिटर्न नहीं दाखिल करने से हैं। रिटर्न दाखिल नहीं करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं में ज़्यादातर संस्थाएं या तो निष्क्रिय हो चुकी है या फिर उन्हें किसी भी तरह का अनुदान नहीं मिलता है। परिणामस्वरूप, 19,000 स्वयंसेवी संस्थाओं का एफ़सीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया। ग़लत इस्तेमाल, संस्था का उद्देश्य बदलना (डायवर्जन) या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जुड़े वास्तविक उल्लंघनों की संख्या बहुत कम है। गृह मंत्रालय की एफ़सीआरए वेबसाईट पर ऐसे दर्जन भर ही मामलों को सूचीबद्ध किया गया है जहां ऐसे किसी उल्लंघन के लिए किसी संगठन के एफ़सीआरए को या तो निलम्बित कर दिया गया है या रद्द कर दिया गया है।
भारत में अधिकांश निजी कल्याणकारी अनुदान साधारण कल्याण और राहत (उदाहरण के लिए ग़रीबों को खाना खिलाना और आपदाओं के बाद बचाव और पुनर्वास) कार्यों में लगाए जाते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकार से मिलने वाला धन उन सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए दिया जाता है जो सुविधाएं सरकार सीधे अपने स्तर से नहीं देना चाहती हैं। सीएसआर फ़ंडिंग भी अनुच्छेद VII में सूचीबद्ध चुनिंदा गतिविधियों तक ही सीमित है। इसमें कई महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, शोधकार्य, सशक्तिकरण और संघर्ष समाधान जैसा बड़ा हिस्सा बिना किसी घरेलू सहयोग के छूट जाता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जहां भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विकास के साथ तालमेल रखने के लिए समझ और बौद्धिक दृढ़ता विकसित करने की ज़रूरत है। यही कारण है कि इन मुद्दों पर काम कर रहीं संस्थाएं सीमा पार यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर होती हैं।
लोक कल्याणकारी संस्थाओं को अपनी बिक्री या शुल्क से मिलने वाले कुल राजस्व का 20 प्रतिशत से अधिक स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, ये संस्थाएं ऐसे काम तभी कर सकती हैं जब यह व्यापारिक गतिविधि उनके लोक कल्याण उद्देश्य से जुड़ी हुई हों। इसलिए लोक कल्याणकारी संस्थाओं को व्यापारिक संगठन के रूप में देखना कठिन है।
इस क्षेत्र से जुड़ा एक और सबसे बड़ा मिथक (हालांकि इस फ़ैसले में इसे संदर्भित नहीं किया गया है) भारत में स्वयंसेवी संस्थाओं की संख्या को लेकर है। इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनकी कुल संख्या 30.17 लाख है। यह आंकड़ा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन4 द्वारा जारी 2009 की रिपोर्ट पर आधारित है। इस आंकडें में सक्रिय और निष्क्रिय सभी पंजीकृत संस्थाओं और ट्रस्टों को शामिल किया गया है। आय कर पोर्टल पर कर-मुक्त कल्याणकारी संगठनों और धार्मिक इकाइयों की कुल संख्या 2,20,225 दिखाई गई है। इस सूची में सभी कर-मुक्त इकाइयों (स्कूलों एवं अस्पतालों) को शामिल किया गया है और यह आंकड़ा वास्तविकता के ज़्यादा नज़दीक प्रतीत होता है। सरकार के एनजीओ दर्पन पोर्टल के अनुसार इनमें से सिर्फ़ 1,39,097 इकाईयों को सही अर्थों में ‘ग़ैर-लाभकारी संस्था’ कहा जा सकता है। इसमें एफ़सीआरए पंजीकरण वाले संस्थान (16,888) और बिना एफ़सीआरए पंजीकरण वाले संस्थान (1,22,209) दोनों शामिल हैं। इस तरह स्वयंसेवी संस्थाओं की वास्तविक संख्या शायद 33 लाख के आंकड़े का 5–10 प्रतिशत ही है।
जब इस फ़ैसले से मिलने वाले वास्तविक लाभ के बारे में सोचें तो हमें यह विचार करना चाहिए कि: अगर विदेशी अनुदान को हतोत्साहित करना सरकार का राजधर्म है तो उन्हें देश के भीतर जनकल्याण को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक और सार्थक कदम उठाने के बारे में भी उतनी ही तत्परता से सोचना चाहिए। ऐसा हुआ तो यह स्वयंसेवियों, दानदाताओं और वंचितों, हम सभी के लिए एक वास्तविक जीत होगी।
—
फुटनोट:
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
सार्वजनिक भूमि ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका इस्तेमाल समुदाय के लोग सार्वजनिक हितों के लिए करते हैं। इनमें जंगल, चारागाह, तालाब और कूड़ा इकट्ठा (वेस्टलैंड) करने वाली जगहें होती हैं। ये ग़ैर-नक़द, ग़ैर-बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का आधार होती हैं। ऐसी ज़मीनें स्थानीय लोगों के ईंधन, पानी, तेल, मछली, जड़ी-बूटी, विभिन्न प्रकार की फल-सब्ज़ियों के अलावा उनके पशुओं के लिए चारा आदि की ज़रूरतें पूरी करती हैं। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि ग्रामीण घरों की कुल आय में आम ज़मीन से होने वाली आय का योगदान 12 से 23 प्रतिशत के बीच होता है। कार्बन के क्षेत्र में भी इन ज़मीनों का योगदान होता है और ये जैव विविधता के भंडार और देशी ज्ञान की निशानियों में बदल जाती हैं।
भारत में सार्वजनिक भूमि के क्षेत्रफल में लगातार कमी आ रही है। 2005 से 2015 के बीच अकेले चारागाह के रूप में प्रयुक्त होने वाली ज़मीन पहले से 31 प्रतिशत कम हुई है। औद्योगीकरण की तेज गति से इन जमीनों पर पड़ने वाला बोझ बढ़ा है। लोग अब इनका उपयोग घर-मकान बनाने के साथ-साथ खेती में करने लगे हैं। इसके अलावा ‘उर्वर’ ज़मीनों की गहरी खुदाई से आसपास का परिदृश्य भी तेज़ी से बदल रहा है।इन सबमें एक नई जुड़ी चीज़ है भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रांति (क्लीन एनर्जी ट्रैंज़िशन)।

निजी ज़मीनों की तुलना में सार्वजनिक ज़मीनों का क़ानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होने की सम्भावना कम होती है। इसलिए सार्वजनिक जगहों का अतिक्रमण और उस पर निजी स्वामित्व का दावा करना बहुत आसान हो जाता है। अस्पष्ट सीमाएँ महँगी और अपूर्ण प्रवर्तन की स्थिति पैदा करती हैं और भूमि और सम्पत्ति क़ानूनों में अतिच्छादन इस समस्या को कई गुना और अधिक बढ़ा देती है। इस समस्या से निपटने के लिए 28 जनवरी 2011 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक व्यवस्था को सक्रिय बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया। जगपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब सरकार और अन्य नाम वाले मामले में कोर्ट ने सार्वजनिक ज़मीनों के सामाजिक-आर्थिक महत्व को मान्यता देते हुए राज्य सरकारों को अतिक्रमण हटाने के लिए योजनाएँ तैयार करने का निर्देश दिया। उसके बाद गाँव के सार्वजनिक उपयोग के लिए ऐसी सभी ज़मीनों को ग्राम पंचायत को वापस करना था।
इस फ़ैसले से ग्रामीण समुदायों में अपनी उन सभी ज़मीनों को वापस पाने की आशा जाग गई जो अतिक्रमण के कारण उनसे छिन गई थीं। इसके अलावा इस फ़ैसले ने मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा, प्रबंधन और बहाली के लिए राज्य सरकारों को तंत्र विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया। इसने लोअर कोर्ट के लिए देश में सार्वजनिक ज़मीनों पर न्यायशास्त्र विकसित करने के शुरुआती बिंदु के रूप में भी काम किया है।
राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुल भूमि का क्रमश: 36 प्रतिशत और 37 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक भूमि का हिस्सा है। ज़मीन के ये टुकड़े लाखों ग्रामीणों के आत्म-सम्मान, सुरक्षा और आजीविका का साधन हैं। राज्य की अदालतों में सरकारों के अतिक्रमण के ख़िलाफ़ दायर की जाने वाली जन हित याचिकाओं का अम्बार है। इसे ध्यान में रख कर और जगपाल सिंह फ़ैसले के नक़्शे कदम पर चलते हुए 2019 में राजस्थान हाई कोर्ट ने और 2021 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी अपनी राज्य सरकारों को पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल (पीएलपीसी) नाम के स्थाई संस्थानों की स्थापना के निर्देश दिए। इन प्रकोष्ठों में ग्रामीण इलाक़ों में किए गए सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें आती हैं और यह क़ानूनी प्रक्रियाओं के तहत इन मामलों को निबटाकर उन्हें ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को वापस लौटाते है।
आज की तारीख़ में दोनों राज्यों के प्रत्येक ज़िले में दो पीएलपीसी की स्थापना हो चुकी है जिसका प्रमुख ज़िले का कलेक्टर होता है। भारत के दो तिहाई से अधिक अदालती मुक़दमे ज़मीन या सम्पत्ति से जुड़े होते हैं और इनमें ज़्यादातर मामले सार्वजनिक भूमि के हैं। ऐसी स्थिति में पीएलपीसी जैसे संस्थानों की स्थापना इन मामलों में एक स्वागत योग्य हस्तक्षेप है। पीएलपीसी में समुदाय के लोग सीधे तौर पर अपनी सार्वजनिक ज़मीन के मामले का बचाव कर सकते हैं और ज़मीन से जुड़े नियमों और विधानों की जटिलता से बच सकते हैं। इससे पेशेवर क़ानूनी सहायता लेने या अदालत के शुल्क का भुगतान करने में कमी आती है। जिसके कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा काफ़ी कम खर्च में अपने क़ानूनी संसाधनों को वापस हासिल कर लेता है। मुद्दों से निबटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को संस्थागत करने से बहुत जटिल और खर्चीले अदालती तामझाम से बचा जा सकता है और साथ ही न्यायालय के कार्यभार को कम किया जा सकता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय केवल उन मामलों की सुनवाई करता है जिसमें पीएलपीसी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं; एक प्रहरी की भूमिका में रहकर न्यायिक प्रक्रियाओं को नियमों का पालन करने और इन प्रकोष्ठों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की अनुमति मिलती है।
पीएलपीसी को और अधिक असरदार कैसे बनाया जा सकता है?अपनी शुरुआती अवस्था में होने के बावजूद पीएलपीसी क़ानूनी जानकारियों को लोकतांत्रिक बनाने, न्याय दिलवाने और अतिक्रमण के मामलों का तेज़ी से निवारण करने में सहायक साबित हो रहे हैं। हालाँकि अतिक्रमण के मामलों के निबटारों के अलावा पीएलपीसी सार्वजनिक भूमि के प्रबंधन और संचालन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इसलिए इस विषय पर गम्भीरता से सोचने की ज़रूरत है।
अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि जहां स्थानीय स्तर पर पहुँच और उपयोग के अधिकारों को मान्यता दी जा चुकी है वहीं इन्हें औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किया जाता है।
‘ज़मीन’ राज्यों के दायरे में आने वाला विषय है। किसी भी सार्वजनिक भूमि पर जब तक पहले से किसी सरकारी विभाग विशेष (जैसे कि वन विभाग) का मालिकाना हक़ नहीं होता है तब तक क़ानूनी रूप से ज़मीन के उस टुकड़े को ‘सरकारी ज़मीन’ के उपवर्ग (सबसेट) के दायरे में ही रखा जाता है। भूमि रिकॉर्ड के सर्वेक्षण, रिकॉर्ड के रखरखाव की ज़िम्मेदारी भी राज्य के राजस्व विभागों की होती है। इसके साथ ही, पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायतों को गाँव की आम भूमि के प्रबंधन और संरक्षण का दायित्व सौंपती है।
हालाँकि, अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि जहां स्थानीय स्तर पर पहुँच और उपयोग के अधिकारों को मान्यता दी जा चुकी है वहीं इन्हें औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किया जाता है। स्थाई दस्तावेज़ों की सूची में आने के बाद भी आम ज़मीनों से जुड़ी जानकारियाँ नियमित रूप से अपडेट नहीं की जाती हैं। उनकी सीमाओं की स्थानिक पहचान भी ग़ायब हो चुकी हैं। इस तरह की जानकारी सम्बन्धी सूचनाओं की कमी से समुदायों का अपनी ज़मीन पर किया जाने वाले दावे कमजोर हो जाते हैं। इससे सार्वजनिक भूमि का दुरुपयोग शुरू हो जाता है और लोग उसे नज़रअन्दाज़ करने लगते हैं। नतीजतन बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के उन ज़मीनों पर निजी अतिक्रमण को बढ़ावा मिल जाता है। नियमित रूप से सुचारु पीएलपीसी इनमें से कुछ बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर सकता है और सुधारवादी कदम के बजाय अतिक्रमण को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जैसे कि सार्वजनिक भूमि की व्यापक पहचान, सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए एक मज़बूत कदम उठाना और भूसम्पत्ति मानचित्र तैयार करना। ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड में पूरी तरह से सुधार चाहने वाला डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम भी ज़मीन पर निजी स्वामित्व और अधिकार पर केंद्रित है। नवीनतम स्वामित्व योजना में से भी सार्वजनिक भूमि को हटा दिया गया है। इस योजना में आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने और भूमि के कार्यकाल को औपचारिक रूप देने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है। पीएलपीसी भी सार्वजनिक संसाधनों के मुफ़्त उपयोग और स्थानिक रूप से संदर्भित आँकड़े तैयार करने और उन्हें भूमि प्रशासन के सामने लाने के लिए ऐसे ही तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद वे इस तैयार आँकड़ों को पंचायत में पंजीकृत सम्पत्तियों से जोड़ कर, सामाजिक ऑडिट के लिए आधार तैयार कर सकते है और अतिक्रमण पर निगरानी रखने के लिए आधार रेखा का काम कर सकते हैं।
हाल ही में राज्य में बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण से निपटने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडू सरकार को यह निर्देश दिया कि वह राज्य की सभी जल निकायों की उपग्रहीय (सेटेलाइट से) तस्वीरें लें और इन्हें प्रत्येक ज़िले के एक संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग में लाएँ ताकि उन संसाधनों को यथावत सुरक्षित रखा जा सके। पीएलपीसी इस ज़िम्मेदारी को डिज़ाइन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
सार्वजनिक संसाधनों के उत्तरदायी शासन की स्थिति को हासिल करने के लिए अतिक्रमण को अपने केंद्र में रखने वाले क़ानूनी दृष्टिकोण के ऊपर से नीचे के नियम (टॉप-डाउन क़ानून) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन ज़रूरी है। ज़मीन एक राजनीतिक मुद्दा है। संसाधनों से युक्त ज़मीन का एक सार्वजनिक टुकड़ा सार्वजनिक पूँजी होता है और इसमें सामाजिक सामंजस्य और सद्भाव के गुण निहित होते हैं। इसलिए इन संसाधनों के प्रबंधन में पीएलपीसी पंचायतों और ग्राम संस्थाओं को समर्थन देने वाली और अधिक प्रभावी तरीक़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। समस्याओं के निबटान के लिए एक सहायक शाखा के रूप में सामाजिक सम्बन्धों को बेहतर करने के क्षेत्र में काम करने से अधिक न्यायपूर्ण परिणाम हासिल हो सकते हैं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
इस बात में जरा भी शक की गुंजाईश नहीं है कि साल 2020 में कोविड-19 और वेबिनारों ने दुनिया में तहलका मचा दिया था। कुछ विडियो कॉन्फ़्रेन्डिंग प्लैटफ़ॉर्म का कहना है कि महामारी के शुरुआती दौर में विडियो कॉन्फ़्रेन्स और मीटिंग की संख्या में तीन से चार गुना की वृद्धि हुई थी।
वर्चुअल आयोजनों की उपयोगिता को किसी तरह के सबूत की ज़रूरत नहीं है। भौतिक (इन-पर्सन) आयोजनों की तुलना में वेबिनार और वर्चुअल आयोजन अधिक लोगों तक पहुँचने में सक्षम होते हैं।दर्शकों और श्रोताओं की माँग के आधार पर सामग्रियों को उपलब्ध करवाने के इस दौर में वे दर्शकों को उनकी सुविधानुसार बातचीत में हिस्सा लेने का अवसर भी देते हैं। दूसरी तरफ़, कई तरह के आयोजनों (वर्चुअल मीटिंग और कैच-अप कॉल की बड़ी संख्या) के विकल्प वाले समय में दर्शकों को अपने कार्यक्रम से जोड़े रखने के लिए एक अच्छी योजना की ज़रूरत होती है।
वर्तमान स्थिति विकास एवं शोध समुदाय को अपने दर्शकों से जुड़ने के तरीक़ों के बारे में दोबारा सोचने का मौक़ा दे रही है। पिछले कुछ महीनों में लीड एट क्रिया विश्वविद्यालय ने सीखने और प्रसार के विभिन्न प्रारूपों के साथ एक तरह का प्रयोग किया। इस प्रयोग में फ़ायरसाइड चैट से ट्विटर पर होने वाली बातचीत और रन-ऑफ़-द-मिल पैनल चर्चा शामिल है। इस प्रक्रिया से प्राप्त कुछ अनुभव इस प्रकार हैं।
अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते समय संगठनों को व्यावहारिक होना चाहिए। उन्हें यह सोचना होगा कि सीखने और पहुँच के व्यापक रणनीति की सीमा में ही वेबिनारों को आयोजित करवाना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम की योजना में क़ीमती समय और संसाधन निवेश करने से पहले सभी स्तरों पर अपने लक्ष्यों को तय करना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आयोजन की ‘सफलता’ का स्वरूप कैसा होगा और यह आपके संगठन के लक्ष्यों से किस प्रकार संबंधित होगा?
आयोजन की ‘सफलता’ का स्वरूप कैसा होगा और यह आपके संगठन के लक्ष्यों से किस प्रकार संबंधित होगा?
उदाहरण के लिए, आयोजन के स्तर पर आपका उद्देश्य सबूतों, अंतर्दृष्टि, शोकेस इन्नोवेशन, हितधारकों के बीच तालमेल बिठाने वाले क्षेत्रों की पहचान आदि को बढ़ावा देना हो सकता है। दूसरी तरफ़, एक संगठन के स्तर पर आपका उद्देश्य उद्योग के क्षेत्र में अपने ब्रांड को मज़बूत बनाना या नई साझेदारी करना भी हो सकता है।
अपने आयोजन के उद्देश्य के बारे में सोचते समय सीखने के एजेंडे को विकसित करना उपयोगी होता है। जैसे उन सवालों को पहचानना ना जो ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतरों और उनके उत्तर देने वाली गतिविधियों की बात करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि आप समझ सकें कि अपने कार्यक्रम को आपकी पहुँच की रणनीति और संगठन के लक्ष्यों के साथ कैसे एकीकृत किया जाए। विचार-मंथन के इस प्रारम्भिक चरण का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ‘एक प्रतिभागी की तरह सोचना’ भी है। सत्र के अंत में दर्शक किस तरह का ज्ञान अपने साथ लेकर जाने की उम्मीद कर सकते हैं? पहले से ही इन बातों की समझ स्पष्ट होने से आपका आउटरीच अभियान मज़बूत होगा और दर्शकों का सही समूह तैयार करने में आपको मदद मिलेगी।
किसी भी आयोजन में उसका प्रारूप उसकी विषय-सामग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आमतौर पर आभासी आयोजन वेबिनार या वेबकास्ट के रूप में लाईव प्रसारित किए जाते हैं।
वेबिनारों को होस्ट और दर्शकों के बीच दो-तरफा बातचीत की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। आयोजन के लक्ष्यों के आधार पर वेबिनारों और आयोजनों के प्रारूप के कुछ उदाहरण हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:
वहीं वेबकास्ट सूचनाओं का एकतरफ़ा प्रवाह है। यह बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचने में उपयोगी होता है और आमतौर पर इसका उपयोग जानकारी देने के लिए किया जाता है। भाषण, मुख्य भाषण (कीनोट स्पीच) और संवादाता सम्मेलन (प्रेस कॉन्फ़्रेन्स) वेबकास्ट के कुछ लोकप्रिय प्रारूप हैं।
कोविड -19 के कारण बातचीत में विविधता और विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को शामिल करने की ज़रूरत प्रबल हुई है। एक इंटरसेक्शनल नज़रिए का उपयोग करके यथास्थिति की दोबारा जाँच का मामला मज़बूत हो गया है—चाहे वह हमारे द्वारा इकट्ठा किए गए आँकड़े हों या चाहे जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं या हमारे उन फ़ैसलों को लेने के तरीक़े जिनसे उन समुदायों पर असर पड़ता है जिनके साथ हम काम करते हैं। एक आकर्षक और ईमानदार बातचीत के लिए दृष्टिकोण के संतुलन को समझना और प्रतीकवाद से बचते हुए नई आवाज़ों को शामिल करना ज़रूरी होता है। अपने नेटवर्क से बाहर निकलकर दान कर्ताओं, पारिस्थितिकी को सक्षम बनाने वाले लोगों और मध्यस्था करवाने वाले संगठनों (जो आमतौर पर विभिन्न संगठनों के साथ काम करते हैं) से सलाह लेना भी कारगर हो सकता है। अपनी सूची में शामिल लोगों में से ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों, अकादमिक दुनिया के लोगों और नीति निर्माताओं की पहचान करना भी एक अच्छा तरीक़ा है। इसी क्रम में सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और उभरते विशेषज्ञों की जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकता है।

आयोजन के पहले, आयोजन के दौरान और बाद की सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लोगों और प्रणालियों को व्यवस्थित कर लें।
आयोजन के कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय आयोजन की अवधि और दिन तथा समय को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। कोई भी आयोजन सोमवार और शुक्रवार को न करना ही बेहतर माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ़ समय का चुनाव विभिन्न समय क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभागियों पर निर्भर करता है।
फ़ायरसाइड चैट और पैनल डिस्कशन जैसे प्रारूपों के लिए यह सलाह दी जाती है कि विशेषज्ञों से पहले से बात कर लेनी चाहिए। इसमें बातचीत का प्रवाह, मुख्य सवाल और चर्चा के बिंदु, समय-सीमा और लॉगिन लिंक आदि शामिल होता है। अगर समय अनुमति दे तो आयोजक को आयोजन से पहले एक बार सभी वक्ताओं से फ़ोन पर बात कर लेनी चाहिए ताकि आयोजन के दौरान वे एक दूसरे से असहज ना रहे और वास्तविक स्थिति से अवगत हो जाएँ।
वेब कॉन्फ़्रेन्सिंग के पहले से मौजूद टूल या एक नए ऐप को ख़रीदने के बीच का चुनाव करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए: दर्शकों की संख्या, आयोजन की समय-अवधि, और इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ीचर। आयोजन से पहले सभी के साथ मिलकर एक अभ्यास करने से आयोजन वाले दिन सुविधा हो सकती है।
एक सामान्य नियम यह कहता है कि पंजीकरण की कुल संख्या के केवल 40-50 प्रतिशत लोग ही उपस्थित होते हैं। ज़्यादातर लोग वेबिनार की तारीख़ से एक सप्ताह पहले या उससे भी कम समय में अपना पंजीकरण करवाते हैं इसलिए सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियान से पंजीकरण की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इस कारण श्रोताओं के शोकेस, कार्यक्रम की झलक और रचनात्मक हैशटैग अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
प्रेजेंटेशन और मल्टीमीडिया जैसे विजुअल चीजों का उपयोग करते समय डिज़ाइन और विषय दोनों पर ध्यान देना और आभासी रूप से देखने वालों के लिए इन्हें बेहतर बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, प्रेजेंटेशन में इमेज को कम्प्रेस करने से उसे पढ़ने में आसानी होती है।
आयोजन की शुरुआत में ही प्रतिभागियों के साथ आयोजन का प्रारूप और शामिल होने के लिए जारी दिशा निर्देश साझा करना चाहिए। जैसे कि क्या प्रतिभागियों को बोलने की अनुमति होगी? क्या सत्रों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी? विडियो कॉन्फ़्रेन्सिंग के ज़्यादातर प्लैटफ़ॉर्म ऐसे टूल भी इस्तेमाल करते हैं जिनके माध्यम से वेबिनार के दौरान प्रतिभागी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर, चुनाव और भाग लेने के लिए कहने वाले तरीक़ों का इस्तेमाल दर्शकों को जोड़े रखने और आयोजन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। चैट बॉक्स का उपयोग मुख्य संदेशों, महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद दिलाने और समय सारिणी पर नज़र बनाए रखने में उपयोगी होता है। अगर आप प्रश्नोत्तर के लिए समय देना चाहते हैं तब आपको संयोजक की मदद करनी चाहिए ताकि वह बातचीत को महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रासंगिक सवालों की पहचान कर सके।
आयोजन के बाद भी बातचीत को बनाए रखने के लिए आयोजक ब्लॉग्स और इंफ़ोग्राफ़िक्स जैसे आसान प्रारूपों का उपयोग करके वेबिनार की रिकोर्डिंग और मुख्य बातचीत को प्रतिभागियों के साथ साझा कर सकते हैं।
वर्चुअल मीटिंग और कॉन्फ़्रेनन्सिंग टूल का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर होने लगा है। लेकिन बावजूद इसके ऐसे सबूतों की संख्या बहुत कम है जिनसे किसी आयोजन की सफलता के कारगर तरीक़ों के बारे में जाना जा सके। कोविड-19 ने हमें ऑनलाइन बातचीत की तरफ़ मुड़ने पर मजबूर किया है, देखभाल संबंधी भार को बढ़ाया है और हम दूर बैठकर काम करने के दबाव से निबट रहे हैं वहीं डिजिटल थकान आज के कामकाजी जीवन की एक वास्तविकता है।
परिणामस्वरूप काम वाले दिन के बीच में या उसके बाद किसी आयोजन में शामिल होने के अवसर का महत्व बढ़ता जा रहा है। नतीजतन, सफलता के पारम्परिक पैमाने जैसे पंजीकरण की संख्या, शामिल होने वाले प्रतिभागियों की संख्या और बातचीत में शामिल होने वाले लोगों की संख्या आदि को दोबारा देखने की ज़रूरत है क्योंकि लोग अब भी इस नए सामान्य के प्रति ख़ुद को ढालने में लगे हुए हैं।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
—
ज़्यादातर किशोर लड़कियों के लिए करियर के रूप में राजनीति सोच में भी नहीं होता है। कुछ लोगों की रुचि इसमें है भी लेकिन उन्हें भारत में राजनीति में करियर बनाना असम्भव लगता है। ऐसा ही एक उदाहरण चेन्नई की 15 साल की उस छात्रा का है जिसने कहा था कि वह बड़े होने के बाद न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री बनना चाहती है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस लड़की की तरह ही कई ऐसी लड़कियाँ होंगी जो अपने देश की राजनीति में हिस्सा ना लेकर किसी दूसरे देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती होंगी।
भारत को गणराज्य बने 73 साल हो चुके हैं लेकिन हम आज भी समान प्रतिनिधित्व को हासिल करने और युवा लड़कियों के लिए राजनीति को करियर का एक विकल्प बनाने से बहुत दूर खड़े हैं। वर्तमान में हमारे देश में 78 (कुल 543 में) महिला सांसद हैं। 14.3 प्रतिशत की दर वाला यह आँकड़ा 1947 से अब तक का सबसे बड़ा आँकड़ा है। राज्य-स्तर पर यह आँकड़ा और भी कम है—विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में महिला प्रतिनिधित्व का आँकड़ा औसतन 9 प्रतिशत है। भारत में छः राज्य ऐसे है जिसमें एक भी महिला मंत्री नहीं है।
एक देश के रूप में हमने काफ़ी प्रगति की है। भारत के पुरुष और महिलाएँ अब बराबर संख्या में मतदान करते हैं। लेकिन मतदान से परे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मामला अब भी एक अछूता विषय है और इस क्षेत्र में महिलाओं को बहुत अधिक सक्रिय होने की ज़रूरत है। इसमें उम्मीदवारों के लिए प्रचार-प्रसार करना, पद के लिए भागदौड़ करना और राजनीतिक पद हासिल करना शामिल है। थोड़ी और छानबीन करने पर हमनें पाया कि 2019 के चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या 10 प्रतिशत से कम थी। राज्य स्तर पर भी हमें ऐसे ही आँकड़े देखने को मिले जहां 1980 और 2007 के बीच में राज्य विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5.5 प्रतिशत था लेकिन महिला उम्मीदवारों का कुल प्रतिशत 4.4 था।

2019 में उत्तर प्रदेश में किए गए एक अध्ययन से यह बात सामने आई कि महिलाएँ राजनीतिक भागीदारी के कई निर्धारकों जैसे राजनीतिक संस्थानों के काम करने के तरीक़ों और अपने ख़ुद के नेतृत्व की योग्यताओं में विश्वास में पिछड़ी हुई हैं। महिलाओं के लिए ज्ञान, आत्मविश्वास, आवाज़ और आज़ादी राजनीति में उनकी भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह काम युवा लड़कियों के लिए जल्दी किए जाने की ज़रूरत है ताकि वे गम्भीर रूप से सोचने की क्षमता विकसित कर सकें और भारत के भविष्य को आकार देने में अपनी भूमिका निभा सकें।
वर्तमान में हमारे देश में 78 (कुल 543 में) महिला सांसद हैं।
युवा लड़कियों में राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व के निर्माण के लिए काम करने वाली संस्था कुविरा की स्थापना के समय हमने यह पाया कि समाज के ध्रुवीकरण को देखते हुए ज़्यादातर विद्यालय (कुछ प्रगतिशील और वैकल्पिक लोगों को छोड़ कर) और अभिभावक छात्रों से राजनीति के बारे में बात करने से कतराते हैं। इसके कारण युवाओं को मिलने वाली ज़्यादातर राजनीतिक खबरें असत्यापित स्त्रोतों और सोशल मीडिया के माध्यम से होती हैं जिससे हमारे युवाओं में एक क़िस्म की निराशा पैदा हो गई है।
2021 के अक्टूबर में हम लोगों ने 13 साल की उम्र वाले बच्चों के एक समूह के साथ कार्यशाला आयोजित की थी। इसमें हम लोगों ने उनसे भारत के राजनेताओं को लेकर उनकी धारणा व्यक्त करने के लिए कहा। हमनें दो चीजें देखीं:
भारत भर में राजनीति को लेकर युवाओं ख़ासकर युवा लड़कियों की सोच को विस्तार से समझने के लिए हम लोगों ने 24 राज्यों के 11 से 24 वर्ष की उम्र वाले 400 बच्चों और व्यस्कों का आँकड़ा एकत्रित किया। हमें इन आँकड़ों में एक समानता दिखाई दी जिसमें इन लोगों ने भारत की राजनीति के लिए ‘भ्रष्ट’, ‘भ्रमित/जटिल’ और ‘गंदे’ जैसे विशेषणों का प्रयोग किया था।
हमने यह भी पाया कि भले ही लड़के और लड़कियों ने समान रूप से इस बात का जवाब दिया कि वे मतदान करेंगे (जब वे योग्य हो जाएँगे) लेकिन उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर था। 32 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं ने कहा कि वे भविष्य में राजनीति में हिस्सा लेना चाहेंगे वहीं केवल 19.7 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने ऐसी इच्छा जाहिर की। पुरुष उत्तरदाताओं की तुलना में महिला उत्तरदाताओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनके चुने गए स्थानीय प्रतिनिधियों के बारे में कम जानकारी थी। इसके अतिरिक्त, उनमें अपने दोस्तों और परिवार से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने की सम्भावना कम पाई गई।
2019 के चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या 10 प्रतिशत से कम थी।
हालाँकि हमारे वर्तमान राजनीतिक नेताओं के प्रति हमारे युवाओं में विश्वास का स्तर बहुत कम है। लेकिन आँकड़ों के अनुसार लड़कियों की तुलना में दोगुनी संख्या में लड़कों का ऐसा मानना है कि हमारे वर्तमान राजनीतिक नेता प्रभावशाली है (16.4 प्रतिशत बनाम 8.9 प्रतिशत)।
हमारे अध्ययन से यह भी बात स्पष्ट होती है कि छोटी उम्र (11–17 साल) की लड़कियाँ लड़कों की तुलना में राजनीति में अधिक रुचि दिखाती हैं लेकिन जब वे मतदान के उम्र में पहुँचती है तब लड़कों की रुचि का प्रतिशत लड़कियों पर हावी हो जाता है (इस तथ्य के बावजूद कि उम्र के साथ दोनों ही समूह में रुचि का स्तर बढ़ता है)।
ऐसी ही स्थिति हाल ही में अमेरिकन पोलिटिकल साइयन्स रिव्यू में प्रकाशित एक अमेरिकी अध्ययन में भी पायी गई। इस अध्ययन से यह बात सामने आई कि बच्चे न केवल राजनीति को पुरुष-प्रधान क्षेत्र मानते हैं बल्कि बढ़ती उम्र के साथ लड़कियों की यह सोच पुख़्ता होती जाती है कि राजनीतिक नेतृत्व ‘पुरुषों की दुनिया’ है। शोध में यह भी कहा गया कि इसके फलस्वरूप लड़कों की तुलना में लड़कियों की रुचि और महत्वाकांक्षा निम्न स्तर की होती है।
न्यूज़ीलैंड की प्रधान मंत्री बनने की इच्छा ज़ाहिर करने वाली उस छोटी सी बच्ची के उदाहरण से हमें भारतीय लड़कियों के लिए संबंधित आदर्श को सामने लाने की महत्ता को समझने में मदद मिली है। दुनिया भर की मीडिया ने प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डेन की प्रशंसा का बहुत अच्छा काम किया है ख़ासकर महामारी पर उनकी शुरुआती कुछ प्रतिक्रियाओं के बाद। इस काम ने दुनिया भर में लड़कियों के लिए उन्हें अपना आदर्श मानने में अपना योगदान दिया है। अमेरिका में किए गए शोध से यह पता चलता है कि समय के साथ समाचार पत्रों में महिला राजनेताओं पर अधिक खबरें प्रकाशित करने से युवा लड़कियों में राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की सम्भावना प्रबल होती है।
हमारे सर्वेक्षण से यह बात भी स्पष्ट हुई कि अपने स्कूल या कॉलेज की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेकर और किसी राजनेता को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले युवा उन लोगों की तुलना में राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं जिनके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं होता है।
राजनीति को करियर का एक विकल्प बनाने के लिए हमें युवा लड़कियों और राजनीतिक शक्तियों से जुड़ी सोच को बदलने की ज़रूरत है। पश्चिमी देशों में हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जिसमें टीच ए गर्ल टू लीड और इग्नाईट नेशनल जैसे नागरिक समाज संगठन अगली पीढ़ी की ऐसी महिला मतदाताओं को तैयार करने का काम करते हैं जो आगे चलकर राजनीतिक नेता बनना चाहती हैं और अपने आसपास की राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं। कुविरा का उद्देश्य स्कूलों और स्वयंसेवी संस्थानों के साथ काम करके भारत में इस खाई को कम करना है ताकि युवा लड़कियों के लिए राजनीति को फिर से बनाया जा सके। इसके अलावा हम महिला राजनेताओं को आदर्श के रूप में स्थापित करके राजनीति के लिए सकारात्मक कहानियाँ बनाने और युवा लड़कियों को उनसे जुड़ने के अवसर प्रदान करने का काम भी करते हैं जिनसे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रज्वलित होंगी।
चूँकि 2022 में पाँच राज्यों में और 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं इसलिए शिक्षकों, नागरिक समाजों और लोकोपकारों के लिए यह ज़रूरी है कि वे एक साथ आकर युवा लड़कियों के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिना समान प्रतिनिधित्व के कार्यात्मक लोकतंत्र नहीं हो सकता है।
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें।
भारत में लगभग 60 करोड़ लोगों की उम्र 25 वर्ष से कम है जो हमारी कुल आबादी का लगभग आधे से भी ज्यादा हिस्सा है। इस जनसंख्या की क्षमता की काफी प्रशंसा की जाती है पर फिर भी युवाओं (15–25 वर्ष की उम्र) को कभी-कभार ही उन्हें प्रभावित करने वाले फैसलों की बैठक में शामिल किया जाता है।
पिछले कुछ सालों में किए गए शोधों से यह बात और अधिक रूप से स्पष्ट हुई है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करने और उनके अंदर नेतृत्व कौशल का विकास करने से उन पर और उनके समुदाय दोनों पर सकारात्मक असर पड़ता है।
इस बात के भी पुख्ता सबूत हैं कि शासन और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी होने से प्रासंगिक, असरदार और टिकाऊ समाधान निकलते हैं।
युवाओं से पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमें सिर्फ इतना देखने की जरूरत है कि इन युवाओं ने किस तरह कोविड-19 के संकट के दौरान आगे आकर आपदा से निबटने का नेतृत्व संभाला था। वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के काम से लेकर बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करने और सेवा वितरण में सहायता तक में इन्होनें बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, युवाओं ने यह भी सुनिश्चित किया कि समुदाय के सभी लोगों तक सेवाएँ और सही जानकारियाँ पहुँचें।
यह बात साफ है कि युवा उन सभी चुनौतियों को अच्छे से समझते हैं जिनका वे सामना करते हैं और उनके पास ही इन चुनौतियों से निबटने के रचनात्मक और शक्तिशाली विचार भी होते हैं। हालांकि, नागरिक समाज संगठनों और वित्तदाताओं से लेकर समुदाय के सदस्यों और सरकार तक—पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों की भूमिका यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण है कि वे समाधान के विकास कार्य में शामिल हैं।
आज, कई नागरिक समाज संगठन, सरकारें और अन्य व्यक्ति युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक मंच बनाने के ठोस प्रयास शुरू कर रहे हैं। हालांकि अब भी यह सवाल बना हुआ है कि व्यवहार में इसे लाने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीके कौन से हैं। इस सवाल का जवाब ढूँढने में मदद करने के लिए 10to19: दसरा एडोलसेंट्स कोलैबोरेटिव ने 11 नागरिक समाज संगठनों से युवाओं की भागीदारी को लेकर उनकी समझ और इसे सुनिश्चित करने के उनके वर्तमान तरीकों के बारे में बात की। उनके जवाब इस प्रकार हैं।
हमने भागीदारों से अपेक्षाओं के अनुरूप पारदर्शी संरचनाओं और प्रक्रियाओं के निर्माण की आवश्यकता के बारे में सुना। इसका अर्थ यह है कि ऑनबोर्डिंग और इनडक्शन से पहले युवाओं और संगठनों की अपेक्षाओं के बीच स्पष्ट और एकरेखीय सोच होनी चाहिए।
उदाहरण के लिए, जब अंतरंग फाउंडेशन ने अपने युवा सलाहकार बोर्ड के लिए सदस्यों का चयन करना शुरू किया, तो इसने अपने पूर्व छात्रों के नेटवर्क के साथ अपने भर्ती प्रयास शुरू किए। उनका उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना था कि नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों को न केवल संगठन के दृष्टिकोण, उद्देश्यों और लक्ष्यों की जानकारी हो बल्कि उन्हें कार्यक्रमों के प्राथमिक स्तर का अनुभव हासिल हो और वे इसकी चुनौतियों, फ़ायदों और संभावनाओं को भी समझते हों। इसके अलावा, चयन के समय एक ऑनबोर्डिंग और इनडक्शन के सत्र का आयोजन किया गया। इन सत्रों में सभी सदस्यों से कार्यक्रमों और उनकी भूमिकाओं से उनकी उम्मीदों के बारे में पूछा गया और साथ ही यह भी बताया गया कि संगठन की उनसे क्या उम्मीदें हैं। सभी सदस्यों से सहभागिता की नियमितता और तालमेल, उनके रूचि वाले क्षेत्रों, कौशल को विकसित करने और इस बोर्ड के लिए उनके लक्ष्य के बारे में भी जानकारी मांगी गई। अंत में, लोकतान्त्रिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने यह फैसला किया कि दूसरे हितधारकों के सामने इसका प्रतिनिधित्व दो प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा जो निश्चित समय अंतराल पर बदलते रहेंगे।

2. नियमित प्रतिक्रिया के रास्ते और पहले से तय कैडेन्स (तालबद्ध कदम) का निर्माण
कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए युवाओं से नियमित मिलने वाले सुझाव की जगह को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सलाह देने और इसमें हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता है। इसके लिए सहयोगियों ने उनकी भागीदारी में एक नियमित तालमेल की जरूरत पर ज़ोर दिया जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाएँ हासिल की जा सकती हैं। उन्होनें मिलने वाली प्रतिक्रियाओं और सुझावों पर तेजी से काम करने के महत्व को भी रेखांकित किया।
उदाहरण के लिए, गर्ल इफ़ेक्ट्स टेक्नालजी एनेबल्ड गर्ल एंबेसडर्स (टीईजीए) प्रणाली का निर्माण लड़कियों और 18–24 साल की उम्र वाली किशोर महिलाओं के साथ मिलकर किया गया था। ‘ऑडियोविजुअल सेलफ़ी सर्वेज’ और ‘डाइरैक्ट मैसेजिंग’ जैसी विशेषताओं के माध्यम से इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत आसान है और इसकी उपलब्धता भी सहज है। साथ ही यह अपने उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर काम करता है। इसके अलावा, यह गर्ल इफेक्ट टीम और टीईजीए में नामांकित लड़कियों दोनों को नियमित और सुरक्षित दोतरफा संचार करने और प्रतिक्रिया देने का माध्यम उपलब्ध करवाता है। इससे कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी की प्रतिबद्धता का स्तर समझने में सभी को आसानी होती है और साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि इतने लंबे समय तक उनके जुड़े रहने के पीछे कौन सी प्रेरणा काम कर रही है।
3. युवाओं की बात सुनने के लिए संगठनात्मक क्षमताओं को मजबूत बनाएँ
हमारे काम और हमारी बातचीत के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य हमारे सामने आया जिसमें हमें एक ऐसी सुरक्षित जगह बनाने की जरूरत थी जहां युवा अपनी बात साझा कर सकें, सीख सकें और कार्यक्रम में सार्थक रूप से हिस्सा ले सकें।
इन जगहों को असरदार बनाने के लिए प्रवाह इस दिशानिर्देश का पालन करता है कि संगठनों को खुद ही एक निश्चित मात्रा में क्षमता निर्माण और संवेदीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णयकर्ता युवाओं की बातों को वास्तव में सुन रहे हैं। वे टीम के सदस्यों और युवाओं के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण में विश्वास करते हैं जिनमें युवा विकास सिद्धांतों का शिक्षण/समझ, प्रणाली की सोच आधारित प्रशिक्षण और मुक्त और युवा-केन्द्रित स्थानों की डिज़ाइन के तरीक़े शामिल होते हैं।
युवाओं को सामने लाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दी गई जानकारी उनके रुचि के अनुरूप हो।
वे दस्तावेजों को अनुरूप बनाकर और रणनीतियों को प्रासंगिक, मजेदार और युवाओं के लिए पढ़ने में आसान बनाकर संगठनों की मदद भी करते हैं। युवाओं को भागीदार बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दी जाने वाली जानकारी उनकी जरूरत के हिसाब से हो। ऐसा करने के लिए उनसे साझा किए गए किसी या सभी प्रकार के दस्तावेजों या संसाधनों में शब्दजाल का उपयोग नहीं होना चाहिए और वे दस्तावेज़ उनकी वास्तविकता के संदर्भ में होने चाहिए।
4. युवाओं का क्षमता निर्माण
सहयोगी युवाओं के लिए क्षमता निर्माण को शामिल करने की जरूरत पर भी बहुत अधिक ज़ोर देते हैं। जब युवाओं को रणनीति पर उनके विचार या सुझाव देने के लिए बुलाया जाता है तब उन्हें रणनीतिक सोच, महत्वपूर्ण सोच और संघर्ष समाधान जैसे कौशल मुहैया करवाए जाने चाहिए ताकि वे भाग लेने, शामिल होने और साझा करने लायक हो सकें। युवाओं के लिए ये कौशल भविष्य में जुडने वाले अन्य संगठनों में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दरअसल, सफलतापूर्वक युवाओं के साथ नियमित और सार्थक भागीदारी को सुनिचित करने वाले कई युवा-केन्द्रित संगठनों ने यह प्रस्तावित किया है कि युवाओं द्वारा कार्यक्रमों में निवेश किया गया समय कार्यक्रम के हस्तक्षेप से परे उनके लिए सार्थक होना चाहिए।
उदाहरण के लिए, मिलान फ़ाउंडेशन का गर्ल आइकॉन कार्यक्रम 15 से 17 साल की लड़कियों के साथ काम करता है। हालांकि उनके पास गर्ल आइकॉन के अपने पुराने छात्रों का एक मजबूत नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल वे संसाधनों की आपूर्ति, रोजगार अवसरों की जानकारी और छात्रवृति और मैंटरशिप की सहायता के लिए करते हैं ताकि उनकी निजीगत शिक्षा और नेतृत्व की यात्रा जारी रहे। एक तय टीम उन पूर्व छात्रों के साथ हर महीने फोन कॉल करके, हर चार महीने में मिलकर और तय किए गए सत्रों के माध्यम से संपर्क में रहता है। इस तरह की कार्यविधियों के माध्यम से संगठन ने यह सीखा कि कार्यक्रम के दौरान उन लड़कियों को मात्र स्मार्टफोन जैसी चीज मुहैया करवा देने से कार्यक्रम के बाद भी उन्हें इसका फायदा मिल सकता है।
5. प्रामाणिक जुड़ाव का प्रयास करें
और अंत में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना था कि हम युवाओं को एक अखंड समूह के रूप में न देखें और विभिन्न प्रकार के विचारों और सुझावों को सुनने के प्रति जागरूक रहें।
अपनी संस्थागत ढांचे के भीतर युवा बोर्ड सदस्यों को दो चक्रों तक रखने वाले रीप बेनिफ़िट नाम की एक संगठन ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि अगर किसी संगठन के नेतृत्व और टीम के अंदर विविधता नहीं होगी तब यह अपने युवाओं वाले नेटवर्क के भीतर विविधता को प्राथमिकता नहीं देगा। युवा बोर्ड के अपने दोहराव के माध्यम से रीप बेनिफ़िट लिंग, क्षेत्र, शैक्षणिक क्षमता, भाषा और सामाजिक-आर्थिक समूहों के आधार पर विविधता पर ध्यान केन्द्रित करता है। जबकि विविधता अपने साथ कई नए दृष्टिकोण लाती है वहीं यह संचार के एक आम माध्यम को चुनने, विभिन्न किस्म की वास्तविकताओं के बावजूद समूह के बीच आम सहमति बनाने और सामान्य लक्ष्यों पर संरेखित करने जैसी तार्किक चुनौतियाँ भी लेकर आती हैं। इसके लिए रीप बेनिफ़िट का यह सुझाव है कि संगठनों को नियमों और समूह के लिए काम करने के तरीकों के आसपास एक बुनियादी संरचना और रूपरेखा बनाकर काम करना चाहिए, जिसके आधार पर समूह अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है और बदलावों के लिए सुझाव मुहैया करवा सकता है।
जब हम प्रतिनिधित्व और भागीदारी के बारे में सोचते हैं तब इस बारे में सोचना भी महत्वपूर्ण है कि युवाओं द्वारा निवेश किए गए समय और उनके प्रयासों का भुगतान किस रूप में किया जा रहा है। जैसा कि पहले बताया गया है यह कौशल निर्माण के रूप में किया जा सकता है लेकिन अवसर और इंटर्नशिप उप्लबद्ध करवाकर, प्रमाणपत्र या मान्यता देकर या कुछ निश्चित राशि या प्रतिपूर्ति के रूप में भी किया जा सकता है।
इस लेख को अँग्रेजी में पढ़ें।
—