हालिया समय में विविधता (डाइवर्सिटी) और समावेशन (इंक्लूजन) से जुड़ी चर्चाओं में काफी इजाफा हुआ है। लेकिन क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों (विशेषकर दलित, बहुजन, आदिवासी, श्रमिक वर्ग और अन्य हाशिए के समुदायों से ताल्लुक रखने वाले) को अब भी नीति-निर्माण, नागरिक समाज, शैक्षणिक जगत, विकास क्षेत्र और सरकारी संस्थानों में व्यवस्थागत बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। एक सच्चाई यह भी है कि उनके समावेशन के लिए न सिर्फ संस्थागत ढांचों की कमी है, बल्कि सिस-जेंडर समाज को शिक्षित करने का जिम्मा भी अक्सर उन पर ही मढ़ दिया जाता है।
ऐसी सामाजिक असमानताओं के कारण इस समुदाय के लिए समावेशी और सुरक्षित जगहों की कमी साफ नजर आती है। इस कमी को भरने की दिशा में हमने अकम फाउंडेशन के तहत दो सामुदायिक पुस्तकालयों की स्थापना की है। एक पुस्तकालय का नाम ‘कितापे कथा कोई’ है और ये जोरहाट (असम) में मेरे गांव में स्थित है। दूसरा पुस्तकालय ‘चंद्रप्रभा साईकियानी फेमिनिस्ट लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर’ डिब्रूगढ़ (असम) में स्थित है। ये केवल किताबों से लदे हुए कमरे नहीं हैं। मैं इन्हें राजनीतिक स्पेस मानती हूं। ये स्पेस विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों के युवा क्वीयर लोगों के लिए बनाए गए हैं, जहां वे बिना किसी जजमेंट के सुरक्षित रूप से अपने लिए जानकारी और समझ जुटा पायें।
क्वीयर और ट्रांस लोगों को मुख्यधारा की शिक्षा, आजीविका और नीति-निर्माण प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाने के लिए इन तमाम व्यवस्थाओं को सबसे पहले एक बुनियादी सच को स्वीकार करना होगा: हम समान नागरिक हैं, हमारे समान अधिकार हैं और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह हमारी गरिमा भी महत्वपूर्ण है। समावेशन का सही अर्थ यह है कि वो केवल प्रतीकात्मक नहीं होता, बल्कि निरंतर और संस्थागत बदलाव की मांग करता है। एक ऐसा बदलाव, जिसमें ट्रांस और क्वीयर नेतृत्व को प्रमुखता मिले, सभी संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाये और हमारी पहचान को मान्यता मिले।
मैंने अपने अनुभव से यह सीखा है कि यह बदलाव कई स्तरों पर जरूरी है। स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों को संवेदनशील बनाना और सोशल सेक्टर में आत्ममंथन जैसे कई पहलू इसका हिस्सा हैं। इन सभी स्तरों पर बदलाव से ही मौजूदा व्यवस्थाओं को असल में समावेशी बनाया जा सकता है, ताकि वे हमें गरिमापूर्ण जीवनयापन के मौके दे पायें।
समावेशन की राह समुदायों से शुरू होती है
क्वीयर समुदायों को संगठित करना, विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में, आसान काम नहीं है। आमतौर पर एलजीबीटीक्यूआईए+ से जुड़े आंदोलनों और स्पेस के विषय में जानकारी का अभाव होता है और सही भाषा और शब्दावली की भी कमी होती है। साथ ही समुदाय के पास आगे बढ़ने की कोई स्पष्ट दिशा या उम्मीद नहीं होती। इसलिए लोगों तक पहुंचना जरूरी है, ताकि हम उनसे वहां मिल पायें जहां वे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, हम चाय की टपरियों या घर की छतों पर अनौपचारिक बैठकें करते हैं और छोटे शहरों में प्राइड इवेंट जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस तरह धीरे-धीरे भरोसे की बुनियाद पर समुदाय को संगठित किया जा सकता है।
स्थायी परिवर्तन के लिए यह जरूरी है कि समावेशन को केवल एक अलग-थलग मुद्दे का संघर्ष न समझा जाए। इसे विभिन्न तरह के स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और उन्हें सुलभ बनाने की प्रक्रिया की तरह देखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, मैं अपनी क्वीयर राजनीति को अपने पुस्तकालय के हर पहलू से जोड़ती हूं। एक समावेशी मॉडल बनाने के लिए हम पुस्तकों के चयन से लेकर तमाम तरह के इवेंट (प्राइड-थीम वाले रीडिंग सत्र, नारीवादी स्टोरीटेलिंग सत्र, आइडेंटिटी पर वर्कशॉप आदि) आयोजित करने पर विशेष ध्यान देते हैं। जब लोग दूसरों की कहानियों में अपने अनुभवों की गूंज सुनते हैं, तो उनके बीच एक जुड़ाव बनता है। इसी जुड़ाव को आधार बनाकर हम अधिकारों, नेतृत्व, नारीवादी राजनीति और सामूहिक देखभाल जैसे विषयों पर बातचीत करते हैं।

इसी प्रक्रिया के तहत हमारी एक मुहिम, ‘नो मोर होल्डिंग माय पी’ की शुरुआत हुई। इस पर हमारा ध्यान तब गया जब एक ट्रांस छात्र ने बताया कि उन्हें बाइनरी-जेंडर आधारित शौचालयों का उपयोग करते समय असुरक्षित महसूस होता है। अधिकांश संस्थानों में जेंडर-न्यूट्रल शौचालय मौजूद नहीं हैं। इस साधारण बातचीत ने जल्द एक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे छात्र समूहों, शिक्षकों और कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला। हमने कई संस्थानों में जेंडर-न्यूट्रल शौचालयों के लिए सफलतापूर्वक पैरवी की। इस प्रक्रिया ने सुरक्षा (सेफ्टी), सुलभता (एक्सेस) और अपनापन (बिलॉन्गिंग) जैसे गहरे मुद्दों पर बातचीत के नए रास्ते खोले।
दिखावटी समावेशन की कीमत
कई बार समावेशन के नाम पर जो आडंबर किया जाता है, उससे साफ तौर पर पूर्वाग्रह झलकता है। उदाहरण के लिए, एक बार किसी ने मुझसे कहा कि उन्हें एक पैनल के लिए मेरी जगह कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो एकदम पूर्वोत्तर का दिखता हो। ऐसा तब हुआ, जब मैं स्वयं उत्तर-पूर्व भारत से हूं। ऐसे सतही प्रतिनिधित्व से जुड़ी सोच दिखाती है कि जब समावेशन सम्मान, समानता और संरचनात्मक बदलाव पर आधारित नहीं होता, तो वह वास्तव में खोखला होता है। प्रतीकात्मकता (टोकनिज़्म) लोगों को महज चेहरों में बदल देती है। ऐसे में उनका सुविधानुसार इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उन्हें संस्थाओं के निर्माण में एक आवश्यक भागीदार नहीं माना जाता है। बहुत सी संस्थाएं इस दुष्चक्र में फंसती हैं। उदाहरण के लिए, वे महिलाओं को केवल लैंगिक मुद्दों के पैनल में शामिल करती हैं या ट्रांस व्यक्तियों को केवल ट्रांस अधिकारों से जुड़े विषयों पर ही मंच देती हैं।
इसलिए संस्थानों, गैर-लाभकारी संगठनों और समूहों को खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने चाहिए। क्या हाशिए पर मौजूद समुदायों के लोग वास्तव में उनकी भर्ती प्रक्रियाओं, नेतृत्व संरचनाओं और नीति-निर्माण में शामिल हैं? या उन्हें केवल दिखावटी विविधता या प्रतिनिधित्व का कोटा पूरा करने के लिए अपने साथ जोड़ा जाता है?
उतना ही महत्वपूर्ण यह देखना भी है कि भर्ती के बाद क्या होता है? क्या आपके संस्थागत परिवेश में वंचित पृष्ठभूमियों के लोगों को सहजता से रहने, फलने-फूलने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है? इसके लिए मानव संसाधन नीतियों, कार्यस्थल संस्कृति, और सहयोगी ढांचे की पुनर्रचना जरूरी है, ताकि उनके लिए सुरक्षित, गरिमामयी और अपनेपन का माहौल सुनिश्चित किया जा सके। कुछ अहम सवाल यह हो सकते हैं: क्या आपकी सामूहिक स्वास्थ्य योजनाओं में जेंडर-अफर्मेटिव केयर शामिल है या ट्रांस कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ सुलभ नहीं हैं? आपके संस्थान की नीतियां पॉश (कानून) अनुपालन, मासिक धर्म अवकाश या सुरक्षा ऑडिट के संदर्भ में ‘महिला’ को कैसे परिभाषित करती हैं? क्या इन नीतियों में जेंडर-विविध लोगों को शामिल किया जाता है या ये महज सिस-हेट बाइनरी को और मजबूत बनाती हैं?
हर स्तर पर कर्मचारियों का नियमित और गहन प्रशिक्षण जरूरी है, ताकि वे जाने-अनजाने में पूर्वाग्रह से दूर रहते हुए एक सम्मानजनक व समानुभूतिपूर्ण कल्चर बना सकें। इसके बिना, सबसे अच्छी नीतियां भी सतही बनकर रह जाती हैं।
स्थायी परिवर्तन के लिए यह जरूरी है कि समावेशन को केवल एक अलग-थलग मुद्दे का संघर्ष न समझा जाए।
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों का पुनर्वितरण भी जरूरी है। समावेशन का मतलब यह होना चाहिए कि हाशिए की आवाजें न केवल सुनी जाएं, बल्कि वे नीतियों को आकार दें, टीमों का नेतृत्व करें और हर निर्णय के हर स्तर पर उनकी भागीदारी हो।
ट्रांस लोगों के लिए और उनके साथ आजीविका की पुनर्रचना
हमारी एक बैठक के दौरान एक युवा ट्रांस व्यक्ति ने मुझसे पूछा, “क्या हमारे लिए भीख मांगने और सेक्स वर्क से परे भी कोई भविष्य है?” उसके सवाल में छुपी पीड़ा से मुझे गहरा आघात लगा।
भारत में ट्रांस व्यक्तियों के लिए आजीविका के सफल मॉडल लगभग न के बराबर हैं। यही कारण है कि हमारे समुदाय के कई लोग आज भी भिक्षावृत्ति या सेक्स वर्क जैसे रूढ़िवादी तरीकों से अपना गुजारा करने के लिए विवश हैं। यह उनकी पसंद नहीं मजबूरी है, क्योंकि मुख्यधारा का समाज उन्हें कोई दूसरा विकल्प ही नहीं देता। इन व्यवसायों को प्रतिबंधित करना, हेय दृष्टि से देखना या इनका अपराधीकरण करना समस्या का हल नहीं है। इसके उलट हमें जीवनयापन के लिए विकल्प सुनिश्चित कर नए अवसरों के द्वार खोलने चाहिए।
जब तक कोई संगठन विशेष रूप से जेंडर और सेक्शुएलिटी पर काम न कर रहा हो, ट्रांस और क्वीयर लोगों को भर्ती प्रक्रिया में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है — विशेषकर नेतृत्व और निर्णय से जुड़ी भूमिकाओं में।
उदाहरण के लिए, यदि कोई संगठन श्रम अधिकारों, कृषि या शिक्षा पर काम करता है, तो वह जेंडर बाइनरी से बाहर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने में रुचि नहीं दिखाता। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें यह जरूरी ही नहीं लगता है। लेकिन सच यह है कि ट्रांस और क्वीयर लोग हर क्षेत्र में मौजूद हैं। इसलिए चाहे कोई नीति जेंडर या सेक्शुएलिटी पर केंद्रित हो या नहीं, वे उससे समान रूप से प्रभावित होते हैं।
मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में कुछ समुदाय-आधारित संगठन ट्रांस व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक आजीविका के अवसर तैयार करने पर काम कर रहे हैं। वे कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ मिलकर कौशल निर्माण और प्लेसमेंट के मौके बनाते हैं। इसमें रिज्यूमे सुधारना, सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण देना और कॉर्पोरेट परिवेश से परिचय जैसे पहलू शामिल होते हैं। इस मॉडल से कुछ तात्कालिक सफलता भी देखी गयी है। उदाहरण के लिए, कई ट्रांस लोगों को नौकरी मिली और उन्हें इससे फायदा भी हुआ। लेकिन हमारे पास अभी भी दो-तीन साल से आगे का डेटा नहीं है कि ये लोग इन नौकरियों में कितनी स्थिरता से टिके रह पाए या इन संस्थानों में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

बीते कुछ समय से दक्षिण भारत में ऐसे ट्रांस व्यक्तियों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो लघु स्तर के कामकाज से अपने लिए कमाई सुनिश्चित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, चाय, फोटोकॉपी या कपड़ों की दुकान या स्टॉल चलाना। ऐसी कोई भी पहल अमूमन स्वतंत्र रूप से या स्थानीय सिविल सोसाइटी संगठनों के समर्थन से शुरू की जाती हैं। यह उद्यमशील आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सार्थक बदलाव का प्रतीक है।
हमारे जैसे कुछ संगठन सामुदायिक योगदान इकट्ठा कर और स्थानीय सरकार से समन्वय बनाकर आजीविका के मॉडल विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, हाल ही में हमने एक ट्रांस महिला का सिलाई व्यवसाय शुरू करने में उनकी सहायता की। हमारी रणनीति अब यह है कि ऐसे हस्तक्षेपों को जिला स्तर पर मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे हमें नतीजे भी मिलें और सहयोग भी। अगर ऐसा होता है, तो हम राज्य स्तर पर एक विशिष्ट ट्रांस आजीविका नीति के लिए पैरवी कर पायेंगे।
अधिकारों के बिना पहचान निरर्थक है
जब तक हम सरकारी संस्थाओं में होने वाले भेदभाव का संज्ञान नहीं लेंगे, आजीविका के विषय पर ईमानदारी से बात नहीं की जा सकती है। हमारे लिए ट्रांस आईडी कार्ड और आश्रय गृह बनाये गए हैं। लेकिन जब तक हमारे पास कमाई के साधन, गरिमा और संसाधनों पर अधिकार न हो, ये सुविधाएं व्यर्थ प्रतीत होती हैं।
हाल ही में एक बैठक हुई, जिसमें लगभग 15 सामुदायिक सदस्य और सरकार के विभिन्न विभागों व योजनाओं (आजीविका मिशन, स्वास्थ्य मिशन और सामाजिक न्याय विभाग) के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें कई ट्रांस और क्वीयर प्रतिभागियों ने भेदभाव से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इनमें बार-बार एक वेदना उभरकर सामने आयी — जब समुदाय के लोग सरकारी सहायता या सेवाएं लेने जाते हैं, तो अधिकारियों का उनके प्रति बेहद अमानवीय व्यवहार होता है। एक प्रतिभागी ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए एक टिप्पणी साझा की, जो इस पक्षपाती मानसिकता को उजागर करती है: “इन लोगों को काम देने का क्या फायदा, ये लोग तो नाचेंगे।”
हमें ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों की जरूरत है जो समुदाय की वास्तविकताओं को पहचानें।
ऐसे बयान समाज में गहरी जड़ें जमाए ट्रांसफोबिया, जातिवादी सोच और रूढ़िवादी धारणाओं को दर्शाते हैं। ऐसे में समुदाय के लोगों के लिए अपने अधिकारों तक सम्मानपूर्वक पहुंच पाना असंभव हो जाता है। इसका समाधान केवल नीतिगत बदलावों से नहीं होगा। इसके लिए हमारी मानसिकता में मूलभूत बदलाव, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और संस्थागत कल्चर में भी परिवर्तन की आवश्यकता है।
कुछ सरकार-समर्थित आजीविका मॉडल इस दिशा में उम्मीद जगाते हैं। उदाहरण के लिए, ओडिशा सरकार का एक उल्लेखनीय मॉडल है, जिसमें ट्रांस व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है और उन्हें नगर निगम के कचरा प्रबंधन तंत्र से जोड़ा गया है। ये एसएचजी व्यावसायिक रूप से संचालित होती हैं, नियमित आय अर्जित करती हैं और राज्य-प्रेरित समावेशन का एक सकारात्मक उदाहरण हैं। ट्रांस व्यक्तियों को कचरा-प्रबंधन में औपचारिक, वेतनयुक्त भूमिकाओं में शामिल करना उनकी दृश्यता और स्थिरता, दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। लेकिन इस मॉडल के भीतर भी काम की परिस्थितियों, वेतन समानता और निर्णय लेने की शक्ति जैसे पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टि बनाए रखना आवश्यक है।
एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक चुनौती यह है कि जब हम सरकार के पास आजीविका योजनाओं या नीति समावेशन की मांग लेकर जाते हैं, तो वे डेटा मांगते हैं — विशेष रूप से आंकड़े। चूंकि ट्रांस आबादी की संख्या कम है और समुदाय के कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं हैं, इसलिए हमें अक्सर इन योजनाओं से बाहर कर दिया जाता है। पहचान पत्र, दस्तावेजीकरण और आधिकारिक रिकॉर्ड में हमारी दृश्यता (विजिबिलिटी) को लेकर लगातार टकराव बना रहता है।
हमें ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों की जरूरत है जो समुदाय की वास्तविकताओं को पहचानें। साथ ही हमें राज्य का समर्थन चाहिए, जो शर्तों या शोषण पर आधारित न हो। इसके अलावा, हमें शिक्षा में आरक्षण, सार्थक रोजगार कोटा और बुनियादी ढांचे में समावेशन की भी सख्त जरूरत है।
केवल शर्तों पर आधारित फंडिंग समर्थन पर्याप्त नहीं
ट्रांस समुदायों की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक यह है कि वित्तीय संस्थाएं हम पर भरोसा नहीं करती। बहुत ही कम बैंक या ऋणदाता ट्रांस व्यक्तियों को ऋण या क्रेडिट देने के लिए तैयार होते हैं। औपचारिक वित्तीय सहायता के बिना किसी व्यवसाय की शुरुआत करना या उसे बढ़ाना लगभग असंभव हो जाता है।
इसलिए फंडिंग देने वाली संस्थाओं को यह समझना होगा कि ट्रांस-नेतृत्व वाले संगठनों को अनेक और परस्पर जुड़ी हुई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हम अनेक हाशियों पर एक साथ काम करते हैं। हमें वित्तीय और मानसिक दबाव झेलते हुए भी उन लोगों के सामने अपनी वैधता सिद्ध करनी पड़ती है, जो न हमारे जीवन को समझते हैं, न हमारे काम को और न ही हमारी चुनौतियों को।
फंडिंग एजेंसियों के लिए एक जरूरी सीख यह है कि वे यह सोचें कि वे अपनी सहायता को किस तरह से नियंत्रित करती हैं। अधिकतर फंडिंग कठोर प्रस्तावों, परिणाम-आधारित मॉडलों और सेक्टर की पूर्व-निर्धारित प्राथमिकतों पर आधारित होती है। ये ढांचा ट्रांस, क्वीयर, दलित और विकलांग समुदायों द्वारा संचालित जमीनी संगठनों की स्वाभाविक और निरंतर बदलती वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता।
इसके अलावा, मौजूदा फंडिंग ढांचे के भीतर यह सवाल भी जरूरी है कि वास्तव में फंड मिल किसे रहा है? अक्सर देखा गया है कि ऐसे बड़े गैर-लाभकारी संगठनों को ही फंडिंग मिलती है, जो पहले से ही नेटवर्क और संसाधनों से लैस होते हैं। वहीं छोटे, समुदाय-आधारित समूहों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या उन्हें बहुत सीमित समर्थन के साथ संघर्ष करना पड़ता है। हैदराबाद के मित्र क्लिनिक का बंद होना इसका एक जीवंत उदाहरण है। जब यूएसएआईडी ने अपना समर्थन वापस लिया, तो ट्रांस स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक अहम जगह हमेशा के लिए खो गयी। ऐसे में आगे की राह क्या है? आखिर ट्रांस स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है?
अब समय आ गया है कि फंडिंग जगत को लेन-देन आधारित मॉडलों से आगे बढ़ना होगा। हमें असल में लचीली, बहुवर्षीय ग्रांट्स की जरूरत है। ऐसी फंडिंग जो केवल परिणामों पर नहीं, बल्कि लोगों पर विश्वास जताये। जहां सिर्फ आंकड़ों और रिपोर्टिंग पर नहीं, बल्कि रुककर सोचने, मंथन करने और नए सिरे से चीजों को बनाने पर ध्यान दिया जाये। जहां समानता केवल एक कागजी दावा न होकर, एक सार्थक वादा हो।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें।
__



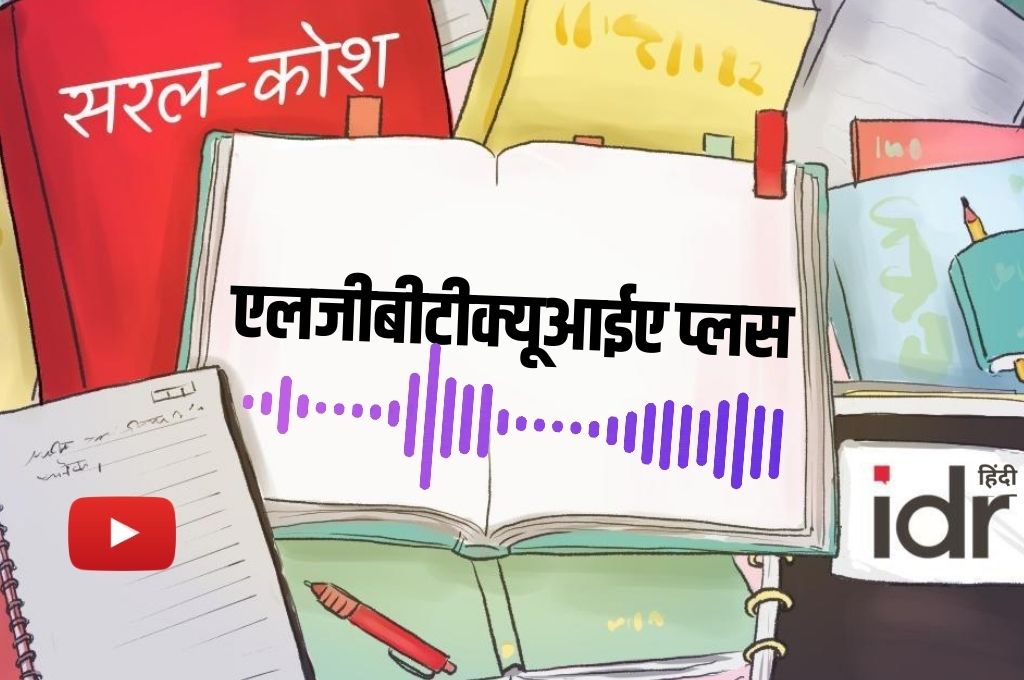

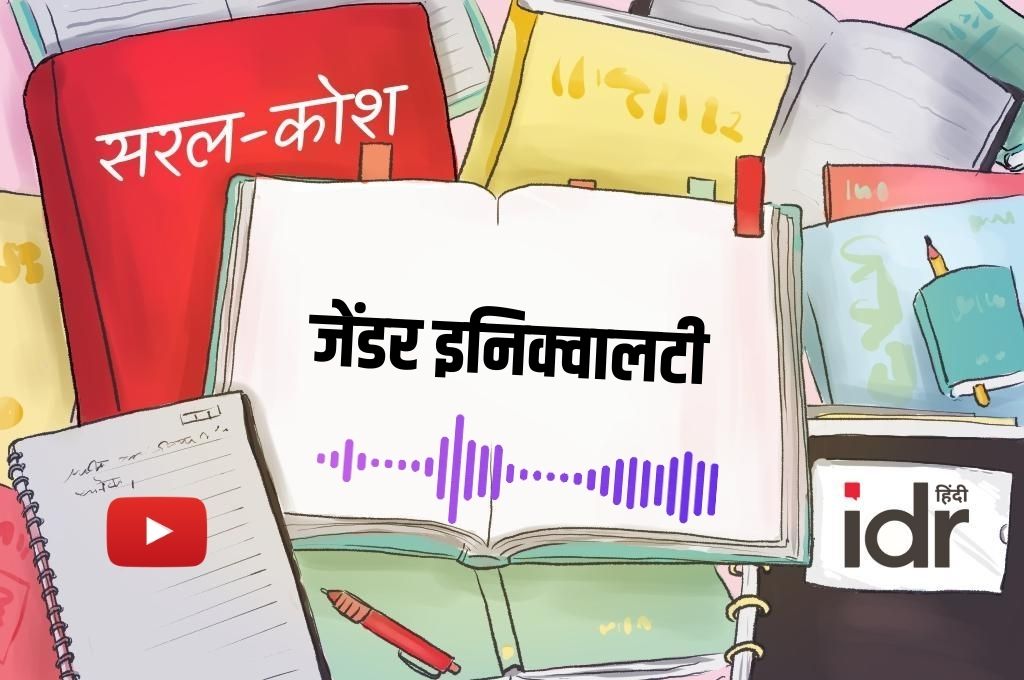
गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपके ईमेल का पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *